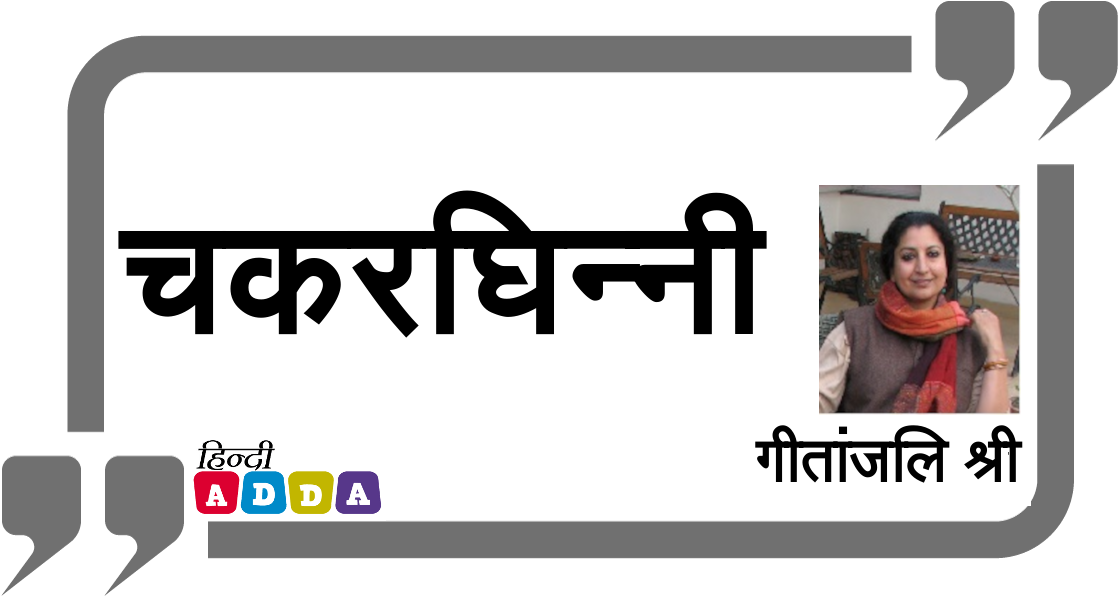चकरघिन्नी | गीतांजलि श्री – Chakaraghinnee
चकरघिन्नी | गीतांजलि श्री
मैंने फिर कोशिश की। जैसे लेखन में करती हूँ। कि फिर शुरू करूँ तो अब के खत्म कर पाऊँगी। पर इतना ही हुआ कि जहाँ मुड़ना था तन लचपचाया, पल भर को पंजों पर डिगडुग सँभला, और फिर उसी रफ्तार से बढ़ चला।
एक फेरा और।
फिर एक और।
राउंड पे राउंड मैं मारे जा रही थी। बिना रुके।
मैं रुक नहीं पा रही थी।
चिल्लाऊँ? कि रोको मुझे? खींच के बीच राह? जैसे झूला झुलाती बच्ची बसमेरीबारी करती झूले को खींचती है और दाएँ बाएँ बाएँ दाएँ असंतुलित से झटकों के साथ झूले को रोक देती है। रुक…झटका…लचका… रुक गया।
पर मैं ठहरी बेहद प्राइवेट आत्मा। पुकारूँ? जोर से? अनजान किसी को? किसी को? सवाल ही नहीं! गोल गोल चक्कर मारती रहूँगी और उम्मीद करूँगी किसी की नजर नहीं पड़ी और रुक जाऊँगी जब रुक पाई।
वैसे अभी ठीक ही था, खास कोई नहीं देखने दाखने को, और पहिया भी तो द्रुत् से मंथर से थम तक आते आते आता है! आदमियों की टोली निकलनी शुरू ही हुई थी, फ्लैटों के बीच के लॉन में जमा होने पर अभी इतने चौकन्ने नहीं थे कि देखें एक निवासी लगी हुई है फ्लैटों के चारों ओर सैर में!
ये मेरी मॉरनिंग वॉक, दिन प्रतिदिन की। और आदमियों के निकलने की घड़ी मेरे लौटने की।
बस यहीं जरा सा लोचा हो गया आज। पैर एकदम से थम नहीं पा रहे थे।
मैं उनके रुकने का इंतजार करने लगी।
आदमी ताली बजाने लगे। अपनी बाकी टोली को जगाने।
एक मल्टी स्टोरी से दूसरी मल्टी स्टोरी के बीच की खुली जगह में उनकी तालियाँ और जोर से बजतीं। ये तो कोई बात नहीं हुई! क्या करूँ, गेट खोल के बाहर निकल जाऊँ और किसी दूर के पार्क में अपनी इस चक्रगति को ठिकाने लगाऊँ?
पर दूसरे पार्कों में जाना कब का बंद कर दिया था। और उस बेफिक्री को कि छोड़ो पीछे बंद दीवारों की तूतू मैंमैं और छानो दुनिया को, उठाओ फाटक का पल्ला और निकल पड़ो।
फाटक पर अभी ऊँघा समा बाकी था। गार्ड रूम का दरवाजा अधखुला था और टेबल फैन की आवाज आ रही थी। सो रहा होगा!
खंबे पर बत्ती ऑफ हो गई।
जग रहा होगा!
तो मैंने अपनी गैरइरादा चाल बाइरादा बनाई और फाटक के सामने से फट फट निकली। कौशल से मोटर गाड़ियों के बीच दाएँ बाएँ बाएँ दाएँ जैसे नौका चालन करती। जरा सी जगह और उस पर गाड़ियाँ!
हर बार सोसायटी मीटिंग में छिड़ती कि गाड़ियाँ यहाँ न ठूँसो, फाइन लगाओ, पहली पर कम, दूसरी पर ज्यादा, और बीच की एक अकेली हरे रंग की कहलाने वाली जगह को सीमेंट सपाट करके कार पार्क बना दो और क्या करेंगे अगर आधी रात में एंबुलेन्स बुलानी पड़े, फ्लैट से गेट तक मौत की गारंटी, रात को दिल का दौरा न पड़ने दो?!
इतनी सुबह भी नहीं, मैंने मुचामुच गाड़ियों के पार जाते हुए तय किया। हालाँकि सवेरा हरकत की तैयारी में आ रहा था। ड्राइवरों का आना शुरू। कोई इंजन रिरिया उठा, गाड़ियाँ धुल पुँछ रही हैं। बच्चे स्कूल जाएँगे, और जनता काम पे। ये सब हो हवा जाए, फिर आने दो दिल के दौरे शौरे!
पर अभी मेरी चिंता हार्ट अटैक नहीं थी, मॉरनिंग वॉक थी, जो रुकना नहीं चाह रही थी और कभी भी सब देखने लगेंगे। ऐन वही चीज जिससे बचने के लिए मैंने बाहर जाना छोड़ दिया था और अपनी ही सोसायटी में चलना शुरू कर दिया। मुँह अँधेरे, जब सोसायटी वाले अभी सोते हैं। और मैं नहीं दिखती। न उनको, न खुद को।
क्योंकि उन्हें दिखो तो खुद को भी दिख जाते हो!
सामने वाला दिखा देता है हमें हमारी छवि! उसकी आँखों में आ जाता है कि लड़की तुम्हारा काजल बाढ़ हो गया, मैडम आपका ब्रा स्ट्रैप कहाँ भाग रहा है, और बाल हुए जाते हैं सफेदी की जय जयकार, और पेट तो कपड़ाफाड़ आजादी पर तुल गया, और वैसे ये किस ढब के कपड़े पहनती हैं आप, न जनाना, न मर्दाना, न पूरब, न पश्चिम!?
हँस भी लेती थी उनकी आँखों में अपनी तस्वीर देख कर। किस खाँचे में डालें मुझे, वे समझ नहीं पा रहे, और अगर अपने अजूबेपन पर इतराती नहीं, तो भी बुरा तो नहीं ही लगता था मुझे। इन फाटक वालों का इधर उधर खिसक जाना कि कैसे तो इसका अभिवादन करें!? गार्ड, प्लंबर, बिजली चैप, धोबी, सारे के सारे जो हाउजिंग सोसायटी की मरम्मतबाजी को थे। न ‘माता जी नमस्ते’ बनता, न ‘बहन जी नमस्ते’ मुँह से निकलता, न ही ‘गुड मॉरनिंग डॉक्टर साहिब’ या ‘सर जी’ कह पाते, जो उनके लिए था जो आदमियों वाली नौकरी करने लगी है। पर लेखिका, अनजानी, और रंग ढंग उलझट्टा!
मैं ही मजा लेने को आँखें मिला देती और वे ऐसे देखना चाहते कि जैसे मैं हूँ ही नहीं!
आज मैं हूँ गोल गोल!
बजरी पर जूते फटकारती मैं फिर वापस। मैं फिर आगे। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट।
कुछ कारें तो निकल गईं। बजे बजरी। हाँ ये जगह पिछले चक्कर में नहीं थी।
हेज के साथ साथ।
बजे बजरी।
कोने पे इकलौता पेड़। सेमल। लाल लाल फूल बरसाता है। मैं कुचलती हूँ। तुम गिराओ, मैं हर राउंड में कुचल दूँगी।
हेज से लगी मैं चल रही हूँ। गिलहरी भी बाउंडरी के तार पे। गिलहरी और मैं! चलते हुए। बढ़ते हुए।
अगले पेड़ तक। मुर्झल्ला आम। फफूँदी सा बौर। महक जरा जरा।
फिर हेज जिसे सब हरियाली कहते हैं।
अगला कोना। पीपल का पेड़। उसकी जड़ से फूटे हैं नए पत्ते और पुराना मंदिर। उसके नीचे से फिर घूमो। वर्तुलाकार घुमाव।
फिर फाटक। मेरे बैरी ये दो पैर। मेरा चकरघिन्नी मन। मेरा बजरियाता तन।
तालियाँ रुक गईं। माने पूरी मंडली पहुँच ली। इमारतों के बीच से मैंने कनखी मारी। हाथ ऊपर। हरी ओम की गुहार अब होगी। हरी ओम हरी ओम।
अब मैं थकने वाली हूँ मुझे लगा।
अब लोग देखने वाले हैं यह भी।
लोगों का देखना मुझे सख्त नापसंद है। अपना अक्स उबाऊ हो जाता है। उस ऊब से बचने के लिए भीड़ में खोने की मंशा उठती है। भीड़ में खोने के लिए साड़ी, शलवार कमीज, ऐसे सबके जैसे कपड़े, डाट लेते हैं। डाट के सोचते हैं अब निश्चिंत होकर किसी भी पार्क में जितना भी चाहो भ्रमण लगा सकते हो। सेहतअंगेज सैर कर सकते हो।
क्योंकि
सैर तो करनी ही थी। सब करते हैं। इसमें मैं सबके जैसी हूँ!
लिहाजा उम्र जो भी, लिंग जो भी, वर्ग जो भी, हर भेद जो भी, सबके सब करें वॉक। वॉक वॉक वॉक। कोई करे जॉगिंग, रीबॉक और नाइके में। दूसरा उठाए बाँहें सतर और मार्च अनंत। कोई बनाए बाँहों को चप्पू, कोई बनाए चक्कू। कोई चले, रुके, सिर पे खड़ा हो जाए, फिर चल पड़े। पर चलें सब के सब।
मैं भी, अनुदिन, लगातार, बिला फेल, बिला रोक, कभी कभी बिला रुक! हरी ओम हरी ओम की पुकार से लगभग ताल मिलाती। ऐसे जैसे कभी नहीं रुकूँगी, चलती रहूँगी, सैर तंद्रा में चली गई हूँ और चलती जा रही हूँ।
वैसे
मैं गजब की वॉकर हूँ। मगर जैसे लेखन में खुद को देखते हुए नहीं लिख सकती, यानी कोई देखता हो तो, उसी तरह चलना भी टूट जाता है अगर खुद को देखने लगो। यानी कोई देखने लगे।
चलना मेरे लिए जैसे लिखना।
जैसे मेडिटेशन। ध्यान। एकतान। वॉक-बिंदु पर अंतर्नेत्र फोकस। वॉक वॉक वॉक। बिंदु केंद्र। वॉक वॉक। बिंदु गायब। बस वॉक। अंदर बाहर बजरी की धुन। बन गए वही ध्वनि। बिसर गए गर्दिश में। ब्रह्मांड में समाहित।
मगर
मगर तब जब कोई देखे नहीं। वर्ना उकता जाओगे अपनी झलक से। थक जाओगे अपने अक्स से। कपड़े बदल डालोगे तो भी वह सामने होगा। आखिर ठोढ़ी का ढब और कंधे मचान तो वही पुराने रहेंगे! लोग भी पुराने होंगे। हैरान, परेशान, नजर भोंकू, नजर भौंकू।
एलर्जी हो जाती है। किसी को अंडे से। किसी को धूल से। किसी को घूरे जाने से, जैसे मुझे। तब करना पड़ता है घेरे को छोटा और अब यहाँ ही चलती हूँ।
सुबह सुबह। जब अँधेरा अभी पसरा पड़ा है। पहले कि उजाला दुनिया को नंगा करे और वह मुझे।
रुका जाए, मैंने सहज स्वर में खुद से कहा।
मानो मालूम नहीं कि बार बार यही कोशिश तो कर रही हूँ! हरी ओम जाने कब से। कहीं दरवाजा कोई खड़का, किसी की कमीज का रंग चमका, और मेरी चाल मुस्तैद; आगे पीछे नजर खाली ओर मैं फिर, फिरफिरफिर,
रुकजाबायाँ पैर – थमजादायाँ पैर।
जरा डगमग और फिर आगे!
अभी भी लेकिन मैं धीर ही थी। झट घबराने लगूँ ऐसी नही हूँ। धुकड़ पुकड़ को केचुआ मान भीतर अँधेरे में लुका देती हूँ और धीर गंभीर चलती जाती हूँ। बशर्ते कि उसके बारे में सोचूँ नहीं। चूँकि सोचा नहीं – जैसा केचुआ चाह रहा था – कि वह सर्प बनके उछल आएगा। और मुझे पूछना पड़ेगा। कहीं है तो नहीं यह घबराने लायक स्थिति?
इसका जवाब मैंने मुल्तवी कर दिया था।
फाटक फिर आ गया और गार्ड मुझे देख बाअदब खड़ा हो गया।
वाह, लगातार सामने पड़ने ने मुझे सलाम पाने के काबिल बना दिया।
सलाम, मैंने सर हिलाया, वेग से आगे निकलने के पहले, पर, तभी समझ आ गया कि वह डे गार्ड से ड्यूटी बदलने उठा था, बस!
हरी ओम वाले हँसने लगे। हाथ ऊपर आकाश की तरफ उठा कर। गाल फुलाके, मुँह फाड़ के। पागलों की तरह। ठहाकों से सेहत बनाते।
हा हा हा हा हा!
हो हो हो हो हो!
हि हि हि हि हि!
हु हु हु हु हु!
मुझ पर नहीं।
न…हीं…?
मुझ पर तो नहीं!
इमारतों के बीच से उनकी हँसी मेरा पीछा करती। मैं रल्ला सी निकल जाती। एक कउवा साथ साथ फुदकता चला। तू भी हँसता है? घूरता है? डरता नहीं। देख कउवे, तेरे देखने पे कोई गुरेज नहीं, मैं गोल गोल चलूँगी।
लोग और निकलने लगे थे।
मैंने चेहरा सँभाला, पैरों को धिक्कारा, शर्ट नीचे खींची, हाँ घुस गई थी नितंबों के बीच, गर्मी भी तो उठान पर थी, और मैं चलती रही। गोल पे गोल। हेज से सटी बजरी पे, मल्टी स्टोरी इमारतों के चारों ओर। सेमल से आम से पीपल से फाटक से सेमल से आम से पीपल से फाटक से…। रेस करो तो सात मिनट का राउंड, सौम्य चलो तो दस, बुढ़ऊ बनो तो आधा घंटा तक। एक राउंड पाँच सौ कदम। दो हजार डग पूरे तो एक मील पूरा। और सौ कैलोरी कम और दिल फेफड़े त्वचा की दमक ज्यादा, जरा कुछ तो, बुढ़ापा दूर सरक जाए, जरा मरा तो, उमर बढ़ ली, मिनट दर मिनट, और नींद हो गई गहरी, मीठी, घूम के लौट जाओ जब।
सब चंगा मानो, मैंने आतुरी दबाई, और चलती चलो, ठोढ़ी राइट, कंधे मचान, बाँहें मार्च ऑन, साँसें घमासान, पैर निर्दयी, पैर बेईमान।
और सुनो, किसी को क्या पता मैं कब से यहाँ हूँ? जो स्कूल बस पकड़ने निकली है उसने एक ही पलक तो देखा मुझे और गई। वे ऑफिस को चले, देखा, गए। अखबार वाले ने अपनी बाजीगरी आजमाई, देखा, और गया। जब जिसने देखा उसी पल मैं निकली हो सकती हूँ। घूमने। आपस में दरियाफ्त करेंगे कि तुमने कब देखा और हमने कब?
हाँ जी, मैंने तभी शुरू किया है जब आपने देखा!
इतना ही जरूरी बस, कि अपनी शुरुआत का चिट्ठा न खुलने दूँ। घंटों पहले – या और, मुझे क्या पता – का।
मंदिर की बगल से निकली, अपनी टाँगों और अपने परिवेश से तारतम्य बने होने का भाव ओढ़े और बेधड़क घूमती रही।
गुड मॉरनिंग, कोई बुदबुदाया। मैं जोश से पास से निकली। आज सारा गोश्त-ए-थुलथुल झटक देने की ठानी है, ऐसे!
कुछ मैं भी बुदबुदाई पर हम अलग हो चुके थे। मैं सेमल के नीचे थी जहाँ से मुड़ना पड़ता है।
रुकने की कोशिश नहीं की। कहीं वह देख रहा हो मुड़ कर? शर्ट खींची, फिर तो नहीं अंदर? लुढ़कती चली।
जैसे कंकड़।
चोर निगाह इधर उधर। आगे बढ़ो लेफ्ट राइट। अगला मोड़ यानी अगला पेड़ आम का मिरगिल्ला। तीव्र घुमाव धीमा चलो। मुड़ने का टाइम यानी रुकने का टाइम यानी कोशिश का टाइम यानी बेमुरौव्वत इन टाँगों से उम्मीद करने का टाइम यानी कोशिश तो की, धीरे भी हुई, रुकी पर नहीं। चुन्नी सी फड़फड़ा के आगे।
मैं कंकड़, मैं चुन्नी, चकरघिन्नी, फिरती गोल गोल सोसायटी के भीतर और
अबक्याकरूँ?
इतना साफ हो चुका था कि जिसे मैं रुकती गति समझना चाह रही थी वह था बदन का मोड़ पर डुगडुगाना कि बजरी के संग संग घूम लूँ वर्ना जा लड़ूँगी तने से या फाटक से या खंबे से।
यह मगर मैं जानती हूँ कि कोशिश मैं किए जा रही थी और वो कोशिश यह भी थी कि सर्प केचुआ बना चुपका रहे और चेहरा मेरा शांत रहे। एस ब्लाक की लेखिका, तंदुरुस्त, फुर्तीली, तंदुरुस्ती और फुर्ती बरकरार रखने मॉरनिंग वॉक में पिली हुई और इसमें अजीब क्या है?
इसमेंअजीबक्याजनाब?
मतलब मामला संतुलन का। संतुलन बरतने का। संतुलन दरसाने का। रुकने की नाकाम कवायद और सर्राटे से चलते पैरों के बीच सहजपन की डोर खींचने का।
कि सहज और बामकसद है ये होना – लट्टू, धूमकेतु, औरत।
सहज ये घूमना। सहज ये स्पिन।
हाय कि जो कर रहे हैं उसमें सहज रहें।
सहज दिखें।
सहज महसूसें।
सहज हो जाए तेरी आँखों में छवि मेरी।
सहज है ये, का प्रस्ताव रखें नया और यू.एन. उसे मंजूर कर दे।
थका देती है यह सहजपन की चाह।
मैं थकने लगी थी। तन में कम, मन में अधिक।
प्रश्न यह भी कि कितना वजन आज ही छिजाना है और चाहती भी हूँ मैं ऐसा वाह वाह फिगर?
हाय, सुस्ता लेने दो मुझे जमाने की भीड़ में छिप कर, मेरी थकी आत्मा की पुकार।
हँसना बंद हो गया। अब योग शुरू था। फ्लैटों के बीच से मैंने देखा। जैसे एनिमेशन फिल्म। टुकड़ा टुकड़ा जुड़ के बनती। अब नाव। अब मछली। अब साँप।
एक बूढ़ा आदमी, लाठी टेकता, कमर पे दोहरा झुका हुआ।
लाठी रखी।
सुस्ताया।
खड़ा हो गया।
टेढ़ा बकरा मगर सीधा।
रीढ़ लहरिया मगर सीधी।
सिर आकाश को, पाँव धरती पे।
मैं हैरान।
इधर वर्जिश, उधर वर्जिश।
मैं हैरान।
एक औरत कौन सा जानवर बनी है?
उकड़ूँ बैठी।
टाँगें उलटाए।
उलझाए।
पाँव कान पे, सिर पाँवों के बीच।
हथेलियों पर टिक के झूल रही है।
अगले राउंड में देखा वह जॉगिंग सूट में।
अगला राउंड, कहाँ गई?
अगला राउंड, झाड़ के पीछे जॉगिंग सूट तहा रही है।
अगला राउंड, गार्ड की ड्रेस में।
अगला राउंड, कहीं आदमी तो नहीं?
अगला राउंड, तो क्या हमारी सोसायटी ने औरत गार्ड रख ली है?
अगला राउंड, तो क्या मैं सोचती हूँ मैं ही इस जमाने की औरत जो अलग कुछ करने लगी?
अगला राउंड, अपनी याद आ गई क्योंकि कब तक न आती कि पैर हमारे हावी हैं और बछेड़ीपन के चक्कर हैं। थकान लौट आई, दर्द भी और अनचाही नजरें भी।
बिलाशक अब नजरें बढ़ गई थीं। मेरी छवि उनमें पुरानी पहचानी। हैरत उनमें स्थायी कि ये कौन क्या किस चौखटे में फिट? डे गार्ड झेंप के अलग मुड़ जाता मेरे फिर फिर फाटक पे प्रकट होने पर।
लोग भी वे आ गए थे जो दिन भर ठहरेंगे – प्रेस वाला, सब्जी वाला, फल वाला, गेट के बाहर। अब यह इत्मीनान कैसे करूँ कि एक बार देखेंगे और चले जाएँगे बिना ये जाने कि कब से और कब तक यही रील चल रही है।
आपस में कानाफूसी भी करने लगे हों वर्ना ये कामवालियाँ घरों में घुस के उनकी बाल्कोनी पर ‘नमस्ते मैडम’ करने आज तक तो झाँकी नहीं! औरतें भी औरतों के संग अपना कुरेदूपन नहीं छिपा पातीं!
बहरहाल मैं कर ही क्या सकती थी सिवाय गोल गोल चक्कर मारने के? क्या मैं सब कुछ कर चुकी थी – दूर पार्क के बड़े घरों से लेकर उससे छोटे, फिर और छोटे, फिर पास और और पास के घेरे में, और वापस उसी बिंदु पर पहुँच गई जहाँ से भागी थी? वही राउंड राउंड।
एक वादा मैंने तब किया। कि यह जोखिम अब नहीं उठाने की। बहुत कर ली राउंड राउंड सैर। करना है तो फ्लैट में करूँगी, छोटा है तो क्या? दस चक्कर यहाँ जुड़ के कुछ बनते हैं तो पचास वहाँ।
अच्छा सौ।
चलो दो सौ।
जितने भी करूँगी, वहीं करूँगी, अपनी दीवारों की हिफाजत में।
और पाऊँ कि वहाँ भी रुक नहीं पा रही तो मार तो सकूँगी अपनी काया को जोर से दीवार में या सोफे में या अपनी मेज पे और खुशी से सिर फटने दूँगी और बहने दूँगी खून उस जगह जहाँ मैं लिखना प्रिफर करती हूँ और लहूलुहान मौत में घुस जाऊँगी, अकेली निश्चिंत।
यहाँ इतना भी हक नहीं मुझे। कि तने में, दीवार में, गेट से, लड़ जाऊँ, किसी तरह झटके से घूमने पे। ओमाईगॉड मैंने कल्पना की, कैसे हँसी मंडली योगा शोगा छोड़ मेरी तरफ दौड़ पड़ेगी और कितनी सारी आँखें एक संग मुझ पर झुक मुझे घूरेंगी और मेरा खून किधर, कैसे, बह रहा होगा और मेरे कपड़े और मेरी खाल और मेरा जबड़ा न जाने कैसे घुचे मुचे फटे? क्या मालूम मैं बच्ची की तरह सुबकने लगूँ?
नो, नहीं, मैं पब्लिक में नहीं रो सकती।
नहीं, नो, मैंने अपने को फटकार पिलाई, आँखों में उमड़ते आँसुओं पर। बिल्कुल नहीं पता था मुझे कि मैं कब से घूम रही हूँ पर स्पीड मेरी हवाई जहाज और ओमाईगॉड मैं थक गई थी, जिस एहसास पर आँसू फिर उमड़ने को हो गए।
लोग थे कि जो शुरू किया था, पूरा करके उठ पा रहे थे। हँसी, योग, सब पूरे हुए, गाड़ियाँ भी बैक हुईं, निकल गईं। मैं ही – न बैक, न ब्रेक।
कार पार्क बल्कि अब पार्क था भले ही बजरी का। खाली खाली।
मेरे जूते उस पर बजते।
बिना व्यवधान और घोर संकल्प से, लग सकता है, मैं चलती रही।
हरी ओम मंडली उर्फ हँसी मंडली उर्फ योग मंडली अब रामनाम कर रही थी। मेरी हर झलक पे वे चीखते राम नाम एक, राम नाम दो।
राम नाम तीन।
राम नाम चार।
मैं गोल गोल।
राम नाम सत।
राम नाम सत।
मेरे कानों को लगा।
तब वह उछला, फन उठा के, केचुए से साँप बन के? मेरे अँधेरों से निकल के, और सटाक मेरे चेहरे पर फैल गया फुफकारता – ये हो क्या रहा है? इसका अंत होगा क्या? इसका अंत होगा?
या मेरी जैसी औरतें बस शुरू करती हैं, फिर चलती रहती हैं गोल गोल गोल गोल! बड़े घेरे से छोटे से छोटे…
चूर चूर।
जैसा कि कोई भी मेरी दशा में होगा। चल रही हैं सुबह से, पौ फटने के पहले से, मटमैले उजाले की बढ़त में।
सुबह से अब तक कितने घंटे हो गए होंगे, मैंने सवाल किया?
जिस पर सवालों का अंबार लग गया। कि क्या सिर्फ सुबह से? कहीं कल शाम से? या कल सुबह से, या परसों से?
अब मैंने याद करना चाहा कि सैर पर निकलने से पहले क्या किया तो शायद अनुमान लगे कि किस टाइम – दिन? – से निकली हूँ? पर सहसा जो क्रियाएँ याद आईं वे आम थीं और उनका अलग कोई समय नहीं होता, विशिष्ट कोई पहचान नहीं होती। कि चाय पी, सोई, ब्रा पहना, हाजमे की गोली ली, त्रिाफला पानी में घोल कर पिया। सवाल फिर भी कि ये नितक्रम आज किए कि कल कि और पहले? हथेली मुँह के आगे रखी – चलते हुए और ‘हाह’ करके साँस छोड़ी और उसे नाक की तरफ फूँका कि मंजन सूँघ पाऊँ, कितना ताजा है, अंदाजूँ?
निबट ली, पेट पर हाथ रखा? हल्का है कि भारी? और सू सू? ब्लैडर कहाँ है, हाथों से खोजा?
जो अच्छी सूझ नहीं थी, क्योंकि सू सू अभी ही किया हो तो भी वह याद करते ही फिर आ जाती है! सू सू, जम्हाई, अलादीन का जिन!
अब क्या, चक्कर काटते काटते पूछने लगी, इस नई सूसूलगीहै को मैं कहाँ बिठाऊँ?
बेवकूफीप्रद बात से बेहतर कुछ नहीं किसी ट्रैजेडी को मुकम्मल बनाने के लिए। दर्द का लिबास बार बार जोकराना होता है। नब्बे बरस की बुढ़िया अपनी नातिन की शादी के लिए तैयार हो रही है और झुर्रियों की लड़ियाँ पहने अपनी गरदन पर बहू बेटियों के हार ट्राई ऑन कर रही है, ये पहनूँ कि ये, जैसे उसके गले को निहारने बरात आएगी! आखिरी साँसें गिनता मरीज रेडियो थेरपी में ढेर हो रहा है पर जिद ये कि अलग रंग और डिजाइन की टोपियाँ लाओ, जो फबेगी वह मेरे बाल उड़े सिर को चाहिए। और हम, जो निकले इस दिन घूमने और घूमे ही जा रहे हैं और सू सू भी आ रही है!
ऐसी करुणा महिला वर्ग के प्रति कभी जो पहले मुझमें भरी हो? वॉक और ज्वारभाटा सी उफनती दबती लहर। काश कि बूँद बूँद चुआती बढ़ सकती इस विद्रोही सैर में!
आदमी भी, मुझे पता है, इस चपेट में मुश्किल में होता। पर यह भी हो सकता है कि आदमी होती तो इस स्थिति में ही न होती? नहीं, सच्ची! बार बार हालात के फेर में निकल न जाना पड़ता। निकल के घूरती नजरों से मुकाबला न करना पड़ता। चूँकि किस आदमी का ब्रा स्ट्रैप झाँकता है या ऐसा कुछ? उस पार्क से, इससे, पास, न लौटना पड़ता। अँधेरे पल, लुके कोने, ढूँढ़ने न पड़ते, जो करना था, उसे करने। जो करना था वही करना न पड़ता!
टट्टी पेशाब से मात खाई औरतों से ढेरों हमदर्दी के संग मैं चलती रही। मेरी मॉरनिंग वॉक में नया रुख आया, कह सकते हैं। कहाँ दबा के रख लेती हैं जब इस तरह दिन और लोगों के उजाले में होती हैं हम सब?
यह तक सूझ उठा मुझे, चलते चलते, – अब इसे दोहराने की जरूरत क्या? – कि मान लो देवी सीता पर भी यही मुसीबत आन पड़ी हो? लग आई और जाना था? जब किस्सा चरम पे था? पति बूँद बूँद बेइज्जती कर रहे थे?
दुख, जलालत, तिरस्कार की गरिमामय लपेट भी जोकराना! हिंदू देवी, हिंदू नारी, पतिव्रता, सेवारत, हाथ जोड़े खड़ी है, चेहरा अपमान में नहाया हुआ, माँ जननी फट पड़ो, मुझे, मेरी लज्जा के साथ, छुपा लो। वह नीचे गईं मगर ऊपर हो गईं, राम ऊपर थे मगर नीचे गिर गए!
पर
उस अभिमानी पल में उन्हें मेरी तरह लग आई हो? लज्जा बढ़ न जाती? विनती और विनीत न हो जाती?
फिर भी वे खुशनसीब कि छिप पाईं महान आत्मसम्मान के मुलम्मे में।
मगर मैं? क्या गरूर माथे पर पोतूँ, उजली धूप में जोकराना गति से गोल गोल चलती और ब्लैडर को बंद रहे… बंद रह… काबू…काबू…।
पैंट नीचे करके कूदूँ? क्योंकि कूदना तो पड़ेगा, मेंढक की तरह, क्योंकि पैर ये खुदगर्ज, दया धर्म दिखाने से रहे, एक पल अवकाश भी न देंगे?
तो फिर एक ही बात हो सकती थी… पर कैसे कहूँ… नहीं, नहीं कह सकती… नहीं… अपने से भी नहीं… कान बंद…। …!
बस चलते चलते चलती रही और पल पल और गरम होते सूरज ने बाकी जो करना था किया।
हाँ, सूरज उरूज पे था और धूप बढ़ गई थी। लोग मगर घट गए थे। शुक्र है! क्योंकि अप्रैल की दोपहरों में कोई, कब तक, बाहर रहेगा? वही जिसके पास कोई चारा न होगा! गेट वाले भी छायेदार सायों में बचे खुचे हो गए। धोबी, दुकानदार, सब। माली ने तय कर लिया कि लॉन, बाग, सारे की निराई, गुड़ाई, पानी हो चुके, अब सो लो। सुबह वाला व्यस्त वेग नहीं रहा।
मुझमें छोड़ कर! या मेरे पैरों में। जो ड्यूटी की तरह कायम थे। ड्यूटी में निर्लज्ज, मेरे संकोच पे हिकारती। चलते रहे, चलाते रहे।
पैरों की क्या कहूँ जब वे मेरे होकर भी मेरे नहीं, पर मैं (वैसे अब सोचती हूँ कहाँ हूँ मैं, पैरों में नहीं, दिल में, माथे में, पेट में, पैरों में तो नहीं?) शिद्दत से महसूस करती हूँ जो भी मैं महसूस करती हूँ। गर्मी का खयाल आ गया तो ढेरों गर्मी लगने लगी।
संभव है, क्यों नहीं, कि दिन चढ़ने का नतीजा था। महीना ग्रीष्म का, वक्त दोपहर का। घड़ी और कैलंडर तो बांधे नहीं थी पर कयास लगा सकती थी।
कहाँ चलूँ कि साया मिले? तीन पेड़ बाउंडरी पे! कोनों पर, जहाँ घुमाव आता था। कोशिश करने लगी कि पेड़ से पेड़ तक रेस करती जाऊँ (जो वैसे भी कर रही थी) नंगी हेज के संग संग, और पेड़ों के नीचे धीमी हो जाऊँ (जो वैसे भी होती थी)।
मैं साये से साये तक फाँदने लगी। जैसे जलती रेत पर एक परछाईं से दूसरी तक कूदते जाया जाता है। बीच के दरमियान को लगभग, पाँव बिना नीचे धरे, लाँघते!
क्या मैं उड़ती सी दीख रही थी? पेड़ से पेड़ से पेड़ तक?
पेड़ से पेड़ से पेड़ बस देखो और बीच की तचन मिटा दो तो तीन पेड़ क्या जंगल बन जाते हैं?
इस तरह चल रही थी मैं उस निष्ठुर अप्रैल के दिन, अपनी शुरुआत याद करने में असमर्थ और अपने अंत को पकड़ पाने में भी। तेज धूप में जलती, बचती, जलती…।
प्यास लगने लगी। पाइप दिखने लगा। या पाइप दिखने लगा और प्यास लगने लगी।
माली महोदय गमछा मुँह पर ओढ़े सो रहे थे, पाइप गमले के पास क्यारी में चलता छोड़! बिल्डिंग के बीच। मुझसे दूर मगर पास। मेरे पास फिर भी दूर।
हर बार दिखता। प्यास बढ़ाता।
तब मैं इस अभ्यास में लगी कि पाइप जहाँ था उस ओपनिंग पर गुजरते हुए दायाँ पाँव जरा और दाएँ फटक दूँ, नीचे रखने के पहले। नौकरी पहले मिल गई, हुनर बाद में सीखा! तो क्या? निरे ऐसे। डाक्टर, इंजीनियर, ड्राइवर, दो चार को मारा, कुछेक पुल गिराए, गाड़ियाँ फोड़ीं और सीख गए।
मैं भी करते करते कर गई।
पहले पाँव फटका।
फिर पाइप को किक मारा। अपनी तरफ गिराया।
गमले पर फेंका।
फिर दाहिने को झुक, चुल्लू में पानी उठा लिया।
उठा भी लिया, कुछ पी भी लिया।
एक्वागार्ड और आर ओ का पानी नहीं था वह, पर इन मौकों पर ऐसी बातों की दरकार नहीं होती।
वैसे, सच बताना है तो, पीपल के नीचे उगे मंदिर में चढ़े परशाद के टुकड़े, गरी और चना और इलायचीदाना, भी मैंने ऐसे ही उठा लिए। गिलहरी, चिड़िया, चींटी से गई बीती तो नहीं, हमारी भी इक जान है चारा माँगती।
जरा झुकी,
जरा और
हर राउंड में जरा और
और चील झपट्टा लग गया
और मैं गिर के तमाशा भी नहीं बनी।
फिर सतर और लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट।
बाद में पूछने वाली थी कि कब मैंने खाया और कब पिया, उसी रोज या अगले रोज या उसके भी बाद, मगर वक्त पहली चीज थी जो मैंने गँवाई उस अजीब घड़ी में, जब भी वह थी, और इसलिए मैं बता न पाऊँगी।
फिर जलते सूरज की आदत पड़ गई। न दहकान थी, न पसीना।
या सूरज ही शीतल हो चला था।
इस पर जरूर मेरा ध्यान गया कि स्कूल के बच्चे लौट रहे हैं और अंदर जाकर अपनी माताओं को लेकर अपने बरामदे बाल्कोनी पर आकर मेरी तरफ इशारे मार रहे हैं। स्पष्ट नही, फिर भी। पता तो लग ही जाता है।
शायद…?
हाँ शायद उन्होंने ही, औरतों और बच्चों ने, काम से लौटे आदमियों को खबर दी कि लगता है कोई औरत सुबह से वॉक कर रही है। या कब से? और लोग बाल्कोनी पर जमा होने लगे और शाम की लाली में खड़े मुझे देखने लगे। यह जतलाते कि थक के लौटे हैं काम काज, ट्रैफिक, के बाद और अब पना, चाय, लस्सी, रूहअफजा पीने क्यों न निकलें अपनी ही बाल्कोनी पर, चाहे हो या न हो कोई बावली जो मैराथन ढंग से गोल पर गोल पर गोल चक्कर काट रही है।
सबने देखा – एक ही पल में नहीं जैसा बता चुकी हूँ पर जब जिसके आगे मैं पाँव पटकती पड़ जाती – और बिना बूझे नजर हटा ली।
या क्या मालूम मैं ही देख रही थी और वे सब वही कर रहे थे जो हर रोज करते हैं? बेशक किसी ने मुझे रोका नहीं, कूद के मेरी राह में, जबरन कंधे बाँहें खींच के मेरा पाँव रस्सी में फँसा के मुझे गिराया नहीं, ना ही जाल फेंक कर उसमें मुझे जकड़ दिया। मैं आजाद थी बशर्ते उनकी राह में व्यवधान न बनूँ। जो मैं नहीं बनी, थोड़ा बाएँ, थोड़ा दाएँ, झुकने बलखने में माहिर, बिना उन्हें या उनकी गाड़ियों को ठोकर मारती, चलती हुई।
लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वे समझ नहीं पा रहे थे कैसे मुझे मना करें? उन्हीं सब की तरह जो अभिवादन करने से कतराते थे कि क्या कहें? क्या मालूम ये मन ही मन कुढ़ रहे हों पर कैसे तो मुझे हाथ लगाएँ? गार्ड से कहें? पुलिस से कहें? पुलिसवुमैन से कहें?
इस पर तो मैं मर ही गई। बिना मरे यानी! बस पानी पानी। इस कदर खुराफाती लगती हुई। मुझे पता था, मेरा रोंआ रोंआ जान रहा था कि मेरा अनजाना ढंग उन्हें परेशान कर रहा है। नाहक चर्चा होगा। मखौल बनेगा। उनकी हाउजिंग सोसायटी को लेकर फब्तियाँ कसी जाएँगी। प्रेस वाले भी कैमरे शैमरे लेकर पहुँचेंगे। कोई समझ नहीं पाएगा कि मुझे कैसे रोकें – ये भी नहीं कि मैं खुद भी नहीं जानती – पर इतना ज्यादा मंच पर होना सबको खलेगा। बहू बेटियों वाले। एैरे गैरे पहुँचेंगे मेरा नाटक देखने के बहाने उनके घरों में ताक झाँक करने। बच्चे अलग पढ़ाई लिखाई छोड़ बाल्कोनी पर भागे जाएँगे – अब क्या कर रही है, रुकी या अभी भी चल रही है? जो चिंता की बात होगी आज के कॉम्पटिशन के जमाने में और घटती नौकरियों की दुनिया में। इसका खेल है क्या, सब सोचेंगे? कौन सा नारीवादी शगूफा अब खिला रही है? जोर से प्रतिवाद करने से इसलिए भी वे डरेंगे कि क्या पता ये नारी आंदोलन वालों को जमा कर दे उनके दर पे धरना देने?
ओह ओह मैं अपराधबोध से भरने लगी और सोचने लगी पूरी ईमानदारी के साथ कह दूँ, सच उगल दूँ, और चिरौरी करूँ कि तमाचा लगा के पहले मुझे गिरा दो, फिर धर दबोचो और हिलने न दो।
मेरी आत्मा पर इतना बोझ और फिर भी चक्कर काटे जा रही हूँ।
क्रांति होगी कोई, इन सिरफिरी औरतों की, बड़बड़ा रहे होंगे।
मुझे समझाना पड़ेगा। मुझे विनती करनी पड़ेगी। कि समझें। उनकी बहुत बातें हैं जिनसे मैं सहमत नहीं, पर इस दफे मैं दूसरी तरफ नहीं हूँ, उन्ही की साइड पर हूँ और जैसा कहते हैं अबला नारी हूँ, किस्मत की मारी हूँ, हारी हुई कहानी हूँ, अलबत्ता कुछ नए घुमाव के साथ!
ऐसे नहीं चल सकता।
मतलब ऐसे नहीं चल सकती।
मुझे बिना लाग लपेट पूरा खुलासा करना होगा। माफी माँगनी होगी, जो मैं ऐसी हूँ, जैसी हो गई हूँ। मेरे तन मन आत्मा इस निराले गोल मेल में!
मैंने कातर नजर उठाई, अपनी चाल में नेक इरादा डाल उससे ताल मिलाई और बढ़ी, कि जो दिख जाए उसी को समझाऊँ।
धुर सामने, फाटक पर, चिट्ठियों की गड्डी फेंटते इंजीनियर साहब।
‘हैलो’ मैने मुँह खोला, उनके करीब आते हुए, ‘सुनिए टुक…।’
पर वे गार्ड को कस के डाँट पिला कर सर उठा के निकल गए।
गार्ड ने भी अनदेखा किया, जरूर चिढ़ के, कि मैंने उसको फटकार पाते देख लिया।
अब किससे, मैं चलती चली, दोनों तरफ चौकन्नी देखती। सोसायटी का प्रेजिडेंट दिखा, माली को डाँटता कि झाड़ें क्यों छाँटीं और डालें क्यों ट्रिम की? आपकी तो सातवीं मंजिला शान, दूसरे कहते, ऊपर से हरियाली सराहो, पर हम तो नीचे जहाँ कीड़े मकोड़े, मच्छर, शायद साँप भी, निकलते हैं, तो काट दो।
छाँटो, न छाँटो, के बीच माली रूठा खड़ा था और प्रेजिडेंट उर्फ रिटायर्ड आई.जी. ऐसे जैसे हाथ में पुलिस का डंडा अभी भी!
पर यह पल गरूर दिखाने का नहीं है, मैंने तय किया।
‘मिस्टर आई.जी.’ मैंने शुरू किया।
वे मुझसे कुछ गज की दूरी पर, उसी राह पर जिसकी मैं खाक छान रही थी।
‘मिस्टर प्रेजिडेंट’ मैंने हाथ सलूट में उठाया। थोड़ा पहले से ही चालू, क्योंकि उनके पार निकल गई और अपनी बात पूरी न कह पाई तो क्या आगे बजरी को सुनाती निकलूँगी? आई.जी. साहब मेरे संग संग बाअदब दौड़ने नहीं वाले कि मैं अपनी दो टका बात पूरी कर सकूँ!
पर जैसी मेरी उनसे अपेक्षा भी थी, जनाब ने सरसरी निगाह मुझ पर फेरी और कि-त-ने मगरूर ढंग से मुँह उधर, हाथ से हवा में यों वार करते कि मक्खी उड़ा रहे हों।
उफ्फ, तमाचा लगाना चाहिए, मैंने बेबस चलते सोचा। ये सामंती टुकड़े किसी युग के, अंग्रेजों की औलाद, फासिस्ट जल्लाद।
मुझे मगर जरूरी काम है, तमाचों, तानाशाहों, पर गौर करने का ये समय नहीं।
समय होता तो अपनी मंशा पर शक कर लेती शायद। अपने को यह बता लेना कि इन हैरतमंद, परेशान, चकित, जनता, बच्चों की खैरख्वाही में तैयार हो गई हूँ कि मुझे शिकार मान लो और पकड़ लो, ना कि यह मेरी आखिरी उम्मीद थी कि रुक पाऊँ उस अजीबोगरीब दिन की उस अजीबोगरीब गश्त में।
पर जब पूरे जहान को यह बीमारी है तो मुझे अलग कर के क्यों देखा जाए कि करते हैं जो करते हैं खुद के लिए मगर मानते हैं परहित के लिए, कि यह तो संवेदना और भलमनसाहत हमारी!
मैंने फिर कहने की कोशिश की। फिर और फिर। जो रास्ते में या पास में दिख जाए उसी से।
माफ करिएगा…
सुनिए…
प्लीज…
हे…
एक्स्क्यूज मी…मैं…नहीं…मगर…
हर बार नाकामयाब।
मेरे चलते चलते सूरज डूब गया और इलैक्ट्रिक बल्ब जल उठे। उन पर अँधेरा लहरा रहा था और मैं चक्कर काट रही थी और अपनी सुनवाई की चेष्टा किए जा रही थी। सोसायटी के एक एक बाशिंदे से।
बदतमीजी से, लापरवाही से, सब ऐसे पलट जाते अलग, कि मैं कुछ भी नहीं।
तब तक शाम गहरा चुकी थी और फ्लैट लैंप की तरह जल उठे थे।
आठ बजे होंगे, मैंने अनुमान लगाया, जब आरती का मजमा निकलने लगा। हर राउंड में पीपल के नीचे थोड़े और लोग आ जाते। इसी सोसायटी के पांडे पुरोहित आ गए। और औरतें दीया जला के पूजा करने लगीं और सभी भक्ति में एकजुट हो गए।
मैं झेंपी झेंपी निकली, कई कई बार, इस अड़ में पक्की कि इतनों में एक से तो कह ही दूँगी। भजन प्रार्थना वालों में दया की कमी न होगी। अरज ही तो सुना रहे थे। मेरी भी अरज सुन लो।
बार बार आ जाती, झेंप से अलग देखती, धार्मिक सौहार्द से शीश झुकाती, आँखें मिलाने के फेर में आँख मिलाती।
यह आखिरी मौका न फिसल जाए हाथ से, हर चक्कर में और विकल हो रही थी। तो मैंने हर बार, मंदिर की बगल से परेड मारने के दौरान, संपर्क की कड़ी अभी से बनानी शुरू कर दी। हर बार सिर अतिरिक्त जोरों से हिलाया और जिससे आँख मिल गई उसकी तरफ पूरी पूरी मिन्नत आरजू से देखा। आँखों से याचना करती कि प्लीज… अरज… सुनो… मेरी… पूजा के उपरांत हाँ हाँ, एक तरफ रुकी हूँ, मतलब ठिठक के नहीं, चलते हुए ही रुकी हूँ और ठिठक के क्यों नहीं वही तो… अरज…सुनो…मेरी…, एक राउंड लगा कर आती हूँ फिर बताती हूँ, अधूरी बात अगली किस्त में, अगला राउंड अभी आई, भूलना नहीं, पूजा के बाद इधर मुखातिब होना, जब फुरसत हो जाएगी, और सुनना और पकड़ लेना मुझे और रोक देना और बाँध देना।
कृपया…। एक।
मेहरबानी…। दो।
प्लीज…। तीन।
विवश…। चार।
आरती के बीच घूम घूम के मैं अपनी प्रार्थना कर रही थी।
अब, मैंने कहा, एट लास्ट, जब भीड़ हटने लगी।
सुनिए…
ये जो हो रहा है…
तय करके नहीं…
न कोई षड्यंत्र…
सुनिए तो सही…
भीड़ और छँटी। मुझसे, मुझ पर गुजरती से बेजार, बेखबर, अंधे, बहरे, गूँगे।
‘हे।’, मैंने आवाज लगाई।
‘आप मुंझे खास पसंद न करते हों तो भी।’
मैं बिलबिलाई।
‘ओके, आप मुझे नापसंद करते हों तो भी।’
मैं चिल्लाई।
‘नफरत करते हों तो भी क्या?’ मैं गरज पड़ी।
कोई सुन नहीं रहा था।
आरती की थाली तक मेरे धुर आगे से यों ले जा रहे थे जैसे अगरबत्ती का धुआँ, आरती, आचमन, कुछ मुझे नहीं मिलना चाहिए।
धर्म और क्रूरता, करारा कुछ उस पर मैं उनके मुँह पे कह सकती थी। पर कहने की तो कुछ और कोशिश कर रही थी। और कर इतना ही पा रही थी कि अर्ज बनी उनके बीच से निकल जाती हर बार, पर सुनो यह मेरे बावजूद है, चिल्लाती।
और वे मेरी बगल से निकले चले जा रहे थे, निकलते ही जा रहे थे। जैसे मैं वहाँ थी ही नहीं। जैसे मैं सूखा तिनका हूँ हवा में बेआवाज सरकता जिसे देखने की जरूरत नहीं। सच्ची, वे बेझिझक अपने अपने फ्लैट में लौट गए और कोई कोई तो मजा लूटने बाल्कोनी में भी आ बैठे, व्हिस्की, जिन, रम, बर्फ पे उँड़ेल के और पकौड़े शकौड़े खाते रहे एकदम बेपरवाह कि ठीक उनकी नाक के नीचे एक बेचारी औरत फँस गई है, थक गई है, अकेली पड़ गई है, सहारा चाह सकती है।
कोई संदेह नहीं कि किसी ने दिखावा करना भी लाजमी नहीं समझा कि मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे मेरी सनक में कुदकने छोड़ दिया। वे पीते रहें, खाते रहें, उनके माल असबाब सलामत रहें तो परेशानी क्या और किसकी? बस उनकी राह में रोड़ा न बनो।
सो तो मैं कहाँ थी, उनके सामाँ से अलग, दाएँ बाएँ होते हुए चलने में मेरा कोई सानी नहीं।
सिर्फ सेमल ने कोई भेदभाव नहीं किया और मुझ पर और बाकी सोसायटी पर अपने नर्म नर्म फाये गिराने लगा। एक मेरे कंधे पर फिसला, एक मेरी नाक पर टिक गया।
Download PDF (चकरघिन्नी)
चकरघिन्नी – Chakaraghinnee