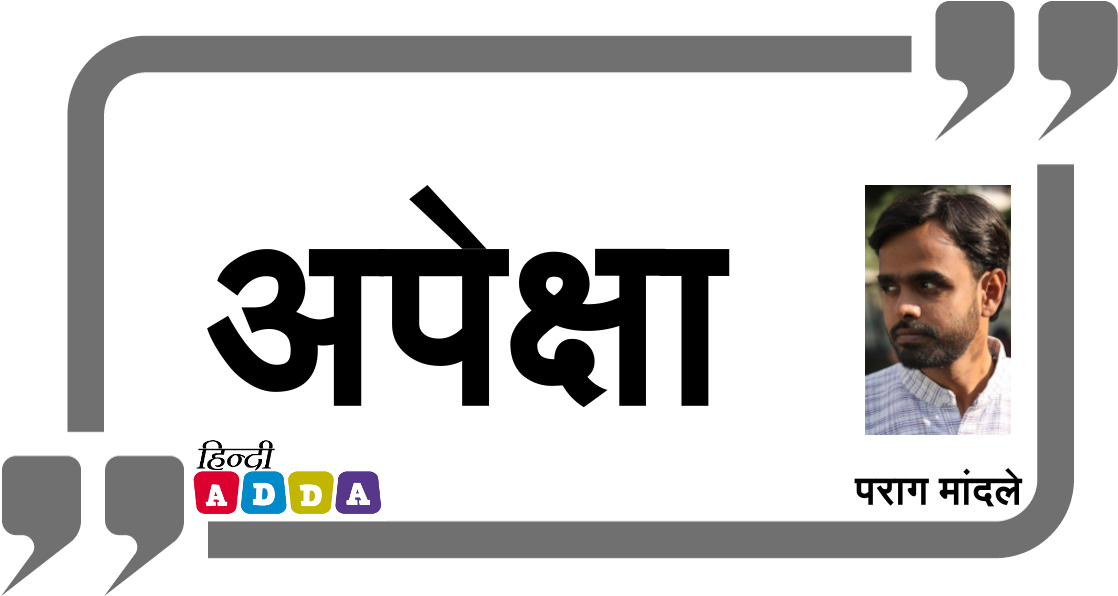अपेक्षा | पराग मांदले – Apeksha
अपेक्षा | पराग मांदले
उन दिनों कुछ भी सामान्य नहीं था।
न मेरा जीवन, न मैं और न मेरी दिनचर्या।
एक जुनून-सा छाया हुआ था दिलो-दिमाग पर।
अपने-आप को खो देने का जुनून। अपने-आप को भुला देने का जुनून।
उसी जुनून ने मुझसे एक बहुराष्ट्रीय कंपनी की ऊँचे पद वाली नौकरी छुड़वा दी थी और ले आया था इस छोटे-से शहर के छोटे-से अखबार की छोटी-सी दुनिया में।
वास्तव में उन दिनों मेरी मनःस्थिति ही कुछ ऐसी थी। जीने की कोई ख्वाहिश भीतर नहीं बची थी और मरने की कोई राह मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। मैं मरना चाहता था मगर आत्महत्या नहीं करना चाहता था। और माँगने से मौत मिलती नहीं है कभी। सो जीना मजबूरी बन गई थी मेरी। मगर उन दिनों मेरा जीना भी एक तरह से अपने-आप को मिटा देने की कोशिश करते हुए समय काटना था। कम से कम मेरे तमाम यार-दोस्त और रिश्तेदार यही कहते थे। उनकी हर दिन की नसीहतों से तंग आकर मैंने अपना शहर ही छोड़ दिया था।
मोटी तनख्वाह और रुतबे वाली मेरी नौकरी किसी और के लिए चाहे जितनी आकर्षण की वजह हो मगर मुझे उसमें कोई रुचि नहीं थी। उसे छोड़कर मुझे कुछ खोने का एहसास एक पल के लिए भी नहीं हुआ। उन दिनों मुझे लगता था कि अब मेरे पास खोने के लिए ऐसा कुछ नहीं है, जिसका मैं अफसोस कर सकूँ। एक निम्न-मध्यमवर्गीय परिवार की पृष्ठभूमि से उठकर इस मुकाम तक जिसकी खातिर मैं पहुँचा था, जब वही मेरे साथ नहीं थी तो बाकी बातों का अर्थ ही क्या था मेरे लिए? अपने लिए मैंने बस एक को ही चाहा था। उसे चाहने के बाद मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं चाहा। जो चाहा, जो पाया सब उसके लिए। अपने जीवन में मैंने केवल उसका सपना देखा, बाकी सारे सपने, उसके सपनों को पूरा करने के लिए थे।
हुआ क्या था, यह मैं आज तक नहीं समझ पाया। सच तो यह है कि मैंने इस पर बहुत अधिक विचार भी कभी नहीं किया। मेरा हमेशा यह मानना रहा कि जो हो गया है, वह सबसे मुखर और प्रखर सत्य है। उसके कारणों की मीमांसा कर लेने पर भी, जो हुआ है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन संभव नहीं है। ऐसे में व्यर्थ की माथापच्ची का क्या लाभ? मेरे भीतर कुछ बनकर दिखाने के, कुछ कर गुजरने के सपने जगाकर वह अचानक क्यों मुझसे दूर हो गई, यह मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ। मैं यह भी तय नहीं कर पाया कि उसने सचमुच मुझसे प्यार किया भी था या नहीं। मुझे सिर्फ इतना मालूम था कि मैंने उसे दिल की गहराइयों से चाहा था, पूजा था। उसके बिना जीना मेरे लिए सिर्फ जहर के घूँट पीना था। और मैं सचमुच वही कर रहा था।
कहने के लिए मैंने एक कमरा किराये पर ले लिया था, मगर वहाँ रहने का अवसर बहुत कम आता था। मेरा अधिकांश समय अपने अखबार के दफ्तर में ही बीतता था। दोपहर से लेकर देर रात तक वहाँ हर तरह का काम करना और फिर रात को भी कई बार वहीं सो जाना। अखबार का दफ्तर सही मायने में मेरा पहला घर था। चूँकि मैं काम में अपने-आप को डुबो देना चाहता था, इसलिए इस मामले में मेरी कोई पसंद-नापसंद नहीं थी। जो भी काम मेरे सामने होता, मैं उसे पूरा करने में जी-जान से जुट जाता। खबरें बनाना हो, लेख लिखने हों, खबरों और लेखों को संपादित करना हो, प्रूफ देखना हो, कोई रिपोर्ट तैयार करनी हो, किसी संवाददाता सम्मेलन में जाना हो। मेरे लिए कुछ भी अवांछित या अस्वीकार्य नहीं था। जाहिर है, अखबार के मालिक मुझसे अत्यधिक प्रसन्न थे। इसलिए और भी ज्यादा प्रसन्न थे कि इतना सब कुछ करने के बावजूद मेरी कोई माँग नहीं थी। मगर इतना मुझे स्वीकार करना होगा कि वे मुझे, मेरी बात को पूरा सम्मान देते थे और मेरे लिए अधिक से अधिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने का प्रयास भी करते थे।
उन दिनों कुछ भी सामान्य नहीं था।
मेरा जीवन तो असामान्य था ही, मेरे जीने का ढंग भी असामान्य था। और असामान्य थी मेरी दिनचर्चा भी। ऐसे ही दौर में अचानक बड़े असामान्य तरीके से मनीषा का मेरे जीवन में आगमन हुआ। शहर अपेक्षाकृत छोटा था। आधुनिकता वैसे भी उस दौर में बहुत धीमी गति से अपना सफर तय करती थी। टी.वी. का आगमन उस समय उस शहर में हुआ ही था। चुनिंदा धनवान लोगों के घर में टी.वी. हुआ करता था और उस पर आने वाली फिल्म, चित्रहार और हमलोग तथा खानदान जैसे धारावाहिक देखने के लिए पूरा मोहल्ला जमा हो जाता था। बच्चों में तो बाकायदा हर बार आगे बैठने के लिए झगड़े हो जाया करते थे।
जिस मकान में मैंने एक कमरा किराये से लिया था, वहाँ दो और किरायेदार रहते थे। उस मकान में प्रवेश का एक ही मुख्य दरवाजा था। उसमें प्रवेश करते ही सामने एक आँगन-सा आ जाता था। उसके दाहिनी ओर जहाँ तीनों किरायेदारों के संयुक्त प्रयोग के लिए शौचालय और स्नानगृह बना हुआ था, वहीं बाईं ओर दो किरायेदारों के घरों के प्रवेशद्वार थे। उन दोनों किरायेदारों के पास दो-दो कमरे थे। मुख्य प्रवेशद्वार के ठीक सामने मेरा इकलौता कमरा था, जहाँ मैं मुश्किल से कुछ समय रहा करता था। बाकी दो किरायेदारों में से एक मनीषा का परिवार था।
मनीषा के पति के बारे में मेरी जानकारी बहुत सीमित थी। जितना मुझे पता था और जो कुछ बाद में पता चला उसके अनुसार वह कोई बीस-बाईस साल का लड़का था। उन दिनों शहर के एकमात्र डिग्री कॉलेज से बी.ए. कर रहा था और साथ ही साथ एक प्राइमरी स्कूल में नौकरी भी कर रहा था। पिता थे नहीं। माँ गाँव में रहती थी, जहाँ उनका घर और कुछ खेती थी। नया-नया गौना हुआ था। नई बहू को ठीक से प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से माँ उन दिनों वहीं आई हुई थी। वह पूरी तरह से रूढ़िवादी और परंपरागत विचारों वाली अधेड़ महिला थी, जिसने जवानी में ही अपने पति को खो दिया था और बड़ी मुसीबतें झेलकर अपने इकलौते बेटे को बड़ा किया था। स्वभाव से बहुत सख्त। बहू सारा समय लंबे से घूँघट में रहे, इतना ही उसके लिए काफी नहीं था। अपनी सास के सामने मनीषा को अपने पति से भी बात करने की अनुमति नहीं थी। बाहर कहीं जाना उन दिनों उन दोनों के लिए किसी सपने की तरह था। दो कमरे के उस घर में पति-पत्नी को एकांत बहुत कम सुलभ होता था और आपस में बात करने का अवसर भी।
उन दिनों यदा-कदा मेरा जब भी मनीषा से सामना हुआ, मैंने उसे लंबा-सा घूँघट निकाले हुए ही देखा। एक-आध बार ऐसा भी हुआ कि मैं अचानक उसके सामने तब आ गया जब उसके चेहरे पर घूँघट नहीं था। ऐसे समय वह हड़बड़ी में झट से अपने चेहरे पर लंबा-सा घूँघट खींच लिया करती थी। हालाँकि मैंने उसकी ओर कभी ध्यान नहीं दिया। मेरी उन दिनों किसी लड़की में ही कोई रुचि नहीं थी। पच्चीस साल की उम्र में ही मानो मेरे भीतर अधेड़ावस्था का वैराग्य आ गया था। यह स्थिति कुछ दिनों तक बनी रही।
उन दिनों यदि मैं देर रात को दफ्तर से कमरे पर आ भी जाता तो देर सुबह तक सोया रहता था। मेरी सुबह तब होती थी जब और लोगों की दोपहर शुरू हुआ करती थी। मेरी इस आदत से उस मकान में रहने वाले सभी लोग परिचित थे। एक दिन न जाने कैसे देर रात को सोने के बावजूद मेरी नींद सुबह जल्दी खुल गई। मैं मुँह-हाथ धोने को बाहर निकला तो सामने मनीषा दिखाई दी। शायद अभी-अभी नहाकर बाहर आई थी, क्योंकि उसके गीले बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे। वह आँगन में लगी डोरी पर कपड़े सुखा रही थी। उसका ध्यान मेरी ओर नहीं था मगर न जाने क्यों मैं हमेशा की तरह उसे अनदेखा नहीं कर पाया। पहली बार मैंने इस बात पर ध्यान दिया कि उसकी उम्र मुश्किल से सत्रह साल थी। उस समय उसका धुला-धुला-सा चेहरा किसी ताजे खिले फूल की तरह लग रहा था। मैं उसे देखकर अपने दरवाजे पर ही ठिठका खड़ा रह गया। कपड़े डोरी पर डालकर जैसे ही वह मुड़ी, उसका ध्यान मेरी ओर गया। मुझे देखकर वह कुछ सकपका गई। उसने तुरंत सिर पर पल्लू लेना चाहा, मगर हड़बड़ी में आँचल उसके हाथ नहीं आया। घबराकर वह दौड़ती हुई अपने घर में घुस गई। मुझे उसकी इस घबराहट पर हँसी आ गई। मैं हँसता हुआ हाथ-मुँह धोने के लिए स्नानगृह की ओर बढ़ गया मगर न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हुआ कि दो बड़ी-बड़ी आँखें दरवाजे के पीछे से अब भी मुझे देख रही थीं।
उस समय बात वहीं खत्म हो गई। कुछ देर बाद तैयार होकर मैं हमेशा की तरह अपने दफ्तर पहुँच गया। दिन भर काम में व्यस्त रहा। रात को जब सारा काम खत्म करके थककर कुछ पलों के लिए कुर्सी पर सिर टिकाकर बैठा तो मुझे भयभीत हिरनी-सी विस्मय से भरी हुई दो बड़ी-बड़ी आँखों का ख्याल आ गया।
इसके बाद शुरू हुआ एक खेल, आँख-मिचौली का। रोज सुबह मैं जब भी अपने कमरे से बाहर निकलता, मेरे मन में यह ख्याल आ ही जाता कि शायद मनीषा मुझे दिखाई दे। यदि मनीषा सामने पड़ जाती तो हमेशा की तरह जल्दी से अपने चेहरे पर घूँघट खींच लेती। मगर दो-तीन दिनों में ही मुझे इस बात का एहसास हो गया कि मुझे देखकर घूँघट खींचने के बीच का अंतराल बढ़ने लगा है। इस सिलसिले को अभी एक सप्ताह ही बीता था कि एक दिन मैंने पाया कि उस अंतराल में ही एक मुस्कराहट मनीषा के चेहरे पर खिली हुई थी। उसके बाद मैंने भी यह चाहा कि उस मुस्कराहट के बदले में मेरे होठों पर भी मुस्कराहट आए मगर न जाने क्यों मेरे होठों की मुस्कान पूरी तरह से खिलने की जगह अधबीच ही मुरझा जाया करती थी।
कुछ दिनों बाद एक दिन जब मैं दफ्तर जाने के लिए अपने कमरे से निकला तो सामने मुझे मनीषा दिखाई दी। उसने मुझे देखा मगर उस दिन पहली बार मुझे देखकर चेहरे पर घूँघट नहीं खींचा। उस दिन उसके चेहरे पर उभरी मुस्कराहट में गहराई थी। उसकी इस अदा ने मेरी मुरझाई मुस्कान में एक नई जान फूँक दी। अपने-आप मेरे चेहरे पर भी मुस्कराहट उभर आई। हालाँकि मैं ठहरा नहीं, मगर बहुत दिनों बाद उस दिन मैं किसी जिंदा लाश की तरह दफ्तर नहीं पहुँचा। सारा दिन बहुत प्रफुल्लित होकर मैंने काम किया। बहुत दिनों बाद मैंने महसूस किया कि मेरे भीतर जीवन का कोई अंश अब भी बचा हुआ है। अभी सब कुछ खत्म नहीं हो गया है।
उस दिन के बाद मनीषा से जब भी मेरा सामना होता, यदि आसपास कोई और न होता तो फिर वह परदा नहीं करती। हम दोनों एक-दूजे को देखकर मुस्कराते। मुझे कई बार महसूस होता कि मनीषा मुझसे कुछ बात करना चाहती है, मगर तय नहीं कर पाती है कि बात किस तरह से शुरू की जाए। वैसे भी जिस माहौल में वह रह रही थी, उसमें यह बात न आसान थी और न सामान्य। मैं समझ सकता था कि वह बिना परदा किए मेरे सामने आती है, इसके लिए उसे अपने मन के भीतर पसरी रूढ़ियों और परंपराओं की कितनी जड़ों को काटना पड़ा होगा। गाँव की एक लड़की, जो अपनी सास के सामने अपने पति से भी बात नहीं कर सकती थी, एक पराए पुरुष से बिना किसी औपचारिक परिचय के किस तरह बात करती? बात किस तरह शुरू की जाए, इस बात की कशमकश उसके चेहरे से कई बार साफ-साफ झलकती थी। कभी-कभी मैं सोचता कि मैं ही अपनी ओर से पहल करके उसकी इस मुश्किल को आसान कर दूँ। मगर मैंने ऐसा किया नहीं। वास्तव में मैं यह देखना चाहता था कि वह बातों का सिलसिला किस तरह शुरू करेगी। मैं जानता था कि ऐसा होने में बहुत अधिक देर नहीं है।
हुआ भी ऐसा ही। एक दिन जब मैं दोपहर के करीब दफ्तर जाने के लिए निकला तो सामने ही मनीषा दिखाई दी। हमेशा की तरह मुझे देखकर वह मुस्कराई। मैं भी मुस्कराया। उस दिन हमारे तीसरे पड़ोसी के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। मनीषा का पति स्कूल चला गया था और सास भी कहीं गई हुई थी। मैं आगे बढ़ ही रहा था कि कुछ हिचकिचाते हुए मनीषा ने पूछा, ‘आप किसी अखबार में नौकरी करते हैं ना?’
मैं सुखद आश्चर्य से भर उठा। मुझे लगा जैसे वह बोली नहीं है, कोई अल्हड़-सी पहाड़ी नदी अपनी उन्मुक्त लहरों पर सवार होकर मचलती हुई कुछ आगे बढ़ी है। मैं कुछ देर तक उसकी आवाज की खनक में ही खोया रहा। फिर मेरा ध्यान गया कि मनीषा अभी भी अपने प्रश्न के उत्तर की प्रतीक्षा कर रही है। मैंने स्वीकृति में सिर हिला दिया।
‘बहुत काम करना पड़ता होगा न आपको? आपका ज्यादातर समय तो दफ्तर में ही बीत जाता है।’ उसने बात को कुछ आगे बढ़ाया।
मैंने मुस्कराकर कहा, ‘हाँ, काम तो करना पड़ता है, मगर फिर भी तुमसे तो कम ही काम करता हूँ मैं।’
इस बात पर खिलखिलाकर हँस पड़ी वह। उसकी वह सिंदूरी हँसी में नहाकर मैं भी सिंदूरी-सिंदूरी हो गया। उस हँसी ने मानो बहुत से बंधन तोड़ डाले थे। मैंने कहा, ‘अच्छा, मैं चलता हूँ।’ उसने मुस्कराकर स्वीकृति दी। बाहर निकलते हुए न जाने क्यों मेरा बहुत मन किया कि अभी तुरंत मैं किसी ऊँचे हिम शिखर पर पहुँच जाऊँ और जी भर कर चिल्लाऊँ। उस दिन मैं दिन भर सालों से भूले हुए बहुत से पुराने गीत गुनगुनाता रहा।
उस दिन के बाद जब भी अवसर मिलता, मनीषा और मेरे बीच बातें होने लगीं। टुकड़ों-टुकड़ों में हुई बातों से मुझे पता चला कि मनीषा की शादी जब वह केवल दस साल की थी, तभी राकेश के साथ हो गई थी। उसने गाँव के स्कूल से ही मैट्रिक तक की पढ़ाई की थी। छह माह पहले ही उसका गौना हुआ था। उसकी सास बहुत सख्त स्वभाव की थी और उसे बहुत बंधनों में रखा करती थी। उसके पति राकेश की कभी अपनी माँ का विरोध करने की हिम्मत नहीं होती थी। वह माँ की हर बात में हाँ में हाँ मिलाया करता था। इन छह महीनों में उसकी राकेश के साथ भी बहुत कम बातें हुई हैं, क्योंकि सास के सामने वह उससे बिलकुल बात नहीं कर सकती है। पति के साथ बाहर कहीं जाना तो बहुत दूर की बात है, वह अपनी सास के साथ भी केवल एक-दो बार ही सिर्फ मंदिर तक गई है।
मुझे लेकर मनीषा के भीतर बहुत जिज्ञासा थी। वह मेरे बारे में बहुत कुछ जानना चाहती थी। उसे मेरा जोगियों का-सा जीवन बहुत विलक्षण और रहस्यमय लगता था। जब भी अवसर मिलता, वह खोद-खोद कर मेरे बारे में, मेरे अतीत के बारे में ढेरों सवाल करती। मैं भी यथासंभव उसकी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करता।
एक दिन यूँ ही उसने पूछ लिया, ‘आप शादी क्यों नहीं कर लेते?’
मैंने कहा, ‘सब कुछ तो तुम्हे बता दिया, फिर भी पूछती हो कि मैं शादी क्यों नहीं करता?’
इस पर वह बोली, ‘मगर इस तरह कब तक अकेले जीवन गुजारेंगे आप?’
मैंने हँसकर कहा, ‘जब तक तुम्हारे जैसी कोई लड़की मुझे मिल नहीं जाती।’
‘मेरे जैसी?’ मैं तय नहीं कर पाया कि उसके प्रश्न में उल्लास था या आश्चर्य।
‘हाँ तुम्हारे जैसी’, मैंने कहा, ‘क्योंकि तुम तो मिलोगी नहीं।’
उसके चेहरे पर अचानक शर्म और खुशी के ढेरों कँवल एक साथ खिल उठे। फिर शरारत से मुस्कराती हुई वह बोली, ‘मेरे जैसी लड़की मिलेगी तो बरबाद हो जाएँगे आप।’
खिलखिलाते हुए मैंने कहा, ‘तुम्हारे जैसी लड़की मिले तो मैं बरबाद होने के लिए भी तैयार हूँ।’
उसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो उठा। निगाहें वह उठा नहीं सकी, काँपते अधरों से उसने कुछ कहना चाहा, मगर वह भी नहीं कह सकी। मैं कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर हौले से मैंने उसके गालों को थपथपाकर कहा, ‘तुम बहुत भोली हो मनीषा, शायद इसीलिए मुझे अच्छी लगती हो।’
उसने कुछ कहा नहीं। दोनों हथेलियों से अपना चेहरा छुपाया और घर में भाग गई।
उस दिन पहली बार मैं दफ्तर नहीं जा पाया। दरवाजा बंद करके चुपचाप बिस्तर पर पड़ा रहा। प्रश्नों का एक पूरा सागर मेरे सामने पसरा हुआ था। एक-एक प्रश्न की लहरों में डूबता-उतराता मैं न जाने कब तक सोचता रहा और फिर थककर नींद के आगोश में चला गया। सपने में बार-बार घूम-फिर कर घबरायी-सी चंचल हिरनी की-सी सहम-सहमी दो बड़ी-बड़ी आँखें मेरे जेहन में दस्तक देती रहीं और बार-बार पूछती रहीं, ‘मेरे जैसी?’
उसके बाद कुछ दिनों तक मैं मनीषा का सामना करने से बचता रहा। इसका कारण बहुत सीधा था। मैं भीतर ही भीतर यह स्पष्ट रूप से महसूस कर रहा था कि मैं तेजी से उसके मोहपाश में फँसता चला जा रहा हूँ। मैं यह भी महसूस कर रहा था कि मनीषा भी मेरी ओर आकर्षित है। मैं इस स्थिति से बचना चाहता था। मैं इस बात को भली-भाँति जानता था कि अपने पहले प्यार के झटके से मैं अभी तक ठीक तरह से उबर नहीं पाया हूँ। ऐसे में दूसरा कोई भी झटका मेर सारे जीवन को तहस-नहस कर सकता था। इसके अलावा मनीषा के साथ अपने रिश्ते की कोई मंजिल मुझे दूर-दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। अभी तो वह पूरे अठारह साल की भी नहीं हुई थी। फिर वह शादीशुदा थी और कुल छह-सात माह पहले ही उसका गौना हुआ था। उसके और मेरे बीच बहुत तरह का और बहुत लंबा फासला था। इस रिश्ते को किसी तरह की वैधता देने की कोई सूरत या संभावना मुझे दूर-दूर तक नजर नहीं आ रही थी। और किसी को दिल की गहराइयों से बेइंतिहा चाहने के बाद मैं किसी अनैतिक रिश्ते का हिस्सेदार कतई बनना नहीं चाहता था।
मैं दुविधा में डूबा हुआ था। क्योंकि इन तमाम बातों को जानने-समझने और मानने के बावजूद दो आँखों का जादू मेरे दिलो-दिमाग पर छाया हुआ था। किसी ऊँचे पर्वत की चोटी पर उगे किसी पौधे पर अपनी पूर्णता में खिले फूल की तरह था उसका सौंदर्य। ऐसा फूल जिसका नाम भी हमें नहीं पता, जो हमारे जाने-पहचाने गुलाब, कमल, चमेली, मोगरा, चंपा, जुही, रजनीगंधा से बहुत अलग है, मगर फिर भी अपनी संपूर्ण सादगी के साथ उसमें असीम आकर्षण है, विलक्षणता है। जो हमें बाँध लेता है। एकटक देखने के लिए हमें मजबूर कर देता है। सौंदर्य मैंने बहुत देखा था। मनीषा बहुत सुंदर नहीं थी। गोरा रंग था, मगर नाक-नक्श सामान्य ही थे। लेकिन उसकी आँखें। मानो कोई चंचल हिरनी अपने झुंड से बिछुड़कर अनायास वन की सीमा से बाहर निकलकर गाँव की सरहद में आ गई हो और घबराई हुई विस्मय से चारों ओर देख रही हो। उसकी आँखों में क्या नहीं था? चंचलता, विस्मय, संदेह, घबराहट, प्यास और न जाने किस चीज की तलाश। मैं लाख चाहने पर भी उन आँखों से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था। और भीतर ही कहीं मैं यह भी महसूस करता था कि शायद मैं उन आँखों से पीछा छुड़ाना चाहता भी नहीं था।
‘क्या करूँ, क्या ना करूँ’ की उलझन में कुछ दिन निकल गए। इस बीच सप्रयास मैं मनीषा के सामने आने से कतराता रहा। एक-दो बार मनीषा सामने आई तो भी मैंने निगाहें नहीं मिलाईं। हालाँकि उसकी ओर देखे बिना ही मैं जानता था कि मनीषा के चेहरे पर बेचैनी और उदासी के मिले-जुले भाव हैं। वैसे दुखी मैं भी कम नहीं था। जब मैं मनीषा की बेचैनी और उदासी के बारे में सोचता तो मेरा दुख और गहरा जाता था। वास्तव में मैं उसे इस तरह की परिस्थिति में नहीं डालना चाहता था। मगर यहाँ मैं खुद ही तय नहीं कर पा रहा था कि मेरे लिए क्या करना उचित है और क्या नहीं।
ऐसे ही एक दिन जब मनीषा से मेरा सामना हुआ तो मेरे पास निगाहें चुराकर निकल जाने की कोई राह नहीं थी। समय सुबह का ही था। रात को मैं देर से दफ्तर से आया था और हमेशा की तरह देर सुबह तक सोया हुआ था। दोपहर अभी हुई नहीं थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक की आवाज से मेरी नींद खुल गई। मेरे दरवाजे पर दस्तक! ऐसा अपवादस्वरूप ही हुआ करता था। मैंने कुछ आश्चर्य के साथ दरवाजा खोला। असली आश्चर्य मेरे सामने था। खुद मनीषा। मैं अचकचा गया। एक ही झलक में मैं अपने सामने के दोनों दरवाजे देख गया। पड़ोसी के दरवाजे पर ताला था और मनीषा के दरवाजे पर कुंडी। मैं अवाक्-सा खड़ा हुआ था। मनीषा ने धीरे से पूछा, ‘क्या मैं भीतर आ जाऊँ?’
हड़बड़ाकर मैं दरवाजे से परे सरक गया। मनीषा ने हल्के-से दरवाजा भेड़ दिया। फर्नीचर के नाम पर मेरे पास केवल एक कुर्सी थी। जमीन पर गद्दा बिछाकर मैं सोता था। मनीषा कुर्सी के पास ही जमीन पर सँभलकर बैठ गई और बोली, ‘आप भी बैठिए ना।’
मैं कुछ इस तरह सकुचाकर उस कुर्सी पर बैठा जैसे कि वह कमरा मेरा न होकर किसी अपरिचित का हो।
मनीषा कुछ देर तक मुझे गौर से देखती रही। फिर मुस्कराकर बोली, ‘कैसी अजीब बात है न, घबराना मुझे चाहिए और घबरा रहे हैं आप।’
मैंने अचकचाकर कहा, ‘नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है।’
वह हौले-से मुस्कराई और बोली, ‘आपका चेहरा तो कुछ और बता रहा है, मगर चलिए, आप कहते हैं तो मैं मान लेती हूँ।’ कुछ पलों तक वह खामोश रही मानो जो कुछ बोलना चाहती थी, उसे बोलने की हिम्मत जुटा रही हो। फिर बोली, ‘आप सोच रहे होंगे, कैसी बेशर्म लड़की है यह, और बेहया भी। इस तरह चोरी-छुपे एक पराए मर्द के कमरे में चली आई। मगर मैं क्या करूँ, जीवन में न चाहते हुए भी बहुत कुछ हो जाता है और न चाहते हुए भी बहुत कुछ करना पड़ता है।’
मैं उस पल को जैसे कान और आँखों के बीच बँट गया था। कान उसकी बातें सुन रहे थे और आँखें कुछ विस्मय के साथ उसे देख रही थीं। एक पल ठहरकर वह बोली तो इस बार संबोधन आप की जगह तुम हो गया था। उसने कहा, ‘दरअसल आज की तिथि में मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है, जिसकी मैंने चाह की हो। न मैंने कभी ऐसा पति चाहा था, जो अपनी माँ से इतना घबराता हो कि अपनी पत्नी से कभी यह पूछने की हिम्मत भी न कर पाए कि वह कैसी है या उसकी क्या इच्छा है या उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। ऐसा पति, जिसके होने का एहसास अधिकतर सिर्फ रात को बिस्तर पर ही होता है। मैंने ऐसी सास भी न चाही थी जिसके लिए अपनी बहू किसी जेल में बंद कैदी से ज्यादा कोई हैसियत न रखती हो। ऐसा घर, ऐसा माहौल भी मैंने कभी नहीं चाहा था जहाँ अपना सुख-दुख बाँटने के लिए दीवारों के अलावा कोई और न हो। यहाँ तक कि मैंने तो कभी यह भी नहीं चाहा था कि ऐसी परिस्थितियों में कोई तुम्हारी तरह इस तरह से अचानक मेरे जीवन में आ जाए कि मेरे सारे अस्तित्व को ही झकझोरकर रख दे। मगर न चाहते हुए भी ऐसा हुआ। न चाहते हुए भी तुम आज मेरे जीवन की एक हकीकत हो।’
इतना कहकर खामोश हो गई थी मनीषा। पता नहीं, बोलते हुए थक गई थी या अपने कहे हुए की मेरे ऊपर होने वाली प्रतिक्रिया देखना चाहती थी। मैं गहरी सोच में डूब गया। दरअसल जिस स्थिति से मैं इतने दिनों से बचने का प्रयास कर रहा था, वही मेरे सामने अपने विकराल रूप में आ खड़ी हुई थी। मनीषा जो कह रही थी, उसका मुझे बहुत हद तक अनुमान था। टुकड़ों-टुकड़ों में हुई बातों में वह इसमें से बहुत कुछ बता चुकी थी। मैं यह भी जानता था कि ऐसी परिस्थितियों में उसका मेरी ओर आकर्षित होना कोई अजूबा नहीं था। मगर मेरी चिंता दूसरी थी। इस बारे में मेरे भीतर कोई किंतु-परंतु नहीं था कि मैं किसी अनैतिक संबंध का इच्छुक नहीं था। सामाजिक दायरे में इस रिश्ते का कोई भविष्य मेरी सोच के दायरे में नहीं आ पा रहा था। मैं जानता था कि जाने-अनजाने मनीषा ने कुछ उम्मीदें मुझसे जोड़ ली होंगी और सच यह था कि मैं उसे निराश भी नहीं करना चाहता था। मगर अपने सिद्धांतों पर कायम रहते हुए उसकी उम्मीदों को पूरा कर पाने की कोई राह मुझे दिखाई नहीं दे रही थी।
कुछ पल ठहरकर मनीषा बोली, ‘हाँ, यदि अनुमति दो तो एक विनती जरूर है मेरी। दो बोल ना सही, मगर एक निश्छल मुस्कान मेरे लिए बचाए रखो। बहुत कुछ सहा है मैंने, मगर नजरें चुराती तुम्हारी आँखों की मार सहने की हिम्मत नहीं है मुझमें।’
मैं फिर सोच में डूब गया। उस समय कुर्सी के हत्थे पर अपना चेहरा टिकाए बैठी थी मनीषा। अपने दिल की बात कह लेने के बाद एक संतोष का भाव था उसके चेहरे पर, और फैली हुई थी मासूमियत। निश्छलता, बच्चों जैसी। जिस तरह बिना किसी लाग-लपेट के उसने अपने दिल की बात कह दी थी, उससे मैं स्वयं आश्चर्यचकित था।
मनीषा की जगह शहर की कोई पढ़ी-लिखी आधुनिक लड़की होती तो उसके साथ सहज मित्रता के संबंध की मैं कल्पना कर सकता था, मगर जिस माहौल से निकलकर मनीषा आई थी और जिस माहौल में वह रह रही थी, उसमें इस तरह की बात पूरी तरह से असंभव ही नहीं अकल्पनीय भी थी।
मेरे भीतर संकोच इस बात को लेकर भी था कि मनीषा की उम्र बहुत कम थी। भावों और विचारों की अपरिपक्वता उसमें संभव थी। मैं यह तय नहीं कर पा रहा था कि कुछ समय बाद जब समय, उम्र और परिस्थितियाँ उसे परिपक्व बना देंगी तो क्या यही बात वह तब भी कह सकेगी? कहीं ऐसा न हो कि कल अपनी नादानी पर उसे पछतावा हो। वह किसी अपराध-बोध से ग्रसित हो जाए। ऐसे में इस अबोध शिशु-सी निश्छल लड़की के लिए जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा।
लेकिन बहुत सोचने के बाद भी मैं कुछ तय नहीं कर पाया। जब अपनी सोच का बोझ उठाना मेरे लिए मुश्किल हो गया तो किसी तरह मैंने उसे पुकारा, ‘मनीषा!’ उसने चौंककर मेरी ओर देखा। उसके विशाल नयनों में उस पल अनगिनत प्रश्न सिमट आए थे। मेरा गला अचानक सूख गया। थूक निगलकर अपने स्वर को भरसक कोमल बनाने का प्रयास करते हुए मैंने पूछा, ‘मुझसे क्या अपेक्षा है तुम्हारी?’
कुछ व्यंग्य से मुस्करा दी मनीषा मेरे प्रश्न पर। मैं उस समय आश्चर्य और संकोच से भरा हुआ था। वह बोली, ‘तुमसे क्या अपेक्षा रखूँगी मैं? सच तो यह है कि अब मेरी परमेश्वर से भी कोई अपेक्षा नहीं है। पिता ने जितना कर्तव्य निभाया, उससे अधिक मैंने कभी नहीं चाहा। गौने के बाद पति से जरूर कुछ दिन यह अपेक्षा रही कि उनसे मुझे प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सहानुभूति और संवेदना मिलेगी। मगर धीरे-धीरे यह अपेक्षा भी नहीं रही। इसके बाद मैंने किसी से कोई अपेक्षा नहीं की। तुम्हें देखा, न चाहते हुए भी तुम्हें चाहा, मगर तुमसे कोई अपेक्षा नहीं की मैंने। तुमने उस दिन कहा, ‘तुम बहुत भोली हो मनीषा, शायद इसीलिए मुझे अच्छी लगती हो’, तो मुझे सब कुछ मिल गया। बिना अपेक्षा के ही तुमने इतना क्या कहा, सारे जीवन का सुख और आनंद सिमटकर तुम्हारे इस वाक्य में आ गया और मैं तृप्त हो गई। अब इस तृप्ति से बढ़कर कोई मुझे क्या देगा? फिर मैं क्यों तुमसे भी कोई अपेक्षा रखूँ?
मैं भौचक्का उसे देखता रह गया। गाँव की एक साधारण-सी सीधी-सादी और कमउम्र लड़की इस तरह से सोच और कह सकती है, यह मेरी कल्पना से भी परे था। मैं तो स्वप्न में भी कभी इस बात की कल्पना नहीं कर सकता था। मैंने तो उसे हमेशा ही बहुत भोली, मासूम और नादान समझा था। मैंने एक बार फिर ध्यान से उसकी ओर देखा। मगर कहाँ कोई परिवर्तन था? अब भी वह उतनी ही भोली, उतनी ही मासूम और उतनी ही पवित्र लग रही थी, जैसी हमेशा लगा करती थी।
अब सोचने में मुझे बहुत समय नहीं लगा। मुझे लगा, अब सिर्फ एक ही बात है जो मुझे मनीषा से कहनी चाहिए। उसे लेकर मेरे भीतर किसी तरह का किंतु-परंतु नहीं था। मैंने सोचा, आज यदि मैं यह नहीं कहूँगा तो बहुत बड़ा अपराध करूँगा, जिसकी भरपाई फिर ताउम्र नहीं हो पाएगी। मैंने हौले से उसका चेहरा अपनी हथेलियों में थामा और पूछा, ‘जीवन-पथ पर मेरा साथ दोगी मनीषा?’
इस बार चौंकने की बारी मनीषा की थी। उसने आश्चर्य से भरकर मेरी ओर देखा। उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वह यह तय नहीं कर पा रही थी कि उसने जो सुना था, वह सच था या नहीं। मैंने फिर पूछा, ‘जीवन-पथ पर मेरे संग चलोगी मनीषा?’ अब संदेह की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। आश्चर्य के भाव अब भी उसके चेहरे पर थे मगर उसकी आँखों से अविरल अश्रुधारा बह चली थी। वह कुछ कहना चाहती थी मगर शब्द थे कि उसके गले से बाहर नहीं आ पा रहे थे।
मैंने कहा, ‘तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है मनीषा। तुम्हारी भावनाओं को मैं समझता हूँ और तुम्हारे इन आँसुओं से छनकर आ रही स्वीकृति को भी मैं समझ रहा हूँ। अब कुछ मत कहो। कुछ कहने-सुनने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। संसार जो कहे और समाज जो समझे मगर हमारा हृदय और ऊपर बैठा वह परमेश्वर इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि आज से, अब से तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूँ।’
मनीषा मेरे पाँवों से लिपटकर फूट-फूटकर रो पड़ी। मैं जानता था, उसकी आँखों से आँसुओं के साथ बहुत सारी उपेक्षा, तिरस्कार और कुचले हुए अरमान निकल रहे थे। एक नए जीवन की शुरुआत के लिए इनका निकल जाना ही बेहतर था। एक लंबे समय बाद उसके हृदय को प्यार का सहारा मिला था। मनीषा ने जो पाया था, वह उसका अधिकार था। मेरा हृदय जानता था, मैंने उसे कुछ नहीं दिया था। जिसे किसी बात की कोई अपेक्षा न हो, उसे कोई भला क्या दे सकता है?
Download PDF (अपेक्षा )
अपेक्षा – Apeksha