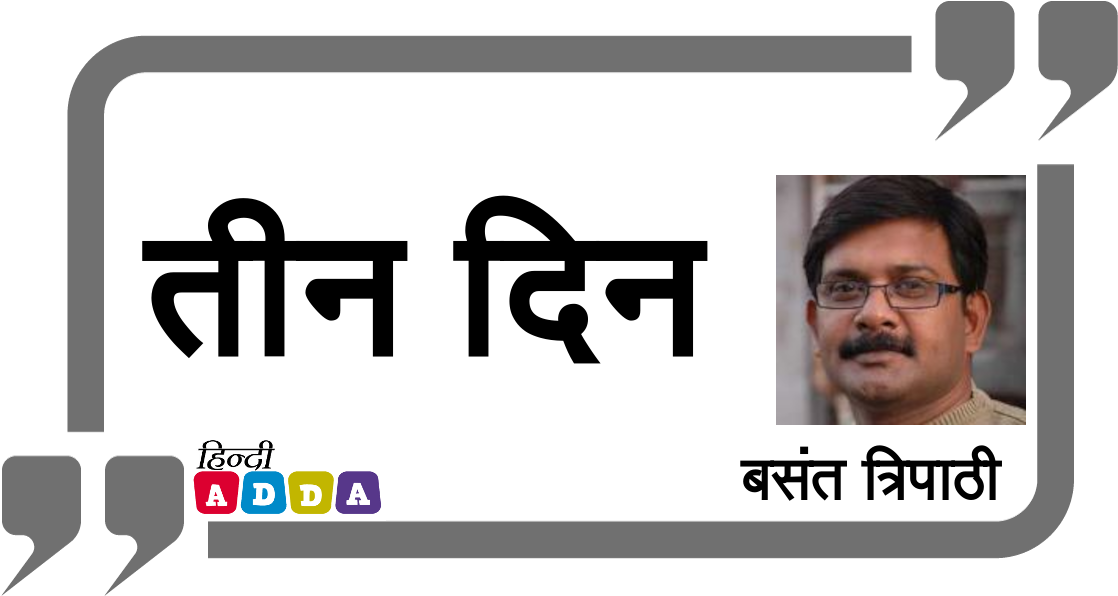तीन दिन | बसंत त्रिपाठी – Teen Din
तीन दिन | बसंत त्रिपाठी
‘उच्च श्रेणी के पौधों और जंतुओं में भिन्नता की पहचान आसान है लेकिन निम्न श्रेणी के पौधों और जंतुओं में नहीं, क्योंकि उनकी जैविक प्रविधि में दोनों ही वर्गों की विशिष्टताएँ होती हैं। युग्लीना और वोल्वोक्स ऐसे ही निम्न श्रेणी के जीव हैं। उन्हें जंतु-विज्ञान और वनस्पति-विज्ञान दोनों में ही रखा जा सकता है।’
प्रो. सिन्हा पिछले बत्तीस वर्षों से पौधों और जंतुओं के मूलभूत अंतर और उनकी जैविक जटिलताओं को अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को समझाते रहे हैं और आज भी, कल के अपने लेक्चर की तैयारी की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आज… वोल्वोक्स… युग्लीना… फाँस की तरह उनके जेहन में कोई बात चुभ गई। उन्होंने कुर्सी की पीठ से अपनी पीठ टिका दी और किसी गहरी चिंता में डूब गए।
थोड़ी देर तक इसी तरह बैठे रहने के बाद प्रो. सिन्हा अपनी तैयारी को अधूरा छोड़ फिर बालकनी में आ गए। भिखारी अब भी वैसे ही बैठा था… उकडूँ… उसकी नंगी पीठ को दिसंबर का युवा सूरज चमका रहा था। प्रोफेसर की आँखें भिखारी पर टिकी थीं और वे मंत्र की तरह बुदबुदा रहे थे… निम्न श्रेणी के जीव… वोल्वोक्स और युग्लीना… निम्न श्रेणी के जीव… वोल्वोक्स और युग्लीना…
अभी दो घंटे पहले से लेकर गुजरे तीस वर्षों के लंबे अंतराल में प्रो. सिन्हा ने कभी इतनी बेचैनी महसूस नहीं की जितना कि वे अब कर रहे थे।
(इससे पहले कि मैं आगे का हाल बयान करूँ, जरूरी है, आप प्रो. सिन्हा से परिचित हो जाएँ।)
प्रो. सिन्हा दुनियावी भाषा में बेहद नीरस, एकाकी और पागलपन की दुनिया का दरवाजा खटखटाते एक अधेड़ व्यक्ति हैं। दुनिया उनके लिए अनुपस्थित है और वे दुनिया के लिए। उनके और दुनिया के बीच केवल उनका पेशा और जरूरत भर की चीजों का रिश्ता है, जिन्हें कॉलेज से लौटते हुए वे किसी भी दुकान से खरीद लिया करते हैं।
तेजी से दौड़ रहे महानगर के उस अपार्टमेंट में रहने वालों के लिए प्रो. सिन्हा एक अजीब से व्यक्ति थे। उनके अलावा वहाँ रहने वाले सभी लोग सभ्य, शरीफ और दुनियादार थे। सीढ़ियाँ चढ़ते-उतरते जब उनकी नजरें मिलतीं तो औपचारिक मुस्कुराहट से एक-दूसरे का अभिवादन करते, शब्द लेकिन तब भी खामोश ही रहते थे। खामोशी उनका धर्म था, हालाँकि सभी अपने-अपने कामों में कोलाहल के आदी थे। फिर भी प्रो. सिन्हा की चुप्पी उन्हें खलती थी।
चुप्पी में भी कुछ अनकहे से शब्द होते हैं। सभी उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। प्रो. सिन्हा की चुप्पी लेकिन खालिस थी। बिना किसी मिलावट के शुद्ध और बुझी हुई चुप्पी!
प्रो. सिन्हा का पूरा नाम दामोदर शक्तिपद सिन्हा है। औसत कद के दुबले-पतले अधेड़ व्यक्ति, उम्र छप्पन साल, माथे पर घाव का गहरा निशान, नाक थोड़ी लंबी और नुकीली, लेकिन आँखें… बुझ रही सिगड़ी के अधजले कोयले-सी। वे इस अपार्टमेंट के सबसे ऊपरी माले में पिछले सत्रह वर्षों से रह रहे हैं। उन्हें जानने वाले उनके बारे में कुल इतनी ही बातें जानते हैं। इसके अलावा एक और बात, कि वे एक निजी कॉलेज में वनस्पति-विज्ञान के रीडर और विभागाध्यक्ष हैं और कॉलेज से घर की कुल तीन किलोमीटर की दूरी पैदल ही तय करते हैं।
बीसवीं शताब्दी के समाप्त होने में अभी तीन साल बाकी थे। बाजार को इक्कीसवीं सदी के नाम का एक नया, चमचमाता मोहरा मिल गया था लेकिन यह मोहरा प्रो. सिन्हा के आगे नाक रगड़ता था। उनके पिता शक्तिपद सिन्हा सेना में हवलदार थे और द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान, 1940 में, मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ते हुए लापता हो गए थे। प्रो. सिन्हा को तब माँ की गर्भ में आए कुल तीन महीने ही हुए थे। युद्ध में लापता होने के कारण हवलदार शक्तिपद सिन्हा मरे हुए मान लिए गए थे लेकिन उनकी पत्नी ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया।
द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बरसों बाद तक माँ या तो बालक दामोदर को पाल-पोस कर बड़ा करने के लिए रात-रातभर जागकर कपड़े सिलती रही या अपने पति का इंतजार करती रही। उसने अपने दूर-पास के सभी रिश्तेदारों से बड़े क्रूर तरीके से रिश्ता तोड़ लिया था।
माँ अपने बच्चे दामोदर को प्यार नहीं करती, ऐसा नहीं था, लेकिन उनका दिमाग अपनी जगह से हिल गया था। वह उपस्थित दुनिया से लगातार अनुपस्थित होती जा रही थी। दामोदर ने अपने किशोर वय में ही देखा कि माँ को हिस्टीरिया का दौरा पड़ने लगा था। दौरे के क्षणों में माँ बहुत हिंसक हो जाती थी और हिटलर को चुन-चुनकर मर्दाना गालियाँ बकती थीं। उस समय दामोदर कोने में सहमा खड़ा माँ को एकटक देखता रहता। ऐसे ही दौरे के दौरान माँ ने एक बार पीतल का भारी लोटा उसके सिर पर दे मारा था जो उनकी निशानी के रूप में प्रो. सिन्हा के माथे पर आज तक है।
दौरे के बाद माँ अक्सर बेहोश हो जाती थी। माँ के शांत हो जाने के बाद दामोदर धीरे-धीरे उनके पास जाता और मुँह पर पानी के छींटे मारता। थोड़ी देर बाद माँ को होश आ जाता और वो कपड़े सिलने लगती। प्रो. सिन्हा ये कभी नहीं जान पाए कि होश में आने बाद माँ को अपने पिछले कृत्य याद रहते थे या नहीं। लेकिन उनके जेहन में आज तक घृणा और हिंसा से सनी वे आँखें और शांत होते समय उनमें उतरता शून्य खुदा हुआ है।
किशोरावस्था तक आते-आते दामोदर भी एक चुप्पे आदमी में बदलता चला गया। कक्षा में वह एक चुप छात्र था और इतना चुप कि मास्टर की छड़ी खाकर भी सी-सी की आवाज नहीं करता था। दोस्त तो, खैर, उसका कोई था ही नहीं, सहपाठी अक्सर तंग किया करते थे, जिनका उस पर कोई असर नहीं होता था। वह जितना बाहर से कटता गया, उतना ही भीतर का संसार खुलता गया।
दामोदर अपनी मेहनत से प्रो. सिन्हा में बदल गया, लेकिन माँ की बीमारी ठीक न हुई। कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी पा जाने के बाद प्रो. सिन्हा ने बहुत कोशिश की कि माँ को अपने साथ शहर ले आए लेकिन माँ तैयार नहीं हुई। उसे अब तक अपने पति का इंतजार था। अंततः हारकर प्रो. सिन्हा रोज पैंतीस किलोमीटर अप-डाउन करने लगे।
प्रो. सिन्हा महसूस कर रहे थे कि माँ धीरे-धीरे मौत की ओर बढ़ रही है, लेकिन वे कुछ कर नहीं सकते थे… और सच पूछो तो कुछ करना भी नहीं चाहते थे। पच्चीस साल से उन्होंने माँ को एक रहस्यमय दुख में तड़पते देखा था। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक होने के बाद भी माँ की तड़प कम नहीं हुई। इसलिए प्रो. सिन्हा की आंतरिक अदालत ने मौत को, तड़प से मुक्ति के एकमात्र उपाय के रूप में स्वीकार कर लिया था।
लेकिन मुक्ति… मौत… इतनी आसान नहीं होती।
अंतिम समय में प्रो. सिन्हा जब भी कॉलेज से लौटते, माँ उन्हें अपने सीने से चिपटा लेती और माफी माँगने लगती और बार-बार अपने पति की शिकायत करती। उन्हें शायद लगता था कि उनके पति उसी कमरे में ही है। कई बार वह अपने पति से शिकायती लहजे में बात भी करती थी। वह बातचीत इतनी त्रासद और कातर होती थी कि प्रो. सिन्हा आज भी उसे याद करते हुए सहम जाते हैं। माँ कहती थी –
‘इतने बरसों बाद लौटे हो… न मेरी फिक्र न दामोदर की… हाँ, तुम्हें तो वीर कहलवाने का शौक था न… शहादत की जल्दी मची थी न… लेकिन देखो, तुम्हारी शहादत बेकार गई… मैंने तुम्हें कभी शहीद नहीं कहा और न ही अपने सामने किसी को कहने दिया… मैंने पेंशन तक नहीं ली… तुम्हारी मौत कभी मुझसे जीत नहीं पाई… तुम्हारी मौत बेकार गई…।’
फिर सहसा अपने जवान बेटे से माफी माँगने लगती।
प्रो. सिन्हा आज तक समझ नहीं पाये कि माँ उनसे माफी क्यों माँगती थी? जब माँ मरी तब भी उनकी हथेलियाँ माफी माँगने की मुद्रा में ही आपस में जुड़ी हुई थीं।
माँ की मौत के बाद प्रो. सिन्हा ने अपने आपको सार्वजनिक जीवन से पूरी तरह काट लिया। उन्होंने घर में ताला लगाया और उसे चुपचाप ढह जाने की खुली छूट देकर इस शहर में बस गए। वे सामान के नाम पर माँ का पुराना ट्रंक, अपनी किताबें और कुछ कपड़े ही साथ लाए थे। शुरुआती तेरह साल तक वे एक किराये के मकान में रहे और फिर शहर के इस सभ्य और शांत इलाके में फ्लैट खरीद लिया, जिसमें कि अभी वे रह रहे हैं।
आज रविवार का दिन था। प्रो. सिन्हा हर रविवार को किसी जरूरी काम की तरह सुबह-सुबह निकल जाते और बेवजह सड़क पर घूमते रहते थे। घूमने के दौरान शहर का कोई भी चेहरा या दृश्य उनके भीतर आकार नहीं लेता था। दो-तीन घंटे अपने आप में डूबे हुए घूमते रहने के बाद वे अखबार, दूध का पैकेट, सब्जियाँ और अंडे लेकर लौट आते।
आज जब वे लौट रहे थे एक भिखारी को अपार्टमेंट के गेट के बाहर उकड़ूँ बैठे हुए देखा। भिखारी शौच की मुद्रा में जमीन पर बैठा था, अपने दोनों हाथों की उँगलियों को गालों पर रखे हुए। उसकी हथेली के निचले हिस्से ठुड्डी के पास एक-दूसरे को स्पर्श कर रहे थे। भिखारी की आँखें बिल्कुल स्थिर थीं। उसका चेहरा चमक से मुक्त था। बाल अपना रंग खोकर भूरे हो चुके थे और आपस में उलझने लगे थे। हाथों और पैरों में जान बाकी है या नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। पैरों को तो जमीन ने जैसे जकड़ रखा था!
प्रो. सिन्हा भिखारी को घूरते हुए उसके पास से निकले। भिखारी उन्हें थोड़ा अजीब-सा लगा, विशेषकर उसकी बैठने की मुद्रा।
अपने फ्लैट के भीतर आकर प्रो. सिन्हा ने सारा सामान मेज पर रखा और बालकनी में आ गए। भिखारी वैसे ही बैठा था। वे उसे गौर से देखने लगे।
भिखारी को देखते हुए प्रो. सिन्हा के आंतरिक संसार में कौन-से परिवर्तन हो रहे थे, ये वो खुद नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके भीतर का उदास रंग तेजी से बदल रहा है। वह इतनी तेजी से बदल रहा था कि उसे बर्दाश्त करना उनके बूते के बाहर की बात थी।
हालाँकि भागने का उन्हें अभ्यास था। पिछले तीस वर्षों से भागते-भागते वे भागने के इतने अभ्यस्त हो चुके थे कि उन्हें अब प्रयास भी नहीं करना पड़ता था। भागना उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था।
प्रो. सिन्हा ने इस बार भी अपने अभ्यास पर भरोसा किया और भीतर आकर कल के अपने लेक्चर की तैयारी करने लगे। लेकिन इस तैयारी ने प्रो. सिन्हा को फिर उसी दुनिया में ला पटका, जिससे वे भाग जाना चाहते थे! निम्नश्रेणी के जीव… वोल्वोक्स और युग्लीना…।
वे बाल्कनी में आ गए और अपनी आँखें भिखारी की पीठ पर गड़ा दी। दो घंटे तक बिना हिले-डुले एक ही मुद्रा में कोई कैसे बैठा रह सकता है !
सूरज आसमान का छोर पकड़कर चढ़ते-चढ़ते ठीक आसमान के बीचोंबीच धमक चुका था। उसकी चमक भिखारी की नंगी, खुरदुरी और मटमैली पीठ को सहला रही थी। प्रो. सिन्हा उस नामुराद जिस्म में किसी हरकत का मंसूबा पाले बालकनी में तैनात थे। बरसों बाद उनकी आँखें किसी मनुष्य पर थिर हुई थीं। लेकिन यह मनुष्य अपने मनुष्य होने का कोई संकेत नहीं दे रहा था। प्रो. सिन्हा परेशान हो गए और चिढ़कर फिर भीतर आ गए। उन्होंने अपना डिसेक्शन बॉक्स खोला और एक गुड़हल के फूल की चीर-फाड़ करने लगे, जिसे वे रास्ते से उठा लाए थे।
गुड़हल की सारी पंखुड़ियाँ नोचने के बाद प्रो. सिन्हा ने हल्का-सा चीरा लगाया और उसके तन को फैलाकर भीतर के सफेद कणों का मुआयना करने लगे। वे आवर्धक लैंस द्वारा इतने गौर से फूल को देख रहे थे मानो उसके भीतर किसी जरूरी चीज को तलाश रहे हों। फिर अधूरी तलाश की बेचारगी के भाव से भरकर उस चिथड़े-चिथड़े फूल को डस्टबीन में डाल दिया और बिस्तर पर लेट गए। उनकी आँखें घूमते पंखे पर टिकी थीं और दिमाग गहरे पानी में निर्मित भँवर की तरह शांत, लेकिन चुंबकीय आकर्षण से भरा था। आँखों के भीतर धीरे-धीरे वर्तमान का अँधेरा पसरने लगा, जिसे गुजरे जमाने की धूल ने लपेट रखा था। वे अपनी आँखें, चेहरे और दिमाग में जलन महसूस करने लगे।
प्रो. सिन्हा बोझिल कदमों से उठे। अपनी आँखों और चेहरे को अच्छे से धोया और बालकनी का दरवाजा बंद कर दिया। वे उस वर्तमान में नहीं आना चाहते थे जहाँ से बेलौस अतीत का नंगापन दिखाई पड़े। उनके भीतर, उनकी ही इच्छा के विरुद्ध एक ऐसा युद्ध शुरू हो गया जिसके उद्देश्य तक से वे वाकिफ न थे। वे जितना उसे टालते जाते, उतना ही वह बढ़ता हुआ विकराल रूप लेता जाता।
प्रो. सिन्हा ने कई तरह से अपने आपको बचाने की कोशिश की – अपनी प्लास्टिक की पुरानी चप्पल निकालकर उसे रगड़कर धोया, रात के जूठे बर्तनों को मल-मलकर साफ किया, कुछ नई प्रजाति के पौधों के नाम याद किए, मैले कपड़े धोने के लिए उन्हें बाल्टी में भिगो दिया, शक्कर के डिब्बे के भीतर जो चींटे चल रहे थे उन्हें चम्मच से निकाल-निकालकर आजाद कर दिया, गैस के बर्नर को सुई से साफ किया, और ऐसे ही कई काम; जिनकी कोई परिभाषा या औचित्य उनकी शब्दावली में नहीं था, लेकिन नहीं, बाहर जो दृश्य उन्हें चुनौती दे रहा था, उससे बचने का कोई सीधा रास्ता उनके पास नहीं था। दो-तीन घंटे तक अपने आपको बचाने की असफल कोशिश करने के बाद वे अपनी ही इच्छा के विरुद्ध, मानो मंत्र-बिद्ध हो, खुद को बालकनी में खड़ा पाया। यह ठीक-ठीक कब हुआ, उन्हें खुद नहीं मालूम।
सूरज को पृथ्वी को अभी अलविदा कहने में देर थी और भिखारी अब भी वैसे ही बैठा था… उकड़ूँ…।
प्रो. सिन्हा को महसूस हुआ कि जैसे हजारों लाल चींटियों ने उनके वजूद को घेर लिया है और अपने महीन अम्लीय डंकों से उनके जिस्म को छेद रही हैं। उनकी आत्मा, जिसे बरसों पहले ताबूत में बंद कर समुद्र में फेंक दिया गया था, अचानक उनके शरीर में प्रविष्ट हो गई थी। उसे राख और पत्थर के चूरे से रगड़ा जा रहा था… किर्र किच्… किर्र किच्… उनके दाँतों में दर्द की ठंडाई दौड़ गई। अब भागना बेकार था। किसी ने उनकी अपलक निस्तेज आँखों में नाखून चुभो दिया था।
प्रो. सिन्हा गौर से अपने सामने के चुनौतीपूर्ण दृश्य को देखे जा रहे थे। आज बरसों बाद माँ, उन्हें अपनी आँखों के अलावा पूरे वजूद के साथ याद आई। वे मानसिक यातनाएँ याद आईं, जिनके दहशत भरे साए में उनका खामोश बचपन घिसट-घिसटकर बीता था और उनकी रंगहीन जवानी धूसर और बदरंग अधेड़ावस्था में बदल गई थी। भिखारी जमीन पर अचल था और वे अपार्टमेंट के तीसरे माले में। ट्यूशन से घर जाती लड़कियाँ हँसी-ठिठोली, धक्का-मुक्की करती और एक-दूसरे की चोटियाँ खींचती हुई लौट रही थीं। उन्होंने न तो भिखारी को देखा और न ही प्रो. सिन्हा को। प्रो. सिन्हा चाह रहे थे कि कोई एक पल के लिए ही, चाहे घृणा भरी दृष्टि से ही सही, उन्हें देखे। लेकिन दौड़ती अलमस्त दुनिया से वे अनुपस्थित हो चुके थे। और अब भिखारी अनुपस्थित हो रहा था।
अचानक प्रो. सिन्हा को न मालूम क्या सूझा, वे तेजी से अंदर आए और डिसेक्शन बॉक्स से ब्लेड निकालकर अपने बाएँ हाथ की तर्जनी को हल्के-से चीर दिया। खून की एक पतली धार फर्श की ओर दौड़ गई। प्रो. सिन्हा आश्चर्य से अपना खून देखते रहे। मालूम हो रहा था कि उनके खून का रंग लाल नहीं है, उनकी नसों में खून नहीं बल्कि प्रोटोप्लाज्म की ठंडी धार दौड़ रही है। वे आँखें फाड़े फर्श पर फैलते खून को देख रहे थे। उन्होंने अपनी नाड़ी दबाई, दिल पर हाथ रखकर देखा, लेकिन धड़कन का नामोनिशान नहीं था। प्रो. सिन्हा ने अपने आप से ही पूछा – ‘क्या, मैं इनसान हूँ?’ उन्हें अपने प्रश्न का कोई मुकम्मिल जवाब नहीं मिला। और हारकर वे पढ़ने की मेज के सामने की कुर्सी में धँस गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी डायरी खोली और तारीख डाला – ’17 दिसंबर 1997′ और लिखने लगे –
‘मेरी तीस बरस की अघोषित और निरुद्देश्य चुप्पी आज धराशायी हो रही है, बल्कि हो चुकी है। आज ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा पूरा जीवन साइकस के छितरे पत्तों की तरह का हो गया है, जिसमें कोमलता का नामो-निशान नहीं! और वह भी एक भिखारी के कारण…!
‘भिखारी मैंने देखे नहीं हैं, ये बात नहीं है। लेकिन इसमें कोई ऐसी बात है जिसने झील से मेरे शांत मन में, कंकड़ नहीं, एक बड़ा और भारी पत्थर पटक दिया है, और जिसकी ‘छपाक्’ ने मेरी छप्पन बरस की जिंदगी और पचास बरस के ठहराव को एक झटके से चकनाचूर कर दिया है। क्या मेरी असाध्य और बेगैरत चुप्पी इस तरह तार-तार हो जाएगी? इस भिखारी के चेहरे में आखिर ऐसा क्या है जिससे मैं उबर नहीं पा रहा हूँ, बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ…?
‘इसके चेहरे में वितृष्णा और विवशता का ऐसा ठहरा-सा भाव है, जो मुझे बोनसाई पेड़ों में दिखाई पड़ता है। बोनसाई पेड़ों को देखकर मेरे भीतर एक अव्यक्त क्रोध जागता रहा है। मुझे घृणा होती है उन्हें गमलों में सजाया हुआ देखकर। लगता है किसी वृद्धि चाहने वाले वृक्ष पर मुट्ठी भर धूप और कार्बन डाई ऑक्साईड फेंककर उसे जीवित रखा जा रहा है। उसे न तो मरने दिया जा रहा है और न ही जीने। केवल अपनी विकृत और कापालिक सौंदर्य-वृत्ति की तृप्ति के लिए एक मूक जीव के प्रति इतना बड़ा अनाचार… सचमुच वर्गों-उपवर्गों के खाँचे में विभाजित दुनिया में वे लोग आसानी से खप सकते हैं जो या तो समर्थ हैं या समर्थ होने की संभावना से भरे हैं, निम्नश्रेणी के जीव तो… यदि मेरे पिता नाजी सैनिकों द्वारा कैद कर लिए होंगे तो मृत्यु पर्यंत इसी तरह का जीवन जीत रहे होंगे…।’
‘पिता’ लिखने के बाद प्रो. सिन्हा बहुत देर तक उनका चेहरा याद करने की कोशिश करते रहे। पिता को उन्होंने बहुत बचपन में एक पुरानी तस्वीर में देखा था। माँ उस तस्वीर को थामे शून्य में निहारती रहती थी। भरसक कोशिश के बाद भी जब उन्हें पिता का चेहरा याद नहीं आया तो वे उठे। उन्होंने पलंग के नीचे से माँ के काले ट्रंक को खींचकर बाहर निकाला और उसे खोला।
माँ की मौत के तीस बरस बाद, आज पहली बार प्रो. सिन्हा उनका ट्रंक खोल रहे थे। ट्रंक के कब्जे कुछ ऐसे जम चुके थे कि जब उसे खोला गया तो उसमें से ‘चूँ-चूँ’ की आवाज आई। प्रो. सिन्हा को लगा कि यह माँ के रोने की आवाज है। वे कल्पना करने लगे कि रोते समय माँ का चेहरा कैसा दीखता? अपनी कल्पना में उन्हें अव्यक्त आनंद मिला। क्योंकि उनके भीतर माँ के दो ही चेहरे थे – शून्य को ताकता हुआ खामोश चेहरा या फिर घृणा और पागलपन से भरा हिंसक चेहरा; और आज उन्होंने माँ का तीसरा चेहरा तलाश लिया था – रोता, बिलखता, आँसू टपकाता चेहरा। प्रो. सिन्हा को अपनी यह उपलब्धि ‘फॉदर ऑफ बॉटनी’ थियोफ्रेटस से भी अधिक महत्वपूर्ण लगी, जिन्होंने पाँच सौ वनस्पतियों की सूची बनाकर वनस्पति-विज्ञान की नींव डाली थी।
ट्रंक के भीतर काँच की कुछ चूड़ियाँ थीं, एक बंद गले को कोट था, जिसकी सीवन कोहनी के पास उधड़ी हुई थी और ऐसी ही कई अपरिभाषित चीज़ें, जो अपनी वस्तुगत भौतिक सच्चाई से जुदा होकर ट्रंक में बंद थीं। उनकी परिभाषाएँ माँ की देह के साथ भस्म हो चुकी थीं। ट्रंक के ढक्कन में एक लोहे का पॉकेट था, जिसमें एक ब्लैक एंड ह्वाइट तस्वीर रखी थी। तस्वीर में कई जगह लोहे की कत्थई फैल चुकी थी, उसकी चमक धुँधली पड़ गई थी। मालूम पड़ता था कि उसे कई बार चूमा गया है और वह कई-कई बार आँसुओं से भीग चुकी है।
प्रो. सिन्हा तस्वीर को हाथों में लिए, उसे गौर से देखते रहे। तस्वीर से कोई मुकम्मिल चेहरा उभर नहीं रहा था, सो वे उपलब्ध अंगों के आधार पर अपनी कल्पना से एक चेहरा बनाने लगे। उन्होंने जो चेहरा बनाया था वह उनके अपने चेहरे से हू-ब-हू मिलता था। उन्होंने एक अलग चेहरे की कल्पना की कई कोशिशें की, लेकिन घूम-फिरकर वे अपने ही चेहरे पर पहुँच जाते। फिर ये दोनों ही चेहरे अपार्टमेंट के बाहर बैठे भिखारी से मिलने लगते और अचानक लगता कि दरअसल वे सभी बोनसाई हैं… जीवित, लेकिन जीवन से कोसों दूर… और माँ अपने दोनों हाथ जोड़े उनसे माफी माँग रही है और अपने गर्म आँसुओं से उन्हें सींच रही है। माँ कोशिश कर रही है कि वे बढ़ें लेकिन कोई अदृश्य हाथ उनकी जड़ें कतर जाता है… मुँह अँधेरे… चुपचाप… और यह क्या … माँ भी बोनसाई में बदल गई!
प्रो. सिन्हा मेज पर लौटे और अपनी डायरी में जो कुछ लिखा था उस पर एक खड़ी लकीर खींच दी।
माँ के मरने के बाद प्रो. सिन्हा पिछले तीस वर्षों से बिला नागा डायरी लिखते रहे हैं और लिखना भी कैसा? वे डायरी खेालते, उसमें तारीख डालते और एकाध घंटा चुपचाप निहारने के बाद पन्ने पर एक खड़ी लकीर खींच देते। बीच में चार-पाँच मौके ही ऐसे आए थे जब उन्होंने डायरी के पन्ने पर कुछ लिखा था। अंतिम बार लगभग तीन साल पहले उन्होंने पन्ने पर एक शब्द लिखा था – ‘मैं…’ और फिर उस पर कलम चला दी थी। यह प्रो. सिन्हा की शब्दों से एक खामोश बगावत थी। एक ऐसी बगावत, जो इतिहास, वर्तमान या भविष्य के पन्ने पर कभी दर्ज न हो सकेगी। डायरी के सफेद पन्ने पर कलम चलाते हुए प्रो. सिन्हा के चेहरे पर वही भाव रहता था जो किसी मुजरिम को सजा-ए-मौत का फैसला सुनाते वक्त जज के चेहरे पर रहता है। प्रो. सिन्हा अपने बीते दिन को रद्द करते हुए संतोष और दर्द के चक्रव्यूह में फँसे रह जाते थे।
तीस बरस बाद आज ऐसा पहली बार हुआ कि पन्ने पर खड़ी लकीर खींचने के बाद वे पलंग पर लेट नहीं गए बल्कि कुछ सोचकर नए पन्ने पर फिर आज की तारीख डाली और लिखने लगे –
‘आखिरकार मैं वनस्पति-विज्ञान की ओर क्यों चला आया? क्या मेरे भीतर इस ओर आने की कुछ खास विवशताएँ थीं? मैं वनस्पति-विज्ञान की दुनिया में शामिल चीन्ही-अचीन्ही वनस्पतियों में आखिर क्या तलाशता रहा हूँ? क्या मुझे कभी अपने आप से ही यह अपेक्षा रही है कि मैं किसी ऐसी नायाब वनस्पति या सिद्धांत की तलाश कर लूंगा कि दुनिया मुझे मेरी उपलब्धियों के कारण याद रखेगी? नहीं, यकीनन नहीं; महज उपलब्धियों के कारण मैं अपने निःशब्द अकेलेपन से सार्वजनिक जीवन की दहलीज पर खींच लाया जाऊँ, यह तो कल्पना में भी असंभव है। मैं अपने अकेलेपन को नोबेल पुरस्कार की शर्त पर भी खोना नहीं चाहता! फिर इस ओर आने की कौन-सी वजह थी?
‘पेड़-पौधे मेरे अकेलेपन के साथी रहे हैं, लेकिन मैंने उन्हें गमलों में कभी नहीं लगाया। मैं दूर खड़ा उन्हें निहारता रहा हूँ, बंद कमरे में बैठा उनके बारे में सोचता रहा हूँ। मुझे हमेशा लगता रहा है कि उनका जीवन इस दुनिया के समस्त जीवों से अधिक उपेक्षित और उन्मुक्त रहा है। किशोर वय से ही पेड़-पौधों और मेरे बीच एक ऐसा शब्दहीन संवाद बन गया कि मुझे शब्दों से नफरत हो गई।
‘शोर से घृणा लाजिमी है लेकिन ‘शब्द’ से घृणा! और यह भी कितनी विचित्र, कितनी विरोधाभासी मनःस्थितियों का जटिल घालमेल है कि ‘शब्दों’ के प्रति अपनी घृणा को मैं शब्दों में ही व्यक्त कर रहा हूँ! दरअसल ‘शब्द’ का तात्पर्य मेरे लिए उनकी उच्चारित ध्वनियों से है। मैंने अपनी जरूरत के मुताबिक ‘शब्द’ की परिभाषा गढ़ ली थी, निहायत निजी और व्यक्तिगत! ‘शब्द’ की यह परिभाषा चूँकि आपसी संवाद का सबसे विश्वसनीय पुल है इसलिए संवादों के प्रति एक स्वाभाविक घृणा मेरे भीतर पलती और बढ़ती गई। मेरे पीठ पीछे ‘शब्द’ और ‘घृणा’ के बीच एक नया और अनोखा समीकरण ठीक-ठीक कब विकसित हो गया, यह मैं जान ही न सका।
‘इसकी एक वजह तो शायद माँ की आँखों का बुझा अंगार, उनकी आँखों में पसरा हुआ विराट मरुस्थल या विवश चुप्पी ही होगी। क्या इसीलिए माँ अपने अंतिम समय में मुझसे माफी माँगती रही थी? क्या ऐसी चुप्पी ने कभी ऐसे भिखारी से बात की होगी जो चुप दुनिया का नागरिक है और अजीब तरह से जमीन पर सिमटा हुआ बैठा है!’
सहसा प्रो. सिन्हा उठे और बाल्कनी से नीचे झाँका। शीत का कुहरीला अँधेरा फैल चुका था। अपार्टमेंट के तीसरे माले से भिखारी केवल एक काला धब्बा जान पड़ता था।
‘वैसे भी यह भिखारी या मैं, एक काले धब्बे के सिवाय क्या हैं?’ प्रो. सिन्हा ने मन ही मन सोचा। वे फिर मेज पर न जा सके। उन्होंने बत्ती बंद कर दी और बिस्तर पर लेट गए।
नींद ने प्रो. सिन्हा को झपट कर कब अपने पंजे में दबा लिया, वे जान ही न सके। बिल्ली या चील के पंजे में छटपटाते किसी चूहे की तरह उनकी रात कटी। वे न तो सो रहे थे और न ही जाग रहे थे। सोने और जागने के बीच की किसी स्थिति को वे रात भर आधी बेहोशी में झेलते रहे। उनकी डायरी का खुला हुआ पृष्ठ भी सहमा हुआ और बेचैन था।
सुबह जब उनकी नींद पूरी तरह टूटी, बाहर उजाला हो चुका था। उठते ही बालकनी की ओर से एक अनगढ़ और योजना-विहीन शोर के बगूले ने उन पर हमला किया। प्रो. सिन्हा की छटपटाती खुमारी टूट गई। वे हड़बड़ाकर बालकनी की ओर भागे।
नीचे, लोगों की भीड़ थी। भीड़ से थोड़ा हटकर सड़क के किनारे महानगरपालिका की एक बीमार गाड़ी खड़ी थी। और कुछ मुर्दे जैसे चेहरे वहाँ खड़े लोगों से पैसे इकट्ठे कर रहे थे। उन्हीं में से एक अपार्टमेंट में घुस आया था और लोगों के दरवाजे खटखटा रहा था।
प्रो. सिन्हा को समझते देर न लगी कि रात में ठंड से अकड़कर भिखारी की मौत हो चुकी है और महानगर के सफाई कर्मचारी इस सुअवसर का फायदा उठाकर लोगों से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं।
पूरा दृश्य ही भयंकर ढंग से अश्लील और घृणित था। भिखारी की लाश एक ओर पड़ी थी। दो-चार आवारा कुत्ते दूर बैठे उसे ललचाई नजर से देख रहे थे। शायद कुत्तों ने रात में लाश को चख भी लिया था। लाश पूरी तरह नंगी और मुड़ी हुई थी जिस पर उस सभ्य कॉलोनी के किसी सभ्य नागरिक ने कॉलोनी की सभ्यता का खयाल करके एक पुरानी और फटी हुई चादर डाल दी थी।
प्रो. सिन्हा ने भीड़ को देखा। भीड़ की व्यग्र आँखों में अपरिभाषित हिंसा की सैकड़ों रेखाएँ तैर रहीं थीं। उन्होंने उत्सुकतावश पास के पेड़-पौधों पर नजर डाली। वे खामोश थे, बिल्कुल खामोश; भीड़ ने हालाँकि उन्हें अपने में शामिल कर लिया था लेकिन फिर भी वे पूरी तरह निर्लिप्त थे। प्रो. सिन्हा को पहली बार पेड़-पौधों की निर्लिप्तता खल गई। उनकी आँखों के आगे अँधेरा छा गया और सिर चकराने लगा। उनका जी मचलने लगा और महसूस हुआ कि आँतों के भीतर से पिघलता हुआ लावा तेजी से हलक की ओर बढ़ रहा है और एक पल की भी देरी हुई तो नीचे खड़े लोग उनकी उल्टियों से सन जाएँगे। वे जैसे-तैसे अंदर की ओर भागे और देर तक बेसिन पर झुके रहे। अंततः जब उन्होंने अपना सिर उठाया तो उनकी आँखें लाल थीं और चेहरा किसी पौधे की तरह लग रहा था, निर्लिप्त और उदासीन। एक ऐसा पौधा, जिसमें कोंपल फूटने की क्षमता नष्ट हो चुकी है !
तभी दरवाजे पर दस्तक हुई।
पस्त कदमों से लगभग घिसटते हुए प्रो. सिन्हा ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर जामुनी रंग की वर्दी पहने एक खौफनाक-सा आदमी खड़ा था। दरवाजा खुलते ही उसने रटे-रटाए वाक्य बोलने शुरू कर दिए – ‘साब… कल रात तुम्हारी बिल्डिंग …एक मौत… पैसा…’
प्रो. सिन्हा कुछ भी सुन नहीं पा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि यह अजीब-सी शक्ल वाला जीव किसी दूसरे ग्रह का है जो अपनी अटपटी आवाज में कुछ कह रहा है। शायद कह रहा है – ‘कल रात तुम्हारी बिल्डिंग के बाहर एक भिखारी की मौत हो गई है। लेकिन वह मौत नहीं बल्कि हत्या है और मैं हत्यारे को जानता हूँ। तुम उसका नाम सुनोगे…?’
‘नहीं-नहीं…’ प्रो. सिन्हा भय से काँपने लगे। उनका चेहरा पीला पड़ गया और पसीने की बूँदें उभर आई। उन्होंने भड़ाक से दरवाजा बंद कर दिया और कान लगाकर सुनते रहे कि दूसरे ग्रह का वह विचित्र जीव गया या नहीं। जब उन्हें यकीन हो गया कि बाहर कोई नहीं है तो उन्होंने दरवाजे की दरार से झाँका। बाहर सचमुच कोई नहीं था। उन्होंने दरवाजा थोड़ा-सा खोलकर इस बात की तसदीक भी कर ली। फिर दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर बिस्तर पर लेट गए। बालकनी की ओर से आवाजों का उठता हुआ धुआँ फ्लैट के भीतर बहुत देर तक फैलता रहा।
स्थिति को सामान्य होते-होते यानी आवाजों को और दिनों की आवाजों की तरह होते-होते दिन के बारह बज गए। प्रो. सिन्हा की हिम्मत नहीं हुई कि वे इस भीड़ से होते हुए कॉलेज जाएँ।
वह पूरा दिन प्रो. सिन्हा के लिए बहुत ही यातनादायी था। उनके शरीर ने जैसे जीने से इनकार कर दिया था। आँखें छत से चिपकी रहीं। दो दिन से उनके पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया था लेकिन उन्हें भूख भी नहीं लग रही थी। उन्होंने अपने एक-एक अंग के बारे में सोचा लेकिन उन्हें उद्देश्य का कोई संकेत नहीं मिला। उन्हें पहली बार अपनी निरर्थकता का दुखद और तकलीफदेय एहसास हुआ।
शाम बीत रही थी। सूरज आसमान में दहककर बुझ चुका था। शहर रोशनी में नहा रहा था। रोशनी के छींटे कमरे के अँधेरे में तरह-तरह से पड़ रहे थे। प्रो. सिन्हा ने उठकर बत्ती जलाई और डायरी खोलकर लिखने बैठ गए –
‘आज मैं हार गया। लेकिन जीतने की कोई इच्छा क्या मेरे भीतर कभी रही थी?
जीतना आखिर होता क्या है? और मैं किसके खिलाफ लड़ रहा था?
‘मुझे हमेशा लगता रहा कि मैं एक पेड़ की तरह अपना जीवन निःशब्द जी लूँगा। एक ऐसे पेड़ की तरह, जिसके फूल और फल भले ही अनुपयोगी हों लेकिन वह धूप में अपना भोजन बनाए और उसे निजी तौर पर इस बात एहसास हो कि उसमें जीवन है। लेकिन… पेड़ों से प्रतिस्पर्धा…? क्या यह कभी संभव है? पेड़ों का भाव-शून्य जीवन क्या एक पल के लिए भी मुझे मिल सका? मैं माँ की आँखों में फैली वीरानी को कभी भूल नहीं पाया और आज तो मैंने पेड़ों के घृणास्पद कृत्य को भी लेख लिया! वे कैसे निर्लिप्त थे, निर्लिप्त नहीं बल्कि अभिशप्त, अपनी उदासीनता और चुप्पी के लिए अभिशप्त! उन्होंने अपनी चुप्पी में भी लेकिन धरती को ऑक्सीजन दिया है, अपनी डालियों में पंछियों को जगह दी है उनके प्रजनन और प्रणायातुर आह्लाद के गवाह रहे हैं, लेकिन मैं…’
प्रो. सिन्हा आगे कुछ भी लिख नहीं पाए। वे चुपचाप कमरे में बैठे रहे। उनके भीतर लहरें उठ रहीं थीं, उठती हुई लहरें आपस में टकरा रहीं थीं, जिस्म समुद्र में बदल चुका था और ठीक आगे भयंकर मरुस्थल था। उछलता समुद्र और जलता मरुस्थल उन्हें स्वाभाविक लगा, मानो उनके बीच कोई विरोधाभास ही न हो। मरुस्थल, समुद्र और उसकी लहरों को कमरे में लड़ता हुआ छोड़कर वे चुपचाप छत पर आ गए।
आधी रात बीत चुकी थी। शहर की रोशनियाँ आसमान में कुछ दूर तक जाकर दम तोड़ देती थीं। प्रो. सिन्हा आश्चर्य से आसमान को देख रहे थे। उन्हें सचमुच याद नहीं आ रहा था कि पिछली बार उन्होंने कब आसमान को इतने गौर से देखा था। लग रहा था जैसे पैदा होने के बाद पहली बार वे आसमान देख रहे हैं। पूरा आसमान तारों की टिमटिमाहट से भरा था और बीच में खड़े होकर चाँद अपना उजला रंग उछाल रहा था। आसमान का विस्तार उन्हें बहुत सुखद लगा। अपने छप्पन सालों को जब आसमान के सामने रखकर देखा तो उन्हें अपने आप से घृणा हुई। वे दुनिया के किसी बिल में अपने छप्पन सालों को छुपा देना चाहते थे। लेकिन काश कि वे ऐसा कर पाते…?
प्रो. सिन्हा आसमान की अदालत में चाँद और तारों को हाजिर-नाजिर जानकर देर तक माँ से, पिता से और अपने आप से जिरह करते रहे। बीच-बीच में कनखियों से वे उस जगह को भी देख लेते, जहाँ पिछली रात के किसी क्षण में भिखारी की मौत हुई थी। उन्हें महसूस हुआ कि वहाँ अभी भी दो थिर आँखें हैं, जो उन्हें घूर रही हैं! उधर जिरह समाप्त हो चुकी थी, फैसले की घड़ी आ चुकी थी। प्रो. सिन्हा अपने आपको कमजोर दलीलों के लिए कोस रहे थे। उन्हें इस बात का अफसोस था कि कितने कम शब्दों के साथ उन्होंने अपना जीवन गुजार दिया।
प्रो. सिन्हा लौट आए। लेकिन आसमान को तो अपना फैसला सुनाना था और उसने अपना फैसला सुना दिया। प्रो. सिन्हा ने लौटते हुए ही सिर झुकाकर फैसला स्वीकार किया और अपने फ्लैट के अंदर आकर दरवाजा बंद कर दिया।
उस दिन आधी रात को प्रो. सिन्हा ने पूरे मनोयोग से खाना बनाया-भात, दाल, सब्जी; अचार और पापड़ भी थाली में रखा और भरपेट खाना खाकर सो गए। उस रात वे इत्मीनान से सोए।
प्रो. सिन्हा देर से सोए थे लेकिन सुबह बिल्कुल तरोताजा उठे। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर चाय का एक भरपूर कप पिया और तैयार होकर कॉलेज निकल गए।
प्रो. सिन्हा आज लोगों को और दिनों की अपेक्षा कुछ अलग से लग रहे थे। अक्सर वे चाबी से चलने वाली गुड़िया की तरह सधे कदम और धीमी गति से चलते थे, मानो कब्र से सीधे उठकर कोई लाश चली आ रही हो। लेकिन आज उनकी चाल में कुछ व्यग्रता थी। कदम सहज नाप-तौल का विरोध करते हुए उठ रहे थे, कपड़े हालाँकि हमेशा की तरह बेतरतीब थे। आज लोगों ने देखा कि प्रो. सिन्हा कुछ सोचते हुए से चले आ रहे हैं जो लोगों के लिए रहस्यपूर्ण था।
व्यग्रता और हड़बड़ी के साथ प्रो. सिन्हा स्टॉफ रूम में रखे मस्टर पर हस्ताक्षर किया और कुर्सी खींचकर बैठ गए। वे हमेशा हस्ताक्षर के बाद सीधे अपने विभाग में चले जाते थे इसलिए वहाँ बैठना अन्य सहकर्मियों को थोड़ा अजीब लगा।
स्टॉफ रूम में उनके चार-पाँच सहकर्मी बैठे हुए थे, जिनसे आज तक उनकी कोई बातचीत नहीं हुई थी। प्रो. सिन्हा के आने से पहले वे आपसी हँसी-ठठ्ठा में व्यस्त थे लेकिन प्रो.सिन्हा की उपस्थिति ने उन्हें चौंका दिया। वे असहज हो गए और प्रश्नांकित नजरों से एक दूसरे को देखने लगे। आखिरकार गणित के प्रो. सिद्दीकी ने स्टॉफ रूम में अचानक पसर गई इस चुप्पी को तोड़ा –
‘डॉ. सिन्हा, बी-एस.सी. फायनल की प्रैक्टिकल परीक्षाएँ आप कब से ले रहे हैं?’
जवाब प्रो. सिन्हा ने फिर अपनी खालिस चुप्पी से दिया और प्रो. सिद्दीकी की स्थिति फिर असहज हो गई।
प्रो. सिन्हा पूरे कॉलेज में उपहास के घोषित पात्र थे। छात्रों को उनके नोट्स की जरूरत थी क्योंकि इस बड़े शहर में वनस्पति-शास्त्र की इतनी सारगर्भित जानकारी देने वाला दूसरा कोई नहीं था, लेकिन फिर भी मौके-बेमौके वे उन्हें छेड़ने से बाज नहीं आते थे। अपने सहकर्मी प्राध्यापकों और प्रयोगशाला में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए, खैर, वे पागल और औघड़ तो थे ही। केवल प्रो. सिद्दीकी ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे, जिन्हें उनका वेल विशर माना जाता था हालाँकि प्रो. सिन्हा ने आज तक उनसे भी कोई बातचीत न की थी। इसलिए प्रो. सिद्दीकी भी कॉलेज में पाव भर पागल तो मान ही लिए गए थे।
आज जब प्रो. सिन्हा ने प्रो. सिद्दीकी की बात का फिर कोई जवाब नहीं दिया तो वहाँ बैठे दूसरे लोग आँखों ही आँखों में मुस्कराने लगे और प्रो. सिद्दीकी उनकी आँखों से निकलते बाणों को सहते रहे। प्रो. सिन्हा चिड़िया की तरह उत्सुक आँखों से सबको देखते रहे। आज उनकी आँखें ऊँट की तरह अधमुँदी और भाव-शून्य नहीं थी।
इस छोटी-सी घटना के बाद सहकर्मी पुनः अपनी स्वाभाविक बातचीत में लौटने लगे। प्रो. सिन्हा के आने से पहले जिस मुद्दे पर वे हँसी-ठठ्ठा कर रहे थे, वह था – प्रजापिता ब्रह्माकुमारी की कुछ चेलियों का अगले सप्ताह कॉलेज में होने वाला व्याख्यान। कॉलेज के प्रिंसिपल यद्यपि रसायन-शास्त्र के प्रोफेसर थे लेकिन अपनी आध्यात्मिकता के लिए कुख्यात-विख्यात थे। उन्होंने एक जवान साध्वी को वैराग्य पर व्याख्यान देने के लिए अगले सप्ताह आमंत्रित किया था।
‘मनुष्य कितनी भी वैज्ञानिक प्रगति क्यों न कर ले उसकी आध्यात्मिक आवश्यकता, भौतिक आवश्यकता से ऊपर ही होती है।’ प्रो. चौबे ने कहा।
जो बात पहले मजाक में चल रही थी, अब वह गंभीर होने लगी थी। प्रो. चौबे प्रिंसिपल साहब के आदमी थे। उनका वक्तव्य दरअसल एक चुनौती था। उन्होंने विजयी मुस्कान से लोगों को देखा। उनकी आँखें जैसे चुनौती दे रही थी कि है कोई माई का लाल यहाँ, जो प्रिंसिपल के खिलाफ जा सकता है?
‘आध्यात्मिक जरूरत ही सब कुछ है तो आप जनाब, भौतिक सिद्धांत के मसलों को समझाने में अपनी जिंदगी क्यों जाया करते हैं! क्यों नहीं लोगों को तंत्र-मंत्र और प्रार्थना की नई-नई तरकीबें सिखाते? रहा सवाल नोट्स का, तो वो बाजार में मिल ही जाता है। और हम सब बाजार में ही तो बैठे हैं, बड़े-बड़े बैनर और पोस्टर लगाकर अपना-अपना माल बेचने के लिए।’ प्रो. सिद्दीकी तिलमिलाए हुए तो थे ही, उन्होंने बहुत खीझ के साथ अपनी बात रखी और उनका सीधा इशारा प्रो. चौबे के प्राइवेट ट्यूशन की ओर था।
‘जिंदगी की जरूरत पूरी करते हुए आप लोग भूले रहते हैं कि यह भौतिक जरूरत है कि आध्यात्मिक; और बात जब फलसफे की आती है तो शातिराना तरीके से आध्यात्मिकता के पिछवाड़े खड़े हो जाते हैं। दरअसल ‘आप लोगों’ का पूरा जोर ‘पिछाड़ी कल्चर’ पर है।’ प्रो. सिद्दीकी के ‘आप लोगों’ का सीधा इशारा प्रिंसिपल साहब और उसके चम्मचों की ओर था। उन्होंने ‘पिछाड़ी कल्चर’ कुछ ऐसे अंदाज में कहा था कि स्टॉफ रूम में बैठे सभी लोग हँसने लगे। प्रो. चौबे को ऐसे पलटवार की उम्मीद न थी। वे तिलमिला गए।
ठीक उसी समय स्टॉफ रूम में बैठे लोगों ने देखा कि प्रो. सिन्हा के चेहरे पर मुस्कुराहट की एक पतली रेखा खेल रही है, जो किसी आश्चर्य से कम न था। उन्हें मुस्कुराते देखकर प्रो. सिद्दीकी का हौसला बढ़ गया और उन्होंने पूछा – ‘क्यों डॉ. सिन्हा, इस बारे में आपकी क्या राय है?’
जवाब में प्रो. सिन्हा ने ‘हूँ’ कहकर सिर हिलाया और उनके सहकर्मियों ने पहली बार क्लास-रूम के बाहर उनकी आवाज सुनी। तभी पीरियड की घंटी बजी और सभी अपने-अपने लेक्चर के लिए चले गए।
प्रो. सिन्हा भी चुपचाप उठे और अपने विभाग से चॉक, डस्टर, रोल कॉल और किताब लेकर क्लास-रूम की ओर चल पड़े। क्लास-रूम में घुसते ही हमेशा की तरह उन्होंने पंखे बंद किए, दरवाजे पर कुंडी चढ़ाई, इशारे से खिड़कियों को बंद करने का निर्देश दिया और कुर्सी खींचकर चुपचाप बैठ गए कोई आधे मिनट तक इसी तरह बैठे रहने के बाद उन्होंने अपना रोल कॉल खोला और अटेंडेन्स लेने लग – ‘टू हंड्रेड ट्वेंटी वन, ट्वेंटी टू, ट्वेंटी थ्री…।’ अटेंडेंस लेने के बाद उन्होंने किताब खोली और आज का विषय ढूँढ़ने लगे। फिर अचानक जैसे उन्हें कोई बात याद आ गई। उन्होंने किताब बंद किया। ब्लैक-बोर्ड में बनाई गई उल्टी-सीधी तस्वीरों और लिखे वाक्यों को मिटाया और फिर साफ ब्लैक बोर्ड पर आज का विषय लिखा –
‘इकोलॉजी’, उसके नीचे कोष्टक में लिखा – ‘पारिस्थितिकी’।
वनस्पति-विज्ञान में रुचि रखने वाले छात्रों के बीच प्रो. सिन्हा के लेक्चर बेहद लोकप्रिय थे। इसका एक कारण तो उनकी भाषा थी। व्यग्रता ओर हड़बड़ी से अलग उनकी संयत भाषा एक झील की तरह शांत और मद्धम थी। क्लास में उन्हें बोलते हुए सुनना विषय में बहने के समान था। प्रो. सिन्हा शब्दों का उच्चारण ऐसे करते थे मानो शब्दों को निचोड़कर उसमें से अर्थ को बाहर निकाल लिया गया हो। वे अपने नोट्स तो अँग्रेजी में देते थे लेकिन समझाते हिंदी में ही थे। उनकी हिंदी बहुत साफ थी। चित्र बनाकर समझाते हुए अँग्रेजी नाम लिखने के साथ-साथ कोष्टक में हिंदी नाम भी लिख देते थे।
प्रो. सिन्हा ने अपना लेक्चर शुरू किया।
‘इकोलॉजी… यानी पारिस्थितिकी… इसे जानना, महसूस करना और अपने आपको जाने हुए के प्रति जिम्मेदार बनाना मनुष्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। जीव अपनी तात्कालिक आवश्यकताओं के अनुरूप जीवन को बदलता है, जीवन को बचाने का संघर्ष करता है और पराजित होकर नष्ट हो जाता है। नष्ट होना जीव का जन्मसिद्ध अधिकार है… मृत्यु सर्वाधिक जायज सत्य…’
प्रो. सिन्हा का लेक्चर आज भिन्न तरह का था। अमूमन विषय के बाहर के एक भी शब्द का इस्तेमाल न करने वाले प्रोफेसर ने अभी तक विषय के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा था। वे किसी दार्शनिक की तरह बोले जा रहे थे लेकिन भाषा में थोड़ी उत्तेजना थी।
‘इकोलॉजी को जानना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे जाने बिना जीवों की व्यवहारगत विशिष्टताओं को नहीं समझा जा सकता…’
‘सर, लेकिन इकोलॉजी का मतलब क्या होता है?’ एक छात्रा ने प्रश्न किया। दरअसल यह पहली बार हो रहा था कि प्रोफेसर ने विषय की आवश्यकता पर तो बोलना शुरू कर दिया लेकिन विषय की परिभाषा या अर्थ को स्पष्ट नहीं किया था।
प्रो. सिन्हा को शायद अपनी गलती का एहसास हुआ क्योंकि वे तुरंत विषय पर लौट आए –
‘इकोलॉजी का अर्थ है जीव तथा उसके आस-पास के वातावरण के… इंटर-रिलेशनशिप…’ थोड़ा रुककर प्रो. सिन्हा ने कहा, मानो इसी शब्द का तलाश रहे थे, ‘…पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। वनस्पतियों में एवं जंतुओं में इकोलॉजी का अध्ययन भिन्न-भिन्न तरीके से होता है। जंतुओं में चूँकि स्थान बदलने की क्षमता होती है इसलिए वातावरण में परिवर्तन होने पर वे अनुकूल वातावरण की ओर चले जाते हैं। वनस्पतियों में अपना स्थान स्वयं बदलने की क्षमता नहीं होती, वे अपनी स्थिति में जमे रहने के लिए शापित हैं इसलिए प्रतिकूल वातावरण का सबसे अधिक प्रभाव वनस्पतियों पर पड़ता है। वनस्पतियों से संबंधित वातावरण समय-परिवर्तन के साथ बदलता है जबकि जंतु समय-परिवर्तन अथवा स्थान-परिवर्तन द्वारा अपने को वातावरण के अनुकूल बनाते हैं…।’
प्रो. सिन्हा ने एक धीमी आह भरी तथा थोड़ा फिसलने के बाद फिर विषय पर लौट आए –
‘…इकोलॉजी’ शब्द का सबसे पहला प्रयोग सन् 1865 में विख्यात जूलोजिस्ट रेटर ने किया। इसकी तीन प्रमुख शाखाएँ हैं –
(I) स्वयं पारिस्थितिकी
(II) समुदाय पारिस्थितिकी
(III) ऑटेकोलॉजी…
तीसरा नाम लिखकर प्रो. सिन्हा थोड़ी देर तक उसका हिंदी नाम सोचते रहे, शायद उन्हें हिंदी नाम याद नहीं आया क्योंकि आगे का कोष्टक उन्होंने मिटा दिया था।
‘…ऑटेकोलॉजी’ इसके अंतर्गत किसी एक प्राणी या किसी एक जाति के प्राणियों के जीवन पर वातावरण द्वारा पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है…’
सहसा प्रो. सिन्हा ने अपना लहजा बदल कर कहा – ‘चलो, थोड़ी देर के लिए अपने विषय के भीतर ही हम अपनी तर्क शक्ति यानी लॉजिक की परख करें… ऑटेकोलॉजी… याद रखो, किसी एक प्राणी पर वातावरण द्वारा डाले गए प्रभावों का अध्ययन… मान लो कि वह प्राणी मनुष्य है, एक ऐसा मनुष्य जिसके पिता सेकेंड वर्ल्ड वार में मारे गए हैं… थोड़ी देर के लिए, मान लो कि ऐसा हुआ है! …और …उसके आस-पास का जैविक वातावरण सर्वथा उसके प्रतिकूल है… तब उस मनुष्य की क्रिया-कलाप कैसी होगी… उसका बिहेवियर कैसा होगा…?’
प्रो. सिन्हा ने पहली बार छात्रों से प्रश्न किया था। प्रश्न करते हुए मजा आया। वे विषय से बाहर चले गए थे इसलिए छात्र दिलचस्पी ले रहे थे, विशेषकर वे छात्र जिन्हें यह विषय बहुत बोर करता था।
‘लेकिन सर… आपने अभी कहा था कि पौधे अपनी जगह खुद नहीं बदल सकते, आपने एक वर्ड यूज किया था… शा… शापित… समथिंग लाइक दिज। जबकि आदमी तो जंतु की श्रेणी में आता है, और जंतु अपना स्थान बदल सकते हैं, मूव कर सकते हैं, इसलिए वह आदमी भी अपनी जगह बदलकर अपने आपको वातावरण के जैसा बना लेगा।’ एक वाचाल छात्र ने कहा।
‘…यही तो असल मुश्किल है माई डियर…’ प्रो. सिन्हा ने मुस्कुराते हुए कहा। ‘तुम लोगों ने बचपन में कई कहानियाँ सुनी होंगी कि अमुक आदमी, आदमी नहीं बल्कि पेड़ था या पत्थर था, या कि बना दिया गया था…’
‘…यस सर, अहिल्या…’ उसी छात्र ने तत्परता से कहा।
‘…एब्स्यूलिटली करेक्ट… तो यह जो मनुष्य है, जिसके पिता सेकेंड वर्ल्ड वार में मारे गए थे और जिसके आस-पास का जैविक वातावरण उसके विपरीत था, दरअसल एक वृक्ष था, लगभग पचास वर्ष पुराना वृक्ष! वनस्पतियों की दुनिया का एक नागरिक! वह जन्मा तो मनुष्य के रूप में ही था लेकिन बाद में वृक्ष बन गया था या कि शायद बना दिया गया था… इसलिए वह जंतुओं की तरह अपना वातावरण बदलने के लिए मूव नहीं कर सकता था। वातावरण को अनुकूल बना लेना तो खैर उसके बूते के बाहर की बात थी। अब बताओ, इस वृक्ष का क्या होगा…?’
क्लास-रूम में चुप्पी छा गई। छात्र जिज्ञासा से प्रो. सिन्हा का चेहरा ताक रहे थे और प्रोफेसर हल्के-हल्के मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे से साफ जाहिर था कि उन्हें मुस्कुराने का अभ्यास नहीं है।
अंततः एक शांत-सी छात्रा ने क्लास रूम में फैली चुप्पी को तोड़कर थोड़ा झिझकते हुए कहा – ‘सर, यदि उसमें मूव करने की कैपिबिलिटी नहीं है तो उसे नष्ट होना होगा।’
‘एक्सलेंट आन्सर…’ प्रो. सिन्हा ने चहकते हुए कहा। उनको देखकर लग रहा था कि उनके द्वारा खोजे गए किसी बहुत बड़े सत्य पर मासूम मुहर लगा दी गई है।
तभी पीरियेड के खत्म होने की घंटी बजी। प्रो. सिन्हा ने अपना सामान समेटा और यह कहे बिना कि ‘बाकी कल’, जो कि वे हमेशा कहते थे, क्लास रूम से बाहर निकल गए।
प्रो. सिन्हा की यह अंतिम क्लास थी।
Download PDF (तीन दिन)
तीन दिन – Teen Din