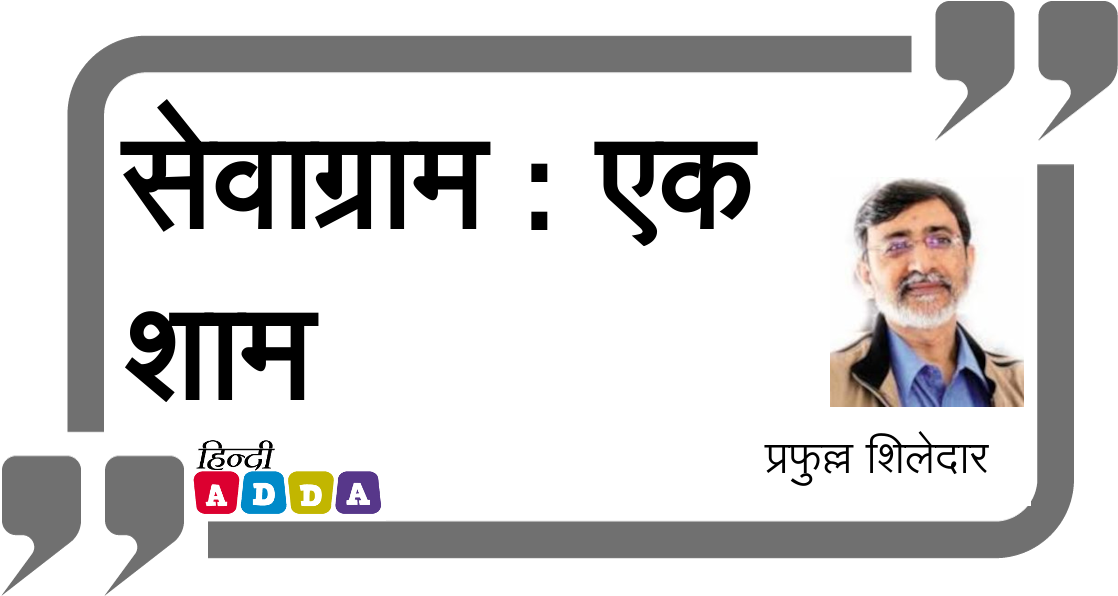सेवाग्राम : एक शाम | प्रफुल्ल शिलेदार
सेवाग्राम : एक शाम | प्रफुल्ल शिलेदार
मिट्टी से लिपे हुए उस कवेलुदार झोंपड़ी से
तो तुम कब के निकल चुके हो
तुम चारदीवारी के भीतर समा जाने वाले तो कभी थे ही नहीं
तुम वहाँ पर बस कुछ पल के लिए रुके थे
इसलिए व्यर्थ है तुम्हें वहाँ ढूँढ़ना
क्योंकि तुम तो हवा बनकर पूरी दुनिया में फैल चुके हो
तुम वहाँ टिके थे कुछ पल
लेकिन वो तुम्हारा पीठ नहीं
इसे जानते हुए भी लोग आते है यहाँ
तुम्हारी गंध को साँसों से खींच लेते भीतर तक
और घुला देते हैं अपने खून में नमक की तरह
समूचे परिसर में बिछी मोटी सी रेत पर
साँझ का अँधेरा घना होकर बिखर जाता है
कुटिया में जो तुम्हारी चीजें रखी हैं
उनके इर्दगिर्द भी जमा होता है अँधेरा
पर उसमें घुली होती है बकुल की गंध
इसलिए वो सूखा सा नहीं होता
जमीन पर बिछी रेत पर डाली जाती हैं लंबी दरियाँ
रखा जाता है एक दिया जिसकी बाती निश्चल
इकतारे की सीधी ठेठ लय
सामुदायिक प्रार्थना के धीमे स्वर
एक पेड़ के गिर्द गोल चबूतरे पर
मेरे साथ बैठा होता है दूर से आया एक कवि
वह अपना अकेलापन मेरे सामने खोलने लगता है
अपनी कैंसर से बीमार पत्नी को अकेला छोड़कर
किस वादे को पूरा करने वह यहाँ आया
इसकी कहानी में बंधता जाता है
वह ऐसी किसी बात को नहीं मानता
कि किसी के किसी जगह रहने से पवित्र हो जाती है वो जगह
उसने भी कभी नहीं माना विचारों से अधिक किसी भी चीज को
वह बताता रहता है
अपने यहाँ आने का अर्थ
जकड़ लेती है वह शाम
उसकी पकड़ से अपने पाँव खींचकर निकालते हुए
एक सफेद गाड़ी में बैठकर
मैं वहाँ से लौटता हूँ।
(मराठी से हिंदी अनुवाद स्वयं कवि के द्वारा)