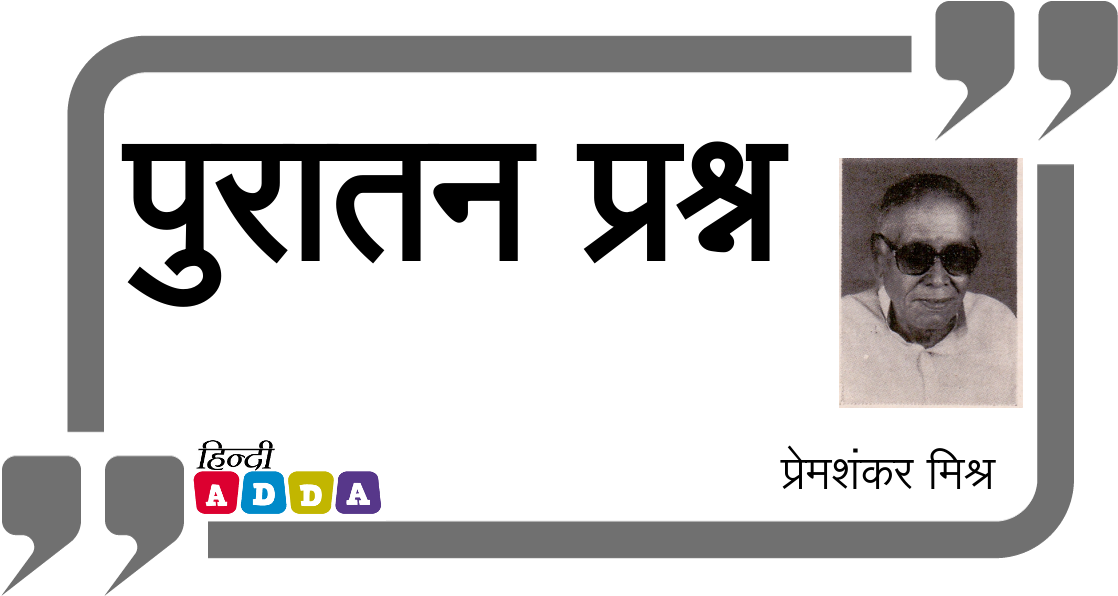पुरातन प्रश्न | प्रेमशंकर मिश्र
पुरातन प्रश्न | प्रेमशंकर मिश्र
खुद के रचे गढ़े
निशातबाग के फूलों की
जानलेवा खुशबुओं से आहत
एक अनुभूतिजीवी जंतु
रोज काफी रात गए|
छूछी दस्तकें दुहराता है
खोलकर छोड़ दिए गए रेडियो की भांति,
बिना किसी क्रम के
रात रात घड़घड़ाता है।
सहानुभूति की आँखे खुलती हैं
जीर्ण रसहीन
सूखी सख्त शहतीर में
अपनी ही गति की
एक निरूद्देश्य, निस्तत्व
तस्वीर बनाती हुई
आसजीवी भीलनी का
यत्न और न्याय
साफ-साफ उभर आता है।
सोचता हूँ
रेत का व्यवहार
पुरखों की अधोगति
प्यास की राहें
नहीं क्यों रोक पातीं
और
मदजल भरे नयनों का
फुदकता
रागजीवी हिरन वन का
सोचता हूँ
क्यों न बातें सुन रहा है?
सामने ही
छटपटाते प्राण की ध्वनि
चीखती है
किंतु फिर भी
हर सुनी को अनसुनी करता
नियति का रीतिधर्मा यह खिलौना
जान में
अनजान में
क्यों नाश अपना बुन रहा है?
प्रश्न यह कितना पुरातन
रोग यह कितना सनातन!