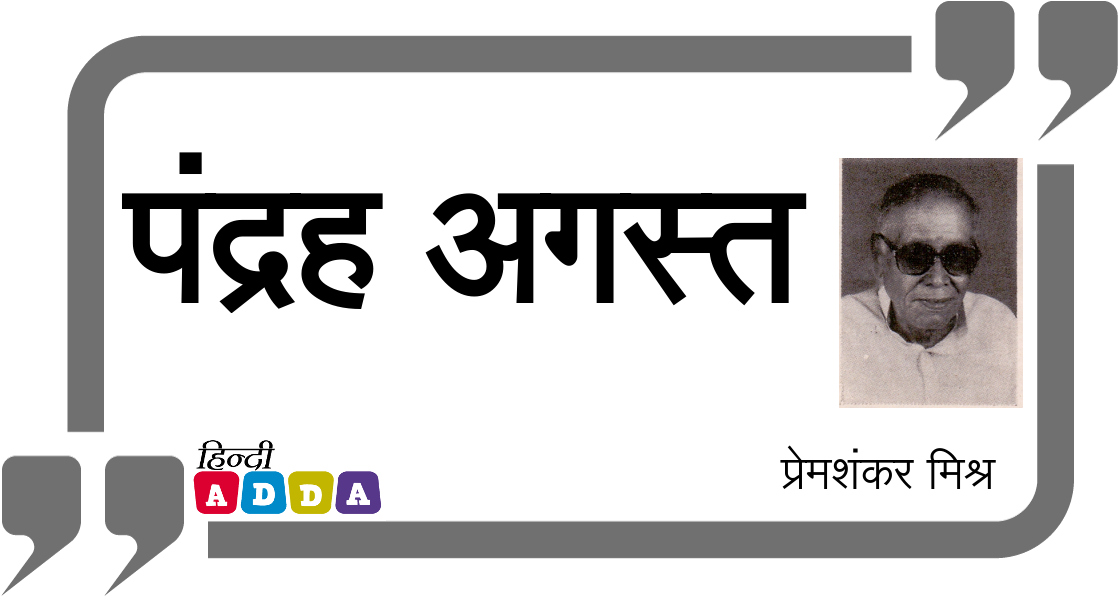पंद्रह अगस्त | प्रेमशंकर मिश्र
पंद्रह अगस्त | प्रेमशंकर मिश्र
मानवता की प्राणवायु
जब कालरात्रि में लय होती थी
जर्जर भारत
हँफर-हँफर कर
दो हिचकी तक पहुँच चुका था
और मनुज
युग-युग का भूलापहली सीढ़ी पर अपनी
चक्कर करता
थका हुआ सा
क्लांत और विश्रांत
क्षुब्ध नतमस्तक होकर
कुहनी टेके
अपने में अपने को खोकर
अंधकार के महासिंधु में
डूब-डूब उतराता जाता
उस अदृष्ट पर आँख गड़ाए
”संतोषम्” कह जीता जाता।
जीवन के इस घोर निबिड़ में
तेरा कुछ आभास मात्र पा
एक पुरुष ने
हमें दिखाई
तेरी ऊबड़ खाबड़ मंजिल
और
उसी कंकाल प्राण ने बाँह पकड़
झकझोर जगाया
सोते युग को।
मानवता ने ली अँगड़ाई
पर
इतना पर्याप्त नहीं था
फिर क्या होता?
युग मानव ने
एक हाथ में लिए
सत्य का दीप
अहिंसा स्नेह डालकर
निज जीवन वर्तिका बनाई
और
विनय की लकुटी टेके
डगमग कंपित
युग्म डगों को
तेरी संकरी और कंटीली
पगडंडी की ओर बढ़ाया।
”स्वतंत्रता अधिकार हमारा”
गुरु गर्जन ललकार समझ
तेरे बलिपथ पर
खड़े-खड़े लग गई भीड़।
नर नारी और आबालवृद्ध
सब निकल पड़े
”जय महाक्रांति” कह छोड़ चले
कितने जन
अपने चरण चिह्न
जलियाँ की वह होली आई
इक्कीस और इकतिस का क्या
सन् बयालिस का महाप्रलय
कितने यौवन धन लुटे
मिटे कितनी बहिनों के भाल बिंदु
कितनी माताओं के गोद के
छिने लाल।
बर्बरता का अट्टहास
मानवता का वैधव्य रुदन
कितने निरीह बालक
अनाथ हो त्राहि-त्राहि जब बोल उठे
तक जाकर मुझसे मिले
अरे पंद्रह अगस्त
तुम आजादी के नवल ज्वार
पावन प्रभात।