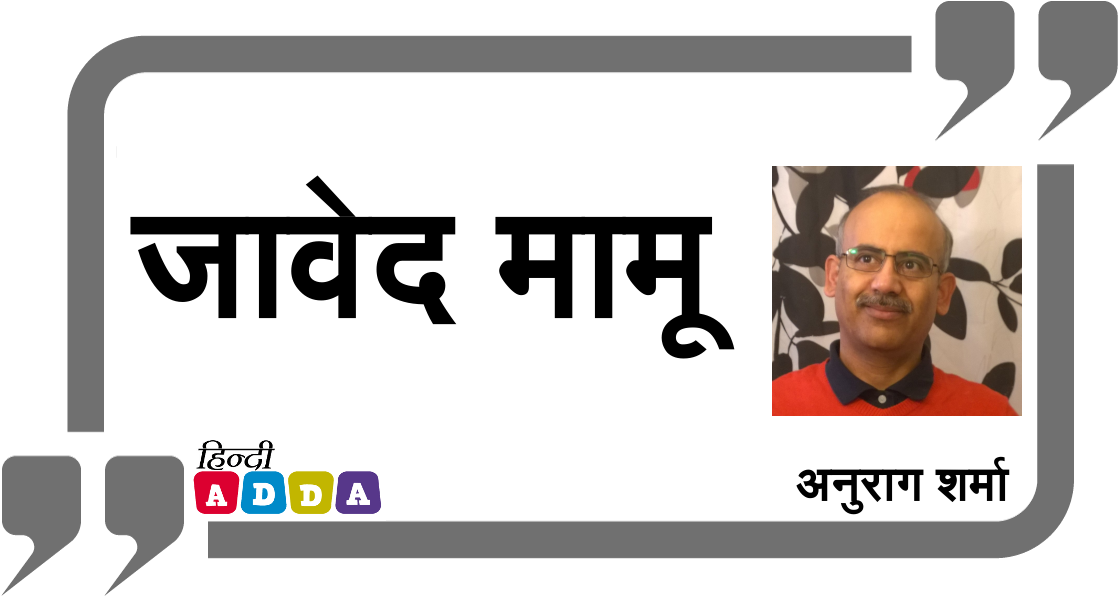जावेद मामू | अनुराग शर्मा – Javed Mamu
जावेद मामू | अनुराग शर्मा
काफी देर से स्टेशन पर बैठा था। रेल अपने नियत समय से पूरे दो घंटे लेट थी। देसाई जी की बात सही है कि आम भारतीय ट्रेनों की लेटलतीफी से इतना त्रस्त रहता है कि आपातकाल में रेल को वक्त पर चलाने के बदले में अपनी आजादी गिरवी रखकर भी खुश था। रेल के आते ही मेरा गुस्सा और झुँझलाहट दोनों हवा हो गए। दौड़कर अपना डिब्बा ढूँढ़ा और सीट पर कब्जा कर के बैठ गया। मैं बहुत खुश था। खुश होने की वजह भी थी। इतने लंबे अंतराल के बाद बरेली जो जा रहा था। पूरे तीस साल और तीन महीने बाद अपना बरेली फिर से देखने को मिलेगा। न जाने कैसा होगा मेरा शहर। वक्त की आँधी ने शायद अब तक सब कुछ उलट-पुलट कर दिया हो। जो भी हो बरेली का अनूठापन तो कभी भी खो नहीं सकता। किसी शायर ने कहा भी है :
हिंदुस्तान का दिल है दिल्ली,
और दिल्ली का दिल बरेली
आज मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ और जहाँ भी हूँ, उसमें बरेली का बहुत बड़ा हाथ है। मेरे बचपन का एक बड़ा हिस्सा बरेली में गुजरा है। जैसा कि सभी लोग जानते-समझते हैं हिंदुस्तान की जनसंख्या मुख्यतः हिंदू है। मगर बरेली वाले जानते हैं कि हमारे शहर में हिंदुओं से ज्याद मुसलमान बसते हैं। हमारे मुहल्ले में सिर्फ हमारी गली हिंदुओं की थी। बाकी तो सब मुसलमान ही थे। कुछेक मामूली फर्क के अलावा बरेली के हिंदू और मुसलमान में कोई खास अंतर न था। वे सदियों से एक-दूसरे के साथ रहते आए हैं और 1847 में उन्होंने एक साथ मिलकर एक साल तक बरेली को अँग्रेजों से आजाद रखा था। बरेली के “लक्ष्मीनारायण मंदिर” को लोग आज भी “चुन्ना मियाँ का मंदिर” कहकर ही बुलाते हैं। इलाके में एक हमारा मंदिर था बाकी सब तरफ मस्जिदें ही दिखती थी। हमारे दिन की शुरुआत अजान के स्वरों के साथ ही होती थी। मुहर्रम के दिनों में हम भी दोस्तों के साथ हर तरफ लकड़ी के विशालकाय ताजिओं के जुलूस देखने जाया करते थे। कहते हैं कि बरेली जैसे विशाल और शानदार ताजिए दुनिया भर में कहीं नहीं होते। होली-दिवाली वे हमारे घर आकर गुझियाँ खाते, पटाखे छोड़ते, रंग लगवाते, और मोर्चे लड़ते थे। ईद पर मेरे लिए सेवइयाँ भी लाते थे।
सच तो यह है कि एक परंपरागत ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर भी मुझे वर्षों तक हिंदू-मुसलमान का अंतर पता नहीं था। काश! मेरा वह अज्ञान आज भी बना रहता तो कितना अच्छा होता। हमारे घर में किराना जावेद हुसैन की दुकान से आता था और सब्जी-फल आदि बाबू खान के यहाँ से। आटा नसीम की चक्की पर पिसता था और मेरी पतंगें नफीस की दुकान से आती थी। हमारा नाई भी मुसलमान था और दर्जी भी। हमारा पहला रेडियो बिजली वाले तनवीर अहमद की दुकान से आया था और भजन के वे सारे रिकॉर्ड भी जिन्हें सुन-सुनकर मैं बड़ा हुआ।
मेरे आस-पास बिखरे भाँति-भाँति के लोगों में जावेद हुसैन एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने मेरे बाल मन को बहुत प्रभावित किया। वे मेरे मामा जी के मित्र थे इसलिए मैं उन्हें भी मामू कहता था। हमारे घर के सामने ही उनकी परचूनी की दुकान थी। मैं लगभग रोज ही सामान की पर्ची लेकर लेकर उनकी दुकान पर जाता था और घर-जरूरत का सामान लाया करता था। उनके दूसरे ग्राहकों के विपरीत मुझे किसी चीज का भाव पूछने की आवश्यकता न थी क्योंकि हमारा हिसाब महीने के अंत में होता था। उनकी दुकान में मेरा समय सामान लेने से ज्यादा उनसे बातचीत करने में और अपने से बिल्कुल भिन्न उनके दूसरे ग्राहकों की जीवन-शैली देखने-समझने में बीतता था। उनकी दुकान वह स्थल था जहाँ मैं अपने मुस्लिम पड़ोसियों को नजदीक से देखता था।
वे सभी गरीब थे। उनमें से अधिकांश तो इतने गरीब थे कि आपमें से बहुत से लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उनके कपड़े अक्सर गंदे और फटे हुए होते थे। आदमी और लड़के तो आमतौर पर सिर्फ उतने ही कपड़े पहनते थे जिनसे शरीर का कुछ जरूरी भाग ढक भर जाए। लड़कियों की दशा भी कोई खास बेहतर नहीं होती थी। हाँ, औरतें जरूर नख-शिख तक काले या सफेद बुर्के से ढँकी होती थी। तब मुझे यह देखकर भी आश्चर्य होता था कि अधिकांश बच्चों का सर घुटा हुआ होता था। इसी कारण से वे बच्चे अक्सर एक-दूसरे को “अबे गंजे” कहकर भी बुलाते थे। अब मैं जानता हूँ कि उनके सर घुटाकर उनके माता-पिता बार-बार बाल कटाने के कष्ट से बच जाते थे और गंजा सर उन बच्चों को थोड़ा साफ भी रखता था जिनके लिए नहाना भी किसी विलास से कम नहीं था। जो भी हो वे सभी बच्चे मेरी तरह गंभीर और बोर न होकर बड़े ही खुशमिजाज, जीवंत और रोचक थे।
मुझे घर में कोई पालतू जानवर रखने की आज्ञा नहीं थी। इसके कई कारण दिए जाते थे। एक तो इससे उस पशु-पक्षी की स्वतंत्रता का हनन होता था। दूसरे यह कि अधिकांश पालतू पशु-पक्षी घर में आने लायक शुद्ध भी नहीं माने जाते थे। इस नियम के कुछ अपवाद भी थे। जैसे, हमारी एक मौसी के घर में एक सुंदर बड़ा सा तोता था जो सभी आने-जाने वालों को जय राम जी की कहता था। कुछ रिश्तेदारों के घर में कुत्ते भी पले थे। बाद में कुछ बड़ा होने पर पता लगा कि तोता और कुत्ता प्रकृति से अहिंसक माने जाते थे और यह दोनों ही पूर्ण शाकाहारी भोजन पर बहुत अच्छी तरह पल जाते थे। मुझे याद है कि मौसी के तोते को मेरे हाथ से अमरुद और हरी मिर्च खाना बहुत पसंद था। मेरे मुसलमान पड़ोसियों के पास गजब के पालतू जानवर थे। पिद्दी, लालमुनिया और रंग-बिरंगे बज्रीगर से लेकर बड़े-बड़े कछुए तक, जो भी जानवर आप सोच सकते हैं वे सभी उनके पास थे। और अक्सर मैं बड़ों की निगाह बचाकर उन जानवरों के साथ खेल भी लेता था।
जावेद मामू दो अखबार मँगाते थे, एक हिंदी का और दूसरा उर्दू का। हिंदी समाचार पढ़ते समय जब भी उनके सामने कोई नया या कठिन शब्द आ जाता तो वे मुझसे ही सहायता माँगते थे। मैं उनको उस कठिन हिंदी शब्द को आम बोलचाल की भाषा में अनूदित करके समझा देता था। उदाहरण के लिए, वह मुझसे पूछते थे, “यह सोपानबद्ध क्या होता है?” और मैं उन्हें उसका उर्दू समकक्ष “सीढ़ी-दर-सीढ़ी” बता देता था। वह अक्सर कहते थे कि अगर मैं न होता तो उनके हिंदी अखबार के आधे पैसे बेकार ही जाते। इसी बहाने से वे कभी-कभी मुझे हिंदी ब्रिगेड का नाम लेकर चिढ़ाते भी थे। उदाहरण के लिए, वे कहते, “अच्छा खासा नाम था बनारस, बोलने में कितना अच्छा लगता था, यह हिंदी वालों ने बदलकर कर दिया वाणाणसी…”
वाराणसी को अपने अजीब मजाकिया ढंग से नाक से वाणाणसी कहते हुए वह “णा” की ध्वनि को बहुत लंबा खीचते थे। आखिर एक दिन मैंने उन्हें बताया कि वाराणसी का एक और नाम भी था। बनारस से कहीं ज्यादा खूबसूरत और उससे छोटा भी। जो किसी भी भाषा और लिपि में उतनी ही सुंदरता से लिखा, पढ़ा और सुना जा सकता था जैसे कि मूल संस्कृत में। वह प्राचीन नाम था – काशी। “काशी” नाम सुनने के बाद से उनका वह मजाक बंद हो गया। आज सोचता हूँ तो याद आता है कि तब से अब तक देश में कितना कुछ बदल गया है। बंबई मुंबई हो गया, मद्रास चेन्नई और कलकत्ता कोलकाता में बदल गया। और तो और बंगलौर भी बदलकर बेंगलुरू हो गया है। मजे की बात है कि इन में से एक भी बदलाव हिंदी ब्रिगेड का कराया हुआ नहीं है। हिंदी ब्रिगेड तो बनारस को काशी कराने की भी नहीं सोच सकी मगर अफसोस कि आज भी सारे अपमान हिंदी ब्रिगेड के हिस्से में ही आकर गिरते हैं।
उस समय की बरेली में हिंदी के कई रूप प्रचलित थे। शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली, देशज उर्दू, ब्रजभाषा, और अवधी, यह सभी बोली और समझी जाती थी। सिर्फ उर्दू की लिपि अलग थी। मैं बहुत साफ उर्दू बोलता था मगर पढ़-लिख नहीं सकता था। मेरे दादाजी फारसी के ज्ञाता रहे थे मगर इस समय वे इस संसार में नहीं थे। जावेद मामू को रोजाना उर्दू अखबार पढ़ते देखकर मेरे मन में भी उर्दू की लिपि पढ़ना-लिखना सीखने की इच्छा हुई। उस दिन से जावेद मामू ने प्रतिदिन अपने काम से थोड़ा समय निकालकर मुझे उर्दू लिखना-पढ़ना सिखाना शुरू किया।
एक दिन मैं उनकी दुकान पर खड़ा हुआ बहादुर शाह जफर की शायरी के बारे में बात कर रहा था तभी एक मौलवी साहब कड़ुआ तेल लेने आए। दो मिनट हम लोगों की बात सुनी और फिर जावेद मामू से मुखातिब हुए। पूछने लगे, “ये सब क्या चल्लिया है?”
“यह हमसे उर्दू सीख रहे हैं” जावेद मामू ने समझाया
“कमाल है, ये क्या विलायत से आए हैं जो इन्हें उर्दू भी नहीं आती?” मौलवी साहब ने बड़े आश्चर्य से पूछा।
जब जावेद मामू ने बताया कि मैं उसी मुहल्ले में रहता हूँ तो मौलवी साहब गुस्से में बुदबुदाने लगे, “कमाल है, हिंदुस्तान में भी ऐसे-ऐसे लोग हैं जिन्हें उर्दू जुबाँ नहीं आती है।”
उत्तर प्रदेश में शायद आज भी गन्ना और चीनी बहुत होता हो। उन दिनों तो रुहेलखंड का क्षेत्र चीनी का कटोरा कहलाता था। बरेली और आसपास के क्षेत्रों में कई चीनी मिलों के अलावा बहुत सारी खंडसाल थी। गुड़, शक्कर बूरा, बताशे और चीनी के बने मीठे खिलौनों आदि के कुटीर उद्योग भी वहाँ इफरात में थे। हमारे घर के पास भी एक बड़ी सी खंडसाल थी। वह खंडसाल हर साल गन्ने की फसल के दिनों में कुछ निश्चित समय के लिए खुलती थी। उन दिनों में आस-पास के गाँवों से किसान लोग मटकों में शीरा भर-भर कर अपनी बारी के इंतजार में खंडसाल के बाहर सैकड़ों बैलगाड़ियों में पंक्ति बनाकर खड़े रहते थे। मीठे शीरे की खुशबू हवा में फैली रहती थी। उस खुशबू से जैसे मधुमक्खियाँ इकट्ठी हो जाती हैं वैसे ही छोटे-छोटे गंजे और शैतान बच्चों के झुंड के झुंड वहाँ इकट्ठे हो जाते थे। कभी मौका लग जाए तो वे माँगकर शीरा खा लेते थे। और कभी जब शीरा घर ले जाना हो तो चलती बैलगाड़ी के पीछे चुपचाप लटककर एक-आध मटका फोड़ देते थे और टपकते शीरे के नीचे चुपचाप एल्यूमिनियम का कोई कटोरा आदि लगाकर उसे भर लेते थे और जब तक गाड़ीवान को पता लगे, भाग जाते थे। अक्सर दोनों पक्षों के बीच गालियों का आदान-प्रदान होता रहता था। गाड़ी वाले कोई मीठी सी ठेठ देहाती गाली देते और गंजी वानर सेना उसका जवाब उर्दू की निहायत ही भद्दी गालियों से देती। कभी कोई चोर पकड़ में आ जाता था तो किसान उसे मुर्गा भी खूब बनाते थे और तरह-तरह की हरकतें जैसे बंदर-नाच आदि करने की सजा देते थे। बेचारे गरीब किसानों की मेहनत के घड़े टूटते देखकर अफसोस भी होता था मगर आमतौर पर यह सब स्थिति काफी हास्यास्पद होती थी।
कभी-कभी शीरे की चाहत में बच्चे किसानों की खिदमत में अपने आप ही कुछ बाजीगरी या शेरो-शायरी करने को उत्सुक रहते थे। बैलगाड़ी वाले किसान लोग अक्सर कोई विषय देते थे और शीरा पाने के इच्छुक बच्चे उस शब्द पर आधारित शायरी गाकर सुनाते थे। और जनाब, शायरी तो ऐसी गजब की होती थी कि मिर्जा गालिब सुन लें तो खुद अपनी कब्र में पलटियाँ खाने लग जाएँ। ऐसे समारोहों के समय छोटे बच्चे तो मजमा लगाते ही थे, राहगीर भी रुककर भरपूर मजा लेते थे। मैं भी ऐसी कई मजलिसों का चश्मदीद गवाह रहा हूँ इसलिए बरसों बीतने के बाद भी बहुत सी लाजवाब शायरी हूबहू प्रस्तुत कर सकता हूँ। प्रस्तुत है ऐसी ही एक झलक, मुलाहिजा फरमाएँ – विषय है “गंजी चाँद”:
पहला बच्चा, “हम थे जिनके सहारे, उन्ने जूते उतारे, और सर पे दे मारे, क्या करें हम बेचारे, हम थे जिनके सहारे…”
दूसरा बच्चा, “गंजी कबूतरी, पेड़ पे से उतरी, कौव्वे ने उसकी चाँद कुतरी…”
एक दोपहरी को जब मैं जावेद मामू से बात कर रहा था उस समय कुछ उद्दंड बच्चों ने पत्थर मारकर एक गाड़ीवान के कई सारे घड़े एक साथ तोड़ दिए और गाड़ी के पीछे लटककर उनमें से बहता हुआ शीरा बर्तनों में इकट्ठा करने लगे। एकाध घड़े की बात पर कोई भी किसान कुछ नहीं कहता था मगर तीन-चार घड़े टूटते देखकर इस किसान को काफी गुस्सा आया और उसने ग्रामीण बोली में उन बच्चों को जमकर खरी-खोटी सुनाई। जब उसे लगा कि बच्चों पर उसकी बोली का कोई असर नहीं हुआ तो उसने शहरी जुबान में चिल्लाकर जोर आजमाया, “जरा देखो तो इन छुटके डकैतन को, कोई तो बतावै कि यह मुसलमान बालक ही काहे हमार घड़ा फोड़त हैं?
हालाँकि उस गाड़ीवान की व्यथा, शिकायत और आरोप तीनों में सच्चाई थी, उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा असहज हो गया था। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कहूँ। जब तक मैं शब्द ढूँढ़ पाता, जावेद मामू ने पलटकर जवाब दिया, “बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाई तुम, हिंदू अपने बच्चों की और उनकी पढ़ाई की परवाह करते हैं। हमारे लोग तो इन दोनों से ही लापरवाह रहते हैं।”
किसान बिना कुछ कहे चलता गया। बच्चे जावेद मामू की आवाज सुनकर छितर गए। मैं पाषाणवत खड़ा था कि मामू मेरी ओर उन्मुख हुए और एक पुरानी हिंदी फिल्म का गीत गुनगुनाने लगे, “तालीम है अधूरी, मिलती नहीं मजूरी, मालूम क्या किसी को दर्द ऐ निहाँ हमारा…”
मैं सोचने लगा कि उन पंक्तियों में उनके समाज का कितना सजीव चित्रण था। शायद मेरा ध्यान पाकर उनको आगे की पंक्तियाँ गाने का हौसला मिला। निम्न पंक्तियों तक पहुँचने तक तो उनकी आँख से अश्रुधार बहने लगी, “मिल जुल के इस वतन को ऐसा बनाएँगे हम, हैरत से मुँह तकेगा सारा जहाँ हमारा…”
वे रुँधे हुए गले से बोले, “राजू बेटा, मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान को दुनिया के सामने शान से सर ऊँचा करके खड़ा करने वालों में हिंद के मुसलमान सबसे आगे खड़े हों।”
मुझे अच्छी तरह याद है कि उस समय फखरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति थे। और वह पहले नहीं बल्कि डॉक्टर जाकिर हुसेन के बाद भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे। उनकी पत्नी बेगम आबिदा अहमद ने बाद में बरेली से चुनाव भी लड़ा और सांसद बनी। ऐवान-ऐ-गालिब की प्रमुख बेगम बाद में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा भी बनी।
इस घटना के तीन दशक बाद जब मैं ट्रेन में बैठा हुआ था तब मुझे इस इत्तेफाक पर खुशी हुई कि देश के तत्कालीन राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम न सिर्फ मुस्लिम थे बल्कि एक वैज्ञानिक भी थे जिन्होंने देश का सर ऊँचा करने में बहुत योगदान दिया था। बिल्कुल वैसे ही जैसा सपना जावेद मामू देखा करते थे। तीस साल में कितना कुछ बदल गया मगर अफसोस कि इतना कुछ बदलना बाकी है। बरेली के आसपास के मुस्लिम इलाकों में ग्रामीणों के झुंड ने पोलियो निवारण के लिए आने वालों पर अज्ञानवश हमले किए क्योंकि उनके बीच ऐसी अफवाहें फैलाई गई कि इस दवा से उनके बच्चे निर्वंश हो जाएँगे। छोटी-छोटी बातों पर फतवा जारी कर देने वाले धार्मिक नेताओं में से किसी ने भी अपने समाज के लिए घातक इन घटनाओं को संज्ञान में नहीं लिया है। न ही अभी तक इन अफवाहों या हमलों के लिए जिम्मेदार किसी आदमी को पकड़ा गया है।
मैं विचारमग्न था कि, “हाशिम का सुरमा…” और “बरेली की लस्सी…” की आवाजों ने मेरा ध्यान भंग किया। मेरा स्टेशन आ गया था। मैं ट्रेन से उतरा तो देखा कि तित्लू मुझे लेने स्टेशन पर आया था। इतने दिन बाद उसे देखकर खुशी हुई। हम गले लगे। तित्लू के साथ उसका पाँच-वर्षीय बेटा पाशू भी था। पाशू बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा कि तीस साल पहले तित्लू दिखता था।
घर के आसपास सब कुछ बदल गया था। इतना बदलाव था कि अगर मैं अकेला आता तो शायद उस जगह को पहचान भी न पाता। घर की शक्ल भी बदल चुकी थी और उसके सामने की इमारतें भी एकदम चकाचक दिख रही थी। खंडसाल की जमीन बेचकर लाला जी ने बाहर कहीं बड़ा व्यवसाय लगाया था। खंडसाल की जगह पर एक शानदार इमारत बन गई थी। तित्लू ने बताया कि यह भव्य इमारत जावेद मामू की है जहाँ उन्होंने एक आधुनिक आटा चक्की लगाई है। वे अभी भी परचूनी की दुकान चलाते हैं मगर यह दुकान उनकी पुरानी बित्ते भर की दुकान से कही बड़ी और बेहतर है।
मैं मामू की फ्लोर मिल की ओर चल रहा था। जब तक मैं जावेद मामू को देख पाता, तित्लू ने मुझे उनके बारे में बहुत सी नई बातें बताई। जावेद मामू हर साल दो बच्चों के स्कूल की किताबों का प्रबंध करते हैं। बीस साल पहले जब यह अफवाह उड़ी कि किसी ने मुहर्रम के जुलूस पर पत्थर फेंका है तो गुस्साई मुस्लिम भीड़ हिंदुओं की दुकानें जलाने के लिए दौड़ पड़ी। मामू सीना तानकर उन लोगों के सामने खड़े हो गए और उन्हें चुनौती दी कि एक भी हिंदू की दुकान जलाने से पहले उन्हें मामू की दुकान जलानी पड़ेगी। बाद में उन्होंने सबको समझाया कि लूट और आगजनी किसी एक समुदाय को नहीं जलाती है, यह देश का चैनो-अमन जलाती है और इसमें अंततः सभी को जलना पड़ता है। भीड़ ने उनकी बात को ध्यान से सुना और माना भी। उनकी उस तकरीर के बाद से मुहल्ले में कभी भी टकराव की नौबत नहीं आई। तित्लू ने बताया कि मामू के बेटे वासिफ ने हाल ही में डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की है और दिल्ली में एक महँगे अस्पताल की नौकरी को ठुकराकर पास के मीरगंज में ग्रामीणों की सेवा का प्राण लिया है।
जावेद मामू की बूढ़ी आँखों ने मुझे पहचानने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाई, “अरे राजू बेटा तुम, मेरे हिंदी के मास्साब!” वे अपनी चिर-परिचित मुस्कान के साथ मेरी ओर बढ़े। अपनी बाँहें फैलाकर वे बोले, बेटा पास आओ, इतने दिनों बाद तुम्हें ठीक से देख तो लूँ…”
जब मैंने आगे बढ़कर उनके चरण छुए तो उनकी आँखों से आँसू टप-टप बह रहे थे।
Download PDF (जावेद मामू)
जावेद मामू – Javed Mamu