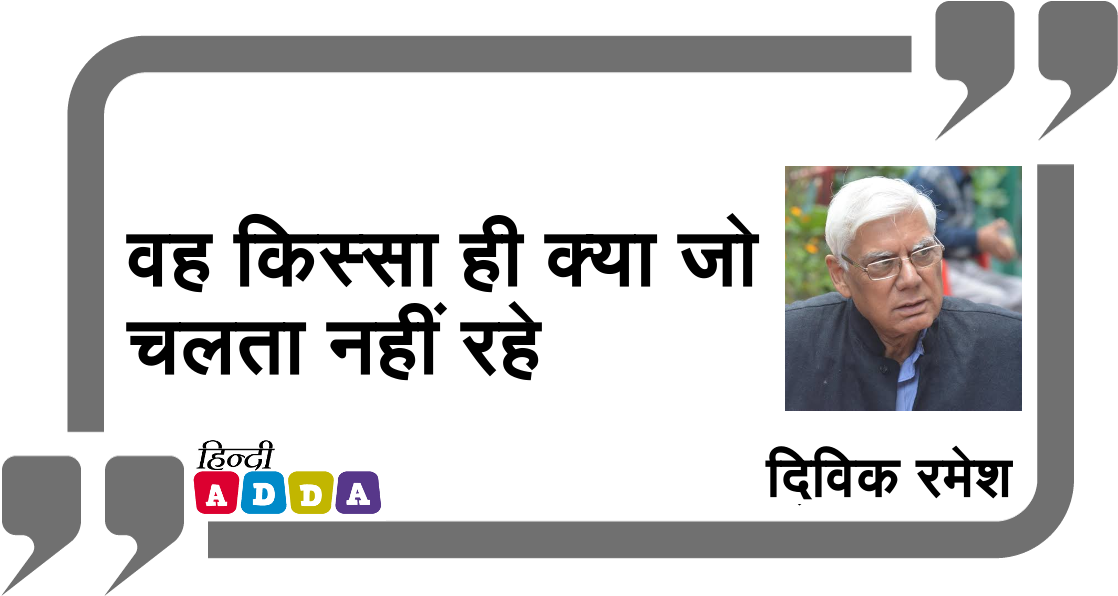वह किस्सा ही क्या जो चलता नहीं रहे | दिविक रमेश
वह किस्सा ही क्या जो चलता नहीं रहे | दिविक रमेश
किस्सा यूं है
कि गवाह पाण्डेय –
और चौंक पाण्डेयपुर का
रास्ता-सारनाथ
और धूल से अँटा, मुश्किल से पहचान में आता ‘ऑटो’
और हड्डियों को संभालते-संभालते ऑटो में,
मैं और पाण्डेय।
लाज से या कहूं शर्म से गड़ी जाती सड़क।
जगह-जगह
फटी साड़ी से गड्ढे।
ठहरिए भी
तनिक सब्र भी कीजिए जी
किस्सा भी आएगा
बगल ही में तो है।
पहले सुन तो लीजिए पेट की भी
बिखरा जा रहा है जिसका सब-कुछ
इधर-उधर।
ले रहा है टक्कर हमारे हौसलों से पूरी।
हिचकोले थे कि नहीं, ले पा रहे थे सांस तक।
दम बहुत था, पर ऑटो में
जबकि चालक ज़रूर बिदक लेता था जब-तब।
और भींच लेते थे हम अपनी-अपनी जेबें।
तो किस्सा यूं है
कि गवाह है, पाण्डेय और चौंक पाण्डेयपुर का
कि हम दोनों
सारनाथ से ज़्यादा राह पर थे लमही के
और जा रहे थे मिलने प्रेमचन्द के पात्रों से।
ख़ैर
पहुंचे तो अच्छा लगा सबकुछ भूल कर
सामने था प्रेमचन्द-द्वार लमही का
और थे दोनों ओर
खड़े, कुछ बैठे भी
पात्र प्रेमचन्द के, कुछ हांफते पर उत्सुक।
थे
कि वे भी आए थे, वहां धूल-धक्क़ड़ खाते
हमारी ही तरह ऑटो पर, बैलगाड़ी तो कहीं दिख नहीं रही थी।
पेट तो इनके भी रहे होंगे हमारी ही तरह
और सड़कें भी शर्म की मारी।
लगा
कि न वे पहचान पा रहे थे हमें
और न हम ही उन्हें शायद।
सिर चढ़ कर बोल रहा था धूल का महत्व दोनों ओर ही।
कितना एकाकार कर सकती है धूल भी
अगर आ जाए अपने पर।
जानता हूं, जानता हूं
टिप्पणी की ज़रूरत नहीं थी न
पर कोई विदेशी तो नहीं है न
ठेठ यहीं के है, इसी देश के
सो टिप्पणी तो ससुर मिली ही होगी न जन्मघुट्टी में
धरी रहती है जो ज़बान पर।
लो फिर कर गए टिप्पणी।
क्या सचमुच नहीं चाहता मन आज इतराने का देश पर!
तो किस्सा यूं है
कि धूल ओढ़े
धूल बिछाए
धूल खाए
और धूल ही पेश किए एक दूसरे को
हम
अपनापा खोकर भी बहुत अपने दिख रहे थे एक दूसरे को।
जितने ललकाए हम थे उतने ही तो दिख रहे थे पात्र प्रेमचन्द के भी।
लगता था
जाने कब तक की अटकी पड़ी प्रतीक्षा आंखों में
टप-टप
टपक पड़ी थी।
संधाए आकाश में कोई देवता नहीं था
बस जाने कहां से आकर
त्रिलोचन मंद-मंद मुस्कुरा रहे थे
और बगल में निराला आज़ादी का गीत गुनगुना रहे थे
जबकि नागार्जुन ढपली बजा रहे थे
और शमशेर संभाल-संभाल कर फूल बरसा रहे थे।
पता नहीं पाण्डेय का ध्यान तब किस ओर था
पर इतना तय था
कि वह उस दृश्य से महरूम रह गया था।
दूर-दूर तक कहीं कोई शिकायत नहीं थी।
धुल चुकी थीं प्रेमचन्द के पात्रों की आंखें।
सुरसुरा कर देह
बैलों तक ने झाड़ ली थी धूल-मिट्टी जमी कब की।
सुध तो ली थी न किसी ने उनकी।
कैसा लगा होगा उन्हें
कैसा?
सोचता हूं
जैसे बहुत दिनों के बाद
गांव लौटा हो बेटा
बहुत दूर शहर से
घर बना चुका है जो वहीं, हो चुका है वहीं का उसका पता।
किस्सा यूं है
कि अब आगे और कुछ नहीं–
होता भी क्या-मामूली आदमियों का मामूली किस्सा!
कि मुझे याद हो आया था
जर्मनी का न्यूरमबर्गशहर
कि शहर के स्टेशन के बाहर का चौराहा
कि चौराहे की सड़क के एक ओर खड़ा लेखक
और दूसरी ओर पिद्दी बना राजकुमार
और उसको डांटता हुआ एक नन्हा बालक तना
और उसकी बेकरी-मां, यानी पात्र लेखक के।
बस न वहां अंटा था लेखक धूल से
और न ही पात्र उसके।
और देखिए न
दर्शक भी नहीं।
तो किस्सा यूं है
कि वह किस्सा ही क्या
जो चलता न रहे।
तो चलते है।