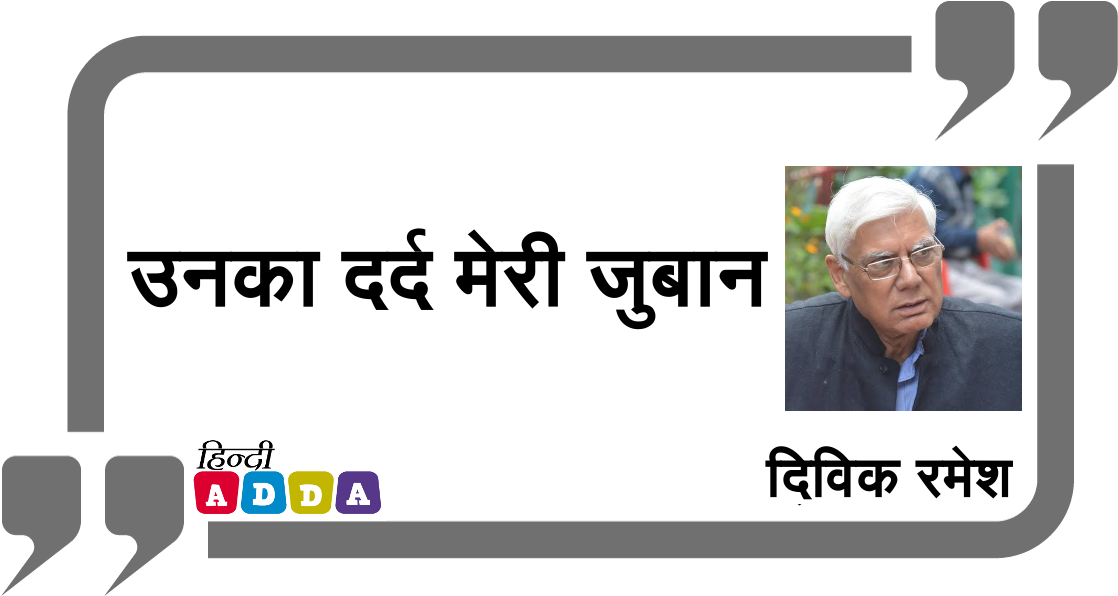उनका दर्द मेरी जुबान | दिविक रमेश
उनका दर्द मेरी जुबान | दिविक रमेश
हमारे समय की सबसे बड़ी त्रासदी
शायद वह आतंकवादी भी नहीं है
जो भून डालता है महज भूनने के लिए
जिसके पास है भी कोई समझ या दॄष्टि –
संदेह ही बना रहता है।
हमारे समय की सबसे बड़ी त्रासदी
शायद यह है
कि हमारे ही सामने, हमारे ही मुहल्लों में
हमारी ही समझ की छतों के नीचे
हमारे दर्दों को भी हमारा नहीं रहने दिया जाता।
बस छीन लिया जाता है हमसे –
न कोई कीमत, न कोई मुआवजा!
कैसी त्रासदी है न
होते ही उनका
हमारा दर्द हमें ही पहचानने से इनकार कर देता है –
ओपरा ओपरा होकर आंखें चुराता है।
बड़े घर के कुत्तों-सा लगता है घूमने बड़ी बड़ी गाड़ियों में।
कहां-कहां तक पहुंच नहीं हो जाती –
क्या इमारतें और क्या बड़े-बड़े होटल।
कुर्सी मेज़ों पर खाने उड़ाता है।
कोई कान तक नहीं देता था जिनकी और
अब देखिए औकात उनकी –
कितना बड़ा अभिनेता हो गया है –
निकल-निकल भोंपुओं से
कैसा रंग जमाता है।
उसके दर्दीले ठुमकों पर
पूरी दुनिया नागिन-सी झूमती है।
हमारा दर्द
जो हमें भिखारी तक बना देता था
पहुंचते ही मंचों पर
हमें दाता की मुद्रा में ला देता है।
और कवच ओढ़े हमारे दर्दों के वे
(जिनके नाम लेने तक में खतरा है हमें)
हमारी त्रासदी के देवता बन बैठते हैं।
और हम?
हमें तो पता ही नहीं चलता
कब क्या हो जाते हैं हम।
हां, आहे-बगाहे
जाने क्यों लगता है लगने
कि उनके भोंपू ही नहीं अन्दोलन भी
लादे अपने कंधों पर
उन्हें ही ढोते हैं।
ढोते हैं जैसे ढोते रहे हैं अपनी मजबूरियां
अपनी भूख और प्यास भी
और डरों में लिपटा अपना गुस्सा भी।
क्या नहीं है यह भी हमारे समय की सबसे बड़ी त्रासदी ?
हमारे समय की सबसे बड़ी त्रासदी तो यह भी है
कि ताकत है हममें
पर जीते हैं ताकत की मुद्रा में।
हममें युद्ध है
पर जीते हैं युद्ध की मुद्रा में।
हममें गुस्सा है
पर जीते हैं गुस्से की मुद्रा में।
हम फेंक सकते हैं उखाड़ कर
पर जीते हैं उखाड़ फेंकने की मुद्रा में।
हममें समझ है
पर जीते हैं समझ की मुद्रा में।
हमारे समय की सबसे बड़ी त्रासदी शायद यह भी है
कि हम महज बहस करते हैं
और वे उलझाए रखते हैं हमें बहसों में जिन्हें वे आश्वासन कहते हैं
हमारे मरने का इंतज़ार करते हैं
और एक दिन हम सचमुच मर जाते हैं –
यानी उनके धैर्य पर अपने अधैर्य को कुर्बान कर देते हैं
जबकि इच्छा उन्हीं की होती है ऐसी, पर अदृश्य।
वे महज मुद्रा में होते हैं बहस की, कहां समझ पाते हैं!
हार-गिर कर
समझ पाते हैं तो बस इतना ही –
क्या जाता है अपने बाप का
जो होता है
होते रहने दीजिए।
तो फिर बनते रहिए बेवकूफ
क्या जाता है अपने बाप का भी।