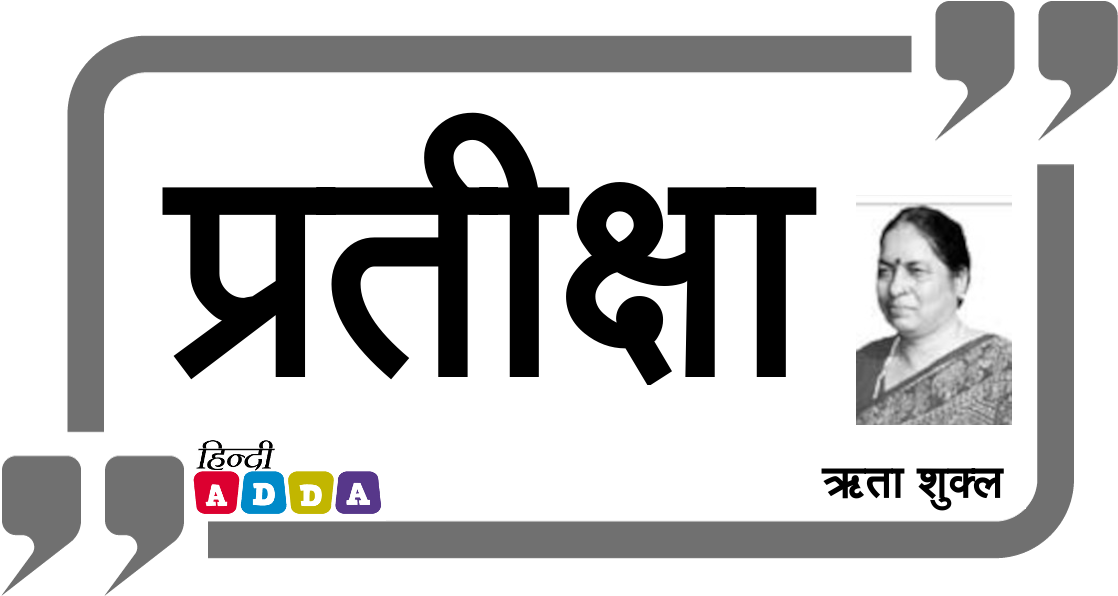प्रतीक्षा | ऋता शुक्ल – Pratiksha
प्रतीक्षा | ऋता शुक्ल
पड़ोस में किसी के यहाँ पुत्रोत्पत्ति हुई है शायद ! सोहर की मीठी लय सुनाई पड़ रही है, काँसे की थालियाँ एक साथ खनखना उठी हैं, फिर किसी कौशल्या की गोद में कोई राम अवतरित हुआ है। हवा की तरंग पर चढ़कर आ रहे सोहर के पारंपरिक बोल मेरे कानों से टकरा रहे हैं -राजा दशरथ हीरे-मोती लुटा रहे हैं, रानी कौशल्या अपनी देह के आभूषण उतारकर दे रही हैं।
घर-घर बधावा बज रहा है। आज अवध में राम का अवतार जो हुआ है।
रानी कौशल्या यानी सोनहुला काकी और अवध यानी गरीबी के धुँधलके में जीवन-मरण का त्योहार मनानेवाला भोजपुर का छोटा सा गाँव तिवारीपुर। इसी गाँव के सिवान पर बैलगाड़ी का रंगीन ओहार उठाकर तेरहवर्षीया नववधू सोनहुला काकी ने असीम कौतूहल से झाँका था। कदम की टहनी पर बैठी कोयल कूक उठी थी – कुहू-कुहू।
काकी ने लजाकर तुरंत ओहार नीचे गिरा दिया था, ‘क्या कह दिया दइमारी कोइलिया ने, तुम सुंदर हो।’
‘मैं सचमुच सुंदर हूँ क्या?’
काकी ने हाथ की मुंदरी निहारी तो पैरों में पड़ी झाँझ झनकार कर उठी। बैलगाड़ी के आगे-आगे पैदल चलते बिहारी काका, मलमल का गुलाबी कुरता, पीली धोती, पैरों में आलता, आँखों में काजल। सोनहुला काकी अपने सजीले दूल्हे की एक झलक देखकर लाज से दोहरी होती अपने आप में सिमट गई थीं।
पड़ोस का नवजात शिशु केहाँ-केहाँ-करके रोने लगा है। उसे भूख लगी होगी, उसे माँ का दूध चाहिए।
सोनहुआ काकी ने ब्याह के तत्काल बाद ही मातृत्व के कोमल सुख का अनुभव पा लिया था। उम्र के सत्रहवें साल में वे माँ बन गई थीं।
काकी के पैरों में हमेशा बजती रहनेवाली साँस, उनकी नकबेसर, उनकी चटकीली रंगीन साड़ियों के साथ-ही-साथ उनके रोचक किस्से-कहानियों का जादू हर साँझ हमें उनकी दहलीज तक खींच ले जाता था।
चिरायता की शक्ल की उनकी नकबेसर के बड़े आकार को देखकर टोले की लड़कियाँ अकसर ही मजाक करतीं, ‘यह छूँछी है या छूँछा, काकी?’
काकी जी खोलकर हँसती, ‘अब सरसों के दानावाला जमाना बा, तब इहे चाल रहे।’
दोनों गोरी बाँहों पर मोटे-मोटे गोदने, गले में कटावदार हँसुली, पैरों में झाँझ, माथे पर तेल में पिघलाए हुए सिंदूर का टीका… सोनहुला काकी का यह श्रृंगार अब भी मेरी आँखों में है।
उनकी बड़ी-बड़ी आँखें मुझे हर घड़ी घेर-बाँधकर अपने पास बुलाती रहती थीं और मैं बाहर से नीचे जाने का कोई भी मौका कतई नहीं छोड़ती थीं। छोटे-छोटे सवाल पूछकर काकी को परेशान करने में बड़ा मजा आता था, ‘काकी, आपकी दोनों बाँहों पर ये गोदने क्यों हैं? आपकी साथियाँ इतनी चटक कैसे रहती हैं? काकी-काकी, एक बार फिर वही झाँझवाला किस्सा सुनाइए न।’
काकी पहले तो मुझे एक बनावटी ताड़ना देतीं, ‘चल हट, बतबनवनी कहीं की। चउदह-पनरह बरिस के बिटवनी, काम-काज सिखबू कि हमरा पीछे-पीछे घूमत रहबू?’ फिर वे बतातीं, किस तरह सास की गोदी में लेटकर उन्होंने गोदना गोदवाया था। उनके समय में सब औरतों को गोदना गोदवाना जरूरी था। काकी की सास ने उन्हें गोदने का महत्त्व समझाया था, ‘मरला प-सब निसानी छूटि जइहें, इहे गोदनवाँ साथे जइहें। जम के दुआरी इहे पहिचान रही।’
किर्र… किर्र… ।गोदना गोदनेवाली नटिनी की बारीक सुई काकी की कोमल चमड़ी में चुभती हुई फूल-पत्तियाँ उभारती गई थी और काकी की आँखों से टप-टप आँसू बहते गए थे।
काकी का झाँझवाला किस्सा सबसे मजेदार था। सोमेश्वर भइया जब उनके पेट में थे, तब एक रात अचानक उनके दोनों पैर सूज गए थे। पल-पल पैरों की सूजन बढ़ती ही जा रही थी। यहाँ तक कि उनकी झाँझ पैरों में फँसकर चुभने लगी। तकलीफ बहुत बढ़ गई तो बिहारी काका झाँझ कटवाने के लिए गाँव के भगेलू सुनार को बुलाने गए। अब काकी चंग पर चढ़ गर्इं, ‘मरि जाइब त मरि जाइब, बाकी बाहरी मरद के सामने गोड़ ना उघारिब।’
बात पूरे टोले में फैल गई। तब बूढ़े वैद्य पंडित सरजू प्रसादजी ने खबर भिजवाई, ‘कनिया से कहो, गुनगुने पानी की बालटी में पाँव डुबोकर बैठ रहे। कुछ फायदा होगा।’
सूजन तो खैर कम हो गई थी, लेकिन गाँव भर में बात फैल गई थी कि काकी के पाँव भारी हैं, और इसी लाज से काकी रातोरात नैहर चली गई थीं।
मैं हर बार काकी से अपनी ओढ़नी रँगवा लाती। उनकी रंग-बिरंगी साड़ियों पर मेरी आँखें अटककर रह जाती थीं। कपड़े रँगने का कितना आसान तरीका था उनका। हरसिंगार के फूलों को सिलबट्टे पर पीसकर नारंगी रंग निकाला जाता। पटहारिन के यहाँ से लाल-हरे रंगों की पुड़िया आती और पलक झपकते रंगों के घोल में डुबो-डुबोकर साड़ियाँ और ओढ़नियाँ अलगनी पर लटका दी जातीं। नैहरवालों की याद सोनहुला काकी की छाती में पुराने जख्म की तरह हमेशा टीसती रहती थी। सावन-भादों के महीने में गंगा का पानी उमड़ता हुआ जब गाँव के चारों तरफ खेतों में लहराने लगता, तब ऊँचे अरार पर खड़ी काकी की आँखें अपने आप बरसने लगतीं। गंगा की विनाशकारी बाढ़ ने उनके पूरे परिवार को एक ही बार में अपनी चपेट में ले लिया था। सबसे ज्यादा याद करती थीं वे अपने छोटे भाई किशून को।
‘घर में सबसे सुन्नर, सबसे तेज हमार भाई। आखिरी दिन तक कहत रहे, गंगाजी बढ़ियाइल जात बाड़ीं। घर के मोह छोड़ि के दिदिया के गाँवे चले के चाही। लेकिन माई-बाबूजी केहू ओकर बात के सुनवाई ना कइल।’
मेरे ब्याह के दूसरे साल बिहारी काका चल बसे थे। सोनहुला काकी की झाँझ बजते-बजते अचानक खामोश हो गई थी। सोमेश्वर भइया तब बी.ए. मे पढ़ते थे। चटकीले पहिरावे की जगह कोरी साड़ियों में लिपटे सोनहुला काकी के श्रृंगार-विहीन रूप की कल्पना मुझे सिहरा जाती। काकी के विधवा वेश को झेल पाने की सामर्थ्य मेरे भीतर नहीं थी। अच्छा ही हुआ कि मैं गाँव से बहुत दूर चली आई थी।
बिहारी काका के गुजर जाने के बाद सोनहुला काकी का जीवन वैसा निर्द्वंद्व नहीं रह गया था। सामा-चकइया का करूण विदाई गीत काकी के जीवन में साकार उतर आया था। सामा खो गया था और चकइया उसे ताल-ताल, बन-बन, आकाश-पाताल सब जगह खोजती फिर रही थी, वह अपने साथ चकइयाँ के सारे गीत भी समेटकर लेता गया था।
गाँववालों ने काकी को सलाह दी थी, ‘सोमेसर को अब अपनी बपौती सँभारनी चाहिए। दुखिया महतारी को भी धीरज बँधेगा, बेटा नजर के सामने रहेगा।’
सोमेश्वर भइया की आगे पढ़ने की इच्छा थी। सोनहुला काकी ने भी बेटा का ही पक्ष लिया था। उनकी हमजोलियों ने उन्हें ऊँच-नीच भी समझाया था – ‘सहर की हवा लग गई तो लड़का बहक जाएगा। कच्ची उमर है और अब तो बाप का साया भी सिर पर नहीं है। देखा नहीं, अवधेस नरायन का बेटवा? डागदरी पढ़ने गया था, इसाइन से परेम बियाह कर बैठा। भाई-बाप कुल-खानदान सब छूट गया।’
सोनहुला काकी ने एक ही बात से सबको चुप करा दिया था, ‘जवन सोमेसर के खुसी, तवने हमार खुसी। हम कबहीं कवनो जबरदस्ती ना करब।’
सोमेश्वर भइया ने पटना विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एम.ए. की डिग्री ली और वहीं प्राध्यापक हो गए।
सोनहुला काकी बिना किसी प्रतिवाद के बेटे की हर बात मानती गई थीं। सोमेश्वर भइया को अपने साथ पढ़नेवाली एक पंजाबिन लड़की भी गई। न सगुन उठा था, न हल्दी चढ़ी थी, न बारात सजी थी, न बधावे बजे थे। काकी अपने बेटे के साथ अकेली ही पटना चली गई थीं। बहू की मुँह-दिखाई जो करनी थी। बरसों पुरानी पोटली में सहेजकर रखा गया कंठा उसके गले में पहनाना था। एक बार काकी ने वह भारी-भरकम कंठा मुझे दिखाया था। पुत्रवती होने की असीस के साथ काकी की सास ने वह कंठा उनके गले में पहनाया था। पता नहीं,काकी की सुशिक्षित, विजातीय वधू को उनका उपहार पसंद आया या नहीं? काकी तो दूसरे ही दिन गाँव लौट आई थीं।
गाँव की कुछ औरतों ने आपस में इशारेबाजी भी को थी, ‘इतनी जल्दी लौट आर्इं, सरदारनी बहू के साथ एक दिन भी नहीं ठहर पार्इं? तंदूरी रोटी का सवाद तो चख आतीं… अब क्या करेंगी सोनहुला देई? बड़ा बेटे का गुमान करती थीं। निकल गया न पखेरू हाथ से।’
सोनहुला काकी की चुप्पी हरेक की बात का जवाब बन बैठी थी। असाधारण रूप से गुमसुम रहना स्वभाव था।
दस वर्ष बाद गाँव जाने का मौका मिला। नन्हे सिद्धार्थ का मुंडन करवाना था। अम्मा ने मनौती मानी रखी थी, गाँव के काली चौंरे पर ही उसका मुंडन होगा।
जैसे-जैसे बस गाँव के करिब आती जा रही थी, मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। सोनहुला काकी से मिलने के लिए मेरी आकुलता असंयत हो उठी थी। पूरा सुफर काकी की चर्चा करने में ही कटा था। अम्मा ने बहुत सी बातें बताई थीं।
काकी के सगे देवर ने उनके अकेलेपन का फायदा उठाकर उन्हें बेघर-बार करने की पूरी साजिश की थी। बहलाने–फुसलाने का काकी पर कोई असर न होता देखकर उन्होंने काकी के दोनों बनिहारों को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। काकी अपने धखर खेत की जुताई के लिए खुद ही हल-बैल लेकर फेंटा बाँधे निकल आई थीं। बाद में गाँववालों ने काकी के देवर की खूब थुक्कम-फजीहत की थी। दोनों बनिहार भी अपने लालच की बात स्वीकारते, काकी से माफी माँगते उनके पास लौट आए थे।
‘कुछ भी कहो, सोनहुला ने बड़ा तप किया। गाँव में अकेली रहकर अपने बूते पर सबकुछ सँभालती रही। न किसी के सामने हाथ पसारा, न किसी के सामने अपना दुखड़ा रोने गई।’
गाँव के पास बस रूकी। पश्चिम पट्टी के खेतों की मेंड़ पर सबसे आगे मैं सिद्धार्थ को लिए हुए। पीछे से ताकीद करती अम्माँ, ‘कोड़ाई का खेत है, ऊबड़-खाबड़ जमीन। सँभलकर चलो, इतनी जल्दी क्या है?’
जल्दी थी। सोनहुला काकी से मिलने की जल्दी।उनसे जी भरकर बातें करने की उतावली मेरे पैरों में गति भर रही थी। दूर दिखाई पड़ रहा था बड़का टोला। आम, इमली, कटहल और महुआ के पेड़ों से घिरा हुआ। पहला घर हमारा, दूसरा सोनहुला काकी के देवर का और तीसरा सोनहुला काकी का।
बाँस की रंगीन चंगेरी लेकर काकी महुआ बीनने निकला करती थीं। ‘सुकिया उगे ओकरा पहिले बगइचा में निकलि के महुआ बीने के उछाह बूझे के होखे त… हमरा साथे चल बचिया। महुआ के महक में डूबल पीठ बतास बहत रहेला। आठो अंग से गीत के इनकार फूटे लागेला।’
महुआ टपकने का मौसम नहीं था, लेकिन महुआ के पेड़ के नीचे पहुँचकर सोनहुला काकी के वे मीठे अनुभव एकबारगी मेरी चेतना में उभर आए। काकी का प्रिय गीत, जिसे वे महुआ चुनते समय अकसर ही गुनगुनाया करती थीं, मेरे कानों में बजने लगा था।
‘आजु मोरे राम अवधपुर अइहें… ’
मैंने चलते-चलते अम्मा से सोमेश्वर भइया के बारे में पूछ लिया, ‘काकी के राम-सीता आजकल कहाँ हैं अम्मा?’
‘कौन? सोमेश्वर? वह तो विदेश चला गया। उसकी बहू भी साथ ही गई है। कोई छह महीने हुए होंगे।’
गाँव की अपनी अँगनाई में पहुँची तो मिलनेवालों की भीड़ लग गई। मेरे बचपन की सखी सावित्री ने मुझे अँकवार में बाँध लिया।
‘काकी कैसी है सावित्री?’ मेरा पहला सवाल यही था।
‘सोनहुला काकी की बात पूछ रही है, सखी?’
‘काकी बउरा सी गई है। सोमेसर भइया के विलायत जाने के बाद काकी के नाम उनका एक पारसल पहुँचा था – चार साडियाँ और थोड़े से रूपए। काकी बेटे की सौगात को छाती से लगाकर अपनी कोठरी में बंद हो गई थीं। दिन भर बिना खाए-पीए वैसी ही पड़ी रही थीं। हम लोगों ने बहुत चिरौरी की, लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला था। आधी रात के सन्नाटे में काकी की कोठरी से सोहर गाने की आवाज सुनाई पड़ी थी –
‘आजु मोरे राम अवधपुर अहइँ –
राम के बइठइबोरे सोने के सिंहासन,
सिया जी के आँचर ओट … .
आजु मोरे राम
‘सोनहुला का गीत सुनकर गाँव भर की आँखें भर आईं थीं। अब सोनहुला काकी नहीं बचेगी, सखी।’
‘बेटे की ममता ने उसे एकदम सुखा दिया है। तू देखेगी तो पहचान भी नहीं सकेगी। दिन-रात अपनी कोठरी में पड़ी कराहती रहती है, जैसे कोई ताजी व्याई गाय अपने मरे हुए बछड़े के लिए डकर रही हो।’
बाँस के झिलंगे खटोले पर लेटी सोनहुलाकाकी मेरे सामने थीं – मारकीन की मटमैली साड़ी से देह ढँके। सींक–सी दुबली। दोनों बाँहे बढ़ाकर उन्होंने मुझे अपनी छाती में समेट लिया।
काकी की मुसकान का हँसकर साथ देनेवाले गोदने के फूल अब सूखी चमड़ी के साथ चिपके नीचे झूल रहे थे। पतली, नुकीली नाक में चिरायता अब भी था। काकी हँसने की नाकाम कोशिश कर रही थीं। ‘हमार नाति राजा के गोदी में दे बचिया। दमाद बाबू ना अइले?’
काकी निखहरे खटोले से उठीं तो उनकी नंगी पीठ पर कड़ी मूँज की बिनावट के निशान उभर आए थे। मैं हाथ बढ़ाकर पीठ सहलाने चली तो उन्होंने मना कर दिया, ‘पीठ के दाग मत देख बचिया, छाती के दाग देखा सकतीं त देखइती रे।’
काकी ने उठने की कोशिश की थी। वे सिरहाने रखे टुटहे संदूक तक जाना चाहती थीं। लेकिन खटोले से उठते वक्त उनके पैर थरथरा गए थे और वे वापस बैठने की कोशिश में गिर पड़ी थीं।
‘क्या हुआ काकी, कुछ चाहिए क्या?’ मैंने हड़बड़ाकर उन्हें थाम लिया था।
‘ना रे, अब कुछ ना चाहि। बहुत सुख मिलल, बहुत राज कइलीं।’
काकी ने संदूक खोलने को इशारा किया था, एक काली पोटली निकलवाई थी और उकसे भीतर से कब का मुड़ा-तुड़ा पाँच रूपए का नोट निकालकर सिद्धार्थ की नन्ही मुट्टी में दबा दिया था।
‘काकी, ऐसा मत कीजिए काकी, आपका आशीर्वाद ही काफी है, देना तो हमें चाहिए।’
‘दूर पगली … ।’ काकी की चिर-परिचित परिहासमयी मुद्रा एक बार फिर वापस लौट आई थी, ‘सुन, तनि बतबनवनी के बात। बेटी के धन हम लेब? हमरा कवनो कमी नइखे बचिया।
‘जब ते बीमार पड़लीं, टोली-पड़ोस से दू मुट्ठी भात, दू गो रोटी साँझ पराते मिल जाला। गाँव के लोग दान दच्छिना में जनव मोट-महीन बस्तर देला, पहिर लेईला। अब का चाही? नाती के देब-तह हमार अगिला जनम सुधरी बचिया।’
काकी को ज्वर हो गया था। उस रात मैं सावित्री के साथ काकी के पास ही रह गई थी।
ढिबरी की मद्धिम रोशनी में मैं और सावित्री काकी के पायताने बैठी उनके तलवे सहला रही थी। तभी वे अचानक उठ बैठी थीं, ‘क्या हुआ काकी?
‘जइसनसबद सुनात बा बचिता?’
‘कुछ तो नहीं काकी, आप सो जाइए… ’
‘आँख नइखे लगत रे, बहुत बैचेनी बा। कहीं टोल-पड़ोस में लडिका भइल बा का? फुलहा थरिया बाजत बा?’
वे देर तक खटोले पर इधर-से-उधर छटपटाती रही थीं। फिर उन्होंने लेटे-लेटे ही उँगलियों पर न जाने कौन सा हिसाब लगाया था, ‘आजु कातिल के पूरनमासी ह-सबित्तरी?’
‘हं-काकी।’
काकी ने आँखें खोलकर सावित्री से निहोरा किया, ‘आजु उहे सोहर सुना दे बचिया।’ सावित्री गाने लगी –
‘राज सिया मोरे आँख के पुतरी
दूनो बिना जगत अन्हार
आजु मोरे राम… ’
काकी की आँखें झर-झर बरसने लगीं। उनका आँचल भींग गया। गीत के थमते ही उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर आँखें बंद कर लीं। ‘भगवान जंगल-झाड़ सब में कुसल राखतु, अजुए बबुआ के जनम भइल रहे बचिया।’
सोनहुआ काफी के भीतर बरसों पुरानी प्रसव पीड़ा ताजी हो गई थी। कानों में काँसे की थालियों का खनखनाता शब्द खटोले पर पुराने कपड़ों में लिफ्टा नवजात शिशु… ।
क्या इसी दिन के लिए सोनहुआ काकी ने वह पीड़ा सही थी?
*
अम्मा कहती हैं, ‘सोनहुला की भी अपनी जिद है। सोमेश्वर ने कई बार चिट्ठी लिखकर उसे अपने पास बुलाया था, लेकिन वह जाना ही नहीं चाहती। देखो, आखिरी समय तक कौन सी दुर्गति होती।’
मैंने भी काकी से यही सवाल किया था, ‘सोमश्वर भइया ने बुलाया तो आप गई क्यों नहीं, काकी?’
एक लंबी चुप्पी के बाद काकी ने मेरे सवाल का जवाब सवाल में ही दिया था, ‘रानीआ कउआहंकनी में बवनों फरक बा कि ना बचिया? बेटा–पतोह के दुआरि हम कउआहंकनी बने जाई?’
मैं उनकी बात समझ नहीं पाई थी – सोमेश्वर भइया इतने आदर से बुला रहे थे, फिर काकी वहाँ के अपने जीवन की तुलना कौआ हाँकनेवाली के जीवन से क्यों कर बैठीं?
कुछ समझाने के बदले काकी ने सोमेश्वर भइया की चिट्ठीयों का एक छोटा या पुलिंदा सामने कर दिया –
‘अम्मा, तुम्हें गाँव छोड़कर मेरे पास आ जाना चाहिए, तुम बार-बार मना क्यों कर रही हो? यह मत समझना कि यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत है या तुमसे कोई काम लिया जाएगा। तुम्हारी बहू खुद ही बहुत होशियार है। मुझे तो गाँव में अपनी बदनामी की चिंता है। लोग यही कहेंगे कि बूढ़ी माँ अकेली खट रही है और लड़का मौज कर रह है।’
‘अम्मा तुम मेरी बदनामी करवाने पर तुली बैठी हो। सुना है कि लोग तुमको दान किया हुआ साड़ी-कपड़ा दे जाते हैं और तुम हाथ पसारकर ले लेती हो।’
‘छिह अम्मा, मेरे पास नहीं आना चाहतीं, मत आओं, लेकिन तुमने घर का पुश्तैनी टुकड़ा खोरी वाला धंधा शुरू कर दिया, मुझे बहुत अफसोस है।’
काफी चिट्ठियाँ पढ़ते वक्त मेरे चेहरे के उतार-चढ़ाव को र्निमेष देखती रही थीं। फिर उन्होंने एक फीकी हँसी हँसकर कहा था, ‘बताव बचिया, सरधा-परेम से केहू दे जाए त हम कइसे ना लेई? एकरा में कवन बदनामी बा? सगरी जिनगी गाँव में कटुल, अब मरत बेर गाँव के माटी के सहर में बसे जाईं?’
काकी की एक ही साध थी। सोमेश्वर भइया अपनी बहु के साथ साल में दो-चार दिनों के लिए भी कभीआ जाते तो उनकी छाती जुड़ा जाती। लेकिन सोमेश्वर भइया पूरी तरह नाराज हो गए थे। सावित्री ने बताया था कि काकी अपनी पंजाबिन बहू के जापे में पटना गई थीं, लेकिन दस दिनों में ही वहाँ से लौट आई थीं। शहर की जिंदगी उन्हें काल-कोठरी सी लगी थी। उनका दम घुटने लगा था। ‘एहिजा हम अपना मन के रानी बनल रहब बचिया। जब ले जियब, एह जिनगी प हमरे अधिकार रही। गाँव के बेटियन-पतोहियन से हमार मन मिल गइल बा। हम अब कतहू ना जाइब।’
काकी को एक ही पछतावा था; सोमेश्वर भइया काकी को अपनी इच्छा के अनुसार चलाने की जबरदस्ती तो करते रहे, लेकिन उन्होंने उन्हें समझने की कोशिश क्यों नहीं की? “छोटहन बिरवा होखे त दोसरा जगह रोपला पर जड़ पकडि लेई बुढ़वा बिरिछ के सौर एक बेर उखड़ जाए त दोसरा जगह कबहूँ ना लागि सकेला।”
काकी का तर्क भी ठीक ही था। उनकी रुचियाँ, उनकी तमाम इच्छाएँ गाँव की माटी में रम गई थीं। पटना की हवा उन्हें रास नही आती।
मैंने काकी को उस रात बार-बार समझाया था, ‘आप सोमेश्वर भइया की याद में अपनी देह मत घुलाइए। शांति से हंस-बोलकर बाकी जीवन काटिए।’
‘जब तक साँस, तब तक आस, बचिया। कबहूँ ना कबहूँ बबुआ गाँव लवटिहें, एही उम्मीद में जियत बानी।’
पड़ोसी से आती ढोलक की थाप अब शांत पड़ गई है। आनंद की लहरों पर छलकते गीतोंके बोल खामोश हो चुके हैं।
भूख की पहली अनुभूति से फूटनेवाला नवजात शिशू का क्रंदन भी अब नहीं सुनाई पड़ रहा है। शायद उसे माँ के वक्ष से बहते दूध की धार ने तृप्त कर दिया है। मातृत्व की नई गरिमा से आहृादित वह माँ अब भी अपने शिशु को थपकियाँ देकर आश्वस्त करती सुला रही होगी।
*
गाँव से लौटते समय पच्छिम पट्टीवाले खेतों तक सोनहुआ काकी साथ आई थीं धीरे-धीरे लाठी का सहारा लेकर। मेंड़ पर खड़ी काकी ने हाथ हिलाकर विदाई दी थी।
इसी मेंड़ पर चलकर कभी सोमेश्वर भइया गाँव से बाहर गए होंगे। काकी की उम्मीद भी अभी तक सोई नहीं है। पता नहीं, उनके राम अवधपुर लौटेंगे भी या नहीं।
Download PDF (प्रतीक्षा )
प्रतीक्षा – Pratiksha