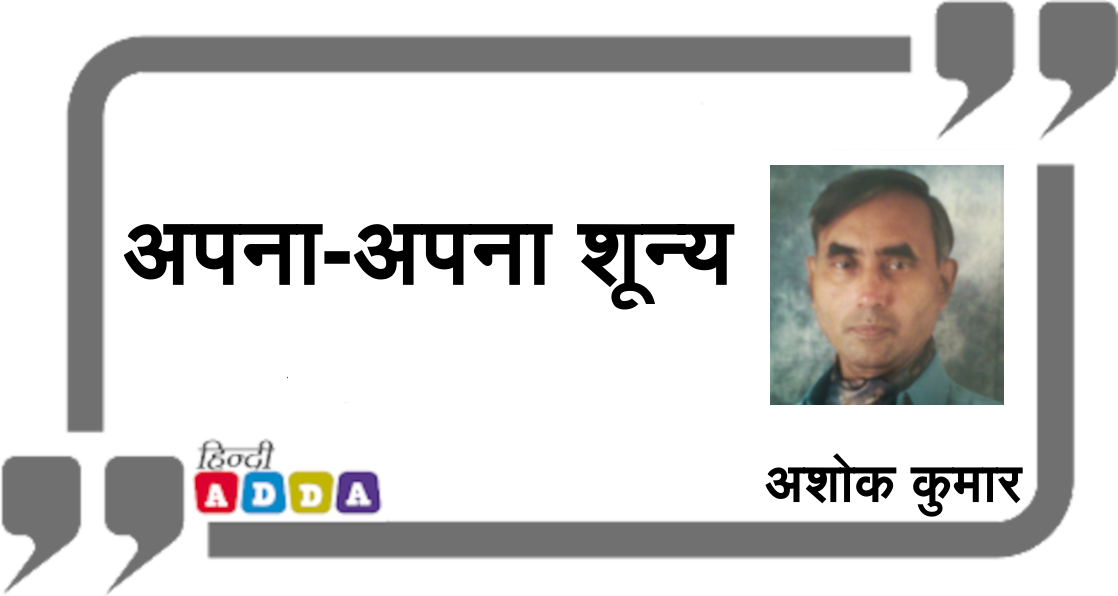अपना-अपना शून्य | अशोक कुमार – Apna-Apna Shunya
अपना-अपना शून्य | अशोक कुमार
प्रकृति अपूर्ण है और पूर्णता की तलाश में भटक रही है। पेड़-पौधे हों, जीव-अजीव हों, इनसान-जानवर हों, कीड़े-मकोड़े हों, अपूर्णता सब में है। हर एक के अंदर एक शून्य है। कुछ खाली है। कमी है। और इसीलिए हर एक को पूर्णता की तलाश है क्योंकि आनंद केवल पूर्णता में है। कष्टों का, दुखों का निवारण केवल पूर्णता में है। हर एक के अंदर की यह अपूर्णता उसके अपने प्रकार की अपनी है और वैसी ही अनोखी है जैसे के उसका अकार या उसका मन और हर एक की यह अपूर्णता, शून्य व्यक्त भी उसकी अपनी तरह अलग-अलग और अपनी अनोखी तरह ही होता है। हर एक का व्यवहार और आचरण उसके इन्हीं शून्यों को भरने की कोशिश है। उसकी अपनी अपूर्णता से पूर्णता की ओर का सफर। आनंद की तलाश, सुख की प्राप्ति, मनुष्य की दैवत्य से तादात्म्य की कोशिश! इत्यादि-इत्यादि…!
जैसे अंकगणित का शून्य एक को लाख और करोड़ बना देता है, अंदर का शून्य लोगों को पता नहीं क्या-क्या करने की ओर प्रेरित करता है और क्या-क्या करने पे मजबूर करता है। सही भी, गलत भी। वैसे भी सही क्या है और गलत क्या है! अंदर का शून्य केवल शून्य होता है। एक वैक्यूम, एक खालीपन। उसका अमीरी गरीबी, इकलौतेपन या रिश्तों के अंबार या सामाजिक यश होने न होने से कोई संबंध नहीं है। क्योंकि ये सब बातें तो वाह्य हैं, शून्य तो अंदर है। मन के सारे क्रियाकलाप तो इस शून्य को भरने के हैं। और मन की भटकन और आकांक्षाओं को अमीरी, गरीबी, यश इत्यादि से क्या लेना देना? और क्या लेना-देना उसका उम्र से! क्या कभी बड़े-बड़ों को समझ में आता है कि वे जैसे हैं वैसे क्यों हैं? जैसा बर्ताव करते हैं वैसा ही क्यों करते हैं? …उम्रें गुजर जाती हैं लोग अपने आपको ही नहीं पहचान पाते। अक्सर लोग खुद अपने व्यवहार, अपने रिएक्शनों से खुद ही चकित रह जाते हैं। फिर दीपक, बाड़ और गोविंद तो बच्चे थे।
झाँसी के नरसिंघ राओ टौरिया मोहल्ले में यूँ समझिए की बस ये तीन ही आठ-दस साल की उम्र के थे और या तो बड़े हो गए थे या बड़े हो रहे थे। तीनों के मकान एक-दूसरे से जुड़े हुए थे। एक तरफ बाड़ का छोटा सा मकान जिसका चबूतरा बहुत बड़ा था। शायद उसकी वजह ये रही हो की उन्होंने उस पर बगैर कुछ बनवाए उसे वैसे ही छोड़ दिया हो। बाड़ के घर की एक दीवार से जुड़ा हुआ गोविंद का मकान था जिसे नाजिर जी का घर कहा जाता था। नाजिर जी का इसलिए क्योंकि गोविंद के ताऊ जी जिनका ये मकान था वे कचहरी में नाजिर रह कर रिटायर हुए थे। उन्हीं के नाम पर इस मकान का नाम पड़ गया था और चला आ रहा था। नाजिर जी के मकान के दूसरी तरफ की दीवार लगी थी दीपक के मकान से जो कि उस मोहल्ले का ही नहीं बल्कि शहर के तीन चार बड़े-बड़े मकानों में से एक था और उसे श्रीवास्तव साहेब की हवेली के नाम से जाना जाता था। तीनों मकानों के दरवाजे एक मैदाननुमा खाली जगह में खुलते थे। वहाँ बच्चे खेलते भी थे और जाड़ों में कभी-कभी बड़े लोग जब आँगन में धूप नहीं आती थी तो कुर्सी डाल कर बैठ भी लेते थे।
आजादी के बाद जिस तरह शहरीकरण ने अपनी जड़ें फैलानी शुरू की उसके नतीजे ये हुए के लोग गाँव से शहर और शहर से और बड़े शहर की ओर पलायन करने लगे। उसी की बदौलत हवेली भी अकेली रह गई वरना इसमें एक बार में पचीस से कम लोगों ने खाना नहीं खाया। अब तो खैर हवेली ही हवेली रह गई है और उसमें रह गए हैं श्रीवास्तव साहेब, उनकी बूढ़ी बेचारी माँ और उनका सबसे छोटा लड़का दीपक। दीपक की माँ उसकी पैदाइश से ही पागल थी सो उनका होना न होना बेकार था। कहते हैं दीपक से बड़ा भाई जब पैदा हुआ था उसके एक साल के अंदर ही वे पागल हो गई थी। इस बारे में भी तमाम किस्से थे कि किसी की नजर लग गई, किसी ने हवेली की खुशियाँ देख कर कोई करनी कर दी… जो भी हो… बहरहाल दीपक और उसके बड़े भाई की पाल-पोस, पढ़ाई-लिखाई सब श्रीवास्तव साहेब ने अकेले ही की। दीपक जब तक पाँच साल का हुआ तब तक उसका बड़ा भाई शहर के बाहर पढ़ने जा चुका था।
दीपक कतई तौर पर अकेला रह गया था। तो स्कूल से आ कर क्या किया जाए? या तो खाली छतों पर दौड़ लगाई जाए या बाहर की खाली पड़ी जगह में गिल्ली-डंडा खेला जाए… बरसातों में तो वो भी नहीं। क्योंकि सारे मोहल्ले के लड़के तो उस दौरान कंचे खेल रहे होते थे और कंचे खेलने पर घर में सख्त मनाही थी। ‘कंचे आवारा लड़के खेलते हैं’ …अच्छा अगर स्कूल कि छुट्टियाँ हों तो? तो क्या करें? …इसलिए होता ये था कि गोविंद, दीपक और बाड़ तीनों आपस के घरों में जब, जैसा मन हुआ तब-कुछ खेलने चले जाते थे।
नाजिर जी घनश्याम स्वरूप सक्सेना का एक छोटा भाई था, श्याम स्वरूप सक्सेना था। इसलिए कि पिछले दस सालों से वो लापता है और है भी कि नहीं ये भी किसी को मालूम नहीं। गोविंद उन्हीं की औलाद था। गोविंद की माँ थी। और जैसे कि तमाम हिंदुस्तानी औरतें हिंदुस्तानी घरों में इन हालात में जी लेती हैं वैसे ही वे भी जी रही थी। बाहर वो ही शिष्टाचार, वो ही रीति-रिवाज, वो ही जैसे सब कुछ ठीक-ठाक है और अंदर…! अंदर क्या है ये शायद वे भी ठीक से नहीं जानती होंगी? क्योंकि अपने बारे में सोचने की न तो कभी पुरातन समाज ने औरत को फुर्सत दी है न ही इजाजत, और दो चार पल उधार जोड़-जाड़ कर अगर उसने अपने हाल का अवलोकन कर भी लिया तो जिन सीमाओं में वो बाँध दी गई थी उन्हें तोड़ना मुश्किल ही नहीं गैर मुमकिन था। बहरहाल… घनश्याम स्वरूप जी अब रिटायर हो चुके थे और घर में मर्दों के नाम पर या तो वे थे या फिर गोविंद! औरतों के नाम पर गोविंद की माँ और उनकी जेठानी घनश्याम जी के औलाद कोई थी नहीं।
नाजिर जी, घनश्याम स्वरूप सक्सेना बड़ी रोबीली पर्सनालिटी के थे। सफेद मूँछें, सफेद बाल, गोरा रंग और जब वे अपनी सफेद धोती और कुर्ते में छड़ी ले कर निकलते थे तो क्या मजाल कि ऐरे गैरें की नजर मिलाने की भी हिम्मत पड़ जाएँ। नाजिर जी दो बार ही घर से निकलते थे। एक सुबह जब वे नरिया बाजार तरकारी खरीदने जाते थे और दूसरे शाम को जब वे किले के मैदान की तरफ घूमने जाते थे। जिंदगी एकदम रूटीन से बे-जलजला-ओ-तूफान चल रही थी कि एक दिन न जाने उनको क्या सूझी घरों के सामने पड़ी खुली जगह के एक कोने में उन्होंने मुनगे का दरख्त बो दिया। जिसने घर के तुलसीघरे में कभी जल नहीं चढ़ाया उसने पेड़ लगा दिया और रोजाना सुबह शाम उसमें पानी देने जाने लगा तो ताज्जुब तो होना ही था। ‘मुनगे का पेड़ है – ‘सक्सेना साहेब ने कहा – ‘फलियाँ आएगी तो सारे मोहल्ले वाले खाएँगे।’ इत्तेफाक से पेड़ जम गया और बढ़ने लगा फिर सावन की फुहारें शुरू हो गई सो पेड़ की परवरिश से फरागत हो गई। लेकिन बस क्वार में पितृ पक्ष खत्म हुए ही थे कि नवरत्रि की दूझ को नाजिर जी ने घर में मधुमक्खियाँ पालने का कार्यक्रम शुरू कर दिया। दिन भर उसी में लगे रहते थे। छत्ता लगा तो उनकी बीवी बेतरह चिल्लाई। ‘मक्खियन से डसवाहो? मार डारहो!’ लेकिन नाजिर जी ने भरोसा दिलाया कि कुछ नहीं करेंगी ये पालतू मक्खियाँ हैं।’ नजरायन के कलेजे को ठंडक जब पहुँची जब शहद निकलना शुरू हो गया। लेकिन उनका चिल्लाना तब फिर शुरू हो गया जब बोतल भर भर के शहद नाजिर जी दुनिया को बाँटने लगे।
‘मुफ्त?’
‘अरे हम पैसा कमाने के लिए थोड़ो किए हैं ये सब… हमको शौक रहा हम कर लिए… बैठे-बैठे क्या करें… और आज तक कभी किसी के लिए कुछ किए हैं क्या?’
इस तरह सक्सेना साहेब अपना खालीपन भरते रहे और जिंदगी काटते रहे।
तीसरा था बाड़-बाड़ डोंगरकर! मराठी थे, झाँसी ग्वालियर और इंदौर तो मराठी लोगों का गढ़ है। यही लोग कभी वहाँ राजगद्दी भी सँभालते थे। या तो पहली वजह से दूसरी रही हो या दूसरी के कारण पहली… इतिहास कौन जाने… और लिखा हुआ इतिहास कितना सच्चा है यह भी कौन जाने! बाड़ के पिता थे, माँ थी और एक छोटा भाई था। उसका घर काफी छोटा था। अंदर जाओ तो एक जरा सा कमरानुमा पड़ता था जिसे चाहे तो पौर कह लीजिये चाहे तो छतरी-चप्पल रखने की जगह। उसके बाद कोई छह सात फुट का जरा सा आँगननुमा और उसके बाद दोनों तरफ एक एक कमरा। छज्जे थे लेकिन छत पे जाने का कोई इंतजाम न था। गर्मियों में ये लोग बाहर खुली जगह में चारपाई डाल कर सोते थे। पिता हनुमंत राव को अन्ना बुलाया जाता था और माँ को आई। खाना-पीना रस्म-ओ-रिवाज सब करीब-करीब महाराष्ट्रियन पद्धति का ही था। करीब-करीब इसलिए क्योंकि अब सब कुछ न तो पूरी तरह महाराष्ट्रियन रह गया था न इस तरफ का ही हो पाया था। कुछ था एक बैलेंसिंग एक्ट! भाषा हालाँकि आपस में अक्सर मराठी ही बोलते थे लेकिन उसका लहजा बाकायदा और बिलकुल हिंदी की तरह ही होता था। बाड़ के यहाँ सब कुछ अपना था। अंदर, बंद, स्वयं में संतुष्ट। दरवाजा बंद किया तो दुनिया से विदा ले ली। इसलिए बाड़ के यहाँ दीपक और गोविंद का जाना कम और बाड़ का इन दोनों के यहाँ आना ज्यादा होता था।
हनुमंत राव की माली हालत कोई खास अच्छी नहीं थी। रेलवे के किसी महकमे में क्लर्क थे। झाँसी रेलवे का जंक्शन था, लोको वर्कशॉप था इसलिए रेलवे यहाँ बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी और ज्यादातर लोग रेलवे के मुलाजिम थे या फिर कचहरी के क्योंकि झाँसी जिले के और आसपास की सारी तहसीलों के दीवानी और सेशन के मुकदमे यही आते थे।
दीपक, गोविंद और बाड़ तीनों ही अपनी-अपनी तरह अपने अंदर कही कांप्लेक्सेस के मारे थे और अकेले थे। लेकिन इनमें से किसी को न इस बात का एहसास था न ये सब समझने की उनमें बुद्धि थी की उनके अंदर की साइकोलॉजी क्या रंग ले रही है और जो कुछ भी ये करते सोचते हैं वैसा क्यों करते सोचते हैं। उम्र होगी कोई आठ-दस साल। जवानी गदराई नहीं थी लेकिन गदराने को तैयार बैठी थी। सबसे ज्यादा गर्मी गोविंद को चढ़ रही थी। वो पहले तो दीपक के नौकर पे हाथ फिराता रहा फिर एक दिन बोला – ‘यार एक दिन आओ दोपहर में, दिखाऊँ तुमको जलवा। ‘दीपक जरा शरीफ किस्म का था, समझा तो नहीं… लेकिन ‘जलवा’ देखने में क्या है! …बाड़ से गोविंद इतना खुला नहीं था। सो गर्मी की दोपहर में एक दिन गोविंद ने दीपक के आने के बाद दरवाजा बंद कर लिया। घर में दोनों औरतें काम निबटा कर जरा लेट रही थी। नाजिर जी दोपहर की नींद ले रहे थे।
‘एय्य्य…!’ गोविंद ने अपने नौकर के बटन खोलते हुए कहा – ‘ये देखो…!’ गोविंद कमर के नीचे एकदम नंगा हो गया। फिर उसने अपने छोटे-से को हिलाया और दीपक से कहा – ‘अब तू दिखा।’
दीपक पहले तो शर्माता, टालमटोल करता रहा फिर उसने अपने जाँघिया के नाड़े को अपने हाथों में थाम ही लिया के ‘चलो हो ही जाएँ। बोला – ‘यार… मेरे एक तिल है यहाँ पर…।’
‘देखें-देखें…’ और गोविंद ने दीपक का नाड़ा पकड़ कर खींच दिया। एक तो था ही, दूसरा भी नंगा हो गया।
हुआ हवाया कुछ नहीं क्योंकि उम्र ही ऐसी नहीं थी कि कुछ हो सकता। न कोई कुछ जानता था। लेकिन गोविंद अक्सर अब दीपक के सामने कपड़े उतार कर अलग-अलग तरह से करतब करने कि कोशिश करता। दीपक को पहले तो कुछ समझ ही में नहीं आता था। मजा भी नहीं आता था… लेकिन गोविंद क्योंकि दोस्त था इसलिए वो उसे इस तरह एक्सेप्ट करने लगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं। पार्टिसिपेशन का तो खैर, दोनों का ही, सवाल नहीं उठता था।
ये सेक्स था भी और नहीं भी था। सेक्स अँग्रेजी भाषा में जना और आजकल सर्व-व्याप्त बड़े महदूद मानी वाला शब्द है। अगर इसके मानी और फैलाया जाए और अगर इसे औरत और मर्द के दर्मियान से उठा कर समझा जाएँ तो दरअसल सारा कुछ इस जग में सेक्स ही है। पूर्णता की तलाश। पूर्णत्व से ही निकलकर अधूरा हो कर, अपने स्रोत की तलाश में भटकता हुआ। एक से दूसरे के प्रति आकर्षण जो केवल नर और मादा ही नहीं बल्कि उससे कहीं ऊपर। शायद अर्धनारीश्वर और पूर्ण-पुरुष कि व्याख्याएँ ही इसे सही रूप में समझा पाएँ। अंदर के मानवीय शून्यों को भरने की तलाश शायद इसी का नाम है। स्थूल रूप से इस गुण को सतही तौर पर सेक्स ही माना जाता है। शायद दीपक और गोविंद अपने-अपने शून्यों ‘लकुनाज’ की भरपाई इस तरह उन्हें भूलने की कोशिश से करते हों! लेकिन ये तो वे जानते नहीं थे।
बाड़ की उदय करंदीकर से ज्यादा पटती थी। दोनों मराठी बोलते थे। उन दोनों का एक दूसरे के घरों में आना-जाना था। बाड़ का उदय के घर में ही ज्यादा वक्त बीतता था। उदय का घर उसी मोहल्ले में तीन मकान छोड़ कर था। उदय के यहाँ जाने के पीछे दो बातें थी। एक कि उदय के यहाँ काफी बड़ा और खुला-खुला आँगन था जिसमें इधर-उधर फूलों के पौधे लगे थे और वो बाड़ के घर के उस छह फुटा टुकड़े से कहीं बड़ा ‘आँगन’ था जहाँ वो दुनिया पर दरवाजा बंद कर के आसमान निहार सकता था। और दूसरी बात थी ज्योत्स्ना! उदय की बहन। ज्योत्स्ना करंदीकर अच्छी खासी लंबी थी। छरछरा बदन, गोरा रंग… लेकिन बस। दाँत उसके जरा-जरा बाहर निकलते हुए से थे। खूबसूरत वो नहीं थी लेकिन उसकी हँसी बहुत बेबाक और दिल से निकलती हुई होती थी। वो बाड़ से बड़ी थी तकरीबन छह-सात साल लेकिन वो बाड़ को अच्छी लगती थी और उसे उसके पास होने में एक अजीब से न बताए जा सकने वाले सुख का अनुभव होता था। अब इसमें कोई मर्द-औरत की बात नहीं थी, क्योंकि बाड़ अभी इस उम्र तक ही नहीं पहुँचा था। लेकिन शायद वो ही बात अपने अंदर के खालीपन को शून्य को भर पाने कि इच्छा…!
जो भी हो! बाड़ घंटों वही रहता। कमरे उस घर में ज्यादा नहीं थे। पानी आँगन में ही चिमनी लगा कर गर्म किया जाता था और नहाना धोना ज्यादातर आँगन में ही होता था। और ज्योत्स्ना को नहाने के बाद गीली साड़ी में लिपटी देख कर बाड़ नजर हटा न पाता था। फिर घंटों अपनी खलवत के तसव्वुर में इस तस्वीर को दोहरा-दोहरा कर देखता रहता।
एक दिन बाड़ वही था। उदय को किसी काम से माँ ने ऊपर बुलाया था। ज्योत्स्ना स्कूल से आई-आई थी। उसने कापियाँ रखी, चप्पल उतारी और हाथ मुँह धोने के लिए साड़ी का पल्लू समेट कर पीठ पर डाला कि पीछे से बाड़ आकर उससे चिपट गया।
‘काय करतोय बाडू…?’ (क्या करते हो बाडू)
‘मला चाँगला वाटता! (मुझे अच्छा लगता है)
‘सोड… सोड मला…!’ (छोड़ो-छोड़ो मुझे)
इतने में उदय के जीना उतरने की आवाज भी आई और बाडू को ज्योत्स्ना को छोड़ना पड़ा। वो नहीं चाहता था कि उसकी ये बात कोई और जान पाए। कभी-कभी बड़े हो जाने पर भी कुछ बातें होती हैं जिन्हें हम किसी के भी साथ शेयर नहीं करना चाहते। कहीं किसी हद तक हर शख्स ‘इंडिविजुअल’ है। ये ‘सोशल एनिमल’ वाली बात तो सोसाइटी को सूट करती है… बहरहाल! बाडू को अपनी समझ में ज्योत्स्ना से प्यार हो गया था। ये बात और है कि उस उम्र और उस जमाने में प्यार के माने भी उसे कितने मालूम थे।
ज्योत्स्ना की सहेली थी गीता निगम। दोनों एक ही स्कूल में दसवें दर्जे में पढ़ते थे। गीता गदराए बदन की भरी-भरी साँवली सी लड़की थी। चेहरा भी उसका गोल-गोल था। कद उसका ठीक ठाक था लेकिन उसकी बनावट कुल मिलाकर उसे करीब-करीब नाटी नहीं तो नाटी होने का भरम जरूर पैदा करती थी। बड़ी-बड़ी, गोल-गोल, काली-काली आँखें, लंबी चोटी में गुँथे घुटनों तक लटकते बाल, तेल पिया चमकता चेहरा और हमेशा साफ सुथरी साड़ी। उस जमाने में सभी लड़कियाँ इस उम्र से साड़ी पहनने लगती थी। गीता जरा फैशनेबुल थी। माँ उसकी थी नहीं। पिता भर थे। बाकी सिर्फ एक बुआ थी जो मऊरानीपुर में रहती थी और तीन-छह महीनों में कभी चक्कर लगा जाती थी। बस! घर का सारा काम गीता करती थी। पिता जी कलक्टरी में हेड क्लर्क थे। सुबह दस बजे साइकिल पर खाने का डिब्बा बाँध कर जाते शाम को साढ़े पाँच बजे वापस आते। रात को गीता पिताजी को खाना खिलाकर खुद खाती और फिर पढ़ने बैठती। दिन में झाड़ू लगाने, बर्तन माजने वाली एक थी जो आती थी। बाकी वक्त गीता का या तो खाली होता था या पढ़ाई में बीतता था या फिर घूमने-फिरने में। घूमने-फिरने का उसे बेहद शौक था। और उसकी चाल में तब और तुर्शी और आँखों में और चमक आ जाती थी जब ‘जै-जै’ इधर-उधर कहीं दिखाई दे जाता।
जै-जै राम शरद! सुडौल, खाया-पिया, दंड पेला कसरतिया बदन, चमकता चेहरा, लंबा कद और ऊँचे सुर की भरी आवाज। अखाड़े और कुश्ती का बादशाह! शहर का मशहूर दादा… क्या मजाल कि कोई उसे सलाम किए बगैर गुजर जाएँ। उम्र में बड़ा हो तो पूछे तो जरूर कि ‘भाई जै-जै, सब खैरियत?’ और जै-जै भी शिष्टाचार से हाथ जोड़कर नमस्कार करे। सब जानते थे कि एक बार जै-जै खिलाफ हो गया तो बेड़ा गर्क! सरिए, फरसे, साइकिल की चेनें, हॉकियाँ, चाकू और भी न जाने क्या-क्या? तमंचे तब तक फैशन में नहीं आए थे। जवानी जोश पे थी। लेकिन कसरतियों का उसूल था कि लड़कियों की तरफ रुझान नहीं रखते थे। इसलिए जै-जै को अंदाजा तो था गीता की नजर का… उसकी नजर भी गीता को देख तो लेती ही थी, लेकिन वो इस तरफ भाव नहीं देता था। गीता को उसके तेवर, इधर-उधर बे-वजह किसी को हड़का देना, दम दे देना बहुत भाता था। गीता अपने ख्यालों में कितनी बार जै-जै के साथ अखाड़े में उतर कर उसे कुश्ती में मात दे चुकी थी। जिंदगी में लेकिन उसे धीरे-धीरे लगने लगा था कि जै-जै किसी लड़की के चक्कर में नहीं आने वाला।
मजा ये था कि इत्तेफाक से अगर जै-जै कहीं किसी ओट में खड़ा हुआ होता या गीता की नजर उस पर न पड़ती तो गीता दिखी नहीं की जै-जै बड़ी जोर से खँखारता और फिर ‘आख-थू…’ यूँ ही… फिजूल… या फिर बड़ी जोर से डकार लेते हुए ‘ॐ-तत्सत्त’ की आवाज करता ताकि गीता उधर मुड़े और उसे एक नजर देख ले। साथी जै-जै के सब जानते थे। गीता की तरफ किसी की क्या मजाल शहर का कोई आँख उठा कर देख तो ले… ‘दद्दा का माल’ जो था… और जै-जै का दिल दोहरा हो कर अखाड़े और दुनियादारी की दुविधा में पड़ा है ये भी सब जानते थे।
‘दद्दा! अब जे तो बताओ के कब तक चलेगा ऐसे?’ मुन्ना ने पूछा। मुन्ना करीबी था, पूछ सकता था।
‘कैसा?’ जै-जै ने समझा मगर फिर भी न समझते हुए बोला।
‘जेई …उतै बे फिर रईं तुमाए लिए और इते तुम खखार रये उनके लिए… तो ये जो ‘ॐ तत्सत’ हो रिया… जे कब तक एसई चलेगा?’
‘चुप बे …साला …लड़की देख के खखारा क्या मैंने?’
‘नई वो तो तुमाये मोह में मच्छर चला गया होगा इसलिए खखारा, लेकिन नैक उनकी भी तो सोचो… बे फिर रईं मीराबाई बनी …तुमाये भजन गाती… उनका क्या होगा?’
‘बहुत मेहनत से बनती है बॉडी बेटा! अखाड़ा, कसरत, दूध, मलाई… ऐंह… क्या क्या नई किया मेंने…! क्या इसलिए?’ जै-जै ने मुन्ना की पीठ पैर धौल जमाई।
‘तो फिर किसलिए? …जे जो बॉडी बनाई, इत्ती बढ़िया बनाई तो किस लिए बनाई? ऐंह…? …ऐसे इ बेकार करने के लिए…? …तो अब बखत आ गया है जिसके लिए बनाई है उसे दे दो… घर बसाओ! कोई काम धंधा डाल लो।’
‘शाबाश बेटा… उसका बाप तो तैयार बैठा है कन्यादान के लिए… लोग ताने देंगे सो अलग।’
‘बाप को तैयार कर लिया जाएगा और रही बात लोगों की सो किस साले में हिम्मत है जो दद्दा के खिलाफ जाए! …आग लगा देंगे झाँसी भर में।’
इतने में बड़े-बड़े गिलासों में मोटी-मोटी मलाई डली लस्सी आ गई और पाँच-छह जितने भी थे साथ में सब ने पी। बात गई आई हो गई। लेकिन गर्मी की शाम में मुन्ना की वो बात जै-जै के जहन में इत्र की खुशबू की तरह घुस गई। कई बार ख्याल आया कि गीता लड़की तो अच्छी है। भरी-भरी! ले जाओ इसको ग्वालियर …वहीं शादी कर लेंगे पंडित बुला के। फिर वापस आए तो कोई क्या कर लेगा। लेकिन बस ये सब वो कभी-कभी सोचता ही रहा।
गीता की जिंदगी का खालीपन उसके सामने आए दिन मुँह बाए खड़ा हो जाता था। अपनी तन्हाइयों में जै-जै का ख्याल बहाना था, सहारा तो नहीं था। इसी आपा-धापी में गीता बारहवीं पास हो गई और निगम साहेब ने उसके लिए शिवपुरी में रिश्ता भी ढूँढ़ निकला। ठीक-ठाक लोग थे। लड़के के पिता दाँत के डाक्टर के नाम से जाने जाते थे। डाक्टर क्या थे… थे कुछ बहरहाल! …एक डिग्रीनुमा भी कुछ उन्होंने अपने नाम के आगे लगा रखी थी बोर्ड पर और दाँत उखाड़ते-बैठाते भी थे। तो डाक्टर हो गए। आजादी के बाद ऐसे तमाम किस्म के डाक्टरों को सनद दे दी गई थी। लड़के ने भी कुछ छह-आठ महीने का दरभंगा वगैरह से कोर्से किया था सो वो भी दाँत का डाक्टर बन गया और बाप की गद्दी सँभालने लगा।
शादी में बरात कोठी कुआँ की धर्मशाला में ठहराई गई। वो जै-जै के इलाके में थी। सो जै-जै और उसके साथियों ने बारातियों की भरपूर सेवा की। सेवा की गई अपने इलाके की लड़की के ब्याह के नाम पर, लेकिन सब जानते थे कि जै-जै के दिल में उसकी मोहब्बत उससे ये सब करवा रही है।
गीता चली गई। जै-जै के तने-तने गठीले सख्त बदन को छूने, महसूस करने के ख्वाब ले कर। जै-जै ने उस दिन विदा के बाद रोज से कम से कम तीन गुना दंड पेले और काफी देर तक बावड़ी में बैठा दूध के कटोरे पे कटोरे डकारता रहा, अकेले। कोई आता तो वो उसे भगा देता।
पिछले दो-तीन सालों में दीपक की आवाज में कुछ भारीपन आना शुरू हो गया था। अब गोविंद से उसका मिलना कम ही होता था। गोविंद के ताऊ जी गोविंद को गणित की ट्युशन पढ़ने भेजने लगे थे। बाडू कभी-कभी आ जाता था वरना दीपक अकेला घंटों छतों पर टहलता रहता कभी झिंझरी पर खड़ा इधर-उधर देखा करता। पतंग उड़ाने का उसे शौक बहुत था लेकिन कभी ठीक से उड़ा नहीं पाया न किसी से उड़ाना सीख ही पाया। उसका बड़ा भाई छुट्टी में आता था, एक आध महीने के लिए, तो वो भाई कम और दूर का मेहमान ज्यादा था। उसे तो ये भी याद नहीं रहता था कि दीपक किस दर्जे में पढ़ता है और जरा-जरा सी बात पे दे दनादन थप्पड़ पे थप्पड़… शायद उसका अपने शून्यों, अपने लकुनाज, को भरने का यही तरीका होगा। इसलिए दोनों में रिलेशनशिप कहने भर को ही थी।
दीपक के पिता उसके अकेलेपन को समझते थे इसलिए उन्होंने उसमें तरह-तरह की किताबें पढ़ने की आदत डलवा दी थी। किताबें उस जमाने में इतनी महँगी भी नहीं थी। उसके बाद दीपक ने खुद अपने आप को पढ़ने और फिर लिखने में समो लिया। कोर्से की किताबों में अलबत्ता उसे कभी दिलचस्पी नहीं रही। फिर और रास्ते खुलते गए छोटे-छोटे मुशाइरे, छोटी-छोटी नशिस्तें, स्थानीय अखबारों में पार्ट टाइम काम, लिखना और उससे सीखना, ऐसे जैसे कोई छोटी सी नाव खुली हवा मैं आवारा, लहरों के साथ रोमांस करती हुई इठलाती – अठखेलियाँ करती चली जाएँ, यूँ ही… लापरवाह… न जाने कहाँ…या कहीं भी! …दीपक को इसमें मजा इसलिए आता था कि वो इस सब में अपने बारे में और अपने से जुड़ी तमाम बातों को भूल जाता था। जीवन का सत्य तो यही है न, आनंद की तलाश। इसी में तो सब भटक रहे हैं फिर चाहे वो गद्देदार कुर्सी पर बैठने की इच्छा हो या ठंडा पानी पीने की या नेता बनने की या फिर कोई और… जिसको जिसमें आनंद मिले! और आनंद अपूर्णता में कहाँ।
वैसे तो शाम को अक्सर दीपक घर पर होता नहीं था लेकिन अगर हुआ तो जैसे ही आरती की घंटी की आवाज आई कि सीधे प्रसाद लेने पूजा वाली कुठरिया में पहुँच जाता था। उसकी दादी करीब अस्सी की तो होंगी या होने आई होंगी लेकिन साहेब जाड़ा गर्मी बरसात, क्या मजाल कि उनका नियम बदल जाएँ? भिनसारे उठती थी। घर का करीब-करीब एक हिस्सा ही उनकी तरफ था। एक आँगन जिसमें वे नहाती थी, उससे लगे हुए दो कमरे, एक दालान जो चौके में जा कर खुलती थी। उसी के बगल में ठाकुर जी के लिए एक कमरा, जिसमें ठाकुर जी का ही सामान रहता था गद्दा, चद्दर, धूप, ऊदबत्ती, कपूर, चंदन, पोथियाँ और भी कुछ-कुछ इधर-उधर का छोटा मोटा। वहाँ किसी का भी दाखिला मना था। छुआ-छूत बहुत मानती थी, जरा चौके में किसी ने कदम रख दिया कि उस दिन वो खाना न खाएँ। वे खुद सुबह-सुबह उठकर पवित्र हो कर सीधे पूजा में बैठ जाती थी। पूजा करीब दो घंटे चलती थी। फिर सीधे उठकर चौके में जा कर चाय बनाएगी, नाश्ता बनाएगी, सारे घर को बुला कर खाने के लिए देगी, फिर खुद खाएँगी। घर में ले दे कर वो ही एक औरत थी। उसके बाद खाने का सारा इंतजाम करेंगी। दाल निकालना, चावल बीनना वगैरह… ताकि जब महराजिन आए तो खाना बना सके।
दोपहर में जरा लेटे तो लेटे नहीं तो पापड़-वापड़ कुछ बनाना हुए तो वक्त कट गया और अगर कोई मिलने-मिलाने आ गया तो फिर तो बस… लेटने आराम करने का सवाल ही नहीं… तब तक फिर चाय बनाने का समय हो गया। वे अक्सर कहा करती थी कि गरीबी बड़ी बुरी चीज है। ‘हमारे पिता के पास पैसा होता तो हम को दोहजु से काहे ब्याहते?’ दीपक के बब्बा से हालाँकि उन्हें कोई शिकायत नहीं थी लेकिन फिर भी उनके दिल में ये ख्याल बराबर बना रहा कि जिस शख्स से उनकी शादी हुई उसकी पहली बीवी मर चुकी थी और वे उसकी दूसरी बीवी थी। बब्बा के मरने के बाद जब भी फुर्सत मिलती सर्दी की दोपहरों में वे रामायण या कल्याण पत्रिका के पुराने अंक ले कर बैठ जाती और एक एक लफ्ज जोड़-जोड़ कर पढ़ने की कोशिश करती। धीरे-धीरे इसी तरह उन्होंने पढ़ना सीख लिया था। शाम को दिया बत्ती के समय उनकी पूजा फिर चलती थी, करीब डेढ़ घंटा। उसके बाद आरती… फिर भोग। वो भोग लेने घर के छोटे-छोटे बच्चे खूब जमा हुआ करते थे। अब तो खैर कोई रहा ही नहीं… दीपक भी बड़ा हो गया। लेकिन जब भी वो घर में होता भोग लेने जरूर जाता। आरती में भी खड़ा होता। ये और बात है कि बाद में दादी जिस हाल में जिस तकलीफ के साथ मरीं वो देखने के बाद दीपक ने फिर कभी पूजा की तरफ रुख नहीं किया और ग्रेजुएशन तक, जब तक वो झाँसी में रहा। यही सोचता रहा कि इतनी पूजा करने का क्या सिला मिला दादी को? …कोई उसे यह नहीं समझा पाया कि पूजा कोई भगवान के लिए थोड़े ही करता है। और क्या हर शख्स रामायण बार-बार, राम कथा जानने के लिए ही पढ़ता है?
उधर गीता के ब्याह के बाद निगम साहेब अकेले भी हो गए थे और जमाने के डर से बेफिक्र भी हो गए थे। कहानियाँ तो उनकी बहुत दिनों से मोहल्ले में घूमती थी लेकिन ठीक से कोई कुछ जानता न था न कह पाता था… अब मौका मिला तो निगम साहेब ने अपने घर में झाड़ू-बर्तन करने वाली को बाकायदा रख लिया। कोई क्या करेगा …बातें करेगा? …पीछे से हँसेगा! हँसे…! निगम साहेब को जो अच्छा लगा उन्होंने किया।
श्रीवास्तव साहेब अपने जमींदार पिता की इकलौती औलाद थे इसलिए प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं लेकिन परोक्ष रूप से, पैसे से, संसाधनों से, लोगों को जोश दिलाने से, आजादी की लड़ाई में बराबर हिस्सा लेते रहे। चंद्रशेखर आजाद, भगवानदास माहौर, मास्टर रुद्र नारायण जैसे तमाम आजादी के सिपाही उनसे छुप-छुप कर मिलते रहते, मदद लेते रहते और अगर कभी जरूरत आन पड़े तो हवेली के पिछवाड़े शरण भी लेते रहते। ये मामला १९४७ के बाद समाप्त हो गया। श्रीवास्तव साहेब खाली हो गए तो बहुत विचलित रहने लगे। लेकिन उनकी पत्नी की बीमारी और बच्चों की परवरिश ने उनके पास कुछ और सोचने का समय ही नहीं छोड़ा। दीपक जब हाई स्कूल पास हो गया और उन्हें लगा कि अब वह बड़ा हो गया है और अपना ख्याल खुद रख सकता है तो उन्होंने हवेली के पिछवाड़े के तीन कमरों को जोड़ कर एक वीथीनुमा बनवा दी और वहाँ खोल दिया एक पुरातत्व का संग्रहालय जैसा और कुछ कुर्सियाँ डाल कर बना दिया एक रीडिंग रूम। ‘संग्रहालय’ में तमाम आस-पास के गाँवों/मंदिरों से लाई गई मूर्तियाँ, पुराने-पुराने सिक्के, डाक टिकट और इस प्रकार के कई और मोनुमेंट्स लाए गए ताकि नई पीढ़ी का इतिहास से संबंध बना रहे। रीडिंग रूम में उन्होंने भारत में अँग्रेजी राज से जुड़ी और अँग्रेजों के भारतियों के ऊपर अत्याचार पर लिखी गई तमाम किताबें और दस्तावेज रखे। इस निजि ‘म्यूजियम कम रीडिंग रूम’ को श्रीवास्तव साहेब स्वयं सुबह नौ बजे खोलते थे और दोपहर के एक बजे तक खुला रखते थे। इसमें आने, देखने, पढ़ने की कोई फीस नहीं थी।
कुछ दिनों बाद जब दीपक ग्रेजुएशन के लिए कानपुर चला गया और उसकी माँ जो अपनी किस्मत के किसी भोग भुगतने के लिए जी रही थी चल बसीं, श्रीवास्तव साहेब और उनकी माँ ही हवेली में रह गए।
आजादी के बाद जिस प्रकार का ‘डेवलपमेंट’ शुरू हुआ उसके चलते झाँसी में नगर पालिका ने खंडेराव दरवाजा तोड़ कर सड़क चौड़ी करने का ऐलान कर दिया। लोगों ने आपस में तो खुसुर-पुसुर करना शुरू कर दिया लेकिन सामने मुखालफत करने की हिम्मत किसी की न पड़ी। श्रीवास्तव साहेब ने सुना तो बोले खंडेराव दरवाजे का तो रानी लक्ष्मीबाई के अँग्रेजों से युद्ध के दौरान बहुत महत्व रहा है। इसे मैं टूटने नहीं दूँगा। सबने सलाह दी ‘काहे इस झंझट मैं पड़ते हो। सरकारी काम है आड़े आओगे तो अंजाम अच्छा न होगा। कोर्ट, कचहरी, मार-पीट, लाठी चार्ज, सजा हवालात कुछ भी हो सकता है और एक बार इज्जत पे आँच आई तो बदनाम।’
श्रीवास्तव साहेब ने नगर पालिका के चेयरमैन से बात की। उसने हँसी में उड़ा दिया। जिस दिन दरवाजा तोड़ने का कार्यक्रम तय था श्रीवास्तव साहेब अपने तीन दोस्तों को ले कर दरवाजे के सामने बैठ गए। बोलो ‘अब तोड़ो!’ अब चार आदमियों को मार कर दरवाजा तोड़ने की हिम्मत तो नगर पालिका में थी नहीं। धमकाया गया, धकियाया गया, समझाया गया, पुलिस बुलाई गई, कलक्टर आया, कमिश्नर आया… लेकिन तब तक इन चारों की देखा देखी शहर के तमाम और लोग भी आंदोलन में जमा होने लगे। जै-जै और उसके साथी भी इससे जुड़ गए और मजमा बढ़ता गया। मामला तीन दिनों तक चला। न वहाँ से श्रीवास्तव साहेब हटे न लोग। अखबारों ने रोज छापा। तब मामला ‘डिस्कशन’ पर आया। मिल कर तय किया गया कि दरवाजा न तोड़ा जाए, दरवाजे के बीचोंबीच एक खंभा और खड़ा करके दो तरफा सड़कें निकाली जाएँ ताकि आवा-जाही भी सुचारु हो जाए और इतिहास की निशानी खंडेराव दरवाजा भी न तोड़ा जाए।
कुछ दिनों बाद इसी खंडेराव गेट के पास हनुमान जी के मंदिर से जरा पहले गोविंद ने सनद मिलने के बाद अपना वकालतखाना खोल लिया था। वकालत भी ठीक ठाक चलने लगी थी। फिर न जाने उसे क्या सनक सवार हुई कि उसने तय किया कि मंगलवार की शाम को उसके पास जो भी मुवक्किल आएगा उसका मुकदमा वो बगैर फीस लिए लड़ेगा।
कुछ दिनों ऐसे चला फिर अचानक वो सब कुछ छोड़-छाड़ कर हरिद्वार जा कर साधु हो गया। कुछ साल पहले बद्रीनाथ से जो पंडा जी आए थे कहते थे कि ‘शायद’ उन्होंने गोविंद को केदारनाथ की तरफ जाते देखा था। लेकिन उसे पहचानना मुश्किल था और दुनिया से अब उसका कोई वास्ता नहीं रह गया था।
किसको किसका शून्य कहाँ और कैसे ले जाए, क्या पता?
Download PDF (अपना-अपना शून्य)
अपना-अपना शून्य – Apna-Apna Shunya