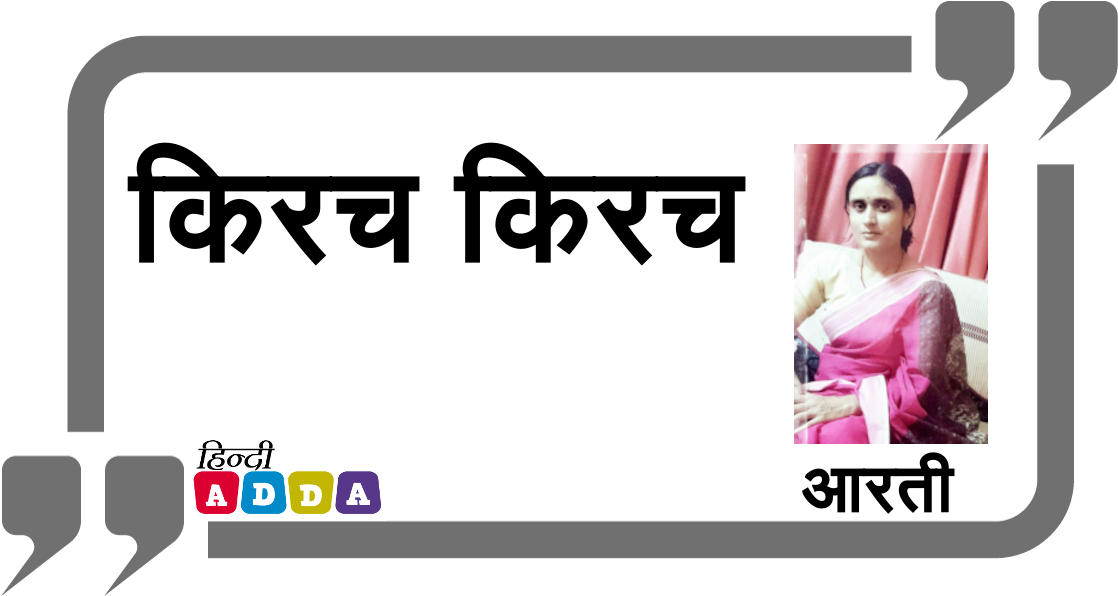किरच किरच | आरती
किरच किरच | आरती
यह सब कुछ काँटों की सेज में सोने जैसा था
फिर भी मैं सोई और
ऐसा लगा कि कई जन्मों तक सोती रही
इन दिनों और उन दिनों भी यही किया मैंने
ना कहना चाहकर भी कहा ‘हाँ’ और ‘हाँ’
मैंने ‘ये’ किया
मैंने ‘वो’ किया
इसलिए कि
सब चाहते रहे ‘यही होना चाहिए’
कुछ विचित्र लगा कि यह सब
भीड़ सा काम करते हुए भी मैं
अलग और विशिष्ट रेखांकित हुई
और वह महीन आवाज जो लगातार गूँजती रही
उसे अनसुना किया मैंने
नासमझ बनी रही
ठेलती और तोड़ती रही खुद को किरच किरच
ये काँच के टुकड़े थे
ऐसे टुकड़े जिनमें न तो प्रतिबिंब दिखता
ना ही आर पार
इन टुकड़ों को समेटती
मेरी पाँचों उँगलियाँ लहूलुहान हुई हैं
और रेशे रेशे बिखरा है मेरा अस्तित्व
इन प्रक्रियाओं से गुजरते जाने
कि निषेध के पाले में खड़ी होने के बावजूद
कोई हुंकार न भर पाने के बाद
मैं दूर कहीं भागकर गुम होना चाहती हूँ
किसी गुफा के अँधेरे कोने में छिपकर
उजास के तिनकों को मुट्ठियों में समेटना चाहती हूँ
दौड़कर किसी पहाड़ पर चढ़ना और चीखना चाहती हूँ
घुस जाना चाहती हूँ उस बियावान में
जहाँ आवाजें हर प्रश्न के उत्तर ढूँढ़ लाती हैं