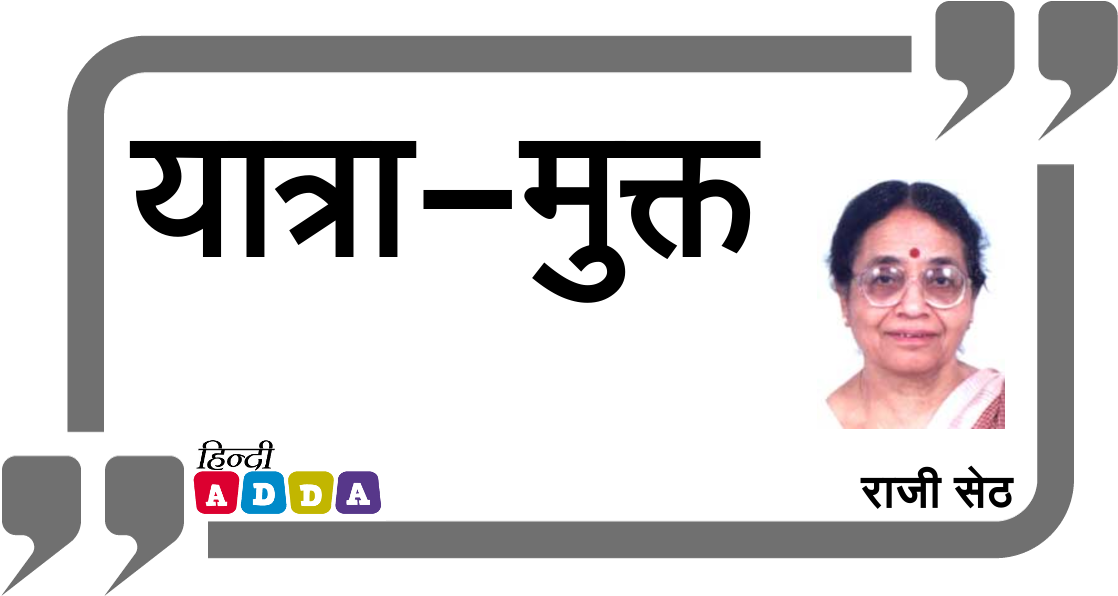यात्रा-मुक्त | राजी सेठ – Yatra-mukt
यात्रा-मुक्त | राजी सेठ
किट्टू…ओ किट्टुआ! आवाज़ भीतर से उठकर हवेली के पिछवाड़े दौड़ती- थरथराती चली आई थी। रात के दस बजे हैं। अस्पताल से खरीदारी करते हुए घर लौटने में देर हो जाती है। अभी वह पढ़ने बैठने की मंशा को उलट-पलट ही रहा था।
इस नाम से उसके भीतर-बाहर आग लग जाती है। किशन नहीं तो ‘किशना’ कह लो, ‘किशनू’ कह लो, पर इस दरबार में किस बात की सुनवाई है। बापू पर झुंझलाओ तो वही एक उत्तार
”मालिक हैं, कुछ भी कहें…क्या फर्ष्कष् पड़ता है!”
क्यों…फर्ष्कष् क्यों नहीं पड़ता? अपने ही नाम को इस तरह तोड़-मरोड़कर हाथ में दे देने का फर्ष्कष् क्यों नहीं पड़ता? हाई स्कूल के सर्टिफिकेट पर लिखा ‘कृष्णचंद्र’ भी उसी का नाम है। पढ़कर लगता है कि किसी के नंगे बदन पर कपड़े पहना दिए हों। अक्षरों पर हाथ फिरा-फिराकर देखता है…वह तो वैसे के वैसे लेटे रहते हैं चुपचाप, पर भीतर कुछ पानी की सतह की तरह द्रवित होकर ऊपर चढ़ने लगता है।
”आगे क्या लगाएंगे बापू?” उसी सपने में डूबते उसने एक दिन बापू से पूछा था।
”आगे क्या का क्या मतलब?”
”मेरा मतलब है…उपनाम…सरनेम? …नहीं समझते? मतलब जात क्या है हमारी?”
”कौन ससुर तू राज-दरबार में बैठा है…जात क्या है हमारी!” बापू ने उसकी नकल बनाते हुए कहा, ”यहां बैठे जून सुधर गई तुम्हारी…तू साला दर- दर…”
बापू ही सब मटियामेट कर देते हैं तो दूसरों से क्या शिकायत!
आवाज़ थी कि सन्नाटे को चीरती फिर से आई थी। एक ख़ास तरह का खुरदरापन उसमें चीख़ रहा था। व्यर्थ सोच रहा था कि खाना टाल जाए। खा लेने पर नींद धर दबाती है, पर अब कुछ नहीं हो सकता। उस आवाज़ को टाला नहीं जा सकता था। उसे सुनकर किसी खिलाड़ी की तरह चूने की सफेद रेखा पर से दौड़ पड़ने की तत्परता उसके खून के स्वभाव से मांगी जाती थी।
भीतर गया। काम कुछ भी ख़ास नहीं। तरुण बाबू को अपनी सोने की चादरें एकाएक गंदी लगने लग गई थीं और वह उन्हें बदलवाना चाहते थे। अभी…एकदम…तुरंत, यह भूलकर कि चादरें हर शनिवार को अपने-आप बदल दी जाती हैं, और आज तो मंगलवार ही था।
वह अब नहीं चूकते…किसी एक मौके पर भी नहीं। घात में बैठे रहते हैं कि कैसे उनकी ही उम्र में उन्हें लांघ जानेवाली उसकी उं+चाई को पीसकर रख दिया जाए। अपने अहं को सेंकने का यह खेल उन्हें पसंद आने लगा हैपुकारना और आदेश लेने को तत्पर खड़ी दासता को अपने सामने खड़ा कर लेना। बड़े मालिक बिस्तर से बंधे हैं। यह हकष् उन्होंने अब अपने को खुद दे लिया है।
वह चुपचाप चादरें बदलता है…तरुण बाबू की उपस्थिति को भूलकर। काम पूरा करके जाने को तत्पर होता है कि एक कठोरता गूंजती है, ”रुको
…बैठो।”
कहां बैठे? उनके पैरों के पास? गलीचे की बाहरी कोर से थोड़ा हटकर? और कोई जगह वहां नहीं है।
”सुना नहीं…मैंने कहा, बैठो…”
स्वर में सीधी खड़ी निर्विकल्प कठोरता। वह पाजामा समेटकर बैठ जाता है।
”इस टेबल के नीचे जो अख़बारों की गड्डियां हैं, उसमें से कपिलदेव की बल्लेबाजी के सारे फोटो ढूंढ़ निकालो…मेरे एलबम के लिए…”
इस तरह का काम? …पढ़ाई का बोझ…रात का यह पहर। भूखे-प्यासे। उसके भीतर जम्हाइयां अकड़ने लगती हैं पर उसकी देह को अपने ही आदेशों को टाल जाने की आदत है। चित्रा ढूंढ़ निकालता है तो तरुण बाबू को वह अपर्याप्त लगते हैं। ‘एक्शन’ के साथ ‘नेरेशन’ भी उन्हें चाहिए। ”नेरेशन…क्यों
…क्यों नेरेशन नहीं समझते? …तुम तो बड़े हेड मास्टर हो!”
यह कील कहां ठोंकी गई है, वह जानता है…बिना आंख उठाए भी जानता है। यह घाव है जो तरुण बाबू के मन में सतत रिसता है। यह वैभव और ऐश्वर्य उनका है…स्वामित्व उनके भाग्य का है पर ये उपलब्धियां और सफलताएं क्यों उनकी नहीं हो पातीं? यह किट्टुआ क्यों सीढ़ी-दर-सीढ़ी लगाकर चढ़ता है और वे? …इस हवेली के उत्ताराधिकारी वे…!
फर्श से उठा तो देखा, तरुण बाबू ने पैर सामने की टेबल पर रख लिये हैं और मुंह के आगे एक अख़बार…जैसे न देखने योग्य वस्तुओं के आगे एक दीवार। खिन्न हो आया।
कोठरी में आया तो पढ़ने बैठने के संकल्प की फूंक निकल चुकी थी और भूख भड़क आई थी। ऐसे में संकल्प को पेट से बांधकर पढ़ने बैठना? …नहीं, इतनी-सी हिम्मत भी उसे उस समय अपने भीतर से गायब मिली…क्या होगा पढ़कर? …पुस्तकों के रास्ते आगे और आगे की सीढ़ियां चढ़ना और बिना भविष्य के शून्य में झूल जाना…इससे तो अच्छा था, वह इन किताबों को ईंट- पत्थर समझता और अपनी हदों से बाहर फेंक देता। इन किताबों ने ही दूभर कर रखी है उसकी ज़िंदगी…न इधर, न उधर। अच्छा रहता, वह भी बापू की तरह…
हवेली ने बापू का लड़कपन देखा, जवानी देखी, अब अधेड़ापा भी देख रही थी। गिरजाघर में ब्याही जाने वाली वधू की पोशाक की तरह उनका लड़क- पन अपनी मां के पीछे-पीछे इन्हीं फर्शों पर घिसटता-पड़ता ख़त्म हो गया था। उनका सपना वहीं तक था। इस आंगन में अपनी मां के पीछे भागते-दौड़ते जवान हो जाना, टहल-सेवा के शऊर सीखना, कचहरी से लौटे मालिक के पैरों को जूतों से खाली करना, शौच के लिए लोटा भरना। चाकरी के नित नए तरीके सोचते रहना और पुकारे जाने पर ‘जी-हजूरी’ का ऐसा मिश्रीनुमा रसायन घोलना कि मालिक को भी आंख उठाकर देखना पड़े।
आठवीं में वह प्रथम आया था और तरुण बाबू फेल हुए थे। मालकिन के इधर-उधर रिसते ममत्व की शह पाकर वह उनके पास जाने की फिराक में ही था कि बापू ने अपनी आंख की कठोर वर्जना से उसे वहीं…उस दहलीज के पास ही खड़े-खड़े सुन्न कर दिया। मालकिन का गिलौरीदान तख्त पर रखते ही लपककर आए और उसकी बांह पकड़कर वापस कोठरी में ठूंस दिया।
”वहां जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई बड़ा तीर नहीं मार लिया है तूने? …जानता नहीं तरुण बाबू का रिजल्ट? कैसा लग रहा होगा मालकिन को…”
वह बुझ गया। नया-नया यहां आया था। नहीं समझ पाता था, क्यों बापू का अपना सुख हवेली के दुख के सामने एकाएक इतना छोटा पड़ जाता है?
बापू को ये सब सवाल परेशान नहीं करते थे। यहांहवेली के बीचोबीच खड़े उनके जिस हिस्से की हवेली को ज़रूरत न होती, उसे बापू अपने लिए भी फालतू समझने लगते।
यह कितनी अजीब बात थी कि अपनी शादी के बाद भी अपने बीवी- बच्चों को लेकर गांव में रहने का अरमान उनके मन में नहीं पनपा था। मां को गांव में ही रख छोड़ा था। हफ्ता-दस दिन में आते…कभी-कभार टिक भी जाते पर सांझ ढले शहर जाने को ऐसे लपकते जैसे अब उन्हें अपने घर लौटने की जल्दी हो।
गांव में रहती मां कभी-कभी हवेली चलने का हठ करती। बापू की सतत अनुपस्थिति ने उसके बचपन को दरजा दे दिया था। वह कोरी कमीज पहनता। …कामदार दोपल्ली टोपी लगाता और मां को लेकर बस के अड्डे चल पड़ता।
बापू उन्हें देखते ही आग-बबूला हो जाते, ”चैन नहीं पड़ती उहां…आ जाते हैं खाने…हियां क्या खाना धरा है? खाकर आए होते।”
यह सब सुनना उसे अखरता। तुरंत कह देना चाहता घर से खाकर चले होने की बात, पर पास घूंघट में बैठी मां चुटकी काटकर उसे बरज देती। बाद में बताती कि खाने के बहाने कुछ देर तो बैठेंगे।
बापू बगलें झांकते मालकिन को ख़बर करते, झेंपे हुए से। एक पैर दहलीज के भीतर एक बाहर, ”वोऽ वो आए हैं। चले आते हैं हियां मरने। हियां क्या खाना धरा है?”
मालकिन खिलखिलाकर हंसती, ”अरे, आए हैं तो खिलाओ-पिलाओ…खातिर करो…।”
पर बापू झींकते-बुदबुदाते रहते। एक काली-सी बटलोई में नमक और चावल डालकर भात पकाते, और खुद गुड़ की डली मुंह में डालकर पानी पी लेते।
”यहां किस बात की कमी है?” मां खीजती।
”कमी नहीं तो हम ही लूटकर खा जाएं,” बापू का तर्क होताहमेशा हवेली के हकष् में झुका हुआ।
मां के मरने पर उसने पहली बार बापू को कई दिन तक घर में रहते देखा थासांझ का धुंधलका…आसमान में ठहरी हुई पीली आंधी की घुटन…कोठे के बाहर दालान में मां ज़मीन पर लेटी हुई…सिर ढका हुआ…साड़ी का पल्लू आंख के पपोटों से नीचा। वह ख़ूब जोर-जोर से सांस ले रही थी। बापू कुछ दूरी पर दीवार के सहारे बैठे ‘सिरी राम-सिरी राम’ का सीत्कार कर रहे थे।
”तनिक हाथ तो दे लाला!” ताई की वह पैनी-सी खीज उसे अभी तक याद है।
बापू उठकर आए तो थे पर ऐसा कुछ करने का शऊर शायद उनके हाथों में नहीं था। टुकुर-टुकुर देखते भर रहे। मां के आखिरी सांस भरने के बाद ही उनका हाथ मां के माथे पर गया। एक बार उन्होंने मां की कलाई पर अपनी उंगलियां फिराईं और फिर चुपके से बांह को नीचे रख दिया।
मां की दाह के बाद वह बापू के आमने-सामने हो गया था। अब तक बीच में एक आड़ थी। उस आड़ में वह बापू को एक बेगानी जिज्ञासा से देखा करता था। वह आड़ अचानक खींच ली गई। सब कुछ उघड़ गया था एकाएक। इस सामने के लिए वह कतई तैयार नहीं था और बापू द्वारा किए इस प्रश्न के लिए तो बिलकुल भी नहीं कि
”क्यों बे, अब तू कहां रहेगा?”
”मैंऽऽ मैं?” ऐसे अछोर आकाश के नीचे खड़ा वह एकाएक रो पड़ा।
बापू शायद पसीज गए, ”मैं तो पूछ रहा था कि तू गांव रहेगा या शहर?”
इस बात का उसके पास क्या उत्तार था। गांव रहेगा तो कहां रहेगा, शहर जाएगा तो कहां जाएगा…पर बापू के सामने कोई ऐसा संकट नहीं था। उनका जीवन एक ऐसा बहाव था जो हवेली की दीवारों को छूते ही खुद एक भंवर बन जाता था।
उसके जीवन का अनुवाद भी बापू ने अपनी तरह कर लिया था। बर्तन- भांडे, कपड़े-लत्तो, हांड़ियां, मथानी, सूप, छलनीसब बांट दिए और उसे लेकर हवेली आ लगे। सिर ऐसा झुका हुआ जैसे उनके कुपुत्रा के बोझ से हवेली की नींवें लड़खड़ाने लगेंगी।
उसे यहां लाकर तो बापू और भी निश्ंचित हो गए। इतना पास बिठाकर तो बिलकुल ही भूल गए। क्यों नहीं सोचते कि वह इन चौहद्दियों, दीवारों और दालानों में क्या करे? यहां न संतू था, न जग्गी, न खेत, न कुएं, न मैदान, न बावड़ियां। यहां न पैर छपछपाने की छूट है, न सिंघाड़ों की छीना-झपटी, न रातोरात ईख की चोरी का आनंद। यहां भीतरी बरौठे से लगी एक कोठरी थी और बापूज़ो मालिक के कचहरी से लौटते ही चाहते कि किशना किशना न रहकर भाप बन जाए। तरुण बाबू उसके समवयस्क थेलगभग दो साल बड़े। उन्हें देखकर पहले-पहल वह ख़ूब उत्साहित हुआ था पर शीघ्र ही समझ में आ गया था कि वह समवयस्कता दूर से दीखती एक टकटकी भर है…एक मनाही
…एक पुख्ता बेदर्द दीवार और अब तक तो अपने परीक्षा-परिणामों से उसने उन्हें और भी नाराज़ कर दिया था।
बस…एक मालकिन थीं…तख्त की चकाचक उजली चादर पर कलफदार साड़ी पहने बैठी वह पान की गिलौरियां उलटती-पलटती होतीं। उनकी चूड़ियां छमछम बजतीं और चेहरा दपदप चमकता।
अपनी कोठरी से निकलकर दालान से जुड़े बरौठे की उं+ची दहलीज के पार वह झिझकता खड़ा होता।
”क्यों रे…वहां क्यों खड़ा है? आ जा अंदर,” वह खुद ही पुचकार लेतीं।
वह बहुत धीरे-धीरे आगे सरकता…दीवार के सहारे। …वैसे बुलाने को न टाल सकने के कारण।
”क्यों रे, तुझे बोलना नहीं आता?”
वह सकपका जाता। करधनी के ऊपर के उनके गुदाले मांस पर गड़ी अपनी आंखें हटा लेता। गुलाबी साड़ी की प्रतिच्छाया की आंच में तपा हुआ उनका चेहरा…वह अवाक् रह जाता।
वहां दिन-प्रतिदिन हड़ियल होती जाती सूखे तन-बदनवाली उसकी मां… इन्होंने ज़रूर कभी ध्यान से उसकी मां को नहीं देखा होगा। देखतीं तो ज़रूर कुछ करतीं। आखिर उसका गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला इन्होंने ही करवाया
था।
बापू नहीं समझ सकते थे कि अपने नतीजे के दिन वह क्यों उनके आस- पास मंडरा रहा था…क्यों? बापू झिड़ककर उसे कोठरी में ठूंस ज़रूर गए थे,पर वह वहां बैठा नहीं रह सका। इस तरह नाकारा-निकम्मा सिध्द कर जाने में उस समय उसे कठिनाई पड़ रही थी…पीले-पीले नतीजे के कार्ड पर इतनी सारी लाल रेखाओं के रहते।
मालकिन बड़ी अलमारी में बने ठाकुरद्वारे के सम्मुख बैठी घी में रुई की बाती भिगोती संध्या की पूजा का जुगाड़ कर रही थीं। उनका चेहरा प्रफुल्ल नहीं है, यह देखकर पहले तो वह भयभीत हुआ फिर…
”सुन रे!…” एक उदास आवाज़ ने उसे टेरा, ”यहां आ…ले!” मालकिन की बंद मुट्ठी उसकी मुट्ठी में खुल गई थी, ”सुना है, तू पहला पास हुआ है
…जा, जलेबी खा ले।”
उसका चेहरा दीप्त हो आया। हठात् उसने बढ़कर मालकिन के चरण छू लिये। मालकिन भर-सी आयीं, ”हां, जा जा! खुश रह…खूब,” एक उसांस उसका पीछा करती रही।
बाहर आकर उसने मुट्ठी खोली। उसमें दो रुपये का मुड़ा-तुड़ा नोट था। एक झनझनाहट-सी उसके भीतर दौड़ गई। यह पुरस्कार उसे मिला हैउसे! बापू के बीच-बचाव के बिना…सीधे मालकिन से…बापू सुनेंगे तो अवाक् रह जाएंगे। उनके आने तक वह जागता बैठा रहेगा। जलेबी खाने भी नहीं जाएगा।
बापू आए तो बेहद घिरे हुए थे। मालिक ने दसवीं में फेल होने पर तरुण बाबू की धुनाई की थी। अपने और उसके भविष्य की अभी से दीखती आहटों की वास्तविकता खोलते हुए तुलना की थी, ”तुमसे तो अच्छा किशना है, लालटेन लेकर पढ़ता है, लेकिन फर्स्ट आया है।”
”तो फिर उसे ही गोद ले लीजिए!” धृष्ट निगाहों से मालिक को घूरते तरुण बाबू छत पर चढ़ गए। मालिक घायल हुए थेभीतर-बाहर दोनों। दुख,विषाद, ताप, क्रोध, चिंता…क्या कोई एक बात रही होगी मन में!
बापू इसी सबको लादे-लादे भीतर आए। अब उसके लिए यह कोई नई बात नहीं थी। बापू हवेली की आंख से हंसते, हवेली की आंख से रोते हैं,जानता था।
कोठरी में घुसकर कुरता खूंटी पर टांग बापू पड़ गए…गुड़ और पानी लिये बिना। इस अभ्यास का टूटना…?
वह दीवार की टेक लगाकर ज़मीन पर बैठा थाप्रतीक्षा करता। पर बापू के चेहरे पर वह दूरी…नहीं, अब वह और प्रतीक्षा नहीं कर सकता था।
”बापू, देखो!”
”क्या है?”
”देखो तो पहले…मालकिन ने दिया है फर्स्ट आने का…” एक गद्गद भाव से उसने नोट को बापू की आंखों के सामने लहरा दिया।
बापू झटके से उठ बैठे, ”क्या? मालकिन ने दिया है?”
”हां! मालकिन ने…खुद बुलाकर…जलेबी खाने के लिए…”
उनका चेहरा लौट आयाउसे साक्षात् सीधा देखता हुआ…उसके सामने बैठे होने को धारण करता हुआ। नहीं तो अब तक…
बापू ने उसे पास खींच लिया, उसके सिर पर सरकता हुआ उनका हाथ गर्दन के पीछे के भाग से चलकर उसके कंधे पर टिक गया। उसे नया-सा लगा
…बिलकुल नया। उसकी गंध या पहचान उसके भीतर नहीं थी कहीं। वह विचलित हो गया।
बापू ने उसे बांहों में भर लिया, ”तू देख रहा है न, तरुण बाबू की आदतों से मालिक को कितना क्लेश है। औलाद आदमी किस दिन के लिए पालता
है…”
बापू फिर खो गए! ‘किस दिन’ के प्रसंग को छूते ही मालिक के साथ हवेली में जा खड़े हुए।
बापू की जकड़ का इस तरह एकाएक शिथिल हो जाना उसे ख़ूब अखरा, पर वह क्षण-भर पहले के छाती भर स्पर्श को ही संजोता बैठा रह गया। इस भरे-पूरे क्षण में वह बापू की उस बेध्यानी को भूल गया और उस स्पर्श को तह करके भीतर कहीं संभालकर रख लिया। नहीं, वह अपने बापू को ऐसे किसी संताप में तपने नहीं देगा। औलाद की उपयोगिता पर प्रश्नचिद्द लगाने वाला मालिक नहीं बनने देगा।
इसी खलबलाहट में उसे देर रात नींद आई थी। दिन चढ़े तक वह सोता रहा। शायद…और भी सोता रहता यदि बापू उसके चेहरे पर टकटकी लगाए उसे उठा न रहे होते, ”स्कूल को देर हो जाएगी बिटवा…”
वैसा दुलार? …और बापू से? …उस सुख को वह आंखें मींचे भोगता रहा।
”तेरे लिए दूध बांध दिया है…अब तेरी पढ़ाई बड़ी हो गई है न? …चल, जल्दी उठ, मुझे जाना है। मालिक उठ गए हैं।”
यह पुल नया था। दो छोरों के बावजूद एक कमान के रिश्ते से सांझा। वह तो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसे क्या नया-नया, भला-भला लग रहा था।
पता नहीं क्यों ऐसा हो गया था…पर हो गया था…। उसके और तरुण बाबू के बीच एक खामोश-सी होड़ छिड़ गई थी। जहां कोई संबंध नहीं था, वहां संबंध बनने लगा थाअाड़ा, तिरछा, काले कलुष के स्वभाव वाला। हार-जीत का गणित रास्ता काटने लग गया था। कोई तुलना नहीं थी…हो भी नहीं सकती थी। तरुण बाबू अंग्रेज़ी तर्ज क़े किसी मॉडल स्कूल में पढ़ते थे, वह सरकारी स्कूल में। उन्हें गाड़ी छोड़ने जाती थी, वह पैदल धूप में तपता जाता था। उन्हें टीचर घर पढ़ाने आते थे, वह लालटेन की रोशनी में…नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं थी, जहां वह और तरुण बाबू एक-साथ खड़े हों, और तुला में पड़ा न्याय उसके हकष् में हो।
हवेली की बातों को लेकर वह हमेशा बापू की आड़ में खड़े रहना चाहता है। फिर भी अकसर एक ठंडा क्रूर किस्म का आमोद उसकी शिराओं में बजने लगता है। बापू की पहुंच और पहचान से परे। बापू उसे देख पाएं तो निष्प्राण कर दें? …छितरा दें…इसलिए वह भरसक बचता है। पूरे मनोयोग से पढ़ाई में लगा रहता है। जानता है, कोई और रास्ता नहीं है तरुण बाबू को पछाड़ने का…मात देने का। ज़रूरी है कि दत्ताचित्ता होकर, इधर-उधर देखे बिना उपलब्धियों के पहाड़ पर चढ़ता चला जाए और चोटी पर खड़ा होकर अपने को दूसरों के देखने के लिए छोड़ दे।
दसवीं में उसकी फिर फर्स्ट डिवीजन आई थी। विद्यालय की तरफष् से ‘सर्वगुण संपन्न’ विद्यार्थी का चमचमाता हुआ एक कप उसे पुरस्कार में दिया गया। आने वाले दो वर्षों के लिए वज़ीफा भी मिला। तरुण बाबू के हमेशा की तरह किसी ‘अदृश्य यत्न’ से नंबर बढ़ाए गए।
बापू प्रसन्न होने की बजाय डर गए। हकलाने लगे। कप को उसके हाथ से छीनकर उन्होंने जाड़ों की गुदड़ी के नीचे ठूंस दिया।
”क्यों बापू?” वह छिल गया।
”रहने दे…रखा रहने दे, वहीं।”
”क्यों, बापू, क्यों?” एक अंधड़ उसके भीतर उद्विग्न हो रहा था।
बापू का चेहरा जैसे घाटी में उतरती धूप की परछाईं, ”…नहीं, बेटा! यह सब किसी से बर्दाश्त नहीं होने का,” कहकर वह तेज़ी से हवेली की ओर चल निकले। कोठरी के अंधेरे में वह खड़ा रह गयाअाहत। अकेला।
बापू उसे खाना देने भी नहीं आए! शायद बचते रहे। महरी के हाथ खाना भेज दिया।
उस शाम वह अकेला पीपल के नीचे बैठा बाहर के बड़े कुएं की चर्खी को निशाना बनाकर पत्थर मारता रहा और बंदरों को मुंह चिढ़ाता रहा। मालकिन को भी अपना कप दिखाने की उसकी इच्छा नहीं हुई…वहीं कहीं उसी गूदड़ के ढेर के नीचे पड़ी सिसकती रही।
बापू क्यों नहीं समझते, इन सब बातों से कुछ नहीं होता? एक नफष्रत उसके भीतर गहरी होती है। अपना ही गला दबाकर दम तोड़ती बापू की खुशी उसके गले पर ऐसी बेरहम खरोंचे छोड़ जाती है जो सतत पड़पड़ाया करती हैं। बापू जिस चीज़ को ढांपते हैं, वह और उघड़ती है। जिसे मिटाना चाहते हैं, वह और गहरी उतरती जाती है।
आखिर किस बात से डरते हैं बापू? अपने को मार सकने की पराकाष्ठा में से उगती पुनर्जन्म की संभावना से? …लगता है, दासता की दलदल में पुश्तों से बैठे वह अपनी कोठरी में उगती उजास से डरते हैं। उतना-सा अपने को मिला हुआ अधिकार भी सह लेने की क्षमता उनके भीतर नहीं है। क्यों वह निचाई के चरम को अपनी पूरी उठान में पा लेना चाहते हैं?
नहीं, ऐसे नहीं चल सकता…आज रात वह बापू से खुलकर बात करेगा। जो कुछ वह नहीं देखना चाहते, उसे समझाएगा। उनके पंगु हो चुके पैरों में ताकत भरेगा। बांह पकड़कर उन्हें इस आंगन के परे ले जाएगा, आत्मा की उस सीलन से परे।
वह पड़ा-पड़ा प्रतीक्षा करता रहा। बापू ख़ासी देर से आए। कमरे में उनके घुसते ही उसने लालटेन की बत्ताी उकसा दीज़ताने के लिए कि वह अभी जाग रहा है।
बापू ने घूरकर देखा पर कुछ बोले नहीं, बल्कि कुरता उतारे बिना दीवार के साथ धसककर बैठ गए, पसीना पोंछते हुए।
”क्या हुआ बापू?”
”कुछ नहीं…टायर बदलने में पस्त हो गया। तरुण बाबू…”
”तुम तरुण बाबू के साथ क्या करने गए थे?” बापू की अधबीच ढांप-ढूंप को उसने उघाड़ा।
”कल दावत है उनके दोस्तों की…पास हुए हैं न? …कुछ सामान लाना था।”
”तुम्हें यह सब अच्छा लगता है, बापू?”
उसे पूरी आशा थी कि वह ‘हां’ कहेंगे, मालिक के प्रति अपनी सदाशयता की दुहाई देंगे, पर वह चुप रहे…थके-थके आहत।
बापू का इस तरह अचानक अपने-आप उसकी पकड़ में आ जाना… ”बताओ न बापू!” वह उस सिरे को छोड़ना नहीं चाहता था।
”अब क्या है…जिनगी कट गई…इस उमर में अब काहे का रोना…”
”हम कहीं बाहर चले जाएं तो?”
कुछ देर खोये-खोये-से वह उसे टोहते रहे, ”नहीं रे…दिल के मरीज हैं मालिक…अब मैं उन्हें छोड़कर कहां जाउं+गा!”
”और भी कोई सोचता है कि वह दिल के मरीज हैं?”
”तभी तो…तरुण बाबू ही कुछ ढंग के होते तो…”
”तुमने ठेका लिया है उनका? उन्हें…”
”उन्हें चाकर ही चाहिए तो बहुतेरे मिलेंगे।” यह कथन उसके मन में तड़फड़ाया पर अपने को रोक गया। चोट किसी और पर नहीं, बापू के मर्म पर पड़ती…चाकरी के खोल के नीचे छिपी उनकी धवलता पर।
”मालिक की चाकरी तक तो ठीक है बापू, पर तरुण बाबू? …सोचो ज़रा, तुम्हारी उम्र का भी उसे कोई लिहाज़ नहीं।”
बापू गुम। चारपाई की पूरी लंबाई में अपने को तानकर कराहते-से। जाने उसे क्यों लगा कि उसके ठहर गए बचपन ने बापू को उस नरक में झोंक रखा है। हवेली अब कोई पहले वाला शीतल प्रवाह नहीं है जिसके किनारे बैठ सब अपने-अपने हिस्से की शीतलता पा लें…उसकी नींव में अंगारे धधकने लगे हैं, पर बापू हैं कि…उनका जुड़ाव दीवारों से नहीं, नींवों से है। वह उन्हीं हादसों से डरते हैं जो हवेली की नींवों को डोला सकते हैं और तरुण बाबू हैं कि दोनों हाथों से नींवों में अंगार भर रहे हैं। कुछ नहीं हो सकता था…बापू को यहां से निकाल कर ले जाने के सिवा…!
कल रात दिल का दौरा-सा पड़ा था मालिक को। कोई उत्तोजना नहीं थी उस समय। प्रकट क्लेश का कोई कारण भी नहीं। पहले अजीर्ण का वहम हुआ था, पर हींग के लेप, चूर्ण और तारपीन की सिंकाई के बाद भी कुछ नहीं बना तो डॉक्टर ने दिल के दौरे का निदान किया था। बापू लस्त-पस्त थे,टूटे हुए… ”यह तो और भी चिंता की बात है। घुन लग गया है मालिक के मन में।”
तीन महीने आराम का डॉक्टरी आदेश। तरुण बाबू को जैसे किसी ने पंख काटकर घर में डाल दिया हो। खाट से लगे पिता…आगतों का तांता…काग़ज़- पत्तार…उन्हें पढ़ाई चौपट करने का बहाना मिल गया। आने-जाने वालों को उन्होंने जल्दी ही ज़ाहिर करना शुरू कर दिया था कि वह इस भाईचारे के कृतज्ञ हैं, परंतु इसके बिना भी चल सकता है। उन्हें और भी ढेरों काम होते हैं, आदि- आदि।
इस तरह सबके हाथ बंटती शाम उन्होंने समेट ली थी और दोस्तों को महफिल जमाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था।
बापू को जैसे किसी ने चारों छोरों से बांध दिया हो, वही टिके रहते हर समय मालिक के आगे-पीछे। मालकिन की अनभ्यस्त हड़बड़ीभरी चिंता को पूरे दिन धीरज से थामे रहते पर कोठरी में आते ही उस आच्छादन को अपने पर घिर आने देते। उस चिंता की गूंजें फिर सारा दिन दीवारों से टकराया करतीं।
”देह में दु:ख हो तो आदमी पस्त पड़ा रहता है पर मालिक? …उनकी देह में कोई घाव नहीं है। उनका मन जख्मी है, मन…समझते हो बिटवा, और ऊपर से तरुण बाबू…सब आने-जाने वालों को टरका दिया…तनिक उनका मन बहलता…”
वह पहले से ही भन्नाया बैठा था। मंगल ड्राइवर ने उसे बताया था कि कल रात तरुण बाबू को महफिष्ल से अलग ले जाकर जिरह-मिन्नत,समझाई- बुझाई में लगे थे बापू कि तरुण बाबू ने उन पर हाथ उठाया था। मंगल बीच में न पड़ा होता तो…
उसे मालिक के प्रति चिंता की इन गुजलकों में कोई रस नहीं…कोई रुचि नहीं। रुचि है बापू में…बापू की मुक्ति में, जो प्रति क्षण जटिल होती जाती थी। उसने बापू की बात का कोई उत्तार न दिया।
कुछ उत्तार न देने से बापू ने बात आगे न बढ़ाई। अपने को खाट के हवाले कर दिया।
वह मन-ही-मन नाराज़ था, अत: पलटकर देखने की ज़हमत नहीं उठायी। लालटेन की रोशनी में सिर झुकाकर पढ़ने का नाटक करता रहा।
‘गट-गट’उन्होंने सुराही से पानी पलटा। पानी पीकर वह वहीं पैरों के बल बैठे रहे। उस तरह उनका बेमतलब बैठे रहना उसे जाने कैसा लगा।
”मांग क्यों नहीं लिया पानी?” उलाहना-सा देते हुए उसने खामोशी को छेदा।
बापू गुम रहे। उठे और लेट रहेअांखें खोले। एक रूठापन चेहरे पर जमकर बैठा।
वह जाने क्यों दहल गया! कौन किससे नाराज़ है और क्यों?
”पैर दाब दूं बापू?” अपने होने को उसने महसूस कराना चाहा और उत्तार पाए बिना अपनी हथेलियों को उनकी पिंडलियों पर टिका दिया।
”नहीं…नऽऽहीं…” एक बहुत कमज़ोर-सी मनाही उधर से उठी फिर निष्प्राण हो रही।
पहली बार लगा, बापू के खून में बहती शांति और आराम को वह स्पर्श कर पा रहा हैदूर तक। बापू तक पहुंच पा रहा हैसीधे। और बापू भी अपने को हवाले किए हैंउसके, अपने बेटे के।
तब से उसके भीतर कुछ तय-सा हो गया। बापू की भाग-दौड़ को उसने अपने सिर पर ले लिया। उनकी तरह सारा-सारा दिन मालिक के कक्ष में जाकर तो नहीं बैठता था, पर असावधान भी नहीं रहता था। फल, सब्ज़ी, दवा-दारू, डॉक्टरसब काम पहल करके करता था और बापू को उस भाग-दौड़ से बचा लेता था। उनका वैसा खटना…धूप में भागते-फिरना…एक पैर घर, एक बाज़ार में रखे रहना उसे अखरता। अच्छा लगता, जब बापू उस सुख को भोगते दीखते
…रीझ-रीझकर…
उन्हें भी पता नहीं क्या हुआ था! किसी बनैले पशु ने अपने सींग उनकी पसलियों में गड़ा दिए थे। उन्हें अब खुद दरारें दीखती थीं। मालिक चित,मालकिन चिंतित, तरुण बाबू आंगन के बीचोबीच एक लठैत की तरह खड़े। एक पल न लगे और लहूलुहान कर दें…रिश्तों और बातों की नज़ाकत को भूलकर।
अब उनके पैर दौड़ते थे बार-बारक़ोठरी की तरफ। लालटेन की रोशनी में सिर झुकाए अपना भविष्य बांचते छोरे की तरफ। एकाध फल या मिठाई का ठौर हाथ पर रखो तो घूरेगा…’कब गए थे?’ …’क्यों गए थे?’ …’जानते तो हो तुम्हारी ग़ैर-मौजदूगी में यहां भूचाल आ जाता है।” वह कब इन बातों की खबर रखता है। …कैसे रख पाता है?
रात लेटते हैं तो उसके हाथ पिंडलियों को आ पकड़ते हैं। पहले ‘न-नुकर’ करते थे आदत के बंधे। यह सब उन्होंने बांटा है, कभी पाया नहीं…अब चुप रहते हैं। पिंडलियों और हाथों के बीच गायब होती जाती पीर की लहरों को महसूसते सो जाते हैं।
बीच रात अंधेरे को घूरती एक टकटकी जाग उठती है। कितना कुछ पीछे से दौड़ता आता एक गोला-सा बनकर छाती में गड़ने लगता है…क्या किया उन्होंने सारी उमिर? जिनगी गला दी। किशना की मां भूखी-प्यासी गई। न उसकी देह देखी, न जीव। तीन-तीन बच्चे अधबने गिरे…वह कहां चेते?क्या सोचा करती होगी मरने से पहले?
दूर पड़ गई बातें फड़फड़ाकर आती हैं और काटती चली जाती हैं अारी की तरह। अब तक क्या किया…मालिक की देहरी पर सिर झुका तो झुका ही रहा। सो तो ठीक, इसका क्लेश मन में नहीं है…पर देहरी और सिर के बीच एक काठ का शहतीर भी है, इस पर उनका ध्यान क्यों नहीं गया…क्यों नहीं!
महरी के लड़के को कोठरी के दरवाज़े के बीचोबीच देख ही उसका माथा ठनक गया। वह लंबी कमीज से अपनी बिना नेकर की टांगें ढांपे वहां बेफिक्र-सा बैठा था और बापू छटपटा रहे थे बेतरह।
दोपहर, पानी की भरी बाल्टी हाथ में लिये कुएं की चीकट पर से पैर फिसल गया था उनका। हल्दी-चूने का लेप…लोगड़ की सेंक…तेल मालिश…कुछ काम नहीं आया। अस्पताल दिखाने गया तो भरती कर लिया गया, ज़रूरी था। दायीं जांघ की हड्डी टूटी थी और बायां घुटना चूर हुआ था। ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है पर उसका फैसला एक बार का पलस्तर खुलने के बाद होगा, डॉक्टर ने कहा था।
एक-दो दिन तो हवेली को बापू का न होना ख़ूब अखरा। अब तक तो वहां के ज़र-ज़मीन को भी उनके तलुवों की आदत पड़ गई थी…पर जल्दी ही यह आसन उसे सौंप दिया गया। बापू न होंगे तो उसे जुतना पड़ेगा, वह जानता था, फिर भी हर समय बापू की तरह घर के आंगन में हिरते-फिरते रहने का हौसला उसमें नहीं। कोठरी में बना रहता और बुलाए जाने पर काम में से खींच लिये जाने का अप्रिय भाव ओढ़ता हुआ हाज़िर होता। मालकिन अनदेखा कर देती। पर तरुण बाबू…अब कोई बचाव नहीं था। अब किशना उनके ठीक सामने थाअपनी निरीहता में भी उनकी अयोग्यता को प्रखर से प्रखरतम कर देने वाला दंश।
घर से चला तो आच्छन्न था। कपिलदेव की बल्लेबाजी के चित्राों के तक़ाज़ों के साथ लिथड़ती आती हिंसा की झुलसन। उसे लगा था कि गई रात इतना समय व्यर्थ न जाता तो टेस्ट में और अच्छे नंबर आते। अस्पताल की ओर पैर रखते ही वह सारा क्षोभ तरोताज़ा हो आया। बापू और हवेली…उसके भीतर कहीं कुछ गड्डमड्ड हो जाता है। वहां लपलपाती हिंसा के लिए दंड दे सकने का एकाधिकार यहां बापू के सामने आकर एकाएक उसके हाथ लग जाता है, पर बापू की इतनी प्रफुल्ल मुद्रा देखी तो गुम हो रहा। वह उसे असाधारण उत्साह से भरे लगे। पिछले दो-तीन दिन तो नीम-बेहोशी और हड्डियां बिठाने की पीड़ा में लस्त-पस्त हुए रहे।
”सुनो बिटुवा,” उनका उत्साह अपने से बाहर बह रहा था… ”यह जो चार नंबर का मरीज है न, इनका मामला तीन साल से कोर्ट में पड़ा है। मैंने कहा, तुम आओगे तो सारा काग़ज़-पत्तार कर दोगे…”
बापू ऐसे कह रहे थे जैसे वह कोई विद्यार्थी न होकर वकील हो और दुनिया में न्याय देने का एकाधिकार उसका हो…
ऐसा गर्व से दपदपाता चेहरा…उसका तनाव छूमंतर हो गया। वह स्टूल पर बैठ गया…बापू की दो अलग-अलग दिशाओं में घूमती आंखोंको देखता। एक आंख उसको देखती थी, दूसरी उसके होने के असर को
दूसरों पर।
बहुत-बहुत भला लगा उसे…बापू का उन छोरों से परे निकल आना, नहीं तो इन सब दिनों वह एक उसी सवाल को हाथ में थामे मिलते थे…
”मालिक कैसे हैं? उनसे मिलकर आए?”
”हां!”
”मालकिन से?”
”उनसे भी…!”
”कुछ कहा?” उनका चेहरा एक टकटकी बन जाता।
”नहीं!” पहले वह झड़प से सच कह देता था, पर कितनी जल्दी बापू की आंखें धुआं-धुआं हो जातीं, चेहरा राख-सना! बाद में वह खुद उस चेहरे के सामने से डरने लगा। तब तक तो बापू ने भी अपने जिज्ञासु हौसले को अपनी जेब में रखना सीख लिया था पर वह नहीं चाहता था कि अभागे मालिक की तरह उसके बापू का मन घायल होता रहे।
अगले दिन वह आते समय अपनी जेब से आधा पाव अंगूर ले आया। बात चलाकर बोला, ”आज मालिक तुम्हें पूछ रहे थे।”
बापू खिल आए। उसके हाथ का लिफाफा झपटकर बोले, ”मालकिन ने भेजा होगा?”
वह चुप रहा। एक-एक अंगूर बापू ऐसे खाने बैठे जैसे दाने-दाने में अमृत- घट संचित हो।
वह परितृप्ति उसे भीतर कहीं छील गई। हवेली से आए झोंकों के इतने आश्रित बापू? उस स्थिति को उसने छितरा देना चाहा। तड़पकर बोला, ”यह मैं लाया हूं तुम्हारे लिए,” और उस डोर को तोड़ दिया।
अस्पताल में यह जो बिस्तर भर स्वतंत्राता थी और उन दोनों के बीच का नरम-नरम आलोक, उसे वह संचित रखना चाहता था। हथेलियों की आड़ देकर …चाहे हथेलियां झुलस ही क्यों न जाएं।
बापू यहां आराम में थे। दर्द की घड़ियों के अलावा परितृप्त। रोटी मिलती थी…फुर्सत और गप्प। आसपास के रोगियों के बीच अपनी उम्र की अधेड़ाई से पाई आधा गज़ उं+चाई। शाम तक तो उनके पास बातों की एक पूरी पोटली जमा हो जाया करती थी जिसे वह उसके आते ही दस्तख़ान की तरह बिछा देने को आतुर मिलते। अच्छा लगता था उसे।
बापू हवेली से कटकर कितना मुक्त हो गए थे! काली चीकट से फिसल कर कहीं और पहुंच गए थेमनुष्यों, संबंधों, दुखों-दर्दों में अचूक तरीके से लप- लपाती जीवन की लालसा के बीचोबीच। कितना अचंभा…कितनी ललक…नई चीज़ों के रू-ब-रू होने का कितना लबालब आनंद…हर समय चाकरी का टोकरा उठाए रहने वाले बापू को वह कितने नए चेहरों में देख रहा था। साथ वाली खाट पर पड़े युवक को पिता द्वारा खिलाने-पिलाने का दृश्य देख वह भीग-भीग आते। रोज़-रोज़ चर्चा करते। चर्चा उनके कौन-से हिस्से को सेंकती है, जानता नहीं था क्या?
अस्पताल पहुंचा तो घिरा हुआ थामाथे के दायीं ओर छोटा-सा घाव। आंखें तनाव से बोझिल। चाहता तो टाल दे सकता था पर ज़रूरत नहीं समझी।
”क्यों रे?” बापू ने जैसे ही खखोला उसने उगल दिया। तरुण बाबू से जो हुआ, वह तो बताया ही, जो नहीं हुआ वह भी बताया।
”तुम्हें नहीं मालूम, ऐसे अटेंडेंट बनाकर क्यों ले जाना चाहते थे मुझे। गोल्फ खेलते पीछे-पीछे दौड़ता आदमी उन्हें पालतू लगता हैउनका कुत्ताा!”
”तुमने क्या कहा?”
”कहना क्या था। मैंने कहा, घर में मालिक पड़े हैं, अस्पताल में तुम पड़े हो, मैं नहीं जाउं+गा।”
”फिर?”
”बोले, ‘अस्पताल में सैकड़ों लोग पड़े हैं, मर तो नहीं जाते।” ”…तरुण बाबू!” मैंने कड़ककर कहा, ”…छोटे मालिक कह।” वह चिल्लाए…और मेरे माथे पर ऐश-ट्रे दे मारी।
”हूंऽऽ।” बापू सोच में धंस गए, ”मालकिन ने कुछ कहा?”
”कुछ नहीं, मुझे इशारा करके वहां से चले जाने को कहा।”
”मैं कहता हूं, तू उसके मुंह क्यों लगता है?”
”मैं मुंह लगता हूं…? …अभी तक तो नहीं लगता था…पर अब लगूंगा
…ऐसी दूंगा बच्चू को…”
”नहीं-नहीं,” वह भयार्त हो आए, ”तुम तो जानते हो, मालकिन, मालिक दोनों उससे बचते हैं, फिर तेरी क्या बिसात!”
”जानता हूं, बचते हैं…क्योंकि बच सकते हैं।”
बापू का चेहरा मलिन हो आया, कातर डरा हुआ, ”न, बिटवा, उनके लिए सारी जिनगी खपा दी, कभी पलटकर नहीं देखा…अब बुढ़ापे में…”
”तुमने ज़िंदगी खपा दी, पर मैं…”
क्षण भर वह चुप हो रहे…, ”हां, किशना, तुम…मेरा क्या है, तुम्हारी ही तो बात है…तू जा…कहीं भी निकल जा…मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा। तू चला जा…मैं सच कहता हूं, कहीं भी चला जा…नौकरी ही करनी है तो कहीं कर लेना…अपनी आंखों से…देख-समझकर। जा, गांव में चला जा, ताऊ के पास…बुरे हैं तो क्या…अपना मारेगा तो छांह में तो फेंकेगा…तू यह सब नहीं सह सकेगा…वह छाती दूसरी थी…तेरी मां का मरना सह गई…तेरा खूंटे से बंधना सह गई…नहीं, नहीं…सोच किशना सोच, जा यहीं से कहीं निकल जा…”
वह आपे में नहीं थे। एक विक्षिप्त उत्तोजना उनके सिर चढ़कर बोल रही थी।
”बस…बस करो बापू!” वह घबरा गया, ”कहां चला जाउं+…पूंजी रखी है मेरे पास? …कैसे चला जाउं+…तुम्हें छोड़कर…तुम तो सारी उम्र मालिक से किनारा नहीं कर सके और मैं तुम्हें छोड़ जाउं+…अपने बाप को? …ऐसी हालत में…तुमने इतना नीच, इतना नालायक समझा है मुझे…” कहकर वह बाहर लपक लिया। उसकी उखड़ी भर्राई, आवाज़ सारी सांझ उनका पीछा करती रही।
एक आंधी उनके भीतर उफन रही है। इन सब दिनों का सुख-चैन किसी ने मुट्ठी में भींच दिया है। हाथ माथे पर जाता है, जैसे वह रुई के फाहे के नीचे लपलपाता घाव किशना के नहीं उनके माथे पर आ चिपका हो। टांग ऊपर स्टैंड से बंधी है…पीठ में करवट न ले सकने की बेबसी…वह उन्हें याद नहीं रहता। यह रुपया भर माथे का घाव सुलगता है…लपटें छोड़ता है…
मन में चैन नहीं। मन हवेली में बिंधा हुआ…किशना…तरुण बाबू…मालकिन…मालिक। एक-एक चेहरा…एक-एक दृश्य साफष् दिखता है उन्हें यहां लेटे-लेटे। कौन किससे क्या चाहता है…कौन किससे कैसा बर्ताव करता है। कौन मारता है…कौन सहता है। वे सबके खून का रंग जानते हैं…नस-नस पहचानते हैं। हवेली की दीवारें भी उनसे बोलती हैं। अब वहां से कुछ नहीं मिलने का…ईंटें-ही-ईंटें…वार-ही-वार…दीवारों का पलस्तर उधड़ रहा है। सब कुछ भरभरा- कर गिरेगा…अब दबेगा किशना…सिर्फ किशना…उन्होंने उसे खूंटे से बांध रखा है…खुद खाट पर पड़े आराम भोगते हैं। खाते हैं…पीते हैं, बतियाते हैं…वह घर में बैठा चोटें खाता है। कराहें उठती हैं, मन की दीवारों पर बजती हैं धमाधम।
कुछ भी तो नहीं पता, वे कब खाट से उठेंगे…उठेंगे तो क्या पहले जैसी भाग-दौड़ हो पाएगी…न हो सकेगी तो कौन उन्हें ढोएगा…हवेली में लपकती आती अंधी आग। किसे जलाएगी…किसे बचाएगी। वह कुछ नहीं कर पाएंगे…खाट पर पड़े-पड़े किशना के माथे की चोटें देखा करेंगे। तू चला क्यों नहीं जाता किशना…भाग क्यों नहीं जाता? तू कहता है, तू मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है…हां, कैसे जा सकता है…
पर…पर मैं तो तुम्हें छोड़कर जा सकता हूं…जा सकता हूं किशना…सच कहता हूं, मैं जा सकता हूं बेखटके…संतोष के साथ…शांति के साथ…कपड़ा इधर से काटो या उधर से…क्या फर्ष्कष् पड़ता है! दोनों छोर अलग हो जाते हैं। नहीं किशना, नहीं…यह मरना नहीं, मुक्ति है। मैं बीच से निकल गया तो सब कड़ियां अलग हो जाएंगी। एक दरवाज़ा बंद हो जाएगा। एक सिलसिला खत्म हो जाएगा…
अपने को वह उस भूमिका में सोचने लगते हैंक्या हो सकता है? यहां बंधे-बंधे…जमादार? …फिनायल? …चाकू? …गले या कलाई की नसें…देखा जाएगा, फिलहाल तो किशना…
एक गद्गद उत्तोजना उनके मन में लहरा गई। वह कुछ कर पाएंगे। किशना को उसका भविष्य दे पाएंगे। उन्होंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। न देखा, न भाला, न दुलारा, न संवारा…मालिक की पीठ पीछे उन्हें ढूंढ़ता-ढूंढ़ता अभागा इसी तरह बड़ा हो गया। …देखा जाए तो उनके पास देने को था ही क्या…एक अपना आप और दूसरा पसीने की गंध से लिखा हुआ गुलामी का इतिहास। इन दोनों में से एक ही चीज़ है जो वे किशना को दे सकते हैं…कहीं तू भी तो इसे आत्महत्या नहीं समझेगा…नहीं समझेगा, न बचवा। इस हत्या का पाप मुझे नहीं लगने का…नहीं, नहीं लगने का मेरे बचवा…तुम जान जाओगे
…ज़रूर जान जाओगे। ख़ूब सारा मोह मेरे मन में है…खूब, खूब। मोह-माया- ममता न होती तो यह सब क्यों…
राहत-सी हुई। जितना सोचते थे, उतनी ही चैन पड़ती थी। भय, ताप, बेचैनी कुछ भी नहीं। उतने मजबूर नहीं हैं जितना अपने-आपको लगते थे…कुछ कर रहे हैं…कुछ तो कर पा रहे हैं!
मन कोमल है…हलका है…प्रतीक्षा में है। किशना आया तो माथे की चोट देखकर इरादे फिर से हरे हो गए भीतर।
”आ जा यहां!” उन्होंने उसे प्यासी लालसा से देखा। खाट पर बिठाया। पीठ पर हाथ फेरा, फिर हाथ थामे लेटे रहे।
किशना इन सब स्पर्शों-संवादों से परे था, बोला, ”बापू, मालकिन ने बुलाया था कल रात…बहुत देर बातें करती रहीं…”
वह हैं कि कुछ भी सुन नहीं रहे हैं…बस देख रहे हैं उसे। जी में आ रहा है…बुक्का मारकर रो पड़ें…उसे छाती से बांध लें और वैसे बंधे-बंधे अपने मरने की कामना करें। उस विकट इच्छा को लेकर मरें तो फिर उसी में जनमेंगे…आगे- आगे तक यह हिसाब चलता रहेगा…
”सुना नहीं बापू?”
”हां, क्या कहती थीं मालकिन?”
वह चकित है। वह पहले वाली हवेली के नाम से चट उठ बैठने की बापू की उतावली कहां गई? बापू कहां खोये हैं? सारे रास्ते वह क्या कुछ सोचता आया था! यह सब बातें कितनी नई हैं…बापू की आंखों में आंसू ला देने वाली। मालकिन ने कहा थातरुण बाबू ने ग़लत किया है…तुम्हें मारा है…वह मूर्ख है, अल्हड़ है…ठीक हो जाएगा…न हो जाएगा तो सब तुम्हारे बापू की तरह किस्मत वाले तो नहीं होते…तू सयाना है, समझदार है किशना…भूल जा। तुझ पर इस समय सबका भार है। मेरा…मालिक का…तुम्हारा…घर का। कहती थीं, वह सब जानती हैं…समझती हैं। कॉलेज की फीस मुंशी के हाथ भिजवा दी है…कुछ दिन छुट्टी की अर्जी भी दिलवा दी है। कहती थीं…उन्हें मुझ पर भरोसा है…तरुण बाबू से भी ज्यादा भरोसा…
”तुम सुन क्यों नहीं रहे बापू?” वह झल्लाया।
”सुन रहा हूं…सिर्फ तुम्हें ही सुन रहा हूं, किशना।”
”मालकिन ने कहा, उन्हें मुझ पर बहुत भरोसा है…तरुण बाबू से भी ज्यादा…तुम्हारे बाद मुझ पर…सिर्फ मुझ पर…”
”तुम क्या सोचते हो?”
‘सोचूंगा क्या…भरोसा है तो ठीक है। पर मैं सच कहता हूं, बापू, मैं इस ममता-वमता के चक्कर में नहीं आने वाला। वह मुझे बांध रही हैं तुम्हारी तरह। मैं नहीं बंधने वाला। तुम्हारे लिए मैं यहां बैठा हूं…सिर्फ तुम्हारे लिए…तुम जब तक चंगे नहीं हो जाते, तब तक बैठा हूं…। जो कहोगे, करूंगा,जैसे रखेंगे रहूंगा, पर यह जान लो, मैं तुम्हें उस जालिम के हाथ नहीं छोड़ने का…तुम्हें साथ लेकर जाउं+गा…तुमने अब तक मुझे बांधकर रखा है,मैं अब तुम्हें बांधकर रखूंगा…छोडूंग़ा नहीं…चलोगे न बापू? …तुमने आज तक कभी मेरी बात नहीं मानी…कभी मेरा मन नहीं रखा…इस बार…इस बार…
उन्होंने किशना का हाथ छाती पर रख रखा था। होठ फड़फड़ा रहे थे। और बंद आंखों की कोरों से पानी चलता चला आ रहा था, छलाछल।
Download PDF (यात्रा-मुक्त )
यात्रा-मुक्त – Yatra-mukt