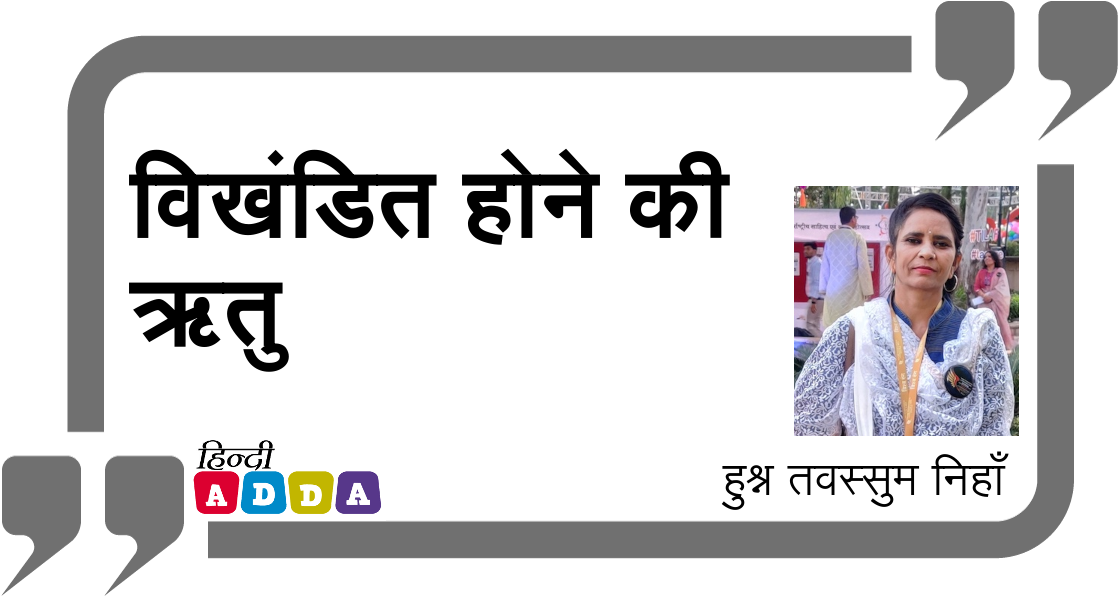विखंडित होने की ऋतु | हुश्न तवस्सुम निहाँ – Vikhandit Hone Ki Rtu
विखंडित होने की ऋतु | हुश्न तवस्सुम निहाँ
आज, उसे जेल की सलाखों के पीछे देख अंतस किसी अव्यक्त पीड़ा से रुंध गया।
पूरे नौ वर्ष बाद हमारी मुलाकात हुई थी। मुलाकात क्या कुछ पल आमने-सामने रहे। एक मित्रा से भेंट करने बनारस आया था। उसी से पता चला अंचल आजकल यहीं की जेल में सजा काट रही है। सुन कर भीतर चींटियाँ-सी रेंग गईं। जीवन-नाट्य के जिन दृश्यों का पटाक्षेप सदैव के लिए हो चुका था वही-वही दृश्य साँप-सीढ़ी की तरह जेहन में उतरते चले गए थे। मेरा रोम-रोम थर्राने लगा था। क्षण भर को जिस्म सूखे पत्ते सा काँप गया। हँसोड़ राज तो ये बात यूँ ही सी कह कर रह गया था और अब पैग पर पैग चढ़ाए जा रहा था। किंतु मैं… ? मेरे भीतर तमाम सुरमई विस्मृत सन्नाटे पंख फटकारते उठ बैठे थे। पूरे वजूद पर एक निढालपन तारी हो गया था।
जो थोड़ा पिया-पियाया था उसका नशा भी काफूर। कहाँ कि मैं वाइन की मस्ती में सोफे पर पड़ा अड़रा रहा था, कहाँ कि हाथों के तोते उड़ गए, ये क्या कह गया था राज
‘यू नो… रोहित… वो तेरी ‘अंचल डॉन’ आजकल यहीं की जेल में चक्की पीस रही है… ।’
कहने को तो वह कह गया था किंतु मैं… ?
मैं नींद आने का बहाना करके उठ कर बेडरूम में चला आया था जो उसके
घर का गेस्ट रूम था। आ कर लेट गया। सामने अंचल ही अंचल नाच रही थीं।
आँखें बंद। सामने धानी पैरहन में सुर्ख चुनरी डाले अंचल। गुलमोहर की छाँह।
पलाशी मौसम। सेमल को छू-छू के बहती हवाओं की स्पर्शिका। हाथों में हाथ लिए-दिए बैठे रहना और बूझते रहना कई-कई रंगोंवाले सवाल। जैसे अंचल थी –
‘तो क्या सोचा तुमने, सावन बन कर आओगे न?’
उसकी लंबी चोटी को सहलाता विमोहक जवाब –
‘बेशक, यदि बरखा बनके तुम मेरी प्रतीक्षा करोगी।’
किसी अनावश्यक किंतु जायज आशंका से वह मगर सहम गई थी –
‘रोहित, कोई-कोई ऋतुएँ हमारे विखंडित होने के लिए ही आती हैं।’
‘हम इन्हें विखंडित होने देंगे तब ना… ! हम इन्हें हैमंतिक गह्वर में भरकर
समेट लेंगे विखंडित होने के लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा… देखना… ।’
‘सच?’
‘हाँ… सच… ।’
मैं सहसा स्वयं ही बोल पड़ता हूँ और आवाज के साथ ही आँखें खोलता
हूँ। अंचल की छाया गायब… ।
सच ही कहा उसने। कोई-कोई ऋतुएँ हमारे विखंडित होने के लिए ही आती हैं। जीवन में कितनी बार खंड-खंड हुआ हूँ… कितनी बार… । वास्तव में विखंडित हुआ कौन… मैं… और कौन! मैं मरा हुआ बिस्तर पर पड़ा रहा। जब जागा तो कमरे में धूप का पीलापन दौड़ चुका था। नित्य-कर्म से फारिग हुआ फिर राज को यहाँ-वहाँ की पट्टी पढ़ा के साढ़े नौ तक घर से निकल गया फिर जिला जेल के लिए बस पकड़ी। रास्ते भर आँखों में अंचल का फूल-पत्तियों से लक-दक वजूद कितने ही कोणों से लश्कारे मारता रहा। उसके गोल चेहरे पे फैलते सुबह के रंगों का तिलस्म अपनी ओर खींचता सा लगता। कितनी सारी उधेड़बुन में मसरुफ था मैं स्वप्निल अतीत की उँगली थामे जाने कब मैं जेल प्रांगण में पहुँचा और जाने किस क्षण वह मेरे सम्मुख थी। जिस क्षण उसे देखा, मेरा आप मुझे धसकता सा नजर आने लगा। कितनी ही वाणियों में सृष्टि धिक्कार बैठी मुझे। बेशक, स्त्री भी एक सृष्टि है… । वह भी रचती है। और मैं था सृष्टि-हन्ता… । पुरुष रचना तो नहीं कर सकता, किंतु रचनाओं को विखंडित करने में उसका जवाब नहीं… आदम… तुसी ग्रेट हो… । कैसी विडंबना थी, मेरे पापों की सजा वह भुगत रही थी। सताई भी गई थी और दंड भी उसे ही मिला था। किसी ने बताया –
‘इन आठ सालों में पहली बार कोई इस महिला से मिलने आया है… ।’
मुझे कुछ चुभ गया जैसे। उसकी माँ तो उसे सजा होते ही चल बसी थीं।
फिर कौन आता उससे मिलने। इस निर्मोही संसार में उसका था ही कौन… सलाखों के पीछे, पूरे मनोबल के साथ मनोभावों में अजब दृढ़ता लिए वह रणचंडी सी खड़ी थी। उसके ऐसे विचित्रा तेवर देख मैं ही सहम गया। हालाँकि शारीरिक रूप से काफी कृशकाय हो चुकी थी, किंतु चेहरे पर तेज ही तेज था। जैसे उसे उसी रोज की प्रतीक्षा थी। और अब वह अविजित थी। अपनी ही राख से पैदा हुई थी ये फीनिक्स अंचल। बालों में सफेदी दौड़ने लगी थी और श्रांति युक्त होंठों पे सयास शाम का उजाला फैल गया जैसे दूर किसी ग्राम्य झोंपड़ी में सँझा-बाती की गई हो।
कुछ गोल-मोल बादल उसके चेहरे पे आ-जा रहे थे। सतत-शून्यता मेरे भीतर एक उत्तप्त-उजास भरती जा रही थी। वह मेघमाला पाँवों में पत्थर बाँधे मेरी जानिब बढ़ती आई थी। मैं स्वयं को सँभाले जा रहा था। उसकी क्षीणता मेरे भीतर घुलती जा रही थी। वह निराला की कविता सी मेरे सम्मुख खड़ी थी। मुझे देखते ही उसकी आँखों में उत्कर्ष की आभाएँ फूट पड़ीं। सचमुच वह विजयी हुई थी जीवन के इस महत्वपूर्ण संघर्ष में। वो संघर्ष जो सदैव नारीत्व व पुरुष अहं के मध्य होता है। और जिसमें नारीत्व का ही हनन होता रहा है। उसी का पतन हुआ है। और उसी को हारना पड़ा है। किंतु वह किसी विशिष्ट किस्म की औरत थी वर्ना मुझ जैसे अहंकारोन्मत्त पुरुष को यूँ जमीन ना चटा पाती। दूसरों पर विजय पाने के लिए अपनी इंद्रियों पर विजय पा लेना नितांत आवश्यक है। और इसी तपस्या में वह खरी उतरी थी। उसने खून किया था अपनी एक-एक भावनाओं का। संवेदनाओं का। इच्छाओं का। और विजय पा ली थी संसार की सारी पौरुषेय मानसिकताओं और विकृत विसंगतियों पर। एक-एक पुरुष के अहं को तोड़ के रख दिया था उसने। उसकी विषाक्त मुस्कान गहराती जा रही थी जो मेरे लिए विष का काम कर रही थी। मैं क्षण-क्षण किसी भावोन्मुख क्लांति में घुल रहा था। रिस रहा था। रिसता ही जा रहा था। उसने जो सजा आठ वर्षों में भुगती थी, वही दंड मैं क्षण भर में भुगत चुका था। उसने सच कहा था –
‘… तुम्हें तो हर दिन सौ बार मरना है, रत्ती-रत्ती मरना है रोहित… ‘
शरीर प्राणहीन हो गया पाँव लड़खड़ाने लगे। मैंने बढ़कर सलाखें मुट्ठी में भींच लीं। किसी घायल पक्षी-सा निढाल… । सलाखों पे सिर टिका दिया। आँखें बंद हो गईं। जिस्म थर्राने लगा। किंतु मेरी आशा के अनुरूप कुछ भी ना हुआ। ना तो वह चीखी, ना चिल्लाई। ना बेवफा कहा… ना विश्वासघाती। मैंने बड़ी मशक्कत से चेहरा पुनः उठाया और धक्क से रह गया। अंचल वहाँ से जा चुकी थी। सामने एक धुंध सी फैल गई। एक किलकारीनुमा चीत्कार भीतर एक पीड़ा उघाड़ गई। रह-रह के झुरझुरी दौड़ जाती शरीर में। उन यातना जनित क्षणों को शब्दों में भी एक बार की अभिव्यक्ति कर पाऊँ तो शायद मुक्त हो जाऊँ। किंतु नहीं, इन शिथिल, अशिथिल लोहित क्षणों की वीरक्तियाँ कभी भी अभिव्यक्ति नहीं पा सकेंगी। और मैं यूँ ही सा भीतर ही भीतर अपने मनोवेगों में रिसता रहूँगा। बहरहाल, मैं कातर हो उठा। निःसंदेह वह जा चुकी थी। अब मुझे उसके लौटते कदमों की खाक में से ही अपना व्यतीत चुनना था। सहसा मैं चौंक पड़ा। संतरी बता रहा था कि मैं मिल चुका। भारी मन से लौट चला। सही कहती थी वह –
‘कोई-कोई ऋतुएँ हमारे विखंडित होने के लिए ही आती हैं… ।’
इस विखंडित होने में वह अकेली कहाँ रही। भले ही अलग-अलग… किंतु जितना वह बिखरी उससे ज्यादा मैं… ईश्वर ने मुझे संतानविहीन बनाकर उसका प्रतिरोध ले ही तो लिया। पत्नी अर्द्धविक्षिप्त होके रह गई। मैं अलकोहलिक। अब यही मेरा ठिकाना रहा। और बस्स। मैं सम्मोहित सा आया और बिस्तर पर ढेर हो गया। सहसा मैं अपने पूर्व वैभव जनित अतीत के संग एकाकार होने लगा। कितने ही अतीतांश मुस्से आ-आ के लिपटने लगे। मानस पटल पर एक-एक चित्रा उभरने लगे… बारी… बारी… बारी… बारी।
मेरे पिता का साड़ियों का व्यवसाय था। विशेषतः बनारसी साड़ियों का। कई-कई शहरों में हमारे साड़ियों के शोरूम थे। इसी प्रसंग में मेरा बनारस आना-जाना लगा रहा थ। हील-हवेल कर पढ़ाई किसी तरह पूरी कर मैं पिताजी के व्यवसाय में लग गया था। माँ मुझे पाँचवाँ साल लगते-लगते संसार से विदा हो चुकी थीं। पिताजी के साए ने ही सारे दायित्व निभाए। दौलत की रेलमपेल थी और मैं पिताजी का सिर चढ़ा। पिताजी के अत्यधिक दुलार, प्यार,कु-स्वतंत्राता और वैभव के खुले आयामों ने मुझसे कई गुना कु-प्रवृत्तियों को जन्म दे डाला था। मैं हद भर घमंडी और स्वच्छंद युवक था। जुनूनी इस कद्र कि क्षण भर में ही इधर की दुनिया उधर कर सकता था। लड़कीखोर इस हद तक कि चार सिरहाने तो दो पैंताने चौबीस घंटे मौजूद मिलतीं। कॉलेज,स्कूल के ही दिनों से दिलफेंकू। कॉलेज तक पहुँचते-पहुँचते ये प्रवृत्ति सिर चढ़कर बोलने लगी। लड़कियाँ मेरी लच्छेदार बातों में चक्करघिन्नी बनके घूमती रहतीं। इस परिप्रेक्ष्य में मेरे कॉलेज की लड़कियों में भी दो-दो गुट बन गए थे। एक वो जिस पर हमेशा मेरी कृपादृष्टि रहती थी, दूसरा वो जिन्हें मैं पास फटकने तक नहीं देता और वे मेरी आगोश में समाने के सपने बुनती भर रह जातीं।
इस मामले में मैं ‘चूजी’ तो नहीं, पर चंट और तिकड़मी जरूर था। मैं हमेशा निचली बस्तियों से आई मध्यम निम्न या निम्नवर्गीय लड़कियों पर ही हाथ साफ करता था। किंतु कहा ना वह किसी विशिष्ट किस्म की औरत थी। मुझे याद आ रहा है। जब पहली और अंतिम बार उसने मेरी वैभवोन्माद में डूबी कोठी में प्रवेश किया था। एक पुलकते अबोध के साथ। वह मेरे सामने खड़ी निरंतर गिड़गिड़ाए जा रही थी।
‘रोहित, तुम इतने पाषाण-हृदय कैसे हो गए। देखो ना… ये तुम्हारा बच्चा…
मेरा बच्चा… हमारा बच्चा… हमारा अपना बच्चा। क्या तुम इसे इसके बाप का नाम नहीं दोगे… क्या तुम चाहोगे कि मैं कलंकिनी कही जाऊँ… ये अबोध समाज का पाप कहा जाए… ?’
बेशक वह मेरा ही बच्चा था। मेरा ही खून था। और अंचल बुरी तरह से छली गई थी… मेरे ही द्वारा। काश! वह मुझमें सुसुप्त असुर को पहचान पाती तो शायद आज इस दुर्भाग्यपूर्ण जीवन जीने से बच जाती… । किंतु उसे मैंने इसका अवसर ही कहाँ दिया था। विधवा माँ की इकलौती संतान, कहाँ तक इस दुरूह और असुरक्षा की स्थिति को झेलती। इस भीड़-भड़कम मुक्त संसार में मेरा रम्य सान्निध्य और संबल पा कर बहुत राहत महसूस की थी उसने। मुझ दुराचारी और व्यभिचारी को देवता समझ बैठी थी वह। और मैं था कि… ।
वह भी क्या करती, केवल दो ही तो कलाएं थीं मुझमें। एक लड़कियों को विश्वास में ले कर उनकी मनोरम संवेदनाओं को किसी रेशमी बाहुपाश में जकड़ लेना। दूसरा वक्त निकाल लेने के बाद उनके भ्रम को छलनी-छलनी कर डालना… । और ज्यादा हो तो दौलत से उनका मुँह बंद करना। किंतु अंचल मेरी सोचों से कहीं आगे निकली थी। मैंने लाखों रुपऐ दे ले कर उसका मुँह बंद करना चाहा और उसने करोड़ों के बीच मुझे नंगा कर दिया। वह बच्चे को ले कर मेरी ड्योढ़ी तक आ पहुँची थी। और वह अंचल ही थी जिसने मेरी कोठी की ओर रुख करने का साहस किया था। उसका ये साहस देख मैं दंग रह गया था। गुस्से से पागल मैं दहाड़ पड़ा था –
‘अंचल, तुम्हें कोठी में घुसने किसने दिया?’
‘रोहित, ये पूछो मुझे रोकने का साहस किसमें है… ?’
वह दृढ़ निर्भीकता से बोली तो मैं स्तब्ध रह गया। वो डरपोक अंचल इतनी साहसी कैसे हो गई… ।
मैं फिर गरजा
‘क्यूँ आई हो… ?’
‘तुम्हारी शराफत आँकने।’ उसने सपाट लहजे में कहा।
‘हुँ… ह… तुमसे किसने कह दिया कि मैं शरीफ हूँ… ।’ मैं कुटिल मुस्कान लिए बोला।
‘तुम्हारे व्यक्तित्व के उत्कर्ष ने रोहित… ‘ चारों ओर एक उड़ती दृष्टि डालती हुई बोली वह…
‘तुम जैसे झूठे मान-सम्मान का मुखौटा ओढ़नेवाले अपने चेहरों पे ना सही पर अपनी दीवारों पे कालिख पुतवाने से जरूर भय खाते हैं… ‘उसकी दबी धमकी पर मैं बिफरा।
‘और तुम उसी भय को हथियार बना इस कोठी में चहकने के सपने देखने लगीं… अपनी चीथड़ों और पैबंद से रची-बसी दुनिया को भूल गईं… कैसे विश्वास कर लिया कि… ।’
‘एक धनाढ्य व्यापारी के घर की बहू बनने का सपना भला कौन लड़की नहीं देखेगी? एक समाज सुधारक, विद्वान और संत स्वरूप व्यक्ति के बेटे पर भला कौन लड़की आसक्त नहीं होगी, उस पर भरोसा नहीं करेगी। वैसे, तुम भूल रहे हो रोहित कि इन चीथड़ों में सेंध हमेशा कोठीवालों ने ही लगाई है। क्योंकि कमल हमेशा कीचड़ में ही खिलते हैं। कोठियों की आबोहवा तो सिर्फ कैक्टस उगाती है… ‘
‘और तुम कैक्टस की झाड़ियों में आश्रय ढूँढ़ने चली आईं… ‘
‘आश्रय नहीं अधिकार कहो। काँटों के बीच पूरे अधिकार के साथ खिल पड़ने का मर्म तुम नहीं समझोगे रोहित।’
‘इंट्रैस्टिंग… , वैसे कहना क्या चाहती हो?’
मैं तप्त निगाहें उस पर चुभाते हुए बोला। उसने उसी दग्ध दृष्टि से मुझ पर प्रहार किया।
‘इसे अपना लो… ।’ एकदम कठोर और तटस्थ स्वर। उसकी इस ढिठाई, सख्ती और साहस पर मैं चकित था। भीतर-भीतर सुलग गया। जी चाहा खींचकर थप्पड़ रसीद करूँ। बड़ी आई अधिकारवाली। ये डब्बे, खोलियाँवाली भी ना। जरा सा मुँह क्या लगा लो कि मर्द को अपनी जागीर समझने लगती हैं। अगर ऐसे ही सैंपुल बटोरता घूमता तो अब तक बच्चों की फौज लिए फिरता। स्… साली… ये लड़कियाँ भी ना पूरी उल्लू होती हैं। क्षणिक-उन्माद को जीवन भर का रोग बना लेती हैं।… अरे, कोई भी सिस्टम अपना लेना चाहिए था। सरकार ने तमाम सहूलतें मुहैया करायी हैं।… मगर नहीं वो तो माँ बनके रहेंगी। मूर्खता खुद करेंगी फिर अधिकार बघारने चली आएँगी। हुं… ह… नाली के कीड़ों का महलों में रेंगना कभी शोभा दिया है। अधिकार ना हुआ, रोटी का टुकड़ा हो गया… , मैं सोफे पर लंबा होता हुआ बोला –
‘लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं।’ मैंने बच्चे की तरफ इशारा किया। मुझमें अराजकता और हेठीपन पूरी तरह व्याप्त था। अंचल के कंपित होंठ भिंच गए।
गहरा निःश्वास छोड़ती बोली –
‘जरूरत तो मुझे भी इसकी नहीं है रोहित।’ लहजे में विष घोलती बोली।
‘तो… ?’ मैं आशंकित सा चौंका।
‘इसे अपना लो।’ बच्चे को इंगित करती बोली। उसने अपनी जिद दोहरायी तो मैं तिलमिला गया। आँखों में संदेह घनीभूत होने लगे। सुषुप्त मनःस्थिति एकदम से सजग हो उठी। अंचल का मस्तिष्क शायद दूने वेग से चलने लगा था। उसके चेहरे पे एक भयावह तटस्थता उतर आई। मैं देख रहा था कि एक ममत्व सुख पा कर ही लड़कियाँ कैसी मजबूत और परिपक्व हो जाती हैं। और उतनी ही मात्रा में उद्दंड भी। वो छुई-मुई सी घोंचू, दब्बू आँचल आज कैसी आँधी-तूफान जैसी घुमड़ रही थी। मैं तो दंग रह गया। उसके एक-एक जुमले पर बगलें झाँकने लगता।
उसका चेहरा अजब-गजब रंग बदल रहा था। आँखों के भाव स्पष्ट नजर नहीं आ रहे थे। होंठ थर्रा रहे थे। फिर भी मैं सँभलता सा बोला – ‘ऐसा नहीं होगा। तुम्हें मेरी प्रेस्टीज का ख्याल होना चाहिए… ।’
कहते हुए मैं सोफे पर ही करवटें बदलते हुए आगे बोला
‘हमारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाना चाहती हो… ‘
उसे धक्का सा लगा। चेहरा पीला पड़ गया। सारे लफ्ज गले में ही अटक गए। आँखों में नितांत खालीपन भर आया। मैं प्रयास कर रहा था उसके चेहरे पे दौड़ती लहरों को पढ़ने का। उसके भीतर से उठते हुए धुएँ में कुछ तलाशने का। मैं सोच ही रहा था कि वह आगे बढ़ी।
‘अगर तुम्हारी प्रेस्टीज का ख्याल करूँ तो इसकी प्रेस्टीज का क्या करूँ?’
कहते हुए उसने बच्चे को सामने पड़ी टेबल पर लिटा दिया। उसकी ये ढिठाई देख मैं चक्कर खा गया। तन-बदन में आग लग गई। आँखों में खून उतर आया। दन से उठा और रिवॉल्वर खींच उसकी ओर तान दिया –
‘मैं कहता हूँ उठाओ इसे… ‘ दहाड़ पड़ा। पूरा बदन गुस्से से काँप रहा था।
बेकाबू होता हुआ चीखता जा रहा था।
‘अंचल… उठाओ इसे… वर्ना एक-एक गोली तुम्हारे भीतर उतार दूँगा – अंचल… ।’
‘अब सिहरने की बारी उसकी थी। चेहरा फक्क। आँखों में बादल मंडराने लगे। शरीर कोमल बेल की तरह काँपने लगा। सारी हेठी हवा हो गई। एकदम मरियल। भीगी बिल्ली। सहमी-सिमटी। हालाँकि क्षण भर को उसे ले कर मन में एक आर्द्र धारा रेंग गई थी। उसकी इस निरीहता ने कहीं-ना-कहीं मुझे हॉन्ट जरूर किया था। मन के कयास में एक सहानुभूति या दया का भाव जरूर जागा था। उस एक क्षण को खुद से घिनाया था मैं। अपनी ही छत के नीचे एक अबला पर मैं बंदूक ताने खड़ा थ। प्रेम के मनोहारी क्षितिज पर मैं खंजर लिए खड़ा था। अगर वह मुझे कायर कहती तो बुरा क्या था? वह निष्कलुष व बेबस सी खड़ी थी। बेशक मैं भीगा था एक क्षण को। किंतु नहीं। मेरी जरा सी भी आर्द्रता उसके भीतर दबी चिंगारी को हवा दे सकती थी। मेरी जरा सी भी कमजोरी मेरे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती थी। उसका दबा हुआ विद्रोह जाग उठा तो… ?
नहीं-नहीं मैं अति संवेदनशीलता में अपना ही गला स्वयं नहीं काट सकता था। भावुकता जी का जंजाल बन सकती थी। फिर मेरे लिए ये कोई रेअर केस तो था नहीं। मैं संवेदनाएँ दबा ले गया। प्रतीत हुआ वह एकदम से हार चुकी है। या हरा दी गई है। लगा ढह जाएगी। मैं पुनः रिलैक्स होते हुए रिवॉल्वर टेबिल पर डाल सोफे पर पड़ रहा। अंचल भी शायद सँभलने का प्रयास कर रही थी। मुझे लगा एक कातर निगाह से उसने मुझे देखा। ऐसा लगा ऐन बरखा में ही किसी हरकते वृक्ष को जड़ समेत उखाड़कर फेंक दिया गया हो।
मैं अपनी मनोवृत्ति के चलते विवश था। भावावेश में कोई भावुक कदम उठा कर भयंकर भूल करना नहीं चाह रहा था। भावनाओं का अतिक्रमण हालाँकि जीवन भर करता रहा। किंतु भावावेश में बहना ही नहीं सीख पाया। बहरहाल उसकी निर्दोष भावनाओं और बेलाग समर्पण का मान भर रखने को इतना ही झुका ‘मेरा अंतिम निर्णय यही है अंचल, तुम इसे ले कर यहाँ से चली जाओ। मैं तुम दोनों को खर्च महीना वार भिजवाता रहूँगा। शर्त ये कि तुम इस रहस्य को रहस्य ही रहने दोगी। आगे तुम्हारी मर्जी… ‘
मैंने पैतरा भांजा।
यक-ब-यक क्या हुआ कि उसके मुखमंडल पर उजास फैल गया। आँखें दमक उठीं। गहरी साँसें खींची। मानो प्रारब्ध पर ही सब कुछ छोड़ निश्चित हो लेने का प्रयत्न कर रही हो। स्वयं को भरसक सँभालती हुई कंपित भावों से आगे बढ़ी ‘ठीक है’ कहती हुई वह बच्चे की तरफ बढ़ी। मुझे संतोष हुआ,रिवाल्वर सफल हुआ। लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। आँखें मूँद के इत्मीनान की साँस लेते हुए सोफे पर पड़े-पड़े मैंने भरपूर अंगड़ाई ली। मन हर्षातिरेक में झूम रहा था। जैसे कोई जंग फतेह कर ली हो। चेहरा हल्की स्मित से महक गया था। मैं बस, जीत ही गया था, किंतु अगले ही क्षण हठात् उछल पड़ा। बच्चा नहीं, वह तो रिवॉल्वर उठाने बढ़ी थी। आँख झपकते ही उसने मुझ पर रिवाल्वर तान दिया। मैं बौखला गया।
‘अ… अंचल… म… मुझे मारोगी… !’
‘नहीं रोहित, इतनी आसानी से तो भले लोग मरते हैं। तुम्हें तो हर दिन सौ बार मरना है। रत्ती-रत्ती मरना है… ‘
मैं बुरी तरह काँप रहा था। हेकड़ी मेरी धरी की धरी रह गई। वह चिल्लाई।
रोहित, इस नामुराद की जरूरत ना तुम्हें हैं ना मुझे, और जिस चीज की जरूरत किसी को ना हो उसे खत्म ही कर देना चाहिए। उसका संकेत बच्चे की तरफ था। उसकी मंशा से में काँप गया।
अमरीकी कहावत है ‘मुहब्बत में नाकाम औरत के इंतकाम से शैतान भी डरता है।’
अंचल में वही औरत उतर आई थी। कुछ भी कर गुजरने को उतारू। मैं साहस करके बोला
‘अ… अंचल… ये तुम्हारा बच्चा… ‘
वह फट पड़ी।
‘बच्चा होगा तेरा, मेरे लिए तो अभिशाप है। कलंक है। तुम राक्षस लोग… लड़कियों को छलने में माहिर होते हो। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल मत लगाना कि मुझ जैसी लड़कियाँ तुम राक्षसों के छलवों को उम्र भर ढोएँगी।… मिस्टर रोहित तुमने मुझे छला है। और मैं तुम्हारे इस छलावे का खून करूँगी।’
उसकी आँखों से वाकई खून टपका आ रहा था। मैं बुरी तरह थर्रा रहा था।
मैंने पुन साहस किया – ‘अंचल… तुम्हारे सीने में माँ का दिल… ‘
पर मैं अपनी बात पूरी ना कर सका।
‘शटअप… ‘
वह चीख रही थी
‘इसी कोमल हृदय के हाथों औरतें छली जाती रही हैं आज तक। सृष्टि ने हमें माँ का दिल दिया है और इसी दिल ने हमें तिल-तिलकर जीने और मरने को मजबूर किया है। मगर रोहित मैं अपने दिल से वात्सल्य का कण-कण निकाल चुकी हूँ। मैं खून कर चुकी हूँ अपने हृदय का। अपने मातृत्व का। अब मुझे केवल तुम्हारे हृदय की चिंता है।’
वो घायल शेरनी उबल रही थी और मैं बौखलाया सा सोच रहा था ‘ये क्या हो गया… पासा ही पलट गया।’ मैंने उसका ध्यान तोड़ने के लिए हल्की सी हरकत की और उसी क्षण एक झन्नाती गोली मेरा दायाँ पैर चीर गई। हमेशा साथ भरी बंदूक रखने की हनक आज मेरे ही काम आई। मैं दर्द के मारे चीखकर सोफे पर ढुलक गया, किंतु दूसरे ही क्षण सँभलते-सँभलते दायाँ हाथ फुर्ती से बच्चे की तरफ बढ़ाया, किंतु छू भी नहीं पाया था कि हॉल एक हृदय विदारक चीख से गूँज गया। दीवारें कराह उठीं सृष्टि तड़प उठी। वो मेरी अपनी ही चीख थी जो रिवॉल्वर की आवाज और अंचल की दहाड़ के साथ और भी भयावक हो उठी थी। बच्चा खून से लथपथ पड़ा था। अंचल गिरकर बेहोश हो गई थी। रिवॉल्वर दूर जा गिरा था। कोई-कोई ऋतुएँ हमारे विखंडित होने के लिए ही आती है। इसका मर्म उस दिन समझ में आया। तबसे विखंडित ही होता रहा।
बहरहाल मैं काँपते, कराहते और लँगड़ाते हुए फोन की तरफ बढ़ गया और डायल करने लगा वन जीरो जीरो।
Download PDF (विखंडित होने की ऋतु)
विखंडित होने की ऋतु – Vikhandit Hone Ki Rtu