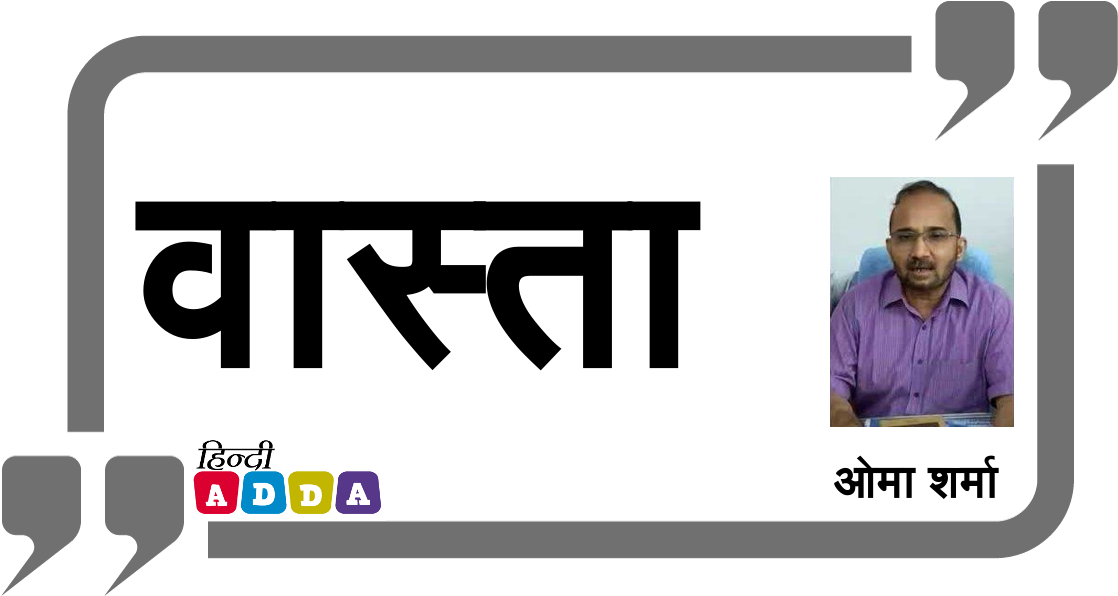वास्ता | ओमा शर्मा – Vasta
वास्ता | ओमा शर्मा
भाई कोई कुछ भी कहे, अपना खून अपना ही होता है। अब सुखदेव भैया को ही लो। कोई सोच सकता था कि ग्यारह साल बाद वो यूँ घर आ धमकेंगे? बिना बुलाए। सुबह ही सुबह।
मगर तुमने कब से टैगोर की धजा धर ली सुक्खू भैया जो बिलाँद भर की दाढ़ी ताने फिर रहे हो छाती पर। बायीं आँख के ठीक नीचे गेरुआ मस्सा यथावत नहीं पसरा होता तो एकबारगी मैं ही उन्हें पहचानने में गच्चा खा जाता। लाज बच गई। शुक्र है, दरवाजा मैंने ही खोला, लीना ने नहीं।
‘सुक्खू भैया तुम!’
अकस्मात मेरी आँखें फैल गईं।
कोई दूसरा बिसरा परिचित होता तो मेरे मुँह से ‘तुम’ निकलता?
‘हाँ भाई मैं… क्या नहीं हो सकता?’ भैया कुछ मजे लेते से मुस्कराए। सुखद आश्चर्य दे देने के मलिन से गुमान से लैस।
बात बढ़ाने का मौका था नहीं इसीलिए तो उनकी तोहमत को ‘आओ आओ’ में हिलगाकर उन्हें अंदर ले आया – अपने ‘स्टडी’ में जहाँ सुबह का अखबार अधखुला पड़ा था। उन्हें पानी दिया, हालचाल लिया और बतियाने के लिहाज से सामने बैठ गया।
‘हिंदी का भी मँगाते हो जयदेव या ये ही है बस।’
उनके सवाल ने मुझे चौंकाया। मैं तो खैर अखबार पढ़ने में लगा ही हुआ था मगर सुक्खू भैया तुम क्या इतने दिन बाद मेरे यहाँ हिंदी का अखबार बाँचने आए हो। और ये जयदेव-फयदेव क्या है? सीटू के अलावा तुम्हारे लिए मेरा कोई दूसरा नाम था? खैर, अंग्रेजी अखबार को उन्होंने आदतन छुआ भी नहीं। सोफे से उसे एक तरफ समेटकर, बिना नजरें मिलाए लगभग अपने आपसे कहने लगे, ‘भाई रे भाई, कितनी किताब इकट्ठी कर रखी हैं। है कोई हिसाब!’
मैंने कोई प्रतिवाद नहीं किया तो चुहल करते से बोले, ‘तूने सारी पढ़ रखी हैं या धूल जमाने के लिए रख छोड़ी हैं।’
‘अब नौकरी ही पढ़ने-पढ़ाने की है भैया तो किताबें तो जमा होंगी ही। सारी तो मेरी हैं भी नहीं। आधी तो लीना की होंगी, सोशयोलॉजी की।’ मुझे कहना पड़ा।
‘बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं।’
उन्होंने एक टटोलती-सी निगाह मेरे वजूद पर फिराई। अभिप्राय लीना से था।
‘सुबह का कॉलेज होता है उसका। आज थोड़ा जल्दी निकल गई क्योंकि एग्जाम्स चल रहे हैं। ग्यारह-बारह तक आ जाएगी। बच्चों का स्कूल भी सुबह जल्दी का है। वैन से जाते हैं।’ मैंने भरसक सिलसिलेवार कहा।
‘बच्चे कौन-कौन-सी क्लास में आ गए… बड़े हो गए होंगे?’ कहते हुए भैया किसी अपराधबोध में लजा से गए।
मैंने तफसील से बताया और पूछा, ‘चाय लेंगे या दूध?’
‘तू खुद बनाएगा’ यानी चाय पी लेंगे।
‘उसमें कौन बड़ी बात है!’ दोनों लोग वर्किंग हों तो घर-गृहस्थी के छुटपुट काम तो आदमी को आ ही जाते हैं। चाय तो मामूली बात है। पति द्वारा बनाई चाय कामकाजी पत्नी के अहम को खास पोषण भी देती है।
चाय की सुड़कियों के दौरान ही उन्होंने अपना बाकी हाल भी सुनाया था कि मनीष, यानी मेरा भतीजा चीनू अब छब्बीस का हो गया है। बी.कॉम. के बाद उसने इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से एम.बी.ए. किया है। बड़ी भतीजी मनीषा भी ग्रेज्यूएशन करके घर बैठी है। छोटी यानी प्रतिभा ने अभी बारहवीं के इम्तहान दिए हैं। कोमल यानी भाभी ठीक-ठाक है। बस थोड़ा बी.पी. और घुटनों के दर्द की शिकायत रहती है। और उनकी जिंदल स्टील की एकाउंटेंट की नौकरी जिंदाबाद चल रही है।
कुछ देर बाद भैया फ्रेश हुए और नाश्ता किया। इस दौरान हम ऐसे ही घर-बार की बातें करते रहे। भैया सफर की थकान से लदे थे। सोफे पर लेटने से पहले उन्होंने एक अजीबोगरीब सवाल कर डाला, ‘अरे जयदेव, तुम्हारे घर में साँप-वाँप तो नहीं निकलते हैं?’
‘यहाँ साँपों का क्या काम?’ मैं पहले चौंका था मगर बाद में सँभलकर उन्हें आश्वस्त करने लगा। साँप छोड़िए, कोई मुच्छड़-सा काकरोच घर में हाय-तौबा मचवा देता है।
‘नहीं, बाहर तुम्हारे यहाँ काफी पेड़-पौधे और हरियाली है न, और फिर नीचे (ग्राउंड फ्लोर) का मकान, इसलिए पूछा।’ वे अपने भय पर लेप चढ़ाने लगे।
‘नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से लेटिए।’
धीमे-धीमे सही मगर उन्हें मेरी बात पर यकीन-सा हो आया था और थोड़ी देर बाद सोफे पर ही सतर होकर खर्राटे मारने लगे थे।
गर्मी की छुट्टियों में कैरियर की साइकिल चलाकर हर मंगलवार को छतारी के दुराहे पर बंदरों को गुड़-चने चुगाने के बावजूद, हनुमान बाबा तीसरी दफा भी भैया से इतने प्रसन्न नहीं हुए थे कि डिग्री कॉलिज में दाखिले की सहूलियत दिलवा दें। भैया का कॉलिज जाने का बहुत मन था क्योंकि ठेका-कूद में अखिल भारतीय स्तर पर भविष्य की पहचान दिलाता झरोखा उन्हें वहीं से खुलता दिखता था। मगर होनी को जो मंजूर।
नतीजे के बाद पिताजी, भैया और भाभी को (और साल भर बाद हम सबको) दिल्ली ले आए थे ताकि दिन भर प्रेस की मशीनमैनी में खटने के बाद, जिदगी के चौथे पहर में स्टोव पर तड़का-दाल बनाने की जहमत से बरी हो जाएँ। भैया को भी यह बाखुशी मंजूर लगा था क्योंकि गली-मोहल्ले के लड़के बिना किसी फुसफुसाहट के यह मत अभिव्यक्त करने लगे थे कि सुखदेव बहुत दूरदर्शी लड़का है… वह बारहवीं में ‘पंचवर्षीय योजना’ बनाए बगैर नहीं मानेगा ताकि शिक्षा की नींव खूब पुख्ता हो जाए…।
उस लिहाज से प्रेस के कंपोजीटर की नौकरी कोई बुरी नहीं थी।
मगर बहुत जल्दी ही भाभी ने, माँ के हिसाब से, जटोला (भाभी का गाँव) वाले तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। वे बात-बेबात भैया से लड़तीं, देर से सोकर उठतीं, तीन साल के चीनू पर भभक निकालतीं या नहाने में घंटों लगातीं। यह मुझे बहुत बाद में पता चला कि उन्हीं दिनों वे चीनू के छोटे भाई के आने की तैयारी में थीं।
जिंदगी के मनहूस दिन भी भुलाए नहीं बनते हैं। चौदह नवंबर (बाल दिवस) के चक्कर में, दोपहर की शिफ्ट के उस सरकारी स्कूल में – जैसा हमारी जमात कहा करती थी – आधी छुट्टी ‘सारी’ हो गई थी और मैं कोई चार-सवा चार तक घर आ गया था। माँ सब्जी लेने मंडी गई हुई थी। चीनू अभी आदतन सो रहा था। मैं उसके मासूम, मदहोश चेहरे से चुहुल कर रहा था कि तभी भाभी दूध का भरा गिलास सिरहाने रख गईं जिसे नादानी में-दूध पीने के अपने खानदानी शौक के चलते – मैं अपना समझकर तुरंत गटक गया। अपने मनपसंद छोटे तकिए पर उल्टे सोते चीनू और मुझे दूध की मूछें साफ करते देख भाभी यकायक फट पड़ीं, ‘बालक के हलक का निवाला निगलकर कुजात कैसा लाड़ लड़िया रहा है… अब इसे क्या मैं तेरी अम्मा का पिलाऊँगी।’
मेरी गलती तो जाहिरा थी। शाम को दूध आने में अभी देरी थी मगर उसके लिए इतना विषैला अपमान।
‘तेरी अम्मा मर गई है जो मेरी अम्मा का पिलाएगी।’ प्रत्युत्तर में उसी अलीगढ़ी फुर्ती से लफ्ज बेसाख्ता मेरे मुँह से छूट पड़े।
उनके सामने ‘तू’ संबोधन का यह मेरा पहला और आखिरी प्रतिवाद था जिसके पीछे की हिमाकत को मैं आज तक नहीं समझ पाया। कुछ चीजें गोकि वक्त हमसे करवा ही डालता है।
और तभी, फिल्मी दुनिया में जिसे ‘एंट्री लेना’ कहते हैं, भैया ने वही लेकर मेरे ऐसा रेंप्टा रसीद किया कि निमिष भर को मैं सन्न रह गया। मगर फौरन ही बेकाबू होकर रो पड़ा। प्रेस में बिजली की खराबी के कारण वे जल्दी आ गए थे और मेरी कल्पनातीत बदतमीजी के आँखों देखे स्वरूप पर तिलमिलाहट से भरभरा उठे थे। चिकित्सा की तीसरे वर्ष की पढ़ाई कर रहे भूदेव भैया के साथ, पता नहीं किस अदृश्य प्रतिद्वंद्विता के कारण, सुक्खू भैया का रिश्ता थोड़ी तनातनी का ही था, मगर मुझ पर वे जान छिड़कते थे। मेरे लफ्जों को भाभी उन्हें बाद में बतलातीं तो वे उन्हें ‘लगाया हुआ’ समझकर यकीन से परे कर देते। मगर एकतरफा ही सही यहाँ तो उन्होंने सब कुछ अपने कानों से सुना था, आँखों के सामने। और क्या गुंजाइश बच सकती थी? किसी फिल्मी रील की तर्ज पर मौका-ए-वारदात पर थोड़ी देर बाद ही सब्जी का थैला उठाए माँ आ धमकी। मेरी जानिब जैसे दंगाग्रस्त क्षेत्र में सशस्त्र पुलिस की टुकड़ी आ गई हो। भाभी चीनू की माँ थी तो माँ मेरी माँ थी। दूध पी लिए जाने पर कोई अपने भाई पर ऐसे हाथ उठाएगा – उसके लिए मामला इस कदर पारदर्शी था। भैया दलील देते रहे मगर माँ ने एक न सुनी।
देर शाम को पिताजी जब थके-हारे प्रेस से घर पहुँचे तो उन्हें अविलंब ही भैया-भाभी की करतूत सव्याख्या परोस दी गई। पूरे मोहल्ले को हाजिर-नाजिर मानते हुए पिताजी ने भैया को खूब खरी-खोटी सुनाई और उनकी नामर्दी को ललकारा। दो मर्दों के द्वंद्व को एक दर्शक की लाचारी से देखकर मैं मन-ही-मन प्रफुल्ल हो रहा था क्योंकि वक्त काटने के लिए तब तक घर में टी.वी. आया नहीं था। जिस घर में औरतों की चलती है उसे बर्बाद होने से भगवान भी नहीं बचा सकता है, अपने इस ख्याल से मुतमईन पिताजी भैया को घर से निकाला देने की सलाह में गरज रहे थे जो उन्होंने अंततः मान ली थी। भाभी की तमाम बेशर्म मिन्नतों को एक तमाचे से दरकिनार कर वे रात के उसी पहर घर से बाहर निकल गए।
घर में रोज-रोज की कलह से, मैंने सोचा यह एक अनन्य राहत भरी निजात थी मगर मुझे ताज्जुब हुआ जब किसी गुड्डे की तरह मुझे झिंझोड़कर पिताजी मिसमिसा पड़े, ‘…बैठा-बैठा गूलर सेक रहा है दलिद्दर… जा भागकर भैया को लिवा ला… तू ही तो राड़ की जड़ है ससुरे…।’
आलस और असमंजस को परे फेंक मैं नंगे पैर ही भाग लिया और बंसल की चक्की के पास भैया को जा पकड़ा। वे ट्रेन पकड़ने की सी चाल में लंबे-लंबे डग भर रहे थे। साथ मिलाने के लिए मुझे तो हकीकतन भागना पड़ रहा था। मुरव्वत में मैं भैया से लिपट गया और भर्राए गले से उनसे घर लौटने की मिन्नतें करने लगा। भैया ने अपना पता नहीं कौन-सा संतुलन रखते हुए मुझे परे हटाकर कहा, ‘तू अपना मैथ्स पढ़ जाके… हर बार थुकाने वाले नंबर लाता है।’
उन्होंने सब कुछ इतनी तिक्त घृणा से फेंका कि उन्हें मनाने की मेरी हिम्मत जवाब दे गई। लौटा तो माँ-पिताजी दरवाजे के बाहर टकटकी लगाए खड़े थे और भीतर से भाभी का रुदन रिस-रिसकर आ रहा था।
अब सब कुछ वैसा ही था जैसे अंधड़ के बाद की बरसात से निथर जाता है… रीता रीता। पिताजी की वही हालत थी जो पानी में सिरा दिए जाने पर धधकते कोयले की होती है… देर रात घर से कूचकर भैया ने उनकी (या कहूँ सबकी) हवा निकाल दी थी और वे टेलीफोन छाप बीड़ी के मुसलसल खींचते कशों में पूरे मामले में हुई अपनी चूक की शिनाख्त कर रहे थे। मतलब मैं तो यही सोच रहा था।
कहाँ जाएँगे भैया इतनी रात को? अगर वाकया 15 अगस्त की छुट्टी के आसपास का होता तो स्टेशन या ऐसी पचासियों जगहों पर रात काटना मुहाल न होता। मगर यह तो नेहरू चाचा का नवंबर था। और कुछ नहीं तो लगे हाथ पूरी बाजू की कोई जरसी ही डाल जाते।
घंटे भर बाद जब दरवाजे पर एक आहिस्ता-सी थपथपाहट हुई तो मैं सकते में आ गया… जरूर भैया की लाश की सूचना देता सेवकराम चौकीदार होगा। मैंने धड़कते हिये से साँकल खोली। भैया की परछाईं देख आश्चर्य भी नहीं व्यक्त कर पाया । उधर भैया अंदर घुसे और बिना मुड़े ही अपनी वाली कुठरिया में चले गए।
अगले रोज छुट्टी थी। माँ ने उसी तरह उठकर सबसे पहले बिना टीप भरे बरामदे के फर्श पर अपनी नारियल वाली झाड़ू लगाई, कोयले जमाने के बाद दहकाने के लिए अँगीठी को सही दिशा देखकर बाहर रख दिया और दूध की आपूर्ति बढ़ाने के लिए आदतन उसमें एक गिलास पानी मिला दिया। पिताजी ने भी सुबह उठकर हाजत के बाद दसेक मिनट उसी तरह खरखराकर गले की अँतड़ियों की खैर-खबर ली मगर निस्तब्धता में चाय की सुड़कियाँ भरते-भरते उन्हें खबर लग गई थी कि वे बुखार की गिरफ्त में जा चुके हैं।
भैया-भाभी की कुठरिया से भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद जब तीन साल के चीनू ने अपनी तुतलाहट में माँ को ‘अम्माजी गुदमोलिंग’ कहा तो माहौल की मनहूसियत टूटी अवश्य मगर इतनी नहीं कि यथास्थिति बहाल कर दे। फुसलाकर आधा गिलास दूध पिलाने के बाद माँ ने उसे एक मतलबपरक चुग्गा डाला।
‘तेरी मम्मी नहीं उठी अभी।’
‘मम्मी तो छो लही है।’
‘और पापा?’
‘पापा तो उठ दये।’
सोने-जागने के क्रम की इन लैंगिक अशिष्टता पर पिताजी जो अमूमन जरूरी टिप्पणी दर्ज कर सकते थे, बुखार की कराहट के चलते उन्होंने जाने दी। अपनी तोतली जुबान में चीनू ने और जो अयाचित मुखबरी की उसका खुलासा दोपहर चढ़ते तब हुआ जब घर के आगे एक टेंपो रुका और भैया अपना अटैची-संदूक उसमें लादने लगे।
बड़ी बोझिल दोपहर थी वह। भाभी को दिन चढ़ रहे थे और पिताजी बुखार की अशक्ति में खोए पड़े थे। वक्त-बेवक्त भाभी को और उनकी मार्फत भैया को खूब खरी-खोटी सुना देने के उत्तर भारतीय संस्कार के बावजूद बड़ा बेटा होने भर के कारण माँ ने भैया के लिए जो मुलामियत आरक्षित कर रखी थी, सामने खड़े टेंपो के चलते उसे बर्दाश्त करना उनके बूते के बाहर हो गया था। अफरा-तफरी में एकत्र हो आईं मोहल्ले की कुछ बुजुर्ग महिलाएँ अपनी बहुमूल्य राय में, पूरे मामले के गैर-जरूरीपन के लिए सीधे-सीधे बदलते जमाने को दोषी ठहरा रही थीं। सामान रखने की आवाजाही के बीच उनमें से किसी ने टोका भी कि ‘भैया सुक्खा, परिवार में थोड़ी-बहुत कहा-सुनी तो चलती ही रहती है… किसने कही, किसने सुनी। गुस्सा थूक और भिजवा दे टेंपो को वापस।’ भैया ने इस बात पर ज्यादा कान नहीं दिए थे मगर तभी एक पुछल्ला उनके कान में आ पड़ा, ‘अपनी औरत के चक्कर में आकर तू अपने माँ-बाप और छोटे भाइयों से न्यारा हो जाएगा?’ भैया की भंगिमा एकदम फट पड़नेवाली हो गई। फट पड़ते तो शायद अच्छा रहता मगर उस अंगार को उन्होंने अपने तईं जैसे-तैसे निगला और टेंपो में सामान की जमावट में फिर मशगूल हो गए। मोहल्ले की औरतों के इस विचार से अलबत्ता कहीं-न-कहीं मैं सहमत हो रहा था कि यह झगड़ा तो एक बहाना है, कोमल तो अर्से से ही न्यारा होने की योजना बना रही थी।
रवाना करने से पहले नए पते की पर्ची टेंपो को टिकाने के बाद, भैया-भाभी जब बुखार में तपते पिताजी और टेसुए बहाती माँ के पाँव छूने आए तो माँ की अश्रुधारा और उदग्र हो उठी। माफी माँगते हुए मैं भी बिलखकर भैया से लिपट पड़ा था मगर भाभी की ‘इस देहरी पर दुबारा न चढ़ने’ की प्रतिज्ञा के चलते मामला दो-तरफा विगलित होने से जरा-सा बच गया। और सच, भाभी ने अपना कौल बाकायदा रखा। जीते-जी गली नं. 5 के सैंतालीसवें मकान की देहरी उन्होंने कभी नहीं चढ़ी। भैया चीनू और वाकए के बाद जन्मी मनीषा और प्रतिभा को लेकर छठे-छमाहे जरूर दर्शन करा जाते थे। उस मुख्तसर मुलाकात में ही पता चल जाता था कि भैया अपने बच्चों की अंग्रेजी के प्रति किस कदर सचेत हैं। माँ भाभी के बारे में एकाध चलताऊ सवाल पूछकर पारिवारिकता की जिम्मेदारी से बरी हो जाती थी। वैसे माँ का रवैया भी हेठीपूर्ण ही था। मुझे अक्सर लगता कि भाभी की तरफ से की गई रियायतपूर्ण पहल उनके बीच जमी बर्फ को बहुत कुछ पिघला सकती थी। उसके बाद तो माँ ने ऐसी खाट पकड़ी कि वह संभावना ही जाती रही। उधर संभावित मस्ती के सात बरस, पहरों के बीच रहकर मिली हाली आजादी का स्वाद (और किसी कमजोर क्षण में उसके खामखा छिन जाने की आशंका) भाभी को ज्यादा हसीन लगता रहा होगा वरना उनमें वह तल्खी मैं नहीं गौर कर पाया जो इतने बेरहम रवैये की दरकार करती। यह भी हो सकता है कि यह स्त्री मानसिकता की मेरी समझ के परे की बात रही हो। यह ‘देहरी’ भर की बात तो नहीं थी क्योंकि बैंक में पीओ लग जाने के दूसरे बरस अपने विवाह से पहले जब मैं उन्हें मनाने गया था तो उन्होंने बड़े पेशेवर अंदाज में ‘खुशी की बेला है सीटू, एक मैं न आई तो क्या फर्क पड़ जाएगा… गड़े मुर्दे क्यों खड़े करो…’ कहकर अपनी जान छुड़ा ली थी।
‘काजल तो बड़ी भाभी ही लगाती है।’ मैंने तुरुप चाल चली।
‘सोमा लगा देगी।’ वे मँझली भाभी की मौजूदगी का कवच मानो गोद में रखे बैठी थीं।
‘लेकिन आपकी शिकायत किससे है… मुझसे, माँ से या उस देहरी से।’ मैंने सीधे-सीधे दरयाफ्त किया।
एक फीकी, निर्लज्ज हँसी से भाभी ने बात का सिरा बदल दिया जब उन्होंने बैठे-बैठे ही मिनी (मनीषा) को अपने चाचा के लिए चाय चढ़ाने की गुहार लगा दी।
मैं अपना-सा मुँह लेकर लौट आया। बहुत सोचने के बाद मेरे हाथ बस एक सूत्र-सा ही हाथ लगा… कि तब न्यारा होने के चंद रोज बाद भाभी का मिसकैरेज हो गया था, जिसे फैसले की हेकड़ी के चलते भैया-भाभी ने किसी को नहीं बताया मगर ‘चीनू के छोटे भाई’ की असमय हत्या की आश्वस्ति के लिए मेरे सुझाए तीनों विकल्प संयुक्त रूप से अपराधी थे। उसके बाद शायद जंग-पर-जंग चढ़ती रही थी।
भैया के उठने से पहले लीना कॉलिज से आ गई थी और उनके अप्रत्याशित आगमन पर अचरज करे जा रही थी। इसलिए और भी कि दिल्ली का वह ‘घर’ भूदेव भैया-सोमा भाभी का सिमटकर रह गया था। सुक्खू भैया उसमें होते ही नहीं थे।
‘कितने बजे पहुँचे?’
‘कोई आठ बजे।’
‘कुछ खाया-पीया?’
‘हाँ सैंडविच खिला दिए थे।’
‘लंच में क्या खाना है?’
‘कुछ भी बनवा लो।’
‘कुछ भी क्या, जो पसंद हो बनवा लो। शोभा आई तो नहीं।’
‘नहीं शोभा तो नहीं आई मगर वो प्रेसवाला कपड़े दे गया है।’
‘कोई खास वजह?’ अपने हैंड बैग को ड्रेसिंग टेबल पर पटकते हुए लीना पूछने लगी।
‘अरे खास वजह क्या होगी, कपड़े बनाकर तो वह दूसरे दिन देता ही है।’
‘तुम रहोगे वही… मैं कपड़ों की नहीं, भैया की बात कर रही हूँ।’
‘मुझे कोई सपने आते हैं… वैसे रास्ते की थकान रही होगी। गर्मी का मौसम है। आर्डिनरी से ही आए होंगे। अभी तो आए ही हैं… उठेंगे तो पता चलेगा।’
भैया ने जो बताया उसका लब्बोलुआब यह था कि दूसरे वर्ष में लुढ़क जाने के बाद चीनू बी.कॉम. में पास तो हो गया था मगर तीसरे दर्जे में। बी.कॉम. में दाखिले के वक्त सी.ए. करने का जो ख्वाब हर विद्यार्थी देखता है, उसने भी देखा था मगर दूसरे वर्ष के बाद उसे अहसास हो गया कि ‘गुप्ता प्रोफेशनल’ के यहाँ हिसाबी खातों की समकालीन दुरुस्ती से परिचय कराता ‘टेली’ का साफ्टवेयर सी.ए. का न सही मगर जिंदगी का विकल्प हो सकता है, इसलिए भैया ने फंड से कुछ राशि निकालकर उसे वहाँ जबरन ठेल दिया था। अनुभवहीनता के कारण दसियों जगह से ठुकराए जाने के बाद वह एक कंपनी के खाते लिखने-देखने के काम में लग गया था। मगर नसीब देखिए! महीने भर में वह कंपनी ही उठ गई। कई जगह बेचारे ने हाथ-पाँव मारे मगर सब बेकार। एक-दो जगह डेटा एंट्री का भी काम करता रहा। खाली बैठने से अच्छा यही लगा कि इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय से एम.बी.ए. कर ले मगर उसे भी आज तीन साल हो गए। उनसे या भाभी से उसकी बातचीत बंद-सी ही है। कद-काठी में खूब निकल आया है। कुछ टोको तो अर्रा के आता है। भाई ये बताओ कि ये मंदी क्या चीज है जो इतने दिनों से लोगों को तबाह करने पर लगी है? हमारी तो कुछ समझ नहीं पड़ती। जिंदल स्टीलवालों ने भी एक-तिहाई स्टाफ घटा दिया है। चार-छह महीने में उनका भी घर बिठा दिया जाना तय है। नहीं बैठेंगे तो झारखंड के किसी डिपो में पटक दिए जाएँगे। मनीषा को भी ग्रेजुएट हुए दो-तीन साल हो गए। न कोई कामकाज का हिसाब बैठा है और न रिश्ते का। अपने कॉलिज की सौंदर्य प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रही थी। उधर भी जोर मारा मगर बिना संपर्क या पैसों के इस दुनिया में कुछ होता है क्या? अभी नौकरी के लिए पैसा नहीं है, फिर दहेज के लिए कहाँ से जुटाएँगे।
अपनी शक्ल पर दाढ़ी बढ़ाने का कौल उन्होंने इसलिए उठाया था कि इस इम्तहान की मार्फत (ऐसे दूसरे इम्तहानों की खबर मुझे बाद में भी लगी जिसमें शामिल थे भैया के मंगलवार और शनिवार के उपवास, हर पूर्णिमा को वृंदावन जाकर गोवर्धन की परिक्रमा, कच्ची हल्दी की गाँठ को हरदम कमीज की जेब में डालकर चलना और सुबह घर से निकलते समय, देहरी की धूल को माथे पर पोतना) मनीषा के लिए कोई रिश्ता या मनीष के लिए अदद नौकरी का इंतजाम हो जाए तो यूँ ही सही। वैसे डेढ़ साल पहले एक नामी ज्योतिषी ने उन्हें बताया था कि उनकी विकट पारिवारिक तकलीफ का कारण उनके ऊपर एक खास नक्षत्र की कुदृष्टि है जिससे निजात पाने के लिए उन्होंने यथा सुझाया अनुष्ठान करवा लिया था। ‘उधर तेरी भाभी को भी जोड़ों का दर्द बहुत रहता है। वजन बढ़ गया है सो अलग।’ प्रतिभा के बारे में उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा मगर मनीषा के रिश्ते के लिए मेरठ छावनी के निकट के अनुभव को वे कभी नहीं भूल पाते हैं। लड़का बीमा कंपनी में एजेंट था और डेढ़ कमरे के अपने मकान में माँ-बाप के साथ रहता था। कॉलोनी में तारकोल की सड़क बननी बकाया थी हालाँकि बिजली का कनेक्शन दिया जा चुका था। अरसे बाद कंपनी के एक गाहक से वसूली करने की आड़ में उन्होंने ‘लड़का देखने’ का कार्यक्रम बना लिया था। बड़ा उमस भरा दिन था वह और पते की अस्पष्टता के चलते कोई डेढ़ किलोमीटर का रास्ता उन्हें अतिरिक्त नापना पड़ गया था। तयशुदा कार्यक्रम के बावजूद घर पर न लड़का था, न उसका पिता। पूछे जाने पर लड़के की माँ ने दरवाजे की झिरी से इसी बावत उन्हें चलता कर दिया था… ‘लड़के वाले’ होने के दर्प से उपजी ऐसी निष्ठुर निरपेक्षता से कि पानी की त्राहि-त्राहि मचाते सूखे गले के लिए वे एक गिलास की भीख भी नहीं माँग सकते थे। निस्तेज, बेमन से जैसे ही वे मुड़े कि झाड़ियों से निकलकर एक साँप सामने फन फैलाकर उनका मुआयना करने लगा।
चार-पाँच पल बेकली से मौत को साक्षात अपने भीतर उतरते देख उनके जेहन में पता नहीं कैसे यह ख्याल आए बगैर नहीं रहा कि जिंदल वालों को उनकी कारस्तानी का पता चलेगा तो सब लोग क्या सोचेंगे। उनका पोर-पोर जम गया था। मृत्यु की इस निस्तब्ध जंग से अनजान लड़के की माँ दरवाजा भेड़कर कब का भीतर जा चुकी थी। खैर, अब उस बारे में वे और क्या बताएँ, सिवाय इसके कि भूमि तल के किसी अपरिचित मकान से घुसते वक्त एक कड़क मटमैली रस्सी उन्हें आज भी पाँव में लिथड़ी दिखती है। ‘मगर सीटू, सही कह रहा हूँ, मुझे उस रोज अगर किसी ने बचाया तो वह थी माँ के आशीर्वाद की परछाईं… मुझे अक्सर माँ की याद आती है… तुझे आती है?’
पता नहीं भैया ने किस अनुभव का सिरा माँ से जोड़ डाला। एक अव्यक्त सहमति के अलावा ऐसी हालत में कहने को कुछ बनता ही नहीं था। ‘चीनू को बड़ा प्यार करती थी… मुझे तो लगता है मेरे-तेरे से ज्यादा वह चीनू को प्यार करती थी… और उधर चीनू, कोमल से चाहे सीधे मुँह बात न करे मगर बात-बेबात ‘अम्माजी-अम्माजी’ की धुन टेरता रहेगा। सच है या झूठ मगर मैंने कहीं पढ़ा था कि आत्माएँ तीसरी पीढ़ी में उतरकर अपना वजूद तलाश करती हैं। और चीनू को तो मैं रोज देखता हूँ… स्टील के कप में उसी स्टाइल में सुड़ककर चाय के घूँट भरता है, नहाने के बाद माँ की तरह दुर्गा की मूर्ति के सामने माथा टेकना कभी नहीं भूलता, गर्मी हो सर्दी, मुँह ढँके बगैर कभी नहीं सोएगा और हद तो ये है कि कई बार रात को, सपने में, साते-सोते, माँ की तरह ‘सुक्खू-सुक्खू’ बड़बड़ाकर मुझे हिदायतें देने लगता है।’
किसी यकीनन असरकारी बात के आवेग की तृप्ति से भैया रुके और फिर चहककर बोले, ‘क्या कहोगे आप इसे?’
स्कूल से लौटे प्रतीक और रागिनी ने दरवाजे की घंटी न बजाई होती तो भैया पता नहीं कितनी देर उस अंतःप्रदेश की सैर कराते जिसमें मुझे भी सुकून मिल रहा था। उन्हें देख भैया जोश से भर उठे मगर भैया की लाख मनुहार और मेरी सख्त हिदायतों के बावजूद दोनों बच्चे भैया के सुझाए ‘बड़े ताऊजी’ के खिताब के आकर्षण से नहीं बँध पाए। उनके लिए भैया के बूढ़े होते, खिचड़ी दाढ़ीवाले अजनबी चेहरे से भी बड़ी अड़चन या प्राथमिकता कार्टून नेटवर्क पर उस समय आते पावर पफ गर्ल्स का रिपीट शो था जो उन्हें ज्यादा अजीज था। मेरे बैंक के प्रशिक्षण संस्थान की शनिवारी छुट्टी होने के कारण टेलीफोन की चिल्लपों और प्रशिक्षार्थियों की कौतूहल भरी पूछताछ से आज राहत थी। दो दिन से लिखे पड़े एक अंतर्देशीय को मैं संस्थान के डाकखाने डालकर लौटा तो घर में एक अजूबा पसरा बैठा था। दोनों बच्चे भैया के लाए बेसन के लड्डुओं को बेध्यानी में खाते हुए उस ‘बेबी’ ऊदबिलाव की चालबाजी में डूब-उतर रहे थे जिसकी गँवई लटकों-झटकों में सुनाई जा रही रहस्य-कथा में भैया को महारत हासिल थी।
‘क्या ऊदबिलाव ट्री पर चढ़ सकता था?’
‘ट्री पर तो वह खड़े-खड़े जंप मारकर चढ़ जाता था और डाल पर चमगादड़ की तरह लटककर मजे से झूलता रहता था।’
‘क्या ऊदबिलाव रिवर में तैर सकता था?’
‘रिवर में तो वह घंटों, साँस रोककर तैरता रहता था… साबुत मछलियों को गड़पकर खाने में उसे बहुत मजा आता था।’
‘ऊदबिलाव बच्चों को भी खा जाता था?’
‘नहीं, बच्चे तो उसकी कमजोरी थे… यानी था तो वह ऊदबिलाव का बेबी मगर उसे बच्चों का साथ अच्छा लगता था… बच्चों के साथ खेलने में वह अपना खाना-पीना तक भूल जाता था।’
‘तब उसे मम्मी-पापा की डाँट पड़ती थी?’
मन हुआ बच्चों की मासूम प्रश्नाकुलता के क्रम के बीचोबीच मैं भी पूछ डालूँ कि क्या उस बेबी के बड़े भैया भी थे जो माँ-बाप से डाँट पड़ने की अवस्था में अक्सर उस ‘बेबी’ को साइकिल पर चड्डू खिलाते, उसके लिए एक-से-एक दिलचस्प परिकथा बुनते और खुद फेल होते जाने की आदत के बावजूद बेबी को चुपके से पढ़ने की अहमियत के बारे में प्रेरित करते…।
या किसी काले मूँड़वाली की गिरफ्त में आकर उन्होंने उस जंगल से ही तौबा कर ली जिसमें बेबी ऊदबिलाव शहजादे की तरह बिचरता था।
आपसी वार्तालाप में मुझे किंचित दिलचस्पी लेता देख उन्होंने लड्डू की आखिरी पिट्ठी शाइस्तगी से बच्चों के मुँह में ठूँसकर, ‘एक मिनट बेटा’ कहकर बच्चों से मोहलत माँगी और गत्ते के दूसरे डिब्बे को मेरी तरफ बढ़ाकर बोले, ‘तुम्हारे लिए बेसन-मेथी के कोमल ने अलग बनाकर भेजे हैं।’
सुक्खू भैया! तुम भी क्या बेरहम चीज हो। बचपन की मेरी पसंदीदा मिठाई को इतनी देर से झोले में दबाए बैठे हो। साल भर फीकी या शुगर-फ्री की चाय पी सकता हूँ मगर बेसन-मेथी के लड्डुओं को कैसे छोड़ दूँ!
इसरार के बावजूद सुक्खू भैया उसी शाम वापस दिल्ली लौट गए। ‘तुम जानते ही हो कंपनी की हालत कितनी खस्ता हो रही है… चार-छह महीने जितनी हो जाए, हो जाए… बाद में तो वालंटरी भुगतनी ही है।’ उनके इस तर्क के आगे मैं निष्कवच था। अलबत्ता, एक जाहिर-सी बात, जिसे लीना की उपस्थिति में वे परोक्ष रूप से ही कह पाए थे, स्टेशन के रास्ते में यथासंभव नियंत्रण रखते हुए, पिघलकर कह गए। अलविदा के वक्त, करीब से निरीहता में नजरें बिछाकर मेरी हथेली दबोचकर बोले, ‘यार सीटू, चीनू का काम करवाना जरूरी है।’
चीनू को लेकर कई दिनों तक तो मैं खूब बगलें झाँकता रहा मगर यह एक सुखद संयोग था कि संस्थान में अगले माह मेरे सहनिर्देशन में ‘गैर-उत्पादक परिसंपत्तियों का प्रबंधन’ विषय पर आयोजित की जा रही कार्यशाला में बैंक की नोएडा शाखा का वरिष्ठ प्रबंधक (ऋण एवं अग्रिम) विनोद मेंहदीरत्ता भी शामिल था जिससे मेरा मामूली पूर्व परिचय था। तीन सत्रों के मेरे व्याख्यान के बाद हुए लंच ब्रेक में, परिचय पुख्ता करने की खुमारी में वह सेवा का मौका दिए जाने की पेशकश किए जा रहा था हालाँकि मैं जानता था कि बैंक के तीसमारखाओं (टॉप नाचिज) के साथ संकाय सदस्यों के करीबी स्वस्थ संबंधों की वजह से मेंहदीरत्ता जैसे कितने ही प्रतिभागी ऐसी पगडंडियों का सहारा लेते थे।
‘एक लड़का है, मेरा सगा भतीजा, एम.बी.ए. कर चुका है, एकाउंट्स की नॉलिज है, कंप्यूटर भी जानता है… उसे किसी बढ़िया-सी कंपनी में सेट करा दो तो मैं एहसानमंद रहूँगा।’ शाम को अपने चेंबर में बुलाकर, यथासंभव साफदिली से मैंने मेंहदीरत्ता को फटाफट ‘मौका’ दे डाला।
वैसे गुनाह तो अंततः दोनों ही बनते हैं, नौकरी लगवाना भी और न लगवाना भी।
‘ओए देव साहब, तूसी इन्नी छोटी गल के लिए एवें कैंदेओ… त्वाडा पतीझा, साड्डा पतीझा… ओत्थे सॉफ्टवेयर कंपनियों दी लैन लगी हैगी जिने असि फायनेंस कर दे हैं। कुत्ते दे पुतरों ने साडे किन्ने एन.पी.ए. खड़े कर दिते हैं।’
मेंहदीरत्ता के लफ्जों से स्टेशन पर हथेली दबाते भैया का पसीजता चेहरा जेहन में कौंध आया और मैं इस फुरफुरे गुमान से भर उठा कि काश दूर किसी कोने में भैया ने हमारी बात सुन ली हो।
थोड़ा वक्त लगा मगर मेंहदीरत्ता ने अपनी बात रख ली। बैंक ऋण के कागजात तैयार करनेवाले उस कंपनी के मुलाजिम जगरूप दयाल के, पहले छुट्टी पर और बाद में दूसरे किसी काम में खपे रहने के कारण चीनू को फालतू में 10-12 बार नोएडा चक्कर जरूर लगाने पड़े मगर आखिर में बात बन गई। और यह कम बड़ी बात नहीं थी। दिन में फोन करके ही भैया ने अपनी तसल्ली मिश्रित खुशी जाहिर कर दी थी जबकि मैं दूसरे किस्म के डर से ज्यादा परेशान था कि कहीं चीनू वैसा न साबित हो जैसा ‘जुगाड़’ से नौकरी पानेवाले लोग अमूमन होते हैं।
एक-सवा महीने तक कोई खबर नहीं आई तो मुझे लगा सब कुछ ठीक चल रहा है। इस दौरान भैया का एक खूबसूरत ग्रीटिंग कार्ड आया जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएँ प्रेषित की थीं और पुनश्चः में लिखा था कि कुछ छुट्टियों की व्यवस्था करके मुझे सपरिवार दिल्ली घूमने आना चाहिए, खासकर इसलिए कि उस रोज हुई चुटकी-सी मुलाकात के बाद प्रतीक-रागिनी उन्हें इतने अच्छे लगे थे कि गाहे-बगाहे उन्हें खूब हिचकियाँ आती हैं। अंग्रेजी के उद्धरण की मार्फत उन्होंने मुझे बुजुर्गों की कही याद दिलाई कि कैसे खून हमेशा पानी से वजनी होता है। इसके अलावा फोन पर भी भैया प्रतीक-रागिनी से खूब बातें करते, लीना के कॉलिज संबँधी मसलों की जानकारी लेते और फोन रखते-रखते उदारता से सभी के स्वस्थ-प्रसन्न रहने का आशीर्वाद देते।
कुछ दिनों बाद दफ्तर के दौरान ही चीनू ने बूथ से फोन करके सूचित किया कि वैसे तो उसकी नौकरी ठीक-ठाक चल रही है, सिवाय इस दिक्कत के कि प्रबंधन के एक ग्रेजुएट को पता नहीं कंपनी के किस कूढ़मगज ने डेटा-एंट्री के सड़े से काम में लगा रखा था। पहले उससे कहा गया था कि यह शुरुआत के कारण है मगर दो महीने गुजर जाने के बाद भी उसकी शैक्षणिक योग्यता के शतांश जैसा काम मिलता प्रतीत नहीं होता है। मामला कुछ संगीन हो रहा होगा क्योंकि भैया अब मेंहदीरत्ता का हवाला लेकर मुझसे जगरूप दयाल या कंपनी के दूसरे कर्ताधर्ता से सीधे बात करने का हरदम आग्रह करते। मैं इसे कंपनी के अंदरूनी मामले में दखल न देने की अपनी गरिमा से जोड़कर देखता तो भैया यही कहते, ‘तुम देख लेना, फिर भी।’
कई बार टाल-मटोल के बाद जब मैंने इस देखनेवाली बात को वाकई देखने की कोशिश की तो नतीजा ‘एलोवीरा’ की तरह मुझे बेस्वाद से भर गया। न चाहते हुए भी दयाल ने कह डाला… साहब हम मेंहदीरत्ता साहब की बहुत इज्जत करते हैं मगर जिस एम.बी.ए. को ‘प्रशासन’ और ‘प्रबंधन’ का किताबी फर्क नहीं पता हो, ‘टेली’ के तहत जिसे ट्रायल बैलेंस चेक करना नहीं आता हो ओर अंग्रेजी बोलने के नाम पर जिसे साँप सूँघ जाता हो, उसे कंपनी प्रबंधकीय जिम्मेदारी में कैसे खपा सकती है? आपको तो पता ही है कि नॉन परफोर्मिंग एसेट्स में ऑडिट वाले स्टाफ की भी बजटिंग करते हैं… मंदी से दिन-रात लड़ती कंपनी किसी को वह मकाम कैसे बख्श दे जो उसका बाजार-भाव है ही नहीं…।’
दयाल ने मेरी बोलती बंद कर दी। मेंहदीरत्ता से भी बात करके कुछ उत्साहवर्धक हासिल नहीं हुआ तो मैं अपने खोल में लौट आया। हस्तक्षेप की उम्मीद में आए दिन भैया फोन पर प्रोंप्ट करते कि मैं कुछ देखूँ… मेंहदीरत्ता या दूसरे किसी की मार्फत… कोई दूसरी कंपनी या जैसा मुझे ठीक लगे वह…।
भैया को सब कुछ बताना फिजूल था।
शायद भैया भी असलियत जान गए थे।
भैया का फोन आए आज आठ महीने सत्रह दिन हो गए हैं।
Download PDF (वास्ता )
वास्ता – Vasta