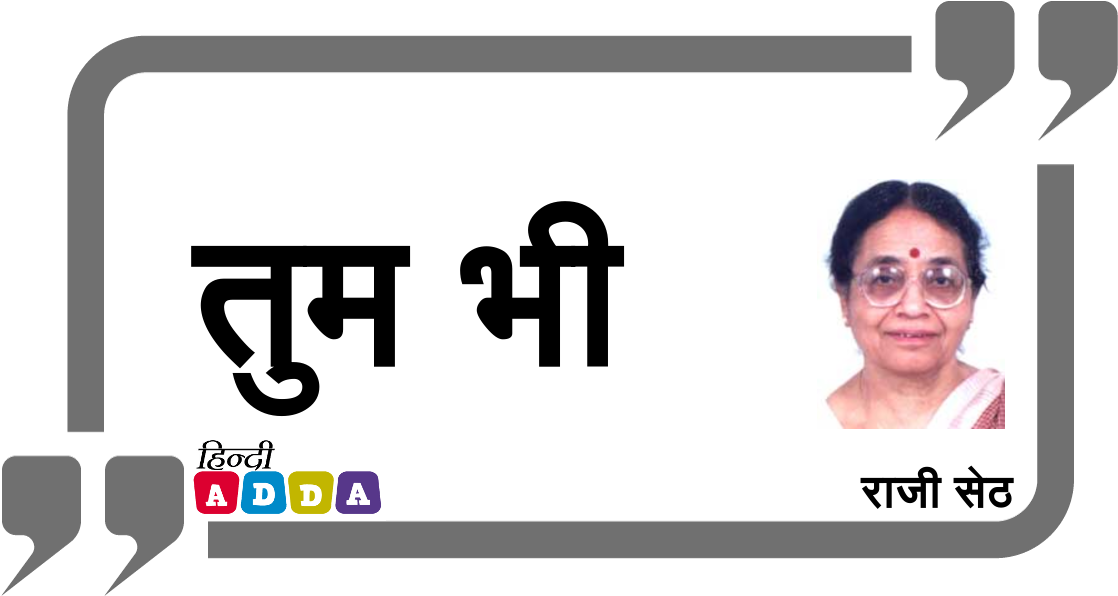तुम भी | राजी सेठ – Tum bhi
तुम भी | राजी सेठ
रात जब उसकी नींद खुली तो आज फिर वह बिस्तर पर नहीं था। दो क्षण अडोल पड़ी रही। बाथरूम की दिशा में कान दिए…रात खामोश थी…कोई आवाज़ न होने से उसे लगा, दिन होने में देरी है…बीच रात का पहर है…सन्नाटे से भरा।
दरवाज़े की सांकल हलकी-सी बजी…खिश्श-खिश्श की ध्वनि। पूर्व ज्ञान न होता तो शायद समझ न पाती कि बोरी घसीटी जाकर दरवाज़े के पीछे रख दी गई है। प्राण जैसे कहीं और बंधे हों, ऐसी सीने के भीतर टंगी जाती सांस
…चुप पड़ी रही।
वह आया…सुराही से पानी उंड़ेला…गटगट पिया और धीरे, बहुत धीरे खाट पर बैठ गया।
”क्यों करते हो तुम यह पाप?” पत्नी ने उठकर उसकी कलाई पकड़ ली। पर यह उसके अपने हाथ में अपनी ही कलाई थी। पति की कलाई पकड़कर यूं कह डालने का साहस उसमें नहीं था…उस क्षण का सामना करने का…पति को लज्जित करने का…बीच चाहे अंधेरे का परदा था…पर अंधेरे में,सन्नाटे में यह सब अधिक साफष् दिखता है, साफष् सुना जाता है।
सवेरे घर बुहारते वह उस कोने में जाना बचा गई। देर से उठते पति के आलस्य को अनदेखा कर गई…बोरी ढोकर ले जाने का अहसास होने पर भी बाहर टिफिन देने न गई…सवी को भेज दिया…।
अनाज के इस मालगोदाम की रखवाली के ही लिए रखे गए थे वह। लाला ने यही सोचकर यह छोटा-सा दो कोठरियों काचाहे टूटा-सा घर उन्हें बिना भाड़े के दे दिया थाअागे एक छोटा-सा सहन और दालान। क्लर्की से कुछ बनता नहीं था। बीमार मां, एक बहन, एक भाई और तीन बच्चे…बहन जैसे- तैसे ब्याह गई थी…भाई होशियार था, अपने पाए वज़ीफे से पढ़ रहा था…कभी- कभार आता था और बड़े भाई के कंधे पर एक नपुंसक दिलासा छोड़ जाता था…अभी उसकी तीन साल की पढ़ाई बाकी थी…तब तक सवी सोलह की हो जाएगी और गुल्लू बारह का। गीतू तो अभी छोटी थीएक का ब्याह, दूसरे की पढ़ाई…। इन दो सुलगते सवालों से आंखें भींच लेना चाहते थे वे…जो कुछ जोड़ा, बचाया था, पिछले साल मां की बीमारी में…’सेरीबरल’…कुछ ऐसी ही टेढ़ी-मेढ़ी बातें कही थीं डॉक्टर ने… ‘पहले बहत्तार घंटे खींच गई तो जी जाएंगी।’ ऐंठे हुए अंगों और ऊपर टंगी हुई पुतलियों के बावजूद मां जी गई थीं।
और जीने की डोर रुपयों की थैली के साथ बंधी यथार्थ की चर्खी पर खिंचती सतत। ऊपर-नीचे। बार-बार…
अपने मन का चोर वह जानती है। उसे लगा करता है, मरना तो है, एक दिन सबको…हर किसी को…क्या फर्ष्कष् पड़ता है! मां जी गईं तो पीछे जीवित रहने वाले सबके-सब। वह, अमर, देबू, सवी, गुल्लू, गीतूसब मर जाएंगे…धीरे- धीरे। सिर्फ डॉक्टर खाएगा और गले पड़ी बीमारी…नहीं तो सब खाते…थोड़ा- थोड़ा…साधकर, संभालकर…
छि:! छि:! क्या सोचती रहती है। अमर जान जाएगा तो क्या सोचेगा…? ‘ऐसा न्याय घरों में नहीं होता…श्मशानों में, अस्पतालों में होता है, लाशें आधी
रात या मुंह-अंधेरे बिकने आती हैं बीस-बीस रुपये में।’ देबू बताया करता है, ‘साइकिलों पर लंबे-लंबे पैंडें मारकर लाशें लादकर लाते हैं सगे-संबंधियों की। बीस-पच्चीस रुपयों की ख़ातिर…’ ‘संबंध तो वैसे ही मर गया है डाकदर साब
…यह तो मिट्टी है…’ ‘यह बात संबंध से ज्यादा जानदार होती है क्योंकि रोटी दे सकती है,’ देबू यह बात अपनी तरफष् से जोड़ देता है।
”बस-बस, देबू…बस कर!” उसने सुनते-सुनते घबराकर कहा था, ”आदमी की चेतना क्या इतनी मर जाती है?”
”किस चेतना की बात करती हो भाभी…शास्तर वाली चेतना की?”
”चुप देबू…शास्तर का नाम न ले…पढ़-लिख गया है, तो इसका यह मतलब तो नहीं…”
”एक बार मेरे साथ अस्पताल चलकर देखो भाभी।”
और अस्पताल गए बिना ही वह देख रही है…देख लेती है। अपने को। अपने भीतर पनपते विषाणुओं को। मां जीवित रहेंगी तो सबके भविष्य का संतुलन डोल जाएगा। देबू की बात इतनी नंगी…इतने पास।
मन की शांति कहीं उड़ गई थी…उठते-बैठते मां की जगह एक लाश दीखने लग गई थी…उसने एक दिन डरते-डरते अमर से पूछा, ”क्या तुम्हें भी लगता है कि…”
”क्या?”
”कुछ नहीं…यही कि पैसे कम होते जा रहे हैं। कितने बचे हैं? तुम तो आज पोस्ट ऑफिष्स गए थे न?”
एक दीर्घ दृष्टि से उसे भांपता वह चुप रहा।
”तुमने जवाब नहीं दिया…कितना बचा है अब?”
”तुम्हें हर बात से क्या मतलब?”
”मतलब क्यों नहीं…सब कुछ तुम्हारे अकेले के सिर…क्या मैं जानती नहीं, अब तो तुम भर पेट खाना भी नहीं खाते…”
”ओह! चुप रह सरना…मैं कहता हं, तू चुप रह…ऐसी दया से मुझे न
तोड़…’ ‘
वह सहम गई।
”आज क्या देबू आया था?” वह खाना खाकर बिस्तर पर लेटा था।
”आया था…सुनो, तुम्हें उससे डर नहीं लगता?”
”किससे? …देबू से…?”
”नहीं, अनाज वाले लाला से…तुम्हारी शिकायत कर दे तो?” वह साहस करके कह गई।
वह धीमे परंतु कठोर स्वर में बोला, ”नहीं।”
”क्यों नहीं…?”
”वह लोगों को लूटता है, मैं उसको लूटता हूं।”
”उसका लूटना ग़लत है तो तुम्हारा भी…”
वह उठकर बैठ गई। अमर कुछ न बोला।
”सुनो, तुम्हें भगवान से भी डर नहीं लगता…?”
”तुम जो डर लेती हो…।”
”उससे क्या होता है…”
”होता है…मेरी करनी मेरे पास रहती है। तुम्हारी तुम्हारे पास…बोझ से मरूंगा तो मैं ही…।”
”ऐसा मत कहो…” पति का मुंह अपनी कांपती हथेली से ढंकती हुई वह बोली, ”हम-तुम दो हैं क्या…?”
फिर वही अंधेरे को घूरती उसकी अबूझ चुप्पी।
”हां, किसी-किसी जगह पर पहुंचकर हम-तुम दो हैं…!”
”कैसे?”
”तुम इसे समझ नहीं सकतीं…। चलो छोड़ो…! मां की तबीयत अब कैसी है…?”
उसने आंखें फाड़कर पति को देखा, ”क्यों, क्या तुम घर में नहीं रहते?”
”मैं? मैं घर में कहां रहता हूं…! कब होता हूं मैं घर में…? मेरे भीतर
तो…” स्वर में एक अबूझ विषाद।
”किस तरह की बातें कर रहे हो तुम…? सुनो, एक बात मानोगे?”
”हूं…।”
”छह महीने के लिए तुम देबू की पढ़ाई छुड़वा दो…वज़ीफे से कुछ मदद होगीछह महीने बाद भी डॉक्टर बन जाएगा तो क्या फर्ष्कष् पड़ेगा।”
”नहीं सरना…देबू की अपनी ज़िंदगी है, अपनी किस्मत…। उसे अपने लिए दांव पर नहीं लगाउं+गा।”
”पर उसकी भी तो कोई जिम्मेवारी है।”
”है, पर मेरी भी तो उसके लिए कोई जिम्मेवारी है।”
”तो फिर…फिर मुझे स्वेटर बुनने की एक मशीन दिला दो…इसमें बुरा तो कुछ नहीं…सब घर बैठे-बैठे करते हैं…”
”दिला दूंगा, अभी तो…जानती हो, मां की बीमारी में सब कुछ हाथ से निकल गया।”
”जानती हूं,” आवाज़ कटार हो आयी।
”उनका इसमें क्या दोष है सरना…? क्या इसके लिए तुम उन्हें माफ नहीं कर सकतीं…?”
सिर से पकड़ी जाकर वह खिसिया गई। फूट पड़ी, ”तो फिर मैं क्या
करूं…? क्या करूं?”
”तुम कुछ मत करो सरना!” एक पीड़ित शैथिल्य से भरा वह सरना को अपने साथ सटाते हुए बोला, ”मेरे पास बनी रहो…इसी तरह…हमेशा…सहना आसान हो जाता है,” पत्नी की हथेली खींचकर उसने अपनी छाती पर रख ली और अपनी उंगलियों से उसकी खुरदरी उंगलियों के पोरों को छूता रहा।
दूसरे-चौथे दिन उसे साइकिल पर बोरी लादकर ले जाते देख सरना का जी
धसक जाता। एक रात पहलेपति का गुमसुम खाट पर बैठे होना…आधी रात गए घिस-घिस आवाज़ें…पसीने से लथ-पथ शरीर…श्रांत होकर सुबह उठना
…निर्वाक्, इधर से उधर डोलना…अक्सर सब कुछ असह्य लगने लगता। एक दिन डरते-डरते बोली, ”किसी दिन तुलवा लिया तो?”
एक लंबी-सी लोहे की छड़अंदर से खोखली, सिरे से पैनी उसने दरवाज़े के पीछे से निकालकर पत्नी के सामने डाल दी। बिना खोले बोरी के पेट में जिसकी नोक भोंककर नमूने का अनाज जिससे निकालते हैं व्यापारीवह औज़ार।
”थोड़ा-थोड़ा हर बोरी से…इतना अनाज तो चूहे भी खा जाते हैं गोदाम में…।”
”तभी तो पसीने से लथ-पथ हो जाते हो…सुनो, कोई और रास्ता नहीं निकल सकता?”
”क्या चोरी का?” कड़वी-सी भड़ास फेंकता वह बोला।
वह आहत हुई। फिर भी दृढ़ता से बोली, ”नहीं, कमाई का…।”
”जिस दिन तुझे दिख जाए, मुझे बता देना…छोड़ दूंगा…। तुम लोगों के लिए ही…” बुदबुदाता हुआ वह बाहर निकल गया। पत्नी अपने ही शब्दों के ताप-संताप में झुलसती रही।
शाम को वह घर आया तो मुंह पर बादल नहीं थे। हाथ में दो बड़े-बड़े कांधारी अनार और संतरों का पैकेट लिये वह सीधा रसोई में घुसता चला आया। गीतू को सामने देख पैकेट नीचे रखे और उसे गोद में उठाकर चूम लिया।
गीतू पहले तो भौचक्क…फिर संतरे लेकर नाचने लगी।
गुल्लू बीच में झपटकर बोला, ”रहने दे, रहने दे, दादी के लिए हैं…डॉक्टर ने बताए हैं।”
”नहीं, तुम्हारे लिए भी हैं बेटे…दादी के लिए वहां रख आया हूं…लाओ, चाय लाओ…” बूट उतारकर वह खरखरी खाट पर पसर गया।
सरना व्यस्त-सी हो आयीएक अनजानी कृतज्ञता से न जाने उसके मन की कौन-सी कोर भीग आयी…पति को चाय का कप उसने कुरकुरे पापड़ों के साथ पास बैठकर पिलाया।
मां एक रात अचानक मर गई। देह औंधी ऐंठी हुई। एक टांग नीचे उतरने की मुद्रा में पाटी से नीचे लटकी हुई…गरदन आधी ऊपर को…आंखें जड़-स्थिर। बिस्तर ऐसी सलवटों से भरा…खूब छटपटाती रही हों जैसे…शायद उन्होंने खाट से उतरना चाहा हो।
वह और सरनादोनों धक् से रह गएअावाज़ ही न निकली। न गंगा- जल, न गीता-पाठ, न दीया, न बाती, न कोई पास…बच्चों का झुंड ज़मीन पर बेख़बर सोया हुआ!
घबराकर मां का शव उन्होंने नीचे उतारा और एक अपराधी आकुलता से बच्चों को झकझोर दिया। पास-पड़ोसी जब तक आए…मौत एक यथार्थ बन चुकी थी।
अमर का मन अंदर से रह-रहकर छीजता रहा।
दाहकर्म…दान, सब उसने समुचित श्रध्दा से किए। मां पहले भी मात्रा उपस्थिति भर थी…पर यह अनुपस्थिति तो? …क्या था जो पसलियों में सलाख की घोंप की तरह उसे बींधता रहा।
दो ही दिन पहले तो…खाट से लगकर रखे मोढ़े पर बैठे अमर की गोद में मां ने अपनी शिथिल कलाई डाल दी। वह चौंका, हाथ का अख़बार उसने नीचे रख दिया, ”कुछ चाहिए मां…?”
”नहीं, कुछ नहीं।” बेहद थकी-टूटी, भरी-सी आवाज़।
मां ने अपना हाथ उसकी गोद से वापस न लिया। एक बोलता हुआ दर्दीला स्पर्श उसे छूता रहा।
”मां!” बचपन के किसी भूले हुए आवेग का झोंका उससे आ लिपटा, ”कुछ कहना चाहती हो मां?”
”नहीं रे! सोचती हूं, तेरे कच्चे कंधों पर कितना बोझ पड़ गया और ऊपर से मैं करमजली…” फिर फफक कर रो पड़ी। वह विचलित हो गया।
”किसी ने कुछ कह दिया है तुम्हें मां?’ उसका इशारा पत्नी की ओर था।
”नहीं, नऽऽहीं रे…” रो पाने में भी असमर्थ मां का स्वर एक घुटी हुई चीख़ की तरह बिखरा।
वह मां के सिर पर हाथ फेरता रहा। मां के बाल रस्सियों के से सूखे, खुरदरे हो गए थे…और अब आंसुओं की धाराओं से गीले हो रहे थे।
”मां! जी छोटा न कर।”
मां के भीतर कोई फोड़ा फूट गया था। सिसकते हुए बोलीं, ”तेरे बाबूजी गए तो लगता था…लगता था, दस घड़ी न जिया जाएगा…अब दस साल से जीती हूं…”
”मां, तुम अच्छी हो जाओगी…” एक खोखली-सी सांत्वना उसके मन में उभरी, फिर होठों में ही डूब गई।
”नहीं! नहीं…!” मां के भीतर उबाल उठा था, ”मेरे जीने में क्या धरा है…तू कमा-कमाकर खुट रहा है…एक बात कहूं बिटवा…”
”हूंऽ।”
”मेरी मिट्टी तो वैसे ही उठेगी…तू क्यों मेरे कारण बच्चों के मुंह से ग्रास छीने है…?”
”तुम्हें क्या हो गया है मां?”
मां फिर फूट पड़ीं, ”सच कहूं बिटवा, मेरा तो दवा-दारू, डॉक्टर, सेवा
सब होता है…और तू रात-रातभर इस मोढ़े पर निढाल पड़ा रहता है। मैं, क्या अंधी हूं? …तू मेरी बात मान, कुछ दिनों के लिए देबू की पढ़ाई छुड़ा दे।”
”देबू अपने उद्यम से पढ़ता है, मां!”
”उसका उद्यम तेरे किस काम…?”
”तू चिंता न कर मां!” एक गहरी सांस उसने भीतर ही रोक ली। ऐसी सहानुभूति से खखोलकर मां उसे अपने ही सामने नंगा कर देती है। कितना दारुण होता है यह, मां अगर जानती…
तीसरे ही दिन मां का यूं मर जाना…इन सब बातों की स्मृति उसे ख़ूब खली। मां के बक्से से निकलींबाबूजी की कुछ बहुत पुरानी चिट्ठियां…बाबूजी के साथ का एक मटमैला मुड़ा-तुड़ा फोटो…थोड़े-से कपड़े…एक शॉल…दो अंगूठियां…दो जोड़े चांदी के बिछुए और सत्तााईस रुपये तीस पैसे…रुपयों को हथेली पर रखे देखता रहा वहमां की जन्म-भर की पूंजी…।
बच्चे और सरना। दत्ताचित्ता पिछले कमरे में जन्माष्टमी की झांकी सजाने में लगे थे। पीछे का अंगड़-खंगड़ सरना ने अपनी पुरानी रेशमी साड़ी से ढंक दिया। पास-पड़ोस से खिलौने और रंग-बिरंगी तस्वीरें मांग ही ली थीं, तो दो-तीन पड़ोसिनों को आरती के लिए न्यौत भी आयी। न्यौत आने पर प्रसाद बनाने का अतिरिक्त उत्साह भी उसमें आ गया। केले, अमरूद मंगाते गुल्लू को वापस टेरकर बोली, ”दो-एक सेब और एक पाव भर अंगूर भी लेते आना। भगवान का काम है।” गद्गद सरना अंदर-बाहर जाते कहती। गुल्लू चला गया तो उसे कलाकंद की याद आयी… ”यह सोच मरी रह-रहकर आती है…बच्चा बेचारा…? शायद अभी दूर न गया हो…,” वह दौड़ी-दौड़ी बाहर आयी।
गुल्लू तो निकल गया था, पर पति दहलीज पर बैठा बीड़ी फूंक रहा था चेहरा घिरा हुआ, भवें घनी होती हुईं।
”छि:-छि:…त्योहार के दिन तो रहने दो…वैसेई उपास का दिन है…यहां कैसे बैठे हो? अंदर चलो, देखो बच्चे कैसे…”
”नहीं, अभी बाहर जाना है,” वह बात काट देने की नीयत से बोला।
”वहां?” फिर बिना जवाब सुने बोली, ”पहले कहा होता। नाहक़ गुल्लू को दौड़ाया। तुम्हीं सब चीज़ें लेते आते।”
वह कुछ न बोला। ढलती शाम को वैसे ही निर्विकार भाव से देखते हुए आधी पी हुई बीड़ी को एक कोने में फेंक दिया।
”कहां जाओगे, इस वक्त?”
”बनिये के यहां…सुबह उसकी स्टॉक चेकिंग हो रही थी, बोला शाम को आना।”
”कल चले जाना,” फिर कुछ सोचकर स्वयं ही बोली, ”नहीं, अभी दे
आओ…। न हो, एक गिलास दूध पी लो…आरती-प्रसाद में तो आज देर लगेगी?’ ‘
”नहीं।”
वह इतने छोटे में उत्तार देता है कि बात को आगे जाते-जाते लौट आना पड़ता है। ”तबीयत तो ठीक है न?” वह उसका माथा छूती बोली।
”हां…बिलकुल,” पत्नी के हाथ की करुणा उसने हौले से परे सरका दी।
पूजन पूरा हुआ। आरोपित प्रसव और कृष्ण-जन्म उपलब्धि के तन्मय उल्लास में बही जाती पत्नी ने अचानक थाली में पैसे डालने को तत्पर उसके हाथ अधबीच थाम लिये। थाली में पड़ते-पड़ते पैसे उसके हाथ में ही थमे रह गए। वह मुंह-बाए देखता रहा। पड़ोसिनें भौचक्क, बच्चे विस्मित। अपने में लौटते हुए सरना ने फौरन सहज होते हुए कहा, ”सवी, जा…जा मेरा बटुआ उठा ला, छोटी संदूकची में धरा है।”
आरती में फिर अमर का ध्यान न लगा। बार-बार पिछड़ता जाता अपना ही स्वर, घर के स्वामी की-सी बुलंद तन्मयता से शून्य। बच्चों और औरतों की छोटी-सी भीड़ में से खिंचता-खिंचता वह एकदम पीछे सरक लिया। पत्नी प्रसाद बांटते इधर-उधर नज़रें दौड़ाती उसे ढूंढती रही। उसने चाहा कि वह प्रसाद पहले पति को देती। पर वह वहां नहीं था। सहन में तुलसी के झाड़ के नीचे के सूखे पत्तो बटोर रहा था।
”मन बुरा न करो। …यह सब भी तो तुम्हारा लाया हुआ है…पूजा में वह पैसे खर्च करना ठीक नहीं था…भगवान का काम है…।”
”मां के मरने पर इतना खर्च हुआ, तब तो तू कुछ नहीं बोली,” एक रूठा हुआ उपालंभ आवाज़ में था।
”कैसी बातें करते हो?” वह तनिक आहत होकर बोली, ‘वह मौत का काम था। मां से कभी दो हाथ करते देखा है क्या तुमने मुझे?”
”मैंने कब कहा?” पत्नी के स्वर की शिकायत पहचान कर वह नरम होता हुआ बोला।
”तुम इतने सुस्त क्यों हो गए? तुम ही बताओ, मैंने ग़लत कहा है?”
”ग़लत-सही मुझसे न पूछ सरना! …यह समझना मेरे बस का नहीं। मैं सब लाकर तुम्हें दे देता हूं। तू जाने, तेरा भगवान जाने।”
”भगवान तुम्हारा नहीं है क्या?” पत्नी ने न जाने कैसे भय से आंखें फाड़कर पूछा।
”मुझे पता नहीं…” बुदबुदाता-सा वह बाहर निकल गया।
औरतें देर तक अंदर शोर करती रहीं।
मां की बरसी उसने कई ब्राह्मणों को न्यौत कर की। ऐसा करते पिता के नाम के श्राध्दों की याद करके हुमका भी। अब तक दफ्तर में ही काम करते लीचड़ जोशीजी की पालथी के नीचे पिता के श्राध्द की चौकड़ी बनी रही। वह भी मां के जीते-जी। यह अशुचिता उसे तब भी अखरती थी और नए-पुराने दु:खों की अनंत पोटलियों के बीच आ धरती थी। ऐसा रोग…पिता को अस्पताल भरती करा पाया होता तो…। डॉक्टर ने तो कहा था, ”ऑपरेशन उन्हें ज़िंदा रखने के लिए है, मारने के लिए नहीं।” पर मरना-जीना भाग्य की बात है…भाग्य और कर्म का हिसाब किस जगह पर तय होता है, वह समझ नहीं पाता…। जी बहुत दु:ख जाता है तो फैसला भाग्य के पक्ष में कर लेता है।
कई और ब्राह्मणों को आया देख जोशीजी कसमसाए, परंतु अमर ने उनके प्रति उदारता ही बरती, ”आप तो घर के ही ठहरे,” कहकर उन्हें भी संतुष्ट किया। मौत के उत्सव में व्यस्तता से इधर-से-उधर डोलती सरना अपनी ही आंखों में बड़ी होती रही।
अब अक्सर अमरौती खाकर उतरी नायलॉन की साड़ी को वह अलगनी पर टांगकर फूल-छपी कड़क कलफदार धोती पहने अपने पर मुग्ध होती बार-बार पति की तरफष् देखती।
वह ठगा-सा उसे देखता रहता। जाने कैसी अबूझ-सी छाया उसके चेहरे से गुज़रती आसपास की वस्तुओं पर जाले की तरह जा लिपटती। ठंडे-से स्वर में पूछता, ”यह कब लाई हो?”
”शंकर-बाज़ार में सेल लगी है न!” वह पुलकती-सी पास दुबककर कहती, ”सुनो सवी के लिए भी मैंने धीरे-धीरे चीज़ें जमा करना शुरू कर दी हैं। ब्याह के समय चार चीज़ें घर से निकल आएंगी तो तुम्हारा हाथ भी…”
”तुम तो कहती थीं, प्राणनाथ जी के यहां शादी करेंगे तो कुछ ख़ास देना नहीं पड़ेगा?”
”वह तो ठीक है। सामने वाला तो कहता ही है…पर अपना भी तो कुछ फर्ष्ज बनता है…”
”फर्ष्ज छोड़ो, सरना! …किसका किसके लिए फर्ष्ज बनता है, और क्यों, यह मेरी समझ में नहीं आता।”
”नई-नई-सी बातें करते हो तुम तो…”
”हां, करता हूं! प्राणनाथ जी की हैसियत को हमारी चार चीज़ों की क्या परवाह पड़ी है?”
”लड़की का रूप-गुण देखकर ले रहे हैं तो इसका यह मतलब तो नहीं…आखिर तुम भी बाप हो…”
”तुम खुद ही केंचुली से निकलना नहीं चाहतीं…और मुझे भी…” अपना वाक्य हवा में टांगकर वह बाहर निकल गया और चहलकदमी करने लगा।
कूड़ा फेंकने वह बाहर आई तो चौंकी, ”अरे, मैं तो समझी थी तुम जगदीप के यहां गए हो…चलो, खा लो।”
हाथ धोकर थाली पर बैठा तो पत्नी ने पीतल का बड़ा कटोरा आगे सरकाते हुए कहा, ”साग चाहे रहने दो…यह खा लो।”
”क्या है यह?”
”थोड़ी खीर बना ली थी।”
खीर की मात्राा देखकर वह चौंका, ”बच्चों को नहीं दी?”
”बच्चे तो ख़ूब छक चुके…हम दोनों रह गए हैं।”
वह थाली को आगे सरकाता हुआ बोला, ”तो फिर तुम भी खा लो साथ ही।”
इस आमंत्राण पर वह भीतर से भीग आयी। उमगाती-सी मुंह देखती रही पर वह निर्वाक् खाता रहा। फिर सोचते हुए बोला, ”आज बच्चों में से किसी का जन्मदिन तो नहीं…तभी तुम खीर बनाती हो।”
वह खिलखिलाकर हंस पड़ी, ”इस महीने में कौन जन्मा था अपने घर…? तुम तो बस…”
न साग अमर ने पीछे सरकाया, न खीर जमकर खायी, ”रख दे, सुबह बच्चे खा लेंगे।”
”तुम भी अजीब हो, कुछ अपनी सेहत का…”
”कौन-सी सेहत?” वह ऐसे कड़वे काठिन्य से बोला कि सरना को मुंह उठाकर देखना पड़ा।
”सेहत भी दो-चार होती हैं क्या? तुम भी जाने कैसे…”
”अच्छा, बस-बस!”
वह अपने बिस्तर में दुबक लिया। पत्नी सोने आई तो जैसे टोहती रही…छाती पर हाथ रखकर। अंधेरे को अपलक घूरता वह निश्चल पड़ा रहा।
प्रो. प्राणनाथ आज फिर आए थे। वही आते हैं। जबकि जाना अमर को चाहिए। उनका आना सरना के पैरों में पंख लगा देता है। अमर के पास सवी को लेकर छोटा-सा गर्व भी नहीं थाउसका रूप जो जन्मजात था और हाई स्कूल में बोर्ड में प्रथम स्थान, उसके अपने परिश्रम का फल। उसका तो बस…उसकी तो बस वह बेटी थी। इसीलिए वह पत्नी के उत्साह में इतना भाग नहीं ले पाता था। सवी पर बरसते उनके वात्सल्य को अविश्वास से देखता रह जाता था।
गुल्लू का मिडिल इन गर्मियों तक…सवी की शादी इन सर्दियों तक। इस साल तो देबू भी तैयार हो जाएगा…तो बस!
शेव करते शीशे के सामने खड़े अमर को अपने चेहरे के पीछे न जाने कितनी लहरियां कांपती नज़र आयीं। लहरों की उस बावड़ी में वह अपने भविष्य का चेहरा टटोलता खड़ा रहा।
खड़ा रहता यदि धोती के सिरे से हाथ पोंछती पत्नी उसे न चौंकाती, ”सुनो, सवी के लिए एक कंठी बनवाना है।”
”क्या?” आश्चर्य के रास्ते धरती पर लौटता वह बोला।
”हां! हां! कंठी…। तुम्हें तो मालूम है, सवी की कब की साध है। मांजी कब से सवी के लिए रखे थीं…बिक गईं…! खैर, छोड़ो पिछली बातों को…”
”प्राणनाथ जी को इन बातों में विश्वास नहीं, रोज़ इतनी बातें कहते रहते हैं, सुनती नहीं हो?”
”उनके कहने से क्या होता है?”
”होता क्यों नहीं, एकदम दूसरे ख्यालों के हैं…नहीं तो लड़के वाले होकर रोज-रोज़ यों चले आते…?”
”वह तो देखती हूं…लड़की की ऐसी ममता करते हैं…छोड़ो, बातों में न उलझाओ…तुम कहो तो मैं आज सुनार के पास जाउं+?”
”नहीं,” वह अलिप्त-सा चेहरे पर साबुन घिसने लगा।
”क्यों?” एक उद्दंड-सा क्षोभ पत्नी की आवाज़ में भी तिर आया।
”क्योंकि उसे कंठी देने का मेरा कोई इरादा नहीं है। कम-से-कम दो तोले की बनेगी…और सोने का भाव मालूम है?”
”मालूम है…। पर कब से साध लिये है छोरी…।”
”इतनी और साधें पूरी हो रही हैं…यह सोचकर सबर करो। एक इसी साध को लेकर मरने की क्या ज़रूरत है? कभी सोचा था तुमने या उसने कि ऐसे घर जाएगी?”
”उसकी किस्मत! उसकी सज़ा तुम उसे क्यों दे रहे हो?”
”सज़ा किसी को नहीं मिलती…सिर्फ मुझे मिलती है…और सब तो…” बाकी का वाक्य वह अंदर घुड़क गया, खीजता हुआ बोला, ”जाओ, मुझे शेव करने दो…देर हो रही है।”
”तुम असल में इस वक्त ज़ल्दी में हो,” कहती हुई वह रसोई में लौट गई, उद्विग्न उतावली में वह तैयार होकर दफ्तर चला गया।
शाम को जब लौटा तो नहीं जानता था कि वह प्रसंग अभी उनके बीच जीवित है। पत्नी ने यह कहकर कि इस समय तुम्हें जल्दी है, लगाम अपने हाथ में रख ली थी। बात शुरू होते-होते ही प्रोफेसर प्राणनाथ आ गए, और उनके साथ ही घर की हवा एक ताज़ा सुगंध से भर गई। इतनी सहज आत्मीयता से वह यहां बैठते-उठते कि उनके जाते-जाते तक तो घर का वातावरण हलका और तरल हो उठता।
पति को उसने हलका सहज देखा तो कलाई थामकर बोली, ”क्या इतनी- सी बात भी नहीं रखोगे?”
उसे उसी क्षण जैसे ताप चढ़ आया। झिड़ककर बोला, ”बेवकूफष्ी मत करो
…कभी तुम अपने लिए कहतीं तो बात भी थी…हिरस समझ सकता हूं…सवी को क्या कमी है? एक-एक लड़का है उनका…ज़मीन-जायदाद है…ऐसे भले विचार हैं…। आगे भी तो देखना है मुझे…पता नहीं, किस-किससे पाला पड़े…दुनिया में सब प्रोफेसर प्राणनाथ ही तो नहीं होते…”
”क्या हुआ…गीतू की शादी तक तो देबू भी डॉक्टर हो जाएगा।”
”डॉक्टर क्यों कहती हो, कहो कुबेर हो जाएगा। इतना भरोसा मैंने किया है किसी का आज तक…?”
”तुमने नहीं किया तो क्या, उसका भी खून इतना सफेद तो नहीं होगा।”
”मैं कर ही क्या रहा हूं उसका, जो आशा करूं? वज़ीफा लेता है, टयूशन करता है, हम लोगों पर तो दो रोटी की मोहताजी भी नहीं रखी है उसने…”
”वह न करे, पर तुम अपनी लड़की के लिए ऐसे पत्थर दिल क्यों हो गए हो…?” चोट करने के तेवर में आ गई थी पत्नी।
”सरना…चुप रहो…मुझे तैश न दिलाओ…” पास रखी काठ की कुर्सी पर बैठ गया वह आक्रामक क्रोध में तपता।
”ऐसी बड़ी बात नहीं कह दी है मैंने कि तुम इस तरह गुस्साओ…आखिर लड़की…”
”ओह! सरना, तुम इतना तो सोचो! मैं कहां से करूं…कैसे करूं…तुम क्या नहीं जानतीं…?”
”इतना करते हो, तो दो-चार बोरियां और…”
सरना की आवाज़ की निरुद्वेग ठंडक और आग के तीरों से उसका पोर- पोर बिंधना। जाने कैसी तेज़ी से वह उठा। फौलादी पंजों से पत्नी के कंधे झिंझोड़कर उसे खाट पर धक्का देकर थरथराता हुआ बोला, ”तू…तू…तू भी…मर गई है मेरे साथ। तेरे पुन्न को देखकर जीता आया था मैं अब तक…मेरा अपना ही बोझ क्या कम था मेरे लिए…?”
Download PDF (तुम भी )
तुम भी – Tum bhi