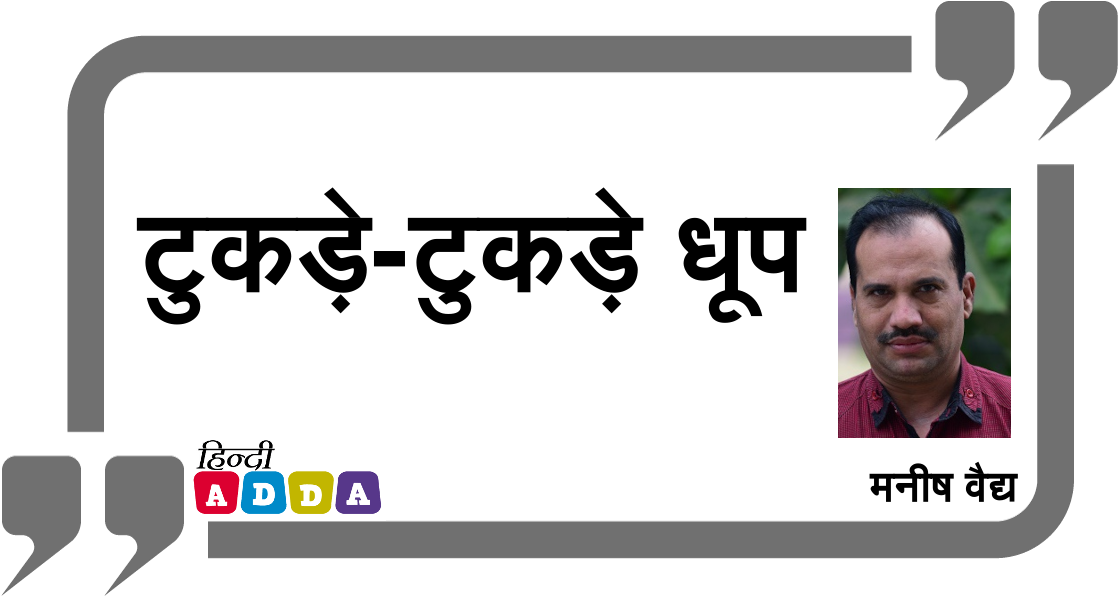टुकड़े-टुकड़े धूप | मनीष वैद्य – Tukade-Tukade Dhoop
टुकड़े-टुकड़े धूप | मनीष वैद्य
खपरैलों वाले इस घर में आसमान से धूप के कई टुकड़े उतर आते। समय के साथ-साथ धूप के इन टुकड़ों की जगहें बदलती रहतीं। सुबह से शाम तक धूप के ये टुकड़े पूरे घर में चहलकदमी करते रहते। खपरैलों के सुराखों से धूप के छोटे-छोटे हिस्से यहाँ-वहाँ से झाँकते रहते। इन टुकड़ों का आकार छोटी रोटी की तरह गोल होता। मानो किसी ने कोशिश कर चाँद की तरह इन्हें गोल-गोल बना दिया है। खपरैलों के सुराख से दाखिल होते हुए नीचे घर के कच्चे फर्श पर आते-आते धूप के इन टुकड़ों में बहुत छोटे धूल के कणों की तरह कुछ होता। अणु और परमाणुओं की तरह। ये कण इतने छोटे और महीन होते कि इन्हें गौर से देखे जाने पर ही देखा जा सकता। धूप के इन टुकड़ों को घर में आवाजाही की पूरी छुट होती। ये कहीं भी जा सकते और कहीं से भी लौट सकते। ये उछल कूद कर घर के सामानों पर चढ़ जाते। धूप के ये टुकड़े कभी पीतल के हंडे पर पड़ते तो पूरा घर सोने की दमक से भर उठता। ये टुकड़े जब बरतन में भरे पानी पर पड़ते तो पूरा घर चाँदी की चमक से भर उठता। सुबह के साथ धूप के टुकड़े घर में निकल आते और दिन भर की चहलकदमी के बाद शाम के धुँधलके में कहीं खो जाते। अगली सुबह वे फिर लौट आते मानों रात उन्हें यहीं झपकी लग गई हो और आँखें मलते हुए वे फिर जाग गए हों। इस तरह वे घर की रोजमर्रा में शामिल हो चुके थे…
रात के अँधेरे में खपरैलों के बीच न कोई सुराख नजर आता और न धूप के टुकड़े। हाँ, चाँदनी रातों में जरूर आसमान का चाँद इन सुराखों से घर में झाँकता सा नजर आता। अँधेरी रातों में शायद अँधेरे के टुकड़े भी इन सुराखों से आते रहे हों। अँधेरों के बीच अँधेरे के टुकड़े पहचाने नहीं जाते, लिहाजा यह मन लिया गया कि धूप के टुकड़ों का तरह अँधेरों के टुकड़े नहीं होते। रात में खपरैलों के बीच की जिन जगहों से घर में जलती चिमनी की पिलपिली रोशनी बाहर के घुप्प अँधेरे के बीच टिमटिमाती रहती, गोया किसी पहाड़ी के नीचे से बस्ती की बत्तियाँ नजर आ रही हों। रोशनी पूरी तरह अनगढ़ होती। न कभी उनके बीच कोई निश्चित अनुपात और न ही कोई निश्चित दूरी। ठीक उसी तरह जैसे किसी बच्चे ने सफेद कागज पर रंग के कुछ छींटे डाल दिए हों। कहीं ज्यादा तो कहीं कम। खपरैलों के बीच की जगहों से आती हुई रोशनी की हलकी परछाइयों से अँधेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अँधेरा खासा बना रहता और दूर तक पसरा हुआ। रोशनी की यह झिलमिल परछाई अगले सात जनम तक उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी लिहाजा अँधेरा अपने पूरे आलसीपन के साथ पसरा रहता।
खपरैलों के बीच की जगहों से इस घर का पुराना नाता था। शायद तब से जब यह घर बना होगा या उससे भी पहले जब घर बनना शुरू हुए होंगे। घर होते तो खपरैलों के बीच जगह जरूर होती। खपरैलों के बीच की जगह का भर जाना शायद घर के न होने की तरह था। घर की अन्य अनिवार्य शर्तों में अघोषित रूप से एक यह भी शर्त थी। खपरैलों के बीच की जगह ही शायद खपरैलों को जोड़े रखती। यदि जगह नहीं बचती तो लोग धूप की उजास और अँधेरे को ही भूल जाते या यह भी होता कि शायद उन्हें समय का ही भान नहीं रहता। धूप के टुकड़ों से दिन का समय और सुराखों से झाँकते आसमान के तारों से वे रात के पहर बताते।
धूप के टुकड़े लगातार अपनी जगह बदलते रहते। कभी रोटी की तरह थाली में नजर आते लेकिन थोड़ी ही देर में थाली से छिटक जाते। भूख बाकी रह जाती पर धूप के टुकड़े थाली से बाहर हो चुके होते। माँ के साथ अक्सर ही ऐसा होता। सबको खिलाने के बाद जब वह अपनी थाली परोसती तो जल्दी ही धूप का टुकड़ा थाली से छिटककर खाली परात में दौड़ने लगता जहाँ अब रोटियाँ नहीं, पपड़ाये हुए आटे की परत चिपकी रहती।
धूप के टुकड़े कभी छुट्टी पर नहीं जाते। वे कभी नागा नहीं करते। मानो सूरज के साथ उनका आना जरूरी ही हो। घर में चहलकदमी करते धूप के टुकड़े सदियों से इसी तरह आते रहे। बिना अपने आने की मुनादी पीटते हुए। मौसम आए और चले गए, त्यौहार आए और चले गए, शादी-ब्याह, जनम-मरण सब कुछ चलता रहा। लेकिन धूप के टुकड़ों का लगातार आना जारी रहा, सदियों से इसी तरह। आज भी वे आ राहे होंगे और शायद सदियों तक आते रहेंगे। यूँ ही बिना नागा किए।
साल-दर-साल खपरैलों को आल-चाल कर दिया जाता लेकिन धूप के टुकड़े अपने लिए जगह निकाल ही लेते। हर साल आषाढ़ के महीने में पिता निसरनी लगा कर खपरैलों की छत पर चढ़ जाते। माँ उन्हें नए खपरैलों का टोपला दे आती। पिता एक सिरे से खपरैल हटाना शुरू करते। मानो घर की छत उघड़ रहे हों। फिर टूटे खपरैलों के टुकड़े, तुअर संटी के टुकड़े और धूल-धक्कड़ को खोडिए की बुहारी से झाड़ते। फिर साबुत खपरैलों से नई छत बनाने लगते वे जिस हिस्से की खपरैल हटाते वहाँ का आसमान घर में उतर जाता, धूप के साथ। खपरैल हटाने के बाद कंकाल की तरह निकल आई बल्लियों और साँकटियों पर फिर से खपरैलों का काम घंटों तक चलता। खपरैलों के टुकड़ों, संटी के टुकड़ों और धूल-धक्कड़ से पूरा घर भर जाता। बल्लियों और साँकटियों के बीच से सारा कचरा पूरे घर में छा जाता।
बरतनों, बिस्तरों, टिन के डिब्बों, पिता की किताबों, हंडे-मटके, माँ के सिंगारदान-सब कुछ धूल-धक्कड़ से पट जाता। घर का कोई कोना साबुत नहीं बचता। यहाँ तक कि भगवान भी। घर के एक कोने में लकड़ी का छोटा सा पाटिया था, जिस पर तमाम भगवान मौजूद रहते थे। राम, हनुमान, कृष्ण, दुर्गामाता, शंकर, गणेश, विष्णु,लक्ष्मी और गरुड़। यानी पूरा देव परिवार। पिता इसे पाटिया नहीं सिंहासन कहते। वे अपनी पूरी उम्र इसे सिंहासन ही कहते और शायद मानते भी रहे। उनके लिए शायद जरूरी भी था ऐसा मानना कि इतने महान भगवान अपना देवलोक छोड़कर जब इस छोटे से कच्चे मकान में आएँगे तो लकड़ी के पटिये पर नहीं बल्कि सिंहासन पर ही बिराजेंगे। तो खपरैलों की आल-चाल के दौरान तमाम धूल-धक्कड़ में अन्य सामानों की तरह देव परिवार भी दब जाया करता। पिता जब खपरैलों की पूरी आल-चाल के बाद छत से नीचे लौटते तो उनकी हालत भी उन्ही सामानों की तरह हो जाती जो घर में धूल-धक्कड़ से सने रहते। वे इस तरह धूल-धक्कड़ से सने हुए लौटते मानो अभी किसी युद्ध में गुत्थमगुत्था होकर आ रहे हों। कभी लगता कि वे एक आदिम लड़ाई के सिपाही हैं जो सदियों से इसी तरह लड़ी जा रही है।
बहरहाल, माँ बुहारी से एक-एक सामान देर तक साफ करती। कुछ घंटों की मेहनत के बाद घर पहले की तरह दिखने लगता। पहले की तरह नहीं, पहले से ज्यादा हल्का और साफ-सुथरा। पिता गरम पानी और उबटन-तेल के जरिये धूल-धक्कड़ से निजत पाने की कोशिश करते। माँ खपरैलों के टुकड़ों को अलग कर लेती। बाद में इन्हें पत्थर से बारीक पीसकर माँ खोर बनाती। यह खोर लीपन के साथ मिलाकर कच्चे फर्श पर लीपी जाती। इससे फर्श सीमेंट की तरह मजबूत हो जाता। पिता नहा-धोकर अपने भगवान से माफी माँगते, देर तक मंत्र बुदबुदाते हुए। पिता कहते –
यदक्षर पथभ्रष्टम मात्रहिनम च यद्भवेत
तत्सर्वम क्षम्यताम देव प्रसीद परमेश्वरम
उन्ही भगवानों से जो थोड़ी देर पहले तक उन्ही की तरह धूल-धक्कड़ से सने हुए थे।
पिता जब खपरैलों की आल-चाल करने चढ़ते तो लगता कि इस बार न तो कोई सुराख बचेंगे और न ही धूप का कोई टुकड़ा घर में दाखिल हो सकेगा। लेकिन पिता की तमाम कोशिशों के बावजूद साल-दर-साल सुराख बच ही जाते। खपरैलों के बीच की जगह से अगली सुबह फिर धूप के टुकड़े उतरने लगते। यह धूप के टुकड़ों की जीत थी या पिता की कोशिशों की हार। हालाँकि ऐसी लडाइयों में हार-जीत तय कर पाना मुमकिन भी नहीं होता। ये लड़ाइयाँ ही ऐसी होती हैं, निरंतर चलने वाली, बिना हार-जीत की परवाह किए, शायद कभी न खत्म होने के लिए, अनिर्णीत ही रह जाने के लिए, खपरैलों के बीच सुराखों और पिता की कोशिशों के बीच भी ऐसी ही लड़ाई थी जो बरसों से इसी तरह जारी थी।
भादौ के महीने में जब जोरदार बारिश होती तो पिता की तमाम कोशिशों के बावजूद खपरैलों के बीच की इन्ही जगहों से बारिश का पानी घर में चूने लगता। पानी चूने की वजह सेघर-गृहस्थी का अधिकांश सामान भीग जाता। कभी-कभी तो साबुत बिस्तर लगा पाने लायक जगह भी नहीं बचती। तब पिता सारी रात सो नहीं पाते। तेज बारिश की रातों में वे चूने वाली जगहों पर बरतन रखते। बाल्टी, तगारी, तपेला, परात यहाँ तक कि लोटे और गिलास भी। फिर इनके भरते जाने और खालीकर इनका पानी फेंके जाने के काम में माँ और पिता देर तक भिड़े रहते। इस मुसीबत से बचने का कोई विकल्प नहीं होता। विकल्प था लेकिन वह उनके बस में नहीं था। जिस घर में रोटियों की कीमत भारी लगे वहाँ अँग्रेजी कवेलू का खर्चा कैसे उठाया जा सकता था। खैर, माँ और पिता ने इसे विकल्पहीन करार दे दिया था। फिलहाल इसका कोई हल उनके पास नहीं था। सिवाय बरतनों में जमा पानी को उलीचते जाने के। पिता सोचते कि सारी बातें वैसी ही हों, जैसी चाही जाएँ, यह तो मुमकिन नहीं हो सकता। इच्छाएँ तो बहुत होती हैं। लेकिन सारी इच्छाएँ पूरी भी तो नहीं हो सकती। वे कहते – जिंदगी के कई रंग होते हैं। जिंदगी के रंग भी तो धूप के टुकड़ों की तरह आते जाते रहते हैं।
माँ-पिता की जिंदगी भी तो धूप के टुकड़ों की ही तरह जगहें बदलती रही बार-बार। नाना के यहाँ से माँ धूप के टुकड़ों की तरह उजास बिखेरती यहाँ पहली बार आई थी। माँ और पिता ने साथ-साथ मेहनत की तो पुश्तैनी उसर जमीन भी ऐसी लहलहाने लगी कि उसकी उजास से गाँव भर में रोशनी के सोते फूटने लगे। कहते हैं कि सुख के दिन ज्यादा दिनों के नहीं रहते। यहाँ भी नहीं रहे। माँ-पिता ने सुनहरे सपने देखना शुरू ही किया था कि तभी उन्हें किसी की नजर लग गई। आस-पास के दो कस्बों को जोड़ने वाली सड़क यहीं से निकली, ठीक उनके ही खेत की छाती पर से। खेत का जो थोड़ा मुआवजा मिला उससे दूसरी जमीन खरीदने के लिए पिता ने बहुत कोशिश की लेकिन इतने से पैसों में कहीं जमीन नहीं मिली। इधर पैसा लगातार खर्च होता रहा। और आखिर में न जमीन बची न पैसा। बची थी तो पिता के बाजुओं में इतनी ताकत कि कभी भूखे सोने की नौबत नहीं आई।
बारिश जैसे-जैसे तेज होने लगती, घर में साबुत जगहें कम होने लगती। माँ कभी बारिश को दोष देती तो कभी पिता की कोशिशों को। माँ का आरोप होता कि पिता ने खपरैलों की आल-चाल के दौरान छेद रख दिए। माँ ऐसे आरोप बरसों से लगाती थी इसलिए पिता अपने बचाव में केवल चुप हो जाया करते। माँ और पिता कई बार ऐसे वाकियों पर एक-दूसरे के लिए आरोप मढ़ते यह बात जानते हुए कि आरोप सही नहीं है। माँ और पिता के बीच इस तरह की तकरार कोई नई बात नहीं थी। आमतौर पर जब-तब होती रहती थी। दोनों ही इसे गंभीरता से नहीं लेते थे। चुप होकर छोड़ दिया करते।
पिता मन में सोचते कि अब इसे कौन समझाये, कोई आदमी भला अपने ही घर की खपरैलों की आल-चाल में छेद क्यों रखेगा। क्या उन्हें पता नहीं कि उनकी एक गलती से पूरा घर गीला हो जाएगा? माँ अक्सर ऐसे मौकों पर अपने गोरधन नाथ को याद करती जिन्होंने अपनी चींटी उँगली पर गोवर्धन पहाड़ उठाकर वृंदावन के अपने लोगों की घनघोर बारिश से हिफाजत की थी। माँ की बात पर न पिता ध्यान देते और न गोरधन नाथ। पर माँ को इसका कोई मलाल नहीं रहता। माँ उस वाकिए को याद कर अब भी सिहर उठती है जब एक घनघोर बारिश की पूरी रात उसने दरवाजे में खड़े-खड़े गुजारी थी, अपने दो बच्चों के साथ। उस रात माँ ने जिंदगी और मौत के बीच एक महीन रेखा पहचानी थी। यह वाकिया पिता कभी याद नहीं करते। उनका मानना है कि कड़वी यादों को सीने से चिपकाये नहीं फिरना चाहिए। ऐसे पल तो आते ही रहते हैं। इन्हें याद कर अपना जी क्यों छोटा करना… आगे बढ़ना है तो अच्छी बातें याद रखो और सब के साथ अच्छा करो तो तुम्हारा भी अच्छा ही होगा।
वह जन्माष्टमी की एक खौफनाक काली अँधेरी रात थी। शाम से ही रह-रह कर बारिश हो रही थी। रात का दूसरा पहर बीतते-बीतते तो मानो बादल ही फट गए। पिता पहले ही रिश्तेदारी के काम से बाहर गाँव गए हुए थे। पिता साथ होते तो माँ उन्हें ही भला-बुरा कहकर हिम्मत भर लेती। पूरा घर बारिश के पानी में चपड़-चपड़ कर रहा था। घर की कच्ची दीवारों से पानी रिस रहा था। चारों तरफ पानी ही पानी। बादल गड़गड़ाते तो दिल बैठने लगता। मन में तरह-तरह की चिंताएँ और आशंकाएँ उठ रही थी। दोनों छोटे बच्चे डर रहे थे। आसमान में बिजली दमकती तो खपरैलों के सुराख से होती हुई उसकी चमक फैलकर माँ की डरी-सहमी आँखों में कौंध जाती। इस रात बारिश का सामना करते हुए उसे पिता बहुत याद आ रहे थे। आज माँ हमेशा की तरह न तो गोरधन नाथ को याद कर रही थी और न ही पिता को भला-बुरा कह रही थी। माँ आज पिता की तरह चुप थी।
शायद चुप्पी के बीच कहीं भीतर की ताकत को इकट्ठा कर रही थी। आज तो मईपला (प्रलय) ही होने को था। बारिश कुछ पल के लिए थमती और फिर शुरू हो जाती। तीसरा पहर बीतते-बीतते घर का पूरा कच्चा फर्श भीग चुका था। पूरा सामान और बिस्तर पहले ही भीग चुका था। जिस जगह माँ अपने छोटे-छोटे बच्चों के साथ बैठी थी वहाँ भी पानी आने लगा था। बौछारों से पूरा बदन भीग रहा था। वह ठंड से कँपकँपा रही थी। जैसे-तैसे बच्चों को बौछारों से बचाने की कोशिश कर रही थी।
इधर बारिश के साथ ओले भी शुरू हो गए। पहले मक्का के दानों की तरह और फिर छोटे नींबू के आकर के ओले। तेजी से गिरते ओले जब खपरैलों से टकराते तो खपरैल टूट जाते। जब खपरैल भी टूट-टूट कर गिरने लगे तो घर में पानी की रेलमपेल मच गई। घर का कोई सामान साबुत नहीं बचा। माँ को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या न करें। पड़ोस वाली रामकन्या पड़ते पानी में माँ को अपने अँग्रेजी कवेलू की छत वाले मकान में चलने के लिए बुलाने आई थी लेकिन माँ ने मना कर दिया। दिन का समय होता तो और भी… रात में दूसरे के घर अकेली औरत दो बच्चों के साथ, पिता होते तो उनके साथ जरूर चली जाती लेकिन आज नहीं… नहीं गई माँ, वहीं डटी रही।
माँ ने सोच लिया था कि जो होगा यहीं होगा इसी खपरैलों वाले घर में। खपरैल छार-छार होते रहे। गृहस्थी का सामान तबाह होता रहा। खपरैलों के टुकड़े बम की सी गति से यहाँ-वहाँ उड़ते रहे और माँ ने अपने अंदर की सारी ताकत को इकट्ठा कर लिया। वह दरवाजे की उस छोटी सी जगह में घंटों तक खड़ी रही बुत की तरह अपने दोनों बच्चों को भींचे हुए। दरवाजे के ठीक ऊपर लकड़ी के दो छोटे पटियों को जोड़ा हुआ था। इससे न तो सीधे पानी टपकता था और न ही खपरैल के टुकड़े सिर में लगने का डर था। बच्ची माँ के सीने से चिपटी थी और बच्चे को उसने अपने पैरों के बीच भींच लिया था। समय गुजरता रहा। चौथे पहर में बारिश कुछ कम होने लगी। पौ फटते ही उजाला टूटे हुए खपरैलों के बीच से घर में आने लगा था। बस्ती के लोगों ने देखा तो हैरत में पड़ गए। इतनी तबाही के बाद भी ये औरत और इसके बच्चे साबुत कैसे बच गए। यह तबाही की रात कई लोगों ने दूसरों के पक्के मकानों में बिताई थी। बस्ती के आधा दर्जन बच्चे, बूढ़े और औरतें मर चुकी थी।
उस दिन घर में चूल्हा नहीं जला। चूल्हे पर चढ़ाने लायक कोई सामान साबुत नहीं बचा था। ओलों और बारिश ने सब कुछ खत्म कर दिया था। सब कुछ। पिता लौट आए थे बाहर गाँव से। माँ पिता को उस रात का हाल सुनाती रही और पिता चुप से सुनते रहे। पिता ने कहा – खत्म होने की कोशिशों से खत्म नहीं होना और तमाम साजिशों और मंसूबों को नकारते हुए फिर-फिर उठ खड़े होना, फिर-फिर साबुत रह जाना ही तो जिंदगी है। धूप के टुकड़ों की तरह।
Download PDF (टुकड़े-टुकड़े धूप )
टुकड़े-टुकड़े धूप – Tukade-Tukade Dhoop