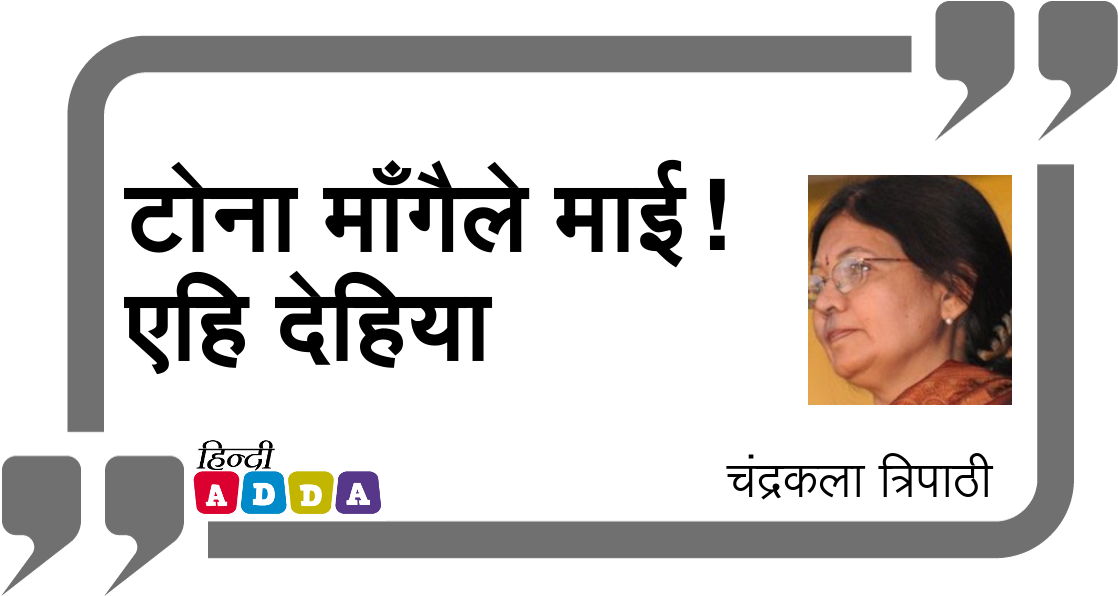टोना माँगैले माई! एहि देहिया | चंद्रकला त्रिपाठी – Tona Mangaile Maee Ehi Dehiya
टोना माँगैले माई! एहि देहिया | चंद्रकला त्रिपाठी
बाद के वर्षों का कोई दिन रहा होगा, जब पंडित की मुंडेर से बगीचे के जरिए दिखने वाले मौसमों के रंग मद्धिम पड़ते गए थे। हुआ यह था कि उस इलाके के एकमात्र बचे बगीचे के सारे पेड़ काट दिए गए थे। कुछ इमारतों के गुच्छे जल्दी ही उसमें उगने वाले थे। यह लगभग सारे भूगोल का हाल था। कस्बा, शहर, गाँव सब बदल रहे थे। सड़कें केवल आमद-रफ्त का जरिया नहीं रह गई थी बल्कि संस्कृति में बदल रही थीं। वे एक लगातार दिखने वाले ‘बाहर’ को बना रही थी। जो लोग बाहर दिखने वाले हाव-भाव, कपड़े-लत्तों और सलीके को अपना रहे थे, वे सब समय के मुताबिक थे। वे सभी लद्धड़ थे जिनके पास ‘बाहर’ बरतना वाला व्यवहार या कपड़े नहीं थे। पंडित के घर में भी कई लोग बाहर का रंग-ढंग सीख चुके थे। घर पहल के मुकाबले काफी बदल चुका था। पहले जहाँ केवल एक लंबा ‘ओसारा’ दो छोटी कोठरियाँ, एक कुआँ, एक आँगन और एक मझोला सा दुआरा था जिस पर सरकार के घर का रसद लाने वाली बैलगाड़ियाँ खड़ी रहती, अब वह तीन मंजिला घर में बदल चुका था। ये अलग बात है कि सारी मंजिलें वैसी ही सँकरी और पुराने किस्म की थीं। पंडित की नई पीढ़ियाँ भले इन मंजिलों पर स्थित कोठरियों को कमरा कहें, मगर थीं वे बेहद सँकरी रिहाइश जिनमें दो रोशनदान और एक चौकोर, लोहे के सीखचों वाली खिड़की थी।
बात बगीचे की हो रही थी। पंडित का पड़ोस था यह बगीचा। बगीचे और पंडित के घर के अगल-बगल वाली यह स्थिति किसी तिलस्मी कथा से कम नहीं थी। बगीचे का एक मँझोला फाटक उस गली में खुलता था जिसमें पंडित का घर था। या यूँ कहें कि सिर्फ और सिर्फ पंडित का घर था।
बगीचे में कभी बड़े सघन और पुराने पेड़ थे। उनके कलात्मक आकार भी थे। नकली गुफाएँ निर्मित थी, झरना था। एक सरोवर जैसा था जिसके किनारे सरपत की ऊँची घनी जुटान थी।
सरोवर में मछलियाँ थी। पानी गहरे रंग का था जिसके भीतर बदलते आकाश की आभा चिलकती रहती। पेड़ों में कैथ, जामुन, अमरूद, शहतूत मौसमी और आम थे। अमरूद के पेड़ नहीं थे। कहते हैं कि कई बार लगाए गए मगर कभी फले ही नहीं। बगीचा बंद रहा करता था। कुछ पहरे-वहरे भी हुआ करते थे मगर बाद के दिनों में तो स्कूली बच्चे न जाने कहाँ-कहाँ से सेंध लगाकर दाखिल हो जाते और घंटों उसमें छुपा-छुप्पी का खेल-खेलते। शाम को कोई बच्चा घर नहीं पहुँचता तो उसके माँ-बाप चौकीदार से चिरौरी कर भीतर का इलाका छान मारते। भीतर लैंप जले होते, प्रपात में खड़ी संगमरमर की जलकन्या नीली चमकती और झूला यूँ ही चर्र-मर्र डोलता। पंडित की नातिन की बेटी थी माधुरी, उसकी स्मृति में बगीचा दिनों-दिन रहस्यमय होता गया था।
बाद में उसने जब महल फिल्म का ऐसे ही डोलता रहस्यमय झूला देखा तो उस पूरे सीन पर उसका विश्वास जम गया था। खामोश सुनसान रात में कई छुपी हुई हरकतें थी। माधुरी को बगीचा ऐसा ही लगता। माधुरी, बन्नू, छगन, मंजू, पुष्पा, सुन्नी तोता, सब उस बगीचे में इकट्ठे जाते, कोई एक-दूसरे से अलग नहीं होता और अगर अलग हो जाता तो चिल्ला-चिल्लाकर बेदम हो जाता। बगीचे से जुड़ी कई कहानियाँ थीं जिनमें बड़े सारे रहस्य थे। बगीचे में मौसम प्रकोप की तरह घूमते थे। जाड़े में बगीचे का जाड़ा सबसे बढ़कर होता। बरसात उसे भयानक दृश्यों में बदल देती और गर्मियों में लू घूमेरी लेती थी। रात का सन्नाटा बगीचे से उठती सरसराहटों को और गाढ़ा कर देता था। सारे बच्चे रात के पखेरुओं को पहचानते थे। बहुत बाद के दिनों की बात है, दिवाली के आस-पास की कोई रात थी, एक घुघ्घू माधुरी के घर की रेलिंग से लटका था। अशुभ और डरावना। उसके बच्चे चमत्कृत रह गए थे कि ऐसे उलटे निराकार लगते पक्षी का नाम उसे पता था। बगीचे की जानकरियाँ जिंदगी भर माधुरी के लिए अजूबा रहीं। गर्मी के दिनों में कोई रात में उठकर बगीचे की ओर देख लेता तो उसकी घिग्घी बँध जाती थी। बगीचे में न जाने कैसा जादू हरहराता रहता था, जो दिन में उसकी साँवली गहराइयों में जाकर छुप जाता।
बाद में बगीचे में कुछ अढ़उल, कनइल और बैर मकोय के झाड़ ही बचे थे, कुछेक बेल के पेड़ भी थे।
वह घर बैजनाथ चौबे का था। बाद के दिनों में वे ऐसे पुरखे हुए कि परिवार उनके किस्सों को बढ़ाता चला गया। दिन बीतने के साथ-साथ उनके विचित्र पुरुषार्थ की कथा गाढ़ी होती चली गई। फेंकना फुआ इस परिवार का झुर्रियों से भरा बुढ़ापा थीं। बच्चे उन्हें बइठकी फुआ कहते क्योंकि अब वे केवल घिसट सकती थीं, उठना, खड़ा होना उनके बस का नहीं था। फुआ की कथाओं में कई मोड़ कई हादसे थे। ऐसा लगता जैसे वे सारे घटित के बीच से गुजरी हों। उस हिसाब से उनकी उम्र होनी चाहिए डेढ़ सौ साल। मम्मा कहते ‘अरे होइ हैं अस्सी नब्बे क, मेहरारून क उमर त अइसै बहुत बुझाला, बचपन जवानी डांक के खाली बुढ़ापै त बचैला।’
फेंकना सबकी फुआ हुई, वैसे वे इस परिवार के रक्त संबंध में नहीं थी, बल्कि गाँव की थीं। ‘दिद्दन’ जो चौबे के एकमात्र पुत्र थे उनकी मुँह बोली बहन थी फेंकना की माँ। बेहद गरीब और तिरस्कृत थीं। दिद्दन ने उन्हें सहारा दिया। गाँव से शहर आई। यहीं फेंकना का ब्याह-गवन हुआ मगर नसीब माँ का ही मिला। तिहाजू वर को ब्याही गई थीं। कई सौतेले बेटे-बेटियाँ थे। पति के मरने के बाद उन सब ने मिलकर फेंकना को इतना सताया कि उनकी एक आँख जाती रही। दिद्दन उन्हें ले आए। उनकी गृहस्थी में फेंकना ने अपना जाँगर खपा दिया। भले ही घिसर कर चलतीं मगर गृहस्थी के सारे काम करतीं। फेंकना का समय इस घर का समृद्ध होता हुआ समय था। उन्हें दो रोटी आदर से मिल रही थीं। ठिकाना मिला था सो अपने बचे हुए समय में वे बच्चों के लिए पुराने कपड़ों का हाथी, घोड़ा बनाती और कहानियाँ सुनाती। बच्चें उन्हें घेरे रहते, दिक करते तो वे धमकाती – ‘सुत रे तोनहन नाहि कोठिया क चुरइल पकरि लेई ऽऽ…।
चुरइल यानी चुड़ैल। माधुरी वगैरह के बचपन तक कोठी और बगीचा मनहूसियत का दूसरा नाम हो चुके थे। वहाँ कुछ देखभाल करने वाले रहते थे। फुआ बताती – ‘अरे बड़ा जगर-गरस मगर है कुल बाकी त ऽऽर
चौबे जिस गाँव के थे उस गाँव की मुख्य प्रजाति चौबे ही थी। कहते हैं कि कई महीनों से बैजनाथ चौबे को सपने में एक नदी दिखती थी, हरहराकर बहते पानी वाली नदी और वे अपनी खजुहट से भरी चिपचिपी खाल खुजलाते हुए जाग जाते। परेशान हो गए थे वे। अपने सपने से भी और खजुहट से भी। एक दिन मुँह अँधेरे उठे और चलते चले गए। गाँव छूटा और कई गाँव छूटे, कचहरी का इलाका आ गया। उबड़-खाबड़ पैरों के नीचे समतल-सपाट रास्ता आता चला गया। चौबे चलते गए और सीधे नदी के किनारे पहुँचे।
चौबे को लगा था जैसे वे किसी नदी के किनारे नहीं बल्कि ईश्वर के आँगन में आ पहुँचे हैं। बिना कुछ खाए-पाए चले थे वे। जीभ प्यास से चट-चट कर रही थी। काँपते पैरों से चौबे नदी के किनारे बने घाट पर रखी चौकियों में से एक पर बैठ गए। चौकी पानी से खिआई हुई बदरंग थी। उचटते हुए उन्होंने भिखमंगों को देखा था। कोढ़ी, लूले, लँगड़े, आन्हर सब अपना कटोरा बढ़ाए सीढ़ियों पर बैठे थे। जब-तब रिरिया उठते। नदी शांत थी। उसकी सतह पर रोशनी के चकत्ते थे। बेहद भुखा गए थे चौबे। निगाह अनायास भिखारियों के कटोरे में पड़ी। सिक्के और कुछ फल वहाँ दिख रहे थे। भूख की चमक से जूझते हुए उन्होंने सोचा होगा कि वे वहाँ उन भिखारियों में कैसे बैठ सकते थे। कमजोरी के मारे मूर्च्छा आने ही वाली थी। एक क्षण को वे सोच गए कि नदी ने शायद उन्हें अपनी गोद में समेटने के लिए ही बुलाया है।
फागुन का उतार था। साँझ से पहले का समय। सीढ़ियों पर चढ़ते-उतरते कुछ ही लोग थे। सब के सब स्थानीय क्योंकि यह किसी पर्व-त्यौहार का समय नहीं था। घाट से लगे ऊँचे मंदिर की घंटियाँ बज रही थीं। कभी कोई तो कभी कोई उन्हें बजा जाता। टन्न की प्रतिध्वनि दूर तक जा रही थी। चौबे ने उचटती हुई आँखों से उस स्त्री को देख लिया था जो आँखे बंद किए धीरे-धीरे सीढ़ियाँ उतर रही थी, जैसे वह प्रतिदिन के सीढ़ियाँ उतरने के अपने अभ्यास को आजमा रही हो। सारी सीढ़ियाँ उतर कर वह जल में उतर गई। हाथों से जल को काटकर उसे आगे बढ़ते चौबे ने देखा। थोड़ी देर बाद हरे रंग के पानी पर उसका सफेद आँचल फैल गया। चौबे सनाका खा गए। औरत डूब रही थी। चौबे को समझ में आया कि शायद वह डूबने के लिए ही नदी में उतरी थी और बंद आँखों से सीढ़ियाँ उतरती हुई वह इस दुनिया को विदा दे रही थी। चौबे भी मरना चाहते थे। पैरों की मवाद से भीगी मोटी लिसलिसी खाल उन्हें असह्य हो चुकी थी। उस पर मक्खियाँ ऐसे भिनभिनातीं जैसे वह किसी जिंदा देह का हिस्सा न होकर कोई सड़ती हुई चीज हो। नदी किनारे लस्त-पस्त बैठे वह पानी की गहराई में उतरने के बारे में ही सोच रहे थे मगर नदी की ओर उनसे एक कदम भी न बढ़ा गया। डूबती हुई स्त्री को बचाने के लिए कैसे वह एकाएक नदी में उतर गए, किस ने उन्हें टहोका कैसे/उन्हें कुछ याद नहीं था।
स्त्री मरना ही चाहती थी। चौबे का सहारा झटकार कर वह बार-बार गहरे जाने लगी मगर उन्होंने उसे छोड़ा नहीं। पानी से लथपथ उस गठरी को जब वे बाहर निकालकर लाए तो एक भीड़ जुट गई थी।
कौन हैं, कहाँ की हैं, कैसे हुआ ये? जैसे सवालों ने स्त्री को घेर लिया था। स्त्री अपनी उस गठरी हुई देह में गुम हो जाना चाहती थीं। बुद्धि से हमेशा कोरे रहे चौबे को न जाने क्या समझ में आया कि स्त्री की तरफ से बोल उठे वे – ‘का करैं बेचारो, गौड़वे सरकि गइल।’
स्त्री कृतज्ञ हुई। सिर का कपड़ा ठीक करती हुई बोली – ‘आपने नाहक बचाया।’
चौबे ने जिंदगी का अब तक का कमाया हुआ सारा अनुभव सारा ज्ञान स्त्री के सामने उड़ेल दिया। अपनी व्यथा भी बताई। बताते-बताते हाथ पैरों की खाल पर चला गया। चौबे चमत्कृत हो उठे – खाल में अब असंभव किस्म की नरमी थी और वह चिनचिनाहट विहीन हो गई थी। चौबे कृतज्ञ हो उठे। नदी के आगे भभर आई आँखों के साथ उन्होंने हाथ जोड़ दिए – ‘वाह रे माई। तोहर किरपा।’ करिया अच्छर भइस बराबर थे चौबे, सो उपकार मानने का और कोई ढंग नहीं था उनके पास।
स्त्री शहर के बड़े ही सभ्रांत परिवार की थी। गोरी और ठिगनी सी उस स्त्री के सिर के बाल तक किसी ने कभी नहीं देखे थे। सिर पर हर वक्त आँचल रहता। डबडबाई सी आँखों पर उस आँचल की छाया पड़ती। सात भाइयों की दुलारी जैसी थी वह। भाइयों ने विराट संपत्ति वाले घर में ब्याहा। ससुर महाराज कहे जाते। कई इलाके थे उनके। शहर में भी उन्हें राय बहादुर की पदवी मिली थी। उनके एकमात्र पुत्र थे सौगंध नारायण सिंह। उन्हीं से ब्याही गई थी वह। दिन बीतते जा रहे थे, दोनों के कोई संतान नहीं हुई। कोठी परिजन-पुरजनों से भरी रहती, हर वक्त की चहल-पहल मगर मलकिन की गोद खाली। खैर रायबहादुर तो बहुत पहले दिवंगत हुए, उनकी पत्नी बहुत दिनों तक जिंदा रहीं। गंडा-ताबीज करती रहीं थी मगर कोई बात नहीं बनी। स्त्री का दुख शायद केवल कोख खाली होना नहीं था। सास के मरने के बाद न जाने क्यों उन्होंने विधवाओं जैसा बाना धर लिया था। बिना सलूके के सफेद साड़ी पहनती। खुद को खप तोप कर रखतीं।
पानी से भीगी हुई उनकी देह सोने की तरह चमक गई थी। पंडित ऐसे अचंभे में पड़े कि देर तक उनसे जागते ही नहीं बना था। खैर बाऊ साहब का रज-गज बड़ा था। विशाल कोठी के दो हिस्से थे। एक हिस्सा खिले हुए कमल सरीखा था, इसी से लगा था बगीचा जिसे ‘वन-उपवन’ कहा जाता। घने पेड़ों के बीच सफेदी से झिलमिलाती एक रिहाइश थी जिसे नौकर-चाकर मर्दाना कोठी कहते। बड़े ठाट-बाट वाला हिस्सा था यह, संक्षिप्त और रमणीय। बाऊ साहब के पिता, रायबहादुर के जमाने में इसकी शान अलग थी। कलात्मक रोशनियों से सजी इस कोठी में बाहर के जंगल की हवा सरसराती रहती थी। उन दिनों तो आस-पास दूर-दूर तक कहीं कुछ नहीं था। मीलों दूर वह रेल पटरी थी जिसका एक छोटा सा स्टेशन था।
पिता का रूतबा बाऊ साहब को नहीं मिला लेकिन अँग्रेजों ने उन्हें भी ऑनरेरी मजिस्ट्रेट की उपाधि दी थी। कुछ चहल-पहल उनके चलते भी थी मगर उसमें राजा साहब वाला रंग नहीं था। बागीचे के बिल्कुल सामने दूसरी कोठी थी जो मुख्य रिहाइश थी। परिवार के लोग उसी में रहते। वह भी खासी बड़ी हवादार और फैली हुई सी थी। एक हिस्सा तो केवल रसोईघर था। सारे हिस्से जुड़े हुए थे और अनंत सीढ़ियाँ जालीदार बरामदे वगैरह थे इस कोठी में। नौकर-चाकरों की रिहाइश भी पिछवाड़े थी। इस विशाल कोठी का एक दरवाजा एक गली में खुलता था। गली बहुत सकरी थी। यह गली भी कोठी का पिछवाड़ा ही थी। कोठी का गली से जुड़ा दरवाजा अंदर एक मेहराबदार बरामदे में खुलता था जो बहुत लंबा था। कोठी के लोग उस दरवाजे से गली में चाहे जब आ सकते थे, वैसे तो ज्यादातर उसका इस्तेमाल नौकर-चाकर ही करते थे मगर कभी-कभार मलिकार लोग भी करते। गली का मुहाना एक चक्कर लेकर उन्हीं दिनों चौड़ी हुई सड़क पर खुलता था जो उन दिनों नई सड़क कही जाती थी। गली के चक्कर के पास बाऊ साहब का ही एक अहाता था जो रसद घर कहा जाता था। बाद में वही रसद घर चौबे का ठिकाना बना मगर वह बात बाद में…।
स्त्री उसी गली में दाखिल होकर कोठी के चौड़े दरवाजे में समा गई। चौबे पीछे-पीछे चल रहे थे, सहसा रुककर ऊपर देख उठे। वे एक विशाल भवन के बंद से मुहाने के पास खड़े थे। चौबे स्त्री से बहुत अंतर रखकर चले थे। शाम धीरे-धीरे रात में बदल गई थी। गली में नीम रोशनी थी। कोठी का दरवाजा खुला तो भीतर की रोशनी झक्क से गली में बिखर गई थी मगर झप्प से बंद हो गई। रसद घर के पास के खंभे की कंदील का मद्धिम उजाला गली में लपक-झपक रहा था। चौबे के लिए सब कुछ बहुत रहस्यमय था। उन्होंने कुछ भी नहीं किया था उस स्त्री के पीछे-पीछे चले आने के अलावा। चौबे अचकचाए तो थे ही अब सहम भी गए। इस अपनी विचित्र यात्रा में शहर के जो हिस्से उन्होंने देखे उसमें गलियाँ ही ज्यादा थीं। स्त्री एक गली से निकलती, दूसरी में घुस जाती। कुछ गलियाँ गुलजार मिली थी तो कुछ बेहद सूनी। जवानी के दिनों में चौबे ने आलिफ-लैला, सीत-बसंत, रानी सारंगा जैसी कहानियाँ पढ़ी थी। उन्हें लगा उनका जीवन किसी गहरे किस्से में प्रवेश कर गया है।
कोठी में दरवाजे के भीतर से एक ठिगना साँवला आदमी प्रकट हुआ। धोती की उसने लाग-बाँध रखी थी और पुष्ट शरीर पर बंडी थी। बाद में चौबे ने जाना था कि वह बाऊ साहब के साथ साये की तरह रहने वाला चरन था। बाऊ साहब झक्क सफेद वेशभूषा में आगे-आगे चलते, तेज-तेज उनका गौर रेशमी वर्ण चमक रहा होता, पीछे-पीछे साये की तरह चरन चलता था। तैनात किंतु सुख-दुख, राग-विराग के किसी भाव से बिल्कुल खाली। वह बेहद अनुशासित और चौकन्ना था।
चौबे के लिए चरन ने एक कोठरी का जुगाड़ कर दिया था। कोठरी एक फैली हुई सी गौशाला का हिस्सा थी। मदन सरदार का इलाका था। यहाँ मदन सरदार बाऊ साहब के गोधन के व्यवस्थापक थे। कई गायें थीं, कुछेक भैंसे भी थीं। एक तरफ नीम के कुछ वृक्ष थे और एक बहुत पुराना बरगद था। चौबे की कोठरी से लगी पाँच कोठरियाँ और थीं जिनमें गायों का चारा खली वगैरह भरे हुए थे। कोठरी में दो बंसखट थीं, यानी कोठरी थी तो मदन सरदार की। मदन ने चौबे को लोटा भर दूध दिया। चौबे उसे गट-गट पी गए। भूखी देह की नसों में दूध कहाँ जाकर गुम हो गया कुछ पता ही नहीं चला।
हम आपको अपने हाथ का पका कैसे खिला सकते हैं महराज, आज इतने से काम चलाइए, कल देखते हैं – मदन ने कहा था।
चौबे अपनी पंडित नस्ल पर कुढ़ गए। इस समय उन्हें केवल अन्न चाहिए था। चौबे की जठराग्नि बहुत बड़ी थी। अत्यंत निर्धन परिवार था चौबे का। बूढ़ी भौजाई किसी तरह सबके लिए अन्न का जुगाड़ करतीं और चौबे को हमेशा यह कहकर परोसतीं कि ‘ला, भकोसा।’
पेट में तड़तड़ाती हुई भूख को दूध ने और जगा दिया था। बसखट पर ढहे हुए चौबे बार-बार अन्न बारे में ही सोचते रहे। मच्छरों-झिंगुरों की सुरताल में डूबते उतराते रात के किसी पहर सो ही गए होंगे बेचारे।
चौबे नाम के ही ब्राह्मण थे। पंडिताई से कोसों दूर। जाँगर चोरी के चलते किसानी से भी वे कोसों दूर थे। डेढ़ के बीघा जमीन और महुआ आम के कुछ पेड़ों के अलावा टुटही मड़ई जैसा घर था। उसी में पाँच परानी पल रहे थे। गाँव में पूजा-पर्व जैसा कोई गंभीर प्रयोजन होता नहीं था। तेरस और धनतरेस सब वहाँ एक ही जैसे थे। दान-पुण्य का रिवाज भी नहीं के बराबर।
कुछेक संपन्न किसानों के यहाँ कभी-कभार श्राद्ध वगैरह के कर्मकांड में पंडितों की संख्या पूरी करने के लिए न्यौते जाते। धोती जनेऊ वगैरह तभी जुट जाते थे। कुछ सुस्वादु भोजन भी मिलता मगर ये प्रसंग जीवन में बस गिने-चुने थे। दरिद्रता केवल उनके जीवन का दुख नहीं था, उनके जैसे कई थे। खेती के लिए गाँठ में भी कुछ चाहिए था, वह तो थी नहीं जाँगर भी नहीं था। दिन सुधरने की जुगत दूर-दूर तक नहीं थी। रात-दिन मड़ई में पड़े रहते। उसी में पैरों की खाल जानवर सरीखी हो गई। दिन-रात मवाद रिसता रहता। खजुहट के मारे बेदम हो जाते। भौजी, बाल-बच्चा सब घिनाने लगे थे। उसी में सपने का ब्यौंत मिल गया। जब नींद आवै तब सपना ओर हर बार वही सपना…।
चौबे के मन में कई बार आया कि अपने साथ घटे हुए को मदन से साझा करें। मदन दिन-रात गाय-भैसों की सेवा में लगा रहता। उसके चेहरे पर स्वास्थ्य और प्रसन्नता थे। लहककर कान पर हाथ रखकर गाता और चौबे को खिझाता – का हो गुरु अरे सुतबै करबा कि हिलबा भी।
चौबे ने यहाँ बसखट को अपना सब कुछ समझ लिया थ। सोये-सोये बहिनी का ख्याल आता। स्त्री को मन ही मन उन्होंने बहिनी संबोधन दे दिया था एक दिन चरन से पूछ ही बैठे कि – ‘बहिनी कइसे हई?’ चरन का चेहरा तन गया। आँखें कपाल पर चढ़ आईं। चौबे सनाका खा गए।
कोठरी में चौबे का खाने-पकाने का इंतजाम हो गया। मदन के लिए खैनी मलते। कभी नीम, तो कभी बरगद की छाया में बैठते लोटा भर दूध का सिलसिला कभी बंद नहीं हुआ। नियमित भोजन मिलने से सुख तो बहुत था घर-दुआर भी याद आने लगा था।
मगर पता नहीं क्या हुआ पुरानी विपत्ति फिर सिर उठाने लगी। पैर की खाल मोटी, खुरदुरी हो उठी। उससे चिप-चिपा सा पानी भी रिसने लगा। जहाँ-जहाँ खजुआते वहाँ काले चकते जम जाते। चौबे हलकान हो उठे। उन्हें लगा कि श्राप फिर अपना सर उठा रहा था।
‘का माई! कऊन अपराध भइल? क्षमा करा मइया!’
चौबे ने फिर नदी को याद किया।
मदन ने देखा तो कहा – अरे महराज! तनी हमरे कमवा में हाथ लगा देवल करा। देहिया के खरच करै के चाही। खरबा, जाँगर तोड़बा त कुछो न होई महराज!
चौबे थे स्वभाव के कामचोर। लोटे-बैठे मदन का खटना देखते। कभी इधर तो कभी उधर करवट बदल लेते। खटिया पर बेलसने का अभ्यास चौबे का पुराना था। गाँव में उनके नहाने का पानी भी कुएँ से उनकी पत्नी निकालती थी। बेचारी को मिर्गी आती थी। एक बार मिर्गी को चलते ही कुएँ में गिरी और मर गई। गाँव भर ने चौबे को धिक्कारा, भौजी जब-तब कोसती रहतीं, मजाल नहीं था कि ताना-मेहन के बिना उन्हें कभी खाना मयस्तर हुआ हो। उनके रोग को भी उनका पाप कहा जाने लगा था। बेटा-बेटी भी पास नहीं आते थे। गाँव घर छूटे कितना दिन हो गया, शायद ही चौबे को वहाँ कोई खोज रहा हो।
मगर यहाँ, यहाँ तो चौबे चेत में आ गए। परिश्रम के बिना यहाँ काम चलने वाला नहीं था, चौबे मदन के काम में हाथ बँटाने लगे। गोबर उठाते, गौशाला बुहारते, सूखे उपले जमाते गाय-भैंसों को नहलाते। रोग का जहर धीरे-धीरे काबू में आने लगा था। फुरसत होती तो चौबे कभी नदी की ओर तो कभी स्टेशन की ओर निकल जाते। शहर धीरे-धीरे उनकी जानकारियाँ आने लगा था।
बाऊ साहब पुश्तैनी रईस तो थे हो। पिता राय बहादुर थे। अँग्रेजों के मददगार थे। रायबहादुर को बख्शीश में बेहिसाब जायदाद मिली थी। दर्जनों कारिंदे थे, नौकर चाकर ड्राइवर बग्गीवान सेवा में थे। राजा-रानी का जोड़ा बड़ा कमाल था। अपनी पत्नी को राय साहब सरकार संबोधित करते। प्रजा के लिए वे बड़ी सरकार थीं। बड़ी सरकार भी किसी स्टेट की राजकुमारी थीं। आभिजात्य उनमें दिप-दिप करता। स्वस्थ लंबी काया, अपार केशराशि और बहुत ललित चेहरे की स्वामिनी थीं। बड़ी सरकार। कोठी भर में वे अभिमान से भरी डोलती। जहाँ से गुजरती उनकी सुंदरता और गुरूर की आभा वहाँ छा जाती। सभी आँखों झुकाए उनके करीब से गुजर जाते। बड़ी मीठी आदेश भरी आवाज थी उनकी। रायबहादुर की संपत्ति के साथ-साथ उनके दिल की भी मालकिन थीं वे।
राय साहब बहुत व्यस्त रहते। अक्सर इलाकों का दौरा करते। शिकार खेलने जाते, अँग्रेजों की दावतें करते। नाच-गान की महफिल सजाते। बड़ी चहल-पहल मची रहती थी कोठी में और बड़ी सरकार सारे सूत्र अपने हाथ में रखतीं। साहेब कोठी में होते तो वे उनके साथ साये की तरह रहतीं। उस जमाने में यह एक अनोखी बात थी। दोनों अगल-बगल चलते, परस्पर आँखें मिलाते। प्रेम प्रगाढ़ था दोनों का। प्रजाजन इस प्रेम से अभिभूत थे। राय साहेब पूरी तरह से बड़ी सरकार के अधीन, उन्हीं पर निर्भर। पतली सुघड़ अँगुलियों से पति को बीड़ा खिलातीं, कहीं बाहर जाते तो सिर से न्यौछावर उतार कर गरीबों में बँटवातीं। राय साहब भी अक्सर उन्हें संग ले जाते। उनके लिए मोटर का दरवाजा वे स्वयं खोलते और सरकार गर्वीली मुस्काराहट के साथ रेशमी वस्त्रों की सरसराहट समेटती बैठ जातीं। वे बजरों पर विहार करने, पार्टियों, में अतिथि और अतिथेय होते। राजा साहब के बाहर होने पर उनकी व्यस्तताएँ अनेक थीं। समाज सेवा वगैरह के काम में भी उनका चक्कर लगता। कभी-कभार इलाकों की देखभाल के लिए निकल जातीं। पति की अनुपस्थिति में अपने होठों पर हँसी सजाकर रखना उनके लिए मुश्किल होता और थोड़ी रुक्ष भी हो जाती थीं। आँखों में कुछ छलकता सा दिखता था, वो साक्षात प्रतीक्षा होती थीं उन दिनों।
उस रात वे अकेली सोई थीं। हुआ यह था कि मर्दानी कोठी में नृत्य की महफिल ढेर रात तक चली थी। सुरूर रात भर मद्धिम-मद्धिम बहता रहा था। सारंगी की उठान में कुछ ऐसा था कि सरकार के कलेजे में जैसे कुछ थहर-थहर गया था। बीच में एक बार साहेब आए थे, नजदीक खड़े भी हुए मगर न जाने क्यों उन्हें लगा था जैसे वे बहुत दूर खड़े हुए हों। बड़ी बेधती निगाहों से उन्होंने प्रियतम को थहाया था। आज वे आँखें चुरा रहे थे। मोटी रुपये की थैली लेकर वे मर्दानी कोठी में चले गए। बहुत रात तक जागती रही सरकार, सबेरे उन्हें ऐसा लगा था जैसे कि वे सोई ही नहीं थीं। वह टूट रही थीं और कक्ष में एक मनूहस सूनापन भर गया था। रोज की तरह का दिन होना चाहिए था। नौकर-चाकर इस काम से उस काम में दौड़ रहे थे। चैत महीने का सवेरा जरा ऊपर चढ़ गया था, इसीलिए ज्यादा चटक भी था। वे समझ गईं कि वे कुछ ज्यादा देर तक सोती रह गई हैं। देह में मलीन किस्म का आलस्य भर गया था और कलेजे में न जाने कैसी तो तकलीफ दरक रही थी।
कुछ सोचती हुई सी वे शयन कक्ष से बाहर आई। झिर्रीदार बरामदे से देखा तो बागीचे से कई मोटरें निकलती दिखाई दीं। रात में आए मेहमान विदा हो रहे थे शायद।
दिन कुछ ही ऊपर उठा होगा कि उन्हें राय बहादुर के भी बाहर चले जाने की खबर मिली। वे धक्क से रह गईं। आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं। उन्हें बताया गया कि वे बेसुध सो रही थीं इसलिए उन्हें जगाया नहीं गया।
कई दिन गुजरे थे इस तरह। राजा साहब की कोई खबर नहीं थीं। मान के कारण उन्होंने खुद किसी से कुछ नहीं पूछा बस स्वयं को ढेर सारे कामों में धँसा दिया था। लोग-बाग के अनुसार ये उनके प्रौढ़ होते दांपत्य के दिन थे। उम्र भी उतार की ओर मुड़ चुकी थी मगर रस भीने दांपत्य ने उनका पारे-पारे खिला रखा था। देह में यौवन की सी गतियाँ बदस्तूर थीं? पति के करीब आते ही उनकी पलकें भारी हो जातीं, ऐसी गम कमरी निकटता थी उनकी। कहीं एक बाल भर भी जगह नहीं थी कि उनके बीच कहीं कोई और होता। निःसंतान होने का भी कोई दुख दोनों को था, ऐसा किसी को कभी पता नहीं चला। फुसफुसाते, बच्चा गोद लेने वगैरह की भी बात चलती मगर उनके निकट किसी को कुछ बोलने का साहस नहीं था।
काफी दिन बीते। कहीं कोई खबर नहीं, अचानक एक दिन सबेरे-सबेरे हलचल मची। राय साहेब की सवारी लौटी थी। बागीचे का घुमावदार रास्ता कई-कई गाड़ियों से भर उठा। अफरा-तफरी मच उठी। अनुमान था कि वे सभी मर्दानी कोठी में कुछ देर रहेंगे और जलपान के बाद रुखसत होंगे। सरकार अपनी लटें सुलझाने बैठ गईं। कई दिनों बाद उन्होंने खुद को दर्पण में देखा। चेहरे के सूखेपन को बरज उठीं। आँखों में प्रेम के डोरे तैर उठे।
भैरों की पत्नी उनके नजदीक आकर खड़ी हो गई थी। न जाने क्यों वे उसे देख उठीं। नौकर-चाकर पर निगाह डालने का चलन कोठी में नहीं था। वे भी उनसे आवश्यक दूरियाँ बरतती थीं। उन्होंने लक्ष्य किया था भैरों की पली का रंग उड़ा हुआ है। उसकी देह काँप रही थी जैसे। कोठी से जुड़ी बातों में इस घटना के कई-कई रूप दर्ज है। कुछेक लोकगीतों में भी यह प्रसंग दर्ज हो उठा है। सरकार के दुखों को लोगों ने बड़ा मान दिया और उनके पक्ष में गीत बनाए। वे उस रानी का दर्द बयान कर रहे थे जिसका पति के प्रति मान टूटा है, विश्वास खंडित हुआ है।
उन्हें याद नहीं कि नीचे स्वागत कक्ष तक वे किन पैरों से चलकर आई थीं। हमेशा आवरण और श्रृंगार में रहने वाली उनकी देह कहाँ-कहाँ से उखड़ी थीं। अधसुलझे बाल कहाँ कितनी गिरे या कि सँभले थे। उन्हें कुछ भी याद नहीं था। राजरानी होकर भी वे एक सामान्य स्त्री की तरह काँप रही थीं। बार-बार उन्होंने सीढ़ियों की रेलिंग को सहारे की तरह पकड़ा, उनकी राजसी गति, चेहरे का दर्प और मुग्ध कर देने वाली मुस्कान न जाने कहाँ खो गई थी। कलेजे में सिर्फ और सिर्फ अनहोनी बज रही थी। अनहोनी तो हुई थी, मगर ऐसी?
बाहर बहुत सारी आवाजें थीं। मर्दानी कोठी की गहमा गहमी की आवाजें नीचे स्वागत कक्ष तक आ रही थीं। विशाल था यह कक्ष। सुसज्जित और विशाल खिड़कियों, पर्दे गलीचे और पेंटिग्स वाला। पूरी सज्जा महँगी और आरामदेह थी। कमरे में एक नरम हवादार उजाला भरा हुआ था। इसी उजालों में सरकार ने एक कुर्सी पर सहमी सी बैठी उस स्त्री को देखा था जिसके माथे पर झीना घूँघर था। पसीने से चिपके बालों के बीच सिंदूर की चटक देखा चमक रही थी। बहुत खोई सी आँखें थीं और वे आँखें उन्हें ही देख रही थीं।
पंडित परिवार की फेंकना फुआ यह सब बताते समय जार-जार रो उठती थीं। कोठी में यह सब चौबे के आने के कई-कई साल पहले घट चुका था। किस्से कहानियों और फुसफुसाहटों में यह सब कुछ इस तरह दर्ज था कि जब उचारा जाता, घाव नया हो जाता था। फेंकना बुआ को न जाने कैसे पता था कि सरकार का नाम राजरानी था। इस कहानी को वे अपने कलेजे की सेंक देकर बताती। बीच-बीच में ऐसे बुक्का फारकर रोतीं कि बच्चे सयान सब दहल जाते। थमी हुई साँस तब वापस आती जब फुआ नाक पोछ-पाछ कर कहानी आगे बढ़ातीं।
राजरानी के व्यक्तित्व में बड़ा ठहराव था। वे इस घटना से धूमिल पड़ जाने वाली नहीं थीं। अँग्रेज अफसरों से वे फर्र-फर्र अँग्रेजी में बात करतीं। हिसाब-किताब पर कड़ी नजर रखती। प्रजा को सजा या पुरस्कार भी वही देती। बस राय बहादुर को एक संतान जनकर वे नहीं दे पाई थीं।
भैरों की पत्नी दरवाजे पर ही ठिठक कर रह गई। वे उस स्त्री की ओर कुछ कदम बढ़ आई थीं। उन्होंने देखा कि वह एक बालिका जैसी थी। घोंसले से गिरे गौरेया के बच्चे की तरह थर-थर काँप रही थी। पलांश में वे सब कुछ समझ गईं। उनकी समूची देह में एक धिक्कार तन गया। इस क्षण भी वे एक सामान्य स्त्री नहीं थीं। सोने के छल्ले में बँधी चाभियों में से एक चाभी निकालकर उन्होंने भैरों की पत्नी के तरफ फेंक दिया और बाहर आ गईं।
चाभी विलास कक्ष की थी। कोठी के सुदूर छोर का इकलौता कक्ष जिसके सामने बहुत खुला हुआ उद्यान था। वह परम एकांत का कक्ष था। वहाँ तक जाने के लिए कई लंबे गलियारे पार करने पड़ते। उस गौरैया जैसी युवती ने सारे गलियारे पार किए। जहाँ से गुजरी कच्चे उबटन की गंध वहाँ फैल गई। रायबहादुर की छाया सरीखे भैरों की पत्नी थी तो बड़ी सरकार की सेवा में मगर उस समय उसकी जिम्मेदारी और थी। इस जिम्मेदारी का कलेश उसे भी असह्य था मगर करती क्या आज की रात उसे ही राय बहादुर के लिए विलास कक्ष सजाना था, सजाना ही था।
बाबू ईश्वरी नारायण सिंह का जन्म उसी बालिका वधू की कोख से हुआ था। मगर यह बात उनको भी बहुत बाद में पता चली थी। लगभग रेख भीगनें की उम्र में। पता चली पिता या बड़ी सरकार के द्वारा नहीं बल्कि कोठी में चल रही फुसफुसाहटों, इशारों को समझकर। उस बालिका का माँ बनना और बालिका से स्त्री होते जाना, कोठी के भीतर का एक दारुण मामला था जिसे सबसे ज्यादा सेवकों-चाकरों ने जाना, मगर उनके मुँह बंद थे। रिश्तेदारों ने भी जाना मगर वे किसी भी प्रकार से इस मामले में शामिल होने की स्थिति में नहीं थे। उनके निकट तो ये रईसी के संसार का स्वाभाविक चलन था। ये क्या कम था कि एक गरीब घर की, बेशक सुंदर बालिका को रायबहादुर ने अपनी संतति के लिए चुन लिया था। कायदे से तो बड़ी सरकार को खुद आगे बढ़कर बहुत पहले इसका जतन करना चाहिए था। इतने बड़े राजपाट का वारिस न होना, सामान्य स्थिति नहीं थी। लाख प्रेमासक्ति हो मगर जगत व्यवहार भी कोई चीज है।
कहते हैं कि उसी रात कोठी से कुछ मोटरें बाहर गईं थीं। उनमें बड़ी सरकार के अलावा कुछ दासियाँ और शायद मुंशी जी थे। खबर फैलाई गई कि वे इलाकों की देखभाल के लिए गईं थी मगर किसी इलाके में उनकी सवारी पहुँचने की कोई खबर नहीं आई। बताते हैं कि कई महीने ऐसे निकल गए थे। राय साहब बालिका वधू के साथ विलासकक्ष में पड़े रहते और कोठी पर नौकरों-चाकरों का राज्य हो गया था। कोई रसद बेचता, कोई बर्तन उठा ले जाता। कई-कई तरीके की लूट मच गई थी। भैरों और भैरों बहू सब कुछ देख कर भी कुछ नहीं कर सकते थे।
यह भी कहते हैं कि उस रात राय साहब नीचे सहन से ही विलासकक्ष में चल गए थे। सरकार के शयन कक्ष में वह एक बहुत सूनी और मनहूस रात थी। इस रात के हिस्से में क्या-क्या था, अब इसे कैसे बताया जाए। धुरी टूट जाने पर पृथ्वी की जो गति होती है, कुछ-कुछ ऐसी ही थी वह रात। सरकार बौरा नहीं सकती थी। स्वयं को लुटा-पिटा नहीं व्यक्त कर सकती थीं। चेहरे पर एक भी मलीन रेखा तक लाने की गुंजाइश नहीं थी। उनकी यातना इन तरीकों में व्यक्त होने से बहुत-बहुत ज्यादा थी। वह एक तहस-नहस से भरी लंबी रात थी जिसमें बार-बार उनका गला सूखता रहा। अँधेरा चारों ओर बरस रहा था। धीरे-धीरे सारी हलचलें खामोश हुई थीं। पेड़ों की पत्तियाँ तक गहरी नींद में थीं। एक गाढ़ा वक्त सब ओर तारी था जब वे अपने छोटे से काफिले को लेकर निकल गई।
चाभियों का गुच्छा उन्होंने अपने युगल चित्र के पास रखे टेबल पर रख दिया था। चित्र में हँसती अपनी छवि की तरफ नहीं, पति की नेहभरी आँखों की और उन्होंने जरूर देखा होगा।
हर चीज की एक उम्र होती है, चाहे फिर वह प्रेम ही क्यों न हो। शायद उन्होंने यह सोचा था, कई-कई महीने बीत गए थे, उनका अता-पता नहीं था।
राय बहादुर ने खोज खबर ली थी। इलाकों में लोग दौड़ाए गए थे। संबंधियों-दोस्तों ने हैरत प्रकट की थी – इतना गुमान, स्त्री होकर?
राय साहब उस गुमान को जानते थे। जल्दी ही उन्हें कोठी की तबाही का पता चल गया। वे घूम-घूम कर चाकरों पर गरजने-बरसने लगे। नए-नए प्रेम में चिंता का कीड़ा अलग लग गया।
सरकार ऐसे ही एक दिन लौट आई थीं। चेहरे से मृदुता कोमलता का लोप हो चुका था। कुचली हुई अंतरात्मा के जख्म भरे नहीं थे। आते ही उन्होंने शासन सूत्रों को पहले से ज्यादा चौकसी से सम्हाल लिया। भैरों बहू चाभियाँ ले आई थी। आए तो रायबहादुर भी थे। सुलह की मिठास से छूने के लिए बहुत करीब आकार खड़े हुए मगर हिम्मत नहीं पड़ी थी – “तुम्हारी छोटी बहन है वहाँ चाकर बन पड़ी रहेगी’ बहलाया था, उन्होंने। नइकी के गर्भ का आठवाँ महीना चल रहा है। यह बात कोठी की हवा में थी।
बेटा हुआ। पुरखों की माटी जगाई गई। काँसे की थाली फोड़ी गई। नार-खेड़ी सुअर की माँद में डाली गई। कई-कई टोने-टोटके हुए और वह ताजा-ताजा जन्मा बच्चा बड़ी सरकार के आँचल में आ गया। अपनी जननी के पास वह केवल स्तनों में दूध रहने तक ही गया।
रातों-रात नइकी का ठिकाना बदल दिया गया था। विलास कक्ष से सीधे वह कोठी की उस अजीब मंजिल पर पहुँचा दी गई जिस पर जाने की सीढ़ियाँ बहुत अँधेरी और सँकरी थी। ऊँचे मुँडेर वाली छोटी सी छत के साथ सिर्फ एक खिड़की वाला कमरा था। आसमान का सारा सन्नाटा वहाँ बरसता था। उस कन्या की दुनिया सिर्फ छोटी नहीं बल्कि बंद हो गई थी।
उस का नाम क्या था फुआ?
का जानी बचवा! सब ओन्है नइकी कहे।
फुआ लगभग फुसफुसाने के ढंग में आ गई थीं। दरअसल तभी उस नइकी की अनेक यातनाओं का दौर शुरू हो गया था। इस सारे इंतजाम के पीछे बड़ी सरकार का हुक्म था। राय साहब फिर उनके करीब बैठने लगे थे, दोनों पहले जैसे बाहर जाते बातचीत भी करते। नए शिशु के जिम्मेदार माता-पिता की तरह दिखाई देते। घर-आँगन गुलजार हो गया था और एक युवा स्त्री ऊँचे बुर्ज की कालकोठरी में डाल दी गई थी। उसका सुख-दुख सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। रायबहादुर उसकी तरफ झाँक भी नहीं सकते थे। सख्त पहरा था सीढ़ी पर और बेइंतिहा फुसफुसाहटें थीं।
नइकी का भोजन-पानी लेकर चंपा जाती थी। एकाध बार रिश्तेदारों के बच्चे दबे पाँव चंपा का पीछा करते ऊपर पहुँच गए। नइकी उनके लिए अजूबा थी। भोजन को वह हाथ न लगाती, बस पानी गट-गट पी जाती। सुंदर कमनीय देह खाँखर हो गई थी। रूखे बाल, चढ़ी हुई सी आँखें…।
एक रात वह देह सरकार के पैरों के पास आकर बैठ गई। कंकाल छाया के पसीजे हुए हाथ उनका पैर टटोल रहे थे। काँप रही थी वह। अपने बच्चे को कलेजे से लगाना चाहती थी मगर वह उसे देख तक नहीं पाई और पुनः उन्हीं अँधेरी सीढ़ियों की तरफ ढकेल दी गई।
उसके बाद उसके कक्ष तक जाने वाली सीढ़ी के दरवाजे पर ताला जड़ दिया गया था।
घटनाएँ कई थी। चंपा बदस्तूर खाना-पानी लेकर ऊपर जाती रहती। उसके साथ एकाध बच्चे भी दाँव देखकर ऊपर चढ़ जाते थे। यह दृश्य उनके लिए कौतुक की तरह था। उन्हीं बच्चों में से एक ने बड़ी सरकार को बता दिया था – ‘ऊपर नइकी तो है ही नहीं!’
भैरों बहू ने पड़ताल की थी। चंपा का झूठ खुल गया था। चंपा भी क्या करती राय साहब का हुकुम था। हफ्ते भर से सरकार भी कोठी पर नहीं थे।
सरकार ने उनके लौटने की प्रतीक्षा की थी। इस मानभंग को उन्होंने बड़ी शालीनता से झेल लिया था।
रात के तीन बजे नीचे सहन से आने वाली सीढ़ियों पर रेशमी कपड़ों की सरसराहट सुनाई दी थीं। चूड़ियों की खनक भी थी और हवा में वह खुशबू भी जिसे उनसे ज्यादा भला कौन जानता।
उसी रात नइकी भैरों बहू की निगरानी में आ गई थी। चाभी अब सरकार के पास थी।
धीरे-धीरे कोठी के बाशिंदों को उस ऊँची मंजिल से आती अनवरत रोने की आवाजें सुनाई देने लगी थीं। उस रुदन में शब्द भी थे। निखालिस भीख माँगने वाले शब्द। उसी समय सबको नइकी की बोली-बानी का पता चला। बीच-बीच में नइकी गीत भी गाती। गले में बड़ी मिठास थी। गीत नीचे तक तैर कर चला आता और कभी-कभार दासियों के कंठ से फूठ उठता – ‘हरि हे बेला फूलौ आधी रात चमेला बड़े भोरे रे हरी।’
सरकार साहेब के मुँह में बीड़ा देतीं। सरकार सुस्त से मुँह फेर लेते। कभी-कभार उनकी आँखों से आँसू बहते। सरकार अपने आँचल से उसे पोंछ देतीं। दोनों के बीच का नेह-छोह अब लाड़-दुलार में बदल रहा था। ईश्वरी नारायण सिंह स्वस्थ सुंदर बालक थे। ठुमुक-ठुमुक कर चलते। सरकार उन्हें कलेजे में लगाकर रखतीं। गीत के टुकड़े उनके भी कान में पड़ते। विरक्त हो कहतीं – ‘पतुरिया कहीं की!’
साहेब और लस्त हो जाते।
आठ बरस बीत गए थे नइकी के उस यातना में, आठ बरस! ऊपर से आते गीत चीत्कारों, गालियों में बदले और फिर अमानुषिक हट्टहासों में।
नइकी पागल हो गई थी।
बहुत जोर आ गया था उसकी देह में। दरवाजा तोड़ दिया था उसने। पशु की तरह अतिनाद करती। सीढ़ियों पर खड़ी हो वहीं से पेशाब कर देती। कूदती हुई नीचे आ किसी के भी सामने अपनी साड़ी उठा देती… सर्वांग नंगी। फुसफुसाती और फिर रोने लगती।
रायबहादुर श्लथ हो चले थे। बहुत बूढ़े…। कई बार उन्होंने नइकी का यह भयानक रूप देखा था। वे रोने लगते। सरकार के चेहरे पर कठोरता बढ़ती गई थी। वे नौकरों से उसे पिटवातीं। खाना-पीना बंद कर देतीं।
कभी-कभी नइकी बहुत कातर कमजोर क्षण में गिड़गिड़ाती – ‘हमार बचवा।’
उसकी लटों में जुएँ पड़ गई थीं। बूढ़े हुए नाखून – डरावना चेहरा और भद्दी मुद्राएँ।
आठ साल के थे बाऊ साहब। उन्होंने उसे इसी वीभत्स रूप में देखा था। चीखती-चिल्लाती कपड़े फाड़ती हुई।
बहुत बाद में उन्होंने जाना कि वह स्त्री उनकी माँ थी।
बाद में उन्होंने सरकार के षड्यंत्रों के बारे में भी जाना। वे जवान हुए मगर बहुत चुप्पे और असामान्य से।
ऐसे ही किसी दिन उस ऊपर की मंजिल का विप्लव खत्म हो गया। लोगों ने सिर्फ यही देखा कि सीढ़ियों की धुलाई हुई और उस मंजिल का दरवाजा खोल दिया गया। हवा सामान्य महक वाली हो चली। एक सूनी निचाटता उन सीढ़ियों पर थी।
भैरों और भैरों बहू का उसी दिन से कुछ पता नहीं चला। सुना गया कि गाँव में उनके नाम काफी जमीन लिखवा दी गई थीं। सरकार अप्रभावित ढंग से सारे काम करती। रायबहादुर की सक्रियताएँ खत्म थीं। बाऊ साहब अट्ठारह बरस के हो रहे थे जब सरकार ने उनका ब्याह रचाया।
लक्ष्मी जैसी सुघड़ पतोहू ले आईं सरकार। हफ्तों घर उत्सव से गुलजार रहा। धन-धान्य लुटाया गया। तंबू-कनात लगे। रात भर पतुरिया नाचती थी – ‘नजर लागी राजा तोरे बंगले पे।’ रायबहादुर विरक्त से सब कुछ देखते।
लोग-बाग उल्लसित थे। बच्चे मग्न थे मगर उनकी पतोहू की प्रतीक्षा का कोई अंत ही नहीं था। अंत हुआ भी नहीं…।
राय बहादुर को लकवा मार गया। सोने जैसी देह गल गई और एक दिन सब कुछ छोड़कर सिधार गए।
नई बहू की देह सूखने लगी थी। आँखों में सवाल उतरे और फिर अनंत उदासियों ने कब्जा कर लिया।
सरकार ने चाभियों का स्वर्णगुच्छ आँचल से बाँध दिया। तरह-तरह से उसे सजातीं, बेटे के करीब ले जातीं।
बेटा आँख उठाकर भी न देखता।
उन चाभियों में पति के मन-हृदय की कोई चाभी न थी। बाऊ साहब मर्दानी कोठी से केवल भोजन के लिए आते पत्नी की तरफ आँख उठाकर कभी न देखते मगर मर्दानी कोठी की रजगज बढ़ गई थी। तरह-तरह की महफिलें सजने लगी थीं।
सरकार सब कुछ देखतीं-सुनतीं। कुढ़तीं, दुख से भर जाती। कोठी के परिचारक घटने लगे थे। पुरानी साख धूमिल हो रही थी। धीरे-धीरे सरकार ने भी खाट पकड़ ली। एक दिन वो भी सब कुछ छोड़कर चल बसीं।
तभी लोगों ने मलकिन को सर्वांग सादगी में ढलते देखा था। सारे आभरण उन्होंने उतार दिए और अपने लिए एकांत चुन लिया।
न जाने कहाँ-कहाँ से जायदाद के दावेदार जुटने लगे थे। कोठी उनके आने-जाने से भरी रहती। बाऊ साहब की किसी चीज में रुचि नहीं रह गई थी। रिश्तेदार कभी इस तो कभी उस कागज पर दस्तख्त कराते। मलकिन और बाऊ साहब दो छोर हो चले थे। बाऊ साहब में अपनी प्रभुता सँभालने का बूता नहीं था और मलकिन सब कुछ से विरक्त थीं।
बस एक कागज पर उन्होंने भी दस्तखत कराया था। रसद घर का मालिकाना चौबे के नाम लिखवा दिया। एक चौड़े अहाते की एक कोठरी, ओसारा कुआँ और पेड़ पालो चौबे के नाम हो गए।
भौजी, एकलौता बेटा बहू, उसका किशोर होता हुआ बेटा एक विधवा बहन और उसकी बेटी चौबे की गृहस्थी में जुट गए।
चौबे के वहाँ बस जाने के काफी दिनों बाद की बात है। एक साँझ कोठी से चौबे का बुलावा आया।
चौबे के हाथ में एक गठरी थमाई गई। नीम अँधेरे गलियारे में मलकिन खड़ीं थी। चारो ओर उजाड़ बरस रहा था। चौबे बहुत डर गए थे। कोठी में अब बहुत नए तरह के लोग-बाग आते। बाऊ साहब मरणासन्न थे। उनके विश्वासपात्र सेवकों को हटा-बढ़ा दिया गया था। भाँजों के हाथ के सारा रूतबा आ रहा था और वे सब बड़े चौकस थे। कोठी के हर आने-जाने वाले पर अब नजर रखी जाती थी।
चौबे गलियारे में खड़े थे। चरनबहू के करीब खड़ी थीं मलकिन – ‘पंडित जी! इस पते पर पहुँचा दीजिएगा।’ चौबे की ओर चरन बहू ने एक कागज बढ़ाया।
झुक कर जमीन छू ली चौबे ने। रोआँ-रोआँ भभर उठा उनका। ऊपर आँख उठाकर देखने तक की हिम्मत नहीं हुई उनकी। उन्हें वही करुण-कातर छोड़ मलकिन लौट गईं। चौबे अपनी नई जिम्मेदारी को लेकर अझुरा गए थे। काँप रहे थे वे। उन्हें बताया गया था कि यह बात किसी को बतानी नहीं है। चौबे ने किसी को नहीं बताया। भौजी को भी नहीं। उनसे यही कहा कि ‘कुछ काम से मेहनाजपुर जाना है।’
जहाँ जाना था उस गाँव का नाम तक नहीं लिया चौबे ने। मुँह अँधेरे निकल गए। पूरा गाँव खोजते रहे, उस पते पर कभी कोई रहता ही नहीं था।
अचंभे में पड़ गए चौबे। लौटकर आए तो पता चला मलकिन चल बसीं। साँप काट लिया था उन्हें।
इतना ऊपर का कक्ष, बेहद साफ-सुथरा। साँप वहाँ आया कहाँ से?
सबके मन में आशंका भी मगर बोलता कौन? चौबे चरन बहू से मिलकर पूछना चाहते थे कि गठरी का करें क्या?
चरन और चरन बहू भी कोठी में नहीं थे। कहाँ बिला गए किसी को नहीं पता।
एकाध बार चौबे कोठी की तरफ मँडराए। नए-नए मुच्छड़ दरबान ने तरेरा – ‘हे पंडित! औकात में रहा।’
चौबे के नाम हुआ रसद घर नए मालिकों को बहुत अखर रहा था। अब भौजी के आगे भेद खोलने के अलावा चौबे के पास कोई चारा नहीं रहा, जार-जार रोते हुए चौबे ने सारी कथा भौजी को सुनाई। भौजी ने जो गठरी खोलकर देखी तो आँखें फटी की फटी रह गईं। झलमलाते हुए सोने कुंदन के अनेक गहने। बाजूबंद, हँसुली, टीका, रामनामी और न जाने क्या-क्या!
का कइल जाय। भौजी और चौबे दोनों सोच में पड़ गए।
लौटाएँ तो किसे लौटाएँ? उन्हें ही देना होता तो यह गठरी चौबे को ही क्यों सौंपी जाती? और वह गलत पता।
चौबे की बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। वे दुख, पछतावा, ग्लानि से भरे हुए थे। मलकिन को याद कर जार-जार रो उठते।
भौजी ने आँगन खोदवा कर गहना उसमें दबा दिया था।
यह चौबे के घर का वह रहस्य था जिसका सिरा कोठियों से जुड़ा हुआ था। बहुत लंबा जिए बाऊ साहब। सब बिस्तर पर होने लगा था – टट्टी-पखाना सब। मलकिन के जाने के बाद घूर-घूर जायदाद बिकने लगी। पतले से सफेद बिस्तर पर बिना हाथ हिलाए बाऊ साहब पड़े रहते।
‘कुसंगी थे बाऊ साहेब!’ माधुरी और बच्चों से आँखें बचाकर फेंकना फुआ ने गुनी मौसी को बताया था।
गुनी मौसी कपड़े के हाथी के पेट में पुराने कपड़े घुसा रही थी। भारी बरसात की रात थी। कोठरी के भीतर सीलन का शीत काँप रहा था।
कुसंगी? बच्चों ने सुन ही तो लिया। माधुरी के जेहन में यह शब्द खुट से जाकर बैठ गया।
फेंकना आजी को लगा कहानी पूरी हुई। गुनी मौसी गुनगुना रही थीं –
टोना माँगैले माई एही देहिया
महला न माँगे, दुमहला न माँगे
जोग माँगैले माई एही देहिया
गला बड़ा अच्छा था गुनी मौसी का। चौबे होते तो उन्हें लगता जैसे यह मालकिन के कलेजे में बजने वाला गीत था।
चौबे की कई पीढ़ियों तक बात पहुँची थी कि आँगन में खजाना गड़ा है मगर खजाना खोजने की हिम्मत किसी ने नहीं की।
बगीचा कट-पिट कर खाली हो चुका था और मौसमों के रंग भी काफी बदल गए थे।
बदले हुए शहर के नक्शे में कोठी का कैसा भी इतिहास नहीं बचा।
Download PDF (टोना माँगैले माई! एहि देहिया )
टोना माँगैले माई! एहि देहिया – Tona Mangaile Maee Ehi Dehiya