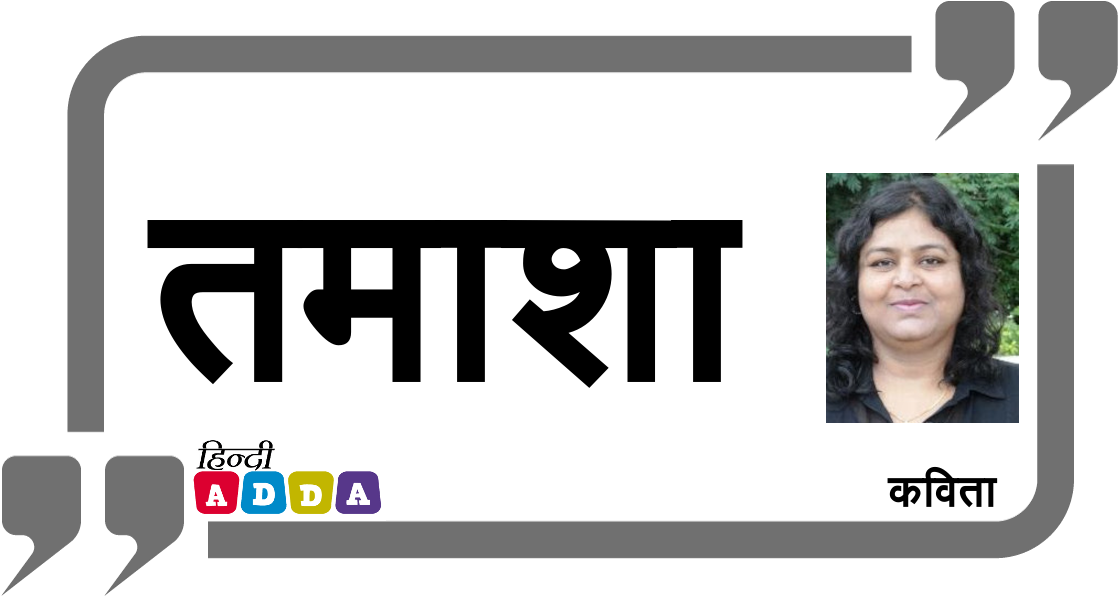तमाशा | कविता – Tamasha
तमाशा | कविता
पहले तीन दिनों की तरह उस दिन भी तमाशा के शो के शुरू होने के पूर्व ही उसके सारे टिकट बिक चुके थे। पर आगे जो कुछ भी हुआ था वह पहले दिनों की तरह नहीं था। घेराबंदी तीन तरफ से थी। आवाजें चहुँ दिश से घेरती, वार करती सी। वह कान बंद कर लेना चाहती, नहीं सुनना चाहती कुछ भी। क्या इसी की खातिर उसने जिंदगी के इतने बरस होम किए। अपना घर… अपने सुख…? यायावरों की तरह भटकती रही इत-उत।
वह जब शो से लौटती सहेजने लगती सब कुछ, एक सिरे से, गृहस्थी, घर बच्चा। जैसे भरपाई करना चाह रही हो अपने स्वप्नों – महत्वाकांक्षाओं की। वह भूल जाना चाहती एक सिरे से पिछला सब कुछ। तेज रोशनी, आवाजें, दर्शक, दर्शक-दीर्घा और अपना अभिनेत्री रूप। इससे थकान और-और गहराता पर अदभुत विश्रांति भी वह इसी में पाती। वह अलग सी हो लेती। अपनी बच्ची की प्यारी माँ, अपने घर के लिए बस एक अदद गृहिणी। गंदे कपड़ों से जूझती, उन्हें साफ करती, तहाती, रखती। गर्मी-सर्दी के कपड़े छाँट कर अलग करती। अच्छे और बेकार कपड़े अलग-अलग। रसोई चाक-चौबंद हो जाती। लेकिन फिर-फिर ऊबने लगती वह इन सब से; जैसे अभी तक वह एक सुघड़ गृहिणी का अभिनय कर रही थी। एक ही पात्र कब तक? और कितनी देर? उसे अलग-अलग चरित्र खींचने-बुलाने लगते अपनी तरफ हाथ हिला-हिला के। इतने आवेग से कि रुकना उसके लिए मुश्किल हो जता।
वह इस मुगालते में नहीं थी कि नाटक करके वह समाज बदल रही है। वह खुद को बदलने के लिए, अपने मनफेर के लिए नाटक करती थी और इतना तो जानती ही थी वह कि हमारे देखे-पढ़े-सुने में से कुछ-न-कुछ छूटा रह ही जाता है हमारे भीतर स्फुलिंग की तरह। कुछ बिल्कुल अनचीन्हा सा। उसे पता तो था ही यह…
‘तमाशा’ उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य, उसकी एक महत चाहना-योजना। जिसके पीछे भागते हुए उसने अपने जीवन के कई स्वर्णिम वर्ष गँवा दिए थे। कई-कई खूबसूरत बरस; सपनों – रंगों से भरे बरस। पर उसे सपनों-रंगों के पीछे भागना भाया ही कब था…? वह तो पीछा करती हुई भागती रही थी उस सच का जो छली था, बहुरूपिया था सोने के मृग जैसा। वह फिर भी भागती रही उसके पीछे लगातार…।
पिता नाटक करते थे और माँ मौका मिलते ही अपनी संगीत साधना में लीन हो लेती। लीन होते ही वह कुछ दूसरी-दूसरी सी दिखने लगती; उसकी हमेशा की प्यारी भोली-भाली, वात्सल्यमयी माँ तो बिल्कुल भी नहीं। उस समय उनके चेहरे पर एक उजास होता। वह उजास की चौंध से घबड़ा जाती। फिर भी वह लपक उसे बाँधती थी। वह माँ को सुनती, बस सुनती रहती बगैर कुछ समझे-जाने। पिता के लिए यह सुविधा नहीं थी उसके पास। पिता अभिनय और घर को बिल्कुल अलग-अलग रखते और नीला को तो उससे कोसों दूर रखना चाहते। क्यों, नीला को यह पूछने का हक नही था और न पिता को कोई बताने की जरूरत।
माँ पिता के नाटक को तमाशा कहती और पूरे जोर देकर कहती – ‘यह तमाशा नहीं तो और क्या है?’ पिता हँसकर ग़ालिब का वह मिसरा दुहरा देते – ‘बागीचा-ए-अत्फाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे।’ तुम कुछ अलग क्या कह गई लक्ष्मी? यह दुनिया ही अपने आप में एक तमाशा है।’ और पिता के लिए माँ का रियाज रिरियाना। माँ आलाप लेतीं पिता स्टडी भीतर से बंद कर लेते। उसे हैरत होती, दोनों कलाकार थे, पूरे तन-मन से कलाकार। कला के रस-रंग मे डूबे हुए। पर एक दूसरे की कला के लिए उनके मन में सहजता नहीं थी। सहजता नहीं थी तो सुहृदयता कैसे होती? उसे हैरत होती। वे दोनों साथ-साथ थे तो आखिर कैसे? हाँ अपने दुनियावी रिश्ते में वे पूरी तरह सहज थे; परिवार और अपनी जिम्मेवारियों के लिए तो और भी ज्यादा।
वर्जना खींचती है अपनी तरफ, बाँधती है लगाव के एक अलग डोर से। माँ सहज प्राप्य थी, उसकी कला भी। नीला चाहते हुए भी नहीं बँध सकी उसके मोह से। पिता का आभामंडल उसे बेतरह खींचता। वह उम्र के उस सत्रहवें बरस में थी जब जिद साँस की तरह बसी होती है हम सबके भीतर। पिता को नाटक में उसी के उम्र की एक लड़की की तलाश थी। नाटक में काम करनेवाली लड़की बीमार हो गई थी अचानक। कोई मिलती भी तो पिता के खाँचे में फिट नहीं आती। बस दो दिन बचे थे। निर्देशक के लिए जीवन-मरण का प्रश्न। नीला जा खड़ी हुई थी उनके आगे। पिता फिर भी नहीं माने थे। नीला ने सत्याग्रह कर दिया था। वह खाई ही नहीं थी कुछ उस पूरे दिन। माँ ने कहा था मान लीजिए उसकी बात। उसे हैरत हुई थी। पिता फिर भी नहीं माने थे। धीरे-धीरे पिता को उसकी हठ के आगे झुकना पड़ा था। उसने बचे एक दिन में पूरा संवाद कंठस्थ कर लिया था; बचे वक्त में पिता जो-जो कहते, जिस-जिस तरह करते वह ठीक उनके अनुकरण में वैसा ही करके दिखाती; उसी आवेग, उसी त्वरा के साथ। पिता के हाथों की जैसे कठपुतली हो वह। पिता चकित थे, माँ नहीं। वह कहती – ‘मछली के बच्चे को तैरना सिखाने की जरूरत नहीं होती कृष्ण।’
पिता माने थे सिर्फ उस एक नाटक के लिए; आगे के लिए एक बड़ा सा पूर्णविराम। नीला जानती थी यहाँ इस बिंदु पर पूर्णविराम तो बिल्कुल नहीं। पूर्णविराम उसकी जिंदगी में कभी आएगा ही नहीं उसे उस वक्त पता था या नहीं उसे ठीक-ठीक याद नहीं। पर एक लंबी यात्र पर चल चुकी थी वह उसी दिन, उसी पल।
मन उसका चंचल था, बहुत चंचल। आवेग भी उतने ही सारे। किसी एक निर्णय पर, एक पड़ाव पर ठहरना, ठहर जाना बहुत ही मुश्किल। जैसे किसी लंबी यात्रा पर निकली हो वह। भागती रही वह कभी पगडंडियों के सहारे। कभी चौड़ी चमकीली राहों पर। पर चौड़ी राहें भी शायद मृग्तृष्णा ही थीं। दो कदम चलो कि फिर वही टूटम-टाट। वही रोड़े-रुखड़े…
पिता का मन रखते हुए उसने विज्ञान संकाय में दाखिला ले लिया, पिता चाहते थे वह इंजीनियर बने। पर थोड़े दिन बाद ही उसका मन इन प्रयोग कक्षाओं से ऊबने लगा। सब के सब नीरस, घिसे-पिटे, बेकार… वह कला में दाखिला लेना चाहती थी। समाजविज्ञान, मनोविज्ञान, साहित्य सब के सब विषय उसे मन से जुड़े लगते। मन के बहुत करीब। और सब से अच्छी बात तो यह है कि इन सबको पढ़ते हुए वह नाटक के लिए समय निकाल सकती थी; ये सारे विषय नाटक करने में सहायक ही सिद्ध होते वह जानती थी। पर यह बात वह पिता से कहती भी तो कैसे? पिता उससे एक नाटक में अभिनय करवाने के अपने निर्णय पर पछताए तो? वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी।
उसने एक रास्ता निकाला था। वह जाकर अपने कालेज के प्रिंसीपल से मिली थी। उनसे अपनी सारी परेशानी बताकर यह अनुरोध किया था कि उसका विषय विज्ञान से बदल कर कला कर दिया जाय। यह पिता के साथ ज्यादती थी। , वह जानती थी कि यह वह गलत कर रही है। पर कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था उसके पास। प्रिंसीपल को इसमें कोई परेशानी नहीं थी। उन्होंने इससे जुड़ी सारी प्रक्रिया को तुरत फुरत निबटा दिया। फिर उसके हाथ एक फार्म थमाया जिस पर पिता के हस्ताक्षर की आवश्यकता थी। वह परेशान हो उठी, बात तो फिर वहीं आ अटकी। वह फार्म उसके पर्स में घूम रहा था लगातार, ठीक हर पल उसके मन में चलते हुए उहापोह की तरह। उसने कला कक्षाओं में बैठना शुरू कर दिया था पर पिता से क्या कहे वह? उस दिन वह सुबह की कक्षा से लौटी थी, पिता घर में ही थे। उन्होंने पूछा था – तुम इस वक्त? वे जानते थे विज्ञान की कक्षाएँ देर तक चलती हैं, उसने धीमे से कहा था – ‘मैंने कला संकाय में एडमिशन ले लिया है। ‘तो फार्म मुझे लाकर देना मैं हस्ताक्षर कर दूँगा।’ नीला इस जवाब से क्षण भर को चौंकी थी। पर उसने तुरंत ही कहा था – ‘फार्म मेरे पर्स में ही है।’ ‘तो दो मुझे।’
वह हँसी थी इस तनावपूर्ण स्थिति में भी। अब सोचो तो उसे अपने ही जीवन के ये दृश्य किसी नाटक के दृश्य की तरह लगते हैं। विगत हमेशा उसके लिए वर्तमान को सहने के लायक बनानेवाला रहा है। खासकर पिता और पिता से जुड़ी स्मृतियाँ। वह तनावपूर्ण से तनावपूर्ण स्थितियों में भी पिता से सब कुछ कह जाती थी। और पिता से कह देने भर से जैसे सब कुछ सहज हो जाता, सँभल जाता।
पर आज पिता नहीं थे। दरवाजे के सामने भीड़ खड़ी थी हो-हल्ला, हंगामे और जुमलेबाजियों से भरपूर। पैसे वापसी के लिए पब्लिक की चिल्ल-पों के बीच हाल का घबड़ाया हुआ मैनेजर बीच-बीच में आकर उसे पुलिस के आने और उसके सुरक्षित निकल जाने का आश्वासन दे जा रहा था।
उसने पिता से ही पूछना चाहा था कि आखिर गलती कहाँ हो गई थी उससे। पर जवाब मिले भी तो कहाँ से? पिता नहीं थे अब उसके पास। सेक्यूरिटी गार्ड उसे पीछे के रास्ते से निकाल ले गए थे। बहुत आगे निकलने के बाद भी भीड़ की आवाजें उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। ‘तमाशा नर्तकियों का गुणगान छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो भ्रष्टता का महिमामंडन नहीं चलेगा… नहीं चलेगा… नहीं चलेगा… नीला देवी बाहर आओ, बाहर आओ-बाहर आओ। हमारे सवालों का जवाब दो, जवाब दो – जवाब दो…’
वह रास्ते भर सोचती रही थी वे औरतें जो अपने परिवार की जिम्मेवारियों की खातिर इस पेशे में आई भ्रष्ट कैसे हो सकती हैं। और फिर इन लोगों को यह अधिकार दे दिया तो किसने कि ये तय करें कि कौन भ्रष्ट है और कौन पवित्र? नहीं उसने कुछ भी गलत नहीं किया। वो ऐसे लोगों की हरकतों को मन से कैसे लगा सकती है। वह किसी के आगे झुकेगी-डरेगी नहीं, उसे सुषमा याद आई जिसके पिता और माँ ने ही उसे तमाशा नर्तकी बनने को मजबूर किया था। कांता भी, जिसने अपनी बहन की शादी और भाई की पढ़ाई की खतिर इस काम को चुना था। जिसकी बीमारी के वक्त भी उसके परिवार का कोई उससे मिलने तक नहीं गया था। और जब ठीक होकर वह अपनी माँ से मिलने गई थी और उसने यह कहा था कि उन लोगों के सुखों की खातिर ही उसने अपनी जिंदगी होम कर दी तो उसकी माँ ने कठोरता से कह था – ‘हमने तो तुम्हें कभी ऐसा करने को नहीं कहा।’
विभा बाई जो बच्चा जनने के तुरंत बाद प्रस्तुति के लिए उठ खड़ी हुई थी क्यों कि वह कांट्रैक्ट से बँधी हुई थी और वह सपना जिसका बच्चा स्टेज शो की अफरा-तफरी में किसे दूसरी नर्तकी के पैरों तले कुचल गया था… ऐसी औरतें… ये सब औरतें कुत्सित कैसे हो सकती हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि विवाह न करने के नियम से बँधी हैं ये, और फिर भी उनके जीवन में पुरुषों के होने पर रोक नहीं है? वह सोच रही थी लगातार…
उसने अपने जीवन के पूरे सात वर्ष झोंक दिए थे इस एक प्रस्तुति की स्क्रिप्ट लिखने और इसकी तैयारी में। शुरुआत में तमाशा थियेटरों के मालिक ही उसे भीतर जाने और बात करने देने से कतराते थे लेकिन धीरे-धीरे वह उन्हें विश्वास दिला सकी कि वह उनका कोई इंटरव्यू नहीं करने जा रही। वह तो तमाशा पर शोध कर रही है कि उसके खास शैली ‘ढोलकी फड़’ और ‘संगीत बारी’ के बीच का अंतर जानने आई है। वह फिल्मों से प्रेरित और भ्रष्ट नृत्य नहीं बल्कि मूल ‘लावणी’ देखना चाहती है। वह जानना चाहती है कि यह कैसा होता है।
पूरे नौ महीने वह उन औरतों से सिर्फ लावणी पर ही बात करती रही थी, वे भी कभी भूले से भी अपने जीवन के बारे में कुछ नहीं कहतीं। हँसती-खेलती, बोलती-बतियाती रहती आपस में। उन्हें लगने लगा था नीला जैसे उनमें से ही एक हो। थियेटर मालिकों को भी अब उनसे कोई दिक्कत नहीं रह गई थी, उनका अंकुश भी कम होता गया था धीरे-धीरे। वह उनके साथ हर जगह जाने लगी थी। पूर्वाभ्यास में हर जगह वह उनके साथ होती, उनका पकाया तीखा मसालेदार मांस शौक से खाती। उन्हें जरूरी सुझाव भी देती। धीरे-धीरे वे सहेलियों सी हो चली थी। सहेली जैसा उनका अंतरंग भी एक हो चला था धीरे-धीरे, अपने आप औए बहुत गुपचुप तरीके से
कभी-कभी कहतीं वे – ‘साथी पति तो नहीं होता न। पति आखिर कैसा होता होगा, बहुत अधिकार जताता होगा स्त्री पर? पर उसे आराम से रखता होगा घर में, रानी बना कर। कितना सुख होता होग इस में? ऐसा ही होता है क्या? वे नीला से पूछती। नीला चुप रह जाती। यह अधिकार जताना, यह घर की रानी बना कर रखना सोचने में जितना सुंदर और सुहावना लगता हो, नीला जनती थी उस कैद की हकीकत। अभी-अभी तो अलग हुए थे सिद्धार्थ और वह। पर वह कहती कुछ भी नहीं। उनके पति नामक फैंटेसी को नहीं तोड़ना चाहती थी वह… या कि एक झूठा बहाना भर था यह? वे जब खुल गई थीं उससे फिर वह क्यों नहीं खुल पाती? उसका आभिजात्य, उसके संस्कार क्यों-क्यों बंद कर देते हैं उसका मुँह।, जबकि वह भी खुलकर कहना चहती है किसी से अपनी तकलीफ; किसी के कंधे पर सिर रख के रो लेना चाहती है जी भर, बहुत अर्से से। और वह तो अभिनेत्री है स्वभाव से ही सबसे घुल-मिल, रच-बस जानेवाली…?
घर सामने आ खड़ा हुआ था चुपचाप। गाड़ी भी इतनी बेआवाज रुकी थी कि चौंक उठी थी। अंतरंग से बहर आना, वह भी इतना अचानक…
उसने खाया नहीं था, पिता की डायरी निकाल ली थी चुपचाप। विश्वास के कितनी बार कहने के बावजूद, पिता के नहीं रहने के बाद से वह इन्हीं में ढूँढ़ती है पिता को… और अपने सवालों के जवाब… जैसे कि दादी ढूँढ़ती फिरती थी रामचरित मानस के रामशलाका में अपने हर प्रश्न का हल।
वह क्रमवार पन्ने पलट रही थी – ‘यदि आप अपने अंतःकरण की गहराई में डूब सकते हैं और तब अपने भीतर को बाहर आने दें तभी एक राह बनती है जिस पर चल कर आप लोगों के अर्धचेतन से संपर्क कर उसके मन के भीतर उतर सकते हैं। और तब आप जो भी कह या समझ रहे हैं लोग उस तक बेरोक-टोक, बेझिझक पहुँचेंगे।
‘नाट्यशास्त्र कहता है, अभिनेता एक पात्र है, पात्र का अर्थ बर्तन भी होता है। पात्र खाली होता है ताकि बाहरी चीजें उसमें समा सकें। अभिनेता को भी खाली होना होता है, रिक्त करना होता है अपने मैं को। इसके लिए ‘मुक्ति’ ठीक-ठीक शब्द है या नहीं मैं तय नहीं कर पा रहा। खाली होने के बाद पुनः स्वयं को भरना और भरे जाने के बाद उलीच देना…।’ वह परेशान थी। यहाँ पिता थे, उनकी बातें भी थी पर हर बार की तरह वह नहीं था जिसकी तलाश थी उसे इस वक्त। वह पन्ने पलट रही थी जहाँ-तहाँ से। फिर भी उसे कुछ ऐसा नहीं मिल रहा था जिसमें तलाश ले वह अपने प्रश्नों के उत्तर। ऐसा पहली बार हुआ था।
विश्वास और उजाला को पता था उदास है वह आज। दोनों जान रहे थे आज क्या हुआ है उसके साथ। फिर भी किसी ने न उससे कुछ पूछा, न उसने कुछ बताया। उसे जबरन खाने की मेज पर ला बैठाया गया था। वे कह-सुन रहे थे कोई दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं बातें। विश्वास के उसकी जिंदगी में आने के पूर्व उसे हमेशा यह लगता था कि घर और काम दोनों दो ध्रुव होते हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा दो समानांतर रेखाएँ जिनका मिलना असंभव है कहीं भी। वह दुखी होती इस बावत तो पिता से कहती भी। पिता हमेशा समझाते – ‘पुरुष और स्त्री के लालन-पालन में फर्क होता है, उनके विकासक्रम में भी। पुरुष एक समय में एक ही काम पर ध्यान लगा सकता है जबकि स्त्रियाँ बचपन से ही एक ही समय में कई बातें सोचती और कई काम करती हैं। तुम मुझे और अपनी माँ को ही देख लो। वह घर भी चलाती है, स्कूल में पढ़ाती भी है और उसने अपनी गायकी को भी नहीं छोड़ा। तुम्हारे लालन-पालन में भी उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। जबकि मैं सिर्फ अपने अभिनय में जुटा रहा। घर और काम दो समानांतर रेखाएँ होती होंगी पर चाहने से क्या नहीं हो सकता। प्रयास करो नीला ये रेखाएँ भी आपस मे कहीं मिलेंगी जरूर। पिता कहते रहे और मैं प्रयास करती रही। प्रयास की नाकामियाँ मेरे चेहरे पर निराशा बन कर जरूर उभरती होंगी। पिता भाँप रहे थे जैसे सब कुछ।
उन्होंने उसे पास बैठाया था एक दिन और बात की शुरुआत भी अपने ही अंदाज में की थी – ‘तुमने विज्ञान पढ़ना क्यों छोड़ा था अचानक …?’
‘मुझे लगा मैंने अपने दवाब में यह निर्णय लिया था और वह मुझे रास नहीं आ रहा।’
‘फिर पत्रकारिता?’
‘उस वक्त मुझे लगा था कि मैं अपने भीतर की बेचैनी और खोज को इस तरह अभिव्यक्ति दे पाऊँगी और मुझे शांति भी मिलती थी उसे करके।
‘फिर…?’
‘मैं उस दिन नववधुओं को जलाए जाने वाले लेख के सिलसिले में ‘बर्न वार्ड’ गई थी। मैं वहाँ पति और सास द्वारा जलाई गई एक लड़की से मिली थी। वह ९०% जली हुई थी लेकिन उस हाल में भी उन लोगों के खिलाफ मुँह खोलने को तैयार नहीं थी क्योंकि उसके दो बच्चे थे जिन्हें उसी परिवार में रहना था और उसके मायके में सिवाय भाई-भाभी के और कोई नहीं था जिन्हें उसमें या उसके बच्चों में कोई दिल्चस्पी नहीं थी।’ नीला चुप हो गई थी कुछ देर को और पिता ने भी नहीं कुछ कहा था इस बीच… ‘एक और औरत थी वहाँ जो गर्भ से थी। डाक्टर ने उसके ससुराल वालों से कहा था वह तो नहीं बच सकती हाँ यदि वे चाहें तो बच्चे को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। वह औरत भी बार-बार अपने पति से रो-रोकर बच्चे को बचाने की गुहार करती रही लेकिन उस आदमी ने अकेले में डाक्टर से यह कहा कि वह नहीं चाहता कि इस बच्चे को बचा लिया जाय, वैसे भी वह इस बच्चे का क्या करेगा? मैं बिल्कुल अवाक थी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे एक मासूम के लिए मन में इतनी दुर्भावना… बहुत दिनों तक मैं वह वार्ड, जले हुए मांस, दवाओं और सड़न को हर पल अपने आस-पास महसूस करती रही। मैंने उस पर लेख लिखा। कालेज में कुछ स्लाइड शो भी किए प्रशंसा और अवार्ड भी मिले मुझे। लेकिन वह गंध, वे आवाजें मेरे चारों तरफ भटकती रहती, मुझे हर पल लगता रहा कि मैं उनके भीतर की पीड़ा को उनके दर्द को ठीक-ठीक अभिव्यक्त नहीं कर पा रही। मैंने केवल प्रशंसा और सराहना भर नहीं चाही थी मै कुछ और चाहती थी… पर क्या…? मैं खुद नहीं जानती थी…’
‘फिर?’
‘नाटकों तक सीधे-सीधे नहीं लौटना चाहती थी मैं, आपका दिल दुखाकर। सोचा था अभिनय के पहले कुछ तैयारी भी हो जाए सो समाजशास्त्र में एम.ए. किया, पुनः मनोविज्ञान में। फिर लगा सब बेकार है, बहुत हो चुकी तैयारी-वैयारी सो मैं नाटकों तक लौट आई। मुझे लगा था अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम यही है मेरे लिए…। लेकिन अब… किया धरा सब कुछ बेकार चला गया… सारी मेहनत जाया हो गई।’
पिता मित्र हो चले थे – ‘इस तरह कुछ भी बेकार नहीं होता नीला तुम्हारे अभिनय में तुम्हारी पूरी यात्रा बोलती हैं… तुम पर गर्व है मुझे और अगर कुछ गलत हो जाए, बिगड़ जाए तो उसे सुधारना समझदारी है न? तुमने तो हमेशा अपने निर्णयों पर सोचा है, तौला है उन्हें…’
नीला चुप थी, चुप ही रही…
‘सिद्धार्थ के साथ अपनी जिंदगी के बारे में क्या सोचा है तुमने?’
‘मुश्किल है पापा, बहुत मुश्किल पर जीना तो होगा न? यह फैसला तो मैंने ही लिया था… शायद नाटक छोड़ना पड़े…’
‘सिर्फ तुमने खुद फैसला लिया था इसलिए? तू नाटक छोड़कर जी पाएगी? खुद को और कितना सजा दोगी नीला?’
‘पर चारा भी क्या है?’
‘उपाय है नीला, तुम खुद सोचो… फिर निर्णय लो… शांत मन से… मन जो कहे… हमेशा की तरह।’
…और विश्वास को पाकर लगा पिता सही थे… और उसका निर्णय भी… यह विश्वास के साथ ही उसने जाना कि घर और काम जिसे वह अब तक दो समानांतर रेखाएँ समझती थी कहीं किसी धुरी पर मिल भी सकते हैं, कि ठीक ही कहते थे पिता।
वह रसोई बनाते-बनाते दिमाग में नाटक को चलने देती। बाहर आती रसोई से तो रसोई के ही कुछ उपकरण साथ लेती आती और अभ्यास-कक्ष के फर्श पर उन्हें यहाँ-वहाँ छोड़ देती। वे ही छोटे-छोटे उपकरण सहयोगी से हो जाते उसके, रूप-भाव बदल-बदल कर।
वह माँ बनने को आई… अब नाटक नहीं कर सकती थी। विश्वास फिर भी उसे रिहर्सल में ले जाते, कई बार सेट पर भी। कभी वह संवाद बेहतर करती तो कभी सेट का डिजाईन तय करती। वे बातें करते लगातार नाटकों की, रात को देर-देर तक जागकर। विश्वास ने उसे लगने ही नहीं दिया कि उसका वास्ता नाटकों से अभी नहीं है। उजाला भी बहुत सब्रवाली बच्ची निकली। बिल्कुल भी शैतान नहीं। घंटों सोती वह। जगी भी हो तो काम करते, रिहर्सल करते उसे टुकुर-टुकुर देखती रहती। उसे लगता माँ को वह ऐसे ही देखती होगी छोटे में।
नाटक जब सिर चढ़कर बोलने लगते वह उजाला को दिन में सोने नहीं देती, खेलती रहती उससे भर दुपहरिया कि दिन भर की थकी वह शाम को जल्दी सो जाए। होता भी ठीक वैसा ही, फिर वह शाम को रिहर्सल में लग जाती, जहाँ सिवा विश्वास के किसी और को आने की इजाजत नहीं थी। एकांत में ही नीला पूर्णतः सजग हो पाती, डूब पाती अपने काम में। एक पत्रकार, नाटककार, अभिनेत्री और निर्देशक के तौर पर अपने काम को अलग-अलग दृष्टि से देखती, जज कर पाती वह। वह दर्शकों से संवाद स्थापित कर रही होती कि अचानक उसके भीतर के पत्रकार को लगता कि यहाँ तो नाटक के सौंदर्यबोध की बलि चढ़ गई। लेखक को कोई दृश्य जँच जाता लेकिन निर्देशक को वही अंश संरचना की दृष्टि से सबसे कमजोर लगता फलतः …इसीलिए वह नहीं चाहती थी कि इस पूरी प्रक्रिया में कोई और उसके सामने या साथ हो, विश्वास उससे अलग नहीं थे।
उसकी रचना प्रक्रिया के इस अजब-गजब ढंग को देखकर विश्वास कभी-कभी उसे खिजाने के लिए कहते यह जो तुम कर रही हो क्या है? समाजविज्ञानी, पत्रकारिता, निर्देशन या अभिनय? वह गर्व से पर कुछ मजाक का पुट लिए हुए कहती – थियेटर पत्रकारिता है यह।
विश्वास ने उसकी तरफ चादर बढ़ाया था, पानी का गिलास भी। सोते वक्त उसे पानी पीने की आदत थी…। वह मुस्कराई थी… सुबह नाश्ते के टेबल से अखबार गायब थी। उसने ढूँढ़ा चारों तरफ पर वह न मिलनेवाला था न मिला। विश्वास नहीं चाहते होंगे कल रात की घटना पर छपी अजीबोगरीब खबरें उसे परेशान या उद्वेलित करें।
विश्वास चले गए थे, उनका बिछावन ठीक करते वक्त चादर के ठीक नीचे अखबारें मिल गई थी उसे। अखबारों में छपा कुछ उसकी सोच से बहुत-बहुत ज्यादा था। वह तो सिर्फ… पर यहाँ तो राष्ट्रीय महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग के अधिकारियों के भी वक्तव्य थे। हद तक चौंकाऊ और विस्फोटक… महिला आयोग की अध्यक्ष का वक्तव्य था – ‘अभिनय एक सशक्त माध्यम है, समाज को सही-गलत की पहचान करवाने के लिए। नीला पंडित बताएँगी कि वो तमाशा की सताई हुई और दुखियारी महिलाओं के दुखों का महिमामंडन कर के महिलाओं और समाज के सामने कौन सा दृष्टांत पेश कर रही हैं? मानवाधिकार वालों ने कहा था कि ऐसी अमानवीय घटनाओं का चित्रांकन या अभिनय भी उसी हद तक अमानवीय कहा जाएगा। सच्चाई के नाम पर किसी घटना या दृश्य का वैसा ही चित्रण उस पूरी कौम, समुदाय और व्यक्ति-विशेष के अधिकारों का उल्लंघन है। क्या नीला पंडित के पास तमाशा थियेटर के मालिक या फिर उन महिलाओं के द्वारा दिए गए अनुमति पत्र है? क्षण भर के लिए नीला का विश्वास अपने आप से डगमगाने लगा था। अपने उद्देश्य, कृति और रचनाकर्म से भी। वह उन लोगों का विरोध कर सकती थी पर इनका? …नीला की बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई थी और विश्वास भी ऐसे में उसे छोड़ कर अकेले चले गए थे। उसे इस तरह अकेली छोड़ कर कैसे जा सकते हैं वह? खुद से ही पूछ रही थी वह…
फोन की घंटी बजी थी, उधर विश्वास ही थे – नीला घबड़ाना बिल्कुल नहीं, मैं शो तक आ जाऊँगा। किसी जरूरी काम से निकलना पड़ा अचानक मुझे। डी.आई.जी. मनोहर राजन ने भी कहा है – नीला जी निश्चिंत रहें फोन की घंटी फिर-फिर बजी थी… उधर हाल का मैनेजर था, सुरक्षा इंतजाम पुख्ता हैं, महौल जल्दी ही ठीक हो जाएगा, वे चिंतित न हों।
तीन दिन बीत चुके थे, आश्वासनों और ऊहापोह के बीच सब कुछ सँभल नहीं सका था। हाँ सँभल और सुलझ जाने की आशा जरूर जताई जा रही थी। नीला करे भी तो क्या उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। रिहर्सल में मन अब बिल्कुल नहीं लग रहा था और ऐसे में नया कुछ करने का दिमाग में आ ही कैसे सकता था। वह बैठी-बैठी बस पुराने दिनों को याद करती रहती। अभी-अभी उसे याद आ रह था पिता के साथ किए गए नाटक के बाद का पहला नाटक। यह उसके एम.ए. का अंतिम सत्र था। पिता को उसने इसकी भनक तक नहीं लगने दी थी। नाटक दहेज-प्रथा से संबंधित था। कालेज भले ही सह-शिक्षावाला हो पर लड़कियाँ इनी-गिनी ही थी उसकी कक्षा में। पर नाटक में काम करनेवाली सब की सब लड़कियाँ ही थी। लड़कों को जैसे इस विषय से ही अरुचि थी। वे ठाने बैठे थे नाटक को नहीं होने देना है। इधर नाटक शुरू हुआ उधर शोर-गुल। उसकी आवाज उनके प्रायोजित शोर-गुल में जैसे गुम होती जा रही थी। उसने जोर-जोर से बोलना शुरू किया। वे और जोर-जोर से हूट करने लगे थे। उसने उधर ध्यान देना बंदकर अपनी आवाज को बुलंद बनाए रखा। उसकी आवाज उनकी आवाज दबाने के प्रयास में तेज, तेज और तेजतर होती जा रही थी। वे सिर्फ उसे हूट ही नहीं भयभीत भी करना चाह रहे थे उनकी आवाजें बेहूदी और गंदी होती जा रही थी। उसको लग रहा था चीख-चीख कर वह अभिनय का बंटाधार किए दे रही होगी। नाटक लगभग आधे पर आ पहुँचा था जब उनके बीच से ही कोई आवाज उठी थी – ‘बहुत हुआ, अब चुप करो… कुछ सुनने भी दो यार।’ फिर इस आवाज के सहयोग और प्रभाव में कुछ आवाजें और साथ आ मिली। आवाजें दबती-दबती कम हो चली थी। उसको लगा उनकी जीत हुई थी। चाहे तो कोई इसे उसकी सोच का बचकानापन कह सकता है। उस दिन नाटक खत्म होते ही पिता बैक स्टेज तक आए थे और उसे गले लगा लिया था। हाँ, वह देख नहीं सकी थी पिता हाल में कहीं पीछे के कतार में बैठे थे, उन्हें लोगों ने इस नाटक के विषय में सूचित कर दिया था।
उसका भय जाता रहा था। उसने पिता से रास्ते में पूछा था – ‘पहले आप मेरे नाटकों में आने का विरोध इस तरह क्यों करते रहे थे? माँ अक्सर कहती मुझसे तुम्हारे पिता भी अन्य फिल्म और नाटकवालों की तरह इस ग्रंथि से पीड़ित हैं कि यह क्षेत्र औरतों के लिए सुरक्षित नहीं है और इसीलिए वे अपने परिवार की किसी स्त्री को इस क्षेत्र में आने नहीं देना चाहते।’ पिता ने हँस दी थी हमेशा की तरह एक संक्षिप्त पर प्यारी हँसी। उस हँसी से उसका दुस्साहस और बढ़ा था… और मेरी तो हिम्मत ही टूट जाती थी। आप मना कर रहे हैं, मतलब जरूर कोई गहरी बात है… आप जो स्वयं नाटकों के दीवाने हैं… उन्होंने हँस कर कहा था – ‘मैं विरोध नहीं कर रहा था, मैं तो तुम्हारी हिम्मत और ताकत परखना चाह रहा था। मैं चाहता था तुम्हारे भीतर इसके लिए ललक हो, पैशन हो और अगर तुम इसे अपनाओ तो अपनी इच्छा से अपनाओ, बस…’
क्षण भर को उनका स्वर मजाकिया हो उठा था। ‘तुम्हारी मम्मी नहीं समझ सकेंगी मेरे मन की बात उनके पास मेरे जितना दिमाग भी तो नहीं। मैं इतनी जोर से प्रतिरोध करता था कि तुम मेरी तरफ खिंचो… अपनी माँ की तरह रिरियाने में अपना मन न रमा दो…’ उसने दुलार में पिता के कंधे को पकड़ कर झुलाया था, ‘यह गलत बात है पापा, मैं माँ को बता दूँगी यह सब। माँ के लिए ऐसी बात करना अच्छी बात नहीं।’ क्षण भर के मजाक के बाद पिता पुनः गंभीर हो गए थे ‘मैं तुम्हारी ईच्छाशक्ति और जीवटता से प्रभवित हूँ। आज तुमने जमकर हिम्मत दिखाई। बहुत कुछ युद्ध की तरह। …नुक्कड़ नाटकों में भी ऐसा ही होता है, आप उनकी ईच्छा से नहीं होते, टिकट खरीद कर नहीं देख रहे होते ये आपको। आप परिहार्य हैं इतने से ही बहुत फर्क पड़ जाता है। आपको अपने अभिनय से बाँधना होता है उन्हें, खींचना होता है अपनी तरफ, मुझे देखो, मैं आश्वासन देता/देती हूँ यह आपको रुचिकर लगेगा, निराश नहीं होंगे आप…’ पहले से दूसरे नाटक के बीच पुनः डेढ़ साल का अंतर था। यह चुप्पी नहीं थी। अगला स्क्रिप्ट उसने बलात्कार पर लिखा। पर केंद्र में बलात्कार न हो कर उसका कानून था। उसने वो सारे तरीके इकट्ठे किए जिसमें बलात्कार दिखाए बगैर भी बलात्कार का इंपैक्ट पैदा हो। इस बार मुकाबला कालेजों के बीच था। कल के विरोध करनेवाले साथी आज उसका मनोबल बढ़ा रहे थे। यह एक छोटी पर लंबी यात्र थी। प्रदर्शन के वक्त घनी चुप्पी थी, तनाव और शांति से भरी चुप्पी। पिता ने इस बार उससे कहा था ‘अब तुम मेरे साथ काम करने लायक हो चुकी हो। मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रहा था। आज वह दिन आखिर आ ही गया। मेरे पास एक स्क्रिप्ट है, क्या तुम मेरे साथ काम करना पसंद करोगी?’
पूरे तीन दिन नाटक का मंचन बाधित रहा और तीनों दिन वह पिता तक उनकी स्मृतियों के सहारे लौटती रही तो सिर्फ इसलिए की उसके प्रश्नों का, ऊहापोहों का हल यहीं कहीं हो। यहाँ तक पहुँचते-पहुँचते उसे यह विश्वास होने लगा था, वह सही जगह आ पहुँची है, न जाने क्यों…
वह मंटो की ‘खोल दो’ कहानी का नाट्यांतर था। उसने पिता की दी पूरी स्क्रिप्ट पढ़ ली थी। पिता ने आखिर यही स्क्रिप्ट क्यों चुना उसके लिए? पढ़ कर जैसे भीतर तक हिली हुई थी वह। इस बीच पूरे तीन दिन बीत चुके थे। चौथे दिन पिता ने पूछा था -‘तुमने स्क्रिप्ट पढ़ ली?’ उसने चुपके से सिर हिलाया था – ‘हाँ…।’ ‘कैसी लगी…?’ उसके पास जैसे शब्द नहीं थे… वह चुप ही रही…। ‘क्या समझा…?’ वह खुद को बटोर कर बोलने की कोशिश में थी… ‘स्त्री की त्रासदी… उसका हर हाल में रौंदा जाना… देश काल …धर्म के नाम पर’ उसके जुबान से शब्द जैसे रुक-रुक कर निकल रहे थे, अटक-अटक कर। वह जैसे स्वयं को अभिव्यक्ति ही नहीं दे पा रही थी, ‘वह’ जो स्वयं को अभिनेत्री कहलाने का, होने का दंभ पालती है।
पिता मुलायम हुए थे – ‘इतना ही नहीं बेटा, सिर्फ इतना ही नहीं। एक पिता को, उसके मन को। उसकी प्रतीक्षा की तीव्रता को, उसके खोज की गहनता को उसके न टूटनेवाले आस को… वह बेटी की खोज में। उसके प्रेम में ऐसे डूबा होता है कि वह उसे अपने ही शरीर में देखने लगता है। मूलतः उसी के रक्त मांस से तो बनी है वह। दुपभ जो बचा रह गया है उसके जाने के बाद वह उसे ओढ़े फिरता है। चूड़ियाँ… सचमुच उसी की कलाइयों में होती है… और उसके हाथ स्वयं वही हाथ जिसे वह उर्दू वर्णमाला के अक्षर सिखाता रहा था बचपन में। ‘
पिता स्क्रिप्ट पढ़ कर पुनः सुनाते हैं उसे – ‘यह एक पिता की कहानी है, जिसने विभाजन के काल-खंड में पागल उन्मत्त भीड़ के बीच अपनी बेटी को खो दिया है। माँ जो एक ओर उन्मत्त भीड़ के द्वारा पेट फाड़ दिए जाने के कारण अंतिम साँस गिनती होती है कहती है आप लड़की को लेकर भाग जाओ। मैं कहाँ बचूँगी, इसे किसी तरह से बचा लो। कुछ ऊहापोह के बाद पिता बेटी को लेकर चल देता है। सिराजुद्दीन और उसकी बेटी सकीना भागे जा रहे हैं कि तभी सकीना का दुपट्टा पीछे कहीं गिर जाता है। अब बाप तो बाप है। वह दुपट्टा उठा लाने के लिए पलट पड़ता है, बेटी के मना करने के बावजूद। पिता पिता से सिराजुद्दीन हुए जा रहे हैं। मैं अचानक बोल उठती हूँ। पिता का हाथ जबरन थामकर – ‘रहने दो अब्बा।’ वह चौंक जाती है पर पिता चौंकते नहीं, रहने कैसे दूँ बेटा… वह तेरा दुपट्टा है। पिता लौटते हैं, दुपट्टा लेकर तो बेटी लापता। वह ढूँढ़ता रहता है उसे लगातार। इस क्रम में उसे आठ लोग मिलते हैं जो उससे प्रकटतः सहानुभूति दिखाते हैं, कहते हैं सकीना एक-न-एक दिन उसे जरूर मिल जाएगी पर ये वही लोग हैं जिन्होंने उसे एक कोठरी में बंद कर रखा है।
सकीना एक दिन पिता को शरणार्थी कैंप में मिलती है, मरणासन्न अवस्था में। वे ही लोग उसे वहाँ छोड़ आए रहते हैं। अगला दृश्य शरणार्थी कैंप का है जहाँ डाक्टर मरीजों का परीक्षण कर रहे हैं। डाक्टर अच्छी तरह से मुआईना कर पाने के लिए पिता से कहते हैं कि वो खिड़की-दरवाजे खोल दें ताकि रोशनी भीतर तक आ सके। लड़की के निर्जीव हाथ ‘खोल दो’ शब्द सुन कर उस अचेतनता में भी अपने सलवार के नाड़े खोलने लगते हैं। कहानी यहीं खत्म हो जाती है। डाक्टर स्तब्ध है इस त्रासदी से। उसके हाथों से ठंडा पसीना आने लगता है। वह जान जाता है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है, बार-बार…
कहते-कहते पिता चुप हो जाते हैं, अजीब निरीह नजरों से घूर रहे हैं उसे। क्या उनके भीतर का पिता जागा है? अपनी बच्ची को आखिर क्या सुना रहे हैं वह? पिता सहेज लेते हैं खुद को। वह खुद भी एक निर्देशक और कलाकार है, सामने भी एक कलाकार – आगे का दृश्य बहुत दुखद है।, बहुत मार्मिक पर आगे देखो – डाक्टर का शरीर ठंडे पसीने से तरबतर है। पर पिता… प्रसन्नता से नाच उठता है, रो उठता है। उसकी बेटी जिंदा है। जिंदा है अंततः वह और उसने उसे तलाश लिया है। हासिल कर लिया है आखिर अपनी बच्ची को। एक जिंदा शब्द से ही कितनी आशाएँ, कितने सपने जुड़े रहते हैं। उम्मीद है यह एक नई जिंदगी की। पिता के मन में एक उम्मीद है सब कुछ के बावजूद वह फिर एक नई जिंदगी देगा अपनी बच्ची को। यह अंत कहानी से अलग है। यथास्थिति से अलग एक स्वप्नजीवी, स्वप्नवादी-आशावादी अंत। कभी भी किसी नाटक या कहानी को किसी एक कोण से नहीं पढ़ना देखना। एक दृष्टि से भी नहीं। अपनी सोच अपनी कल्पना को खुला रखोगी तो… रुककर पिता कहते हैं – यह एक एकल प्रस्तुति होगी। कर पाओगी न? वह इस पूरे प्रकरण में पहली बार पिता की नजर से नजर मिलाकर कहती है – ‘हाँ।’
पिता ने उस दिन एक सूत्र थमाया था – बेटी को तलाशता पिता बेटी में तब्दील हो गया था, बेटी उसके रक्त मांस से ही तो बनी थी।
फिर वह खुद से बाहर कहाँ तलाशती फिर रही है पिता को, फिर वह खुद से बाहर कहाँ सवाल का जवाब ढूँढ़ रही है, पिता क्या करते ऐसे वक्त में? पिता को तो उसने कभी हिम्मत हारते नहीं देखा, किसी भी परिस्थिति में। फिर उन्ही के रक्त मांस से बनी वह…
चौथे दिन नीला फिर नाटक के रिहर्सल में व्यस्त है। संगीतकार गायब है… वह खुद संगीत दे रही है। सुनती तो रही है बचपन भर माँ को उनके सामने बैठ कर। कहते तो थे पिता कुछ भी जाया नहीं जाता… कहती तो थी माँ मछली के बच्चे को तैरना सिखाने की जरूरत नहीं होती। वह वह कहाँ रह गई है… कभी पिता, कभी माँ, कभी बेटी हुइ जाती है। थोड़े हैरत और थोड़ी खुशी के साथ विश्वास और उजाला भी उसके साथ हैं। वे इस कोशिश में है कि तनाव उसके मन से हट जाए। वे नहीं जानते, तनाव तो कब का हट चुका है उसके मन से।
उसने तमाशा के स्क्रिप्ट को माँ-बेटी के संवाद के रूप में लिखा है। पत्रकार बेटी जिसकी तमाशा करनेवाली माँ ने उसे अपने से दूर बोर्डिंग में रख कर पढ़ाया है ताकि वह कुछ कर सके जीवन में। उसकी जिंदगी न जीए। वह इसी शर्त पर बेटी को उस बोर्डिंग में डाल सकी है कि वह उससे मिलने नहीं आ सकती। पढाई पूरी होने पर वह बेटी के लौट आने की खुशी मना रही है। पर जो लौटती है वह एक बेटी नहीं पत्रकार है। वह गले नहीं मिलती उससे सवालों के कटघरों मे ला खड़ा करती है उसकी पूरी जिंदगी को। अपनी पूरी टीम और कैमरे के साथ। वही बार-बार दुहराए जानेवाले घिसे-पिटे सवाल… उसका मन था वह और उजाला कभी साथ-साथ इस नाटक को कर पाती। वही पिता वाली इच्छा। पर उजाला… उसकी तरह उजाला ने भी देखा है बचपन भर उसका पूर्वाभ्यास। शायद इसी से नहीं जुड़ पाई वह कभी नाटक से। उसके पास चुनने को दो चीजें थी संगीत या नाटक पर उजाला तो…
भीड़ बहुत ज्यादा नहीं है। इक्की-दुक्की भी नहीं। अफवाह और खबरें चीजों को सनसनीखेज और बिकाऊ तो बना ही देती हैं… वह टटोल रही है पर्दे के पीछे से दर्शकों को – जेनुईन कौन-कौन… नाटक कब शुरू हुआ, कब खत्म उसे कुछ पता ही नहीं चला, वह वह कहाँ रह गई थी…।
ग्रीन रूम में वह रो रही है फूट-फूट कर। उजाला आकर उसके गले लग जाती है… ‘माँ आप मुझे भी अपने नाटक में कोई रोल देंगी, मैं ठीक-ठीक करूँगी माँ… बोलिए न माँ।’ वह चुप है, उसके भीतर बैठे पिता कहते हैं, क्षणिक आकर्षण है यह, नहीं, अभी नहीं, इतनी जल्दी तो बिल्कुल नहीं। वह चुप रहती है थोड़ी देर… फिर कहती है ‘हाँ…’ वह अभी वह ही रहना चाहती है, पिता की तरह डिप्लोमैटिक होना नहीं चाहती। …उसने आगे जोड़ा है ‘तुम चाहो तो…’
विश्वास आए हैं भीतर, बधाई दी है उसे और कहा है – ‘कोई तुमसे मिलना चाहता है नीला’ …लावणीवाली… नौ गज की साड़ी पहने वह कोई तमाशावाली ही लग रही है पर पहचान की तो बिल्कुल नहीं। उसने उसके चेहरे को गौर से देखा है। वह भी आ कर गले लग जाती है उसके, उजाला और विश्वास की तरह। वह टूटी-फूटी हिंदी में कहती है – ‘जब भी मैं थकी होऊँगी तुम्हारा नाटक देखने जरूर आऊँगी और अपने साथ के पुरुष को बताऊँगी वह जो औरत देख रहे हो न तुम, उस ऊँचे मंच पर, वह मैं हूँ।’
उसकी पीड़ा, उसका ऊहापोह, उसके दुख सब बह चले हैं उसके आँसुओं में। उसे अब किसी की भी परवाह नहीं है…
Download PDF (तमाशा )
तमाशा – Tamasha