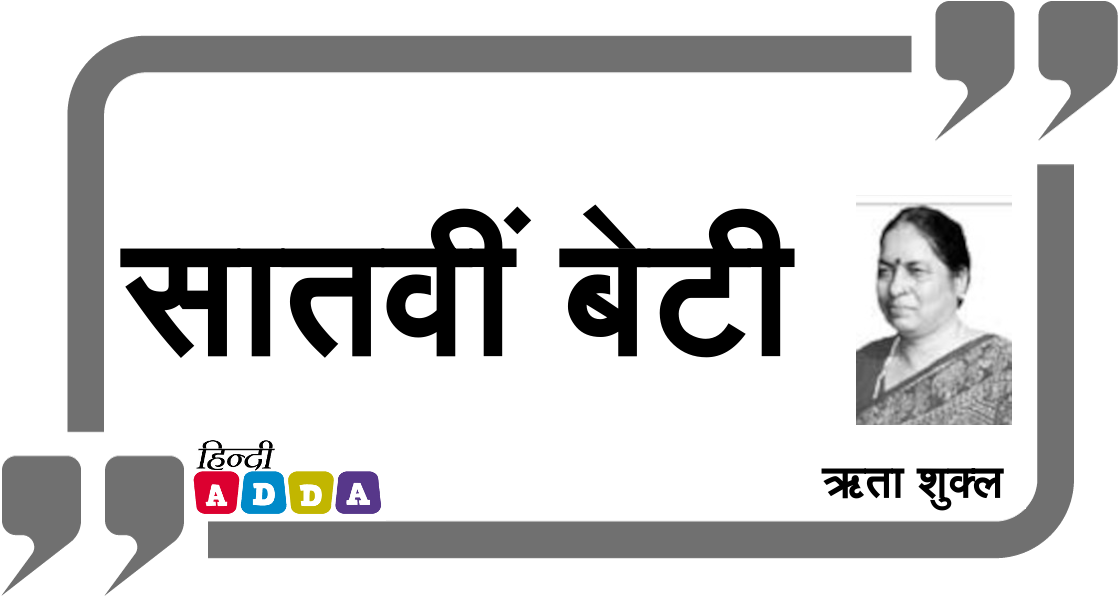सातवीं बेटी | ऋता शुक्ल – Satavi Beti
सातवीं बेटी | ऋता शुक्ल
अक्सर मुझसे लोग यह पूछा करते हैं-आप कहाँ की रहनेवाली हैं…? और मेरी जबान पर एक शब्द आता है-भोजपुर !… फिर लोग थोड़ी आश्चर्यचकित मुद्रा में पूछा करते हैं-पर बोचचाल से तो भोजपुर की बिलकुल नहीं लगतीं?… मैं मुस्करा देती हूँ। वर्षों से हिंदी पढ़ते-पढ़ाते, लिखते-बोलते उसकी शुद्धता के एहतियात का ऐसा अभ्यास हो गया है कि भोजपुरी का हल्का-सा परिचय भी मेरी आवाज में उभर नहीं पाता। मध्यप्रदेश से व्यवसाय के लिए आए जोशी परिवार ने इस आदिवासी इलाके में पाँच वर्षों से लगातार अपनी मैत्री का सिलसिला मेरे साथ बाँध रखा है। मिसेज जोशी हर रविवार की शाम मेरे लॉन में बैठकर बिताती हैं और कटी-छँटी मखमली दूब पर उछलते मेरे पालतू खरगोशों को मोहित-सी देखती वे प्राय: बातचीत का सिरा एक हल्के विनोदी लहजे में उठाया करती हैं-तुम हर रविवार को अपने घर की पूरी व्यवस्था बदल डालती हो ! मैं जब आती हूँ कुछ-न-कुछ नयापन मुझे मिलता ही है। वासवी, तुम कहीं से भी मुझे भोजपुर की नहीं लगतीं।
मैं हँसकर पूछ लिया करती हूँ-क्या भोजपुरियों के कुछ अलग निशान हुआ करते हैं-सिर पर सींग, पीछे पूँछ या और कुछ…? वे उदाहरण दे-देकर अपनी बात स्पष्ट करना चाहती हैं… बुरा मत मानना वासवी, इलाहाबाद से चलकर जब जमशेदपुर आने लगती हूँ तो बक्सर और उसके आस-पास से ही बड़ी-बड़ी तेल पिलाई लाठियों में लपेटी गठरियाँ लिए देहातियों का झुंड भोजपुर की लठमार गालियों की बौछार के साथ जहाँ-तहाँ दिखाई पड़ने लगता है। सीधे पल्ले के लंबे घूँघट का छोर उठाकर आँखें मटकाती औरतों का रेला और उनके साथ मूँछ पर ताव देते, बीड़ी का कश लेते देहाती लड़कों का अनुशासनहीन जमाव। आरा जिला घर बा, कबन बात के डर बा-वाला उनका उजड्ड पोज देख-देखकर सिर में दर्द हो जाता है’… कान के पास बैठकर बिरहा के राग में बेसुरे फिल्मी गीत गाएँगे, चेन खींचकर जहाँ मन हो, वहाँ उतर जाएँगे ! खैर, उनकी बात तो छोड़ो… पढ़े-लिखे हजारों रूपए कमानेवाले अफसरों के घर का भी वही हाल है। जाकर देखो मिस्टर दुबे के यहाँ… डेढ़ हजार रूपए महीने में कमाते हैं, लेकिन सामने बरामदे में एक रंग उड़ी टूटी खाट बराबर खड़ी मिल जाएगी। भीतर सोफे पर बच्चों के जाँघियों से लेकर बीवी का मैला ब्लाऊज, चीकट गमछे, पसीने की बदबू से भरी बनियानें तक पसरी दिखाई पड़ेंगी। ड्राइंग-रूम के कोने में गेहूँ की बोरी रखी रहेगी। और तो और भर-भर चुटकी सिंदूर तेल सनी माँग में उड़ेलकर मैला आँचल ओढ़े मिसेज दुबे तुमसे बात करते समय भी सूप-चलनी का मोह नहीं छोड़ पाएँगी।… इसीलिए तो कहती हूँ कि तुम्हारा यह सलीका, यह सुरुचिबोध मुझे भ्रम में डालता है-क्या तुम सचमचु भोजपुर की हो?
मैं परिहास में बात टाल देती हूँ… चलिए, यही मान लीजिए कि मैं आपके मध्य प्रदेश की हूँ। अब तो हुआ…? … लेकिन मेरा परिहास मिसेज जोशी की आशंका को संतुष्ट नहीं कर पाता।
कौन कहता है कि मैं भोजपुर की नहीं हूँ…? वहाँ का एक-एक संस्कार मेरे अवचेतन में कस्तूरी बनकर रचा-बसा हुआ है। मिसेज जोशी के प्रशंसात्मक वाक्य एकांत में कनगोजर के हजारों पैरों की तरह मेरे कानों में सुरसुराने लगते हैं… । क्यों भोजपुरियों के लिए इतनी अवमानना उनके भीतर भरी है…? क्या ट्रेन के सफर में देखे गए मुट्ठी भर भोजपुरियों के आधार पर ही उनके जीवन की तमाम गहराइयों में उतरा जा सकता है? भोजपुर की गँवई मिट्टी में अनेक सड़ी-गली मान्यताओं के कीचड़-पानी की दुर्गंध के बावजूद पीड़ा में सिहरते पीत-कमल से जो जीवन पलते रहते हैं, उनके लिए मोह इस सुदूर अरण्य-नगरी में आकर बस जाने पर भी मेरी सारी शिराओं में पिघलता रहता है। लॉन की कटी-छँटी दूब और ऐब्सट्रैक्ट आर्ट की छपाई के परदे मेरे व्यक्तिगत सौंदर्यबोध अथवा शहरी संस्कार की गवाही भले ही दे रहे हों पर माँ के गर्भ में पाए गाँव के संस्कार, बचपन में सुनी गाँव की कहानियाँ और जीवन में केवल एक बार उस छूटी हुई जिंदगी का प्रत्यक्ष साक्षी मन घूम-फिरकर उसी दर्द को बार-बार दुहराता है।
कल मिसेज जोशी पड़ोस के एक समाचार को चुटकुला बनाकर सुना गई- जानती हो वासवी, मिस्टर दुबे के यहाँ सातवीं लड़की पैदा हुई है। जोशीजी हाल-चाल पूछने गए थे तो बेचारे दुबे कुनाई वाले चूल्हे पर उबलते हल्दी-गुड़ में उल्टी कलछुल चला रहे थे। सच वासवी, पढ़-लिखकर भी जितना पुरातनपंथी मैंने मिस्टर दुबे को देखा, उतना और किसी को नहीं ! देखना, इनके बारह लड़कियाँ होंगी… और लड़का एक भी नहीं !… वे अपनी भविष्यवाणी पर एक संतुष्टि भरी हँसी हँसती चली गयीं ! मुझे हँसी नहीं आई। बारह लड़कियाँ की यह बात मेरी उँगली पकड़कर मुझे बारह साल पीछे खींच ले गई !
– माँ, माँ, कहानी सुनाओ!
– कौन-सी कहानी वसुली?
– वही, अपने ब्याह वाली !
– अच्छा सुन, …पाँच साल के हम थे, दस साल के तेरे बाबूजी! बीच में था आम का बगीचा और दोनों और दो गाँव ! तेरे आजा हमारे गाँव के स्कूल में पढ़ाते थे। स्कूल से ही सटा हमारा घर था। छुट्टी की घंटी सुनते ही सारे लड़के अपनी स्लेट-किताबों की झोलियाँ उठाकर घर की ओर भागते और तेरे आजा हमारी दालान पर चढ़कर हाँक लगाते-लछिमी, एक लोटा पानी दे दो बिटिया… !!! हम छोटी-सी भगई के ऊपर गाँती बाँधे लोटे के बोझ से लड़खड़ाती उनके पास चली आतीं।… ऐसे ही साल-पर-साल बीतते गए। एक दिन माँ ने हमें चरगज्जी पीली साड़ी पहनाई और माथे पर आँचल डालकर उसका छोर कमर में मजबूती से खोंसते हुए कहा-जाकर गोड़ लाग लेना। आज से ये तुम्हारे ससुर हुए। हमारी कँपकँपाती हथेलियों से लोटा फिसलकर नीचे जा गिरा, फूल की तश्तरी में रखा बताशा छितरा गया – तेरे आजा हो-होकर के हँस जो पड़े थे !
– फिर क्या हुआ…?
– फिर?… ?… फिर दो साल और कटे, हम बारह साल के हुए। तब एक दिन माँ ने लोटे में हाथ डालकर बिलखना शुरू किया-उधर से लगन आया था। फिर पंडित ने मड़वा का, हल्दी का, मटकोड़ का दिन बिचारा और हम नाऊन की अँकवार में बँधे, बैलगाड़ी के ओहार में सिसकते आम का बगीचा पार करके ससुराल चले आए।
– फिर…?
– फिर कुछ नहीं…
– एक लंबी साँस और थोड़ी देर का मौन…
– मेरी छोटी-छोटी हथेलियों से खिंचता माँ का पाढ़दार आँचल और कहानी का अगला सुर…
– तेरे आजा थे तीन भाई! बहुत बड़ा परिवार! पाँच सेर आटे की रोटी बनती। बनिहारों के लिए कलेवा अलग। दस सेर का भात सींझता। दिन-भर लकड़ी का धुआँ, भात का तसला, आटे की परत और चार पहर रात गए तक सास, चचिया सास और देवर-ननदों के जोड़ में कोल्हू पेरे तेल की मालिश…! वे दिन भी बीते! तब सास सरग जा चुकी थीं। ससुर ने बँटवारे के बाद शहर में छोटा-सा मकान बनवा लिया। फिर तेरे बाबजी की नौकरी लगी और हम गाँव छोड़कर पटना चले आए।
कहानी खतम…! माँ की आँखों में नींद क्यों नहीं है? घनी बँसवारी, बड़े-बड़े आम के पेड़ों से घिरा वह छोटा-सा गाँव, बोरसी की कुरेदी गई चिनगारियों-सा बार-बार मेरे भीतर सुलगा जा रहा है। माँ की कहानियों का झूमता-महकता गाँव अनदेखा होते हुए भी मेरे लिए बहुत करीब था। अब भी कच्चे घर के पिछवाड़े रात-रात-भर महुआ टपकता होगा… टप.. टप.. टप… ! ठाकुरबाड़ी में हरसिंगार के फूलों का एक मोटा गलीचा बिछ जाता होगा। चार-चार भैंसों और एक चितकबरी गइया के मीठे दूध को औटाकर उसकी मलाई निकाली जाती होगी। बीजू आम के बोरे आँगन में उलट दिए जाते होंगे और रस की एक-एक परत मोटे कपड़े पर फैलती, अमावट के खटमिट्ठे स्वाद में बदलती जाती होगी। खेतों की मेड़ पर बैठकर कच्ची उमर की किशोरियाँ अचार के बड़े-बड़े टुकड़ों के साथ चने का साग खोंट-खोंटकर खाती होंगी !… मेरी जीभ पर उतरते हरे चने का रस भरा स्वाद मेरी बाल-कल्पना को अधूरी छोड़कर प्राय: गाँव की धूल भरी पगडंडियों की सोंधी महक में डूबने के लिए तड़प उठता।
होश सँभालने के बाद पटने से गाँव जाने का पहला संयोग मिल पाया मैट्रिक के पर्चे पूरे करने के बाद… ! मँझले आजा के बेटे अपने किसी काम से पटना आए थे और मैं उनके साथ लग गई थी। मैंने बताया था-वहाँ तेरे आजा हैं-दोनों के दो बेटे! एक ये रामशंकर काका और दूसरे बीरेसर काका-जिनकी सात बेटियाँ ही हैं। सब तेरी बहनें लगेंगी !
बस हमें एक पक्के कुएँ के पास उतारकर चल दी। हम पैदल चलने लगे। आगे-आगे रमाशंकर काका और पीछे मैं… ! मेरे मन की धुकधुकाहट बढ़ती जा रही थी, इतनी घबराहट तो इम्तिहान का पहला परचा पाकर भी नहीं हुई थी। रमाशंकर काका गाँव का नक्शासमझाते जा रहे थे- चार टोल हैं-तीनों, पाँचों, आठों-बाभनों और राजपूतों के और चौथा चमरटोला-लेकिन रहते उसमें गोंड़, गोप, कोइरी, कुर्मी सब है। वो देख…, सामने जो बगीचा दिखाई पड़ रहा है, उसी में गाँव का स्कूल है। जोगिन्दर, रबीन्दर, सुरेन्द्र-तीनों उसी में पढ़ते हैं।
मैंने पूछा… और काका, लड़कियाँ?
गाँव की लड़कियाँ पढ़ेंगी…? तू एकदम जाहिल है बसूली। उन्हें तो धान कूटना, गेहूँ पीसना, रोटी पकाना-यही सब सीखना है बस… ! तेरी तरह मैट्रिक पास करके वे करेंगी भी क्या? गाँव में जन्मीं, गाँव में ही ब्याही जाएँगी। और क्या? वैसे भी बीरेसर भाई को लड़कियों का पढ़ना एकदम नहीं सुहाता। फिर दो-चार हों तो एक बात भी है – यहाँ तो सात-सात हैं!’’
मैं सहमकर रह गई। पता नहीं, गाँव में मेरी पढ़ाई को लेकर क्या धारणा बने…?
बैंलों के पीछे-पीछे दूर से चले आ रहे एक बुजुर्ग को दिखाकर काका ने कहा – ये बाबूजी हैं – तेरे मँझले आजा!
मारकीन की लंबी गंजी और धूल के रंग की धोती से झलकती दुबली-पतली काठी। मेरी निबंध की किताब में भारतीय किसान का जो हुलिया दिया गया है, ठीक वही !… मुझे देखकर वे ठमक गए… ई कौन रे रमाशंकर? बड़कू की पोती है क्या…? कैसे-कैसे गाँव आने का मन हुआ बिटिया? मेरे पैर छूने के पहले ही उन्होंने मुझे उठा लिया-ना-ना, लक्ष्मी से पैर नहीं छुआते। जा घर जा । हम शाम तक लौटेंगे।
माँ ने ठीक ही बताया था-घनी बंसवारी… बीच से रास्ता बना हुआ ! दोनों ओर से हरे कच्चे बाँस लचक-लचककर पास बुला रहे थे। पर काका ने कहा-छूना नहीं बसूली, बाँस की कड़ी पत्तियों से हाथ छिल जाएँगे।
– काका, कितने बड़े-बड़े आम… !! मैं बगीचे में आकर उछल पड़ी थी।
– शाम को बिमली, शमली, बिंदा, सुरसती के साथ आना। लेकिन पेड़ पर बंदर रहते हैं। डाल हिलाएगी तो खोंखियाते हुए लपक पड़ेंगे।
मैं समझ गई थी – काका चिढ़ा रहे हैं !
आधी खपरैल, आधी ढलाई की छतवाले एकपुराने-से मकान की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए काका ने कहा-देख बसूली ! यह पक्का हिस्सा बड़का बाबूजी… तेरे आजा ने बनवाया था। इधर गाय-बैलों का बथान, बगल में यह कुआँ-, इतना चौड़ा और गहरा कि हाथी डूब जाए तो थाह नहीं मिले। गाँव भर में पहली बार हमारे ही घर में कुआँ खुदा था। तब हम बहुत छोटे-छोटे थे। तेरी माँ का तुरत ब्याह हुआ था। बड़का बाबूजी के बाद से घर की मरम्मत तक नहीं हुई-सब टूटने-फूटने लगा है।
झड़ते चूने, नोनी लगी दीवारोंवाले दालान को पार कर मैं कच्चे आँगन में उतरी। एक टूटी-सी खाट पर छोटका आजा पड़े हुए थे। खुले बदन में हडि्डयाँ-ही-हडि्डयाँ। साँस की धोंकनी-सी चाल से छाती भाथी बनी फूल रही थी, पिचक रही थी। बिछावन में तेल और पेशाब की मिली-जुली गंध। मेरा मन मिचला उठा। वे बिलकुल चल-फिर नहीं सकते थे। दोनों पैरों पर लकवे का असर था-दो सालों से !
मुझे देखते ही मटमैले आँचल को समेटती रमाशंकर काकी, चिथड़ों में लिपटी जापानी गुड़ियों-सी चार छोटी-छोटी लड़कियाँ और मझली छोटी आजी मेरे नजदीक आकर खड़ी हो गयीं। मझली आजी नाटी, साँवली पर हँसमुख औरत थीं। मेरा हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचती हुई वे काकी से बोलीं-टुकुर-टुकुर मुँह निहारती है भला? यह नहीं होता कि दौड़कर पानी-पीढ़ा लाएँ…?
… तेरी माई कैसी है बचवा…? आहा, वही तो मेरी असली कनिया थी। रात-रात भर गोड़ दबाती, कभी एक दिन भी लूगा खुद धोने नहीं दिया।
मैंने माँ की दी हुई चीजें निकालकर आजी के हवाले कीं – सबके लिए जोड़कर साड़ियाँ, कपड़े और मिठाई !
मझली आजी ने सब कुछ समेटकर एक किनारे धर दिया और मेरे लिए सोनपापड़ी लाने अंदर चली गई। इस बीच गुड़िया-सी, फटे जाँघिए के ऊपर उभरा गोरा गुल-थुल पेट हिलाती बिंदा बड़े निर्भीक भाव से ‘दिदिया-दिदिया’ करती मुझसे सटकर बैठ चुकी थी – जैसे बरसों पुरानी पहचान हो। दूसरी लड़कियाँ ललचाई नजर से कभी मेरी ओढ़नी, कभी मेरी सैंडिल, तो कभी मेरे पीछे रखे मिठाइयाँ के डिब्बे को दूर से ही घूर रही थीं। नन्हीं बिंदा ने ही परिचय दिया – इ चंदा हुई, इ रमुली, इ शमली आ – इ हमरो से छोट बबुनी! अब की बबुआ होई!
छोटकी आजी ने बिंदा सहित सबको मेरे पास से भगाने की बार-बार कोशिश की, पर न बिंदा टली और न मैंने उसे टलने ही दिया। चार-पाँच साल की वह बच्ची मेरी सबसे बड़ी गाइड बनी हुई थी। उसी ने खबर दी – माई बेराम बिया।
मैंने बरामदे में बैठे-बैठे ही घर के चारों ओर की स्थिति का अनुमान लगा लिया था। धुएँ से काली पड़ी सबसे नीची खपरैल की कोठरी में पसीने से तरबतर, गम्हौरियों में लिथड़ा रमाशंकर काकी का रूआँसा मुँह। चारों तरफ मक्खियाँ, धूल, गंदगी और उसमें लोटती-पोटती छोटकी काकी की सात बेटियाँ !… सबसे बड़ी सुरसती तब तेरह वर्ष की होगी, पर सीधे पल्ले की साड़ी पहन, मकड़ी के जाले से उलझे बालों का हाथों से लपेटा गया रूखा जूड़ा बार-बार सँभालती वह अभी से पूरी औरत बन चुकी थी। कभी डेढ़ साल की बबूनी को कमर पर लादकर बहलाती, कभी अँधेरी कोठरी में कराहती माँ के पाँव दबाती, कभी सबके लिए भात परसती दीदी कहकर जब वह पुकारती, मुझे बड़ा अजीब लगता। आज तक मैंने कभी खुद खाना निकालकर नहीं खाया था… मैं उससे तीन साल बड़ी थी – फिर भी।
गाँव की जिंदगी ने सुरसती को असमय ही कितना जिम्मेदार बना दिया था। उसकी भाग-दौड़ और लाचारी देखकर मेरा मन घबड़ा उठता। थोड़े ही समय में बहनापा जोड़कर वह पूरी तरह मेरे साथ घुल-मिल गई। मैंने अनुमान लगा लिया था कि इन लड़कियों की हालत मिट्टी के उन छोटे-छोटे टुकड़ों की-सी है, जो खलिहान से उठाए गए अन्न के दानों के साथ-साथ घर के भीतर आ तो जाते हैं, लेकिन अनाज की सफाई में लगी बेरहम उँगलियाँ उन ढेलों को चुन-चुनकर फेंकने की खीझ में उन्हें मसलने से भी बाज नहीं आतीं। रमाशंकर काका के तीनों बेटे अनाज के पुष्ट दाने थे, खाँटी तेल से चिकनाए, लट्ठे के कड़कड़ाते कुरते-पाजामे में सँवारे गए ! उनके लिए छिपाकर सोन पापड़ी, बताशे और मलाई रखी जाती और छोटकी काकी की बेटियों की ललचती जीभ को आँखें तरेरकर बरज दिया जाता। आश्चर्य तो इस बात का था कि दोनों आजियों का दुरदुराना भूलकर वे मिट्टी सनी कठपुतलियाँ सारा-सारा दिन एक कटोरा माँड़-भात पर काटती घर में डोलती रहतीं। मैंने अपने घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं पाया था। मेरी आजी ने तो अपनी इकलौती बहू की कोख से लछमी जनमने की मनोतियाँ भी रख डाली थीं। तब शायद इसलिए कि माँ के बेटे तो दो थे पर कन्यादान का पुण्य देनेवाली बेटी एक भी नहीं। लेकिन यहाँ बीरसेर काका की इतनी सुंदर-सुकुमार बेटियों को भारी बोझ मानकर बार-बार क्यों अपमानित किया जाता है? मेरा मन हो रहा था, मैं उन सबको समेटकर लिए-दिए पटना चली जाऊँ, फिर सबको ढेर सारी मिठाइयाँ मँगाकर खिलाऊॅं। लाल-नीली घेरेदार फ्राँक में वह बिंदा कितनी प्यारी लगेगी।
उस रात खुले चबूतरे पर दरी डालकर मझली आजी, सुरसती, मैं, बिंदा-हम सब सोए। अचानक छोटी आजी के धड़घड़ाकर उठने की आवाज से मेरी नींद खुल गई। वे रमाशंकर काका को जगाकर जल्दी गाड़ीवान को बुलाने के लिए कह रही थीं। काकी की तकलीफ बढ़ गई थी। बीरेसर काका बाहर रहते थे। उनकी गैरहाजिरी में कुछ हो-हवा न जाय-आजी को इसी का डर ज़्यादा था। वैसे भी घर की सात-सात बेटियों की राक्षसी सेना देखकर वे किटकिटाती रहती थीं-न जाने कैसे वंश चलेगा? एक पर एक सात बेटियाँ ! बड़की कनिया के तीन-तीन बेटे हैं। मझली के एक यही बसुली है और दो बेटे, पर इस करमजली के भाग में तो सतभंभा लिखी थीं।
उन्होंने सुरमती के मुँह पर से आँचल नोंचकर गोहार लगाई – सुरसतिया ! गाड़ी में बइठ जो माई के संगे ! हम पीछे से आवत बानी !
सुरसती के साथ मैं भी उठकर गाड़ी में बैठ गई। काकी का गोरा मुँह दर्द की बार-बार उठती लहर का सबूत देता रह-रहकर काला पड़ जा रहा था। पीछे-पीछे काली माई बरम बाबा को सुमिरती छोटकी आजी चली आ रही थी।
बक्सर अस्पताल के सामने बैलगाड़ी रूकी। काकी को स्ट्रेचर में डालकर अंदर ले गए। बरामदे की बेंच पर बबुनी को गोद में लिए सुरसती, मैं और छोटकी आजी। सुरसती ने सुबकते हुए धीरे-धीरे कहा-माई कह रही थी… इस बार भी जो लड़की हुई तो नमक की पोटली उसके मुँह में कोंचकर वह खुद भी जहर खा लेगी। मैं मन-ही-मन काँप उठी-कहीं फिर लड़की हुई और काकी ने सचमुच ही जहर खा लिया तब…?
माँ ने बताया था कि ब्याह कर आई थी तो सोने की छड़ी-सी चमकदार छोटकी काकी पान-फूल से भी नाजुक थी। हँसती तो मकई के उजले दूध भरे दाने से दाँत चमचमा उठते ! काकी का वह रूप तो अब सपना ही बनकर रह गया था। मैंने भी छोटकी आजी की देखा-देखी काली माई का नाम रटना शुरू कर दिया। माँ बराबर कहा करतीं-हमारे खेत बघार अलग हो गए तो क्या, खून का रिश्ता कभी अलग नहीं होता। वही हमारा कुल-परिवार है। आज हम शादी हैं तो क्या, हमारी जड़ तो उसी गाँव में है – उससे कटकर हम अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं सोच सकते। शादी-ब्याह, जन्म-मरण, सुख-दु:ख कोई भी परोजन गाँववालों के बिना कभी नहीं शोभेगा ! मेरी यह छोटकी काकी मुझे गोदी में लेकर दूध-भात खिलाया करती थी। जब मैं दो साल की थी तब माँ-बाबूजी गाँव छोड़कर शहर आए थे।
काकी आठवीं बार दर्द सह रही थी। इसके पहले हर बार चमरटोले की फुलिया आकर घर में ही सब सँभाल जाया करती थी, पर इस बार चार-पाँच दिनों से छटपटाहट थी और पहले की तरह आसानी से काम निबटता न पाकर फुलिया ने अस्पताल ले जाने की सलाह दी थी। सुरसती की गोदी में बबुनी सो गई थी। और उसे बहलाने के लिए मैंने बातों में लगा लिया था।
– सुरसती, छोटका काका कब आएँगे?
– कहाँ दिदिया, बाबूजी तो साल में बस दो बार आते हैं – फगुआ और दशहरा। आठ-दस दिन जो ठहरते हैं, उसी में हमारी जान साँसत में होती है।
– क्यों…? वे तुम लोगों को प्यार नहीं करते…?
उसने फुसफसाकर कहा – आने के बाद एक-दो दिन तो ठीक रहते हैं। फिर न जाने उन्हें क्या हो जाता है ! लात-मुक्का, जूता, लाठी सब उठा लेते हैं। माई से लेकर बबुनी तक किसी को भी नहीं छोड़ते। कहते हैं – सबको बेच दूँगा !… अच्छा हुआ, जो अभी यहाँ नहीं हैं।
– क्यों…?
– अभी रहते तो आजी उनसे अस्पताल का खरच माँगती और वे अपना सारा गुस्सा इस हालत में भी माई पर ही उतारते।
मैं चुप हो रही… ! छोटे काका को समझने के लिए सुरसती का यह छोटा-सा बयान ही काफी था। छोटकी काकी की कराहती हुई आवाज याद कर मेरा गला रूँध आया। कसाईखाने में जिबह के लिए ले जाए जानेवाले बकरे की आँखों में जैसे उसकी आत्मा की सारी कचोट आकर समा जाती है, स्ट्रेचर पर लदी छोटकी काकी की आँखों में आशंका और करुणा की वही छलछलाहट देखी थी। वे आँखें मुझसे सही नहीं जा रही थीं।
भीतर से दोनों हाथ पोंछती सफेद चोगा झुलाती मोटी डॉक्टरनी निकली। उसके पीछे एक काली-कलूटी नर्स थी। देखने से मद्रास की लग रही थी। हमारा कलेजा काँप उठा। आजी की आँखें बंद थीं और होंठ जल्दी-जल्दी हिलने लगे थे।… डॉक्टरनी ने आजी का कंधा छूकर कहा लड़की हुई है।… और आजी पुक्का फाड़कर रो पड़ीं-राग बाँधकर न जाने क्या-क्या कहती हुई।
मैं सुरसती का हाथ पकड़कर अवाक् खड़ी रह गई थी – किसी अघटनीय की संभावना से भयभीत-कहीं काकी ने सचमुच जहर खा लिया तो…?
सुर में बँधी आजी की रूलाई अस्पताल के सूने बरामदे में गूँज रही थी। पीछे खड़ी नर्स ने केछ देर ठहरकर टूटी-फुटी हिंदी में कहा – ऐ बूढ़ी सोहर नई गाना ! अस्पताल है – समझी…?
छोटी आजी ने झमककर रोना बंद करते हुए उसके मुँह के सामने हाथ नचाकर जोर-जोर से गालियाँ दे डालीं – मर-विपतियालगवनी, सोहर गाव-तानी कि रोव-तानी-रे-!
खैरियत थी कि नर्स के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा और वह आजी को खप्ती समझकर हँसती हुई अंदर चली गई।
बारह साल उस बात को बीत गए। गाँव की जिन मिली-जुली यादों को लेकर मैं दूसरे ही दिन पटना चली आई थी उनमें नीम की पत्तियों के कड़वेपन की मात्रा अधिक थी – मुड़-मुड़कर पीछे देखने की मीठी कोशिश कम ! वह कोशिश महज दो गोल-गोल नीली आँखों के प्यार में सिमटकर रह गई थी। बगीचे के छोर तक पहुँचाने आई हुई बिंदा ने ओढ़नी से लटककर मचलते हुए कहा था-दिदिया, हमहुँ साथे जाइब। और सुरसती बार-बार समझाने पर कि ‘दिदिया फिर आएगी’-वह टुकुर-टुकुर ताकती उसी ‘फिर आएगी’ के झूठे आश्वासन से बँधी पीछे छूट गई थी। भीगी आँखों में अपनी स्वरहीन सहानुभूति उड़ेलकर मैंने सुरसती की ओर से मुँह मोड़ लिया था। मैं दुबारा वहाँ नहीं गई। जा नहीं पाई-यही कहूँ तो बेहतर !
छोटकी काकी अपनी आठवीं लड़की के होने पर जहर नहीं जुटा सकीं तब नवीं के होने पर भी उसे जहर कहाँ से मिलता, लेकिन जहरीली तो उनकी पूरी जिंदगी ही बन चुकी थी। चुपचाप बड़ी-बड़ी हाँडियों में उबलते धान-सी वे सींझती रहीं, उबलती रहीं। उनकी छाती में भी तो सपनों का एक संसार बसा होगा-उनकी बेटियाँ राज करेंगी-सुख से रहेंगी, पर राज-राजियों से उनके रूप को, बेटे-बेटियों में स्वर्ग और नरक का फर्क माननेवाली गाँव की हवा ने कीचड़-मिट्टी में लपेट जो दिया था।
गाँव से आए एक लड़के ने खबर दी थी – बीरेसर काका का जुलूस तो बढ़ता ही जा रहा है। पंद्रह रोज हुए उन्होंने अपनी लड़की बिंदा को फुटबॉल की तरह उछालकर फेंक दिया। उसकी एक टाँग टूट गई है, लँगड़ाकर चलती है किसी तरह ! छोटकी काकी दोनों छोटी लड़कियों को लेकर नइहर चली गई है। बिंदा और उसके ऊपर की सभी लड़कियाँ छोटकी आजी के पास हैं। काकी कह गई हैं – अब कभी नहीं आएँगी। भाई-भौजाई के यहाँ कूट-पीसकर गुजारा कर लेंगे। बीरेसर भाई की देखादेखी बड़कू के तीनों लड़के भी लड़कियों को जहाँ पाते हैं धुन देते हैं। बड़ी खराब दशा है वहाँ की।
माँ की आँखों से दो बूँद आँसू चू पड़े थे। छोटकी के नइहर में भी तो हालत अच्छी नहीं है। भाई सौतेला है और उसके अपने ही पाँच-पाँच बच्चे हैं। कैसे गुजारा होता होगा?
मेरी आँखों में दो नीली आँखें उमड़ आई-हमहुँ साथे जाइब !… काश, कि मैं उसे साथ ला पाई होती। गाँव से लौटकर मैंने ‘माँ’ से पूछा भी था-माँ, क्या बीरेसर काका की दो-तीन लड़कियों को तुम नहीं पाल सकतीं? मुझे भी तो कितना सूना लगता है !
पर माँ ने साफ मना कर दिया था – ना बसुली, बीरेसर को तू नहीं जानती। भारी गुस्सैल… , रावण और कंस से भी बड़ा पापी… ! तिवारी वंश का कलंक बनाकर भगवान ने उसे भेजा है। और ऊपर से तेरी छोटकी काकी की फूटी किस्मत… रावण के घर सती-सीता। शराब-कबाब में कोइलरी की कमाई फूँककर साल-साल लड़कियाँ पैदा करने में पीछे नहीं, और यह भी सहन नहीं होता कि लड़कियों पर कोई दया दिखाए। एक बार तेरे बाबूजी ने समझा-बुझाकर चिट्ठी लिखी भी थी तो लाल स्याही में भद्दी गालियाँ लिखकर उधर से आ गई। फिर किसी ने उसे कुछ नहीं कहा !
इधर दो-चार दिनों से गर्मी काफी बढ़ गई है। रात के दो बजे हैं। मेरी खिड़की से झाँकता, खुले आकाश में चतुर्दशी का चाँद तैरता हुआ कच्ची हल्दी के रंग की चाँदनी छिड़कता धीरे-धीरे नीचे उतर रहा है। मेरे कमरे का आधा भाग चाँदनी में धुला हुआ है, आधे भाग में अँधेरा है। यह अँधेरा हिस्सा मेरा गाँव है, जिससे चलकर कई प्रेत-छायाएँ मुझे जकड़ने के लिए चाँदनी के छोर पर अपनी विकराल बँहि फैलाए खड़ी हैं। मेरे सामने से कई डोलियाँ उठ रही हैं। इनमें सुरसती है, सामली है, रमुली है। सातवीं डोली में बिंदा बैठी है। हल्दी रँगी साड़ी में लिपटी कंचन-काया, अंग-अंग पर दप-दप दीपते सामने की पॉलिस चढ़े गिलट के गहने ! ये प्रेत छायाएँ सातों डोलियाँ उठाए अँधेरे की आड़ लेकर भागती चली जा रही है। यह अँधेरा छोटकी काकी के मटमैले आँसुओं में डूबकर और भी गहरा होता चला जा रहा है। वे बाल फैलाए छाती कूट-कूटकर बिलख रही हैं-मेरी बेटियों को मत बेचो ! बीरेसर काका की शराब में डूबी चेतना, बंस के अभाव की पीड़ा और दहेज की सामर्थ्यहीनता के कड़वे आवेग में बनैले सूअर की तरह चीत्कार करती अपने दोनों पंजों को फाँसी के फन्दे बना-बनाकर अपने ही गले तक बार-बार ले जा रही है। दाँत पीसती हुई एक आत्महन्ता मुद्रा जो एक-दो नहीं, सात-सात बेटियों को जिंदा गला घोंटकर मार देने की विवशता के आखिरी किनारे तक पहुँची न मरती है, न जीवित रह पाती है।… डोलियाँ सामने से गुजरती चली जा रही हैं। बीरेसर काका ने पैसे देकर दामाद नहीं खरीदे, लेकिन बेमोल अपनी बेटियाँ तो बेच ही दीं। पीली धोती का छोर कुरते की जेब में खोंसे यह दूल्हों की जमात आगे बढ़ी ! कोयले की खदान से छाँटकर निकाले गए चमकते काले टुकड़े, भोजपुर के पुरुष-रत्नों में से चुन-चुनकर जुटाए गए ठीकरे जो लाठी के जोर पर बीरेसर काका की गाय-सी रँभाती बेटियों को जीवन भर जिबह करेंगे !… और वह रहा बिंदा का दूल्हा। एक आँख पत्थर की… ! बिना पलक झपकाए शीतला के शाप का बदला अपनी क्रूर हँसी में चुकाता बिन की डोली के साथ-साथ चलता। सोने की पुतली को अपने चंगुल में जकड़कर खा जाने के लिए उद्धत काला दैत्य… ! यह आखिरी डोली भी मेरे सामने से दूर चली गई। बाँस-वन को पार करती, कहारों के पैरों तले रौंदी जा रही आम की सूखी पत्तियों की चरमराहट और बिंदा की सिसकियाँ धीमी पड़ती जा रही हैं।
लकड़ी के धुएँ से काले पड़े बर्तनों को रगड़ती बिंदा की गोरी गुलथुल बाँहें बेंत-सी पतली, बेदम होकर झूल पड़ी हैं धुएँ और कालिख में सनी उसकी नीली आँखों से खून टपक रहा है। लात-मुक्कों की चोट खा-खाकर भी उस दैत्य की भूख मिटाने के लिए उसे अँधेरी कोठरी में जलते दिए की ढीठ रोशनी रोज बर्दाश्त करनी पड़ती है। दिन-भर ढेंकी पर धान कूटकर चावल बनाने में अपनी नीली आँखों के चकनाचूर हुए सपनों की भूसी बिखराती वह रात-भर कुटती-पिसती टुकड़े-टुकड़े बिखर जाने के लिए बाध्य है। क्योंकि वह भोजपुर के अँधेरे गाँव की सातवीं बेटी है। गाँव में आनेवाले हर पहुना से उसकी चिरौरी चलती है-एक बार, बस एक बार, माई से मिला दो… ! लेकिन सारे पहुने बहरे हैं और गूँगे भी। बीरेसर के भीतर का बाप कब का मर चुका है। छोटकी काकी पथरायी हुई अहिल्या है। उसकी कोख शायद उस अगले जन्म की प्रतीक्षा में जड़ है, जब उनके मातृत्व को सार्थक बनाता कोई राम उनके आँचल की धूल झाड़ेगा।…
गिलट को सोना बताकर समधी के हवाले करने के बाद बीरेसर काका ने मुँह नहीं दिखाया। बिंदा को सब सहना है, क्योंकि उसके बाप ने उसके सास-ससुर को धोखा दिया है। फिर… एक रात… , बुखार की गहरी बेहोशी में भरपूर रौंदी जा चुकने के बाद बिंदा उन्मादिनी-सी उठकर जलती लालटेन का सारा किरासन अपने ऊपर छिड़क लेती है – भक… ! उसकी तार-तार साड़ी और मैले साये का छोर पकड़ती आग की लपटें उसे घेर रही हैं। सारा गाँव सो रहा है… बिंदा जल रही है। उसकी आर्त्त पुकार एक हिचकी बनकर मेरे कंठ में उभरती है।–दिदिया-! हमहुँ साथे जाइब… !… और मैं पसीने से तर-बतर बदहवास जग पड़ती हूँ। अँधेरा पूरे कमरे में फैल गया है। बिजली चली गई है और बाहर पत्ता तक नहीं हिल रहा।
सहसा मिसेज दुबे के क्वार्टर से रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। कई टार्च की रोशनियाँ एक साथ क्वार्टर के करीब आती दिखाई पड़ रही हैं। मैं दरवाजा खोलकर उधर बढ़ती हूँ। मिसेज जोशी अपने क्वार्टर से निकलकर मिसेज दुबे के क्वार्टर से होती हुई मेरे करीब आ गई हैं-जानती हो वासवी, दुबे की सातवीं लड़की मर गई। बेचारी… ! उसकी माँ एकदम चुप है… । रोना तो दूर रहा, कुछ बोलती तक नहीं। बुढ़िया सास लगातार रोए जा रही है।
मैं सुन्न-सी मिसेज जोशी को देखती हूँ… सातवीं बेटी की माँ का रोना आप नहीं देख पाएँगी मिसेज जोशी ! वह तो मैं देख रही हूँ। पत्थर हो गई होगी मिसेज दुबे। अच्छा ही हुआ मर गई-! जन्म के दो दिन बाद मर जाना कहीं बेहतर है, सतरह साल तक रोज-रोज मरने से !
मिसेज जोशी बौखलाई-सी मुझे देख रही हैं। शायद मेरी आँखों में झाँकती बिंदा की प्रेत-छाया को वे सह नहीं पा रही हैं। अब मैं उन्हें कैसे विश्वास दिलाऊँ कि मैं कच्ची उमर में जल मरनेवाली बिंदा की स्मृतियाँ का शव कंधे पर ढोती भोजपुर के एक अँधेरे गाँव से सीधी उठकर के चली जा रही हूँ और मेरा पूरा संस्कार उस आदिम अँधेरे के विरूद्ध लड़ने के लिए मुष्टिबद्ध हो रहा है।
Download PDF (सातवीं बेटी )
सातवीं बेटी – Satavi Beti