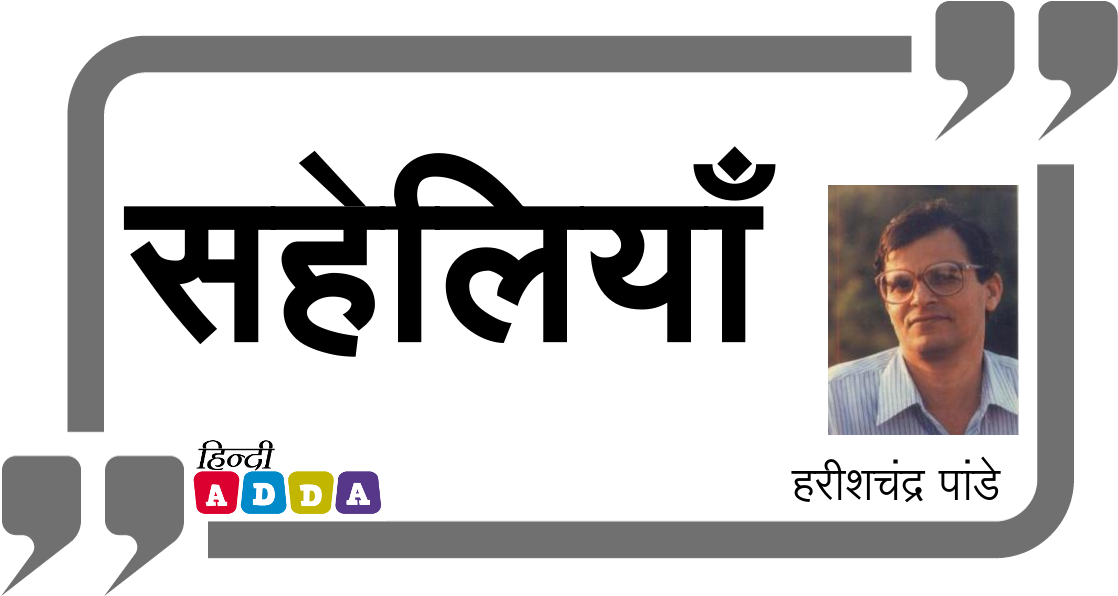सहेलियाँ | हरीशचंद्र पांडे
सहेलियाँ | हरीशचंद्र पांडे
आज बेटी सुबह से ही व्यस्त है
सहेलियाँ घर पर आएँगी
खाना होगा
गपशप होगी खूब
चीजें तरतीब पा रही हैं
ओने-कोने साफ हो रहे हैं
खुद की भी सँवार हो रही है
पिता तक पहुँचती आवाज में माँ से कह रही है
यही पहन कर न आ जाना बाहर
नोयडा से रुचि आई है
बैंग्लोर से आयशा
विश्वविद्यालय के कल्पना चावला हॉस्टल से आएगी तरु
सरोजनी से दिव्या
शिल्पी बीमार है, वह छटपटाएगी बिस्तर पर…
ग्यारह बजे आ जाना था उन्हें
बारह बज गए हैं
बेटी टहल रही है मोबाइल पर कान लगाए
वे शायद आ रही हैं
मोड़ की उस ओर जहाँ आँखें नहीं पहुँच रहीं
आवाजों का एक बवंडर आ रहा है
हाँ, वे आ गई हैं
कॉल बेल दबाने से पूरा नहीं पड़ रहा उनका
गेट का दरवाजा पीट रही हैं थप-थप-थप्प
जैसे यह बहरों का मुहल्ला है
अधैर्य का एक पुलिंदा मेरे गेट पर खड़ा है
वे गेट के भीतर क्या आ गई हैं
कहीं एक बाँध टूट गया है जैसे
कहीं आवाजों के विषम शिखरों का एक आर्केस्ट्रा बज रहा है
कहीं चिपको नेत्रियों द्वारा एक घना जंगल बचाया जा रहा है कटने से
वे अब कमरे के भीतर आ गई हैं
धम्म-धम्म-धम्म सोफों पर ऐसे गिर रही हैं
जैसे पहाड़ खोद कर आई हैं
थोड़ा ठंडा-वंडा
थोड़ा चाय-बिस्कुट
थोड़े गिले-शिकवे…
और अब सबकी सब अतीत में चली गई हैं
एक ग्रुप फोटो के साथ…
वे कॉलेज के अंतिम वर्ष के विदाई समारोह में खड़ी हैं अभी
पहली-पहल बार साड़ी पहने हुए
सब एक बार फिर लजाती निकल रही हैं अपने-अपने घरों से
साड़ी कुछ माँ ठीक कर रही है, कुछ बहन, कुछ भाभी
ऊपर कंधे पर ठीक हो रही है, कुछ पैरों के पास झटक-झटक कर
एक स्कूटर पर पीछे बैठी असहज-असहज है
दूसरी स्कूल वैन में बैठने के पहले
कई बार गिरते-गिरते बची है
तीसरी खुद को कम
देखने वालों को अधिक देख रही है
मरी-मरी जा रही है
भरी-भरी जा रही है
कॉलेज के प्रवेश द्वार पर असहजता का एक कुंभ लगा है
वे अपने ही भीतर डुबकी लगा रही हैं
उनके भीतर ही भँवर हैं भीतर ही चप्पू
भीतर ही मंझधार हैं भीतर ही किनारा
वे उचक-उचक कर चहक रही हैं
चहक-चहक कर मंद हो रही हैं
अब उनकी बातों की जद में सहपाठिनें हैं
वे चौथे लाइन में तीसरे नंबर पर खड़ी बड़ी चुड़ैल थी जो
और वे दूसरे लाइन वाली कितने बहाने बनाती थी क्लास में
भई मिस नागर का तो कोई जवाब नहीं
अभी यह कमरा कमरा नहीं
एक ही पेड़ पर कुहुक रही कोकिलाओं का जंगल पल है
धीरे-धीरे कमरे का सामुदायिक राग कम हो रहा है
अब एक बार में एक स्वर मुखर है
अपने-अपने अनुभव हैं अपनी-अपनी बातें
फिर जैसे अचानक एक रेलगाड़ी लंबी सुरंग में प्रवेश कर गई है
चुप्प
और फिर जैसे अचानक सभी दिशाओं में सूर्य उग आए हैं
पखेरू चहकने लगे हैं
किसी ने मोती की लड़ियाँ तोड़ कर बिखेर दी हैं
खिल-खिल का ऐसा ज्वार कि जैसे
संसार के सारे कलुष धुल गए हों
भीतर हम भी देश-काल से परे हो गए हैं
ये सब सँजो लेंगी इन पलों को
हम समो लेंगे
समय बीत गया है पर इनकी बातें नहीं
अब ये सब टा-टा, बाई-बाई कर रही हैं
इस छोर पर एक माँ कई बेटियों को विदा कर रही है
उस छोर पर कई माँएँ आँखें बिछाए खड़ी हैं
यहीं कहीं एक लड़का कैमिस्ट की दुकान पर खड़ा
एसिड की बोतल खरीद रहा है…