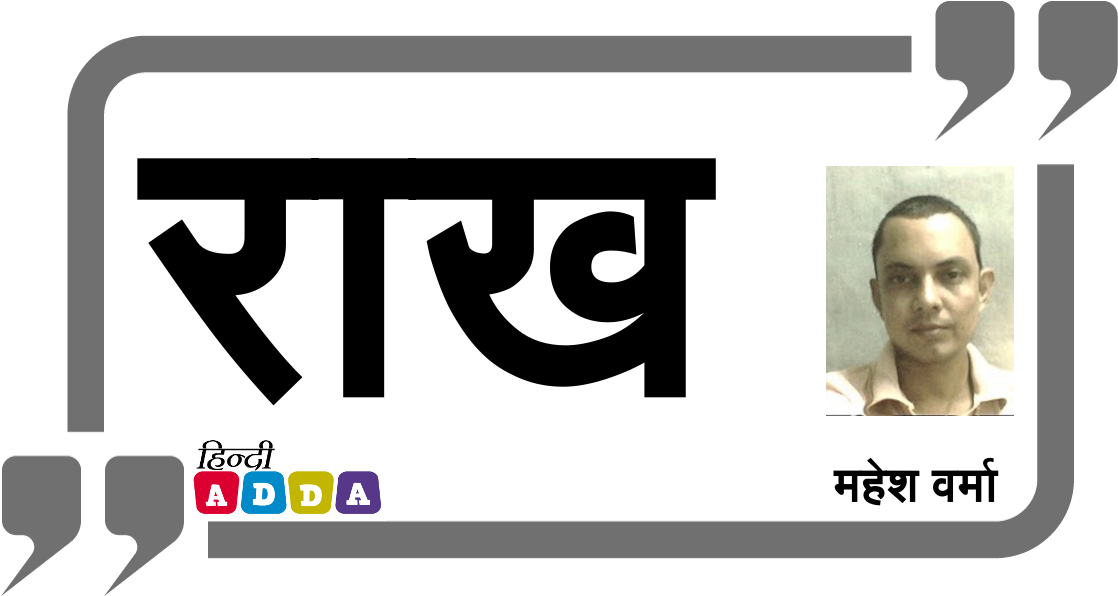राख | महेश वर्मा
राख | महेश वर्मा
ढेर सारा कुछ भी तो नहीं जला है इन दिनों
न देह न जंगल, फिर कैसी यह राख?
हर ओर?
जागते में भर जाती बोलने के शब्दों में,
किताब खोलो तो भीतर पन्ने नहीं राख!
एक फुसफुसाहट में गर्क हो जाता चुंबन
और ज़ुबान पर लग जाती राख!
राख के पर्दे,
राख का बिस्तर,
हाथ मिलाने से डर लगता
दोस्त न दे थोड़ी सी राख।
बहुत पुरानी घटना हो गई कुएँ ताला का पानी देखना,
अब तो उसक ढके हुए है राख।
राख की चादर ओढ़कर घुटने मोड़े
मैं सो जाता हूँ घर लौटकर
सपनों पर निःशब्द गिरती रहती है – राख।