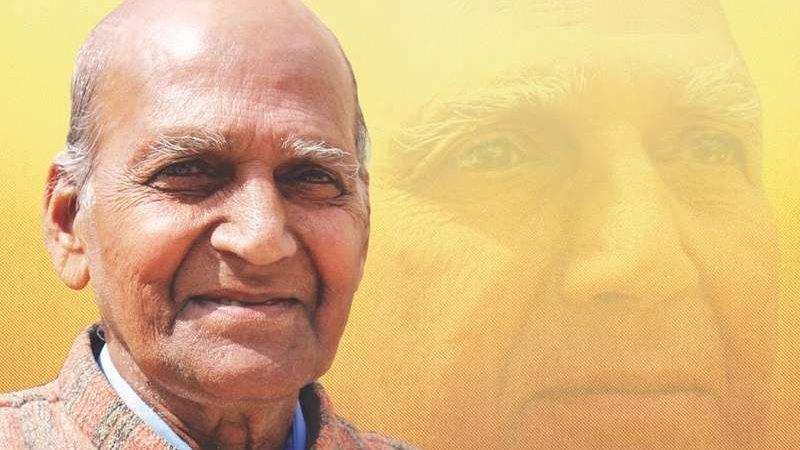अपने घोर फिटमारेपन के दिनों में मेरी रमेश भाई से मित्रता हुई थी। मेरा हाल यह था कि बतौर साहिर लुधियानवी, ‘तालीम है अधूरी और मिलती नहीं मजूरी।’ हायर सेकंडरी के बाद बीएससी फर्स्ट ईयर में कीर्तिमानी नंबरों से फेल होने के बाद एक मामा जी की दया से उनके घर रहकर मैंने ढाई साल का एक डिप्लोमा कर लिया था और मता-ए-कूच-ए-बाजार बनने को तैयार हो गया था। रोजगार दफ्तर में नाम लिखा दिया था और नियम से सार्वजनिक वाचनालय जाकर रिक्तियों के कॉलम चाटता था। दिक्कत यह थी कि पैसों के लिए नौकरी की जरूरत थी और नौकरी के लिए पैसों की। रोज की रोज घरवालों से पोस्टल ऑर्डर और रजिस्ट्री के पैसे माँगने में शर्म आती थी। इसलिए मैं एक अबूझ-अथक-अरूप और अनंत प्रतीक्षा में लीन था कि किसी दिन कुछ ऐसा होगा कि मुझे किसी चमत्कार से अपनी डाक में एक कॉल लेटर मिल जाएगा और परिवार के सारे दलिद्दर कट जाएँगे।
पर बाईगॉड! जैसा खुश-खिलंदड़ा और खिलखिल मैं उन दिनों में रहा, बाद में कभी नहीं। है न अजीब! हिंदी के एक कोई तो भी महान कवि कह गए कि भूखे भजन न होय गुपाला। गुपाला से नहीं हो पाता होगा पर मैं क्या कहता हूँ कि बड़े गुलाम अली खाँ से गुलाम अली गजलवाले तक किसी से भी पूछो – क्या वो भोजन-वोजन करके मंच पर गाने के लिए बैठते हैं? भरे पेट सिर्फ नींद या बदमाशी होती है, भजन तो भूखे पेट ही होता है।
क्या गाता था मैं! कितने शेर याद थे मुझे! पुराने गानों का कैसा चस्का था! कई बार तो गाते-गाते रोने लगता! चल रहा था! कभी राज पेंटर्स के यहाँ दिन भर काम करता, बोर्ड बनाता, जमीन पोतता, कास्टिक सोडे से पुराने पत्तर साफ करता, बॉर्डर बनाता, शेडिंग करता… और गाता रहता… शाम को डेढ़ रुपये मिलते। कभी इकबाल भाई साइकिलवाले के यहाँ छोकरा नहीं आता तो वह मुझे ले जाता। दिन भर पंचर जोड़ता, हवा भरता, पहियों के बाल निकालता, टयूब पकाता… और गाता रहता। शाम को चाय पानी के अलावा दो रुपये मिलते। कभी रेलवे स्टेशन के बुक स्टाल पर दो घंटे के लिए बद्र भाई का रिलीवर हो जाता। जितनी देर में वह खाना खाकर आते, मैं सारी पत्रिकाओं के नए अंक चख लेता। बगल का टी स्टॉल वाला चाय भी पिला देता।
कुल मिलाकर मस्ती थी भाई!
और रमेश भाई साढ़े इक्कीस नौकरियाँ छोड़कर लड़कपन के इस छोटे-से शहर में एम.ए. करने आए थे। जैसे ‘मैं हूँ ना’ में शाहरुख खान। बंबई में शायद किसी बहस के दौरान किसी ने उनसे कह दिया कि मैं बिना पढ़े-लिखों से बात नहीं करता। या किसी दिन कोई डिग्रीयाफ्ता अपनी टाई झुलाता उनके परिश्रम पर लात रखकर उनके सिर पर चढ़ बैठा। ऐसा ही कुछ। आप सोच लो। अब रमेश भाई ठहरे मसिजीवी। फ्रीलांसर लेखक। सुबह कॉलेज अटेंड करते, बाकी दिन भर आम की किस्मों से लेकर हाइड्रोसील तक वायुमंडल के नीचे संभव हर किसी विषय पर लेख लिखते। पढ़ते भी। बीच-बीच में कहानी-उपन्यास भी लिखते। शाम को ‘एलीट’ मैं बैठकर चाय पीते। लॉन में। यह हमारे शहर का एकमात्र रेस्तराँ था जिसमें वर्दीवाले बैरे थे और जहाँ खा-पीकर पेमेंट करने काउंटर पर नहीं जाना पड़ता था।
मैं सार्त्र और काम्यू और कॉलिन विल्सन प्रभृति विद्वज्जनों के नामों और कामों से किंचित परिचित था, तो जैसे खग को खग मिल गया। रमेश भाई ने मुझे एक संभावना के रूप में गले से लगा लिया, और मैं भी लग लिया कि सोहबत का कुछ तो लाभ ‘एलीट’ की ठाठदार चाय और रमेश भाई की लायब्रेरी के अलावा भी, क्या पता, मिल ही जाए।
यह हुई प्रस्तावना, प्राक्कथन, पूर्वरंग या पात्र परिचय, आप जो भी समझ लो। अब कहानी सुनो।
एक दिन दुबले-पतले रमेश भाई अपनी दुबली-पतली लेडीज साइकिल दौड़ाते हुए मेरे कने आए और बोले – चलो नाटक करना है।
मैंने पूछा – कहाँ?
बोले – कॉलेज में?
मैंने पूछा – ठोकना है?
बोले – जोर से।
मैंने पूछा – कब?
बोले – दिसंबर में।
अब मैं समझा कि सचमुच के नाटक की बात हो रही है। कोई मार पिटाई का तात्कालिक मामला नहीं है। मैंने पूछा – कौन सा नाटक?
बोले – वो मैंने सोच लिया है। सेम्युअल बेकेट का ‘वेटिंग फॉर गोडो’।
मैंने पूछा – स्क्रिप्ट?
बोले – वही तो! बनानी है।
मैंने पूछा – अंग्रेजी में?
बोले – हिंदी में।
मैंने पूछा – यहाँ की जनता समझ जाएगी?
बोले – हम किस मर्ज की दवा हैं?
मैंने कुछ सोचकर कहा – रमेश भाई, मैंने नाटक बहुत ध्यान से पढ़ा नहीं है।
बोले – करते-करते पढ़ लेना।
मैंने मुँह बनाकर पूछा – क-र-ते-क-र-ते!!
वह खिलखिल हँसे। जैसे मोगरे के ढेर सारे फूल किसी ने एकदम अपनी अँजुरी से उछाल दिए हो। अब कुछ नहीं पूछा जा सकता था।
घर जाकर सूचित किया कि आज रात और शायद तीन-चार रात रमेश भाई के घर ही रुकूँगा। रास्ते से चाय के लिए दूध लिया, सिगरेटें लीं और रमेश भाई के कमरे पर पहुँच गए।
अब हम थे और रात थी और सेम्युअल बेकेट और वेटिंग फॉर गोडो!
आधा घंटे तक रमेश भाई मुझे द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद के यूरोप के जनजीवन और एब्सर्ड के बारे में समझाते रहे। चित्रकारों और फिल्मों के उदाहरण दे-देकर।
आधा घंटे बाद उबासी लेते हुए मैंने पूछा – एनएसडी में हो चुका है न?
बोले – अल्काजी ने करवाया था।
मैंने पूछा – हिंदी में या अंगरेजी में?
बोले – हिंदी में।
मैंने पूछा – अनुवाद किसने किया था?
बोले – मनोहरसिंह और बज्जूभाई।
मैंने कहा – वहीं से क्यों नहीं स्क्रिप्ट मार लाते?
बोले – क्योंकि उसमें एस्ट्रागॉन एस्ट्रागॉन और ब्लादीमीर ब्लादीमीर ही है।
मैंने कहा – तो अच्छा है न! एक नाम से अमरीकन जैसा लगता है दूसरा रूसी। उदयवीर और मधु जोशी को बना देंगे। तुम बन जाना लकी और मैं बन जाऊँगा गोदो, जो कभी नहीं आता हा हा।
रमेश भाई हँसे, फिर बोले – नहीं। हम बनाएँगे उन्हें आयुष्मान और बलिहारी। एक जीवन का प्रतीक, एक मृत्यु का।
मैंने कहा – और विश्वयुद्ध? उसका क्या करेंगे? और कन्या? कन्या के बगैर नाटक जमेगा? रमेश भाई एक आइडिया है। क्यों न हम इन्हें ‘ज्ञानोदय’ और ‘वसुधा’ बना दें!
रमेश भाई बोले – और गोदो?
मैंने तुरंत कहा – गोदो पाठक!
रमेश भाई बोले – और लकी?
मैंने कहा – रमेश भाई, डेढ़ बज रहे हैं। अब सो जाते हैं। बेकेट को भी आराम करने दो!
रमेश भाई बोले – चाय बनाते हैं। खटिया से कूदे और स्टोव में पंप मारने लगे।
मैं समझ गया, रमेश भाई आज की रात न मुझे छोड़ेंगे, न सेम्युअल बेकेट को।
चाय पीकर थोड़ी चेतना आई तो मैं लड़ पड़ा। कोई मतलब नहीं है द्वितीय विश्वयुद्ध का। वह हमने भोगा ही नहीं। इससे तो आप कोई सरल और समझ में आने वाली चीज चुनते। जैसे बाढ़ या जैसे भूकंप या जैसे अकाल।
रमेश भाई बोले – लेकिन व्यवस्था? उसका पशुबल? प्रकृति को कोसेंगे क्या?
मैं बोला – तो ठीक है, उनकी बस्ती पर बुलडोजर चलवा देते हैं।
रमेश भाई कुछ सोचकर बोले – और बेकेट?
मैंने कहा – वह कौन सा इस गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा था? या पूछने आएगा? अब साहब, कुछ न कुछ उलट-पलट तो होगा जब दो महान लेखक भारत में उसे अपने हाथ लगाएँगे – एक उदीयमान और एक अस्तप्राय…
खुद को अस्तप्राय कहने पर रमेश भाई खिलखिलाकर हँसे और मुझे तकिया फेंककर मारा।
हम दोनों की आँखें सूज रही थीं। हम दोनों के चेहरे दमक रहे थे। चार रातों में हमने मुहावरे की भाषा में गोडो की ऐसी-तैसी करके रख दी थी। हमें अनुभव था। इससे पहले हम मॉम और मोपॉसाँ और बाल्ज़ाक, ओहेनेहरी और विक्टर ह्यूगो की कहानियों के रेडियो नाट्य रूपांतर कर चुके थे जो आकाशवाणी दिल्ली से बजते थे और जिन्हें श्रोता खूब पसंद कर रहे थे। हम सिर्फ यह नहीं करते थे कि ‘हड्डी चूस रहा है’ को ‘केला खा रहा है’ कह देते हैं, बल्कि उस्तादों की रचनाओं का पूरा हाल-हुलिया बदल देते थे। जरूरत पड़ने पर कुछ नए पात्रों की उद्भावना भी कर देते थे। परिवेश को जीवंत बनाने के लिए किसी पात्र को हलका बना देते थे, किसी को लँगड़ा। किसी को बात-बात पर लोकोक्तियाँ मारने वाला तो किसी को कोई खास तकिया कलाम वाला। इससे बड़ा क्रिएटिव सुख मिलता था। उस्ताद हमारा क्या बिगाड़ सकते थे? नाटक श्रोताओं को पसंद आ रहे थे। रमेश भाई की पढ़ाई का खर्चा निकलने में मदद मिल रही थी।
इस बार हमने बड़ा हाथ मारा था। जैसे दो जेबकतरों ने मजाक-मजाक में किसी रात कोई बैंक लूट लिया तो। लेकिन इस प्रक्रिया में एब्सर्ड की थोड़ी धूल-मिट्टी भी हमारी आँख-नाक में घुस गई थी। और किसी ने देखा हो, न देखा हो, बेकेट हमें देख रहे थे।
एक रात बेकेट मेरे सपने में आए। आँखें फाड़े, एकटक देखते रहे। न खुश न दुखी। न कुछ बोले बतियाए। बस, देखते रहे आँखें फाड़े। डर के मारे मेरी आँख खुल गई। समझ में नहीं आया क्या चाहते हैं! हमसे कोई गलती हो गई क्या?
अगले दिन चार सहपाठी बैठाकर कार्बन लगाकर रमेश भाई ने नाटक की आठ कॉपियाँ बनवाईं और फिर पूरी एम.ए. प्रीवियस (हिंदी) कक्षा के समक्ष नाटक का पाठ हुआ। कुछ फायनल वाले भी आ गए। कुछ अन्य भी जो खुद को एनएसडी और पूना फिल्म इन्स्टीट्यूट का संभावित और गौरवशाली प्रत्याशी मानते थे। कुछ अन्य भी-सिर्फ तमाशा देखने। कुछ लड़कियाँ – सिर्फ खी खी खी करने।
कॉलेज का हॉल शानदार था। बल्कि काफी शानदार था। आम तौर पर कॉलेजों में ऐसे हॉल नहीं होते। स्टेज पर दो कारें या दो ताँगे या दस घोड़े एक साथ आ सकते थे। तीन मंजिले मकान का सैट बन सकता था। विंग्स में पचास पीस का ऑरकेस्ट्रा बैठ सकता था। प्रोजेक्ट की सुविधा थी। पहली पंक्ति और स्टेज के बीच इतनी जगह थी कि वहाँ बैडमिंटन खेला जा सकता था। खेला भी जाता था। खास कर पाराशर सर द्वारा- अपनी शोध छात्राओं के साथ। कॉलेज में हर साल एक अंग्रेजी और एक हिंदी का पूरावक्ती नाटक खेला जाता था। बाहर के लोग भी करते थे आकर टिकट लगाकर। मणि मधुकर का ‘रसगंधर्व’ और हमीदुल्ला का ‘उलझी आकृतियाँ’ कुछ रोज पहले ही हो चुका था।
कहिए इसे हमारी गैरईमानदार प्रतिभा का ही कमाल कि लोगों को नाटक के पाठ में खूब मजा आया। वे खूब हँसे। बोले – श्योर हिट है। उदास और चिंतित होकर मैंने रमेश भाई ने कहा – लगता है हम बेकेट को ठीक से समझ नहीं पाए। कुछ पैथोस डालना पड़ेगा। रमेश भाई बोले – ग्रेट मेन थिंक अलाइक। बेकेट पर और गोडो पर उसके समकालीनों ने क्या कहा है, इसे जरा देखना पड़ेगा।
फिर कलाकारों का चयन, रिहर्सल की जगह और प्रॉप वगैरह का निर्णय हुआ और दोस्तो! असली कहानी इसके बाद ही शुरू होती है।
एस्ट्रागॉन कौन? तो तुम। यानी मैं! ब्लादीमीर कौन? तो मीरा गुप्ता। मंजू गुप्ता की छोटी बहन सेकंड ईयर में पढ़ती है। पोजो? मधु जोशी। और लकी? रमेश भाई खुद।
मैं हैरान-परेशान। मैं? मैं क्यों? मैं कैसे? मैं तो कॉलेज का स्टूडेंट भी नहीं हूँ। तुम! तुम ही। तुम ही एस्ट्रागॉन को समझते हो। उसके साथ न्याय कर सकते हो। उसकी ट्रेजेडी को कॉमेडी की मार्फत पोट्रे कर सकते हो। जो कि काफी कठिन काम है। लेकिन मैं जानता हूँ तुम कर लोगे। लेकिन मेरा आप लोगों के नाटक में काम करना! लोग ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे? चिंता मत करो। वो सब हम सँभाल लेंगे।
तब उस रात पहली बार मैंने सारी स्क्रिप्ट को ध्यान से पढ़ा। कौन है एस्ट्रागॉन? कहाँ से आया है? कैसा दिखाई देता है? मूढ़ या मजबूर? ऊटपटाँग बातें क्यों करता है? खुद को खुश रखने की कोशिश करता रहता है या दूसरों को हँसाते रहने की? क्या इतनी हताशा है उसके जीवन में कि उसे लगता है अब जीवन को पटरी पर लाने का कोई प्रयास नहीं किया जा सकता? सब बेकार है! हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि कोई उम्मीद नहीं बची है – बेशक, सिवा गोदो के इंतजार के? कितनी तड़प, कितने आँसू नहीं हैं? उसने जिंदगी के बारे में सोचना ही छोड़ दिया है? घटनाएँ अपने आप हो रही हैं? बगैर उससे कुछ पूछे या बताए? और घटनाएँ भी कहाँ हो रही हैं? जो हो रहा है निरंतर वह तो एक ऊबड़खाबड़ घटनाविहीनता है। सब कुछ एकदम ऊलजलूल और निरर्थक हो चुका है। पागलपन और बेखुदी की कगार पर झूलता यह मसखरा – कभी सचमुच की जिंदगी पा जाए तो क्या करेगा?
…पिछले छह महीने से मेरी डाक में एक भी कागज नहीं आया है। पिछले छह महीने से मैंने कहीं एप्लाई भी नहीं किया है। अखबार देखना भी बंद कर दिया है। रोजगार दफ्तर भी नहीं गया हूँ। हो सकता है मिथिला बाबू मुझे ढूँढ़ रहे हों। मैं कर क्या रहा हूँ? मुझे अपने डूबते परिवार पर दया क्यों नहीं आती? माँ किस-किस तरह दोनों वक्त बच्चों के लिए रोटी पकाती है। ग्यारह साल की छोटी बहन हर गुरुवार को उपवास कर रही है – कि भइया की नौकरी लग जाए! मैं साला मिलिट्री रिक्रूटमेंट बोर्ड जाकर पता क्यों नहीं करता? और वैसे एक बार एपीडब्ल्यूआई की गेंग में लग जाने में भी क्या हर्ज हैं? मेरे साथ पढ़े लड़के कहाँ गए? शायद सब नौकरी पा गए। उनसे मेरा कोई संपर्क नहीं। कॉलेज जाकर देखूँ? शायद वहाँ कोई कॉल लेटर आया पड़ा हो! पोस्ट ऑफिस जाऊँ? क्या करूँ? क्या करूँ? क्या करूँ? मर जाऊँ क्या?
उस महल की आड़ से निकला वो पीला माहताब!
जैसे मुल्ला का अमामा, जैसे बनिये की किताब!
जैसे मुफलिस की जवानी, जैसे बेवा का शबाब!
ऐ गमे दिल क्या करूँ, ऐ वहशते दिल क्या करूँ!
तुम इससे बड़ी क्रूरता मेरे साथ क्या कर सकते थे रमेश भाई, कि मुझे एस्ट्रागॉन बना डालो!
मीरा गुप्ता मधु जोशी की प्रेमिका मंजू गुप्ता की छोटी बहन थी। एकदम छोटी बहन टाइप। जैसे ‘हम लोग’ की छुटकी। पोलिस्टर के सलवार सूट और काला कार्डिगन हमेशा। लेकिन छुटकी की तरह चंचल और वाचाल नहीं, हमेशा चुप और सहमी हुई। उसकी झिझक खुल ही नहीं रही थी। उसे अपनी सारी लाइनें अच्छे से याद होतीं… लेकिन उसकी टाइमिंग हमेशा गड़बड़ा जाती। वह यूनिट के किसी सदस्य के साथ खुलकर बात नहीं कर पाती… जबकि महेंद्र तो उसका पड़ोसी भी था। उसके चेहरे पर हमेशा चुपचाप दुख सहने का भाव रहता, जो स्क्रिप्ट को सूट करता था… लेकिन अभिनय के समय। उससे आगे-पीछे-बीच में उससे अपेक्षा की जाती थी कि वह परिवार के एक सदस्य की तरह हँसेगी बोलेगी। कम से कम अपने कैरेक्टर के बारे में ही सवाल करेगी… बहस करेगी। क्योंकि वह ऐसा नहीं करेगी तो इंप्रोवाइजेशन कैसे होंगे? लेकिन वह कोई उत्साह नहीं दिखाती। उसे अभिनय का कोई अनुभव नहीं था। तो हम कौन से सोहराब मोदी थे। मधु की जो डॉयलॉग डिलीवरी तक गड़बड़ थी। रमेश भाई की सबसे ज्यादा डाँट उसी ने खाई।
रिहर्सल के बीच में मीरा की एक-दो क्लासमेट्स कभी-कभी आतीं। दूर खड़ी देखती रहतीं। मीरा जाती। वहाँ वह कुछ मुस्कराकर बातें करती दिखाई देती। जैसे उसी आयु वर्ग में यह संभव हो।
मैं चिंतित हो गया। ऐसा कैसे चलेगा? ऐसे कैसे हम नायक-नायिका बन पाएँगे? मैंने रमेश भाई से बात की। यह भी चिंतित थे। मैंने कहा – मैं कोशिश करूँ? उसकी उम्र का हो जाने की? रमेश भाई ने सिगरेट जलाई, धुआँ छोड़ा… फिर बोले – करके देख लो।
बस इतनी-सी बात थी। बस यही बात थी। बस इसी तरह बात शुरू हुई थी। मैं रमेश भाई-मधु-मंजू-मीरा को अपने घर चाय पिलाने ले गया। वहाँ मीरा मेरी छोटी बहनों से मिली। लौटते में मैंने उसे अपने बारे में बहुत-सी बातें बताईं। उस दिन से रिहर्सल के ब्रेक में मैं सिर्फ मीरा से बातें करता। उसे कौन से फूल पसंद हैं? कौन सी मिठाई? कौन सा हीरो? कौन से गाने वगैरह।
फिर एक दिन हम लोग मीरा-मंजू के यहाँ चाय पीने गए। मीरा ट्रे में छह गिलास पानी लेकर आई। मैं एक-एक करके छहों गिलास पानी पी गया। खूब हा वा हुई। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। मीरा स्कर्ट-ब्लाउज पहने हुए थी और इस पोशाक में बेहद सहज और रिलेक्स्ड लग रही थी। मुझे उसने अपने बचपन की एक मुटल्ली-सी गुड़िया दिखाई। उसने अपनी स्लैमबुक भी दिखाई जिसमें उसने अपने सभी सहेलियों के ऑटोग्राफ ले रखे थे। उसने हम सबमें से सिर्फ मुझसे आग्रह किया कि इसमें ऑटोग्राफ कर दूँ और अपने बारे में संक्षिप्त जानकारियाँ भरूँ। मैंने ऐसी-ऐसी भरीं कि वह पेट पकड़-पकड़कर हँसती रही।
उस दिन से मैं उसका ‘टैडी बीयर’ हो गया।
और हम दोनों रमेश भाई के नाटक के पति-पत्नी आदर्श और वसुंधरा।
(पर सिर्फ नाटक भर के लिए। क्या वह जानती थी? क्या रमेश भाई के नाटक की खातिर मैं एक लड़की की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहा था? या वह भी जानती थी और नाटक की सफलता के लिए हम दोनों अपना भावनात्मक कचूमर निकलवाने के लिए स्वेच्छा से तैयार हो गए थे?)
‘आदर्श और वसुंधरा बरसों से पति-पत्नी हैं। औलाद कोई नहीं। रिश्तेदार बमबारी में मर-खप गए। फैक्टरी बंद हो गई और आदर्श सड़क पर आ गया। छोटे-मोटे धंधे किए, हर बार नाकामयाब रहा। घर की पूँजी बिक गई। शराब पीने लगा। जुआ खेलने लगा। कितना परिचित यथार्थ है। नाटक में यह सब नहीं। सिर्फ यह कि झोंपड़ी म्यूनिसिपाल्टी वाले तोड़ गए। घर का छोटा-मोटा सामान बिखरा पड़ा है। एक पेड़ के नीचे पनाह ली है। शाम को शायद गोडो आए। वसुंधरा रो रही है और आदर्श कह रहा है कि मैं तो जब नवीं क्लास में था तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि जब हमारी शादी होगी तो मैं हनीमून मनाने के लिए चित्रकूट जाऊँगा।
‘चित्रकूट’ जोर देकर बोला जाता है। सारे हॉल में ठहाका गूँज जाता है। विंग में रमेश भाई उछल पड़ते हैं। और सेम्युअल बैकेट हैं कि घूरे जा रहे हैं।
उस रात फिर सेम्युअल बेकेट मेरे सपनों में आए। घूर रहे थे। बेचैनी से इधर-उधर टहल रहे थे। रुके। मेरी तरह मुँह करके खड़े हो गए। घूरा। कुछ बुदबुदाए। फिर विलीन हो गए।
संसार में दुख है। क्या हमें दुख का कारण मालूम है? बिना कारण जाने निदान? हास्यास्पद नहीं? या ऐसा ही पता नहीं क्या?
दूसरे दिन मैंने रमेश भाई को बताया कि इस-इस तरह रात मेरे सपने में सेम्युअल बेकेट आए थे।
– क्या कह रहे थे? रमेश भाई ने पूछा।
– पता नहीं। समझ नहीं पाया रमेश भाई। पता नहीं फ्रेंच में बोले या आइरिश में।
रमेश भाई बोले – तुम इतने बड़े हो गए तुम्हें फ्रेंच नहीं आती? शर्म की बात है। खैर, वैसे मुझे भी नहीं आती? पर छोड़ो। नाराज तो नहीं लग रहे थे?
– कुछ समझ में नहीं आया रमेश भाई।
– छोड़ो छोड़ो! नर्वस होंगे।
इससे ज्यादा कुछ सोचा भी नहीं जा सकता था। हम घोड़े पर सवार हो चुके थे। घोड़ा दुलकी ले रहा था। रोज रिहर्सल चल रही थी। मंजू जी कॉस्टयूम डिजाइन कर रही थीं। किशन-कुशल पोस्टर-बैनर बना रहे थे। मधु व्यवस्था और प्रबंधन के लफड़ों से अकेला जूझ रहा था। महेंद्र पर्मनेंट प्रॉम्प्टर था। अश्विनी ने प्रकाश व्यवस्था की जिम्मेदारी ली थी। उसकी फोटोग्राफी की दुकान थी। उसके बड़े भाई पूना इन्स्टीट्यूट में थे। मेकअप के लिए प्रकाश आर्टिस्ट से बात कर ली गई थी जो बारह साल बंबई रह चुके थे और बलराज साहनी से नाना पलसीकर तक पता नहीं कि किस-किसका मेकअप कर चुके थे।
सब भिड़े थे। इन दिनों भी क्लासें चल रही थीं। लेकिन जैसे नहीं चल रही थीं। शहर में नई पिक्चरें लग रही थीं। लेकिन जैसे नहीं लग रही थीं। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से रात ग्यारह बजे ‘आपकी फरमाइश’ में एक से एक मारू पुराने गाने आ रहे थे। पर जैसे नहीं आ रहे थे। बॉटानिकल गार्डन में क्रिसेंथमम और देसी गुलदाऊदी के ये बड़े-बड़े रंग-बिरंगे फूल खिले थे। पर जैसे नहीं खिले थे। नवंबर की ठंडी रातों में चाँदनी एक अजीब-सी वहशी तनहाई में सारे कपड़े खोलकर नहा रही थी। पर जैसे नहीं नहा रही थी। हम लोगों के लिए समग्र जीवन और अखिल ब्रह्मांड में सिर्फ एक चीज बची थी -वेटिंग फॉर गोडो। उर्फ प्रतीक्षा और प्रतीक्षा।
रिहर्सल में अक्सर अँधेरा हो जाता। फिर चायोपरांत चर्चा में कभी दस बजते कभी ग्यारह। ठंडी पड़ने लगती। मधु मफलर लपेट लेता। किशन-कुशल मंकी कैप डाट लेते। महेंद्र चमड़े के दस्ताने पहन लेता। मेरे पास सिर्फ एक पतला-सा बगैर बाँहों वाला लाल स्वेटर था जो मैंने कचहरी रोड के फुटपाथ से चार रुपये में खरीदा था। मैं बगल में हाथ घुसेड़े रहता था सिगरेटें फूँकता रहता। फिर भी मुझसे कोई गाना या गजल सुने बगैर कभी गुडनाइट नहीं होती।
एक दिन अपने कपड़ों में से एक भूरा-सा गरम कोट निकालकर रमेश भाई ने मुझे दिया – पहनकर देखो!
क्यों? – हेकड़ी से मैंने पूछा।
– प्रॉप है। कैसा रहेगा?
मैंने पहना। बाँहें कुछ ओछी थीं। मेरे लंबे-पतले हाथ बाहर निकल रहे थे। रमेश भाई ने दस कदम दूर जाकर आँखें मिचमिचाकर देखा। बोले – परफेक्ट! मैंने कहना चाहा – लेकिन यह फटा हुआ तो है नहीं। पर चुप रहा। कोट की गर्मी अच्छी लग रही थी।
वह कोट उस साल मैं फरवरी तक पहनता रहा। माँ ने कहा – ड्राइक्लीन करके लौटाना। पता नहीं किस जादू से इसके लिए उन्होंने एक-एक रुपये के दस सिक्के अपनी पेटी से निकालकर मेरी हथेली पर रख दिए।
लेकिन इधर रिहर्सल चल रही थी उधर इसके समानांतर ही एक नाटक और रहा था।
उदयवीर एंड पार्टी ने हमारे खिलाफ अभियान चला रखा था। हिंदी परिषद की तरफ से अंग्रेजी का नाटक? ऐसा क्यों? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अंग्रेजी का नाटक तो अलग से होता ही है। फिर हिंदी परिषद एक विदेशी नाटक का हिंदी अनुवाद कैसे कर रही है? और अनुवाद क्या प्रामाणिक है? किसी ने देखा? किसने किया है अनुवाद? किसने इसकी अनुमति दी? क्या क्या त्रिपाठी जी के कहने भर से हो जाएगा? कब हुई हिंदी परिषद की बैठक? क्या हिंदी परिषद की बैठक में इस पर चर्चा हुई? अनुमोदन हुआ? क्या हिंदी में नाटकों का अभाव है? ध्रुवस्वामिनी है। स्कंदगुप्त है। नया करना हो तो अंधा युग है। आधे अधूरे है। फिर विदेशी नाटक ही क्यों? सो भी सेम्यूअल बेकेट? किसी ने पढ़ा है यह नाटक? कहाँ से आई स्क्रिप्ट? और सर… सही बात तो यह है कि नाटक अश्लील है। इतने प्रतिष्ठित महाविद्यालय में ऐसा नाटक! महाविद्यालय की सारी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी।
उदयवीर एक-एक प्रोफेसर के घर जा रहा था। समूह बनाकर एम.ए. हिंदी के दस-बारह छात्र इस सिलसिले में प्रिन्सिपल से भी मिले थे। उसने धमकी भी दे डाली थी कि यदि इसे रुकवाया नहीं गया तो वह प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अखबारों में भी छपवाएगा।
उदयवीर के बाप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष थे। वह अकेडेमिक क्षेत्र के कुख्यात विद्वान थे। सारा हिंदी विभाग जानता था कि एम.ए. में पहली और दूसरी पोजीशन उदयवीर और उसकी प्रेमिका निशा की ही आने वाली है। हम चाहे लाख जोर लगा लें हमारा कुछ नहीं होना है। वह बनेगा बाप की तरह प्रोफेसर और हम चलेंगे शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय – बी.एड. करने। कुंठा की ऐसी स्थिति थी कि किशन तड़पकर कहता था – ‘गरीब का धन आशा है मित्रो! हमें प्रतीक्षा करना चाहिए कि अगले सोमवार’ या ‘किसी अगले सोमवार’ पिताश्री को हार्ट अटैक आएगा और हमें उन्हें श्रद्धांजलि देने का ऐतिहासिक सौभाग्य प्राप्त होगा।
विभागाध्यक्ष त्रिपाठी जी अस्वस्थ थे और छुट्टी पर थे। उनकी जगह उनका काम सँभाल रही थीं आशा शर्मा मैडम जो उदयवीर गुट के दबाव में थीं और प्रिन्सिपल के चिंता व्यक्त करते ही हिंदी परिषद की बैठक बुलाने को तैयार हो गईं।
रमेश भाई और उदयवीर में खुले आम खुन्नस थी। सत्र की शुरुआत में जब स्थापित लेखक की प्रतिष्ठा लेकर रमेश भाई एम.ए. प्रीवियस में आए थे, उदयवीर ने रमेश भाई को अपनी कुछ प्रेम कविताएँ दिखाई थीं – इस अनुरोध के साथ कि रमेश भाई ठीक समझें तो इन्हें धर्मयुग-ज्ञानोदय वगैरह में छपवा दें। पढ़ने के बाद रमेश भाई ने कविताओं का पुलिंदा उदयवीर को पकड़ाते हुए कहा था – प्रेम कविताएँ लिखना है तो पहले लड़की के साथ वास्तव में कुछ करके आओ।
लेकिन तमाम योजनाबद्धता और गोपनीयता के बावजूद आशा शर्मा द्वारा आहूत हिंदी परिषद की आपात बैठक में पता नहीं कैसे, खराब तबीयत के बावजूद त्रिपाठी सर आ गए। हालाँकि त्रिपाठी सर बेकेट की स्पेलिंग से भी परिचित नहीं थे, पर वह अपने निर्णय पर डटे रहे और उन्होंने विरोधियों की एक न चलने दी। हालाँकि इसके तुरंत बाद माइग्रेन से उनका सिर फटने लगा और आशा शर्मा मेडम ने ही अपने पर्स से बाम निकालकर उसके सिर की मालिश की। लेकर आई थीं। जानती थीं जरूरत पड़ सकती है।
मीरा अब नाटक में रस लेने लगी थी। मेरे प्रॉप में रमेश जी का एक मुड़ा-तुड़ा बरसाती टोप था। मैंने बीच में माँग निकालना शुरू कर दिया था। ब्रेक में टोप उतार देता। फिर जैसे ही टोप पहनता एस्ट्रागॉन मुझ पर बुरी तरह हावी हो जाता। मैंने चार्ली चैपलिन और राजकपूर को अपनी आत्मा में आमंत्रित कर लिया था कि कृपा करके कुछ दिन यहीं निवास कर लें। रिहर्सल के दौरान मेरी हरकतों पर मीरा खूब हँसती। बेआवाज, पर खूब। मेरे हर डॉयलॉग पर, जेस्चर, पर मूवमेंट पर उसकी हँसी छूट जाती। कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता। जबकि उसे दुख और तनाव में रहना था। हँसना तो बिल्कुल नहीं था। मीरा की हँसी से रिहर्सल बाधित होती। पर रमेश भाई होने देते। उनका सोचना था कि यह हो ही जाना चाहिए। कॉमेडी नारियल का खोल है। इसे फोड़कर ही हम सिचुएशन की ट्रेजेडी तक पहुँचेंगे।
अब दोस्तो देखिए कि कहानी कैसे शुरू होती है।
एक दिन ब्रेक में मैं और मीरा हॉल के बाहर सीढ़ियों पर बैठे धूप खा रहे थे। अचानक मीरा बोली – ‘टैडी बीयर! तुम सुबह से शाम तक यहाँ रहते हो। खाना कब खाते हो? भूख नहीं लगती?’ मेरे बदन में झुरझुरी दौड़ गई। पहली बार किसी ने मुझसे यह सवाल पूछा था। बाकी तो यही समझते थे कि मैं ब्रेक में घर जाकर जल्दी से खा आता हूँ। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। कैसे बताता कि दिन भर बाहर रहकर मैं अपनी छोटी बहनों के लिए चार रोटी बचाता हूँ। मीरा चुपचाप बेहरकत बैठी रही। फिर बोली – ‘दीदी का आज फास्ट था। तो मेरे टिफिन में एक पराठा बच गया है। खाओगे?’ टिफिन उसके साथ ही था। खोला, आगे बढ़ाया। मैंने उसकी तरफ मुँह नहीं घुमाया। मैं रो रहा था। मीरा ने अपनी दोनों हथेलियों में मेरा चेहरा भरकर अपने चेहरे के पास खींच लिया। अपने होंठ मेरे होंठों पर रख दिए। उसकी भी आँखें डबडबा गईं। फुसफुसाकर बोली – लोते नई। लोते नई। अत्थे बच्चे लोते थोली हैं! लो। खाओ। और अपने हाथ से कौर तोड़-तोड़कर मुझे खिलाती रही। मैं आँसू पोंछता रहा और खाता रहा। कुछ देर बाद बोली – ‘आज खिला रही हूँ। कल नहीं खिलाऊँगी। ये मत सोचना कि रोज-रोज खिलाऊँगी। कल मेरा फास्ट है। साबूदाने के बड़े बनाकर लाऊँगी। खाओगे? एक खा लेना। अच्छा आधा खा लेना। अच्छा इत्ता-सा खा लेना मेरे हाथ से। ठीक है?’
ये न होता तो फायनल शो में वह सीन भी इतना मार्मिक नहीं बन पाता जिसमें वसुंधरा रोई थी। जब मैंने रमेश भाई के मुँह पर थूक दिया था। उस शो में मीरा सचमुच रोई थी। हिचकियाँ ले-लेकर।
पोजो एक पूँजीपति है और लकी एक बुद्धिजीवी। और पोजो लकी की पीठ पर सवार है। मूल नाटक में ऐसा ही है। हमने बदल दिया। एक तो इसलिए कि दुबले-पतले रमेश जी छह फुट एक इंच के मधु जोशी को पीठ पर नहीं ढो पाते। दूसरे, हमें लगा अभी हिंदुस्तान में हालत इतनी नहीं बिगड़ी है। हमने लकी के गले में पट्टा डाल दिया। पट्टे में रस्सी डाल दी। रस्सी का सिरा पोजो के एक हाथ में और दूसरे हाथ में हंटर। वह कुत्ते की तरह लकी को लिए फिरता है। लकी पीठ पर पोजो का सामान ढोता है और कोड़े खाता है। आदर्श और वसुंधरा सहानुभूतिवश उसके पास जाते हैं तो वह आदर्श के घुटने में लात मार देता है। उसे किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए। पोजो के शब्दों में उसे आम आदमी की सहानुभूति नहीं चाहिए। दर्द से बिलबिलाता आदर्श गुस्से में भन्नाता लकी के पास जाता है और उसके मुँह पर थूक देता है। शो से पहले ग्रांड रिहर्सल तक रमेश भाई मुझे पर चिल्लाते रहे – सचमुच थूको। जोर से थूको। छीटे उड़ना चाहिए। दिखना चाहिए। लेकिन मैं कभी नहीं कर पाया। कोई भी कैसे कर पाता? हम सब कितना प्यार करते थे। रमेश भाई से!
…रमेश भाई के घुंघराले बाल बिखेर दिए गए थे। पाउडर मसलकर उन्हें अधकचरा बना दिया गया था अधकचरी दाढ़ी चेहरे पर बिखरी थी। मेकअपमैन प्रकाश आर्टिस्ट ने कमाल कर दिया था। अब वहाँ रमेश भाई नहीं थे, विद्यासागर था जिसकी आँखों में नफरत भी थी, मोहब्बत भी और दहशत भी… और मैंने उस चेहरे पर सचमुच थूक दिया था!!
नाटक बदलवाने की मुहिम कामयाब नहीं हुई तो उदयवीर एंड पार्टी ने नया दाँव फेंका। कॉलेज के नाटक में बाहर का आर्टिस्ट क्यों? क्या कॉलेज में कोई आर्टिस्ट नहीं है? कॉलेज के किसी आर्टिस्ट को मौका क्यों नहीं दिया गया? और कौन है ये बाहर का लड़का जो हीरो का रोल कर रहा है? क्या सिनेमा या रंगमंच का कोई मँजा हुआ कलाकार है? क्या एनएसडी से आया है? क्या फीस दी जा रही है उसे? क्या विद्यार्थी निधि का पैसा इस तरह लुटाने के लिए है?
अब लेकिन हम सबके लिए यह हँसने की बात थी। लेकिन मधु के लिए नहीं। ऐसा न हो कि ऐन वक्त पर कुछ लफड़ा हो। वह रमेश भाई को लेकर त्रिपाठी सर के घर गया। आशा शर्मा मैडम के घर गया। छात्र यूनियन के सचिव के घर गया। स्थापित कर आया कि विद्यार्थी न सही, भूतपूर्व विद्यार्थी तो मैं इस महाविद्यालय का हूँ ही। और फिर जरा आप उसकी परफार्मेंस देखिए। रिहर्सल में आइए थोड़ा समय निकालकर। और फिर भी आप कहेंगे तो… बदल देंगे जी। इसमें क्या खास बात है! लेकिन अब कलाकारों के चयन जैसी छोटी-छोटी चीजों को इशू बनाना…!!
एक दिन मीरा मुझसे बोली – हमारे पड़ोस में एक कौशिक जी हैं। तीन साल पहले उन्होंने लव मैरिज की थी। घर वालों ने निकाल दिया तो वाइफ को लेकर यहाँ आ गए। कुछ दिन सोचते रहे क्या करे क्या करें, फिर छोटे बच्चों का स्कूल खोल लिया। जम गया। खूब अच्छा चल रहा है। दोनों उसी में लगे रहते हैं। कुछ टीचर्स भी रख ली हैं। मस्त रहते हैं। अच्छा है न? बोलो, अच्छा है न? कितना अच्छा है न? बताओ न? अच्छा रहेगा न?
मैंने रमेश भाई से पूछा – आजकल मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है रमेश भाई?
रमेश भाई ने चाय का प्याला परे सरकाते हुए पूछा – कैसा?
मैंने कहा – जब से गोडो को हाथ लगाया है, सला डोकरा हर दूसरे-तीसरे दिन सपने में आ जाता है। पूछता-करता कुछ नहीं, बस घूरता रहता है। सारी नींद खराब करके रख देता है। साहित्यिक उठाईगिरी तो पहले भी हमने बहुत की है। यही अपने माल को लेकर इतना पजेसिव क्यों है? अरे भई, तुम मर गए। बात खत्म हो गई। अब छोड़ो।
रमेश भाई ने सिगरेट सुलगाकर एक कश खींचा, ऊपक मुँह करके धुआँ उड़ाया और मुसकराकर बोले – कल मेरे सपने में भी आए थे।
मैने कहा – रीयली? कितने बजे?
– ढाई बजे!
– ढाई बजे तो वह मेरे सपने में थे। मैं रहता हूँ डिग्गी बाजार में, आप रहते हैं कड़क्का चौक में। एक साथ दो जगह वह कैसे पहुँच गए?
– महान लोगों का कोई भरोसा नहीं। वे कभी भी, किसी की भी नींद उड़ा सकते हैं।
मैं सोच में पड़ गया।
कुछ देर बाद मैंने धीमे सुर में कहा – रमेश भाई! लकी की स्पीच वाला मामला तो नहीं है?
रमेश भाई बोले – लकी की स्पीच एकदम बेसिर पैर की बड़बड़ाहट है। एकदम बेमतलब।
मैंने कहा – ठीक है। आपको बेमतलब लगती है। पर ये भी तो सोचो कि इतना बड़ा राइटर है… नोबल लॉरेट… बिना सोचे-समझे तो ढाई पेज की बेमतलब स्पीच रखेगा नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम उसे डिसाइफर नहीं कर पा रहे है, डिकोड नहीं कर पा रहे हैं मतलब!
– कोई नहीं कर पाया आज तक। वह उसने प्रकट में पोजो के मनोरंजन के लिए बोली है। उसके आदेश पर। और सामंतों का मनोरंजन जिन चीजों से होता है उसमें अर्थ कहाँ होता है? पूँजीपति करोड़ों रुपये खर्च करते जो अमूर्त पेंटिंग्स खरीदते हैं, क्या वाकई उसके सौंदर्य के पारखी होते हैं? उसे समझना चाहते भी हैं? या सिर्फ रूप का मोह? या सिर्फ पजेशन का गुरूर! क्या? …तो लकी ने कहा कि ले साले! ले संभ्रांत बकवास का मजा!
…और प्रच्छन्न रूप से वह व्याख्यावादी आलोचकों को चिढ़ा रहे हैं… जिन्हें हर कलाकृति में ‘मानवीय’ और ‘उदात्त’ ढूँढ़ने की कुटेव पड़ी हुई है।
‘कुटेव’ शब्द पर हम दोनों हँसे। कुटैव का हमारे लिए एक ही अर्थ था – हस्तमैथुन।
कुछ देर बाद मैं बोला – रमेश भाई, बेकेट की यह इंटेन्शन भी तो हो सकती है कि बुद्धिजीवी आमजन के लिए इस कदर दुर्बोध नहीं होता तो शायद उसकी यह हालत नहीं होती।
– मैं पॉपुलिज्म के पक्ष में नहीं हूँ। रमेश भाई कड़वाहट के साथ बोले।
मैं थोड़ा बुझ सा गया। फिर पूछा – और लकी? लकी नाम क्यों रखा होगा इस बंदे का बेकेट ने?
रमेश भाई की आँखों में चमक आ गई। मुस्कराकर बोले – क्या समाज इसी भाव से नहीं देखता कवियों-कलाकारों-बुद्धिजीवियों को? सरस्वती के वरद पुत्र। प्रतिभा के पुंज। मेधा के ढेर। जीनियस। सिलेक्टेड वन्स। क्या उनकी ख्याति से लोग ईर्ष्या नहीं करते? उनका लाघव देखकर हतबुद्धि नहीं होते? उनकी चमक देखकर चौंधिया नहीं जाते? जबकि वास्तव में उनकी क्या स्थिति होती है? सुखिया सब संसार है, खावै और सोवै। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवै।
– तो आप क्या स्पीच देंगे?
रमेश भाई ने उठते हुए कहा – वह मैं शो के एक दिन पहले लिखूँगा।
एक बार सारी रात बैकेट मेरे सपने में नहीं आए। उस सारी रात मैं सपने में मीरा के साथ रहा स्टेज से निकलकर हम सीधे स्टेशन गए और फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में जा बैठे। रात का समय था और गर्मियों के दिन। मीरा स्कर्ट-ब्लाउज पहने थी। गाड़ी दौड़ रही थी शटाशट शटाशट। बाहर पीछे छूटते पेड़ और खेत और पहाड़ और चाँदनी। मीरा का छोटा-सा हाथ मेरे हाथ में था। हवा से उसके बाल उड़-उड़कर चेहरे पर आ रहे थे। फिर वह मेरी गोद में सिर रखकर सो गई। मैं उसकी पीठ पर सिर टिकाकर। वह ट्रेन उस रात कहीं नहीं रुकी। जबकि मैं डर रहा था कि ट्रेन रुक गया तो मीरा जाग जाएगी और मुझे अकेला छोड़ किसी अनजान स्टेशन पर उतर जाएगी।
सत्रह-अठारह को शो था। पोस्टर लग चुके थे। निमंत्रण-पत्र बँट चुके थे। तेरह की सुबह कॉलेज गया तो वहाँ कोई नहीं दिखा। हॉस्टल गया। मधु के कमरे में गया तो किशन-कुशल भी वहीं मिल गए। मधु अपने आगे बहुत सारे कागज-फाइलें-फोटोकॉपियाँ बिछाए बैठा था। मुँह में आलपीन दबा रखी थीं।
– क्या है?
– थानेदार की वेकेन्सी है। आज लास्ट डेट है।
– मधु, मेरा खयाल था तुम एम.ए. कर रहे हो।
– जस्ट फॉर नेमप्लेट! पास बैठा किशन कड़वाहट से बोला।
– लेकिन मधु तुम्हारी आइसाइट? तुम्हें माइनस फोर का चश्मा लगता है।
– पाँच हजार रुपये। चिढ़ी आवाज में मधु बोला। खीसे में पाँच हजार होना चाहिए बस।
– मधु, मैं सोचता था तुम शायद टीचिंग में…
– जाने दो यार! उसे परेशान मत करो। जो कर रहा है करने दो। वैसे भी साला होना-जाना तो कुछ है नहीं। तो इस खुशी से भी क्यों महरूम रहें कि हमने पूरी कोशिश की। किशन बोला।
– तुमने भी किया है? मैंने किशन से पूछा।
– किसने? मैंने? नहीं नहीं। मेरा तो सिद्धांत है अकर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु रस्ते रस्ते।
– ऐसी बात नहीं है। प्रतीक्षा भी एक काम है। अब तक चुप बैठा कुशल बोला – हम उदयवीर के पिताश्री के स्वर्गीय होने की प्रतीक्षा नहीं कर रहे?
मेरा दम घुटने लगा। मैं उठकर बाहर आ गया।
मीरा बाहर धूप में बैठी थी। उसकी पीठ काँप रही थी। मैं गया। देखा रो रही है। पूछा -क्या बात है? क्या हो गया? कई बार पूछा। अंत में बोली – सिर दुख रहा है।
मैं उठकर हॉल में गया। रमेश भाई कारपेंटर और हार्टीकल्चरवालों से सेट के बारे में बात कर रहे थे। मैंने धीरे-से कहा – रमेश भाई, दो रुपये देना, मीरा को…
रमेश भाई ने हिप पॉकेट से अपना मोटा-सा पर्स निकालकर मुझे पकड़ा दिया और फिर कारपेंटर से बात करने लगे।
मैं मीरा को लेकर कॉलेज कंपाउंड से बाहर आया। केमिस्ट से गोली ली। होटल से पानी। मीरा को गोली खिलाई। चाय पिलाई। वापस आए। इस पूरे दर्मियान दोनों एकदम चुप रहे।
बात क्या थी, इसका पता शो के बाद चला। मीरा-मंजू के घर में झगड़ा हुआ था। उनके डैडी के दोस्त और उदयवीर गुट के सिखाए कुछ बुजुर्ग पड़ोसी समझाने आए थे। लड़की को ड्रामे में काम मत करने दो। बदनाम हो जाएगी। लोग चलते रस्ते फिकरे कसेंगे। पढ़ाई पूरी करना मुश्किल हो जाएगा। बाल-बच्चेदार आदमी हो। चुपचाप ग्रेज्युएशन कराके हाथ पीले करो और छुट्टी पाओ। इस उम्र में पैर फिसलते देर नहीं लगती। ड्रामा पार्टी में अक्सर ऐसी बातें होती रहती हैं। लड़की को किसी ने बहला लिया तो मुँह काला करवाएगी तुम्हारा बिरादरी में। अभी तो बड़ी भी बैठी है। किसी ने लड़के वालों से जाकर कह दिया कि लड़कियाँ ड्रामे-नाटक-नौटंकी में पार्ट करती हैं तो हो चुका रिश्ता! बद अच्छा बदनाम बुरा। जैसे हमारे बच्चे वैसे तुम्हारे बच्चे। हमें तो ताज्जुब है तुमने पहले दिन से ही क्यों नहीं रोका? दुबे जी बता रहे थे नाटक भी कोई ढंग का नहीं है। मतलब जरा ऐसा-वैसा है। मतलब अश्लील है।
आग लगाने वाले आग लगाकर चले गए। धुआँ सारी रात उठता रहा। पति-पत्नी पसोपेश में। बच्चों को इतनी आजादी देकर गलती तो नहीं की? क्या करें? लड़कियाँ हैं कि छोड़ने को तैयार नहीं। लंबी बहसबाजी के बाद आखिर तय हुआ कि छन्नू चाचाजी का लड़का मुकेश और बगल वाले रामअवतार जी की बेटी सुषमा हर रिहर्सल में साथ जाएँगे, पूरे टाइम साथ रहेंगे और जरा भी कोई ऐसी-वैसी बात दिखाई दी… तो नाटक साला क्या होता है… मैं कॉलेज ही छुड़वा दूँगा। सावित्री गर्ल्स कॉलेज में जाओ अगले साल से!
पूरी यूनिट शो के बाद तक मुकेश और सुषमा की जासूस उपस्थिति से अनजान रही। मंजू-मीरा ने किसी को नहीं बताया। बताने की जरूरत ही नहीं समझी। मन ही मन स्वयं को अपमानित जरूर महसूस करती रहीं।
जब कोई दाँव नहीं चला तो उदयवीर एंड पार्टी ने तय किया कि होने दो नाटक! ऐसी हूटिंग करेंगे कि इनके छक्के छूट जाएँगे। बाहर फोड़े जाएँगे पटाखे और अंदर उड़ा दी जाएगी साँप निकलने की अफवाह। मेन लाइन पर लंगड़ फेंककर फ्यूज उड़ा दिए जाएँगे। किरमिच की फलियाँ लाओ। प्लाजा टाकीज और मेजेस्टिक टॉकीज पर ब्लैक में टिकट बेचने वाले छोरों को पकड़कर लाओ। इनकी तो वेटिंग की ऐसी हालत बनाएँगे कि साले जिंदगी भर याद रखेंगे।
इसलिए शो से एक दिन पहले, यानी सोलह को एक ड्रेस रिहर्सल सिर्फ हूटिंग के खिलाफ खड़े रह पाने का मनोबल प्राप्त करने के लिए की गई। खानदानी हूटर बुलवाकर बैठाए गए। उन्होंने वफादारी से हूटिंग शुरू भी की थी, लेकिन विडंबना यह हुई कि कुछ ही देर में उन्हें नाटक में इतना मजा आने लगा कि बेचारे भूल ही गए कि यहाँ लाए गए थे।
त्रिपाटी सर डर रहे थे। लंबे संशय के बाद उन्होंने प्रिन्सिपल से कहा, बल्कि पूछा कि पुलिस बुलवा ली जाय क्या… क्योंकि मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री हैं और…
प्रिसिन्पल माथुर ने दृढ़तापूर्वक मना कर दिया। नहीं त्रिपाठी जी। चाहे जो हो जाए, मेरे रहते कॉलेज कैंपस में पुलिस नहीं आएगी। (नवयुवक मित्रो! मेरा विश्वास करो! ऐसा भी जमाना था। और यह कोई शताब्दियों पुरानी बात भी नहीं है।)
रमेश भाई से एक उत्तर कहानी बातचीत
स्थान – न तेरा घर न मेरा घर
समय – सैंतीस साल बाद
मैं – रमेश भाई, 1993 में जब सराजेवो की घेराबंदी चल रही थी, सूसन सौंटेग ने बम वर्षा के बीच सराजेवी शहर में अपने कुछ साथियों के साथ ‘वेटिंग फॉर गोडो’ का मंचन किया था। आपको क्या लगता है, उन्होंने ऐसा क्या किया होगा?
रमेश भाई – (दो मिनट रुककर) सूसन सौंटेग कभी भी एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल नहीं रहीं, जैसे घटिया और सनसनीबाज लेखक के पक्ष में भी आवाज उठाई।
मैं – …पीछे मुड़कर देखते हैं तो कैसा लगता है? निरर्थकता बोध का अनुभव होता है?
रमेश भाई – (तीन मिनिट रुककर) ‘प्रतीक्षा और प्रतीक्षा’ में एक डायलॉग था -आदमी सूअर से भी मिले तो कुछ न कुछ सीखता है।
मैं – …किस तरह का समाज बनाना चाहते थे हम? और किस तरह का बन गया समाज?
रमेश भाई – (चार मिनिट रुककर। लंबी उसाँस छोड़कर) कलाकृतियों से समाज नहीं बदलता।
मैं – रमेश भाई! आपको उदयवीर की याद है?
रमेश भाई – …हाँ, वह जयपुर में प्रोफेसर रहा। विभागाध्यक्ष। पिछले साल ही रिटायर हुआ है। अब वीसी बनने के लिए चक्कर काट रहा है।
मैं – उदयवीर कहता था किसान का सत्य वर्षा है…। …और जब तक हमारी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है, आप भगवान से नहीं लड़ सकते।
रमेश भाई – (बहुत देर रुककर। जमीन को घूरते हुए) चौदह साल की उम्र में घर छोड़ने के बाद मुझे भगवान की जरूरत कभी नहीं पड़ी। और मेरा खयाल है मेरे जैसे लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और बढ़ती जाएगी।
मैं – (लंबी चुप्पी के बाद) रमेश भाई, मरना तो सबको है। क्या आप एक संतुष्ट व्यक्ति की तरह मरेंगे?
रमेश भाई – (डबडबाई आँखों से मुस्कराते हुए) बिल्कुल!
(उठकर पहले मुझसे हाथ मिलाते हैं, फिर लिपट जाते हैं।)
एक बार रिहर्सल के ब्रेक में सबसे दूर ऊपर बालकनी में बैठे मैं और मीरा बातें कर रहे थे। ब्रेक के बाद हमेशा की तरह ताली बजाते हुए रमेश भाई ने बुलाया – ‘कमॉन एवरीबडी!’ हमने सुना नहीं। उन्होंने महेंद्र को भेजा। हम लगभग भागते हुए आए। मुझे टोप पकड़ाते हुए रमेश भाई सख्त आवाज में बोले – जरा सँभाल के। वो अभी सेकंड ईयर में है।
मैं भौंचक! क्या हुआ? मैंने क्या किया? किसी ने कुछ कहा क्या रमेश भाई से? ऐसा क्यों कह रहे हैं? शाम तक रिहर्सल चली। सब कुछ ठीक-ठाक रहा। पर मेरा अनमनापन बना रहा। क्या मैं मीरा का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा हूँ? क्या मैं बहका रहा हूँ? क्या मैं अपनी औकात भूल रहा हूँ? क्या मैंने इन पढ़े-लिखों के बीच कोई गँवारों जैसी हरकत कर दी है? क्या कोई मेरे खिलाफ रमेश भाई के कान भर रहा है?
आम तौर पर लड़कियाँ अँधेरा होते ही घर चली जाती थीं। उस दिन पता नहीं क्या बात थी कि मंजू, मीरा और सुधा भी हमारे साथ थीं। अंतिम चाय के बाद हस्बमामूल मुझसे गाने की फरमाइश की गई। मैंने तड़पकर सुनाया –
वो कोई और न था, चंद खुश्क पत्ते थे।
शजर से टूट के जो फस्लेगुल पे रोए थे।
हमारी जो भी मुलाकात थी अधूरी थी
के एक चेहरे के पीछे हजार चेहरे थे।
तमाम उम्र वफा के गुनाहगार रहे
ये और बात है हम आदमी तो अच्छे थे!
मीरा ने मुझे पहली बार गाते सुना था। उसका सारा वजूद पिघली हुई मोमबत्ती बना हुआ था। उस रात दो बजे तक मैं, मधु और रमेश भाई साथ रहे और पत्ते वाली गाजर पर विचार करते रहे कि उसका सबसे अच्छा उपयोग क्या हो सकता है। पत्ते वाली गाजर नाटक को मेरा मौलिक योगदान था। पत्तेवाली मूली सबने देखी होगी, पत्ते वाली गाजर आम तौर पर बाजार में दिखाई नहीं देती। मैंने एक दिन दो पत्ते वाली गाजरें लाकर उन्हें एस्ट्रागॉन के पतलून की दोनों जेबों में ठूँस दिया। इस तरह कि गाजर भीतर रहे, पत्ते बाहर झूलते रहें।
फिर हरिकिशन जी भी दुकान बंद कर आ गए। हमारे एक मित्री। सड़कों पर अँधेरा था। तय हुआ कि रेलवे स्टेशने चलकर चाय पी जाए। वहाँ रात भर चाय मिलती थी। चाय लेकर एक तरफ बैठ गए। हरिकिशन जी ने इसरार किया – बाबू! एक बार और सुना दो प्लीज। शजर से टूट के जा… अहाहा!
बिछड़ते समय रमेश भाई ने अलग ले जाकर कहा – थोबड़ा क्यों लटका रखा है सवेरे से? चीयर अप! दोस्तों की बात को दिल से नहीं लगाना चाहिए! आयम सॉरी। चलो! धौल मारापीठ पर। सारे गिले जाते रहे।
नाटक बेहद सफल रहा। पिछले दस बरस में इस स्टेज पर कोई नाटक इतना हिट नहीं रहा। छठे-सातवें मिनट से ही नाटक ने गति पकड़ ली। ठहाकों पर ठहाके। मेरे हर डॉयलॉग पर, मेरी हर हरकत पर पूरा हॉल हँसी से गूँज उठता। कोई गंभीर दृश्य आता तो एकदम सन्नाटा छा जाता। मधु का धनीराम खूब जमा। और रमेश भाई ने तो रुला दिया। लेकिन मैं उस दमघोंटू माहौल में एक प्रेशर वॉल्व की तरह था। थोड़ी-थोड़ी देर में मैं ऐसा कुछ कर देता कि दर्शकों में हँसी की लहर दौड़ जाती। मैं और मीरा दर्शकों के एकदम डार्लिंग बन चुके थे। मैं कहता ‘अब मैं टोप उतार देता हूँ’ तो ठहाका लगता। मैं कहता ‘अब तो टोप पहन लेता हूँ’ तो ठहाका लगता। पता नहीं कैसे ठसाठस भरे उस हॉल में युवा लड़के-लड़कियों ने एस्ट्रागॉन से कैसा तादात्म्य अनुभव कर लिया था। एकदम अद्भुत। खैर, इसमें मेरा क्या था! मैं तो सिर्फ चार्ली चैपलिन और राजकपूर को इमीटेट कर रहा था। बस यह है कि अच्छी तरह कर रहा था। कितनी किस कदर गहरी और प्यारी छवि बसी है जनमन में इन महान कलाकारों की। और बाकी जो था वह आयरलैंड के उस महान नाटककार का था जिसे शोहरत भी मिली तो परदेस में, और एक विदेशी भाषा में।
पर कमाल था! चमत्कार था। जरा सोचिए… सिर्फ चार पात्र… मंच पर सेट के नाम पर सिर्फ एक पेड़… और त्रिपाठी सर द्वारा घुसेड़ दिया गया थोड़ा-बहुत बॉटेनिकल गार्डन… एक्शन एकदम नहीं… खर्चा कुल हजार-डेढ़ हजार रुपया… और इतना बड़ा हिट!! सचमुच चमत्कार ही था।
विंग में हम उछल रहे थे। बार-बार एक-दूसरे से हाथ मिला रहे थे, गले मिल रहे थे। लड़के-लड़की सब। और रमेश भाई एक ही बात बार-बार दोहरा रहे थे – नथिंग लाइक इट!
दूसरे दिन सुबह मैं कॉलेज पहुँचा तो तीन-साढ़े तीन सौ लड़के मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं आगे-आगे और यह पूरा जुलूस पीछे-पीछे। हर कोई मुझे पास से देखना चाहता था। वे मुझसे हाथ मिला रहे थे। एक-दो ने मेरे साथ फोटो भी खिंचवाए। लड़कियों ने मुझसे ऑटोग्राफ लिए। वे सब रात के नशे में थे। मेरे जैसा सड़कछाप फटीचर रातोंरात उनके लिए जैसे स्टार बन गया था। एक दिन के लिए ही सही… लेकिन यह सचमुच उन्मत्त कर डालने वाला था।
थी। मीरा थी। पीछे बगीचे में। अकेली। साबुन की खुशबू। बाल गीले।
मैं पास जाकर खड़ा हो गया। हम चुपचाप एक-दूसरे को पीते रहे। कुछ देर टहलकर बैठ गए।
– टैडी बीयर!
– ऊँ!
– आज दूसरा और आखिरी शो भी हो जाएगा।
– हाँ।
– कल से क्या करेंगे?
मैं कुछ नहीं कह पाया। मुझे लगा कोई मेरे पैरों के नीचे से जमीन और सिर के ऊपर से आसमान एक साथ खींच रहा है।
कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। एक-दूसरे को देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। कहीं माया न निकले।
– मिलोगे? अचानक उसने पूछा।
…
– मत मिलना।
कहा और खड़ी हो गई। और साइकिल तक गई। और साइकिल पर बैठी। और बगैर एक बार भी मुड़कर देखे चली गई।
सेम्युएल बेकेट एक घुटना मोड़े सिर झुकाए बैठे थे। बेहद उदास। धूसर। ध्वस्त। निरर्थकता बोध से लथपथ। आधी सदी पहले मैंने जो लिखा, कंबख्त अभी तक असंगत-अप्रासंगिक नहीं हुआ! विज्ञान!! प्रगति!! करोड़ों लोग तो आज भी गोडो की प्रतीक्षा ही कर रहे हैं! गोडो – जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा! एक ऐसी सड़क पर जो कहीं नहीं जाती! और एक ऐसे पेड़ के नीचे जो कभी नहीं फलता, उल्टे सूखता जाता है!
…और नौजवान लड़के-लड़कियाँ!!