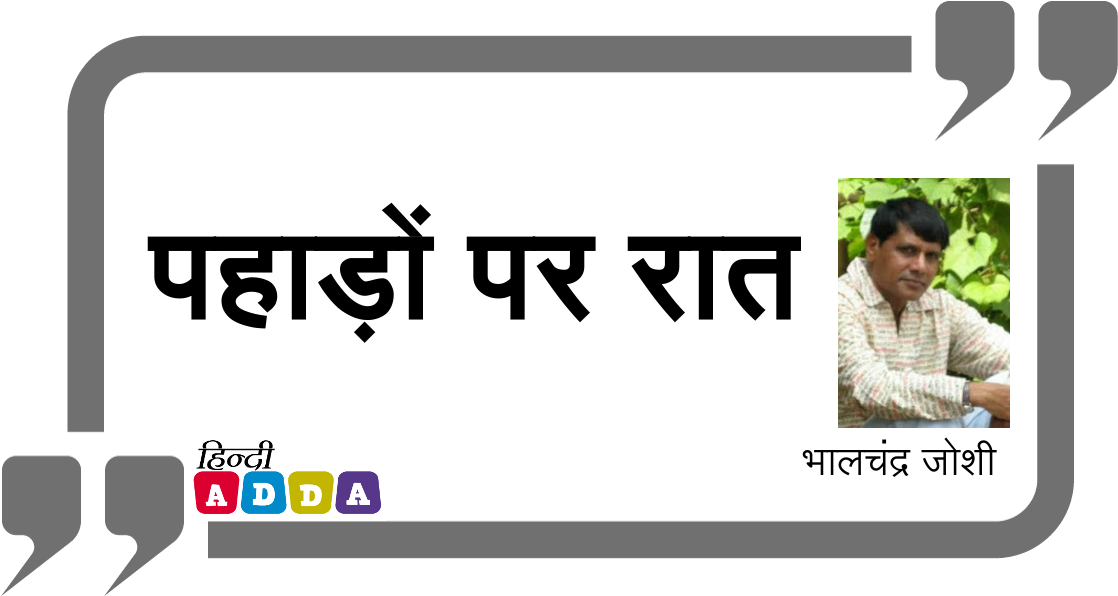पहाड़ों पर रात | भालचंद्र जोशी – Pahadon Par Raat
पहाड़ों पर रात | भालचंद्र जोशी
उसने अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया था। और मैंने भी उसे कुरेदा नहीं था। हालाँकि मैं पूरी तरह खुल गया था। मेरे भीतर की सभी तहें खुल चुकी थीं। यह मेरी कमजोरी है और मैं इससे वाकिफ भी हूँ। लेकिन इसे दूर करने की मैंने कभी कोई कोशिश नहीं की।
मैंने उसकी ओर गरदन उठाकर देखा। उसकी आँखें नशे में बोझिल हैं। मैं उसी चट्टान पर अधलेटा हो गया। शाम पहाड़ों पर उतर चुकी है और आसपास के सभी टापरों में चूल्हा सुलग गया था। माहौल में महुए की कच्ची शराब की गंध फैलने लगी है। दूर-दूर तक नंगे ऊँचे पहाड़ और इन्हीं पहाड़ों पर बेतरतीब खेत और प्रत्येक पहाड़ी खेत पर एक-एक टापरा। शाम अपनी सामर्थ्य से अधिक अँधेरा उठा लाई थी। और पहली ठोकर खाते ही पहाड़ों पर अँधेरा बिखर गया है। पहाड़ के सीने से निकले पेड़ों पर से अँधेरा धीरे-धीरे रिस रहा है। सागौन के पेड़ों के पत्ते धूल से अटे हैं और उनका हरापन अब नजर नहीं आता है, कितनी अजीब बात है। इस क्षेत्र के हिस्से में धूल-ही-धूल है। सड़कें पक्की नहीं हो पाईं, रास्तों पर भी धूल है। इन आदिवासियों के जिस्म पर भी धूल है। टपरों पर भी धूल है। भाग्य भी धूल से भरा है। व्यवस्था के कमीनेपन को भाग्य के खाते में डालने की अपनी चालाकी पर मैं सहसा आश्चर्य करने लगा। बरसों से चल रहे राहत कार्य भी इस धूल को नहीं हटा पा रहे हैं, उल्टे इनकी आँखों में धूल झोंकी जा रही है।
मैंने गरदन उठाकर देखा, टपरे में इकलौते दरवाजे के ऊपर एक नींबू रस्सी से बाँधकर लटकाया है। शुभ के स्वागत के लिए, अशुभ और दुर्भाग्य से सुरक्षा के लिए। नींबू सूखकर काला पड़ चुका है। मैंने सोचा, दरअसल रस्सी से नींबू नहीं, एक सुरक्षाबोध लटकाया है अपने अदृश्य शत्रु के खिलाफ इनके पास सिर्फ नींबू है। काला कमजोर नींबू। लेकिन आपदाएँ अदृश्य दरवाजे से दाखिल होकर उनके जीवन का एक हिस्सा हो चुकी हैं। ये कहाँ गुहार लगाएँ? सभ्य संसार की व्यवस्था में इनके लिए जगह नहीं है। उस व्यवस्था में इन्हें विपत्ति समझकर लोग परे हो जाते हैं। व्यवस्था ने अपने विशाल दरवाजे पर ढेरों नींबू लटका रखे हैं। जो न काले पड़ते हैं और न सूखते हैं, बल्कि प्रकृति के नींबू से ज्यादा कठोर और असरकारक होते हैं, मुझे लगा मेरे भीतर भी कोई चीज धीरे-धीरे सुलग रही है या फिर मैं भावुकता और बौद्धिक बहक की कगार पर डगमगा रह हूँ, बल्कि इस तरह खुद को कहीं दिलासा भी देना चाहता हूँ।
घर गए कई साल हो गए। जिस दिन नियुक्ति पत्र मिला था सोचा भी नहीं था, कि यह इलाका कल्पना से भी ज्यादा बीहड़ होगा और कुछ ही समय में मैं इसका एक ढीठ हिस्सा हो जाऊँगा। साथी के नाम पर मिला यहाँ एक सहकर्मी, हमउम्र विजय। शुरू में मुझे इस आदमी से बड़ी कोफ्त हुई थी। यह आदमी, जो सुबह उठते ही कुल्ला करने के बाद महुए की कच्ची शराब पीना शुरू कर देता है।
सोचते हुए मुस्करा कर मैंने आँखें बंद कर लीं, फिर याद आया, सुबह जल्दी काम निबटाकर पूरे पंद्रह कि.मी. पैदल चलकर वापस दफ्तर पहुँचना है और ‘प्रोग्रेस-पिरोर्ट’ देना है। मुस्कराहट फिर होंठों पर लेट गई। कितनी अजीब बात है। हर महीने हम लोग प्रोगेस-रिपोर्ट भेजते हैं। सालों हो गए। शायद इसके पहले दूसरे भेजते होंगे। लेकिन प्रोग्रेस कहाँ हुई? इन आदिवासियों के टपरों के कवेलुओं का रंग तक नहीं बदला। जो बैल इनको कर्ज में मिले हैं वह खरीदकर हमारा दफ्तर देता हे। ढाई हजार के बैलों में बी.डी.ओ. से लगाकर जाने किन-किन का हिस्सा होता है। और ये मरियल बैल पहाड़ी खेतों में कुछ ही दिनों में मालिक के साथ हाँफने लगते हैं। और फिर बैल और भैंस की योजना का लाभ यह लोग कहाँ उठा रहे हैं? मुझे मालूम है, यहाँ इस पूरे इलाके में कई साहूकारों ने, कई अफसरों ने बैंक से अनुदान में अपने नौकरों के नाम से भैंस और बैल ले रखे हैं। इन आदिवासियों के लिए फार्म पर अँगूठा लगाना और खेत में पौधा लगाना दोनों ही सहज चीजें हैं, लेकिन कौन रोके इन चीजों को। कौन बताए ऊपर, कि बैल और भैंस आदिवासी को न मिलकर उन खेतिहरों को मिल रहे हैं, जिनके पास कई एकड़ जमीन है। वे सुविधा संपन्न हैं। और ऊपर भी कौन बैठा है? कौन सुनेगा? मैंने सिर पीछे चट्टान पर टिका दिया। फिर करवट लेकर देखा, विजय उठकर बैठ गया है। मैं भी उठकर उसके पास चला गया। एक बोतल खत्म हो गई थी, दूसरी भट्टी से हटकर अब ठंडी हो रही है। जल्दी ठंडी हो जाए इसलिए एक आदमी बोतल को पकड़कर नाले के उथले पानी में बोतल डुबाकर बैठा है।
– “ला, देख तो ठंडी हो गई होगी?” विजय चिल्लाकर बोला। बोतल पानी में डुबाकर बैठा आदमी वहीं से हाँक लगाकर बोला, – “बस, जरीक वार छे।” (बस थोड़ी देर है।) वह दोनों हाथों से सिर थामकर बैठ गया।
– “पार्टनर, दो साल हो गए घर नहीं गया हूँ।” मैंने उसके कंधे पर सिर टिकाकर कहा, – “यार मुझे तो लगता है, मैं जन्म से यहीं हूँ। अब मैं भी अपने आप को आदिवासी समझने लगा हूँ। अब तू ही बता, शहरी आदमी और हममें कितने फासले हो गए हैं और इन आदिवासियों से हमारी जिंदगी कितनी मेल खाने लगी है। स्साले हम बम्मन, बनिए की औलादें हैं। दारू, मुर्गा शुरू कर बैठे हैं। सूखी खटिया पर सोना, मीलों पैदल चलने की आदत, यहाँ की बोली का आदत में शुमार, लेकिन… “मैं बोलते-बोलते रुक गया। सहसा कोई चीज भीतर चुभने लगी। मैं बोला, – “इनकी तकलीफें हमारी नहीं हो पाईं।”
वह सहसा मेरी ओर देखने लगा, – “दरअसल हम लोग सिर्फ भावुक होकर रह जाते हैं। इन सब चीजों के लिए भावुकता की जरूरत नहीं होती है।” वह मेरे कंधे पर हाथ धरकर बोला, – “इसीलिए इधर सारी प्रगति कागजी हुई है। इनकी तकलीफें हमारी क्यों हों? ऐसा नहीं हो कि ये तकलीफें ही नहीं रहें। तुम सिर्फ कंधे बदलने की बातें क्यों करते हो?” उसकी आवाज में महुए की तल्खी उतर आई। मैं खामोश हो गया। उसने बात का गलत सिरा पकड़ा था। तभी बोतल आ गई। उसने हाथ लगाकर देखा, बोतल ठंडी हो गई है। उसने कप में डालना शुरू कर दी। – “ले यार, शुरू कर। क्या रखा इन बातों में।”
मैंने कप उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, – “और इन आदिवासियों को भी कहाँ खबर है कि ये तकलीफों में हैं। उन्हें क्या मालूम कि इनके घर, बैल, बकरी, भैंस या बैलगाड़ी जो बैंक से कर्ज में मिली हैं। इन बैल, भैंस के बदले किन-किन लोगों के घर विदेशी साड़ियाँ, टेपरिकार्डर और टी.वी. पहुँच गए। इन्हें क्या मालूम इस गाँव में बन रही सड़क के पैर निकल आए हैं और शहर पहुँच कर मकान की शक्ल में किसी के नाम से तैयार हो चुके हैं।” कहते हुए मन में कड़वाहट भर गई। फिर मुँह बिचकाकर कहा, – “छोड़ यार सब वाहियात बातें हैं” कहकर मैंने एक ही घूँट में कप खाली करके जमीन पर रख दिया। काफी देर पानी में रहने के बावजूद शराब अभी कुनकुनी है। लेकिन हम इसे आदत में ढाल चुके हैं। ताजा शराब बदन निढाल किए दे रही है। मैंने हथेली पर चेहरा टिका लिया और सामने बैठे आदिवासी को घूरने लगा। शहर में होता यह आदमी तो गली-मुहल्ले या शहर में चर्चा का विषय होता। अस्सी की उम्र, काला स्याह बदन। चार पत्नियों का पति और कई बच्चों का बाप। अब भी जंगल से लकड़ी काटकर लाता है। पहाड़ की तरह उसकी काली सख्त पीठ जाने कितने अदृश्य बोझ उठाए हुए है। इन पहाड़ों पर चढ़कर जाने कितने अफसर ऊँचाई हासिल करते चले गए। जाने कितने साहूकारों के घोड़ों की टापों से यह पहाड़ छिलते चले गए होंगे। कुछ आदिवासियों को मात्र कुछ सौ रुपए के बदले वर्षों से इन बगैर ताज के राजाओं की गुलामी करनी पड़ रही है। यह सब तमाम अफसरों से लेकर साहूकारों तक के लिए सामान्य बात है। बल्कि अपने घर, गाँव आए मेहमानों को या अफसरों को इनकी अद्भुत श्रमशक्ति के विभिन्न किस्से सुनाते हैं। कितनी अजीब बात है कि दस किलोमीटर दूर पहाड़ों से उतरकर मात्र पचास पैसे के नमक खरीदने आए आदिवासी की धावक शक्ति की तारीफ करके लोग खुश हो जाते हैं कि लो, हमारे पास भी प्रदर्शन के लिए कुछ अद्भुत है।
कौन इन्हें बताए कि श्रम का यह अवमूल्यन आदिवासियों की पारंपरिक विवशता नहीं, अपितु सुविधाओं के जंगल में अपने मचान को सुरक्षित रखने का हमारा आदिम उपाय है। परंपरा के आकाश के नीचे इन काले पहाड़ों को छोड़ कर हम आसानी से विकास के आँकड़ों पर सवार होकर सभ्य संसार की सुरंग में दाखिल हो जाते हैं। इस कठिन श्रम की पूँजी को पहाड़ी नियति के झोले में डालकर ये लोग कौड़ियों के मोल लुटा देते हैं और इस तरह एक आसान सौदे के हासिल के लिए हम अपने घृणित चालाकी पर पुलकित होते रहते हैं। देह का पहाड़ हो जाना ऊँचाई के गर्व भरे सुख का हासिल नहीं है, बल्कि देह की ऊँचाई से नीचे झाँककर भय की नदी में छलाँग लगाने से पहले की आदिम नृत्य मुद्रा है, जो देखने वालों को आश्चर्य से भर देती है और खुद को अनगिनत दुखों से, क्योंकि विकास के लिए पहाड़ों का लगातार कटते जाना तय है और इसीलिए ये लोग लगातार पहाड़ हो रहे हैं। मैं अपलक उसे देखता रहा। शराब की बहक मेरी सोच को और दूर तक ले जाती, लेकिन मैंने अपनी पलकों को झपकाया गोया ऐसा करके अपनी बौद्धिक बहक को काबू में कर लूँगा। मैं कुछ कहना चाहता था फिर रुक गया। विजय फिर इन सबको कोरी भावुकता में धकेल देगा। मैं फिर उस आदिवासी को घूरने लगा जो अपनी ओर देखता पाकर सहसा बोला, – “डुबी कहाँ लगुन जड़ी जासे?” (तो भैंस कब तक मिल जाएगी?) उसके चेहरे पर बहुत कठिन मायूसी है।
– “हम जाते ही कार्रवाई करेंगे। भैंस तो समझ मिल गई।” मेरे बोलने से पहले ही विजय ठहाका लगाकर हँस दिया और बोला, – “तेरी भैंस की फिक्र तो हमारे बी.डी.ओ. साहब को तेरे से ज्यादा है। अब की गर्मियों में उनको अपनी बेटी की शादी करनी है।” कहकर वह फिर ठहाका लगाकर हँसने लगा। टपरे के पास मात्र एक ढिबरी टिमटिमा रही है। खामोश जंगल में ठहाका देर तक थरथराता रहा। फिर वह कप में शराब डालते हुए बोला, – “पार्टनर उधर वह आखिरी का टपरा है न? बहुत टाप की चीज है, उधर।”
मैंने इनकार करते हुए कहा, – “तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया या ज्यादा चढ़ गई है? ये लोग काटकर फेंक देंगे तो बहुत दिनों तक लाश भी नहीं मिलेगी। और फिर इन भोले-भाले आदिवासियों के साथ, इनके बीच रहकर इनकी अबोध संस्कृति का इस तरह लाभ उठाना ठीक है क्या? मेरा जमीर तो गवाही नहीं देता।” कहकर मैंने अपना कप फिर से एक ही साँस में खाली कर दिया। वह उठकर मेरे करीब आ गया और आँखों में झाँककर बोला, – “क्या सचमुच तू इसी नैतिकता की वजह से इनकार कर रहा है?” और मेरी झुँझलाहट से पहले ही वह ठहाका लगाकर हँस दिया फिर बोला, – “मैं चलूँ, वह नाले पर मेरा इंतजार कर रही होगी।” मै सामने बैठे उन आदिवासियों को घूरने लगा। गठीले, सख्त काले नंगे बदन। लेकिन इन मासूम चेहरों के पीछे छुपी, परिणामों से बेखबर अबोध हिंसक, प्रवृत्तियों को मैं भली-भाँति जानता हूँ। नुकीले तीर और चमकते हुए फालिए की कल्पना से ही मैं सिहर गया और उनके चेहरे से हटाकर मैंने नजरें जंगल में दूर पेड़ों पर उछाल दीं।
सचमुच, भय और विवशता कहाँ और किस तरह आदमी को नैतिकता से जोड़ देती है। हमारे यही भय और विवशता इन आदिवासियों के लिए सुरक्षा कवच है। मैंने कप फिर से भर लिया और धीरे-धीरे पीने लगा। बढ़ता हुआ अँधेरा और तेज कच्ची शराब का असर, बदन निढाल होने लगा। नदी किनारे की गीली रेत में लेटी हुई मादा देह की आकृति मेरे जेहन में उतरने लगी। ये औरतें भी नदी हो रही हैं। लेकिन इन औरतों की नियति इस क्षेत्र की नदियों से ठीक विपरीत है। इन नदियों पर पुल नहीं है। और न कभी बन पाएँगे। लेकिन इन शरीरों पर ढेरों पुल बनते हैं। जिनसे गुजरकर आदमी देह सुख के बीहड़ में उतर जाता है, किसी डकैत की तरह। दूर टपरे में मुर्गा पक रहा है। गोश्त की खुशबू, महुए की शराब की गंध में मिलकर एक आदिम रोमांच से भर रही है। मैंने चट्टान पर सिर टिकाकर नींद को टटोलना चाहा। लेकिन टपरे से उठने वाली भुने गोश्त की गंध मुझे नींद की पालकी से खींचकर शराब की गोद में धकेल देती है। महुए की शराब किसी फिल्मी वेश्या की भाँति अपने निकट खींचकर एक नाटकीय तसल्ली से भर देती है। जिसके सीने पर सिर रखते हुए बराबर नाटकीयता का आभास होता रहता है, लेकिन चाह कर भी फिलहाल उससे मुक्त नहीं हुआ जा सकता है। शराब के ही कंधों पर सिर रखकर पहाड़ों पर इस पहाड़-सी काली रात के उस पार जाया जा सकता है।
दूर के टपरे अँधेरे में धब्बों की शक्ल में नजर आ रहे हैं और नजदीक बैठे आदिवासी उस अँधेरे में खड़े पेड़ों में घालमेल होते नजर आए। मुझे याद आया, पिछले दिनों भोपाल से कोई अफसर आए थे। साँझ ढलने पर उन्हें ये टपरे और आदिवासी काले कैनवास पर फैले गहरे धब्बों की भाँति किसी फ्रांसिसी पेंटिंग की याद दिला रहे थे। नंगे बदन आदिवासी, भूरे, तने पेड़ और सूखे खेत उन्हें कविता का-सा मजा दे रहे थे। चारों ओर फैले पहाड़, हल्के अँधेरे में उन्हें कला फिल्म का दृश्य-सा लग रहा था। एक अशालीन शर्मिन्दगी से मेरा मन भर गया था। आदिवासियों की फटेहाली से उन लोगों के मन में सौंदर्यबोध जाग रहा था। सभ्यता के विकास के लंबे-चौड़े भावों को कुचलता हमोर समय का सच हमारे सामने निर्वस्त्र बैठा है। लेकिन हम इसे भी आसानी से परंपरा और नियति की टोकरी में डाल देते हैं। जबकि यह परंपरा की गति नहीं, हमारे समय के सच की सबसे बड़ी अश्लील दुर्घटना है। जो किसी इतिहास में दर्ज नहीं हो पाई। लेकिन इनकी लंबी-चौड़ी काली देह की स्लेट पर यह इबारत स्पष्ट उभर आई है। इनकी देह का नंगापन हमारे सामाजिक मूल्यों की निर्वसन देह की एक्सरे कॉपी है। सोच को जैसे पंख लग गए। मैंने सिर को झटका दिया। सोचा, शराब पीने के बाद मेरी सोच की दिशा अक्सर बहक जाती है। कच्ची शराब मेरे भीतर की दबी बौद्धिकता को उकसाती है।
फिर एकाएक खयाल आया, कहीं मैं इस तरह अपने अपराधबोध से मुक्त होने की कोशिश तो नहीं करता हूँ? अंततः मैं भी इसी व्यवस्था का एक हिस्सा हूँ। मैंने कप फिर भर लिया। उठकर पास की चट्टान पर बैठ गया। नशे के अतिरेक में गरदन झूलने लगी। मैंने सिर को आगे घुटनों पर टिका लिया। आहट हुई। आँखें मिचमिचाकर देखा, विजय है। नजदीक आकर बैठ गया। उसके चेहरे पर सहजता है। पास बैठे आदिवासी ने उसे भी कप भर कर ला दिया। मैंने एक घूँट लिया और कप टेढ़ी-मेढ़ी जमीन पर सावधानी से रख दिया। फिर विजय से कहा, – “विजय, अगले सप्ताह दिल्ली से दल आ रहा है। आई.आर,डी.पी. योजना से संबंधित।” उसने बुरा-सा मुँह बनाया गोया पूरा कप एक ही साँस में पी गया हो। फिर जमीन पर अधलेटा सा होकर बोला, – “चूतिए हैं स्साले। चले आते हैं। इनको क्या? पुट्ठे के नीचे सरकारी जीप है। गले में कैमरा लटका है थर्मस में कॉफी है। चल देते हैं, दिल्ली, भोपाल से। बगल में खुद की या किसी की भी बीवी और पीछे जीप में योजनाओं की फाइलों के बस्ते से लदा बाबू बैठा लाते हैं। पहले स्साले, खजुराहो, साँची, फतेहपुरा सीकरी या मांडू जाते थे, अब झाबुआ, बस्तर चले आते हैं। सरकारी दौरे को पर्यटन में बदलने का आधुनिकीकरण हो गया है। यहाँ आकर साला कोई भी योजना के बारे में बात नहीं करता। सूखे से चिंतित नहीं होता। बौद्धिकता की उल्टियाँ करने लग जाता है, आदिवासी संस्कृति की फिक्र होने लगती है।” कहते-कहते वह हाँफने लगा। शराब और गुस्से के मिले-जुले प्रभाव से उसका चेहरा तमतमाने लगा। मैं उसका कंधा पकड़ कर बोला, – “छोड़ यार, सब दूर यही है, पूरा हिन्दुस्तान, झाबुआ बना हुआ है। तुम और मैं क्या कर पा रहे हैं यहाँ? फर्क इतना है कि हमारी धड़ के नीचे जीप नहीं है, पैर लटके हैं, वरना हम भी उसी लाइन में खड़े हैं।” बदले में वह कुछ बोलता हुआ रुक गया और फिर उठकर टपरे में चला गया और थोड़ी देर बाद बाहर निकला, उसके हाथ में चीनी की एक प्लेट है। उसमें मुर्गे के मसालेदार गरम-गरम टुकड़े हैं। प्लेट उसने वहीं जमीन पर रख दी, और टुकड़ा उठाकर उसे छिछोड़ने लगा।
मैंने पास बैठे आदिवासी की ओर देखा। वह निस्पृह बैठा है। पहाड़ों के जंगल की सारी सघनता उसके चेहरे पर फैल गई है। मुझे लगा, जंगलों में रहते हुए आदमी जिंदगी में जो मिलता है उसी को बोते चलता है। दुख जलाता है, दुख पकाता है। दुखों को ही खाता है। और फिर दुखों की उल्टियाँ करता है। बी.डी.ओ. अक्सर कहता है, अपनी ऐसी स्थिति से ये आदिवासी संतुष्ट हैं। पविर्तन की कोई चाह इनके भीतर नहीं है। वरना अभी तक कोई परिवर्तन नहीं होता क्या? सरकार कितनी कोशिश कर रही? मैंने सोचा, सरकार? यानी बी.डी.ओ. साहब। मैं बी.डी.ओ. साहब की कोशिशें जानता हूँ ये आदिवासी अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं है। बल्कि अपनी स्थिति के लिए जिम्मेदार को पहचान नहीं पा रहे हैं। इसे वह भाग्य पर छोड़ देते हैं और भाग्य साहूकार की भाँति इनकी जिंदगी में आता है। छोटे-छोटे सुख ब्याज की कीमत पर छीन लेता है। और बड़े सुख का सिर्फ लालच देता है। इतनी सारी वसूली सिर्फ आदिवासी होने के कर्ज के नाम पर। पिछले कई महीनों से वह दफ्तर के चक्कर काट रहा है। दस बजे दफ्तर खुलते-न-खुलते वह बाहर पड़े बेंच पर आकर बैठ जाता है। शाम ढले, ‘कल आना’ के आश्वसन पर चल देता है। सुबह फिर मैं जब दफ्तर आता हूँ तो उसी बेंच पर उसे बैठे देखता हूँ, कई बार मुझे लगा, यह घर जाता ही नहीं होगा। इसी तरह बेंच पर रात भर से बैठा है, बल्कि सदियों से इसी दफ्तर के बाहर बेंच पर बैठा है। किससे कहे? इस गाँव में और कौन है?
गाँव बहुत छोटा है। हमारा दफ्तर। एक स्कूल, एक बैंक, एक छोटा-सा पोस्ट ऑफिस, पुलिस चौकी बस। तहसील सात किलोमीटर दूर। जिला मुख्यालय सैकड़ों किलोमीटर दूर। उसके लिए जो कुछ है हम ही हैं। यही गाँव है। वह फार्म जो हमारे दफ्तर में जिले से सैकड़ों की तादाद में मुफ्त में आते हैं, बी.डी.ओ. के बच्चे उसका रॉकेटनुमा खिलौना बनाकर उड़ाते हैं। लेकिन इन लोगों के लिए वह दुर्लभ है। बाबुओं की खुशामद करके फार्म मिल भी जाए तो सबसे कठिन है उसे भरना। जिनके लिए दस्तखत करना पहाड़ चढ़ने से ज्यादा कठिन हो, फार्म भरने के नाम पर तो वह घिघियाने लगते हैं। फिर स्कूल मास्टर या दफ्तर का बाबू दो, चार या दस रुपए में फार्म भरकर देता है। और फिर उसे बैल, भैंस या बैलगाड़ी के लिए शुरू करना होता है, दफ्तर के चक्कर काटना और सबसे बड़ी त्रासदी तो यह है कि हम लोगों के दफ्तर के लिए जिले से टारगेट तय होता है। मार्च के पहले तक, इतने बैल के केस, इतने भैंस के, इतने बैलगाड़ी के वगैरह, वगैरह…
जल्दी तो हम लोगों को रहती है। लेकिन शातिर शहरीपन, अनुभवी दफ्तरी काइयाँपन इसको कभी चेहरे पर प्रकट नहीं होने देता। एक मोटी रकम के बदले उपकरा की भाँति हम उन्हें लोन देते हैं। जो उनका हक होता है। सहसा मैं ठहाका लगाकर हँस दिया। विजय चौंक पड़ा, उठकर बैठ गया। विजय ने बूढ़े को दिलासा दिया कि, – “चढ़ गई है। कोई खास बात नहीं है।” बूढ़ा मेरे सामने उकड़ू होकर बैठ गया। मैंने चाहा, कह दूँ ठीक से फैलकर बैठ जाओ। लेकिन कह नहीं पाया। जानता हूँ, वह फिर भी इसी तरह उकड़ू ही बैठेगा। हालाँकि वह गिरेगा नहीं। उसके गंदे टेढ़े-मेढ़े पैर जमीन से चिपके हुए हैं। उन्हें सहसा जमीन से अलग करना मुश्किल है।
वह खामोश अँधेरी आँखों से मेरी ओर देख रहा है। मैंने नजरें उस पर से हटा लीं। सहज ही कुछ बोलने भर के लिए बोला, – “तेरा फार्म तैयार हो गया? फार्म भर लिया?”
– “हो” (हाँ) वह स्वीकृति में बोला।
– “किसने भरके दिया? माट्साब ने?” मैंने दोबारा पूछा।
– “नोहि, हमारा गाऊन पुर्यो छे। हींवींज सेर कोथो भणिन आवलो।” (नहीं, हमारे गाँव का लड़का है, अभी शहर से पढ़ाई पूरी करके लौटा है।) वह बचकाने उत्साह में बोला। फिर वहीं से उसने टपरे में किसी को पुकारा। तौलिया लपेटे एक लड़का बाहर आया और नजदीक आकर उसी तरह उकड़ू होकर बैठ गया। प्रचलित पिछड़ेपन की किंवदंतियों की वजह से शहर में हुई उपेक्षा की मार से वह अछूता नहीं बचा है। शहर के प्रति आतंक उसके चेहरे की कालिमा में दब नहीं पा रहा है। किसी विश्वविद्यालय की एकाध डिग्री का तौलिया भी उस आतंक को साफ नहीं कर पा रहा है।
– “पढ़ रहे हो?” मैंने एक फिजूल-सा प्रश्न किया।
– “हाँ।” वह थोड़ा ठहरकर बोला, – “लेकिन, अब पढ़ाई पूरी हो गई है। बी.ए. कर लिया है।”
– “यहीं-कहीं नौकरी क्यों नहीं करते। गाँव में या आसपास कहीं?” इतना कहकर मुझे तुरंत अपनी मूर्खता का अहसास भी हो गया। वह झिझककर बोला, – “नौकरी अपने हाथ में कहाँ? जहाँ मिले वहीं जाएँगे।” उसके चेहरे पर एक संकोच उभर आया। वह बातचीत में बड़ी असुविधा महसूस कर रहा था। मैंने एक लंबी साँस ली और नई बोतल की शराब कप में डालने लगा। मेरे आग्रह पर संकुचित होते हुए उस लड़के ने भी कप थाम लिया। लेकिन अब वह जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया। उसके पैर ज्यादा देर तक जमीन से चिपके नहीं रह पाए। उखड़ गए। बूढ़ा मुग्ध होकर लड़के को देख रहा है। उसकी आँखों में तरलता उतर आई। गोया आँखों से पी रहा हो।
कुछ देर बाद बूढ़ा उठा और भीतर चला गया। लौटकर आया तो बताया, मुर्गा तैयार है। मैंने पलटकर देखा, विजय चट्टान पर चित्त पड़ा है। खाना तैयार होने की बात सुनकर उठकर बैठ गया। खाना वहीं खटिया पर बैठकर खाया गया। उसके बाद बूढ़ा पत्तो में तमाखू लपेटकर बीड़ी बनाने लगा। बीड़ी का एक कश लगाया तो मुझे मस्तिष्क सुन्न होता नजर आया। सस्ती तेज तमाखू, घर में उगाए पत्ते और ऊपर से महुए की शराब का नशा। मैं खटिया पर लेट गया। धुआँ फैलने लगा।
चलने को हुए तो बूढ़ा फिर नजदीक आ गया। बोला, – “हूँ डुबी पासूँ कि?” (मुझे भैंस मिल जाएगी न?) उसने स्वर में घिसट आई याचना को रोकने की कोई कोशिश नहीं की थी। मैंने स्वीकृति में गरदन हिलाकर उसे आश्वस्त कर दिया मैं उसे कैसे बताता कि यह भैंस उसका हक है। जो उसे मिलना है। लेकिन फिर चुप रह गया। नशा तारी हो रहा है। और इसीलिए चेहरे पर उभरती शर्मिन्दगी मैं समेट ले गया।
घर लौटकर हम दोनों ढेर हो गए। दूसरे दिन तो दोपहर तक सोते रहे। दो दिन दफ्तर भी नहीं गए। सुदूर आदिवासी इलाके में अवकाश लेने जैसी कोई औपचारिकता तो होती नहीं है।
दो दिन बाद जब हम दोनों दफ्तर जाने लगे तो मुझे दफ्तर के दरवाजे के पास बेंच पर वही बूढ़ा नजर आया। मैं चौंक पड़ा। मैंने कहा, – “तुम्हारा फार्म तो भर दिया गया है। केस स्वीकृत भी है।” वह बूढ़ा चौंक पड़ा। बाहर निकलते विजय को मैंने रोका तो विजय ने बताया, यह वह बूढ़ा नहीं है। वह दूसरा था। मैं अचकचा गया। मुझे सारे आदिवासी एक जैसे लगते हैं। वही कद-काठी। वही काला रंग। कंधे पर धनुष-बाण। जिस्म पर एक लंगोटी। मैंने उसक कंधा थपथपाया और आगे बढ़ने लगा तो बूढ़ा उठकर मेरे करीब आ गया।
– “मारे फण फरम भरवानु छे। डूबी चइसे।” (मुझे फार्म भरना है। भैंस चाहिए।) उसके चेहरे पर बहुत गीली याचना है। मैंने बहुत जतन से खुद को उस गीलेपन से बचाया।
– “लेकिन तुम्हारे गाँव में तो वह लड़का है। पढ़ा-लिखा। उसे क्यों नहीं कहा? वह सब कुछ कर देता।” मैंने उसे याद दिलाया।
– “साब, पोलो चालि गियो। पोला साबुन काम कार्यो। काहुन फारम भोर्यो, काहला साथ बैंक गुयो। काहला कुठे पुलिस ठेसन। हूँ रोहि गियो। फारम नी भोरायो। पण पोलो काहला धाढ़ा पाछो आवसे। आवसेजू। पोलो बोली ने गुइलो छे।” (साब, वह तो चला गया, उसने सबके काम किए। किसी का फार्म भरा, किसी के साथ बैंक गया, किसे के साथ पुलिस चौकी, मैं चूक गया, फार्म नहीं भरवा पाया। लेकिन साब, वह एक दिन लौटेगा। वह जरूर आएगा। बोलकर गया है।) कहकर वह एक अनजाने उत्साह से भर गया। मैं उससे निगाहें चुराकर सोचने लगा। जंगल का जंगलीपन धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा है, लेकिन सरकार दूसरे सिरे से चिंतित है। वह प्रौढ़ शालाओं के बचकाने उत्साह के दम पर आदिम प्रवृत्तियों के परिवर्तन के सपने देख रही है। उन्हें राजधानी में बैठे हुए यह नहीं मालूम कि प्रौढ़ शालाएँ अपने शैशव काल में ही दम तोड़ चुकी हैं। गाँव में प्रौढ़ शाला सुचारु रूप से चल रही है। इस बात का प्रमाण-पत्र भी सरपंच शिक्षा विभाग को अँगूठा लगाकर देता है। कितनी अजीब बात है कि एक पूरा समूदाय शिक्षा विभाग को अँगूठा दिखा रहा है, लेकिन शिक्षा विभाग अँगूठा चूस रहा है।
मैं आहिस्ता से वापस पलटा तब तक विजय लौट आया। मैंने उसे बताया, – “वह लड़का शहर चला गया। लौटकर आने के लिए। इस बूढ़े का फार्म भरने के लिए। इसे उम्मीद और विश्वास है।” विजय ने मेरी ओर देखा। फिर हम दोनों ने एक-दूसरे पर से अपनी नजरें उठा लीं। मैंने बूढ़े को स्कूल मास्टर के घर भेज दिया। और हम दोनों सड़क पर आ गए। पान की दुकान पर आकर भी हम लोगों की खामोशी नहीं टूटी। सिगरेट खरीदी। सुलगाकर हम दोनों ने एक-दूसरे की ओर देखा, फिर ऐसे मुस्कराए जैसे आज ही मुलाकात हो रही हो। दोनों ने तय किया घर चला जाए। सहज होने के लिए हम दोनों के पास एक ही उपाय है। कच्ची शराब। मुझे मालूम है। स्कूल मास्टर न स्कूल में होगा न घर। पोस्ट ऑफिस भी बंद होगा। वहाँ का इकलौता कर्मचारी डाक लेने पास के गाँव गया होगा। दफ्तर से हटकर पीछे घर की ओर जाने के लिए पलटे तो मैंने देखा, बूढ़ा, बेंच पर बैठा है। मैंने सोचा, अब कभी कोई कला प्रेमी अफसर इधर आया तो कहूँगा, इन पाषाण प्रतिमाओं को देखो, सदियाँ गुजर गई इस बेंच पर बैठे हुए। एक प्रतिमा उठ जाती है तो दूसरी स्थापित हो जाती है। इस बेंच को यहाँ से कोई नहीं हटा पाता है। कोई नहीं। मैंने एक लंबी साँस ली और विजय के कंधे पर हाथ धरकर चल दिया। नुक्कड़ पर आकर गरदन उठाई तो देखा, बी.डी.ओ. साहब सब्जी वाले से नींबू खरीद रहे हैं।
Download PDF (पहाड़ों पर रात )
पहाड़ों पर रात – Pahadon Par Raat