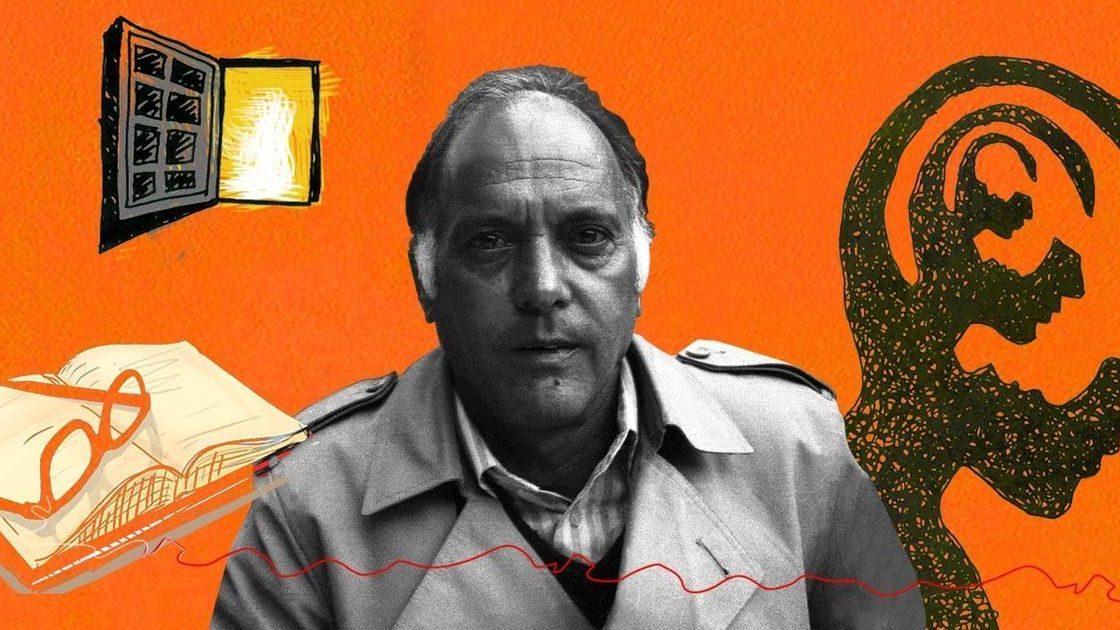कल ही बड़े का खत आया था। वह चार दिन के लिए पत्नी और बच्ची के साथ आ रहा है। माँ अनपढ़। लेकिन पोस्टकार्ड पर लिखी लाइनों से ही पहचान गई थी कि खत संतोष का है। सिर्फ वही है जो सारा पोस्टकार्ड जाया कर दिया करता है। पति बाजार से लौटे तो कहा था – ‘देखना, संतोष का खत है न! क्या लिखा है? सारे आ रहे हैं न?’
एक साथ बहुत सारे सवाल पूछने की आदत बहुत पुरानी है, अभी भी गई नहीं। जब-जब बड़े का कभी-कभार कोई खत आ जाता है वह यही बँधे-बँधाए सवाल पूछा करती है। लेकिन बड़ा आता-जाता बहुत कम है। मास्टरजी को खत का मजमून बताने के बाद हमेशा उसके आहत होने को झेलना पड़ता है। लेकिन लड़के के आने की खबर उसे दे कर उनके दिल में भी छोटी-सी खुशी कूद गई थी। वह बाहर के दिखावे और टीम-टाम में खुद भी विश्वास नहीं करते। लड़के के साल-साल तक न आने का कहीं गहरे में बुरा नहीं मानते। लेकिन यह जरूरी तो नहीं कि हर सवाल का ठीक जवाब किसी को खुशी भी दे। एक बार देर तक न आने की बात की थी तो लड़के ने समझाया का कि बिना वजह से कहीं आना-जाना उसे फिजूल लगता है। कभी कोई बात हुई है, काम पड़ा है, जरूरत आ खड़ी हुई है, तो वह हमेशा क्या पहुँचा नहीं?
कोई जरूरत आ पड़ने पर पहुँचने की बात उन्हें सही लग गई थी। नौकरी से रिटायर होने के बाद, चालीस रुपए की पेंशन मिलने पर, छोटी लड़की की शादी करने पर जरूरतें पड़ती ही रही हैं और जैसे-तैसे बड़ा पहुँचा है। जो हो सका था, किया भी।
पत्नी को भी समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वह ठहरी अनपढ़। आज के आदमी की तरह वह सूखे तर्क तथा कारण के आधार पर न जीती है, न बात करती है। उसने बिफर कर कहा था कि क्या अपने लोग अब सिर्फ काम पड़ने पर ही मिलते हैं? प्यार भी कुछ होता है न? वह पढ़-लिख कर कितना सूखा हो गया है।
लड़के के पढ़ने का विशेष श्रेय माँ को जाता है। सारे विरोध होने के बावजूद कि कॉलेज का खर्चा कौन देगा; और बच्चे भी हैं, उसने पढ़ाई के बारे में डट कर लड़के का साथ दिया था। लड़का पढ़ा, उसकी अच्छी नौकरी लगी। और तब तो उसके दिल में ठंड पड़ जाया करती है जब लड़का अब भी दूसरों के सामने स्वीकार किया करता है कि उसको पढ़ानेवाली, बनानेवाली, उसकी माँ ही हैं।
लेकिन एक दुख उसे हमेशा सताता रहा है। नौकरी बाहर के शहर में लगने पर लड़के का घर आना-जाना कम हो गया। कुँआरा था तो कोई बात न थी। वही पुरानी आदत। अब आस-पड़ोस के लोग लड़के, बहू और बच्ची के न आने की बात पूछते हैं तो वह अपमानित होती है। लोग तो कमीने हैं। यही सोचते होंगे न कि शायद अब लड़के और उसकी घरवाली से बनती नहीं।
इसलिए लड़के के आने की बात पर उसने पति से फिर पूछा था – ‘किस तारीख को आ रहा है? कितने दिन रहेंगे? पता नहीं कपड़े भी साथ लाते हैं कि नहीं। दोनों लापरवाह हैं। मीनू के बारे में कुछ नहीं लिखा? मुझे याद करती है न…’
मास्टरजी ने सारे सवाल सुने, जरूरी सवाल का चुनाव किया और बताया –
‘कल सुबह आएँगे। चार-पाँच दिन रहेंगे।’
दादी को मीनू के आने की खुशी लड़के के आने से कही ज्यादा है। तीन साल की उम्र में कितनी बातें करती है। वह मीनू से मिलने महीने मे एकाध बार जा आया करती है। लड़का और बहू तो बस चुप रहते हैं। उन्हे आपस में बहुत बातें करते कभी नहीं देखा-सुना। उससे क्या बोलेंगे? पहले मिलने जाती थी तो सुबह जा कर शाम को लौट आया करती थी। वहाँ तो दिल तंग पड़ जाता है। लेकिन जब से मीनू ने बोलना शुरू किया है, महीने में दो-तीन दिन लड़के के यहाँ लगा आती है। कितना बोलती है। मरजानी बिलकुल मेरे ऊपर गई है। उसे अपने बहुत बोलने की आदत का पता है, जिसे मास्टरजी बड़-बड़ करना कहते हैं। वह काम करते हुए मुसकरा रही है – चलो, लड़के के घर भी बड़-बड़ करनेवाली पैदा हो गई। कोई तो आया घर की चुप्पी तोड़नेवाला।
आज सुबह से वह झाड़-पोंछ और सफाई में लगी है। बीच-बीच में आस-पड़ोस में जा कर बता भी आती है कि बड़ा आ रहा है, पूरे चार दिन के लिए। यह सूचना देने का उसका मकसद उन्हें बताना है कि देखो हमारी ‘बनती’ है, ऐसी-वैसी कोई बात नहीं।
बाहर रिक्शा रुकने की आवाज आई। वह दौड़ कर दरवाजे के पास पहुँची। रिक्शा में रखा छोटा सूटकेस देख कर उसे विश्वास हो गया कि लोग कुछ दिन ठहरेंगे। अंदर कहीं ठंड पड़ जाती है। दौड़ कर मीनू को उठा लिया। बड़ा सूटकेस उठा कर अंदर आता है। बहू से नमस्ते होती है। हालचाल पूछने पर सिर हिला देती है। माँ को कहीं तकलीफ होती है कि वह उससे खुलती नहीं। लेकिन छोड़ो, अब मीनू जो है।
अब दादा ने मीनू को उठा लिया। महीनों बाद मिली है। इस बीच एकदम से पूरे वाक्य बोलने लग पड़ी है। दादा को बीड़ी सुलगाते देख कर पूछती है –
‘आप क्या पी रहे हैं?’
‘बीड़ी।’
अपने पिता को वह सिगरेट पीते देखती रहती है। यह बीड़ी शब्द उसके लिए नया है।
‘झूठ बोलते हो। सिगरेट है सिगरेट। हाँ।’
दादी मीनू को अपनी गोदी में खींच लेती हैं, चूमती है।
‘हाय राम! कितनी स्यानी बातें करने लग पड़ी है।’
बाहर दूधवाला आया है। माँ बर्तन उठा कर बाहर गई। फिर वहीं से आवाज दे कर पूछा – ‘काका, कितना दूध फालतू लेना है?’
संतोष पत्नी से पूछ कर माँ को बताने बाहर आता है। अभी कुछ और लोग दूध ले रहे हैं। वह माँ से कहता है – ‘जितना रोज लेती हो, ले लो।’
‘काका, हम तो एक पाव ही रोज लेते हैं। दो टैम की चाय ही तो बनानी होती है।’
लड़का यह बताते हुए कि मीनू के लिए दो किलो दूध ले लो, कहीं कसूरवार महसूस करता है। उसे लगता है माँ का चेहरा दो किलो की बात सुन कर क्षण भर के लिए बुझ गया।
उसे याद आया घर में हमेशा इतना ही दूध आता रहा है। हाँ, पाँच भाई-बहनों में जब कभी कोई बीमार पड़ता था तो उसे पीने के लिए दूध मिला करता था बतौर दवाई। तब से दूध देखते ही उसके दिल में बीमार होने का अहसास आ जाता है। अब उसके थोड़े अच्छे दिन हैं। लेकिन दूध से नफरत है। वह अपने अर्धजाग्रत मन में हिसाब भी लगाए जा रहा है कि मीनू सिर्फ चार दिन में यहाँ का महीने भर का दूध का बजट पी जाएगी।
माँ ने नाश्ता बना लिया। पराँठे, चाय अचार। चौथाई सदी से चली आ रही खाने की एक ही फेहरिस्त।
मीनू दादी की गोद में बैठ कर खाएगी। दो-चार ग्रास वह आजकल खा लेती है। वह बड़े गौर से खाने का सामान देख रही है।
‘दादी, अंडा नहीं बनाया?’
कमरे में क्षणिक चुप्पी छा गई। संतोष कहता है –
‘मेरा अच्छा बेटा। ऐसे ही खा ले, कल बना देंगे।’
बहू भी अपनी तरफ से छोटी-सी सफाई देती है –
‘घर भी कभी-कभी थोड़ा-सा ही खाती है।’
‘ममा। झूठ बोलती है। हाँ! थोड़ा-सा नहीं खाती, एक खाती हूँ एक।’ मीनू जवाब देती है। अब संतोष उसे डाँट देता है। माँ मास्टरजी को कहती है कि वह शाम को अंडे लेते आएँ। साथ ही साथ उसका अनपढ़ दिमाग यह अंदाजा भी लगाए जा रहा है कि रात की सब्जी के पैसे अंडे खा जाएँगे। उन दोनों बूढ़ों को रात को सब्जी की जरूरत पड़ती नहीं। सुबह आधा पतीला दाल बन जाती है जो रात तक चल जाती है। बाहर आँगन में सब्जियों का छोटा-सा बाग है। मौसम आता है, थोड़ी सब्जी उगती है, तो ही बनती है। वह सुबह ही बैगन के पौधों के बड़े-बड़े पत्ते उठा कर दो गोल बैगन तलाश चुकी है। छोटे हैं तो क्या, तोड़ लेगी। एक टैम का काम तो चल जाएगा।
मीनू दो ग्रास खा लेने के बाद दूध माँगती है। बहू उठ कर रसोई में जाती है। मीनू की बड़ीवाली बोतल भर कर लाई। मीनू लेट गई और लगभग एक ही साँस में सारा दूध पी जाती है। दादी सोचती है कि पाँच बार में सारा दूध पी जाएगी। वह बहू को सलाह देती है –
‘काकी, इसे रोटी खिलाया कर। अन्न अंदर जाएगा तो कुछ मोटी होगी। देख तो सही, कैसी सूखी पड़ी है।’
बहू पति को नाम ले कर ही बुलाया करती है। बताती है –
‘मैं खिलाने लगती हूँ तो संतोष गुस्से हो जाता है। कहता है इतनी जल्दी रोटी शुरू नहीं करनी।’
माँ संतोष की तरफ देख रही है। बेटा उसे कैसे समझाए कि वह छोटी मीनू के माध्यम से अपना बचपन सुखद रूप में पहली बार जी रहा है। उसे आज भी याद है कि जब से होश सँभाला, हाथ में रोटी का टुकड़ा और चाय का गिलास ही रहा है। अगर बच्ची रोटी खाने की जिद करती है तो उसे अपना घिनौना बचपन याद आ जाता है। तब अन्य बच्चों को बाजार की कोई भी चीज खाते देख कर उसका जी कितना ललचाता था। जब माँ से पैसे माँगने की जिद पर अड़ जाता था तो आम तौर पर पिटाई ही होती थी, क्योंकि घर का राशन-पानी खरीदने के बाद माँ के पास देने को कुछ बचता ही न था। तब उसे अपनी माँ से बेइंतहा नफरत थी – कितनी बुरी है। कभी कुछ नहीं देती। नासमझ जो था। अब जा कर कहीं समझ आया है कि पैसे का, पूँजी का यह गलत वितरण, असंतुलन, वह कुल्हाड़ी है जो हमारे संबंधों को काट कर फेंक देती है।
दादा ने नाश्ता कर लिया। वह बीड़ी सुलगाते हैं तो मीनू फिर टोकती है – ‘दादा यह सिगरेट मत पियो। गंदा। बूवाला। पापावाला पिया करो, हाँ नहीं तो।’
दादा उठ कर आँगन में गए। मीनू की ममा उसे डाँटती है –
‘मीनू! बड़ों से ऐसे नहीं कहते। देखो मैं तुम्हारे पापा को ऐसा कहती हूँ?’
‘हाँ, कहती हो – सिगरेट मत पियो। बू आती है।’
मीनू उठती है। मटकती हुई बाहर आँगन में आ गई। कुछ टमाटर के पौधे हैं, कुछ भिंडी, कुछ बैगन और साग वगैरह। मीनू एक-एक करके सब के बारे में दादा से पूछ रही है। फिर कहती है –
‘मैं इनको छू लूँ, खराब तो नहीं होंगे।’
दादा उसका सिर थपथपा कर छू लेने की आज्ञा देते हैं। साथ ही हिदायत देते हैं कि पत्ते मत तोड़े। थोड़ी देर में छू लेने से उसका मन भर जाता है। पूछती है –
‘दादा, सुंदर फूल कहाँ है?’
उसे अपने घर के छोटे-से आँगन की याद है, जहाँ सारा साल रंग-बिरंगे फूल इठलाते रहते हैं। उन पर उड़ती तितलियों के पीछे वह छोटी-छोटी दौड़ें लगाती है। वह अब भी दादा के जवाब के इंतजार में है। अगला सवाल पूछती है –
‘दादा! तितली कहाँ है?’
सब्जी के पौधों के हिलने से उन पर बैठे मच्छर उड़े। एक-दो ने मीनू को काट भी लिया। अब वह दादा के चुप रहने और मच्छरों के काटने से झुँझला गई। कहती है –
‘दादा! यह पौधे तोड़ दो। गंदे। छी। मच्छर काटता।’
दादा के पास उसके सारे सवालों के जवाब हैं। लेकिन जवाब देने की हिम्मत नहीं पड़ रही। क्योंकि उन्हें फूलों और सब्जी के फर्क का पता है लेकिन मीनू का क्या कसूर। बचपन में शायद उन्हें भी फूल और तितली अच्छी लगती थीं। थोड़ा बड़ा होने पर गरीब- जिंदगी की सच्चाइयों का पता चला। अपने आप फूल भूल गए थे, तितलियाँ भूल गई थीं। मीनू के इन सवालों से वह अंदर से हिल गए। उनका जी चाहता हे कि इसी वक्त खुरपा उठाएँ और सब्जी के इन पौधों को जड़ से काट दें, यहाँ फूल लगा दें, जिन पर तितलियाँ उड़ती रहें। वह नहीं इन्हें देख सके, बेटा संतोष नहीं देख सका। क्या तीसरी पीढ़ी भी बिलकुल पहलेवाली पीढ़ियों की-सी जिंदगी बिताएगी? बिना फूलों के, बिना तितलियों के।
उन्हें पता है कि यह फूल-तितलियाँ शायद मीनू के भाग्य में भी सिर्फ कुछ दिन और हैं। बेटा जो कमाता है, वह जानते हैं। घर के जो खर्चे हैं, वह जानते हैं। बड़ी जल्दी बेटे के आँगन से भी फूलों के पौधे उखड़ जाएँगे, तितलियाँ उड़ जाएँगी, वह जानते हैं। वहाँ भी जल्द ही सब्जियाँ लग जाएँगी, वह जानते हैं। बदसूरती, गरीबी, अभाव, बच्चों की जिंदगी में शुरू से आ जाए तो उनका क्या होता है, वे क्या बन सकते हैं, वह जानते हैं क्योंकि सारी उमर उन्होंने प्राइमरी स्कूल में गरीब बच्चों को पढ़ाया है। लेकिन मीनू को तो अभी इन दुखों का पता नहीं। वह मच्छरों का काटना भूल चुकी है। फिर से पौधों के बीच मटक रही है। उसने बैगन के पौधे के लंबे पतों को हाथ से पीछे किया, गोल-गोल बैगन देख कर चहक उठी –
‘दादा! देखो, कितने बड़े आलू हैं।’
दादा मुसकराए, उसे बताया –
‘मीनू बेटे, आलू नहीं, बैगन।’
‘अच्छा। कितना बड़ा बैगन। मैं एक तोड़ लूँ?’
दादा अब सतर्क हो गए। बैगन की सब्जी बेटे-बहू के लिए कल दोपहर बननी तय हुई है। अभी से मीनू तोड़ लेगी तो खराब हो जाएँगे। वह उसे कहते हैं –
‘मीनू, कल तोड़ेंगे।’
‘नहीं, अभी तोड़ूँगी। बस एक, हाँ।’
वह उसे पकड़ कर क्यारी से बाहर निकालते हैं। अब बच्ची पर जिद सवार हो चुकी है।
वह ऊँचा-ऊँचा रोना शुरू कर देती है। दादी भी रसोई से बाहर आ गई। मीनू अपनी माँ के पस शिकायत कर रही है –
‘ममा! दादा बहुत गंदे हैं। मुझे तोड़ने नहीं दिया।’
दादी मास्टरजी से कहती हैं –
‘तोड़ लेने देते जी! क्या फर्क पड़ता है।’
मास्टरजी खीझ गए। जरा तेज आवाज में बोलते हैं –
‘तो कल सब्जी… ‘
फिर उन्हें खयाल आता है कि बेटे-बहू के सामने तो यह वाक्य बोलना नहीं था। वह कमरे से बाहर चले जाते हैं।
बहू इस आधे बोले गए वाक्य से ही सब कुछ समझ गई। इतना कड़ा अभाव शायद अपनी जिंदगी में उसने पहली बार देखा। पति से बोली –
‘संतोष, कैसे चलाते होंगे घर का खर्चा। सुनो, हर महीने यहाँ कुछ भेज दिया करो न।’
पति कोई जवाब नहीं देता। उसे कैसे बताए कि कहना आसान है, भेजना कितना कठिन। फिर कई बार एकमुश्त बड़ी रकम भी तो घर में देनी पड़ जाती है। वह उसके जवाब का इंतजार नहीं कर रही है। वह जानती है संतोष क्या सोच रहा है। उसके दिमाग के कोनों में इस वक्त छोटी-छोटी रकमें इधर से उधर उछल रही होंगी। आपस में जमा होती, फिर घटती, फिर शेष क्या बचा इसका लेखा-जोखा करती। लेकिन वह भी इस सच्चाई को समझ चुकी है कि एक रकम से दूसरी चाहे जितनी बार घटाओ, शेष कभी कुछ नहीं बचता। बची हुई रकम तो कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोग पहले ही काट लेते हैं।
लेकिन क्योंकि पति-पत्नी जिंदगी का सच एक-दूसरे से हमेशा बाँट कर रखते हैं, इसलिए किस्से-कहानियोंवाला तनाव उनकी जिंदगी में कम ही आता है। वह पति को सलाह देती है –
‘सुनो संतोष। मीनू तो इनका चार-पाँच रुपए रोज का खर्च करवा देगी। ऐसा क्यों नहीं करते, माँ को खर्च के लिए कुछ रुपए दे दो न।’
‘मैंने यह सोचा था। लेकिन पैसे देने की हिम्मत नहीं हो रही। कितना अपमानित महसूस करेंगे। माँ को कितना चाव था मीनू कुछ दिन यहाँ रहे। अब बच्चों का खर्चा मुझसे तो दिया न जाएगा।’
‘ठीक है। यहाँ से वापस जाने के बाद कुछ रुपए मनीआर्डर से भेज देना।’
संतोष चुप। इसे कैसे समझाए कि इन घरों में हर दिन के खर्चे की रकम बँधी-बँधाई होती है। कोई अपना भी कुछ दिनों के लिए आ जाता है तो इनके आनेवाले कुछ दिनों की रोटी खा जाता है। वह जानता है कि अमूमन माँ सुबह ही दाल का आधा पतीला बना लिया करती है, दोनों वक्त के खाने के लिए। एक अतिरिक्त सब्जी बनानी पड़ती है।
मीनू को दुबारा भूख लग चुकी है। हमेशा की तरह आज्ञा देती है – ‘ममा! भूख लगी है। दूध ला।’
अब ममा को भी घर में घट रही हर रोज की त्रासदी का आभास हो गया है। मीनू इतनी जल्दी-जल्दी दूध पीएगी तो शाम तक सारा खत्म कर देगी। ‘नहीं बिट्टू, खाना बन रहा है। आज तो मीनू हमारे साथ छोटी गोगी खाएगी।’
लेकिन मीनू इस तरह के नाटकों से छलावे में नहीं आनेवाली। कड़क कर कहती है – ‘ममा, तू बक-बक मत किया कर। हाँ, नहीं तो। मैं दूध पियूँगी।’
पत्नी संतोष की ओर मदद माँगती निगाहों से देखती है। वह कहता है – ‘यह मानेगी क्या? दे दो। मैं शाम को बाजार से और दूध ले आऊँगा।’
मीनू गटागट दूध खत्म कर देती है। फिर वह रसोई के दरवाजे पर खड़ी हो कर दादी से पूछती है –
‘दादी, तू क्या बना रही है?’
‘अपने लाल के लिए खीर बना रही हूँ। खाएगी न?’
‘हाँ। मुझे खीर बौत अच्छी लगती है।’
दोपहर के खाने के लिए सब बैठे हैं। दादी कटोरी में खीर डाल कर सब से पहले मीनू के आगे रखती है। मीनू खीर को देखती है, फिर मुँह फेर लेती है।
‘खाओ न बेटे,’ – दादी।
‘मैं नहीं खाती।’ – मीनू।
‘क्यों?’ जरा कड़ी आवाज में पूछता संतोष।
‘नहीं खाती। खीर में दादी ने बादाम नहीं डाले।’
दादी असहाय नजरों से मीनू को देखती हैं, समझाती है, ‘बेटे, खीर में बादाम नहीं डालते।’
‘देखो ममा, दादी झूठ बोलती है। तू डालती है बादाम, है न।’
संतोष तीखी आवाज में कहता है –
‘मीनू! चुपचाप खीर खा लो।’
‘नहीं खाती। दादी गंदी है। दादा गंदा है। मुझे एक बैगन नहीं तोड़ने दिया। सब गंदे हैं। ममा, हम अपने घर चलेंगे। हाँ, यहाँ नहीं रहते।’
माँ संतोष के अंधे गुस्से को जानती है, पिता जानते हैं, पत्नी जानती है, लेकिन मीनू तो नहीं जानती। संतोष सुबह से माँ-बाप की छोटी-छोटी मजबूरियाँ देख रहा है, छोटे-छोटे अपमान देख मीनू के इस लंबे वाक्य ने इन मजबूरियों को, अपमानों को आपस में जोड़ दिया। वह उठ कर घुटनों के बल बैठ गया। हाथ लंबा हुआ, दिमाग में बैठी मजबूरियों ने एक खूँखार जानवर का रूप धारण किया, जानवर उछल कर हाथ पर आ बैठा, हाथ पूरे जोर से उठा और मीनू के दाएँ गाल और नाक के आधे हिस्से पर फड़ाक की आवाज के साथ जानवर ने छलाँग लगा दी।
मीनू जमीन पर लुढ़क गई, उसका मुँह खुल गया, लेकिन किसी तरह की आवाज बाहर नहीं आ रही। दादी बेटे को धक्का दे कर परे करती है। मीनू की छाती मल रही है।
फिर बच्ची के अंदर कैद चीख पूरा जोर लगाती है और मुँह के रास्ते बाहर निकल कर कमरे में फैल जाती है। चीख का तीखा हिस्सा दादी, दादा और माँ के दिल के अंदर भी चाकू की नोक की तरह सरसरा कर घुस जाता है।
मीनू का मुँह कुछ क्षणों में ही सूज गया। होंठ पर लहू की बूँद चमक आई। अब वह लगातार हाहाकार किए जा रही है। संतोष खाना छोड़ कर सिगरेट सुलगाता है, दादा बीड़ी सुलगा लेते हैं। पत्नी मीनू को गोदी में ले कर हिला-डुला रही है। फिर उसे उठाए हुए बाहर आँगन में चली जाती है। मास्टरजी बेइंतहा गुस्से में हों तो बेटे की तरह बेकाबू हो जाते है। पत्नी से कहते हैं –
‘बदजात औरत! चार बादाम खीर में डाले नहीं जा सकते थे।’
‘घर में बादाम कहाँ हैं?’
‘उफ, इस घर में कभी भी कुछ हुआ है क्या?’
वह जानती है इस वक्त मास्टरजी को जवाब देना ठीक नहीं। पता उन्हें भी है कि इस घर में बादाम कभी खरीदे ही नहीं गए। वह डरते-डरते बेटे से कहती है –
‘काका, तू पागल हो जाता है। इतना गुस्सा! कितनी जोर से मारा है। खून निकल आया है। कान फट जाता तो? बच्ची को समझ थोड़े ही है। उसका क्या कसूर!’
जानवर दिमाग में वापस आ बैठा। उसके अलग-अलग अंग दिमाग के अलग-अलग हिस्सों में बँट गए। पता संतोष को भी है कि कसूर बच्ची का नहीं। पता उसे भी है कि कसूर किन लोगों का है। लेकिन क्या हो सकता है? कभी तो कुछ होगा ही। वे लोग इतिहास को भूल गए हैं। इतिहास क्या उन्हें मुआफ करेगा?
पत्नी बाहर से ही उसे आवाज देती है –
‘अब चुप भी तुम्हीं से होगी, जरा बाहर बाहर आ कर उठा लो।’
संतोष मीनू को गोद में लेता है। वह उसकी छाती के साथ सिर रख कर और जोर से रोने लग पड़ती है। लेकिन वह उसे छोटी-छोटी कहानियाँ सुना कर जल्दी-जल्दी मना लेता है। मीनू का गाल और होंठ अभी तक सूजे हुए हैं।
सब लोग फिर खाने के लिए बैठे हैं। मीनू अब चुपचाप बिना बादाम की खीर खा रही है। पापा साथ-साथ उसे भालूवाली कहानी सुना रहे हैं। खाना खत्म हो गया। मीनू दादी से कहती है –
‘दादी, जल्दी फ्रुट लाओ। मैं खा कर निनी बाबा करूँगी।’
संतोष मीनू को घूर कर देखता है। वह थोड़ी देर पहले पड़ी मार को भूली नहीं। झट से कहती है –
‘पापा, अच्छे बच्चे फ्रुट नहीं माँगते।’
‘नहीं, बेटा!’
‘अच्छा। दादी, तू फ्रुट मत ला, दूध दे। मै सोऊँगी।’
संतोष और पत्नी याद कर रहे हैं कि घर में रोटी के बाद फल खाने के लिए वे दोनों किस तरह मिन्नतें करते हुए मीनू के पीछे घूमते हैं। वह सौ नखरे करती है, कई बातें मनवाती है, तब कहीं जा कर कुछ खाया करती है। अभावों की मार सच जल्दी ही समझा देती है। छोटी बच्ची है, कोई संदर्भ नहीं समझती, किसी का कुछ का ज्ञान नहीं। फिर भी एक बार मार खा कर सच समझ गई है। अगर ये अभावों से घिरे बैठे, चुपचाप जी रहे लोग सदियों से मार खाने के बाद चुप हैं, अपना जो है नहीं माँगते तो फिर हैरानी कैसी!
दोपहर हो गई। वे तीनों लेटे हैं। दादा-दादी पास ही के कमरे में लेटे हैं। मीनू और पत्नी सो गए। संतोष को नींद नहीं आ रही। वह गुसलखाने जाने के लिए उठता है। गुसलखाने और साथवाले कमरे की खिड़की जिसमें माँ-बाप सोए हैं, साझी है। वे दोनों आपस में बातें कर रहे हैं –
‘अच्छा।’
‘पैसे हैं? आखिरी दिन हैं। खत्म हो गए होंगे।’
‘नहीं हैं। माँग लूँगा।’
छोटी-सी चुप्पी। फिर माँ की आवाज –
‘संतोष जल्दी वापस जाने के लिए कहे तो रोकना मत। अच्छा करता है यहाँ नहीं आता।’
माँ का एक-एक शब्द किसी महामारी के कीटाणुओं की तरह हुआ संतोष के शरीर में प्रवेश कर रहा है। फिर उसे लगता है कि ये कीटाणु दरवाजे से बाहर निकल रहे हैं, निकल गए हैं, आस-पड़ोस के घरों में जा कर लोगों के शरीर में घुस गए हैं। घर-घर में, शहर-दर-शहर कीटाणु पहुँच चुके हैं, महामारी फैल चुकी है। आदमी का आदमी से, माँ का बच्चों से, पिता का बेटे-बेटियों से संबंध काटती महामारी।
यही माँ है। न आने की वजह से कितना गुस्से में थी, झगड़ती थी। खत लिखवाती थी। यहाँ पहुँचे थे तो आज सुबह इसका चेहरा कितना रोशन था। यही माँ है, चाह रही है मीनू, वह और संतोष आज ही लौट जाएँ।
संतोष दीवार पर लगे शीशे में अपना चेहरा देखता है। अपनी सूनी-सूनी आँखों में अपने भविष्य के छोटे-छोटे दृश्य देखता है। मीनू बड़ी होगी, उसकी शादी होगी। वह अपने बच्चों के साथ उसके घर में आएगी। तब शायद उसके साथ भी यही कहानी दुहराई जाए? फिर वह आँखों पर हाथ मल कर इन दृश्यों को मिटा देता है। वह आज ही लौटने का निर्णय कर लेता है।
शाम का वक्त है। संतोष रिक्शा बुला लाया। तीनों रिक्शा में बैठते हैं। माँ कहती है –
‘काका, यह क्या? कुछ दिन रहते।’ वह झूठ बोल रही है।
‘नहीं। कोई जरूरी काम याद आ गया है। फिर आएँगे।’ वह झूठ बोल रहा है।
दादी की आँखों में आँसू देख कर मीनू कहती है –
‘दादी, अच्छे बच्चे रोते नहीं। मैं फिर आऊँगी। तब अंडा भी नहीं माँगूगी, दूध भी नहीं माँगूगी, फ्रुट भी नहीं माँगूगी। पापा गुस्से होते हैं।’
रिक्शा चल पड़ता है। दादा-दादी बहुत देर तक मीनू का हवा में उठा ‘बाय-बाय’ करता हाथ देखते रहते हैं।