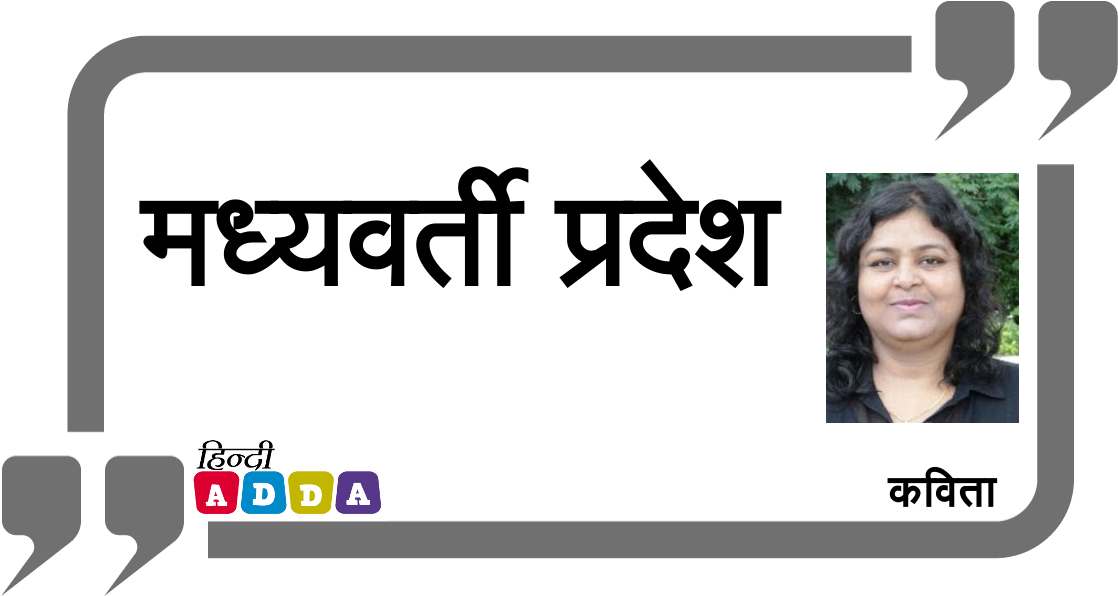मध्यवर्ती प्रदेश | कविता – Madhyavarti Pradesh
मध्यवर्ती प्रदेश | कविता
जाते-जाते उसे लगा कि उसकी यह कोशिश भी जाया गई।
कोशिशें यूँ भी बेकार जाने के लिए ही होती हैं। बेकार होते-होते कहीं कोई साकार हुई तो हुई… हुई तो समझो सब नकार भी सार्थक हो लिया। पर इस बार उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह फिर-फिर उठे… फिर एक कोशिश करे। और अब वक्त भी कहाँ था उसके पास। उम्र के कितने बरस यूँ ही बिता दिए इसी एक आस में कि अब कुछ हुआ… अब कुछ होगा… पर क्या होना था और क्या होता… मामला क्यों न बाबूजी का ही हो, उन्हीं बाबूजी का जो उसे पढ़ कर सुनाते रहते थे –
नरम काई उग आती है, कड़ी चट्टान पर / पानी काट देता है बड़े से बड़े पत्थर को / और हाथ जो शरीर का कमोबेश कोमल हिस्सा है / कठोर संगमरमर पर तराश देता है फूल और पत्तियाँ।
हमेशा से स्थिति ऐसी ही नहीं थी, जब उम्र कम थी उसकी, जब वह भी इसी घर के बाशिंदों में से एक थी जोश और हिम्मत थी उसमें बेपनाह। वह सोचती थी अक्सर, वह बदल सकती है सबकुछ। और वह कोशिश करती रहती लगातार। एक के बाद एक, अनथक।
तब शायद उसे इतनी अक्ल नहीं थी कि वो यह सोचती या कि पूछ पाती कि आपकी तमाम कोशिशें फिर क्यों बेकार हो जाती हैं? मसलन बाबूजी कभी माँ के लिए साड़ी खरीद लाते तो यही कहतीं वे… रहने दीजिए, यह साड़ी ला कर क्या जताना चाहते हैं आप? क्या साबित करना चाहते हैं कि आपको मेरा बहुत ख्याल है। सारी जिंदगी किस तरह मैंने एक-एक, दो-दो सूती साड़ियों में काटी है। तब तो कभी आपको मेरा ख्याल नहीं आया, ढोर-ढंगरों की तरह घर में डाला और भूल गए… और माँ की आँखों से सचमुच आँसू निकल आते। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता माँ का यूँ रोना। माँ का अतीत कँकड़ीला था, लहुलूहान था उनका पूरा शरीर पर बाबूजी फिर भी धैर्य के साथ पेश आते कि कभी न कभी तो ये सारे दाग धुल जाएँगे। कभी न कभी यह सारी कड़वाहट निकलते-निकलते निःशेष हो लेगी। पर कब, उन्हें नहीं पता था। …उन्हें तो बस उस कल की प्रतीक्षा थी।
उन्होंने एक दिन उससे कहा था जानती हो विनी, जब मेरी शादी हुई तो मैं पढ़ता ही था। फिर जब कमाने लगा तो तीन छोटे भाई-बहनों का दायित्व। बाद में जब कमाई थोड़ी बढ़ी और केवल अपना परिवार बचा तो तुम बच्चों का दायित्व… कुछ भी कभी भी अपनी पत्नी के लिए अलग से कर सकूँ इसकी कोई गुंजाइश ही कहाँ थी। और सीता कभी खुश भी न हो सकी मेरी पसंद से। उसकी पसंद बहुत ऊँची और कलात्मक थी। कुछ भी तो कभी उसे उसके मन लायक नहीं दे सका…। सो बाद में जब साड़ी लेने का वक्त होता पैसे ही थमा देता। मेरी औकात में ही सही उसकी पसंद के कपड़े तो होंगे न… वह गलत कहाँ कहती है…
वह लाड़ से बाबूजी के कंधों पर अपनी हथेलियाँ दबा देती जैसे कि वह समझ रही है सब कुछ… ठीक उसी तरह जिस तरह सुबह उसने माँ के छलछलाए आँसू को अपने दुपट्टे के कोर में थाम लिया था। मुश्किल था यह सब कुछ पर उसे इन चीजों को सँभालने का लंबा अभ्यास था। यह एहसास वैसा ही था जैसे किसी नट का तनी रस्सी पर सँभल-सँभल कर चलने का अभ्यास। माँ-बाबूजी मानो रस्सी के दो छोर थे उसे दोनों के दुख छूते। वह दोनों की पीड़ा की सहभागी थी। वह दोनों को खुश रखना चाहती थी। वह दोनों की थी और दोनों की बनी रहना चाहती थी। यह कम दुर्गम न था, पर था तो था…
हालाँकि माँ कहने लगी थी तब तक – उसे तो बस अपने बाबूजी की फिक्र रहती है… कि वह तो हमेशा अपने बाबूजी का ही पक्ष लेगी… शायद जाने अनजाने हो जाता हो ऐसा। अब माँ तो झूठ नहीं बोलती होंगी न… वह जानती थी समय के साथ बदला था बहुत कुछ उसके भीतर भी।
छुटपन में वह जब भी माँ की आँखों में आँसू देखती उसे बाबूजी पर बेइंतहा गुस्सा आता। उसे लगता माँ रोती है तो बस बाबूजी के कारण। वह माँ के पास ही डोलती रहती लगातार। उनके पुनःव्यवस्थित हो लेने तक। उसे बाबूजी बहुत बुरे लगते, बहुत-बहुत बुरे जो माँ को इस कदर रुलाते हैं…
पर बड़े हो कर जाना था यह सच कि जरूरी नहीं है कि आँसू जिसकी आँखों में हो बेकसूर भी वही हो। खासकर तब जब शादी के लायक उम्र हो चली थी उसकी। छोटे और बड़े दोनों भाई अपनी पढ़ाई और नौकरी के ख्वाब में डूबे रहते और माँ बाबूजी के पीछे दिन रात पड़ी रहती उसके लिए योग्य वर की तलाश के लिए। वक्त-बेवक्त की हदें जैसे टूटती जा रही थी। बाबूजी के हाथ का कौर वहीं का वहीं थमा रह जाता। तैयार होते-होते वे बिना शर्ट बदले या बगैर दाढ़ी बनाए ही दफ्तर निकल जाते।
और माँ…? माँ भी कब खा-पी पाती कुछ फिर… और उसका उपवास तो अपने आप हो जाता। ग्लानि भाव से आँखें सूजी। उभरे पपोटे और खुले-बिखरे केश जैसे उसके स्थायी स्वरूप का हिस्सा हो चले थे वह एक स्थायी अपराधबोध से ग्रसित रहने लगी थी। वही है इस सब के पीछे, वही है माँ-बाबूजी के बिगड़े रिश्तों का सबब… सारे कलह-द्वेष की जड़ सिर्फ वही है, वही… सोचती है अब तो आश्चर्य भी होता है। क्यों नहीं किसी कुएँ-नदी में छलाँग लगाई उसने। घर में ही पड़ी नींद की गोलियों तक को नहीं छुआ। हद था उसका धीरज। पर उसके धीरज तो उसके बाबूजी थे। बाबूजी सामने होते तो सारा दुख, सारी उदासी यूँ उड़ जाती फुर्र से खुशगवार हो कर, जैसे रंग बिरंगी तितलियाँ… वह फिर से फुदकने-उड़ने लगती। अपनी पढ़ाई और अफसरी के सपने देखने लगती। पर कब तक? सिर्फ अगले युद्धघोष तक।
बाबूजी ने कह दिया था एक दिन मैं नहीं ढूँढ़ पा रहा कोई रिश्ता, मैं नाकारा और नाकाबिल पिता हूँ… और मैं अब ढूँढ़ूँगा भी नहीं…
बाबूजी ने कहने को तो कह दिया होगा पर इसका परिणाम सपने में भी सोच न पाए होंगे वे। क्षणों की देरी में माँ बिछावन से उतर कर जमीन पर लेट गई थी और चारपाई के पाए उनके सिर पर बजने लगे थे ताबड़तोड़। वे दोनो हतप्रभ थे; पर उसने सँभल के माँ को खींचा था बाहर। बाबूजी ने पाए पर से माँ की पकड़ छुड़वाई थी – यह क्या कर रही हो सीता… तुम जीती मैं हार गया। बाबूजी पहली बार फफक-फफक कर रो रहे थे बच्चों की नाई। तुम जो कहोगी वही करूँगा, पर ऐसा कुछ न करना फिर कभी। वे उससे कह रहे थे, विनी… विनीता, जरा डेटाल और पट्टी तो ला दो… पर वह नहीं हिली थी, बाबूजी के पुकारते रहने पर भी। उसे ऐसा खयाल क्यों नहीं आया? करना तो उसे चाहिए था यह सब… आखिर सारे कलह की जड़ वही तो थी, एकमात्र वही।
बाबूजी सुनी-अनसुनी करते देख उस पर चीखे थे, शायद पहली बार – सुनती नहीं क्या विनी, बहरी हुई जाती है बिल्कुल… मैं कब से कह रहा हूँ… वह फिर भी नहीं हिली थी। खीजकर खुद उठकर सब कुछ लाए थे। वे सुबकते हुए माँ की मरहम पट्टी करते रहे थे, उनके सिरहाने बैठे रहे थे चुपचाप उनका हाथ थामे हुए। वे शायद तब पहली बार टूटे थे…
सबसे अजीब बात तो यह कि माँ चुप हो गई थी बिल्कुल। एक शब्द भी नहीं। यह हैरत की बात थी उसके लिए। माँ और इस तरह चुप, वह भी जब बाबूजी उसके सामने बैठे हों… उसने होंठ बिचकाए थे अपने… कुछ भी हो उसे क्या।
उसके मन में गहरी वितृष्णा जाग उठी थी… अपने लिए… माँ के लिए… और तो और बाबूजी के लिए भी। क्यों सुनते हैं वह यह सब कुछ… क्यों सहते हैं वे सब चुपचाप… ऐसी कौन सी मजबूरी है।
भीतर की सारी वितृष्णा जैसे इकट्ठी हो चली थी, एक गोला गुबार का घुमड़ने लगा था उसके भीतर कि जिस बात के लिए लड़ते-झगड़ते हैं वे, वो हक तो उसका अपना है और वह हक वह उन्हें कभी नहीं देनेवाली। उसने अपने सीने के अंदर संचित सारे आक्रोश को इकट्ठा कर जैसे निर्णय का जामा पहना दिया था…। गजब यह कि क्रोध और दुख इस हद तक घुल-मिल कर बह रहे थे उसके भीतर कि उस क्षण जो कोई भी दिख जाता उसके आगे वह उसका हाथ थाम चल देती।
बाबूजी जानते थे वह भीतर ही भीतर सुलग-धधक रही है। गहरा अवसाद है उसके भीतर। वे फिक्र में रहते यह ज्वालामुखी फूटे नहीं। माँ और घर के दायित्वों से फुरसत पाते ही उसके गुस्से में बाकोशिश पानी उलीचते… विनी सुन तो… वह अनसुना कर देती। वे फिर-फिर पुकारते। उस दिन वे उसे कंधे से पकड़ कर ले गए थे अपने कमरे तक। बिठाया था उसे अपने सामने – बहुत नाराज हो मुझ से…? अरे सुन तो बेटा… मेरी बिटिया मुझसे भी नाराज हो जाएगी फिर कैसे जियूँगा मैं… तेरे साथ का, तेरे प्यार का ही लोभ था वह; जो तुम्हारे माँ की जली-कटी सुनने के बावजूद गंभीरता से तेरे लिए रिश्ता ढूँढ़ने से डरता था। बिल्कुल अकेला हो जाऊँगा मैं, तेरी पढ़ाई तो बस एक बहाना थी। तुम नहीं रही तो कौन होगा जिससे मैं दो बातें मन की कर पाऊँ, जो मेरा खयाल रखे, तुम्हारी तरह। इसीलिए उनकी बात एक कान से सुनता और दूसरी से निकाल देता। पर भूल गया था मैं शायद, ओस की बूँदों से प्यास बुझाऊँगा तो आखिर कब तक…? तुझे तो जाना ही है बेटा अभी नहीं तो फिर कभी… वह उनकी गोद में ऐसे सिमट आई थी जैसे चिड़िया घोसले में दुबक आई हो। अपने भीतर जमे क्रोध और अवसाद के थक्कों को परे धकेलती हुई, अपने ही निर्णय के खिलाफ… मुझे आपको छोड़ कर कहीं नहीं जाना बाबूजी, कहीं नहीं। और वह यह सब बिल्कुल भी उस तरह से नहीं कह रही थी जिस तरह इस उम्र की अधिकांश लड़कियाँ कहती है शादी के ठीक पहले, ऊपर-ऊपर या झूठी-मूठी। पर बाबूजी अपने आप में ही लिप्त थे। सोचो तो तुम्हारी माँ गलत नहीं कह रही थी… उसके मन की कड़वाहट जाते-जाते फिर एकजुट हो गई थी। कपाट भीतर ही जड़ लिए थे उसने – बस कीजिए बाबूजी… उसकी आवाज बहुत दृढ़ थी।
बाबूजी ने शायद उसके कहे को गौर से नहीं सुना था। या कि सुना था भी तो कुछ इस तरह कि जैसे हर बेटी का बाप सुनता या समझता है। वे बेतरह रिश्ते की तलाश में जुट पड़े थे। वह ऊपर-ऊपर संयत थी, भीतर से बिल्कुल भी नहीं। और इस सब की कसूरवार उसकी नजर मे माँ थी, बस माँ।
यही वह वक्त था जब माँ के बारे में या माँ की तरफ से सोचना चाहती वह तो जबरन, मन मार कर या फिर दिमाग से। यही वह समय था जब वह बाबूजी के साथ न होते हुए भी उनके पक्ष में जा खड़ी हुई थी चुपचाप। माँ कहती थी तो शायद ठीक ही कहती थी। वह तो बाबूजी का ही पक्ष लेगी। पर माँ के साथ उसके दो बेटे थे, बाद में दो बहुएँ भी… और फिर उनके बच्चे भी। अकेले तो बाबूजी को ही होना था हर हाल में।
यही वह वक्त था उसकी जिंदगी का जब उसने किसी भी मुद्दे पर एकजुट और एकमत देखा था माँ-बाबूजी को। देर रात जब बाबूजी लौटते तस्वीरों, रिश्तों पर बतियाते आधी रात तक, खुसुर-फुसुर। उस एक दिन ने बदल दिया था सब कुछ… माँ बाबूजी का रिश्ता भी जिसके लिए उसका अब तक का सारा प्रयास निरर्थक गया था। तो क्या वही खड़ी थी उनके रिश्तों के बीचमबीच। वही थी जो उन्हें नजदीक नहीं आने देती थी? बाबूजी माँ के हिस्से का भी वक्त उस पर ही खर्च कर डालते थे या कि वही छीन लेती थी माँ के भी हिस्से का अधिकार? माँ-बाबूजी को एक साथ पा कर उसने ऐसा ही सोचा था। माँ की तकलीफ को भी महसूस किया था उसने उसी क्षण।
अब बाबूजी के पास उसके लिए वक्त कम गया था। उसे चिढ़ होती, नफरत होती। माँ से… बाबूजी से… अपने लिए आनेवाले रिश्तों से… माँ-बाबूजी की एकमत खुशी से। जबकि वे एकजुट होकर उसके लिए बेहतर से बेहतर वर तलाशने में लगे हुए थे।
इसी खुशी से जल कर उसने एक घोषणा की थी। मैं शादी करने जा रही हूँ, जल्दी ही। क्यों… किससे… कब…??? दोषारोपण के, कलह के सिलसिले फिर शुरू हो गए थे। माँ बाबूजी पर इल्जाम लगाती फिरती – लड़की का दिमाग खराब कर रखा था। सब कुछ तो इन्हीं का किया धरा है।
मैं डरती थी इसी दिन से। मुझे पता था… बाबूजी भागने लगे थे उनसे, घर से।
वह खुश होती बाबूजी के पास फिर वक्त हो चला था उसे समझाने-बहलाने के लिए। …और अजीब बात यह कि घर का माहौल इस तरह एक बार फिर बिगड़ जाने से दुखी नहीं थी वह इस बार। उसे अच्छा लग रहा था, भीतर तक अच्छा। पिता घेरते उसे, घेर-घूर कर पूछते कौन है वह… कैसा है… क्या करता है…??? वह बोलती भी तो क्या। पिता उसकी चुप्पी को उसकी जिद समझने लगे थे, पर स्वभाववश उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा था।
सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा हो चला था। कुहुकता… कसकता… सुलगता… और तिल-तिल जलता, सिवाय उसके और बाबूजी के रिश्ते के।
अविनाश से पूछा था उसने एक दिन ऐसे में ही – मुझ से शादी करोगे? वह जानती थी अविनाश उसके लिए कमजोर है। वे और अविनाश साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते थे। चौंक उठा था वह अचानक हुए हमले की तरह इस अप्रत्याशित सवाल से। विनीता उसे अच्छी लगती थी, बहुत अच्छी। वह उसके साथ एक खूबसूरत जिंदगी बिता सके यह उसका सपना था, पर यह भी सच है कि इस बाबत विनीता से उसने कभी कुछ भी नहीं कहा था। यह सपना पूरा हो इसके लिए पहले पढ़ाई जरूरी थी फिर नौकरी और फिर शादी।
विनीता ने चिढ़कर पूछा था – बोलो, बोलते क्यों नहीं… उसने सोचा, अब तक तो वह यह सोचता रहा था सब कुछ कर लिया तो फिर विनीता को कहाँ ढूँढ़ेगा? ढूँढ़ भी लिया तो क्या हालात सब कुछ कहने के लायक होंगे…? अब जब कि विनीता खुद कह रही थी उससे… उसे लगा सपने तो फिर भी पूरे हो सकते हैं, साथ-साथ और धीरे-धीरे भी। पर विनीता अगर चली गई तो… उन्होंने उसी रोज मंदिर में जा कर शादी कर ली थी। शादी कर लेने के बाद होनेवाले विस्फोट को देखने के लिए अपने घर रुकी भी नहीं थी वह।
एक लंबा वक्त लगा था सब कुछ पूर्ववत होने में… पर शायद सब कुछ पूर्ववत नहीं होता, कभी भी।
बाबूजी रिटायर हो चुके थे। परिवार भरा-पूरा हो चुका था। माँ की सत्ता-महत्ता बढ़ी ही थी दिनों दिन। वह बेटों पर राज करती, बहुओं पर राज करती। और उस राज करने के लिए दिन-रात मेहनत में जुटी रहती उस उम्र में भी और इस क्रम में बाबूजी से और और दूर होती जाती। ऊपर का हिस्सा उनका राजमहल था, नीचे का हिस्सा पिता की दीन-हीन कुठरिया सी, उपेक्षित, दयनीय निचाट सा। जहाँ गीजर नहीं, कूलर नहीं, सुख-सुविधाएँ नहीं। था तो उनका निपट-निचाट एकांत। वह देखती और देखकर भी कुछ कर नहीं पाती।
बाबूजी ने अपनी जिंदगी के खालीपन को दूर करने के लिए कई नए शौक पाल लिए थे… बागवानी, हाँ बागवानी में वे दिन भर जुटे रहते। दिन-दिन भर। शायद वक्त कट जाता हो इस तरह। वर्ना जब अच्छी खासी नौकरी थी नौ कर-चा कर थे घर में, बाबूजी ने बागवानी में कभी रुचि नहीं ली थी।
दूसरे, अब वे डायरी में अपने पसंद की कविता की पंक्तियां लिखने लगे थे… दिन, महीने और तारीख डाल कर। अब वह कहाँ थी जिसे बाबूजी कविताएँ सुनाते पहले की तरह। खुद को अभिव्यक्त करने का उन्होंने यह नया तरीका ईजाद किया था।
वह हैरत में थी, वह दुखी थी। बाबूजी की पसंद की कविताएँ बदल रही थी –
दूध के दाँतों से तूने चट्टान को तोड़ना चाहा / मूर्ख क्या सपने देखने के लिए कोई रात काफी नहीं थी।
दुखांत यह नहीं होता कि लहू-लुहान पैरों से हम जहाँ खड़े हों / उस राह में आगे भी बस काँटे ही काँटे हों / दुखांत यह होता है कि हम एक ऐसी जगह आ खड़े हों जो जमीन का आखिरी टुकड़ा हो और जहाँ से कोई राह आगे नहीं जाती।
यह सब कुछ जिस तरफ संकेत कर रहा था वह उस ओर गौर करने से भी डरती थी। वह फोन जल्दी-जल्दी करती, पता चलता बाबूजी घर में है ही नहीं। और अगर होते तो बच्चे भी उन्हें बुलाने नीचे नहीं जाना चाहते। ऐसे में उसे और ज्यादा घबड़ाहट होती। माँ से जब भी बाबूजी का हाल पूछो, रटा रटाया जवाब मिलता – क्या होगा उन्हें? ठीक ही हैं… बाहर का खाते-पीते रहते हैं, उम्र हुई, अब पचेगा यह सब…? वह मन ही मन सोचती घर में है ही कौन उन्हें वक्त पर बना कर देनेवाला। बचा खुचा वह भी बेवक्त नीचे भेज दिया जाता है खा लें बला से न खाएँ…
पिछली बार उसने अपना मोबाईल सेट वहीं छोड़ दिया था – मैं जा कर दूसरा ले लूँगी, इस तरह आप से बात तो कर सकूँगी। वे हँसे थे खुलकर… तू भी न…
बातें भी होने लगी थी उनसे। वे अक्सर अपनी उदासी ढाँपते, लेकिन जितना ही वह उसे ढाँपना चाहते अचके में उतना ही उभर-उभर आता वह; किसी सिकुड़ चुके चादर से बाहर निकल आए अंगों की तरह।
वह माँ को फोन करती – थोड़ा तो वक्त बाबूजी के लिए भी रखो, वे बिल्कुल अकेले… वे उधर से धीरता से कहतीं – वक्त ही कहाँ बचता है, दो रोटियाँ खाने तक का वक्त तो मुश्किल से निकाल पाती हूँ… पाँच-पाँच बच्चों की जिम्मेदारी, चूल्हे-चौके सबका खयाल, तू तो जानती है तेरी भाभियों से नहीं सँभलनेवाला है यह सब… वह प्रतिरोध करती, फिर भी माँ… तू जो माँग रही है विनी वह बहुत मुश्किल है…
बच्चों को भेज दिया करो उनके पास… मैने रोक रखा है उन्हें? वे नहीं जाते तो मैं क्या करूँ… माँ तल्ख हो उठतीं… कुछ काम ही दे दो घर के, तुम्हारी जिम्मेदारियाँ भी बँट जाएँगी… मैं नहीं कह सकती। कहूँगी तो कहेंगे… जिसने सारी उम्र जिम्मेदारियों को मेरे सिर थोपा रहा वह इस उम्र में क्या जिम्मेदारी निभाएगा।
वह लाजवाब की लाजवाब… उसकी इल्तजा, उसके तर्क, उसकी कोशिशें हमेशा की तरह उन पर ऐसे बेअसर जैसे पुरईन के पत्ते से बूँदें ढलक गई हों।
वह हारकर बाबूजी से ही कहती – ऊपर जाकर बैठा कीजिए कभी-कभी। इससे आपको भी अच्छा लगेगा और मन भी हल्का होगा… इससे बहुओं की असुविधा बढ़ जाएगी और… जाता था पहले पर तेरी माँ ने ही संकेत में कहा कि बच्चों को परेशानी होती है। बाबूजी बहुत उदास लगे। मैंने बात बढ़ाने की खातिर ही कहा बच्चों को ही नीचे बुलाकर खेल लिया कीजिए…। बच्चे तुम जैसे थोड़े ही है, घर भी आए तो ये ट्यूशन, वो होम वर्क… ज्यादा दिल्चस्पी ली तो उनके माँ-बाप और… सब यही सोचेंगे उनकी जिंदगी भी तबाह कर रहा हूँ मैं। ‘भी’ शब्द पर जोर देकर बाबूजी जिस तथ्य को इंगित करना चाह रहे थे, मैं भूली कहाँ थी वह बात। वे चुप हुए थे कुछ देर फिर संयत हुए थे – अजीब है न विनी पुरुष उम्र होने के साथ-साथ या यूँ कहो कि रिटायर होने के बाद परिवार के लिए बेकार हो जाता है। और औरत बढ़ती उम्र के साथ और ज्यादा उपयोगी।
उसने कहा था फोन रखती हूँ बाबूजी। उनकी उदासी जैसे उस तक भी तैर आई थी। उसके खयालों में उनका उदास निचुड़ा चेहरा था। उसका मन हो रहा था वह भाग कर उन तक पहुँच जाए, अभी की अभी। पर अभी बच्चों की परीक्षाएँ थी और उसको अपना मन मारना ही था। मन तो मार लिया था उसने पर अविनाश से जोर देकर कहा था – बच्चों के एक्जाम खत्म होते ही बाबूजी के पास जाऊँगी और जब तक जी चाहे रहूँगी… और बच्चे? …बच्चे यहीं रहेंगे तुम्हारे पास। अविनाश हँस दिए थे… जैसा आप उचित समझें।
बाबूजी को यह खबर देते वक्त वह चहक रही थी। बाबूजी की आवाज भी हल्की थी। वह सोते-सोते सोच रही थी, बाबूजी के साथ कुछ बहुत अच्छे और प्यार भरे दिन बिताने हैं उसे… बिल्कुल छुटपन के जैसे। वह उनका वैसे ही खयाल रखेगी। जिद करेगी। और उनके लिए जरूरत की कुछ चीजें इकट्ठा करेगी… और किसी के भी बगैर जीना और खुश रहना सिखाएगी उन्हें। और अब तो माँ भी टोका-टोकी नहीं करती करें पहले की तरह। इस खयाल से ही उसका मन हल्का हुआ जा रहा था। यह सोचे बगैर कि बीच में पंद्रह दिन और थे। पंद्रह छोटे दिन… पंद्रह लंबी रातें।
उन्हीं लंबी रातों में से एक में हुआ था कुछ… अवसाद के घेरे घेरने लगे होंगे उन्हें। अपनी कोशिशें… अपनी नाकामयाबियाँ… अपना अकेलापन जकड़ने-पकड़ने लगा होगा उन्हें। वे बीच सड़क बेसुध पाए गए थे। कोई अनजान देखे तो पियक्कड़ समझ ले। पर वह कोई परिचित था… यह खबर सुनाते वक्त भी माँ की आवाज काँपी थी या नहीं, वह अपनी जड़ता में महसूस नहीं कर पाई। उसने कुछ भी नहीं कहा था, कुछ भी, प्रतिक्रिया में। फोन रख दिया था बस…
वह सामान बाँध रही थी कि अविनाश ने कहा था – अभी जाकर भी क्या कर लोगी… अस्पताल में किसी को रुकने भी कहाँ देते हैं, वहाँ की अलग ही व्यवस्था होती है। घर आ जाएँ तो जितना जी चाहे साथ रह लेना और देख-भाल भी कर लेना। मैंने मना कब किया है। फिर धीमे से कही थी उन्होंने अपने मन की बात – बच्चे एक्जाम के वक्त तुम्हारे बगैर नहीं रह पाएँगे। मेरे पास तो वक्त… तुम जानती हो दफ्तर…
अविनाश ने जिंदगी में जो कुछ भी चाहा था सब कुछ पाया था, क्रम भले ही थोड़ा उलट-पुलट जाए। वह एक बार आई तो उनकी ही हो गई। पर रोज नई सफलता और रोज नए शिखर… इनके लिए हर दिन एक युद्ध लड़ना था उन्हें और वे लड़ते भी थे। फिर और बातों के लिए समय कब और कितना बचता उनके पास।
उसे तो मानना ही था अंततः… बाबूजी के होश में आने के बाद वह उन से रोज बतियाती। हँसाती उन्हें चाहे उसके प्रयास थोथे और बौड़म से ही क्यों न होने लगे। चार दिन बीत जाने थे और बीत गए।
वह उतर कर सीधे बाबूजी के कमरे की तरफ लपकी थी। वे वहाँ नहीं थे। उसे अजीब लगा था वह आनेवाली थी और बाबूजी अपने कमरे में नहीं थे। फिर उसने सोचा था हो सकता है माँ और भाई अस्पताल से लौटने के बाद उन्हें ऊपर ही ले गए हों। उसे सोचकर अच्छा लगा। वह ऊपर ही चली गई थी। माँ पूर्ववत थी, हमेशा की तरह ढेर सारा बतियाती… जिसमें से आधी बाबूजी की शिकायतें ही थी अभी भी… उनकी जिदें… उनकी लापरवाहियाँ। कोइ दूसरा सुने तो उसे लगे कि कितने गहरे जुड़े हैं वे एक दूसरे से। माँ को बाबूजी का कितना खयाल है। पर सामने वह थी। उसने उकता कर पूछा था – माँ, बाबूजी हैं कहाँ? माँ चौंकी थी – और कहाँ होना है, नीचे ही होंगे, मिले नहीं तुमसे…?
वह फिर नीचे उतर आई थी और एक बार फिर छान मारा था घर का कोना-कोना।
हाँ एक चीज जरूर बची रह गई थी उसकी दृष्टि से। बाबूजी की पढ़ाई की मेज पर उनकी डायरी खुली रखी हुई थी।
शाम होने पर / पक्षी लौटते हैं / पर वही नहीं जो गए थे / रात होने पर जल उठती है दीप-शिखा / पर वही नहीं जो बुझ चुकी थी।
जो जुड़ा होता है टूटता भी ज्यादा वही है। बाबूजी ने अनथक विश्वास किया था उस पर। पर उसने क्या दिया था बदले में।
उनकी दुर्गति का एक सबब वह भी तो थी… तो क्या उसकी लाख कोशिशों के बावजूद भी बाबूजी अब उससे वह जुड़ाव नहीं पाते थे? क्या उन्हें उसके आने का औचित्य पसंद नहीं आया था? यह खयाल ही तोड़नेवाला था उसके लिए…
क्या इसीलिए वे नाराज थे कि वो अस्पताल में थे और वह आ भी नहीं सकी थी। वह खुद को एक भरोसा दे रही थी। उसके बाबूजी उसकी मजबूरी समझते हैं। और फोन पर उसके आने की बात से कितना तो खुश थे वे।
वह और परेशान होती कि बाबूजी आ गए थे कहीं से, मैले-कुचैले से। लग रहा था कितने दिनों से नहाए तक न हों। वह लिपट पड़ी थी उनसे। फिर लाड़ से कहा था – क्या हाल बना लिया है आपने… बगीचे से आ रहा हूँ, हाल-चाल बिल्कुल दुरुस्त है। अभी नहा कर आता हूँ फिर तुमको अपना बगीचा भी दिखलाऊँगा। बहुत सारे पौधे… कहते हुए वे बाथरूम में घुस गए थे।
नहाकर निकले तो बाबूजी सचमुच बिल्कुल ठीक लगे। बीमारी की परछाईं तक नहीं थी चेहरे पर, हाँ, थोड़े दुबले जरूर हो गए थे।
वह बगीचे को देख कर खुश हुई। पौधे बहुत सारे थे, नए भी। सीजनल, डहेलिया, गुलदाऊदी, गेन्दे और ढेर सारे सदाबहार पौधे भी। बाग का वह कोना सचमुच खिल उठा था।
आप कितनी मेहनत करते हैं, बीमारी से उठे हैं फिर भी। अरे मेहनत क्या करनी है, थोड़ा ध्यान देना है बस… वे बचपन की तरह उसकी उँगलियाँ पकड़ उसे बगीचे के पिछले हिस्से में ले गए थे। और इनको तो इतने ध्यान की भी जरूरत नहीं। वह देख कर घबड़ा उठी थी, सैकड़ों पौधे कैक्टस के… न जाने कितनी प्रजातियाँ। कुछ अजीब सा प्रभाव था उनका। उसे जैसे घबड़ाहट और बेचैनी होने लगी। उसने सँभल कर कहा था – एक साथ इतने सारे… यह नया क्या कर दिया आपने? यहाँ तो कभी आम और अमरूद का खूब फलनेवाला पेड़ हुआ करता था। हम तीनों भाई-बहनों ने न जाने कितना वक्त बिताया है यहाँ पर। हम फल तोड़ कर खाते थे, लड़ते-झगड़ते थे, खेलते थे साथ-साथ। बाबूजी रुक कर बोले थे – तुम्हें अच्छा नहीं लगा…? अमरुद तो कब का सूख गया, पिछले साल की आँधी में वह आम का पेड़ भी गिर गया। वीरान पड़ा था यह तब से… वह चुप हो चली थी।
उसने बाबूजी के कमरे में पहले एक हीटर रखवाया था और फिर स्टोर से ढूँढ़ कर एक पुराना गैस स्टोव। फिर माँ के ही किचेन के कुछ पुराने-धुराने बर्तन। वह चाय बनाने लगी थी, बाबूजी के पसंद की पकौड़ियाँ और कभी-कभार मूँग की खिचड़ी। वह दिन-दिन भर बाबूजी से बैठकर बतियाती; धूसर पुरानी यादें धुल-पुँछ कर बैठ जाती उनके संग… वे खेलते शतरंज, ताश और कभी-कभी लूडो भी। उसने बाबूजी को अकेले भी यह सब खेलना सिखाया। उसे अविनाश ने सिखाया था पिंटू के गर्भ में होने के दिनों में। अविनाश के पास उन दिनों वक्त कहाँ होता था। उसने बाबूजी से कहा था सीख लीजिए, काम आएँगे।
वह कहती – देखिएगा, मैं इस बार जब जाऊँगी आपको ऐसा बना कर जाऊँगी कि आपको किसी की कमी नहीं खले, मेरी भी… बाबूजी कहते – देखूँगा… फिर जोड़ते वैसे देख तो रहा हूँ… पर कब तक…? जब तक आप उकता कर भगा नहीं देते मुझे।
अब बाबूजी उसके पसंद की चाय भी बनाने लगे थे अदरख और मसालेवाली। माँ देखतीं तो बहुत घूर कर पर कहती कुछ नहीं। पता नहीं उसके कुछ भी नहीं कहने से वे आहत थी वह या राहत की साँस ले रही थी।
उस दिन बाबूजी की बनाई मूँग की पकौड़ियाँ खा रही थी वह, करारी पकौड़ियाँ माँ और औरों के लिए वह ऊपर भी दे आई थी। वे हँस रहे थे किसी बात पर खूब खिलखिल कि बाबूजी की फोन की घंटी बजी थी।
बाबूजी के चेहरे पर चिंता का भाव आया था, उदासी भी। उन्होंने कहा था – जरूर… आप विनी से बात कर लीजिए।
अविनाश ने कहा था उससे कल ही चली आओ, बंटू का हाथ टूट गया है… वह लिपट पड़ी थी उनसे, उसने सोचा था मन में …यह सब अचानक ही होना था और अभी ही… अभी-अभी तो वह आई थी, अभी तो… पर कहा था उसने इतना ही – जाना होगा बाबूजी।
तो इसमें परेशानी की कौन सी बात है। आ जाना फिर… उन्होंने उसके कंधे थपथपाए थे। वह चाहती थी, एक बार बाबूजी के चेहरे को देखे पर देख न सकी थी। बाबूजी के कहने को ही उसने अपना भरोसा, अपना संबल मान लिया। रात में उसने अपने सामान पैक किए थे। सुबह वह बाबूजी के पास गई थी।
वो कमरे में नहीं थे, बगीचे में भी नहीं। वह चिढ़ी थी… ये बाबूजी भी न…
उसे चिंता होने लगी थी। वह बार-बार बाबूजी को कमरे में तलाश रही थी। उसने दरवाजे के पीछे भी देखा। कहीं बचपन की तरह उसे परेशान करने के लिए कहीं छिप गए हों।
आटो आ गया, माँ ने बताया था… वह बाबूजी को फोन लगा रही थी। घंटी घनघना रही थी दूसरी तरफ… वे उठा क्यों नहीं रहे। भाइयों ने सामान आटो में रख दिया था और कहा था वे तो हमेशा से ऐसे ही…। तू जा बंटू को सँभाल, हम हैं न…
भाई और माँ की ये बातें उसे आश्वस्त नहीं कर पा रही थी। वह सब के मना करने के बावजूद एक बार फिर उनके कमरे तक गई थी, फिर उनकी मेज की तरफ। उसने डायरी का वह पृष्ठ फाड़ कर अपनी हथेलियों में ले लिया था… वह बाबूजी द्वारा दी गई आश्वस्ति और इन पंक्तियों के भरोसे वैसा सब कुछ भी सोचना-समझना नहीं चाह रही थी जो उसके मन को भय के घुमेड़ों की तरह उमेठ रहा था –
तुम चले जाओगे / पर थोड़ा सा यहाँ भी रह जाओगे / जैसे रह जाती है / बारिश के बाद / हवा में धरती की सोंधी गंध…
कहानी में प्रयुक्त कविताओं के लिए क्रमशः राजेश जोशी , अमृता प्रीतम और कैलाश बाजपेयी का आभार।
Download PDF (मध्यवर्ती प्रदेश )
मध्यवर्ती प्रदेश – Madhyavarti Pradesh