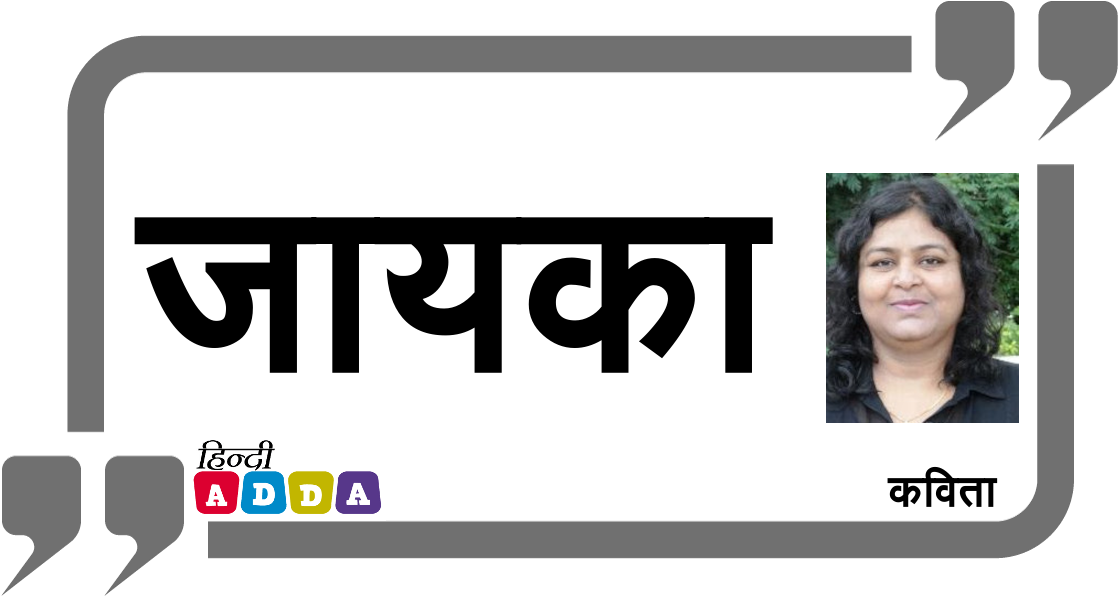जायका | कविता – Jayaka
जायका | कविता
यह शाम मेरे इंतजार की थी, पिछली कई साँझों जैसी ही। इंतजार की घड़ियों जितनी ही धीमी, उदास, बेरौनक। यह शाम बिताए नहीं बीत रही थी।
यह शाम भी धीरे-धीरे रात में तब्दील हो रही थी। बाजार की गहमा-गहमी अब कमने लगी थी। पहले नौ बजे थे फिर साढ़े नौ और अब दस। मेरे जैसे इक्के-दुक्के खोमचे और रेहड़ीवाले भी अब अपना सामान समेट रहे थे। मेरे पाँवों में भारीपन था, हाथों में, मन में… यह जान कर भी कि घर में भाई मेरी राह तक रहा होगा।
औरतों में से कोई नहीं हमारे साथ। वे सुदूर गाँव में हमारे मनीआर्डर, फोन और तीज-त्योहार पर हमारे घर आने की राह देखती रहती हैं… उनकी जिंदगी इंतजार है। एक लंबा-सघन इंतजार…
इंतजार शब्द का ठीक-ठीक मायने अब जा कर समझ आया था मुझे। आज जबकि यह शब्द खिंच कर हुआ जा रहा है इं…त…जा…र… दद्दो, बहिन और भौजी का दर्द अब जा कर मेरी समझ में आया था। भौजी का कुछ जियादा ही। भौजी जिन्हें बूढ़ी दादी और विधवा बहिन का सहारा बन कर सदा गाँव में रहना था। बत्तीस वर्ष की उम्र में ही उनके माथे पर उग आए शिकन, आँखों के नीचे की झाइयाँ और चेहरे की घटती हुई रौनक का कारण अभी-अभी जान पाया था मैं… जो इंतजार के किसी मीठे पल की आशा में जीए जा रही थी…
फलसफों जैसी बातें ‘वह’ बहुत ज्यादा करती थी। अपनी उम्र चेहरे और स्वभाव के ठीक विपरीत जा कर। मैं समझ पाता था या नही, इसकी परवाह किए बगैर। कहती थी, जिंदगी इंतजार जरूर होती है पर उसका फल हमेशा मीठा हो यह जरूरी नहीं। मेरी आँखों में उसका चेहरा कौंधा होगा जरूर इस क्षण, जिसे देखनेवाला कोई आसपास मौजूद नहीं था। मेरी आँखों में आँसू थे पर ठीक-ठीक बता नहीं सकता कैसे? उसके नहीं होने से? उसकी आँखों में होने के या कि वह मेरी आँखों में है यह कोई देख-जान नहीं पा रहा इसके?
उसके पसंदीदा शकरपारे का ढेर अनछुए पहाड़ जैसा खड़ा था मेरी रेहड़ी पर जिसे इलायची और केवड़े की खुशबूवाली चाशनी से सींचता रहा था मैं रात भर। पूरी रात मैं जुटा रहा था उसे अपने मनचाहे रूप, रंग गंध और स्वाद की तासीर तक पहुँचाने में। वैसे प्रश्न तो यह भी है कि अपने या उसके? उसे पुरानी या बासी चीजें पसंद नहीं हैं। एक ही स्वाद भी नहीं…
‘जायका’ दर असल चीजों से ज्यादा हमारी जुबान में बसा होता है। ‘स्वाद’ एक पुलक है, एक तृप्ति। मनोवांछित पा लेने के अहसास जैसा कुछ… स्वाद जिंदगी है, पर जिंदगी कहाँ रुकी रहती है किसी एक ठौर… यह उसके लिखे एक लेख की शुरुआत थी जो शहर के सबसे बड़े दैनिक के रंगीन पन्ने पर छपनेवाले एक स्तंभ ‘जायका’ में आई थी। उसमें मेरी तस्वीर थी मेरी रेहड़ी के साथ। मेरे द्वारा बनाई हुई नमकीन, शकरपारे और तिलपट्टियों के साथ…
पढ़ तो लेते हो न?
मैंने जानबूझ कर अपने ग्रैजुएट होने की बात छुपा ली थी और धीरे से कहा था – हाँ।
गुड, फिर इसे रख लो सँभाल कर। अब तो तुम्हारे खोमचे पर लोगों की भीड़ टूटा करेगी… और सचमुच ऐसा ही हुआ था कुछ। लोगों की भीड़ जुटने लगी थी, मेरी रेहड़ी पर। और मैं उसी भीड़ से बचाता फिरता था अपने शकरपारे। ऐसे-ऐसे रेहड़ी और खोमचे जगह-जगह मिल जाएँगे दिल्ली में, इसके गली-कूचों, पार्कों के किनारे पर, जिनमें कितनों में यही-यही चीजें बिकती होंगी। फिर भी वह आई थी तो सिर्फ मेरे पास… और मुझे और मेरे खोमचे को मशहूर कर दिया थ। यह वही कर सकती थी, सिर्फ वही… कत्थई-भूरी आँखों, गोल नाक और भोले-भाले चेहरे पर पतले से चश्मेवाली वही अनोखी लड़्की।
मैं सोच रहा था घर पर जब भाई पूछेंगे शकरपारे वैसे हीं क्यों लौट आए तो क्या कहूँगा मैं? और कितने बहाने रचूँगा उसकी खातिर। वह आ जाती और बीत जाते मेरे उदास-दुखी दिन। वह आ जाए… आती रहे इससे ज्यादा और क्या चाहा ही है मैंने?
वह आती तो मेरे खोमचे पर जलती बल्ब की रोशनी तेज हो जाड़े की इस धुर साँझ को गर्मी देने लगती। इतनी कि पार्क से सटे इस छोटे से चबूतरे पर पैर लटका कर बैठी वह पूछती – यह जगह कुछ खास है, है न? मैं पूछता क्यों? फिर कुछ नहीं कहती वह। उसकी भूरी-कत्थई आँखें और ज्यादा कत्थई होने लगतीं उस गर्माहट से। दुपट्टे की तरह अपने गले से लिपटा शाल वह उतार देती। कत्थई, हल्के नीले या गुलाबी और बैगनी के बीच के किसी रंग का उसका स्वेटर उसके शाल के हटते ही वातावरण को अपने रंग में रँगने लगता। हाँ उसके पास यही तीन स्वेटर थे, जिन्हें वह जींस पर बदल-बदल कर पहना करती।
उसका कत्थई स्वेटर मुझे बहुत पसंद था। वह उसे जिस दिन भी पहने होती, बच्चों जितनी खुशदिल और चंचल बनी रहती। रेहड़ी पर लगी एक-एक चीज को चखती। चखने के साथ बदलते रहते उसकी आँखों के रंग, चमक और उजास। उस दिन वह न जाने कितनी बातें बतियाती – बचपन की, सहेलियों की, पीछे छूटे घर-परिवार की। पर इन यादों में कोई उदासपन नहीं होता। एक चमकीली सी खुशी रहती उसके इर्द-गिर्द।
हल्का नीला-आसमानी रंग… इन दिनों वह उदास होती। बीते सारे दिन साए की तरह मँडराते रहते उसके इर्द-गिर्द। जिनसे वह मुझे भी मिलवाती थी उन आसमानी दिनों में। मुझे पसंद नहीं होना चाहिए था वह आसमानी स्वेटर, पर पसंद था, कत्थई स्वेटर जितना ही, उससे कम बिल्कुल नहीं। उसकी शोखी, उसका चहकना सब भाते थे मुझे। पर उससे भी ज्यादा कहीं उसका मुझे अपने पास ला खड़ा करना। इन्हीं दिनों में कभी-कभी मेरे घर-परिवार के बारे में पूछती थी वो, पर हमने हमेशा कहा कम, सुना ज्यादा। वह कहती रहती मैं सुनता रहता। इससे उसका कहना तो पूरा होता ही था और मेरा सुन लेना भी। सुनना किसी के करीब आ खड़ा होना होता है, ‘कहना’ किसी को करीब लाने कि कोशिश। यह भी तो कभी उसी ने कहा था।
ऐसे ही एक दिन पूरी बाँहों का स्वेटर न पहनने के लिए डाँटा था उसने। और ऐसे ही एक दिन वह लेती आई थी एक पूरी बाँहोंवाला पुराना स्वेटर। सच पूछो तो वह स्वेटर मुझे बहुत पसंद नहीं था। मेरे पास भौजी के बुने कई स्वेटर थे – गहरे, चटक और चमकदार। पर चूँकि वह लाई थी और मुझे लगा था कि कभी उसने भी पहना हो इसे, इसलिए…
पर इन स्वेटरों से ज्यादा वह मुझे पसंद आती थी सलवार-कमीज में। उसके स्वभाव की तरह खुले-खुले सलवार-कमीज। खूब फूलदार… खूब फैला हुआ परियों की पंख की तरह उड़ता-बहकता दुपट्टा और खूब सारी चुन्नटोंवाला सलवार। जहाँ तक मुझे याद है उसके पास ऐसे दो ही सूट थे। मैंने कहा था उससे एक दिन इन कपड़ों में वह बहुत अच्छी लगती है, कि ऐसे कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं उस पर। उसने भी हँस कर कहा था मुझे भी ये कपड़े बहुत पसंद हैं। माँ के सिले हुए हैं, उनकी पसंद के। इसीलिए बचा कर पहनती हूँ इन्हें… फिर थोड़ी देर के लिए चुप हो गई थी वह… सच यह है भी और नहीं भी। इन कपड़ों को पहनने से बचती हूँ मैं। ये कपड़े यहाँ के चलन से आउटडेटेड कहे जाएँगे, पुराने फैशन के। जब सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं और मेरे पास वक्त नहीं होता है उन्हें धुलने का तभी निकालती हूँ मैं इन्हें। उसकी आँखों में उन अपनी पसंद के कपड़ों को न पहन पाने का दुख ज्यादा था या फिर समय के साथ चलने की ललक, मैं थाह नहीं पाया।
दुख मैने पहले भी ताड़ा था उन भूरी कत्थई आँखों में। वह पहले भी गुजरती थी इसी राह से, लगभग रोज। कि इसी राह से गुजर कर कोई रास्ता जाता था उसके घर की ओर। नहीं, उसके मकान तक, जिसे घर कहने से उसे सख्त एतराज था। रोज उनके बीच कोई बहस होती। रोज चिढ़ते-खीजते गुजर लेते थे वे एक दूसरे के साथ। रोज लड़की जबरन बाँधे गए बैल की तरह घिसटती चली जाती उसके पीछे-पीछे। मुझसे तीन खोमचे आगे के ठेले से वे उबले अंडे लेते या कि आमलेट। मुझे लगता, लड़की मुड़-मुड़ कर देखती रहती है मेरे खोमचे की तरफ।
उस दिन वह अकेली थी। वह झिझकती हुई रुकी थी मेरे खोमचे के आगे। उसने मसालेवाले बेसन में लिपटी मूँगफलियाँ खरीदी थीं और उन्हें चटखारे ले कर खाती रही थी देर तक। अखबारवाले किस्से के ठीक बारह दिनों पहले की बात है यह… उसके बाद वह रोज आने लगी थी मेरे खोमचे पर। ये आसमानी नीले स्वेटर के दिन थे। उसने कहा था एक दिन खुद ही। सड़क पर चलते-फिरते कहीं खड़ी हो कर ऐसे कुछ खाऊँ यह उसे पसंद नहीं था। कपड़े तक उसकी पसंद के… वह मेरा दोस्त था, मेरा सहकर्मी और उस अखबार के मालिक का बेटा भी… मैने वह नौकरी ही छोड़ दी, ऐसे भी कोई जी सकता है क्या…?
अब?
अब ढूँढ़ूँगी कोई नई नौकरी, किसी दूसरे अखबार में। जब तक नहीं मिलती फ्री-लांसिंग करती रहूँगी। फ्री-लांसिंग मतलब अलग-अलग अखबारों के लिए लिखना। अंडे मुझे भी पसंद हैं लेकिन रोज-रोज ऊबने लगी थी मैं उससे। उसे गोल-गप्पे, चाट कुछ भी पसंद नहीं। उन्हें बीच राह खड़े हो कर खाना होता है। उसने कभी नहीं रुकने दिया तुम्हारे खोमचे पर… स्वाद की भी तो कोई अहमियत होती है न जिंदगी में… अपनी पसंद के स्वाद की…
धीरे-धीरे नीले स्वेटर के दिन बीतने लगे थे। कत्थई स्वेटर ज्यादा पहनने लगी थी वह। वह बताती उसके लेख कई अखबारों के संपादक पसंद करने लगे हैं। इनमें से किसी एक में उसे नौकरी मिलने की भी संभावना है। नहीं, तो भी कोई बात नहीं। मन लायक काम, आजादी और पैसे भी चाहे थोड़े कम ही सही मिल तो रहे ही हैं उसे।
मेरी दुकान अब ज्यादा चकमक रहने लगी थी। मीठी-मीठी गमक फैलाती हुई। नए-नए स्वादों की खोज में। उन्हें खोजने का इतिहास रचती हुई। उसकी गमक आसपास के दुकानदारों को चिढ़ाने लगी थी।
वह दिन गुलाबी-बैगनी के बीच के किसी रंगवाले स्वेटर का दिन था। उसने मुझे सौ रुपए थमाए थे। हिसाब ठीक है न, कुछ बाकी तो नहीं? हिसाब साफ ही रखना चाहती हूँ मैं। मैं हतप्रभ था। हिसाब जैसी कोई चीज बाद में रह ही कहाँ गई थी उसके साथ? कभी खुले नहीं होने पर मैं पैसे नहीं लेता तो कभी वह पहल करके कोई बड़ा नोट छोड़ देती थी मेरे पास। फिर…? तो क्या ठीक ही कहते हैं सब दुकानदार। अपना उल्लू साध रही है कि मुझे उल्लू बना रही है वह? अपना खाली वक्त काटने चली आती है वह मेरे पास…। कि बहुत चालू है वह! दुकानदार या दुकानदारी का तो रिश्ता था ही नहीं हमारा। वह आती तो लक्ष्मी भी चली आती थी मेरे पास। बचे-खुचे, बासी-ताजा सब सामान बिक जाते देखते-देखते। मेरी रेहड़ी खाली, पूरी खाली…
मेरी आँखों का अकबकायापन दिख गया था शायद उसे भी। मुझे बहलाने के लिए कहा हो जैसे उसने। तरक्की तभी कर पाओगे जब काम को काम की तरह लेना सीखोगे। रिश्ते और काम दो अलग-अलग चीजें होती हैं…
अगले दिन के कत्थई स्वेटर ने मुझे ढाँढ़स दिया था। कल कुछ नया जरूर बना कर लाना, मीठा। मुझे नई नौकरी मिली है, एक टी.वी. चैनल में। टी.वी. है तुम्हारे घर में? होगी भी तो तुम कब देख पाओगे मुझे, दिन भर तो यहाँ जमे रहते हो… अब तो मुझे खाने-पीने की भी सुध नहीं रह जाएगी।
मुँह मीठा करने-करवाने का दिन था वह। मैने रात भर जग कर खोवे और तिल के लड्डू बनाए थे, बनाते-बनाते सुबह हो गई थी। मैं पूरे दिन उसकी प्रतीक्षा करता रहा, यह जानते हुए भी कि वह शाम ढले ही आती है, और वह तो नई नौकरी का पहला दिन था। उस दिन वह अकेली नहीं आई थी, उसके साथ कोई और भी था। उसने मुझसे रुक कर कोई बात नहीं की यह कोई आश्चर्य नहीं था, आश्चर्य यह था कि उसने उन लड्डुओं का कोई टुकड़ा मेरी तरफ नहीं बढ़ाया था। वर्ना वह तो… आज मैंने बहुत दिनों बाद कोई अच्छी फिल्म देखी… आज मैं खूब हँसी…। आज मेरा आर्टिकल खूब पसंद आया लोगों को… वह कहती थी मुझसे, अपना बनाया खुद कब चख पाते होगे तुम, शुक्र मनाओ कि मैं हूँ और मेरे होने से ये बहाने भी…। वर्ना तुम तो…
जिंदगी को हँस कर जीने के लिए बहाने तलाशना बहुत जरूरी है, वर्ना…
दो-तीन दिनों तक वे दोनों साथ-साथ आते रहे। वह कम बोलती मुझसे, कम चीजें लेती। एक नई हड़बड़ी, एक नई बेचैनी उसके चेहरे पर पुती रहती हमेशा। हमेशा वह पूछती मुझसे – ‘कुछ नया नहीं है क्या?’ पर नए का सिलसिला जैसे थम चला था, लड़की के रुकने और बतियाने के सिलसिले की तरह। जैसे कि नई चीजों के बनने का संबंध उसकी बातों से था, साथ से भी… मैं सोचता रहता पर कुछ भी नहीं सूझता मुझे… मैं फिर भी खुश था, वह आती तो है न; रुकती तो है न मेरे खोमचे पर… इससे भी ज्यादा खुशी इस बात की थी कि वह नया लड़का नहीं रोकता था उसे मेरे खोमचे पर आने से। वह तो साथ-साथ आता था। लड़की के लिबास में गुलाबी और बैगनी के बीच के रंगवाला वह स्वेटर ऐसे चिपका रहने लगा था जैसे उसके वजूद का ही कोई हिस्सा…
इंतजार-इंतजार में बीच के पाँच दिन बीत गए थे। आज की पूरी शाम भी। मैं रेहड़ी समेटने-समेटने को था। मैंने खुद को ढाँढ़स बँधाया, काम ज्यादा रहता होगा… फुर्सत नहीं मिलती होगी।
मैं ठेले को प्लास्टिक से ढँकने के बाद रस्सी से बाँध रहा था। रात के, वह भी जाड़े की रात के साढ़े ग्यारह होने को थे। भाई मेरी प्रतीक्षा में जगा होगा, उसने खाना भी नहीं खाया होगा। कि एक बड़ी सी गाड़ी रुकी थी मेरे ठेले से थोड़ी दूर। एक लड़की उतरी थी लस्त-पस्त और आगे बढ़ चली थी। मर्द स्वर ने टोका था उसे पीछे से- ‘कुछ खाओगी नहीं… तुम्हारा फेवरिट…’
स्त्री ने बगैर पीछे देखे कहा था – ‘ऊब गई हूँ उन्हीं-उन्हीं चीजों से। मैं बदलना चाहती हूँ अपना जायका।’
वे दोनों बढ़ लिए थे नए खुले साउथ इंडियन रेस्त्राँ की तरफ…।
मैंने ठेले को ढकेला था। रात सचमुच ज्यादा हो आई थी, गहरी और काली। मैं उदास होना चाहता था पर मैंने रात की कालिमा और अपनी उदासी दोनों को धकेला था, ठेले के साथ-साथ।
Download PDF (जायका )
जायका – Jayaka