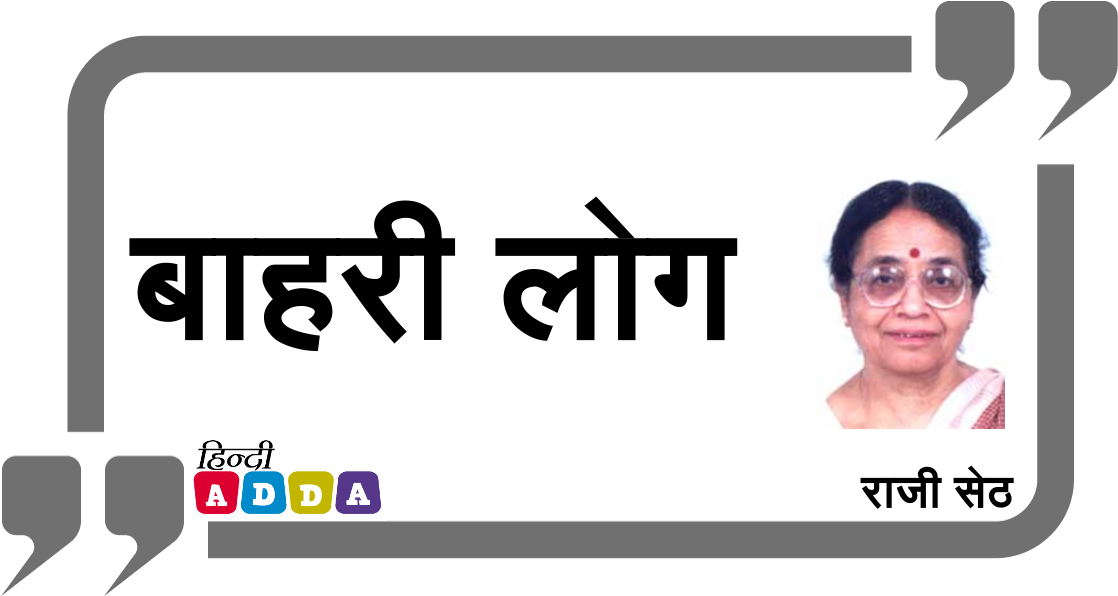बाहरी लोग | राजी सेठ – Bahari Log
बाहरी लोग | राजी सेठ
एक वृद्ध स्त्री…रात के बारह बजे दरवाजा खटखटाती है। दरवाजा नहीं। बेडरूम की खिड़की के टूटे हुए काँच में अपना चेहरा दाखिल कर लेती है .
कमरे की मन्द रोशनी में देह को बॉल्कनी में बाहर छोड़कर उसका अन्दर आ चुका चेहरा एक दहशत पैदा करता है। उस दहशत का अन्दांजा दूसरे को नहीं हो सकता। नीम-ऍंधेरे में बिस्तर पर निस्पन्द पड़े आदमी की दृष्टि के शून्य में उग आती एक गरदन और उसमें से फूटती आवांज।
उस दहशत का अन्दाजा उस गरदन को भी नहीं हो सकता क्योंकि वह खुद दहशत में है।
वह चेहरा बोलने लगा है-”काका नहीं आया अभी तक।” ‘अभी तक’ शब्द को उसने दोहराया-तिहराया है।
नींद के सागर में अध-जगे सपनों-सा हिलोर लेता क्षण पहले ही टूट चुका है। अब कुछ अपनी भी साँस लौट रही है।
”अभी तक माने?” मैं झटके से पलंग के नीचे आ गयी हूँ।
”जानती नहीं हो… अभी तक। कितने बजे हैं… देखा।” उसके उत्तर में एक काट है तीखी, झिड़कती हुई।
धुन्ध कुछ-कुछ साफ हो रही है। इस स्पष्टता में स्थिति की निरापदता भी शामिल है। टार्च उठायी, घड़ी देखी, बताया-”12 बज चुके हैं, 10 मिनट ऊपर हैं।”
”उफ्!” सिहरती लगी।
”आपका बेटा शायद अभी तक दंफ्तर से नहीं आया।”
आँधी में झूलती डाल की तरह उसका सिर जोर-जोर से ”हाँ” में हिला। उस हिस्टीरिया में उसने जाने कितने सहस्त्र पलों की चिन्तातुर मुरदनी को झटककर फेंका होगा। हिलना थमते ही सिसकियों की दाँतों में भींची जाती अवरुद्ध आवांज और खामोशी।
परदा हट जाने से बॉल्कनी के बल्ब से झरती रोशनी की एक कतरन अन्दर चली आयी है।
अब दिमाग दौड़ रहा है। पहाड़…बरसात…टेढे-मेढ़े रास्ते…ढलानें…बिना रेलिंग की पगडण्डियाँ…अन्धे मोड़…ऍंधेरा…मोटर साइकिल की रपटीली फुरती…जवान हो चुके खून का जोश…या शायद शराब…या शायद एक वृध्दा के घर में बैठे होने को भूल जाना…या शायद आदत, जो देखने-समझने की धार को भोथरा कर चुकी हो।
मन में खदबदाती आशंकाओं की कीच। कुछ भी हो सकता है। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है जो उस वृध्दा को थमाकर दिलासे का भ्रम पैदा कर सकूँ। जो हैं, वह डरी हुई सम्भावनाएँ हैं।
उसे थमे हुए क्षण में भी, मुझे लगा अपेक्षा की कोई नोक मेरी ओर तनी है। वह कील उस मटमैले ऍंधेरे में भी मुझे चुभ रही है। निस्सहायता की सुरसुरी मेरे भीतर रेंगने लगी है। वह नहीं जानती, मैं भी यहाँ अजनबी हूँ, आसपास किसी को नहीं जानती।
”सुनिए माँ जी, मैं यहाँ नई आयी हूँ। यूँ ही छुट्टी काटने आ गयी दस-पन्द्रह दिन।…यह घर मेरा नहीं है। यह मेरी दोस्त का फ्लैट है।”
वह मेरे वाक्य का केवल पहला हिस्सा सुनती है-”मैं भी यहाँ नई आयी हूँ। चार-पाँच दिन पहले ही आयी हूँ…अपने बेटे के पास…”
यह वार्तालाप अभी तक कमरे और बॉल्कनी में खड़े दो लोगों के बीच केवल सिरों के माध्यम से हो रहा है।
”एक काम करती हूँ। पड़ोसियों को जगाती हूँ। वह यहाँ के मूल निवासी हैं। चप्पा-चप्पा जानते हैं। वह जरूर कुछ मदद करेंगे। वैसे तो अभी ऐसी देर नहीं हुई है। हो सकता है, आपके बेटे को कोई काम ही पड़ गया हो।”
वह बुदबुदाती है-‘देर से आना था तो कहकर तो जाता।’
यदि आना ही न हो तो? कुशंका से भरी एक आवांज मेरे अन्दर से उठती और मुझ पर झपटती है। जाते समय कौन कहकर जाता है। क्षण आ जाता है एकाएक अचानक और हम हैं कि उसे भूले रहना चाहते हैं।…जीने के आवेश में उसे बेदखल किये रहते हैं क्योंकि उसकी उपस्थिति का डर जीने नहीं दे सकता…बाधा डालता है और एक जीने का ही तो लाभ है, लोलुपता भी है। क्या इसीलिए? …जानबूझकर हम अपने को आश्वासन देते रहते हैं कि हम हैं…हम भी हैं…हम ही हैं।
”चलो फिर बेटी।” वृध्दा की चिन्ता ने मुझे टोका। मैंने चिटकनी खोली। बॉल्कनी की रोशनी के चलते लैंडिग पर ऍंधेरा नहीं है, पर साँय-साँय करता एक अटल अटूट पहाड़ी सन्नाटा साँस ले रहा है।
वृध्दा को देखते ही लगा मैंने इस स्त्री को दोपहर में रेलिंग पर कपड़े सुखाते देखा था। उम्र की लकीरों से कटा-पिटा चेहरा…पतली काठी…संफेद झक्क बाल…सिर पर ओढ़ी सफेद ओढ़नी की माथे तक आयी लेसदार कगार, देह पर धुल-धुलकर बदरंग हो गया टेरीलिन का जोड़ा।
मैंने शाल ओढ़ी। टॉर्च ली। वृध्दा को साथ लिया और सामनेवाले फ्लैट की घण्टी टीपी। ठीक सवा बारह बजे…रात के पहले पहर।
जिन्होंने दरवाजा खोला वे कुनमुनाये हुए नहीं थे। नींद से जगाये-जैसे भी नहीं। उनके कपड़े अस्त-व्यस्त थे। हड़बड़ी में उन महानुभाव ने कुरता उलटा पहन लिया था। वे दोनों अप्रसन्न दीखे थे। देखते-ही-देखते उनके चेहरों पर एक ठण्डी पर्त चढ़ने लगी थी…आँखों में धुन्ध दाखिल हुई थी। अब वह आसानी से वह सब-कुछ नहीं देख सकते थे, जिसे दिखाने के लिए आधी रात उनकी घण्टी टीपी गयी थी।
”माफ कीजिएगा…इतनी रात गये आपको जगाना पड़ा। इन माताजी का बेटा अभी तक दंफ्तर से नहीं आया है। चिन्ता हो रही है।”
दोनों में से पुरुष ने पलटकर दीवार-घड़ी देखी थी…फिर वृध्दा की आँख की तिरमिरी, फिर भवें सिकोड़ीं-”कोई बात नहीं, आ जाएगा। आजकल राष्ट्रपति यहाँ आये हुए हैं। काम चल रहा होगा, दफ्तर में।”
”इस समय तक?”
”क्यों नहीं? वह मेंटेनेन्स विभाग में जो है।”
”फिर भी…” मैं कहना चाह रही थी मेण्टेनेन्स विभाग एक चीज है, राष्ट्रपति का आगमन भी कोई और चीज, मैं जिस चीज की बात कर रही हूँ वह कोई और है। दूसरी बातें तो अनेक हो सकती हैं-बाढ़, भूकम्प, अणु-बम, उग्रवाद, ओले, आग, इन घाटियों और शिखरों के बीच और भी कितना-कुछ हो सकता है, पर इस समय तो एक ही भँवर है…एक माँ है…एक बेटा है…परदेस है…आधी रात है…जोंखिम है…ऍंधेरा है और वह अभी घर नहीं आया। वह एक। वही एक।
”आप बेकार उलझ रही हैं। पहले भी वह कभी-कभी देर से आता है। हम तो कब से देख रहे हैं। उसी दिन तो उसके माथे में चोट लगी थी।”
अब यह पुरुष के साथ खड़ी स्त्री बोल रही थी। एकदम सपाट आवांज। अपने शब्दों को हँसते-से होठों में चबुलाती हुई।
”क्या पहले भी कभी उसे चोट लग चुकी है? किस दिन? कब की बात है?” वृध्दा की हल्की-सी काया जैसे चार इंच उछल गयी हो-
”लगी थी, कुछ दिन पहले। रात-भर चिल्लाता रहा था। हमने एस्प्रिन दी थी। सुबह हस्पताल गया था। टिटनेस का इंजेक्शन भी लगा था।”
”यह कब की बात है? कब की?…वृद्धा को एक रट जैसे लग गयी थी।”
”हो गये होंगे, दो-तीन महीने…अब याद थोड़ेई रहता है!”
”देखो मुझे कुछ नहीं बताता।”
मैं अधीर थी। चिन्ता की नोक पर तड़फड़ाता क्षण पिछड़ता जा रहा था। क्षण में छिपी क्षिप्रता भी। लग रहा था उस समय कुछ हो रहा है कहीं। किसी अज्ञात के ऍंधेरे में। वृध्दा उस ऍंधेरे को चीर देना चाहती है इतने और ऍंधेरों को अपनी चिन्ता में शामिल करके।
”जाओ-जाओ माताजी! सो जाओ। जब आना होगा, आ जाएगा। उसे नौकरी भी तो करनी है कि आपको ही देखना है।” पुरुष पुरुष की तरह था।
”मुझे न देखे”, वृध्दा बिखर गयी-”पर अपने घर तो आये।”
यह वार्तालाप मुझे अखरा था। ”क्या हम इस बारे में कुछ कर नहीं सकते? उसके दंफ्तर तक नहीं जा सकते या फिर पुलिस स्टेशन? आंख्रि दफ्तर तो साढ़े पाँच बजे ंखत्म हो जाता है।”
”वह कौन-सा दफ्तर में बैठा होगा”, पुरुष ने यह बात बहुत धीमे से कही थी। इन्द्रियों की क्षीणतावाली वृध्दा ने निश्चय ही नहीं सुनी होगी।
”जाने से कम-से-कम पता तो लग जाएगा कि वह वहाँ से कितने बजे निकला था। जल्दी से एक चक्कर लगाया जा सकता है। आपके पास तो मोटर साइकिल भीहै।”
”नहीं, नहीं, यह सब बेकार है” पुरुष ने फैसला सुनाया था। वह हर तरह से उस चिन्ता में शामिल होने से इनकार कर रहा था।
”तो फिर?”
”तो फिर यह कि आप लोग जाकर सोइए। माताजी, मैंने कहा न कि आप जाकर सोइए। आ जाएगा। न आया तो देखा जाएगा।” उसने अपनी बगल में खड़ी स्त्री को एक गुझा-सा इशारा किया था।
स्त्री फुर्ती से अन्दर गयी और शाल ओढ़कर बाहर आ गयी। वृध्दा के कन्धों को अपनी बाँह में समेटकर ठेलने का उपक्रम करने लगी-”चलिए, मैं आपको घर छोड़ आती हूँ।”
मुझे लगा था दो फ्लैट्स के बीच जिस पथरीली लैंडिंग पर हम खड़े हैं वह हिलने लगी है, जैसे अन्दर कहीं भूकम्प बन रहा हो। धरती को स्थिर करने के लिए हमने कितना कुछ किया है। मकान बनाए हैं। सड़कें बिछायी हैं। ट्रक, टैंक, टैंकर, रेलगाड़ियाँ चलायीं, फिर भी धरती हिल रही है। इस तरह, एक आवश्यक उद्गार को चोटी से धकेल दिए जाने के कारण।
वृध्दा ठिल रही थी। ठेली जा रही थी। उसके कन्धों को घेरती हथेलियों में एक अनदेखा दबाव था। हिंसा थी। अपने लिए आरक्षित किया जा चुका एक बचाव था। वृध्दा की बाहर तक बहती व्याकुलता के विपरीत।
यह दोनों चीजें साथ-साथ दिखाई देती एकदम बेहूदी-जैसी लग रही थीं। अटपटी। अनैतिक, और मैं थी कि खड़ी-खड़ी देख रही थी।
हाँ। वह मैं ही थी जो खड़ी-खड़ी देख रही थी, कुछ भी नहीं कर रही थी। वह क्षमता पता नहीं किन लोगों में होती है जो सामने से आ रहे आक्रमण की छलाँग को अधबीच निरस्त कर देते हैं और संकट की कगार पर खड़े आदमी को उबार ले आते हैं।
मुझे लगा था मैं वह नहीं हूँ।
मुझे चुभा था मैं वह क्यों नहीं हूँ?
मेरी आँखों के सामने लाचारी से धुँधलाया एक काँच था जिसकी आड़ में उस लैडिंग पर खड़ी मैं उस वृध्दा को ठिलते हुए देख रही थी।
वृध्दा पैर अड़ा रही थी, पर ठिल रही थी।
उस दम्पती के दरवांजे से वृध्दा से हटते ही दृश्य बदल गया। घटा का घनत्व कम-सा हो गया।
अपनी स्त्री के चले जाने से पुरुष अकेला रह गया। वह अब मेरी ओर उन्मुख था। खुलकर हँसने लगा और मुझे समझाने की मुद्रा में आ गया। देखते-ही-देखते उसकी ऍंगुली का पोर अपनी दायीं कनपटी पर आकर गोल-गोल घूमने लगा।
”आपको नहीं पता, इसका पेंच ढीला है। पूरी तरह क्रैक है-बढ़िया। इसे अपना कुछ पता ही नहीं रहता। गैस पर दूध रखती है, दूध उबलता रहता है। नल खोलती है, पानी बहता रहता है। तवे पर रोटी डालते है, जलती रहती है। मालूम है क्यों? क्योंकि यह सदा रावलपिंडी में बैठी होती है। बेवकूफ है पूरी। देश के टुकड़े हुए इतने बरस बीते पर इसका पटरा अभी तक वहीं बिछा है। सोच कर देखिए 45-50 साल क्या कुछ कम होते हैं? मैं तो इसीलिए इसकी बकवास नहीं सुनता।”
”पर इस समय तो…”
”समय-समय छोड़िए, कौन इसके साथ वहाँ बैठा रहेगा?”
मेरी जुबान तालू से चिपक गयी है। मैं कहना चाहती हूँ इस समय की चिन्ता तो अन्धे को भी दीख जाएगी। वैसे भी हम होते कौन हैं जो किसी की दुश्चिन्ता को इसलिए निरन्तर कर डालें क्योंकि हम उस अतीत का हिस्सा नहीं है। इस स्त्री की अवहेलना करें, उसे दंडित करें क्योंकि हम खुद इतिहास की उस सुरंग में फँस जाने से बच गये थे। यह तो संयोग था कि हम उस समय जमीन के किसी दूसरे टुकड़े पर खड़े थे। भूगोल ने हमें बचा लिया था। क्या इसीलिए हम दानाह बने रह सकतेहैं?
”मुझे पता है आप क्या सोच रही हैं। मुझे ‘हार्ट-लेस’ मान रही होंगी”, पुरुष ने मेरे ध्यान को तोड़ा था। ”पर इस औरत ने बोल-बोलकर खुद ही अपनी बात का वजन कम कर लिया है। पगली है पूरी।”
”ऐसे पागलपन के तो और भी कई कारण हो सकता हैं। हो सकते है जितनी सुखी वह रावलपिण्डी में थी, अब न हो पायी हो। आगे का सुधर जाए तो पीछे को कौन रोता है?”
”भगवान जाने, मुझे तो यह सारा सिलसिला कभी समझ में ही नहीं आता। मेरे दफ्तर में भी पाँच-सात लोग हैं, पार्टीशन में लुट-पिटकर आय थे। बिलकुल चंगे-भले, फिर फाऽट हैं। अरे, जो होना था हो चुका, अब उसे ही लेकर रोते रहो…जन्म-भर!”
मैं थी कि कहीं और धकेल दी गयी थी-”आदमी और औरत में क्या फंर्क नहीं होता? आदमी अपने को कितनी तरह से खरच-खपा लेता है। पर औरत? वह भी उस जमाने की औरत, जो दुनिया को बदल देने की भागमभाग में शामिल नहीं है। घर बैठी है…एक चारदीवारी में…उसके सुख-दु:ख भी उसी की तरह उसके पैरों के पास दुबके बैठे रहते हैं, खारिज नहीं होते।”
”यह भी कोई बात हुई?” वह चिढ़ता बोला।
यह साफ है कि मैं जो-कुछ कहना चाहती हूँ पुरुष उसे सुनना नहीं चाहता। उसे अपनी बात को कह देने की उतावली है। शायद लग रहा हो कि अपनी बात को समझाये बिना वह मुझे अपने विश्वास की जद में ले नहीं सकता।
उसकी आवांज आगे चल रही है-”अभी तीन-चार साल पहले इसका आदमी मरा है। यह बुढ़िया इस धक्के को नहीं भूलती। पार्टीशन के दंगों में कहाँ तो बारह घंटे की प्रचंड गोलीबारी से बच निकला और कहाँ इसकी बगल में सोता-सोता मर गया। सच मानिए, मैं तो इसका विश्वास ही नहीं करता। पता नहीं सच कहती है या झूठ कि रावलपिंडी से निकलने के लिए जिस ट्रेन पर बैठा था। वह गुजराँवाला के स्टेशन पर रोक ली गयी थी। बताती है, बारह घण्टे लगातार गोलीबारी हुई थी। सारी टे्रन को ही भून डाला…”
”वह अकेला था?”
”आपको पता नहीं? फसाद शुरू होते ही सब लोगों ने अपने परिवार पहले ही हिन्दुस्तान भेज दिये थे। घर-बाहर, कारोबार की वजह से खुद अटके रहे कि पता लगे हवा किधर को चलेगी। बताती थी कि जब मिलिटरी आयी और फौजियों ने लाशों से भरी उस ट्रेन में घुस-घुसकर हाँक लगायी कि कोई बच गया हो तो बाहर निकल आये, तब इसका आदमी लाशों के ढेर को अपने ऊपर से ढकेलता बाहर निकला। और किस्मत देखिए, दूसरे डब्बे में इनका माल ढोनेवाला एक मजदूर भी बच गया था। उसे निकलने के लिए तुरन्त ही ट्रक मिल गया तो वह हिन्दुस्तान की सरहद पार कर गया और इसका आदमी कैम्पों में धक्के खाता, भटकता एक महीने के बाद अमृतसर पहुँचा। इन लोगों ने तो उसे मरा मान लिया था…अरे मान लिया था पर मरा तो नहीं था। यह मूर्खा उन्हीं बातों को लेकर बैठी रहती है। कोई भी, कहीं भी राह चलता मिल जाए तो हो जाती है शुरू।”
पुरुष की निन्दक निर्दयता मुझे अखर रही थी। क्या उसने वह अखरना मेरे चेहरे पर पढ़ा कि बोला, ”अब यह इसका बेटा है-अपना बेटा। इसकी एक भी बात बरदाश्त नहीं करता। यही सब बातें लड़के से पूछो तो चिढ़ जाएगा। कहेगा यह सब पुरानी बातें हैं, कौन मैंने अपनी आँखों से देखी हैं जो सच मानूँ। वैसे बड़ा ही समझदार लड़का है, एकमद ‘बैलेंस्ड पर्सन’!”
”आप कैसे जानते हैं इतनी सब बातें?”
”अरे यह बुढ़िया पहले भी यहाँ आयी है, आती रहती है। लड़के को अकेला जानकर पीछे लगी रहती है।” पुरुष के चेहरे पर फिर से हिकारत की रेखाएँ खिंच आयी थीं। पता नहीं क्यों वह इस वृध्दा के जीवन-भोग पर विक्रमादित्य की शलाका लेकर बैठा था।
”…देखिए, अब यह लड़का है…जवान है…अभी अकेला है…आजाद है, कहाँ जंजाल पाले। इस दर्द की पोटली को सँभालना क्या आसान है। पर वह लाख मना करे, यह आ ही जाती है इस अकेले की रोटियाँ पाथने। अरे, यह नहीं होगी तो क्या लड़के को रोटियाँ नसीब नहीं होगी। हर समय डपटता रहता है कि बड़े भाई के पास जाकर रहो। उनकी गिरस्ती है। वहाँ बहू है, पोते-पोतियाँ हैं…अच्छे-बुरे जैसे भी हैं…हैं तो सही। पर मजाल कि सुने। असल में मोह बड़ी बुरी चीज है…हैऽऽ किनहीं?”
अब वह समर्थन की चाह से मेरी ओर देख रहा है। उसने सारी कैफियत में मुझसे साझा कर लिया है। उसके हिसाब से मुझे अब उसके दृष्टिकोण में भी साझा कर लेना चाहिए। उसके मुख पर छपी कुछ-कुछ ऐसी अपेक्षा।
मैं निरुत्तर हूँ।
निरुत्तर रहना चाहती हूँ। मेरे पास भी अपने विश्वासों की एक पोटली है जिसे मैं उस पुरुष के हवाले कर देना नहीं चाहती। किसी अपात्र को कहना नहीं चाहती कि सब-कुछ लुट-पिट जाए, गर्क हो जाए, फिर भी जाने कैसे माँ बची रहती है। क्या वह एक सम्बन्ध नहीं सनातनता है? नहीं तो ऐसा कैसे हो पाता कि इतिहास के दर्द को अपने होशोहवास पर झेलती यह स्त्री, एक निचाट नए नगर के परायेपन में एक उद्दंड पुत्र को अपना आँचल देकर सहेजती।
माँ का आँचल किन नाचीज-चीजों पर भी फैल सकता है, पुरुष नहीं जानता। स्त्री जानती है, पुरुष नहीं जानता। नहीं जान सकता। पर ओलों के डर से फलों के नन्हे पौधे तक आँचल से ढाँप दिए जाते हैं, क्या इस बात को भी इस पहाड़ी नगर में रहनेवाला पुरुष नहीं जानता होगा?
वृध्दा के साथ गयी और पुरुष के साथ रहती स्त्री अब लौट आयी है। उसके चेहरे पर एक विजित-सी मुसकान। क्यों नहीं, यह क्या कम किया कि रावलपिण्डी में बने एक बुत को वह किस चतुराई से एक अकेले ऍंधेरे कमरे में स्थापित करके आयी है! जानते हुए कि बिल्डिंग के उस विंग में अभी रोशनी नहीं है। तीन-चार दिन में आने की सुनवाई थी, पर तीन-चार दिन बीते तो कई दिन बीते…
स्त्री खूब प्रसन्न है। अपनी सफलता का ब्यौरा प्रस्तुत कर रही है-”मालूम है कितना काँप रही थी बुढ़िया…कम्बल ओढ़ा दिया है…वह तो बैठ ही नहीं रही थी…मैंने कहा, दूसरों के दरवांजे पर खड़े रहने से क्या होगा। अपने घर बैठे…वह आ जाएगा…पहले भी तो ऐसा हो चुका है।”
मेरा सिर चकराने लगा है। वृध्दा…अकेली…दुश्चिन्ता…घुप्प ऍंधेरा… खाट…कम्बल… कँपकँपी और नसीहत।
पुरुष ने मेरे ध्यान को छिटकने नहीं दिया। ”अच्छा जी, अब आप भी जाकर सोइए। पार्टीशन का तमाशा खत्म”, उसने अपनी एक हथेली पर दूसरी हथेली को बजाया है।
एक अकस्मात् जैसा अन्त।
”अच्छा जी,” मेरे मुँह में पुरुष के ही वाक्य का चिथड़ा फड़फड़ाता बचगयाहै।
उनका दरवांजा बन्द हो चुका है।
मेरा पता नहीं कब हो पाएगा।
अब?
मैं उस लैंडिग पर एकाएक अकेली छूट गयी हूँ-अवसन्न और रीती। लैडिंग की मटमैली रोशनी में इतनी ही अवसन्न एक चुप्पी।
अभी तक तो कहाँ-से-कहाँ तक…भीतर-और-बाहर…आता और जाता शोर था, चिन्ता थी, दर्द था, इतिहास था, भूगोल था।
अभी तक तो वे दोनों थे। पुरुष था, हिंसा थी, क्रोध था, आक्षेप और आलोचना।
अब कुछ नहीं है। चुप्पी है। मैं हूँ और चिपचिप आत्मग्लानि। मेरे आपे को झकझोरती, दूषित करती एक अस्वच्छ-सी अनुभूति। मेरे किये कुछ और नहीं हो सकता था तो उस घनघोर चिन्ता के अन्तराल में साँझा तो हो ही सकता है।
भीतर कुछ असह्य होकर उठा है कि मैं वृध्दा के फ्लैट की ओर चल पड़ी हूँ।
बॉल्कनी में रोशनी है, भीतर घुप्प ऍंधेरा। दरवांजा मुझे खटखटाना नहीं पड़ा था। दरवाजा भिड़ा हुआ था।
दरवाजा खोलते ही रोशनी की उस फाँक में एक गुडीमुड़ी गठरी-सी खाट पर रखी मुझे दीखी।
”माँ जी!” मैंने टॉर्च जलाते हुए धीरे से पुकारा।
”कौन?” वृध्दा ने चौंककर अपने पैरों के पास रखी टॉर्च बड़ी तेज से उजालदी।
”काका नहीं आया”, उसने खाली खोखल आँखें मुझ पर गाड़ दीं।
”आता ही होगा…आ जाएगा”, मैंने ऍंधेरे में आँखें खोलकर डुबकी लगाने की कोशिश की। ”चलिए न उधर चलकर बैठते हैं…रोशनी में…मैं अभी जाग रहीहूँ।”
मुझे लगा था वह हुज्जत करेगी…इनकार करेगी…अड़ेगी पर वह पल-भर में ही कम्बल झटककर जमीन पर खड़ी हो गयी थी। उन्हें तत्पर देख मैं टॉर्च के सहारे ताला ढूँढ़ने लगी थी।
मुझे इधर-उधर हाथ-पैर मारते देखा तो बोलीं, ”क्या चाहिए?”
”ताला ढूँढ़ रही हूँ।”
”वहीं छोटी मेज पर रखा होगा…देखो न मैं कितनी पागल हूँ। भूल जाती हूँ। मेरी याददाशत कब की खो चुकी है।”
”यह सच नहीं है”, याद के चैतन्य का दंड भोगती उस आवांज को मैंने पूरे अधिकार से कहा।
उन्होंने नहीं सुना, नहीं माना। बोलीं, ”तुम चाहे जिससे पूछ लो। तुम्हें उन लोगों ने बताया ही होगा।”
”वे लोग? कौन लोग? बाहरी लोग? आप उनकी बातें मानती क्यों हैं?”
”मानना पड़ता है। आखिर इन्हीं के बीच तो सदा रहना है।” एक सपाट-जैसी स्वीकृति, जैसे रंग-भेद के माहौल में रहते श्यामवर्ण अपने-आप को भी ‘काला’ कहकर पुकारने लगते हैं।
ताला मैंने ही लगाया। बाँह से घेरकर उन्हें अपने साथ सटाया तो सारी देह में एक बिजली-सी दौड़ गयी। मन में भर्राता-सा आवेग…यह जो मेरी देह और बगल की खोह में पूरी तरह सिमट आयी हैं, यह कौन हैं?…क्या हैं?…हमारे इतिहास का अतिजीवित…अतिस्पन्दित अंश…इतना संचित, सुलभ और सुरक्षित।
लगा, रोशनी में आना उन्हें अच्छा लगा। सोफे पर टिककर बैठ जाना भी। वहाँ बैठते ही वह जल्दी-जल्दी पलकें झपकाती इधर-उधर देखने लगीं और आसपास के नएपन का मुआयना करने लगीं।
”चाय बनाती हूँ”-मैंने पूछने की बजाय उन्हें सूचना ही दी। नंजर बचाकर घड़ी भी देख ली। इस समय क्या वह उस चिन्ता से खाली हो गयी थीं?
देखा, अचानक ही वह ठिठुरने-जैसी लगी हैं। अपने दाँतों के बीच एक कँपकँपी को भींच रही हैं।
”आपको ठंड लग रही है?”
”नहीं तोऽऽ…” अपनी पतली-सी चुन्नी की लपेटन वह अपने गिर्द कसने लगी थीं।
अलमारी से शाल निकालकर उन्हें ओढ़ाया तो वह लज्जित-सी हुईं। ”देखो न! याद ही नहीं रहा कि मुझे शाल लेकर आना है। मैंने कहा नहीं था कि मेरी याददाश्त खो चुकी है…लोग ठीक कहते हैं।”
यह आवृत्ति यातनादेह थी। अपनी याद के खोने को खुद मान लेना और अपने पर ओढ़े फिरना, जबकि सच यह था कि वह स्मृति के गलियारे में वैसी-की-वैसी अविचल खड़ी थीं पर उनका आत्मबोध? बाहरी लोग उसे बना-बिगाड़ रहे थे। उनका पगला जाना ठीक ही था।
मैंने अपने को उनके घुटने के पास जमीन पर बैठ पाया-”मेरी बात सुनिए माँजी, ध्यान से सुनिए। आप कुछ भूली नहीं हैं बल्कि जितना आपको याद है, बहुत याद है।…वही तो असली तकलीफ है।”
”कैसे?”
मैं अटक गयी। जो मन में था उसे उनकी भाषा में समझाना मुश्किल लगा। कैसे समझाती कि जो भूल नहीं पाते, समय उन्हें माफ नहीं करता, क्योंकि ऐसे लोग उसकी राह में अड़ते जो हैं और समय है कि उसे हर पल वर्तमान बन जाने कीहड़बड़ीहै।
”क्या मतलब?”
”कोई मतलब नहीं। आप आराम से बैठिए। मैं चाय बनाकर लाती हूँ।”
चाय बनकर आयी तो वह एकाएक छलछला आयी थीं। ”मालूम है काके के पिताजी भी ऐसे ही किया करते थे। नींद नहीं आती थी तो लाची (इलायची) और लौंग की चाय बनाकर पीते थे। मुझे भी जगाकर पिलाते थे…चाहे मैं कितनी गहरी नींद में सोती होऊँ।”
उनकी आँखें एकदम स्थिर हो गयी थीं। वह मुझे फिर उसी सुरंग में दाखिल होती दिखी थीं जिसका उस पुरुष ने जिकर किया था। कमरे की भरपूर रोशनी में एक अद्भुत दीप्ति उनके चेहरे को लीपती उजालती दिखी थी।
उन्हें देखते लगा था हम सब तो मलबे में दबे हुए लोग हैं। यही एक चेहरा है जो इस मलबे में भी प्रज्वलित होकर चमक रहा है। मलबे से विद्रोह ठाने बैठाहै।
अच्छा ही था इस समय वह सब आशंकाओं से परे कहीं और डोल रही थीं, पर उनके बेटे की चिन्ता मेरे मन में दहशत बनकर धड़क रही थी।
उनकी आँख बचाकर मैंने घड़ी देखी। एक बज चुका था। बीस मिनट ऊपर जा चुके थे। घड़ी के हाथ तेजी से आगे भागते लग रहे थे।
अब?…अब?
अपनी दोनों हथेलियों में प्याले को प्यार से सँभाल वह चाय सुड़कने लगी थीं।
पहले दो घँट हलक में अभी उतरे ही होंगे कि उन्होंने सोफे पर चाय छलकाते प्याला नीचे जमीन पर रख दिया था।
”सुनो…सुनो, वह खड़का…उसका स्कूटर…लगता है काका आ गया है।”
वे झटके से उठे खड़ी हुईं और दरवाजे की ओर चलने लगीं। मैं एकदम उनके साथ…उनके पीछे।
अगले ही क्षण लगा था अगुवानी करने जाना व्यर्थ है।
स्कूटर का खड़का पहले तेज…फिर धीमा…फिर और धीमा होता पहाड़ियों में गुम हो गया था।
मैं सहम गयी थी। किसी दुर्घटना की आशंका मन में गाढ़ी होने लगी थी। हम दोनों के बीच पसरी चुप्पी भी अब सहमी लग रही थी।
मैंने चाय का प्याला उन्हें फिर से थमाया जिसे उनके स्तब्ध ध्यान ने लेने से इनकार किया।
मैं चाहती हूँ कोई वार्तालाप…कोई संवाद शुरू करना जिससे वह उस चुप्पी का किनारा छोड़कर आगे टहल आएँ…पर वह रिक्त-जैसी लगीं। अब चेहरे पर कोई चमक नहीं, विलापती-सी वीरानी पसरी थी। धँसी हुई कोटरों में स्थित गोल गङ्ढे, उनमें ऐसा थमा हुआ धुआँ…उनकी आँखों को जैसे इस बार मैंने ठीक से देखा।
इस समय यह चेहरा मुझे भयानक-सा लगा जैसे पसरती झुर्रियों ने उनकी खाल की सारी लुनाई सोख ली हो। वह पहले-जैसी अतीत के कक्ष में प्रज्वलित चेहरे की प्रतिच्छाया मेरे भीतर से भी गुम हो गयी।
एक असभ्य-सी चिन्ता ने मुझे दबोच लिया-वह अगर किसी अकस्मात् में अपने बेटे को खो देती हैं तो इस विभीषिका को अपनी पीठ के कौन से हिस्से पर ढोएँगी?…पिछले अभिशाप से मुक्ति पा लेंगी? याकि दोहरे भार से कुचली जाएँगी? इतना दम-खम इस पतली-सी काया में क्या है कहीं?
”आपको पाकिस्तान छोड़े कितने साल हो गये?” मैं एक निहायत बेवकूंफाना सवाल उनसे पूछती हूँ। जानती हूँ यह सवाल नहीं, संवाद की इच्छा है।
वह उत्तर नहीं देतीं। ओढ़े होने पर भी कँपकँपी में उतरती दिखाई देती हैं। मुख पर एक अड़ियल चुप्पी। यहाँ नहीं, कहीं और चले जाने का-सा भाव, जहाँ तक पहुँच पाना कठिन है।
घड़ी ने दो बजाये हैं। सुई बारह पर टिकने के बाद आगे चलने लग गयी है।
वह उठ खड़ी हुई हैं। जानती हूँ यह उठना नहीं बेचैनी है। दरवाजे को पटाक से खोलकर दरवांजे की चौखट से जा लगी हैं।
दरवाजा खुल जाने से हवा का एक तेंज चपाटा चीरता चला आया है जो उनकी देह से दस गुना ंज्यादा बलवान है।
”अन्दर ही बैठना ठीक होगा माँजी।”
”नहीं।” मेरी बात का उत्तर उन्होंने कड़ाकेदार ‘न’ में दिया है। वह चौखट से सिर टिकाये अविचल खड़ी है। मैं उनके पीछे। आगे-पीछे के क्रम में हमारे चारों पैर दरवाजे पर जम खड़े हैं।
अब और कुछ नहीं। कुशंका, कई परतोंवाला सन्नाटा और चेतना की झिर्रियों में सहसा ही सीढ़ियों पर थपथप की आवांज उभरी है…जो उस सन्नाटे को बड़बोली लगी है।
उनका काका एकाएक…आंखिरी सीढ़ी पर डगमगाता लैंडिंग पर अवतरित हुआ है। उसके पहुँचते ही शराब की गन्ध का एक तेज भभका हवा के कोटर में दाखिल हुआ है।
मेरे दरवाजे पर उन्हें इस तरह खड़े देख वह आग-बबूला हो गया है।
”तुस्सी ऐत्थे?…ऐस्स वेले?…ओपरे लोकाँ दे घर!” (आप यहाँ…इस समय…बाहरी लोगों के घर)।
अपनी साँस-में-साँस आने को पछाड़ते उन्होंने खीझ प्रस्तुत की-”अरे देर से आना था तो कहकर तो जाता।”
”क्यों…क्यों आफत आयी थी?…आसमान टूटा पड़ रहा था?…चलो सीधे…अपने घर।”
लड़के ने थूऽऽ पिच्च जैसी हिकारत से मुझे देखा है और माँ की दुबली-सी बाँह को अपने पंजे की जकड़ के हवाले किया है।
लैंडिंग पर तेज-तेज लपकता वह आगे चल रहा है। वह लिथड़ती-पिछड़ती बेटे के पीछे-पीछे घिसट रही हैं।
(हिंदी कहानी)
Download PDF (बाहरी लोग )
बाहरी लोग – Bahari Log