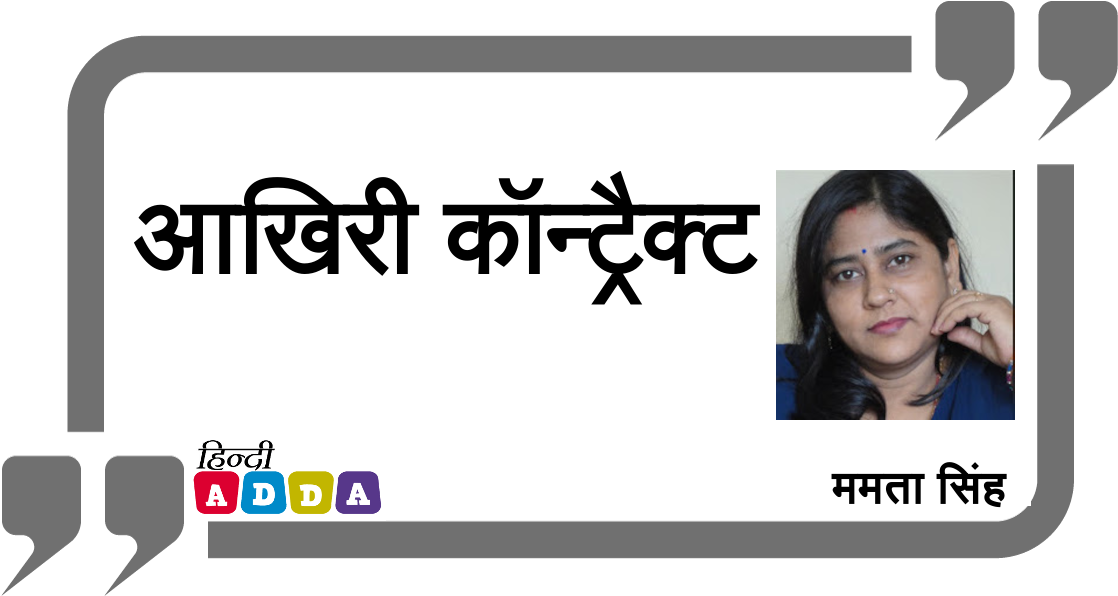आखिरी कॉन्ट्रैक्ट | ममता सिंह – Aakhiri Contract
आखिरी कॉन्ट्रैक्ट | ममता सिंह
कहते हैं इंतजार मीठा होता है, लेकिन यदि पूरी जिंदगी इंतजार बन जाए तो…यही सवाल बार-बार दस्तक दे रहा था कि मैंने झपटकर अपने दिल का कपाट बंद कर दिया, पर कहाँ। बंद करने की कोशिश में दिल की दीवार के भीतर के पट भी खुलते चले गए और मैं घनी सुरंग में गुम होती चली गई। कानपुर शहर की वह आखिरी शाम थी जब मोती झील के सघन बाग की डालियों ने झुक कर सलाम किया था, अमलतास के फूलों को सहला कर उसकी नरमी को अपनी मुट्ठी में समेट कर आगे बढ़ गई थी। सघन पेड़ों के बीच सूखी झील का सारा पानी मेरी आँखों में भर आया था, दुबारा-तिबारा बार-बार मुड़ कर देखा था कि पता नहीं दोबारा कब इस शहर में दाखिल होने मिलेगा।
मम्मी ने आफ़ताब के घर ईद की दावत पर जाते हुए कहा था “उनके यहाँ सिर्फ मुबारकबाद देना, कुछ खाना मत, यह लोग सिंवैयों में हड्डी का चूरा मिला देते हैं।”
– “केसर या पिसे हुए ड्रायफ्रूट की तरह हड्डियों का चूरा भी इनके यहाँ तैयार रखा रहता है क्या?”
उस रोज जब मम्मी को यह बात मैंने याद दिलाई तो वह खिलखिला पड़ी थीं।
– “मुस्लिम परिवार में दोस्ती तो क्या। हमें उनकी परछाईं से भी दूर रखा जाता था।”
…पर फिर भी मम्मी की दाद देनी पड़ेगी वह खुद को राजी कर अपने उस परिवेश को धता बताते हुए उन्होंने ‘ईश्वर-अल्लाह’ को शेक हैंड करवाया और मुझे आफ़ताब को अपना जीवनसाथी बनाने की आजादी दे दी। यह दीगर बात है कि हमें उस शहर को अलविदा कहना पड़ा।
मैंने घड़ी की ओर देखा ‘मूवर्स एंड पैकर्स’ ने टी-ब्रेक लिया था। मैंने भी अपनी स्मृतियों से ब्रेक लिया…
“बेंगलुरु में ठंड कहाँ पड़ती है? इतने सारे गर्म कपड़ों का क्या होगा”…सोचते हुए मैंने वार्डरोब से आखिरी साड़ी तह करने के लिए निकाली और बहुत सारे लम्हे भी तहाने लगी… लेकिन साटन की साड़ी को जितना ही तहाओ, फिसल कर खुल ही जाती है। मेरा मन भी साटन की साड़ी की तरह फिसल कर अतीत की गलियों में ही विचर रहा है। शहर कोई भी हो तंगदिली हर शहर में होती है, मुंबई में भी तंगदिली की बड़ी इमारतें हैं।
“घर किसके नाम पर होगा?” – ओनर ने पूछा था।
“दोनों के”
“कॉन्ट्रैक्ट मैडम के नाम से बनवा लीजिए… आपके नाम से सोसाइटी ऑब्जेक्शन करेगी” – कहते हुए मकान मालिक अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर गोलाई से घूम गया था।
ठीक उसी वक्त मेरे कानों में मम्मी की पुरानी आवाज ने डंक मारा था – “बेटी हम आफ़ताब को घर-जमाई बना लें, तो भी हमारा समाज उन्हें सम्मान के नजरिए से नहीं देखेगा।”
तमाम जिरह करने के बावजूद मकान मालिक ने घर देने से इनकार कर दिया। मेट्रोपॉलिटन शहर का यह मेरे लिए पहला झटका था। इस महानगर में भीड़ का महासागर पनाह पाता है, पर धर्म और संप्रदाय की कुछ जलकुंभियों ने पूरे सागर के पानी को खारा कर रखा है। जैसे-तैसे एक मित्र की मदद से एक लाख डिपॉजिट, दो महीने का किराया एडवांस, ग्या रह महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर हमें अस्थायी मकान मिल गया। उसी एक ही कमरे में बेड, अलमारी, ड्रेसिंग, ड्रॉइंग-रूम के सामान को ठूँस-ठूँस कर सजा दिया गया। फिर शुरू हुई मकान की असली तलाश।
वह झमाझम बारिश का भीगा दिन था। मैं और आफ़ताब बाइक पर सवार होकर एस्टेट-एजेंट के पीछे-पीछे मीरा रोड भाइंदर से लेकर बोरीवली, कांदीवली, मालाड, मालवणी तक के चक्कर काटे। उस रोज हमने दस से पंद्रह घर देखे जिनमें से सिर्फ एक ही मकान में धर्म की दीवार नहीं थी। बकौल ब्रोकर मकान-मालिक धर्मनिरपेक्ष है और मीटिंग करने को तैयार है। 2-बी-एच. का एक आयताकार घर, दीवारें सीलन से मरियल पीली थीं। हॉल के नीचे की दीवारों से पपड़ी झड़ रही थी, बाईं ओर बाथरूम… उसी के सामने रसोई और लगा हुआ जरा सा गलियारा, फिर सीढ़ी चढ़ो तो मास्टर बेडरूम और छोटा बेडरूम, एक तरह का अजायबघर… छोटा कमरा बंद था जिसका हैंडल घुमाया तो चूँ-चर्र की आवाज हुई, साथ ही एक कनखजूरा इठलाता हुआ दीवार की ओर चढ़ने लगा…।
…शी… मेरे मुँह से निकली आवाज को चालाक ब्रोकर नजर-अंदाज करता हुआ बोला – ”व्यू देखो मस्त है”। उसने ‘वॉल-साइज’ विंडो खोल दिया। खिड़की खुलते ही सघन पेड़ की डालियाँ, जो काँच से सटकर मुड़ी हुई थीं, वे खिड़की के भीतर हरहरा कर घुस आईं और लहराने लगीं, उन्हें जैसे खुला आकाश मिल गया हो, मैंने उन पत्तियों को छूकर सहलाया तो एक बुलबुल जो बगल की डाली पर बैठी थी फुर्र से उड़ गई। मैं सोचने लगी यह चिड़िया ना नमाज पढ़ती होगी, ना पूजा करती होगी, ना ही प्रेयर… फिर इसका नाम रखना हो तो क्या रखा जाए? अगर इन चीजों में धर्म का बँटवारा हो जाए, तो इनका उड़ना दूभर हो जाए… कैसे पता चलेगा कि आसमान का कौन-सा इलाका किस मजहब का है।
‘पेंटिंग का एक कोट मारोगे तो घर सॉलिड झक्कास हो जाएगा, इधर डिपॉजिट का भी लफड़ा नहीं… सिर्फ 2 साल का किराया एक साथ देना होगा और टेंशन फ्री’ – ब्रोकर की आवाज मेरे कानों में झन्न से बजी थी।
‘इस सीलन भरे दड़बे में रहने से बेहतर है कि हम मालवणी साइड, गणेश नगर के मुस्लिम इलाके में रहें’ …मैं बुदबुदाई थी।
“उधर आपके नाम का लफड़ा होगा बेन, मैंने कई मुसलमान भाय को गणेश नगर में घर दिलाया है, उन लोगों की सुबह भोंपू पर अजान से होती है, आपको जमेगा बेन? …अपना आफताब भाई तो एकदम क्लीन… अपुन का माफिक है, वो लोग आपको ‘विदाउट बुर्का’ एक्सेप्ट करेगा”? …कहते हुए ब्रोकर ने फाफड़ा जलेबी की प्लेट हमारी ओर सरका दी। कहीं उसके हाथ आया शिकार चंगुल से छूट न जाए, इस गरज से वह हमें पटा रहा था। मेरी आँखों के आगे गणेश नगर का वह इलाका घूम गया जहाँ गलियों के बीचों बीच कुकड़ू-कूँ करती मुर्गि़याँ फुदकती रहती हैं, जगह-जगह कचरे का ढेर, हर नुक्कड़ पर लटकता हुआ मीट। उस की दुर्गंध जैसे मेरे नथुनों में घुस गई हो, बुरका पहने उर्दू-दाँ औरतें… कबाड़ी की दुकानें… गली के मुहाने पर सायकल सुधारने की दुकानें, मैले-कुचैले कपडे पहने अधनंगे बच्चे… बुर्के वाली औरतें घर की बेल बजा कर तोहफे में कभी बुर्का तो कभी नसीहत की घुट्टी दे जाएँगी.. अरे मैं यह सब क्या सोच रही हूँ?
हमारी जिंदगी ग्यारह महीने के कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील हो गई थी… हर आठवें-नौवें महीने बाद घर की तलाश की मुहिम शुरू हो जाती। उस रोज मेरा भयंकर सिर दुख रहा था। वजह थी कई रातों की नींद का गायब रहना। दिन भर कंपनी में ज्यादा काम करना, फिर गृहस्थी और सबसे ज्यादा पीड़ादायक थी मकान की खोज… स्ट्रेस और थकान से बेहाल… उस दिन दफ्तर से जल्दी निकल गई यह सोच कर कि घर पहुँचते ही चादर तान कर सो जाऊँगी। आज घर देखने की मुहिम कैंसिल… हालाँकि घर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, मकान मालिक की दया याचना पर कुछ दिनों की मोहलत मिली है।
अपने आप से गुफ्तगू करती हुई मैं कब अपने फ्लैट के दरवाजे पर पहुँच गई, पता ही न चला। इनसान को जब जिस चीज की बेसब्र तलब हो, वह उस वक्त कतई नहीं मिलती। मैंने देखा घर के ऑटोमेटिक लॉक के ऊपर लगी कुंडी पर फँसा एक ताला मुँह चिढ़ा रहा है।
“अरे..!!! मैंने तो ताला लगाया ही नहीं था… कहीं आफ़ताब ने तो नहीं !!!
…यह तो हमारा ताला है ही नहीं, फिर??”
…कई बार ताले को खींच कर देखा, पीछे मुड़ी, बाकी के तीनों फ्लैट बंद थे। किससे पूछूँ, कौन हो सकता है, वजह क्या होगी, कहीं नल तो नहीं खुला छूट गया…? घर के भीतर कोई हादसा तो… नहीं-नहीं, दरवाजा बाकायदा बंद, सुरक्षित था। फिर यह ताला किसने जड़ा होगा। वॉचमैन से पूछने के लिए गेट पर आई, तो देखा वॉचमैन वहाँ से नदारद। सर में दर्द से जोरदार सायरन बज रहा था, क्या सोसाइटी वालों ने यह ताला लगाया होगा? या फिर मिस्टर राठौर ने? लेकिन उन्होंने ही तो कुछ दिन और रहने का आश्वासन दिया था फिर…? तो क्या मकान मालिक ने हमसे झूठा वादा किया? आफताब भी नहीं आए हैं। जी चाह रहा था खूब जोर से रोऊँ… क्या करूँ पुलिस में कंप्लेन्ट करूँ लेकिन पुलिस भी तो उनकी खास है।
निश्चय ही यह ‘तिलकधारी’ का काम होगा, वॉचमैन खैनी मलता हुआ सामने निर्विकार भाव से खड़ा था… “मैडम उधर हमारी झोपड़ी है, वन रूम किचन। आप चाहें तो उधर दो-चार दिन रह सकती हैं” …उसकी आत्मीयता उस वक्त तेजाब का काम कर रही थी। आखिरकार आफताब आए, ‘तिलकधारी’ जो सोसाइटी का सेक्रेटरी था, हम उससे मिलने गए। भयानक सिर दर्द का असर तो मेरे चेहरे पर था ही, रोई भी थी पर उस वक्त अधिक कातर आवाज में और ज्यादा विनम्रता पहन मैंने उससे अपने किराए के फ्लैट की चाबी माँगी।
“चाबी तो नहीं मिलेगी” वह तो जैसे जंग पर आमादा था आफ़ताब और उसके बीच जम कर झड़प हुई सोसाइटी के दूसरे मेंबर्स ने बीच बचाव जरूर किया लेकिन वह ‘तिलकधारी’ की ही तरफदारी कर रहे थे। “मैं औरत जात से बात नहीं करता” …मेरी कही हर बात को इग्नोर करता हुआ वह बोला। पुलिस थाने से लेकर मैंने महिला आयोग तक जाने की धमकी दे डाली, फिर भी वह टस से मस नहीं हुआ। दरअसल ऐसे तिलकधारियों की हर जगह खास जुगाड़ होती है। हाँ… मेरी धमकियों से इतना फायदा जरूर हुआ कि उसने अपने झगड़ने का सुर तार-सप्तक से मंद्र-सप्तक तक ले आया। लेकिन हमारे फ्लैट की चाबी नहीं दी तो नहीं दी। उस रात हम ने किस-किस को फोन नहीं किया, पर सब ने इसे निजी विवाद का नाम देकर हथियार डाल दिए। अंत में बेबस-लाचार हम उसी मित्र के घर पनाह लेने को मजबूर हुए जिसके परिचय से हमें यह घर मिला था। उसने भी मकान मालिक से बात करने का प्रयास किया, पर बात नहीं बनी। मेरे पति का नाम आफताब है इसलिए हम यह वनवास काटने को अभिशप्त थे। मैंने अपने सिर को दुपट्टे से कसकर बाँध लिया था मन में विचारों का मंथन और सर का दर्द शबाब पर था…।
“हम पूरब को शुभ दिशा मानते हैं वह पश्चिम को, उनका और हमारा कोई मेल नहीं… समाज का हर तबका इन्हें हिकारत से देखता है, लोग तुम्हें भी देखेंगे”… मम्मी के वाक्य हवा में उड़ते हुए आँखों में, फिर दिमाग में पनाह पाने लगे थे… “विधर्मी शादी से हमेशा कष्ट ही मिलता है, जिंदगी के हर मोड़ पर इसका एहसास होगा तुम्हें। इनकी और हमारी पूरी संस्कृति अलग है, हम खाली पेट पूजा करते हैं, वे खाना खा कर नमाज पढ़ते हैं…”। इन विचारों को परे भगाने की गरज से मैंने अपनी आँखें कसकर मीच लीं, करवट बदल कर सोने की कोशिश करने लगी।
“यह मुझे क्या हो रहा है…”
तभी आफताब की हथेलियों का ऊष्म स्पर्श और फिर मैं ग्लेशियर की तरह देर तक पिघलती रही, उसके प्यार के जल से देर तक भीगती रही। खौफनाक विचारों का भँवर आँखों के सामने गोल-गोल नाच रहा था…कहीं ‘तिलकधारी’ …बदमाशों की टोली लेकर यहाँ ना पहुँच जाए, कहीं वह हमारा सारा सामान घर से बाहर न फेंक दें कहीं वह तोड़फोड़ ना करे। मैंने महसूस किया आफताब की भी खुली आँखों में भी डर की सुनामी तबाही मचाए थी।
अगली शाम मकान मालिक से मीटिंग हुई, ग्यारह महीने का किराया एडवांस लेकर उसने हमें कुछ दिन और उसी मकान में रहने की इजाजत दे दी। कुछ दिनों बाद सोसाइटी का वही ‘तिलकधारी’ नगर निगम के चुनाव-प्रचार में मंच से जाति-धर्म और सांप्रदायिकता के खिलाफ भाषण दे रहा था… “हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब आपस में भाई-भाई”। लोगों के मन में उसके भाषण से संवेदना के सूखे तालाब में भी कमल खिल रहे थे। जी चाहा था उससे माइक छीन लूँ और चिल्लाकर बोलूँ – “झूठा है यह, फिरकापरस्त है यह, इसी की वजह से हम आज भी बेघर हैं” …लेकिन सारे शब्द हलक में ही घुट कर रह गए।
“इस तरह हम कब तक भटकते रहेंगे चलो अब ग्यारह महीने के कॉन्ट्रैक्ट से मुक्ति पाकर अपना एक स्थायी आशियाना बनाएँ” …आफ़ताब की यह आवाज सुरंग में ‘इको’ की तरह मेरे कानों में गूँजी थी। उसने मेरे हाथों को अपनी ओर खींचते हुए हथेली पर लिखा था – “…घर”। खुद को हवा की तरह हल्का पाकर आफताब के कंधे पर मैंने अपना सिर रख उसकी शर्ट पर दो पारदर्शी बूँदें टाँक दी थीं।
कुहासे से ढके कॉन्क्री ट के इस वीरान जंगल में आफ़ताब ही वह फूल था जिसकी मुस्कान की पंखुड़ी मुझे गुदगुदाती थी। इस जंगल में हम दोनों एक-दूसरे का हाथ थामे कठिनाइयों के पहाड़ पर चढ़ते जा रहे थे। हमने भी पहाड़ों की नर्म धूप की तरह रेशमी मुलायम घर खरीदने का सपना बोया और उसके अँखुवाने की प्रतीक्षा करने लगे।
असित देसाई मीरा रोड के इलाके का एक बड़ा ब्रोकर था। उसने कई बिल्डिंगों में घर दिखाने के लिए खूब चक्कर कटवाए। फ्लैट पसंद आ जाता तो बिल्डर से मीटिंग की तारीख का इंतजार। अंत में जवाब यही मिलता कि वह किसी गुज्जु परिवार को प्रेफर करेगा।
“असित भाई, पहले ही आफताब का नाम बता दिया कीजिए, अगर बिल्डर राजी हो, तभी घर दिखाइए” आजिज आकर मैंने ब्रोकर से कहा था – “मैं आप लोगों को रितेश भाई शाह से मिलवाऊँगा, तेओ बहू नेकदिल माणस छे… बहु संघर्ष करीने एटला मोटा व्यापारी बणया छे।”
सेक्टर 8 में रितेश भाई शाह की बनाई दो बिल्डिंगें… खूबसूरत गार्डन, सी-व्यू, मैंग्रोव्ज, जहाँ कभी न खत्म होने वाला हरापन है। “आफ़ताब मेरा तो दिल आ गया है इस फ्लैट पर” …आफ़ताब ने पैंट की जेब से रूमाल निकालकर माथे का पसीना पोंछते हुए बोला – “असित भाई बिल्डर से मीटिंग फिक्स करो”
“…फ्लैट में ईद पर बकरा तो नहीं काटोगे” – टेबल पर हाथ से ठक-ठक कर काटने का इशारा करते हुए रितेश भाई ने पूछा था।
“रितेश भाई ईद नहीं बकरीद पर होती है कुर्बानी, इनको मजहब से कोई लेना-देना नहीं” – मैंने तपाक से बोला था।
“शिवांगी बेन आप बाद में धर्म बदलकर बुरका तो नहीं पेनोगे ना”? आफ़ताब के चेहरे पर झल्लाहट साफ दिखाई दे रही थी।
“मेरे को प्रॉब्लम नहीं है मैं खाली सोसाइटी के लिए पूछता हूँ… वो क्या हे ने, 80 परसेंट फ्लैट बिक चुके हैं, इसके लिए उनसे पूछना पड़ेगा, वरना आपको बाद में तफलीक हो जाएगा।”…
आफ़ताब के चिंतित और तमतमाए चेहरे को पढ़ते हुए मैंने कहा “आप फ्लैट-ओनर पर प्रेशर डाल सकते हैं।”
“बेन! तमे हिंदू छे, आ भाई साब के नाम माँ प्रॉब्लम छे। मोटा भाई आप नाम बदल लेवें या बेन के नाम पर एग्रीमेंट कर लेवें” …कहते हुए पान मसाले का पाउच चीरकर मुँह में भर बाकी बातचीत उन्होंने मुँह में भरी पीक के साथ की। उसके पीक का छींटा मेरे ऊपर ना आ जाए, इस डर से झट मैंने अपनी कुर्सी टेढ़ी कर, जरा दूर खिसका ली।
“आपको कितनी किश्त में कितना पैसा देना होगा, इसकी पूरी डिटेल इस कागज में है, आप अभी पाँच लाख टोकन मनी दे दो” …पेंसिल से लिखे हुए हिसाब का कागज थमाते हुए रितेश भाई शाह बोले।
बजट देखकर हम दोनों को जैसे बिजली का शॉक लगा हो लेकिन फिर फंड और लोन की इलिजिबिलिटी याद करके थोड़ी आश्वस्ति हुई।
आधी रात के सन्नाटे में जब झींगुरों का समूह-गान सुनाई दे रहा था, शुक्ल-पक्ष की चटख चाँदनी जंगले से छन-छन कर टुकड़े-टुकड़े बिखर कर झिलमिल कर रही थी, तभी नींद सपनों की उँगली थाम मुझे उस जगह ले गई जहाँ बासंती फूलों की घाटी में फूलों के झुरमुटों के बीच छोटी-सी सुंदर झोपड़ी थी, झोपड़ी के पीछे बहता झरना… झरने पर पड़ती चाँदनी की परछाईं को शिशु की मानिंद पकड़ने की मेरी कोशिश… पेड़ों के कतार के बीच हैमक… हैमक से बाहर आने की कोशिश की और खूबसूरत नजारों को आँखों में कैद करने के लिए आँखें कस के मिचमिचाई तभी एक क्रूर मच्छर ने डंक मारा, हड़बड़ा कर मैं उठ बैठी। हवा के झिंगोले से मैं धम्म से गिर पड़ी। ख्वाबों की नायाब दुनिया तबाह हो गई।
“…आफ़ताब! बिल्डर ने टोकन-मनी की रसीद नहीं दी है… कहीं वह मुकर गया तो…?”
“इतना बड़ा बिल्डर, उसके लिए यह छोटी-मोटी रकम है… सो जाओ” कहते हुए आफ़ताब खर्राटे भरने लगे।
“सुनो अगर सोसाइटी ने ‘ना’ कर दिया तो क्या बिल्डर हमारा टोकन मनी लौटाएगा?”
“उफ्फ… सोने दो ना। आधी रात को चिंता के पहाड़ पर ट्रैकिंग क्यों कर रही हो? सुबह बात करेंगे” …आफ़ताब खीझते हुए हुए फिर नींद की आगोश में चले गए।
“सुबह…? मुंबई रात की बाँहों में जाती है कि बस चंद लम्हों में ऊँची इमारतों के पीछे छुपा सूरज छतों पर अपना आँचल पसार देता है। बेघर लोगों के लिए रात और दिन सब बराबर है। पर हाँ, रात हमारे लिए बड़ी डरावनी होती। दरवाजे पर हुई हवा की दस्तक या खिड़की से बजी हवा की सीटी की आवाज से हम चौंक कर बैठ जाते, रात में कभी बेल बजने पर आफ़ताब किचन में रखा रॉड हाथ में लेकर दरवाजे से सटकर आहट लेते, मैं आफ़ताब की बाँह कसकर पकड़ लेती, झिरी से झाँक कर देखते, कभी वॉचमैन होता तो कभी पड़ोसी।
अगली शाम मेरे मोबाइल पर ‘ब्रोकर मीरा रोड कॉलिंग’ रिंगटोन बजी, मैंने दौड़कर मोबाइल उठाया “हैलो… हाँ कर दिया ना बिल्डर ने? हम जल्द ही ब्लैक मनी का इंतजाम कर लेंगे” – मैं एक साँस में कह गई।
“मेरे पास बिल्डर का वापस किया हुआ आपका टोकन-मनी रखा है, आप आकर ले जाओ” चालाक ब्रोकर की आवाज में उस वक्त कोई धूर्तता नहीं थी, बल्कि घर न दिला पाने की विवशता थी। आखिर उसे भी तो ब्रोकरेज की मोटी रकम मिलनी थी। हमारी मोहब्बत का सेमल की रूई की तरह नरम मुलायम आशियाना बनने से पहले ही ढह गया, पर हम नहीं टूटे, उस जमाने से हमारी जंग जारी रही जहाँ खून के रंगों में ही भेद किया जाता है।
“रफीक भाई! हमें हिंदू इलाके में घर चाहिए” – आफ़ताब के कहे इस वाक्य पर ब्रोकर रफीक का चेहरा हैरत से भर गया।
“इस माहौल में आप हिंदू इलाके में रहना चाहते हैं?”
“मेरा मतलब है साफ सुथरा इलाका… और हाँ मस्जिद से जरा दूर रहे तो बेहतर।”
मेरे चेहरे पर चिंता की लकीरें और बेहाली खामोशी से कुछ कह रही थी, मौके का फायदा उठाते हुए रफीक भाई आत्मीय होकर बोले – “तसल्ली रखिए आपा, हम आपको बेहतरीन घर दिलाएँगे, गोया आपके नाम की अड़चन आएगी। आपने इमाम से निकाह पढ़ा है ना…? क्योंकि हमारे यहाँ बगैर निकाह के शादी को हराम मानते हैं। नाम बदलकर क्या रखा था…? उसी नाम से आप आफ़ताब भाई की नॉमिनी बन जाइए।”
“दुनिया में क्या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, जो मजहब के कोठार में कैद न हो…?” मुझे मजहब के इतने सारे स्पीड-ब्रेकर से घुटन-सी होने लगी थी, गले में पहने ताबीज और श्री-यंत्र निकाल कर मजहब के खाँचे से खुद को आजाद कर लेने का जी चाहा था। मम्मी की बात ने यहाँ भी डंक मारा – “इस बेमेल विवाह से हमेशा सवालों के घेरे में रहोगी, पग-पग पर तुम्हें एहसास कराया जाएगा, तुम एक मुसलमान की बीवी हो”।
“बुरा ना माने तो एक बात कहूँ आपा…?”
ब्रोकर रफीक भाई की आवाज ने मुझे यादों के बयाबाँ से बाहर निकाला था
– “निकाह के बाद बेगम अपने शौहर की हो जाती है। उसकी मर्जी और मजहब के मुताबिक वह चलती है।”
“आप यह टिकली-विकली क्यों लगाती हैं? हमारे मजहब में यह कुफ्र है।”
“रफीक भाई! मेरी तमाम हिंदू फ्रेंड्स टिकली नहीं लगाती और तमाम मुस्लिम सहेलियाँ बुर्का नहीं पहनतीं, वह मेरे साथ मंदिर जाती हैं… आप घर के बारे में बात कीजिए ना।”
“खुदा कसम आपा! अपनी सोसाइटी में आपको शानदार, नायाब घर दिलवा दूँगा, वहाँ न मजहब का किला होगा, न सवालों की बौछार… ना ही कोई आपको तंग करेगा बस… आप अपना नाम शुभांगी से शगुफ्ता, शायना, शमा वगैरह रख लीजिए।”
आफ़ताब से इसी ब्रोकर ने पिछली बार बोला था – दूसरे मजहब में शादी करने से जन्नत का दरवाजा बंद हो जाता है। मैं अपना नाम बदल लूँ तो स्वर्ग का किवाड़ मेरे लिए बंद नहीं होगा…? तनाव के इन पलों में भी मैं मुस्कुरा पड़ी थी, रफीक भाई ने उस वक्त इस्लाम कुबूल करने के तमाम फायदे बताए, लेकिन अपनी बात का हम पर कोई असर ना होता देख, उन्होंने हमें कला नगर के पॉश इलाके में मिस्टर राणे से मिलवाया, जिनकी बिल्डिंग में मिली-जुली कम्युनिटी थी। हमारे घर का सपना वहाँ आखिरकार मुकम्मल हुआ।
सदियों से बोए जा रहे जाति-धर्म के बबूल का वहाँ की सोसाइटी वालों ने बड़ी आसानी से सफाया कर दिया, आफ़ताब और हम सोसाइटी के मेंबर बन गए, कुछ दिन तक हम उनके लिए अजूबा बने रहे पर फिर महिलाओं की किटी पार्टी मेरे बगैर अधूरी रहने लगी। “तुम भी नमाज पढ़ती हो? क़ुरान में होता क्या है? क्या रामायण महाभारत और भगवद्-गीता की तरह ही पाक होता है क़ुरान? ईद मुहर्रम तुम कैसे मनाती हो? तुम वेजिटेरियन हो”? …इस तरह के तमाम सवालों से पड़ोसिनें हमारी जिंदगी में कोई न कोई मसाला ढूँढ़ती रहतीं। हालाँकि हम स्वीकार कर लिए जाने के बावजूद अस्वीकार ही रहे। हमारे रहन-सहन हमारे सौहार्द से वे प्रभावित होकर हमें एक सामान्य इनसान की तरह ग्रहण करते, लेकिन उनके मन में बँधी धर्म की जंजीर उन्हें कस के जकड़े रहती, फिर भी महफिल जमाने वाली औरतों ने अपने मन से जाति-धर्म के जाले काफी हद तक साफ किए और उनकी शिकायत भरी निगाहों में थोड़ी आत्मीयता घुल गई। हम होली की गुझिया, ईद की सिवइयाँ साथ-साथ खाने लगे, इसके बावजूद एक अस्वीकार्य मुसलमान की बीवी को स्वीकार कर भी लिया जाए तो भी डर का कोहराम भीतर मचा ही रहता है।
उस रोज सर्दी की गुनगुनी नर्म धूप काले धुआँधार बादलों में तब्दील हो गई थी, जब कानपुर की हृदय विदारक घटनाओं से अखबार के पन्ने अटे पड़े थे और मैंने रात भर पलकें तक नहीं झपकाई थीं, आँखें मूँदते ही जो देखा नहीं वो दिखाई देने लगता था…।
एक गर्भवती स्त्री दया और करुणा की भीख माँग रही है। सब वहशी बन गए हैं। फिरकापरस्ती के जुनून में वे… स्त्री के पति को निर्ममता से पीट रहे हैं, वह अधमरा हुआ जा रहा है, उसके बदन से खून का फव्वारा बह रहा है और जैसे उस गर्भवती स्त्री के शरीर का सारा खून सूखा जा रहा हो…। अपने पति की पीड़ा को महसूसती वह बेहोश हो गई है, उसका बच्चा उसके गर्भ में ही अपने पिता की चोट से सहम जाता है, छटपटा कर चीत्कार उठता है और गर्भ में ही दम तोड़ देता है। पति की मर्मान्तक पीड़ा, तड़प, उसकी छटपटाहट को अपनी साँसों में महसूस करती… अपने अजन्मे शिशु को खोने की विकल पीड़ा से कराहती, रोती, सिसकती वह स्त्री ‘मुझमें’ तब्दील हो गई हो और अधमरा होता उसका पति आफ़ताब की काया बन गई हो…।
मेरे भीतर से जोरदार चीख निकली, लेकिन घुटकर कलेजे के भीतर ही दब गई। मैं पसीने-पसीने थी। आफ़ताब ने मेरे बालों में उँगलियों से कंघी फिराई, मुझे पानी पिलाया। मैं कसकर उसके सीने से चिपट गई।
“वे…वे…कहीं यहाँ तो नहीं आ जाएँगे? उन्हें कहीं तुम्हारा नाम न पता चल जाए…”
“…शुभांगी… कुछ नहीं होगा। यह घटना कानपुर के गाँव में घटित हुई है। बेफिक्र रहो, यहाँ कुछ नहीं होगा”।
“क्यों बहरामपाड़ा में…? भिवंडी और ठाणे में, जो आग दहकी वह…?” मैंने सुबकते हुए कहा था। कानपुर जैसे तमाम इलाकों की आग महानगर में भी धू धू करने लगी थी। उस रात पच्चीस या तीस लोगों का हुजूम ऊँची आवाज में नारे लगाते हुए सड़क पार कर रहा था। आफ़ताब वॉल-साइज विंडो का पर्दा जरा-सा सरका कर साँस रोके उन्हें देख रहे थे। मैंने पहली बार आफ़ताब को आसमान की ओर उँगली उठाकर कुछ कहते देखा था, रसोई में मर्तबान में शीर-खुरमा रखकर पहली बार फातिहा पढ़ते देखा। उन्होंने अमन-चैन के लिए फातिहा पढ़ी होगी। मैंने मन-ही-मन दुर्गा माता से निवेदन किया – “हे देवी माता, अल्लाह के रसूल से कहकर आफ़ताब की दुआ जरूर क़ुबूल करवा देना” …पर खुशामद-पसंद अल्लाह और भगवान भी उन्हीं की सुनते हैं, जो उनकी नियमित रूप से इबादत और प्रार्थना करते हों। केसरिया पोशाक वालों का हुजूम कई दिनों तक अपनी एकता और भाईचारे के डंके पीटता रहा, कई दिन तक वे ऊँची आवाज में कुछ बोलते हुए हमारे घरों के सामने से गुजरते, धीरे-धीरे उनकी आवाजें मद्धम पड़ जाती, पर मेरे कानों में वो सब साँय-साँय बजता रहता, उनके शोर में बस इतना ही समझ में आता – “गौ मांस का हम बदला लेंगे, इस इलाके में सिर्फ हमारे घर होंगे, सारे बूचड़खाने जला दो, यह हमारा देश है यहाँ सिर्फ हम रहेंगे”।
उन्हीं दिनों एक रात मैं घर लौट रही थी, ऑटो रुका, भारी जाम के बीच सामने से उनका काफिला झंडे लहराता हुआ चला आ रहा था… उफ्फ। वे लाठियों से वार करके दुकानें बंद करवा रहे थे, उनके खौफ से लोगबाग तितर-बितर होकर घरों में और दुकानों के भीतर पनाह ले रहे थे, मेरे माथे पर पसीने की बूँदें चुहचुहा आईं, झुलसती गर्मी में भी हाथ बर्फ हो गए, ऐसा लगने लगा कि वह सारे लोग मुझे पहचानते हैं, आफ़ताब को जानते हैं। बस अब्भी वे आएँगे, मेरे बैग की तलाशी लेंगे, मेरे पति का नाम पूछेंगे, और फिर… उफ… मैंने भगवान, खुदा, जीजस-क्राईस्ट सबको पुकार लगाई… अगल-बगल देखा तो इक्का-दुक्का ही वाहन थे, लोग बहुत कम थे, मेरी धड़कन राजधानी एक्सप्रेस के इंजन की तरह शोर कर रही थी। अपना फोन मैंने झटपट म्यूट कर पर्स में छुपा लिया। कहीं एन वक्त पर ‘आफ़ताब कॉलिंग’ न दिख जाए उन्हें… माथे पर पसीना पोंछने के लिए हाथ फिराया तो याद आया आज ही वेस्टर्न ड्रेस पहना है, आज ही बिंदी नहीं लगाई जो आज भी अपने देश की संस्कृति का विशेष प्रतीक है। फटाफट अपने पर्स से एक बिंदी का पत्ता निकाला और जल्दी से अपने माथे पर बड़ी-सी बिंदी चिपका ली, लिपस्टिक से अपनी माँग पर सिंदूर की रेखा खींच ली, यह मैंने बड़ी सतर्कता से किया कि कहीं वह ऐसा करते मुझे देख ना ले और उन्हें संदेह ना हो जाए कि मैं एक मुसलमान की पत्नी हूँ। पिछले दंगों में ऐसा ही तो हुआ था, अपने बचाव के लिए मुस्लिम महिलाएँ भी माथे पर टिकली लगाकर घर से बाहर निकलती थी लेकिन पुरुषों के पैंट…। छी छी… यह कैसी बातें मैं याद कर रही हूँ, उन्हें क्या पता मैं कौन हूँ और मेरा पति कौन है… उस दंगे के बाद बहुत समय तक मुस्लिम इलाके से गुजरते हुए हिंदू औरतें अपने बचाव के लिए बुर्का पहन कर जातीं… धीरे धीरे उनका काफिला शोर करता हुआ, नारे लगाता हुआ आगे निकल गया और घर पहुँचकर मैंने आफ़ताब को उस रोज घर से बाहर निकलने नहीं दिया था।
बांद्रा और कला नगर के बीच में ही बहराम पाड़ा पड़ता था, वहाँ से गुजरते हुए मन में दहशत होती… मोटर पार्ट की दुकानें… ऑटो के गैराज… बेकरी, सैलून, चाय और पान की टपरियाँ, उन दुकानों में तैनात लंबी दाढ़ी वाले मौलानानुमा दुकानदार जिन्हें देख कर ही मन खौफजदा हो जाता… उन गलियों में तेज आवाज में बजती हुई कव्वालियाँ… गलीनुमा तंग सड़क और दुकानों के बीच से गुजरते हुए अकसर ही वो हादसा याद आ जाता, जो शालू के पति के साथ हुआ था। बताते हुए उसके आँसू ही नहीं थमते थे, उसका पति टाटा कंपनी में वसूली का काम करता था, बार बार पैसे माँगने पर भी दाढ़ी वाले व्यक्तियों का गिरोह गाड़ी की रकम वापस नहीं कर रहा था। एक दिन आपस में कुछ कहा-सुनी हुई और उन्होंने मिल कर शालू के पति के पैरों में, सर में रॉड फँसा कर मारा, अधमरा कर उसे झाड़ियों में फेंक आए थे, कोई फरिश्ता उधर से गुजर रहा था, उसने कराहने की आवाज सुनी… फौरन अस्पताल पहुँचाया और उसकी जान बचाई…। दुकानों में होती खटर-पटर से, छेनी काटने की आवाज मात्र से लगता कि वही रॉड बस मेरे सर पर अभी गिर जाएगी। हमारे घरों के आसपास भी दहशत का साया हर वक्त मँडराता रहता। सुबह और शाम आती हुई अजान की आवाज सुकून की बजाय खौफ पैदा करती…।
दंगे के तीसरे दिन कंपनी के काम से मुझे बाहर जाना पड़ा। मैं आफ़ताब को भी अपने साथ ले गई। चंद रोज बाद जब लौटे, तो काफी हद तक शहर में शांति थी। जगह-जगह बूचड़खानों के स्थान पर चमन बन गए थे, सफाई अभियान जोरों पर था। देख कर दिल खुश हुआ। मीट की एक भी दुकान कहीं नजर नहीं आ रही थी। बेचारे जीव-जंतु भी उन्हें दुआएँ दे रहे होंगे। अपने मन में चमन की इमेज बनाए हम घर पहुँचे। अरे…! यह क्या…? आँखों के आगे अँधेरा-सा छा गया। दरवाजे पर, मुस्कुराने वाले फूल रौंदे जाने के बाद तड़प रहे थे, अधजला किवाड़ हमसे गले मिलकर रोने को आतुर था। लोहे की मजबूत ग्रिल के कारण खिड़की के पर्दे पूरे जलने से बच गए थे और उन पर्दों के जगह जगह ढूहे से बन गए थे। जैसे बच्चे बनाते है – रेत के घरौंदे। पर उनमें निर्माण होता है वहाँ तबाही थी और था उजड़ा हुआ सहरा।
तिनका-तिनका जोड़ा हुआ हमारा नीड़ नष्ट हो चुका था, सांप्रदायिकता की आग में जले घर की नींव बाकी रह गई थी। शायद ईश्वर अल्लाह को इतने प्यार से हाथ मिलाते देख उनके हौसले पस्त हो गए थे। हॉल में बिखरे सामान हमारी गैरमौजूदगी में अपने को सुरक्षित न रख पाने की पीड़ा बयाँ कर रहे थे। सोफा सेट की चोटिल कुर्सियाँ औंधी होकर आर्तनाद कर रही थीं। हॉल के बाद का दरवाजा वह तोड़ने में नाकाम रहे या फिर रसोई में रखे मंदिर और जा-नमाज की जुगलबंदी ने उनके भीतर आग पर पानी डाला हो। शायद प्रेम की ताकत ने नफरत की आग को ठंडा किया हो। खुद से गुफ्तगू करते हुए मैं अलगनी पर टँगे कपड़े एक-एक कर उतारती हूँ और बालकनी में सिर्फ रंग-बिरंगे पिन सजे रह जाते हैं। यह आने वाले अगले परिवार के काम आएगी। रंग-बिरंगे पिन हमारी विदाई से उदास हो गए हैं।
अब यादों के बड़े काफिले से मैं अपना दामन छुड़ाना चाहती हूँ पर कहाँ…! उदासी के बादल ने मेरी आँखों और चेहरे को भिगो डाला है। धुँधलाई आँखों को झटपट पोंछती हूँ, कहीं यहाँ से लौट जाने का फैसला बदल कर आफ़ताब को कमजोर न कर बैठूँ, अब यहाँ रहने का ना तो हौसला बचा है ना ही मन… अब बचा ही क्या है यहाँ… समाज के ठेकेदारों को धता बताते हुए, दिलों की दरारों को जोड़कर तिनका तिनका आशियाना बनाया था, वह भी तार-तार नष्ट हो गया फिर इस शहर से दूर जाने का अफसोस कैसा…।
मूवर्स एंड पैकर्स के कर्मचारी जो टी-ब्रेक पर गए थे वापस आकर तैनात हो गए हैं, मैनेजर ने सामान की गिनती कर कई पन्नों का दस्तावेज मुझे थमाया ठीक घर के कॉन्ट्रैक्ट की तरह। जैसे यही हो हमारा आखिरी कॉन्ट्रैक्ट… इन कर्मचारियों ने बड़ी ही मुस्तैदी और फुर्ती से ट्रक पर सामान लोड किया। आफ़ताब का चेहरा ज्यादा ही मायूस है। किसी भी शहर को छोड़ते हुए हम जैसे खुद से जुदा होते हैं। शहर के साथ-साथ हम जिंदगी के तमाम निजी लम्हों से, तमाम यादों से भी जुदा होते हैं।
“चलो आज इस शहर के महासागर को आखिरी बार सलाम कर लें…” – आफ़ताब अपनी पीड़ा और लाचारी को छुपाते हुए बोले।
“हाँ समंदर के किनारे जगर मगर विक्टोरिया में बैठकर आइसक्रीम खाएँगे” …मैंने अपनी खिलखिलाहट आफ़ताब पर बिखेर दी।
“कल से हमारी नई जिंदगी की शुरुआत होगी, लो पहले आज की सुबह की आखिरी ग्रीन टी तो पी लो” …कहते हुए अखबार हाथों में लेकर मैं पलटने लगी।
“अरे… आफ़ताब हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, हर शहर में आग का दरिया है” मेरे साँसों की रफ्तार बढ़ गई… कान में सायरन-सा बजने लगा।
“सुना तुमने, बेंगलुरु में कल एक बड़ा हादसा हुआ, मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के से शादी की, दोनों कई महीनों तक गुमनाम रहे। अब उस लड़की का पति गायब हो गया है। लोग अटकलें लगा रहे हैं लड़की का भाई पाँच वक्त का नमाजी कट्टर मुसलमान है। शायद उसने उस लड़के को जान से… उफ्फ… खबरें गर्म है कि इसमें कोई बड़ी साजिश है।”
मेरी आँखों के सामने कानपुर के कई दृश्य सजीव हो उठे, पूरी दुनिया कानपुर हो गई। और खौफनाक सैलाब में तब्दील हो गई। आँखों के आगे ‘तिलकधारी’, रितेश भाई शाह, ब्रोकर, हुजूम वाले वे लोग झिलमिलाने लगे। तीन तलाक पर औरतों को फतवा जारी करने वाले मुफ्ती और इमाम की शक्लें चस्पाँ हो गईं… जिन्होंने उस प्रेमी जोड़े के लिए हदीस के लॉ के कुछ पन्ने बदल दिए थे। इस बात की कल्पना से मेरे साँसों की लय में उदास वायलिन बजने लगा… जैसे त्रिशूल और काबा दोनों धरती से उठ कर हवा में तैरते हुए आपस में टकरा रहे हों… इन्हें बचाने के लिए ना कोई सुदर्शन चक्र बचा है, ना ही मक्का-मदीना …धरती की सारी नदियों में लाल रंग घुल गया है, जो तबाह कर देगा… और वो लाल पानी का सैलाब मेरी आँखों से बहने लगा है… फिर चारों ओर घोर अंधकार… ठीक उसी वक्त आफ़ताब की आवाज में रोशनी की एक लकीर चमकी… “डरो मत शुभांगी बचा है समंदर जिसका पानी खूनी लाल नहीं हुआ… उसमें हम घोलेंगे प्यार का गुलाबी रंग..”
Download PDF (आखिरी कॉन्ट्रैक्ट)
आखिरी कॉन्ट्रैक्ट – Aakhiri Contract